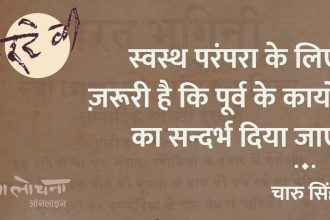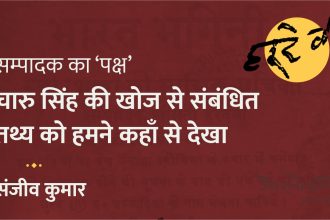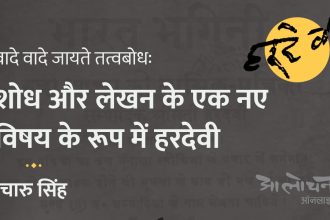सुधीश पचौरी के साथ हिंदी की दुनिया ने बड़ा अन्याय किया है। कुछ भी लिख-बोल जाते हैं, कोई जवाब देके राज़ी नहीं।
बहुत पहले एक वरिष्ठ साथी से एक गॉसिप सुनी थी। हुआ ये कि देवराला सती काण्ड के बाद जनसत्ता के संपादकीय के विरोध में सारे प्रगतिशील-जनवादी मुखर थे, लेकिन सुधीश जी चुप्पी मारे जनसत्ता में अपना स्तंभ लिखे जा रहे थे। जब लोगों ने उनसे विरोध में शामिल होने को कहा तो वे उन्हीं के ख़िलाफ़ ज़हर उगलने लगे। इस पर एक साथी ने कहा, “अरे यार, ये क्या अल्लम-गल्लम लिखते रहते हो? तुम्हें भी पता है, ये ग़लत और बेबुनियाद बातें हैं!” सुनकर सुधीश जी बोले, “ऐसे नहीं चलेगा। लिखकर इसका जवाब दो!” साथी ने छूटते ही कहा, “पागल समझा है क्या? यही तो तू चाहता है!”
तो हिंदी की निष्ठुर दुनिया बहुत पहले जान गई थी कि सुधीश जी क्या चाहते हैं, और उसने कभी उनकी चाहना पूरी न होने दी। कुछ भी लिखते रहें, कोई जवाब देकर उन्हें चर्चा में लाने को राज़ी नहीं।
पर इपंले (इन पंक्तियों का लेखक) इतना निष्ठुर नहीं है। उसके संज्ञान लेने से कुछ होता भले न हो, वह समय-समय पर सुधीश जी की कारगुज़ारियों का संज्ञान लेता रहा है। अरसा पहले, सन 2000 में स्वाधीनता पत्रिका के शारदीय विशेषांक में आलोचना के सूरते-हाल पर लिखते हुए उसने प्रेमपूर्वक सुधीश जी का अनावरण किया था और टिप्पणी की थी कि यह इतिहास का मज़ाक़ ही है कि हिंदी में उत्तर-आधुनिकता का पुरोवाक लिखने का दुर्वह भार सुधीश जी के कंधों पर आन पड़ा है।
संज्ञान लेने का सिलसिला आगे भी चलता रहा, पर अभी अपनी 24 साल पहले की वह टिप्पणी याद आने का कारण है। कुछ समय पहले सुधीश जी ने एक लंबा साक्षात्कार अंजुम शर्मा को हिंदवी के ‘संगत’ कार्यक्रम में दिया है। उसमें सराहनीय आत्मविश्वास और मदारी-नुमा भाषा-कौशल के साथ जिस तरह की बातें कही हैं, उससे इपंले को ध्यान आया कि अरे, 24 साल पहले की वह टिप्पणी तो ज्यों-की-त्यों वैध बनी हुई है! सुधीश जी को पढ़ना वह कब का छोड़ चुका है, इसलिए इस तथ्य पर ध्यान नहीं गया था कि थ्योरी की ‘विशेषज्ञता’ के मामले में वे आज भी वैसे ही हवाबाज़ हैं जैसे तब थे। उनका लगभग दो घंटे का साक्षात्कार सुनने का भी कोई कारण नहीं था, पर लोगों ने बताया कि उन्होंने आलोचना पत्रिका के बारे में, उसके संपादकों के बारे में, और विश्वविद्यालय की वाम राजनीति के बारे में कई आक्रामक बातें कही हैं, इसलिए सुनने का धैर्य जुटाया। अपनी पुरानी राय के आज भी प्रासंगिक बने रहने का अहसास तो उसे फाव में मिला है।
इस टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य उन्हीं आक्रामक बातों की सच्चाई पर प्रकाश डालना है, पर उससे पहले दो-एक बातें साक्षात्कार में आए विद्वज्जनोचित उद्गारों पर कर लेना अच्छा रहेगा।
अंजुम के साथ साक्षात्कार की शुरुआत ही इस प्रश्न के साथ हुई कि “उत्तर-आधुनिकतावाद, उत्तर-संरचनावाद इन सारी शब्दावलियों का हिंदी में एक समय बॉम्बार्ड्मेन्ट हुआ और आपने ज़ोर दिया कि इनके आलोक में ही चीज़ों को पढ़ा जाए। आलोचक पुराने पड़ चुके हैं और आलोचना के लिए भी नयी आलोचना की ज़रूरत हमें है। ये कैसे आपके ज़ेहन में आया था इन सारी चीज़ों को लेकर कि अब इस दिशा में हमको चलना है, और मुझे इसी में लिखना है?”
इसका जो जवाब दिया गया, उसे मैं शब्दशः यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ :
“लंबा जवाब देने की जगह मैं छोटा जवाब दूँगा आपको। ये जो मोबाईल है आपके पास, इसमें पूरी दुनिया बैठी हुई है। ये बॉर्डरलेस है। इसमें आप एक ऐसे साइबर स्पेस में हैं जो दुनिया से जुड़ा हुआ है। आप इसके भीतर, अंदर हैं, बाहर हैं, और अकेले हैं। जो इसमें दिख रहा है, वो कितना रियल है, कितना रियल की फ़ेक है, कितना कॉपी है, कितना हज़ारवीं कॉपी है। टेक्स्ट कैसे इन्टर-टेक्स्ट में बदलता है। कैसे मानी और टेक्नॉलजी एक-दूसरे को इन्टर-टेक्स्ट करते हैं, [दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए] इस तरह से एक-दूसरे में भिदते हैं। मानी कैसे बदलते हैं। और एक चीज़ कि मैंने समीक्षा को, या आलोचक को, या नज़रिये को मैक्सिमम आब्जेक्टिविटी कैसे बने कि मैं अपने दोस्त से बात करूँ तो वो तो कवि हो गया, और जो मेरा दोस्त नहीं, वो किसी खाते में नहीं। मैं इस सब्जेक्टिविटी से बाहर आना चाहता था, एक आलोचक के, एक मामूली स्टूडेंट के तौर पर। कि यार कोई तो ऐसी विद्या होगी कि… अभिनवगुप्त को आप पढ़ें तो उसका दुश्मन और दोस्त कौन है, ये मालूम नहीं पड़ता। मम्मट को पढ़ें तो भी मालूम नहीं पड़ता। तो ये क्यों ऐसे थे? आखिर दोस्त-दुशमन इनके भी रहे होंगे। लेकिन ये तो कोई स्कोर सेटल नहीं करते। इनकी पूरी थ्योरी अलग चलती है, ज़िंदगी अलग चलती होगी। तो ऐसा क्या है? तो उस आब्जेक्टिविटी को जानने के लिए मैं छटपटाता था और कोशिश करता था कुछ मिले। तो धीरे-धीरे पश्चिम में जो मिला—जो बाद में हिन्दुस्तानी थ्योरीज़ में भी, इंडियन थ्योरीज़ में भी मिला जब मेरी आँख, नजर जम गई—स्ट्रक्चरलिज़म मिला। विचित्र बात है कि जो स्ट्रक्चरलिज़म का विधाता है, सास्यूर, वो पाणिनी के एक नुक्ते पर रिसर्च करते-करते यहाँ तक पहुँचा। और ये मुझे संस्कृत के विद्वान ने बात बताई। नोम चॉम्स्की… वो नोबल ले गया, और पाणिनी के एक सूत्र पर ले गया…।”
जवाब थोड़ा और लंबा चलता है, पर उस पूरे का लिप्यंतरण करने का मुझमें धैर्य नहीं है। बस, यों समझिए कि आगे भी ऐसा ही कुछ (कुच्छ भी!) जारी रहता है। क्या आप इस जवाब से यह समझ सकते हैं कि आलोचक को उत्तर-आधुनिकतावाद और उत्तर-संरचनावाद की ओर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वह शुरू में आपको बताता है कि संचार और माध्यम के स्तर पर दुनिया कितनी बदल गई है। और वह भले ही हज़ारों बार दुहराई गई बातें ही दुहरा रहा हो, कम-से-कम बेसिर-पैर की नहीं कह रहा है। लेकिन इस बदलाव से उसकी चली आती आलोचना-पद्धति क्यों बेमानी या नाकाफ़ी हो गई, इसकी ओर आगे एक वाक्य में भी इशारा नहीं है। यह बताने तक की ज़रूरत महसूस नहीं की गई है कि वह बेमानी साबित हुई या नाकाफ़ी, क्यों का सवाल तो बाद का है। फिर अचानक पता नहीं क्या होता है—शायद कुछ भी सूत्रबद्ध न कर पाने की नर्वसनेस है—कि वह सब्जेक्टिविटी-आब्जेक्टिविटी के द्विचर की ओर दौड़ पड़ता है, गोया उत्तर-संरचनावाद की ओर जाने से पहले तक उसके पास जो भी आलोचना-पद्धति थी, वह अनिवार्यतः अपने मित्र को कवि साबित करने और दूसरों को हर सूची से बाहर करने वाली, यानी पूरी तरह से सब्जेक्टिव पद्धति ही थी। उसके कहने से ऐसा लगता है कि वह सब्जेक्टिविटी पहले के सिद्धांतों में ही निहित थी, सिद्धांत के आलोचकीय अनुप्रयोग में नहीं (तभी तो नए सिद्धांत की ज़रूरत के प्रसंग में वह ये बातें कह रहा है)। लेकिन यह बताने के लिए उसके पास एक भी वाक्य नहीं है कि उसे क्यों ऐसा लगता है कि पाठ के केंद्र में ऑथर को रखने वाली मानववादी परंपरा के दायरे में शामिल तमाम आलोचना पद्धतियाँ दोस्त-दुश्मन का फ़र्क़ करना सिखाती हैं या उसकी गुंजाइश मुहैया कराती हैं, जबकि संरचनावाद और उत्तर-संरचनावाद की पद्धति में वह गुंजाइश है ही नहीं? चलिए, यह मान लेते हैं कि वह तो बस संरचनावाद के इस दावे की ओर इशारा कर रहा था कि संरचना के आधार पर पाठार्थ को वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। पर उत्तर-संरचनावाद ने तो इसी वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता के दावे का खंडन किया। तो प्रभु, यही बता देते कि क्या आप भी वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक को पाने की तलाश में वहाँ तक गए और अंततः उस मुक़ाम पर पहुँचे जहाँ वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता असंभव लगने लगती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के मज़े एक साथ लूट लेना चाहते हैं!
कुल मिलाकर, सुधीश जी का यह जवाब कुच्छ भी कहते चले जाने का एक दिलचस्प नमूना है। यह ‘कुच्छ भी’ जब उस जगह पहुँचा जहाँ उन्होंने नोम चॉम्स्की को नोबल पुरस्कार दिलवा दिया, वह भी पाणिनी के एक सूत्र पर, तब इपंले ने लिप्यंतरण के काम को विराम दे दिया। लगा कि इसे ही उद्धरण का चरम बिंदु होना चाहिए। बाद का हिस्सा तो बस उतार ही उतार है। चॉम्स्की को नोबल किस क्षेत्र में मिला, यह भी आचार्य ने बता दिया होता तो मैं उस हिस्से तक अपना लिप्यंतरण ले जा सकता था, पर मेरी और आपकी बदक़िस्मती, उन्होंने बताया नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, चॉम्स्की को न सिर्फ़ नोबल नहीं मिला है, बल्कि भाषाविज्ञान के क्षेत्र में वह मिल भी नहीं सकता है। अगर उन्हें मिलता भी तो नोबल शांति पुरस्कार मिलता जिसके लिए पाणिनी के किसी सूत्र को श्रेय देना मुश्किल होता। साथ ही, जहाँ तक मेरी जानकारी है, भर्तृहरि के वाक्यपदीयम और पाणिनी की अष्टाध्यायी का प्रभाव तो सस्यूर से लेकर चॉम्स्की तक, सब पर है—भारत में दिए गए एक भाषण में खुद चॉम्स्की ने स्वीकार किया कि “कमोबेश आधुनिक अर्थ में पहला जेनेरेटिव ग्रैमर पाणिनी का संस्कृत व्याकरण है”—लेकिन चॉम्स्की अपनी जिन स्थापनाओं के लिए भाषाविज्ञान में जाने जाते हैं, उनका पाणिनी के किसी ‘एक’ सूत्र से कोई संबंध निकाल पाने की योग्यता अभी तक किसी ने प्रदर्शित नहीं की है। लिहाज़ा, यहाँ सुधीश जी को दो कामों का श्रेय मिलना चाहिए: एक, चॉम्स्की को नोबल पुरस्कार दिलाने का, और दो, उनके काम को पाणिनी के ही एक सूत्र का पल्लवन किंवा उच्छिष्ट साबित करने का।
ऐसा ही आला दर्जे का ज्ञान उन्होंने नए इतिहासवाद (New Historicism) के त’अल्लुक़ से भी साझा किया है। स्टीफन ग्रीनब्लाट ने सिर पीट लिया होता अगर उसे हिंदी समझ आती होती और उसने मेरी ही तरह किसी के कहने पर सुधीश जी का इंटरव्यू सुन लिया होता।
पहले इंटरव्यू का यह अंश लिप्यंतरण में पढ़िए, शब्दशः :
‘मार्क्सवादी इतिहास में तो यही बात थी कि भाई अब तक का लिखा हुआ शब्द है जो, वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। लिखित शब्द का इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। अब तक का। तो जो अलिखित है, वो क्या है? इसे लेकर इतिहासज्ञों में वेस्ट में डिबेटें चलीं और न्यू हिस्टोरीसिज़्म का स्कूल खड़ा हुआ, जिसने पहली बार ये कहा कि ‘मिथ’, कहानी, साहित्य, क़िस्से—लोगों के जीवन में जो क़िस्से चलते हैं—वे इतिहास ही हैं। इससे मार्क्सवादियों को बड़ी परेशानी हुई। क्योंकि उनको तो चाहिए था प्रमाण! वे साहित्य को प्रमाण नहीं मानते। वे माइथोलोजी को प्रमाण नहीं मानते। भारत में राम हुआ… रामजी हुए, कृष्ण जी हुए, वे नहीं मानते। मिथ है।’
‘आप मानते हैं?’
‘मैं मानता हूँ। वो मिथ भी हैं, व्यक्ति भी हैं, जिसकी जैसी भावना, वो ले ले। लेकिन वो टेक्स्ट में है अवैलबल, भैया, मैं क्या करूँ? उनको कैसे निकाल दूँ? बचपन से मेरे कान में नाम पड़ता रहता है। … मैं कैसे कह दूँ कि है नहीं? न्यू हिस्टोरीसिज़्म ने, ग्रीनब्लाट ने यह सिद्ध किया, और बाक़ायदा आरगुमेंट करके सिद्ध किया जिसको किसी ने काटा नहीं, कि लिटरेचर फोरग्राउन्ड है हिस्ट्री की। हिस्ट्री से पहले लिटरेचर आया है।’
बमुश्किल 200 शब्दों के इस हिस्से में इतने छेद हैं कि कितना भी कुशल रफ़ूगर हो, हार मान जाएगा। आइए, बिन्दुवार याकि छिद्रवार देखें:
- 1848 में लिखे गए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में 1888 के अंग्रेजी संस्करण में एंगेल्स द्वारा एक फुटनोट जोड़ा गया था जिसमें यह सफ़ाई दी गई कि मूल पाठ में आए ‘अभी तक के समाज का इतिहास’ से आशय लिखित इतिहास से है। फुटनोट जोड़ने का कारण यह था कि इस बीच प्राक्-इतिहास के बारे में और लिखे गए इतिहास से पहले मौजूद रहे सामाजिक संगठनों के बारे में नई जानकारियाँ सामने आई थीं, जिनमें सामूहिक मिल्कियत के अनेक उदाहरण मौजूद थे। इसलिए ‘लिखित’ शब्द आदिम साम्यवादी सामाजिक संगठनों से इतिहास के उस दौर को अलगाने के लिए आया जिसमें वर्ग-संघर्ष ही चालक शक्ति रही। ‘अगर लिखित ये है तो अलिखित क्या है’—यह प्रश्न ही हास्यास्पद है।
- ‘इतिहासकारों के बीच डिबेटें चलीं,’ ऐसा कहने से यह प्रतीत होता है कि नया इतिहासवाद ‘इतिहासकारों’ के बीच की बहसों से निकला कोई ‘सिद्धांत’ है। यह और अधिक हास्यास्पद है। नया इतिहासवाद मूलतः साहित्यालोचन और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र से आया है जिसमें साहित्य और इतिहास के संबंधों की पुनर्परीक्षा प्राथमिकता पर है। यह अंतर्निहित रूप में उस साहित्यिक रूपवाद (न्यू क्रिटिसिज़म) की आलोचना है जो साहित्य को इतिहास से परे एक आइकॉन/अनुसंकेत मानकर पढ़ता है।[i] (Michael Payne. ‘Introduction: Greenblatt and New Historicism’ in The Greenblatt Reader (Edited by Michael Payne), 2005, Blackwell Publishing, Oxford, P. 3.)
- नया इतिहासवाद साहित्य को इतिहास मानता है, पर उसका वह मतलब कतई नहीं है जो उद्धृत अंश में आचार्य सुधीश का है। नए इतिहासवादियों के लिए ‘अतीत में जो कुछ घटित हुआ वह (यानी घटनाओं का समुच्चय) और उन घटनाओं का विवरण (यानी कथा), दोनों ही इतिहास हैं; कही गई कथा की उपयुक्तता पर आलोचनात्मक चिंतन के बीच से ऐतिहासिक सत्य उभरता है। इस तरह इतिहास एक तरह का विमर्श है, और यह इस बात से इंकार नहीं है कि घटनाएं असल में हुई थीं।… अतीत को उसकी पाठीय पुनर्निर्मिति से पृथक होने लायक वस्तु मानना अब संभव नहीं रह गया है।’[ii] (वही, पृष्ठ 3.)
- कथा अपने समय में शामिल है और वह भी कोई भूमिका निभा रही है, इस रूप में कथा को देखना नए इतिहासवाद की विशेषता है। इसका कहीं से यह मतलब नहीं निकलता कि चूँकि राम नामक पात्र कथाओं में वर्णित है, इसलिए आप उसे एक ऐतिहासिक व्यक्ति मान लें। हाँ, इस रूप में उसका अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए कि रामकथा किन विश्वासों और प्रथाओं को वैधता देती है, सामाजिक व्यवहार की कौन-सी मर्यादाएं तय करती है, कुल मिलाकर कैसे एक संस्कृति के निर्माण में वह एक कारक और घटक की भूमिका अदा करती है। यही कारण है कि अलग-अलग रामकथाओं का अध्ययन—यह देखते हुए कि कौन-सी कथा किस चीज़ को स्थापित कर रही है और किस चीज़ का उच्छेद कर रही है—इतिहास का एक दिलचस्प अध्ययन हो सकता है, जिससे संबंधित रामानुजन के लेख को दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के पाठ्यक्रम से निकाले जाने के समय आचार्य सुधीश डीन ऑफ़ कॉलेजेज़ के महत्त्वपूर्ण पद पर रहते हुए उस फ़ैसले की पार्टी बने थे।[iii] (देखिए, मेरी ‘भूमिका’, तीन सौ रामायणें और अन्य निबंध (संपा. संजीव कुमार), 2013, राजकमल पेपरबैक्स, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 7-8.)
- इन सारी बातों की ओर इशारा आपको स्टीफन ग्रीनब्लाट के इस उद्धरण में मिल जाएगा:
‘नया इतिहासवाद आलोचना और इतिहास, दोनों के नीचे से ठोस जमीन खींच लेता है। यह खुद अपनी प्राविधिक मान्यताओं पर सवाल खड़े करता है और दूसरों की मान्यताओं पर भी… इसके अलावा, यह साहित्यिक कृति की जैविक एकता को स्थापित करने से ज़्यादा सरोकार नहीं रखता और कृतियों को बल-क्षेत्रों [जैसे गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय बल का क्षेत्र होता है], असहमतिमूलक कलह और बदलते हितों की जगहों, रूढ़िवादी और रूढ़ि-ध्वंसक प्रेरणाओं की धक्का-मुक्की के अवसरों के रूप में देखने के प्रति अधिक खुला है।… इस किताब में पेश किया गया आलोचनात्मक अमल उन मान्यताओं को चुनौती देता है जो ‘साहित्यिक अग्रभूमि’ और ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि’ के बीच, या अधिक सामान्य रूप में कहें तो कलात्मक उत्पादन और अन्य क़िस्म के सामाजिक उत्पादन के बीच एक निश्चित अंतर की गारंटी करती हैं। इस तरह के अंतरों का वास्तव में अस्तित्व होता है, लेकिन वह पाठ की मूलभूत प्रकृति का हिस्सा नहीं हैं; बल्कि वे कलाकार, दर्शक-श्रोता, और पाठक के द्वारा निर्मित और निरंतर पुनर्निर्मित किए जाते हैं। ये सामूहिक सामाजिक निर्मितियाँ एक ओर प्रदत्त प्रस्तुति-प्रणाली (रिप्रेजेंटेशनल मोड) के भीतर सौंदर्यात्मक संभावनाओं की रेंज को परिभाषित करती हैं, और दूसरी तरफ़, उस प्रणाली को संस्थाओं, प्रथाओं, और विश्वासों—जो पूरी संस्कृति को संघटित करते हैं—के जटिल संजाल से जोड़ती हैं।’[iv] (Stephen Greenblatt. Introduction to The Power of Forms in English Renaissance, Qtd. By Michael Payne, ‘Introduction: Greenblatt and New Historicism’ in The Greenblatt Reader, P. 2.)
- स्टीफन ग्रीनब्लाट के इस बलाघात पर ग़ौर कीजिए कि ‘लिटरेरी फ़ोरग्राउन्ड’ और ‘’पोलिटिकल बैकग्राउंड’ के बीच अंतर करने वाली आलोचना को नया इतिहासवाद चुनौती देता है, और फिर आचार्य सुधीश के उस वाक्य को पढ़िए कि ग्रीनब्लाट ने कहा कि लिटरेचर फ़ोरग्राउन्ड है हिस्ट्री की। क्या नए इतिहासवाद को वे शीर्षासन करते हुए पढ़ रहे थे?
- ग्रीनब्लाट का नाम सुधीश जी ऐसे लेते हैं जैसे वह मार्क्सवाद की धज्जियां उड़ा देने वाला कोई विचारक है। अब यह जानिये कि स्वयं ग्रीनब्लाट का क्या कहना है: ‘मैं अभी भी ऐसी राजनीति और ऐसे साहित्यिक नज़रिये के प्रति खासा असहज हूँ जो मार्क्सवादी विचार से अछूता हो।’[v] (‘I am still more uneasy with a politics and a literary perspective that is untouched by Marxist thought.’ – Stephen Greenblatt. ‘Towards A Politics of Culture’ in The Greenblatt Reader, P. 19)
सवाल है कि नए इतिहासवाद का ऐसा निछछ कुपठन क्यों? सुधीश जी को अपने काम के बारे में जो कुछ कहना था, वैसे ही कह देते! नए इतिहासवाद की ऐसी ग़लत व्याख्याओं से उसे सहारा देने की क्या ज़रूरत थी? इसे ऐसे समझिए कि इस हिंदू-समय में सुधीश जी को हिंदुत्व के अनुकूल ठहरने वाली स्थापनाएं देने की चुल्ल मची है। अभी भी काफ़ी कुछ हासिल करना रह गया है न! तो राम को ऐतिहासिक व्यक्ति बता देने से (और आगे चलकर मुसलमानों के आने से भक्ति साहित्य में महज़ चार आना बदलने की स्थापना को खंडित करने से) उन्हें मौजूदा सत्ताधारियों का कृपापात्र बन जाने की उम्मीद है। पर ये बातें ऐसे ही कैसे कह दें? उसे बौद्धिक वैधता भी तो दिलानी है! और वह वैधता मिलेगी उन संज्ञाओं के सहारे जिनके बारे में, आचार्य का विश्वास है कि, हिंदी की दुनिया कुछ जानती नहीं, पर जिनसे आतंकित ज़रूर हो जाती है। यही विश्वास आचार्य के अंदर अनर्गल बातें कहते जाने का अपूर्व आत्मविश्वास भर देता है। क्या विडंबना है कि हिंदुत्व की शरण गहने में वे अपने तर्क उस ग्रीनब्लाट से निकाल रहे हैं जो पाठ को ‘रूढ़िवादी और रूढ़ि-ध्वंसक प्रेरणाओं की धक्का-मुक्की के अवसरों के रूप में देखने’ की बात करता है और संस्कृति के बारे में जिसकी धारणा है कि ‘विश्वासों और प्रथाओं का जो समूह प्रदत्त संस्कृति को गढ़ता है, वह नियंत्रण की एक सर्वव्यापी टेक्नॉलजी के रूप में कार्य करता है, उन मर्यादाओं के एक समुच्चय के रूप में जिसके भीतर सामाजिक व्यवहार को मर्यादित/सीमित रहना है, मॉडेल्स की एक फ़ेहरिस्त के रूप में जिसके प्रति व्यक्तियों को अपनी सहमति देनी है।’[vi] ( Stephen Greenblatt. ‘Culture’ in The Greenblatt Reader, P. 11.) क्या आप विश्वास करेंगे कि यह विचारक सुधीश जी को हिंदुत्व की छतरी में समाने का ‘पास’ मुहैया करा रहा है?
आचार्य सुधीश के विद्वज्जनोचित उद्गारों पर फ़िलहाल इतना ही। जितनी बातें अभी तक कही गई हैं, वह सिर्फ़ यह बताने के लिए कि खुद सुधीश जी की बातों में ‘कितना रियल है, कितना फ़ेक है, कितना कॉपी है, कितना हज़ारवीं कॉपी है,’ इसका एक ज़ायका आपको मिल सके। इस ज़ायके का फ़ायदा यह है कि आगे वे बातें, जिनके ‘फ़ेक’पन और ‘फेंकू’पन का पता लगाने की कोई पद्धति आपके पास नहीं है, उनकी असलियत सामने लाए जाने पर आपको लगे कि हां, इनका असली होना बहुत संदिग्ध नहीं है।
पर उसकी ज़रूरत विश्वविद्यालय प्रसंग में पड़ेगी। पहले आइए इस पर कि आलोचना पत्रिका और राजकमल प्रकाशन के बारे में उन्होंने क्या कहा। साक्षात्कार में एक जगह (1:30:44/घंटा:मिनट:सेकंड पर) अंजुम उनकी बदज़ुबानी पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं (हालाँकि भालेमानस की तरह उन्होंने उसे ‘बदज़ुबानी’ नहीं, ‘शब्दों का ऐसा इस्तेमाल’ भर कहा है), “नामवर जी के बारे में आपने कहा कि बुड्ढे को मरे हुए एक साल हो गया?”
सुधीश पहले तो साफ़ इंकार करते हैं, “नेवर!” फिर जब अंजुम इस बात पर अड़े रहते हैं कि राजपाल के लाइव में पल्लव से बात करते हुए उन्होंने यह कहा है कि बुड्ढे को मरे हुए एक साल हो गए, तो थोड़ा हील-हवाला करते हुए वे हल्के से मान लेते हैं और बहुत रणनीतिक तरीक़े से, बात को छितरा देने के खयाल से, दूसरी सनसनी की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, “हाँ-हाँ, मैंने कहा होगा, मगर ‘आलोचना’ का एक लाइन नहीं आया।”
अंजुम इस सनसनी में दिलचस्पी नहीं लेते और अपनी बात पर क़ायम रहते हैं, “यही तो है! शब्दों का जो इस्तेमाल है…।”
अब सुधीश कहते हैं, “नामवर सिंह बुड्ढा था, बुड्ढा है। हमारे लिए सीनियर है वो। दैट इज़ बुड्ढा!”
वाह! अगर इतना सम्मानजनक शब्द है तो जान बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे जनाब, समझ नहीं आया! और जान बचाने की वह कोशिश पीछे ही नहीं, आगे भी जारी रहती है! वे अविलंब बुड्ढा-प्रसंग को दुबारा सनसनी की दिशा में ले जाते हैं। उनकी तेज़ी में जैसे यह अनकहा संदेश है कि भैया, मसाला इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है! कहते हैं :
“बूढ़े [इस बार बुड्ढे नहीं कहा] को मरे हुए एक साल हो गए, पर एक लाइन नहीं आई उस आदमी के बारे में जिसने तुम्हें रोटी दी।… मैं ओपेनली कहता हूँ, नामवर सिंह ने ‘आलोचना’ को सींचा, राजकमल को सींचा। आज जो है, उन्हीं की कृपा से है। लेकिन वह मर गया, मर गया वो व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसने तुम्हें सबकुछ दिया, उसके मरने के एक साल होने पर ‘आलोचना’ का जो अंक निकला, उसमें उन पर एक लाइन नहीं थी। क्यों? जिन दो आलोचकों को उन्होंने वहाँ लगाया आखिरी दिनों में, क्या उनका कर्तव्य नहीं था? वो लोग जो उसका चरण चाटते रहे, क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि उनको याद करें?”
इस पूरी बात में जो तथ्य की गड़बड़ी है, उसे पहले निपटा दें, उसके बाद इसकी भाषा और उसमें निहित विचारधारा पर बात करेंगे।
तथ्य यह है कि आलोचना ने फरवरी 2019 में नामवर जी के इंतकाल के बाद उन्हें बार-बार याद किया है, साल भर बाद भी याद किया है, और उपकृत होने के कारण नहीं, इस कारण याद किया है कि वे ऐसे आलोचक और संपादक रहे हैं जिनका योगदान बार-बार याद किये जाने लायक़ है। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनकी सबसे बड़ी स्मृति-सभा दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में राजकमल प्रकाशन ने आयोजित की और आलोचना के अंक में, जिसके मुखपृष्ठ पर नामवर जी की तस्वीर थी, संपादक आशुतोष कुमार ने ‘आखिरी सफ़ा’ स्तंभ उन्हीं पर केंद्रित किया (‘हिंदी आलोचना का आत्मसंघर्ष और नामवर सिंह’/ अप्रैल-जून 2019/ अंक 60)। (दोनों संपादकों ने उनकी मृत्यु के तुरंत बाद अन्यत्र जो स्मृति-लेख लिखे, वे अलग।) आलोचना का वह अंक जनवरी 2019 में प्रकाशित अंक 59 के बाद जून 2019 में आया था।
इसके बाद आलोचना 61 (जुलाई-सितंबर 2019) में पंकज चतुर्वेदी का लंबा लेख प्रकाशित हुआ, ‘हिंदी के हित का अभिमान’। यह अंक अपने समय से थोड़े विलंब से, दिसम्बर 2019 में आया। फिर आलोचना 62 (अक्तूबर-दिसम्बर 2019) में नामवर जी पर पंकज बोस का लंबा लेख प्रकाशित हुआ। कोरोना बंदी के बीच यह अंक जुलाई 2020 में प्रकाशित हो सका। आलोचना 63 (जनवरी-मार्च 2020) में आशीष त्रिपाठी का लंबा लेख प्रकाशित हुआ, ‘अप्रतिहत गरज रहा अंबुधि विशाल’। यह अंक नवंबर 2020 में सामने आया। फिर थोड़े अंतराल के बाद अंक 68 और 69 में दो क़िस्तों में उदय भानु सिंह और राजकुमार द्वारा लिए गए नोट्स के आधार पर ‘मार्क्सवादी आलोचना के इतिहास पर नामवर सिंह के कक्षा-व्याख्यान’ का प्रकाशन हुआ।
अब आचार्य सुधीश ये बताएं कि 19 फरवरी 2019 को नामवर जी के इंतकाल के बाद जब इस त्रैमासिक के लगातार चार अंकों में उन पर लंबे-लंबे (औसतन आठ हजार शब्दों के) लेख छपे हैं, तो उन्हें ये इल्हाम कहाँ से हो गया कि उनके मरने के एक साल पूरे होने पर आलोचना में एक लाइन नहीं छपी! क्या ‘पहली पुण्यतिथि पर विशेष’ जैसा कोई लेबल लगाने पर ही उन्हें संतोष होता? झूठ को सार्वजनिक मंच से बेहिचक बोलने का यह आत्मविश्वास कहाँ से लाते हैं वे?
अब ग़ौर कीजिए इस उद्धरण की भाषा पर। यह भाषा उस मार्क्सवादी-उत्तरसंरचनावादी विचारक की है जो ‘शक्ति के खेल’ की बात करते अघाता नहीं है। अपने साक्षात्कार में ही उसने कई बार इस मुहावरे का इस्तेमाल किया है; महानता पैसे और ताक़त से बनायी जाती है—इस तरह की बातें कही हैं। और वही व्यक्ति यहाँ ‘रोटी देने’, ‘सबकुछ देने’, ‘कृपा करने’, ‘चरण चाटने’ के मुहावरे में बात कर रहा है!
इस भाषा को थोड़ा विखंडित करके देखें। जो व्यक्ति यह कह रहा है कि आलोचना के वर्तमान संपादक नामवर सिंह के चरण चाटते रहे, उसने उन्हें चरण चाटते देखा तो था नहीं (जाननेवाले जानते हैं कि ये संपादक कभी नामवर जी के ‘क़रीबियों’ में नहीं रहे)! फिर वह कैसे इस निष्कर्ष पर पहुँचा? निश्चित रूप से, उसकी धारणा यह है कि अपने आखिरी दिनों में नामवर जी ने जिनको संपादक बनाया, उन्हें चरण चाटने की वजह से ही बनाया होगा! इस धारणा के दो कारण हो सकते हैं। एक, नामवर जी के बारे में इस व्यक्ति की यह समझ हो कि वे चरण चाटने वालों को ही संपादक बना सकते थे। दूसरे, स्वानुभव के आधार पर यह व्यक्ति जानता हो कि बिना चरण चाटे इस तरह की जगह मिलती कहाँ है! अगर पहला कारण सही है तो इसका यह भी मतलब होना चाहिए कि नामवर जी स्मरणीय व्यक्ति नहीं थे। जो चरण चाटने पर प्रमोट करे, उसे आप स्मरणीय कैसे कह सकते हैं? फिर तो पहली बरसी पर उनके बारे में कुछ न लिखा जाना उचित ही होता! ज़ाहिर है, सुधीश जी ऐसा नहीं मानते। इसका मतलब यही लागाया जाना चाहिए कि दूसरा कारण ही सही है। अर्थात, पीछे के उद्धरण से और कुछ साबित होता हो या नहीं, यह ज़रूर साबित होता है कि सुधीश जी चरण चाटने की सामंती परंपरा के अच्छे पालनकर्त्ता रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें दिविवि के कुलपति रहे दिनेश सिंह के सामने कमर से ठीक नब्बे डिग्री पर झुककर सलामी बजाते देखा है, वे तो यह बात जानते ही हैं, पर यहाँ यह बात उनके एक वाक्य के विखंडन भर से उद्घाटित हो रही है।
विखंडन की दिशा में थोड़ा और बढ़ें। उद्धरण के पहले वाक्य में जहाँ वे कहते हैं कि ‘एक लाइन नहीं आई उस आदमी के बारे में जिसने तुम्हें रोटी दी,’ वहाँ ‘तुम’ कौन है? यह राजकमल प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी के बारे में हैं, या आलोचना के संपादकों के बारे में? दोनों में से कौन हैं जिन्हें नामवर जी ने ‘रोटी दी’? नामवर जी की सारी किताबें राजकमल से प्रकाशित हैं, वे इस प्रकाशन संस्था के अत्यंत सम्मानित लेखक हैं, एक ज़माने में इस प्रकाशन संस्था के सलाहकार भी रहे, लेकिन रोटी देना? यह किस तरह के सामंती मुहावरे में प्रकाश-लेखक-संबंध को देखा जा रहा है? और अगर ‘तुम’ का आशय आलोचना के संपादकों से है, तो वे नामवर जी की दी हुई रोटी खाते हैं, यह बात आज तक किसी होशो-हवास वाले आदमी के दिमाग़ में नहीं आई। यह बात अगर सुधीश जी के दिमाग में आई है तो निहायत मौलिक आइडिया है, चॉम्स्की को नोबल पुरस्कार मिलने जैसा ही।
वस्तुतः इस तरह की भाषा किसी और चीज़ की जानकारी देने से ज़्यादा अपने प्रयोक्ता के मन-मिज़ाज की ही जानकारी देती है। सुधीश जिस भाषा में चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वह आइडियोलॉजी की कार्य-पद्धति का बहुत ठोस उदाहरण है। जॉन बी थॉमसन के उस प्रसिद्ध कथन को याद करें कि “आइडियोलॉजी का अध्ययन करना…. उन तरीक़ों का अध्ययन करना है जिन तरीक़ों से [भाषिक रूप में व्यक्त] मा’नी (या संकेतन/सिग्निफिकेशन) प्रभुत्व के संबंधों को बनाए रखने का काम करता है।” (To study ideology… is to study the ways in which meaning (or signification) serves to sustain the relations of domination.) सुधीश जी की भाषा प्रभुत्व और मातहती के संबंध को वैधता देने वाली भाषा है जिसमें कृपाभाव, कृपाकांक्षा और कृतज्ञता बहुत मूल्यवान धारणाएँ हैं। उन्हें नहीं लगता कि नामवर सिंह को आलोचना पत्रिका ने किसी और कारण से याद किया होता, उसे उपकृत होने के कारण याद करना चाहिए था। इसीलिए मैंने पीछे कहा कि नामवर जी को आलोचना ने उपकृत भाव से बार-बार याद नहीं किया है, इसलिए याद किया है कि एक आलोचक और संपादक के रूप में उनका योगदान बार-बार याद किए जाने लायक़ है।
अंजुम को दिया हुआ पूरा साक्षात्कार इस तरह के झूठों और ताक़तोपासक धारणाओं से भरा पड़ा है। मजेदार बात यह कि कई झूठ तो खुद उनकी बातों के अंतर्विरोध से ही उजागर हो जाते हैं। उसे कोई ऐसा व्यक्ति भी पकड़ सकता है जिसके सामने सिर्फ़ साक्षात्कार हैं और जिसे किसी अन्य संदर्भ की जानकारी नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अन्य संदर्भों का इतनी जानकारी है कि उगलने लगूँ तो आचार्य उसी की बाढ़ में बह जाएँगे, पर सार्वजनिक नैतिकता के खयाल से मैं ऐसा करूँगा नहीं। हां, कुछ बातें हैं जिन्हें साफ-साफ़ कहा जाना जरूरी है। अपने साक्षात्कार में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के वामपंथियों को काफ़ी बुरा-भला कहा है। 2008-09 में जब सेमेस्टर प्रणाली लाए जाने के खिलाफ़ विश्वविद्यालय में आंदोलन हुआ, तब वामपंथियों के साथ उनके संबंध का कौन-सा नया अध्याय शुरू हुआ, इसकी चर्चा की है। उस प्रकरण का भेद खोले बगैर यह टिप्पणी अधूरी रहेगी।
सुधीश पचौरी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर, फिर विभागाध्यक्ष, फिर डीन ऑफ़ कॉलेजेज़, फिर उप-कुलपति, फिर कार्यवाहक कुलपति रहे। जिस समय बिल्कुल अफरा-तफरी में, बिना किसी सुचिन्तित प्रक्रिया के, दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली लागू की जा रही थी, वे बतौर हिंदी विभागाध्यक्ष उसके प्रबल पक्षधर थे। वे यह न जानते रहे हों कि हफ़्ते-हफ़्ते भर में पाठ्यक्रम बनाकर अगले सत्र से नई प्रणाली लाने के क्या दुष्परिणाम होंगे, यह संभव नहीं (आगे वे दुष्परिणाम प्रकट भी हुए और दिविवि को अफरा-तफरी में लागू की गई सेमेस्टर प्रणाली का बचाव करने के लिए तथा उन दुष्परिणामों को बुहार कर कालीन के नीचे छिपाने के लिए क्या-क्या करना पड़ा, वह एक अलग क़िस्सा है)। इसके बावजूद वे ऊपर को जाती सीढ़ियों पर नजर गड़ाए, हुक्मरान को अपनी निष्ठा से प्रभावित करने के प्रयास में लगे रहे (दूसरों के लिए ‘चरण चाटने’ का मुहावरा उनके यहाँ अकारण नहीं आया है)। यही मौक़ा था जब उनकी वामपंथियों से ठन गई जो इस तरह से सेमेस्टर प्रणाली थोपे जाने के खिलाफ़ आंदोलन कर रहे थे। शिक्षक संघ ने, जिसमें वामपंथी भी शामिल थे, जल्दबाज़ी में पाठ्यक्रम बनाए जाने के खिलाफ़ हर विभाग में जाकर प्रदर्शन किए, कुलपति के आदेश के और विद्वत परिषद से छल-बलपूर्वक पारित कराए गए प्रस्ताव के पालन में बाधा डाली, और ज़ाहिर है, ऐसा उन्होंने हिंदी विभाग के साथ भी किया। कृपा और कृतज्ञता जैसी शब्दावली में सोचनेवाले आचार्य को यह बात अखर गई कि ये वामपंथी—जिनके, उन्हीं के शब्दों में, कितने ही ‘गंदे काम’ उन्होंने किए—उनकी कुलपति समर्थक पहलक़दमी में बाधक बन रहे हैं। इस तरह तो सीढ़ी चढ़ना नामुमकिन हो जाएगा! सो वे अड़ गए। जहाँ कई अन्य विभागाध्यक्षों ने यूनियन द्वारा बाधा डाले जाने के नाम पर पाठ्यक्रम बनाने का काम रोक दिया और इस आड़ में कुलपति के आदेश पर एक ग़लत काम करते जाने के धर्मसंकट से बाहर निकल आए, वहीं सुधीश जी अपनी स्वामिभक्ति से टस से मस नहीं हुए। ऐसे में यूनियन और वामपंथियों के साथ उनके तनाव को अपने शिखर पर जाना ही था!
यह संदर्भ है सुधीश जी और दिविवि के वामपंथियों के बीच की रार का!
वैसे अगर आप इस संदर्भ के बगैर भी साक्षात्कार में आए उनके शब्दों पर ग़ौर करें तो अंदर दबी सच्चाई की झलक से वंचित नहीं रहेंगे। सुनते हुए आपको आश्चर्य होगा कि यह शख्स आंदोलनकारियों से किस चीज़ की उम्मीद रखता था! वह उनसे इस कृतज्ञता की उम्मीद रखता था कि जिस अधिकारी ने उनके कहने पर कुछ कागज़ों पर दस्तखत किए हों, उसके सामने वे अपने सारे नीतिगत फ़ैसलों का विसर्जन कर दें! वह यह उम्मीद करता था कि वामपंथी लोग आनन-फानन में पाठ्यक्रम बनानेवाले अन्य विभागाध्यक्षों के साथ जो भी करें, कम-से-कम उसे बख्श दें, क्योंकि उसने ‘उनके काम किए’ हैं और अभी उसे कुलपति की नज़रों में अव्वल आना है! आंदोलनकारी वामपंथियों से यह उम्मीद करना वक्ता के सोच के बारे में आपको क्या बताता है? यही कि वह लेन-देन, कृपालुता-कृतज्ञता, ‘रोटी देने’ और ‘चरण चाटने’ की शब्दावली से बाहर सोच पाने में असमर्थ है। यही व्यक्ति जब समाज के शक्ति-संबंधों, भाषा की विचारधारात्मक प्रकृति, विखंडन की पढ़त-रणनीति, मीडिया और सर्वानुमति की मैन्युफैक्चरिंग आदि के बारे में बात करता है, तो क्या आप उससे किसी तरह की गहराई की उम्मीद कर सकते हैं?
वीरेन डंगवाल के बारे में अपशब्द कहने की बात पर घेरे जाने के बाद अपनी सफ़ाई देते हुए एक जगह सुधीश जी ने ठेठ हाथरसी अंदाज़ में कहा है, ‘मैं तो गाली दे दूँ, कोई क्या कल्लेगा?’ बेशक, यही उनकी असलियत है। वे यह मानते हुए कुछ भी कह जाते हैं कि कोई क्या कल्लेगा। इसीलिए उनका साक्षात्कार मेरे जिस विद्यार्थी-मित्र ने मुझे फॉरवर्ड किया था, उसे एक छोटा हिस्सा सुनने के बाद ही मैंने टेक्स्ट किया, “इनसे इसी अनाप-शनाप की उम्मीद थी। बंदा कभी निराश नहीं करता। उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरता है।”