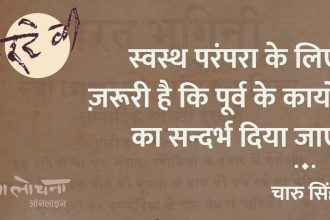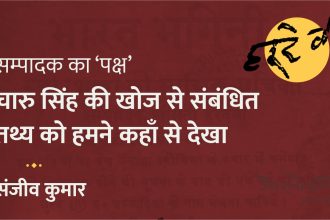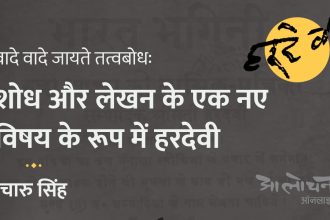We only see what we look at. To look is an act of choice.
—जॉन बर्जर
वह बिल्कुल निजी बातचीत थी जिसने एक दुर्लभ आत्मसाक्षात्कार को संभव किया।
सिनेमा और साहित्य के संजीदा आलोचक जवरीमल्ल पारख से फ़ोन पर बात हो रही थी। 26 नवंबर को शाम साढ़े पाँच-छह के बीच। तारीख़ और समय इसलिए याद है कि उस दिन दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव थे और मतदान ख़त्म होने के बाद समाज-विज्ञान संकाय के भवन से निकलकर सैकड़ों लोगों की भीड़ में मैं बाहर चाय के अड्डे की ओर बढ़ रहा था। पारख जी ने शुरुआती हालचाल के बाद जानना चाहा कि पिछले दो-तीन दशकों में उभरे आलोचकों पर बात हो तो मैं किनके नाम सुझाना चाहूँगा, अपने अलावा। मैंने कहा कि मैं तो भला क्या हूँ, पर आठ-दस ऐसे नाम निकल आएँगे जिनके पास लेखन के गुण और परिमाण, दोनों दृष्टियों से किसी भी सूची में उपस्थित रहने की पात्रता है। ठहर-ठहरकर मैंने कुछ नाम सुझाए (यहाँ बताना ज़रूरी नहीं), उनके बारे में हम अपनी-अपनी राय का आदान-प्रदान भी करते गए। जब मेरी सूची लगभग ख़त्म हो गई, तब पारख जी ने हँसते हुए कहा, ‘तो बंधु, जैसी कि ज़्यादातर प्रगतिशीलों-जनवादियों से उम्मीद की जाती है, आपकी सूची में भी किसी दलित और स्त्री की जगह नहीं है जबकि इस बीच कई दलित और स्त्री आलोचकों ने अच्छा-ख़ासा लिखा है।’ यह एक तेज़ झटका था। सचमुच, मेरी सूची में वे सिरे से ग़ायब थे। पारख जी के ऐसा कहते ही मुझे दलित और स्त्री आलोचकों के नाम याद आने लगे, उनके बारे में हमने चर्चा भी की। ये सभी ऐसे नाम थे जो मेरे सुझाए नामों से किसी भी रूप में कमतर नहीं थे।… पर इस नाम-स्मरण के बाद भी झटके का असर कम न हुआ।
फ़ोन रखने के बाद मैंने झटके के असर से निकलने के लिए मन-ही-मन कई तर्क-वितर्क किए। मसलन, एक—इतनी भीड़ में खड़े होकर बातें करते हुए, जहाँ हर तरफ़ चुनावी उत्सव में इकट्ठा हुए मित्रों का गुलगपाड़ा चल रहा हो, दिमाग़ ठीक तरीक़े से काम कैसे कर सकता है? मैं तो बजरंग तक का नाम सुझाना भूल गया जो हम दोनों के ‘कॉमन’ मित्र हैं, फिर दलित और स्त्री आलोचकों का ज़िक्र न आना कौन-सी बड़ी बात है! दो—दलित लेखन और स्त्री लेखन की अलग श्रेणियाँ बनने का यह दुष्परिणाम है कि आलोचना मात्र की बात आने पर उनका ध्यान ही नहीं आता; जब दलित और स्त्री आलोचना की बात आएगी, तभी ध्यान आएगा। यह उन अलग-अलग खातों के बनने का नतीजा है जिन्हें मैंने नहीं बनाया, जो मुझे बने-बनाए मिले हैं और जिनके बनने में शायद स्वयं दलितों और स्त्रियों की दिलचस्पी रही है।
ऐसी और भी दलीलें दिमाग़ में आती रहीं जिनका लब्बोलुआब यह था कि ग़लती हुई तो है, पर दोषी मैं नहीं हूँ; मुझ पर जाति तथा जेंडर संबंधी किसी भी तरह के भेदभाव का दोषारोपण नहीं किया जा सकता।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये दलीलें फेनबुदबुद के समान क्षणजीवी साबित हुईं। मन में एक-के-बाद-एक इनकी काट आती गई। दूसरे वाला तर्क तो इस मासूम प्रश्न के आगे ढेर हुआ कि दलित और स्त्री लेखन की बात ज़रूर होती रही है, पर दलित आलोचना और स्त्री आलोचना जैसी स्वीकृत श्रेणियाँ कहाँ हैं? इन श्रेणियों को लेकर लिखी गयी किताबें या लेख तो मेरे ध्यान में नहीं हैं! हाँ, अगर इसी तरह आलोचकों की फ़ेहरिस्त में उन्हें शामिल करना भूलते रहे तो निश्चित रूप से ये श्रेणियाँ वजूद में आएँगी, क्योंकि ऐसी श्रेणियों के न बनने का मतलब होगा, दलित और स्त्री आलोचकों का इतिहास-बदर होना। ग़रज़ कि मैं जिन्हें कारण और परिणाम ठहरा रहा हूँ, असल में उनकी भूमिका बिल्कुल उलट है। वे क्रमशः परिणाम और कारण हैं।… और अगर दलित और स्त्री विमर्श को ही दलित और स्त्री आलोचना मानकर इन श्रेणियों के पहले से मौजूद होने की बात की जाए, तब तो मामला और गंभीर है। ये विमर्श क्रमशः दलित और स्त्री के हाशियाकरण के विरोध में खड़े हुए, और आप इन्हें ही दलित और स्त्री आलोचना को हाशिये पर रखने का एक और बहाना बनाए ले रहे हैं! यानी दाख़िले के चयनवाद की शिकायत होने पर आपने शिकायतकर्ताओं के जमावड़े के चारों ओर गोल घेरे बनाकर कहा कि देखो, यह जगह एकदम तुम्हारी है; अब तुम्हें कविता, कहानी, आलोचना, जो-जो करना हो, यहाँ करते रहो। इस तरह कहने को जगह मुहैया भी करा दी और अपनी जगह की अखंडता-अविकलता भी सुनिश्चित कर ली। मुझे सविता सिंह की एक बात याद आई जो उन्होंने ज़ाकिर हुसैन कॉलेज की एक संगोष्ठी में कही थी। बताया कि लेखन के शुरुआती दौर में ही उन्होंने अपना एक लेख नामवर जी को पढ़ने दिया। अगले दिन तारीफ़ तो मिली, पर इस टिप्पणी के साथ कि मुख्य मार्ग छोड़कर पगडंडी क्यों पकड़ रही हो? इस रूपक में मौजूद पदानुक्रम पर अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं।
इसके बाद बारी आई पहले तर्क की। भीड़ के शोर-शराबे में किसी गंभीर मुद्दे पर दिमाग़ ठीक से सोच न पाए और हम कुछ नाम भूल जाएँ, यह तो समझ में आता है, पर भूलने के एक ख़ास पैटर्न का बचाव कैसे करेंगे? दलितों और स्त्रियों को भूलने में ही नहीं, उनके साथ अपने मित्र बजरंग को भूलने में भी एक पैटर्न है, क्योंकि बजरंग का काम मुख्यतः दलित साहित्य पर केंद्रित है। भूलने में कोई पैटर्न न हो तो गफ़लत और बेध्यानी को उसका कारण ठहराया जा सकता है, लेकिन पैटर्न होने पर तो किसी भी समझदार के लिए बात बेध्यानी पर ही ख़त्म नहीं होगी, बेध्यानी का फ़ायदा उठाकर सक्रिय हो जानेवाले मन के उन हिस्सों तक जाएगी जिन्हें अचेतन और अवचेतन कहा गया है। तो क्या सचेत रूप से दलित और स्त्री के हाशियाकरण का विरोध करते हुए भी सोच की किन्हीं दबी हुई परतों में मुझे इस हाशियाकरण से कोई दिक़्क़त नहीं है? यह कहना तो शायद ठीक न होगा कि मैं ऐसा हाशियाकरण ‘चाहता’ हूँ, क्योंकि ‘चाहना’ एक सचेत क्रिया है और चैतन्य रूप से यह हाशियाकरण मैं ‘नहीं चाहता’ हूँ; लेकिन इस ‘न चाहने’ की जड़ें क्या इतनी गहराई तक जा पाई हैं कि चली आती सत्ता-संरचना को ‘नॉर्मल’ मानने का प्रदत्त संस्कार छिन्न-भिन्न हो जाए? अगर यह ‘न चाहना’ मन की बौद्धिक-तार्किक उपरली परत तक, इस फ्रायडीय ‘टिप ऑफ़ द आइसबर्ग’ तक ही सीमित है तो क्या इस आशंका से इनकार किया जा सकता है कि मन का जो हिस्सा इस ‘न चाहने’ से अछूता होगा, वह कई बार बहुत निर्णायक भी हो जाता होगा? क्या वह तर्क और बौद्धिकता के छद्मवेश में आकर कई बार उपरली परत की कार्यसूची भी तय करने लगता होगा? क्या यह सोचकर मुझे डरना नहीं चाहिए कि मेरे ही अंदर ताक़त के वे रिश्ते, जिनका मैं लाभार्थी रहा हूँ, एक आभ्यंतरीकृत परम्परा के रूप में मौजूद हैं और उनका बहुरूपियापन ऐसा है कि उन्हें पहचानकर ख़त्म करना भी मुश्किल है?
अल्थूसे को पढ़ते हुए मैंने समझा जितना भी कम हो, उनकी यह अंतर्दृष्टि मुझे बार-बार उनके पाठों की ओर ले जाती है कि ‘विचारधारा गहरे अर्थों में अचेतन है’। विचारधारा/आइडियोलॉजी का आशय यहाँ राजनीतिक-सामाजिक कार्यवाहियों के प्रेरक किसी ‘वाद’ से नहीं है। वह शक्ति-तंत्र और व्यक्ति के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते उन रवैयों-मान्यताओं का संघटन है जो दमन के चले आते रूपों को धुँधला/ओझल करते हुए व्यक्ति को शक्ति-संरचना में व्यवस्थित करते हैं और वर्चस्व की व्यवस्था का पुनरुत्पादन सुनिश्चित करते हैं। अल्थूसे ने इसे ‘जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के साथ व्यक्ति के काल्पनिक संबंधों के निरूपण (representation)’ के रूप में परिभाषित किया था और ज़ोर देकर कहा था कि ‘विचारधारा निश्चित रूप से निरूपणों की एक व्यवस्था है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इन निरूपणों का “चेतना” से बहुत कम लेना-देना होता है: वे आम तौर पर छवियाँ हैं और यदा-कदा अवधारणाएँ, लेकिन वह चीज़ जिसे वे अधिसंख्य लोगों पर आरोपित करते हैं, सर्वोपरि संरचनाओं के रूप में है, और यह आरोपण उनकी “चेतना” के बरास्ते नहीं होता।…लोग अपनी विचारधाराओं को “जीते” हैं… चेतना के एक रूप के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी “दुनिया” की एक वस्तु के तौर पर—ख़ुद अपनी “दुनिया” के तौर पर।’
लेकिन अल्थूसे के लिए विचारधारा के अचेतन होने का अर्थ यह नहीं है कि उसे ‘जीते’ हुए भी हम उसे जानते नहीं हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रसंग में ग़ौर किया। यह अर्थ उन लोगों के मद्देनज़र तो हास्यास्पद ही कहा जाएगा जिनके ‘गुप्त’ और ‘प्रकट’ के बीच उस तरह का अंतराल नहीं होता जैसा मेरे मामले में है, यानी जो लोग परम्परा से मिली हुई ग़ैरबराबरी की व्यवस्था का खुले तौर पर समर्थन करते हैं और मुखर रूप से जातिवादी तथा स्त्रीद्वेषी हैं। असल में, यहाँ अचेतन होने का अर्थ है—1. विचारधारा के आभ्यंतरीकरण की प्रक्रिया का चेतन न होना; और 2. अपनी विचारधारा को विचारधारा के तौर पर पहचानने से इंकार करना, उसे स्वाभाविक बात मानना। अल्थूसे कहते हैं, ‘जो लोग विचारधारा [की गिरफ़्त] में हैं, वे अपने को विचारधारा से बाहर मानते हैं: विचारधारा के प्रभावों में से एक है, विचारधारा द्वारा विचारधारा के विचारधारात्मक रूप का निषेध। विचारधारा कभी नहीं कहती: “मैं विचारधारात्मक हूँ”। यह कहने के लिए, कि “मैं विचारधारा [की गिरफ़्त] में हूँ” (बिलकुल अपवाद जैसा मामला) या “मैं विचारधारा [की गिरफ़्त] में था”, विचारधारा के बाहर यानी वैज्ञानिक ज्ञान [के दायरे] में होना ज़रूरी है।’
शायद इस बात से मैं अपने लिए थोड़ी राहत हासिल कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि मैं विचारधारा की गिरफ़्त में हूँ। ‘हूँ’ अल्थूसे के लिए थोड़ा अपवाद सरीखा मामला है (क्योंकि ‘जो विचारधारा [की गिरफ़्त] में हैं, वे अपने को विचारधारा से बाहर मानते हैं’), पर आप सचेत रूप से क्या सोचते हैं और अचेत रूप से क्या कर बैठते हैं, इसके फ़र्क़ की पहचान कर पानेवाला आत्मसाक्षात्कार शायद इसे अपवाद नहीं रहने देता। मैं वह भी हूँ जो हर तरह की ग़ैर-बराबरी को, वर्चस्व की प्रदत्त व्यवस्था को ग़लत मानता है और मिटाने की सिफ़ारिश करता है, और मैं वह भी हूँ जो अपने अन्दर की किन्हीं परतों में इस व्यवस्था को लेकर सहज है, जो थोड़ी लापरवाही की हालत में—वह भीड़ और शोर-शराबे के बीच पैदा होनेवाली असावधानी के कारण हो या नशे, उनींदेपन, तनाव आदि के कारण—वर्चस्व की इस व्यवस्था के काम आ सकता है, जो दूसरों द्वारा टोके जाने और अपने अन्दर झाँकने के लिए विवश होने से पहले व्यवस्था-अनुकूलित व्यवहार भी कर सकता है।
ऐसा कहते हुए मुझे हिंदी की विचार-परंपरा से अनगिनत उदाहरण याद आ रहे हैं, पर आत्मसाक्षात्कार को आत्मसाक्षात्कार ही रहने देना चाहिए। यह किसी और को भी अपनी चमड़ी खुरचने की प्रेरणा दे सके, इतना ही काफ़ी होगा।
(‘आलोचना’ के सहस्त्राब्दी अंक-67 में प्रकाशित संजीव कुमार का आख़िरी सफ़ा)