वागीश भैया कौन थे? या फिर, वागीश भैया कौन हैं? यह सवाल उनके परिवार के सदस्यों और विचारधारात्मक साथियों के लिए हमेशा एक गंभीर सोच-विचार उकसाने वाला सवाल बना रहेगा।
दुःख को मापने का कोई पैमाना नहीं होता। किसी के जाने के बाद उनकी कमी का एहसास लंबे समय तक बना रहता है। हम मजाक में कहते थे कि भारत में दो परिवार हैं— संघ परिवार और ‘जुगनू’ परिवार। यह सच है कि जुगनू सिर्फ एक समूह नहीं था, हम सभी के लिए अपना परिवार था।
जब मैं जेएनयू आया, बचपन की परेशानियों के बोझ से दबा हुआ-सा था। उस समय दो लोगों ने मेरी ज़िन्दगी में नयी जान फूँक दी। जैसे कि जेएनयू में आने वाले कई लोग होते थे, मैं भी अपनी पहचान, अपनी आवाज़ और अपनी जगह की तलाश में था। इन दो लोगों में से एक वागीश भैया थे—एक ऐसा व्यक्तित्व जो ताउम्र मुझे हैरान करता रहा।
जब मैं 1992 में ‘जुगनू’ में शामिल हुआ, मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि इसके अधिकांश सदस्य बिहारी थे। इसका मतलब यह था कि मुझे अपनी अंग्रेजी या तलफ़्फ़ुज़ के बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं थी। इस एक बात ने मुझे भाषाई असुरक्षा से मुक्त कर दिया। यह एक निजी क्रान्ति थी।
टेफ़्लास के संगीत कक्ष का मेरा पहला अनुभव एक दूसरी क्रान्ति थी। छात्र वहाँ ऐसे गीत गा रहे थे जो आम बॉलीवुड धुनों से अलग थे। उनमें से एक था, ‘दबेगी कब तलक आवाज-ए-आदम—हम भी देखेंगे’। यह साहिर लुधियानवी से मेरी नयी मुलाकात थी, जिन्हें मैं अब तक सिर्फ़ एक बॉलीवुड गीतकार के रूप में जानता था—जिसके शब्दों को मैं अनजाने में गुनगुनाता था। ‘जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा’ गाता था।
फिर, वे कबीर के गीत गाने लगे। उस पल तक, मेरी पाठ्यपुस्तक-निर्देशित धारणा कबीर को सिर्फ़ एक जुलाहा, एक सरल बुनकर-कवि के रूप में जानने तक सीमित थी। उस दिन, मैं तीन महान लोगों से एक साथ मिला—साहिर, एक शायराना प्रतिभा; कबीर, ज्ञान की एक शाश्वत आवाज; और फिर वागीश भैया, एक बिहारी जिसने मुझे बिहारी उच्चारण के साथ स्पष्ट अंग्रेजी बोलकर आश्चर्यचकित कर दिया। मैं यह देखकर हैरान था कि एक ही व्यक्ति कैसे भोजपुरी मैथिली, हिन्दी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं का जानकार हो सकता है। कई भाषाई दुनियाओं में आसानी से घूम सकता है।
उस समय, ‘जुगनू’ को एसएफआई की ‘सांस्कृतिक शाखा’ के रूप में देखा जाता था, एसएफआई के सदस्यों की अधिक संख्या के कारण। ये वे दिन थे जिनमें बाबरी मस्जिद के विध्वंस का हाहाकार गूँज रहा था। ‘जुगनू’ ने झेलम लॉन में एक दिन का सत्याग्रह आयोजित किया, जिसमें इस विध्वंस का विरोध किया गया। इसमें दिल्लीभर के प्रमुख बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। शाम को हमने मुनिरका की सड़कों पर मौन जुलूस निकाला—एक अनोखा गांधीवादी विरोध। इंडिया टुडे ने बाद में इसे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारत में हुआ पहला विरोध प्रदर्शन बताया।
1993 में, एसएफआई दो हिस्सों में विभाजित हो गईं। इसके बगावती सदस्य आइसा के साथ जुड़ गए, जिसने 1993 में जेएनयूएसयू का ऐतिहासिक चुनाव जीत लिया। नतीजतन, ‘जुगनू’ आइसा के सदस्यों से भर गया, और मैं भी आइसा से जुड़ गया। यह विचारधारात्मक बदलाव वाम से क्रान्तिकारी वाम तक था। यह एक ऐसा युग था जिसके बारे में इतिहासकार बिपिन चंद्र ने एक बार कहा था—“जेएनयू का आदर्शवाद इतना बुलन्द था कि छात्र उसके सहारे दुनिया जीत सकते थे।”
मैं अक्सर सोचता था कि जेएनयू में इतने सारे वामपंथी संगठन क्यों हैं और क्यों ‘इप्टा’ और ‘जुगनू’ अपने सांस्कृतिक प्रभाव के क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वागीश भैया ने समझाया कि ‘जुगनू’ का मुख्य दर्शन बहस को बढ़ावा देना और चुप्पी की संस्कृति को चुनौती देना था—एक अवधारणा जो पाउलो फ्रेरे के शिक्षा सिद्धान्त की बुनियाद है।
‘जुगनू’ ने न केवल राज्य द्वारा थोपी गई चुप्पी की संस्कृति का विरोध किया, बल्कि वामपंथ के भीतर आन्तरिक चुप्पी को भी चुनौती दी। यह तनाव यहाँ तक पहुँच गया कि क्रान्तिकारी गीतों की संरचना क्या होनी चाहिए, क्या उन्हें एक कठोर मार्चिंग ट्यून का पालन करना चाहिए, या क्या वे मेलोडिक संरचनाओं के साथ प्रयोग कर सकते हैं!
इस बहस ने वामपंथ के साथ ऋत्विक घटक के जटिल प्रेम-नफ़रत के रिश्ते को प्रतिबिंबित किया।
आज की पीढ़ी हम पर ईर्ष्या कर सकती है, क्योंकि दस साल की अवधि में, हमने 50 से अधिक स्ट्रीट प्ले किए। हमारा स्ट्रीट थिएटर, जैसा कि वागीश भैया ने सोचा था, समाधान प्रदान करने के लिए नहीं था, बल्कि संवाद को बढ़ावा देने के लिए था—अगस्तो बोआल की स्पेक्ट-एक्टर की अवधारणा के अनुरूप। वह हमें याद दिलाता था कि हमें थिएटर के माध्यम से खूँटा नहीं गाड़ना है।
वागीश भैया मानते थे कि कला का प्रभाव क्षणिक नहीं होना चाहिए। हालाँकि हम उनके द्वारा प्रस्तुत विचारों की परतों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, लेकिन जटिल विचारों को सरल भाषा में व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने हमें हमेशा आकर्षित किया।
बौद्धिक गहराई के बावजूद, उन्होंने वामपंथी संगठनों द्वारा अक्सर अपनाई जाने वाली जटिल भाषा शैली का विरोध किया। वह अक्सर कहते थे, लोग तुम्हें नहीं समझते, साथियों! एक युवा वामपंथी कार्यकर्ता के रूप में, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मेरे विचार अक्सर असंगतता में उलझ जाते थे। मेरे तर्क स्पष्टता की कमी के कारण दुर्बल थे, और मेरी अभिव्यक्ति अराजक महसूस होती थी। वागीश भैया ने धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन दिया, जोर देकर कहा कि तर्कों को सुकर होना चाहिए यदि वे लोगों तक पहुंचने के लिए हैं।
उस समय जुगनू द्वारा तैयार किए गए पैम्फलेट वामपंथी पैम्फलेट्स की तुलना में अधिक रचनात्मक थे। जैसे कि जतीन दास की दाढ़ी और आपका डिसर्टेशन, जिसने जेएनयू में फैलती उदासीनता की आलोचना की। हमारे पैम्फलेट्स अक्सर डियर वुड-बी आउटसाइडर्स से शुरू होते थे, जो जेएनयू में चल रहे बाहरी व्यक्ति बनाम अंदरूनी व्यक्ति के बहस का एक मजाकिया लेकिन तीखा जवाब था।
जुगनू में दो प्रमुख विचार प्रवृत्तियां थीं – एक वामपंथी और दूसरी गांधीवादी। वागीश भैया गांधीवादी आदर्शों की ओर झुके हुए थे, जबकि मैं एक कट्टर वामपंथी था। एक दिन, एक बैठक में, मैंने भगत सिंह के दृष्टिकोण से गांधी की आलोचना शुरू की – हवाई और अतिरंजित आलोचना। उन्होंने सीधे मुझे खारिज करने के बजाय सुझाव दिया कि मुझे हिंद स्वराज, भीखू पारेख के गांधी पर काम, द इंटिमेट एनिमी, और आशीश नंदी के सेवेज फ्रायड को पढ़ना चाहिए। जब मैंने ऐसा किया, तो मेरे लिए एक नई दुनिया, उपनिवेशवाद विरोधी विचार की, खुल गई। उसके बाद से, बिना विषय को ठीक से जाने समझे बहस में शामिल होने से परहेज किया।
वागीश भैया अक्सर मजाज की एक पंक्ति दोहराते थे: बहुत मुश्किल है दुनिया का संवारना तेरी जुल्फों का पेच-ओ-ख़म नहीं है। वह उर्दू में एपिग्लॉटल ख़ ध्वनि के साथ सहज नहीं थे और ख़म को खम कहते थे।हम सभी हंसते थे।
जुगनू वास्तव में माओ के उस कथन को साकार करता था: “सौ विचारों को प्रतिस्पर्धा करने दो और हजारों फूलों को खिलने दो।” वागीश भैया अपने गांधीवादी आदर्शों के साथ, किसी भी दृष्टिकोण को खारिज नहीं करते थे। मैंने एक दिन देखा कि एक दक्षिणपंथी व्यक्ति समूह में शामिल हो गया। हममें से अधिकांश लोगों ने दक्षिणपंथ को हमेशा एक अभिशाप के रूप में देखा था, लेकिन वागीश भैया ने उसके साथ सघन संवाद कायम किया।
‘जुगनू’ जेएनयू में तिरंगा झंडा फहराने वाला शायद पहला वामपंथी संगठन था। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हमेशा समाज के सबसे हाशिए वाले सदस्य होते थे—अक्सर गंगा छात्रावास के एक स्वीपर। हममें से कुछ, जो कट्टर वामपंथी झुकाव वाले थे, वहाँ बस चुपचाप खड़े रहे। ‘जन गण मन’ गाया गया, कई लोग गाने में शामिल हुए, लेकिन हम जैसे लोग चुप खड़े रहे। इसके तुरन्त बाद, एक क्रान्तिकारी गीत आया— ‘इसलिए राह संघर्ष की हम चुनें, ज़िन्दगी आँसुओं में नहाई न हो’। अनूप वशिष्ठ की रचना।
इस तरह के मुखामुखम ने राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बहस को तेज कर दिया, लेकिन इसमें असहमति को न केवल सहन किया गया, बल्कि उसे प्रोत्साहित भी किया गया।
आज जैसा माहौल है, किसी को भी धमकाया जा सकता है, राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। ‘जुगनू’ ने जेएनयू की असहमति की संस्कृति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वागीश भैया हमारे लिए कई मायनों में मार्गदर्शक थे। वे जेएनयू के सफ़दर हाशमी थे—अपनी मौलिक अंतर्दृष्टि के साथ। उनका मानना था कि संस्कृति कर्म को राजनीतिक दलों द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए; इसका अपना राजनीतिक जीवन होता है। वे मानते थे कि स्ट्रीट थिएटर बौद्धिक रूप से उत्तेजक होने के साथ-साथ आत्मीय रूप से आकर्षक भी होना चाहिए। उन्होंने बिहार और बंगाल के भुलाए हुए लोकगीतों को हमारे नाटकों के जटिल विन्यास में बुन दिया। किसी सिद्धहस्त की तरह।
वे हमेशा याद दिलाते थे—अगर हम वास्तव में जीना चाहते हैं, तो हमारे अपने भीतर एक रचनात्मक बेचैनी होनी चाहिए।
पिछले साल, मैंने फेसबुक पर एक कविता देखी—‘काफ़िर हूँ, सिरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए।’ यह मुझे इतनी गहराई से छू गई कि मैंने इसे राग मालकौंस में संगीत में ढाल दिया और उत्साहपूर्वक वागीश भैया के साथ साझा किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने पहले से ही अपना एक संस्करण राग पहाड़ी में बना लिया था। हमारे दिल की धड़कनों में इतना मेल था।
आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ—प्रतिबद्धता, स्पष्टता, लेखन, गायन। वागीश भैया, आपने जिस दुनिया की कल्पना की थी, वह इस डिजीटल युग में दूर होती जा रही है। हम खुद को स्क्रीन के आगे झुका हुआ पाते हैं। ज़िन्दगी का राग छूटता जा रहा है। हमें आपकी जरूरत है। इन स्थितियों को चुनौती देने के लिए, हमें एक बार फिर से जमीन पर उतारने के लिए। मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है आपसे। कृपया वापस आइए। ‘जुगनू’ की डिजीटल उपस्थिति में ही सही, वापस आइए।
—राशिद अली, सीनियर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय

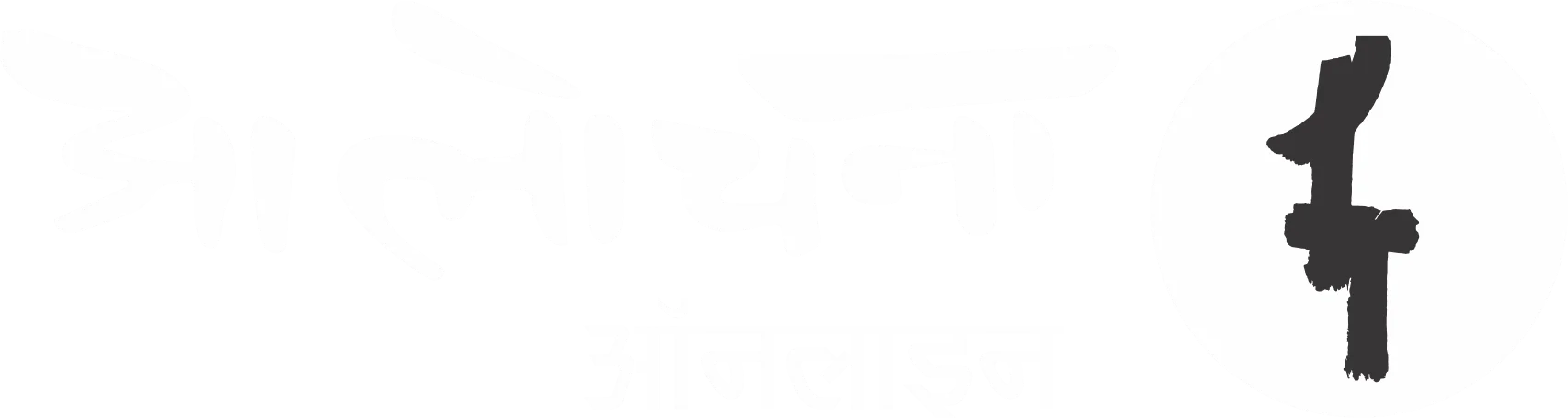
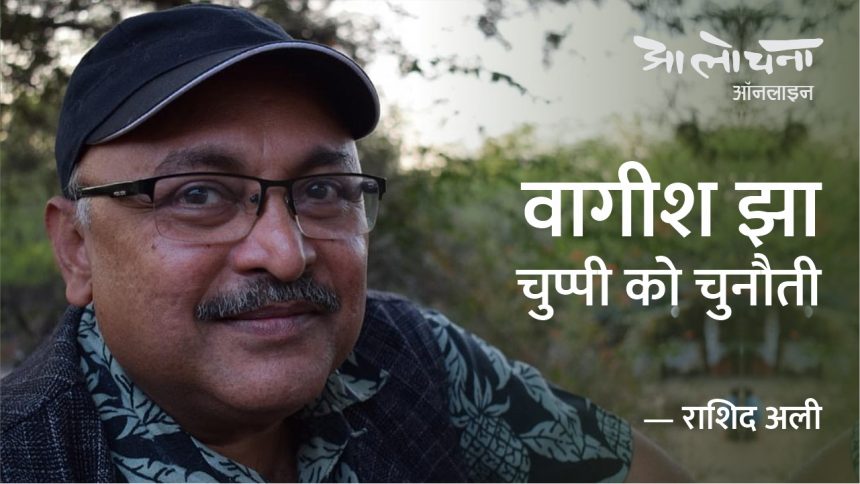
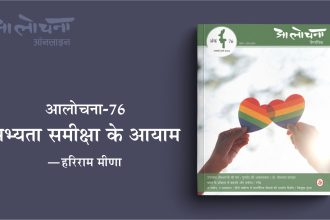
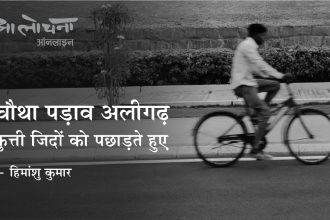
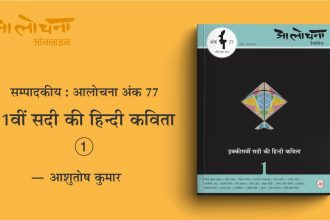
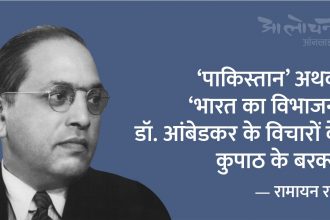
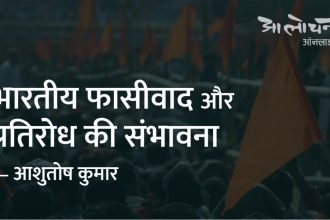

बहुत सुन्दर और इसे Rashid ही लिख सकते थे। शुक्रिया आलोचना।