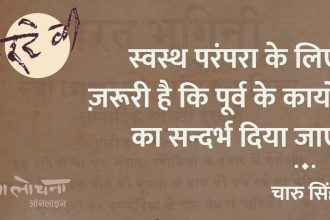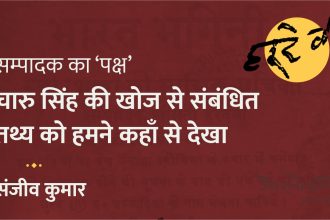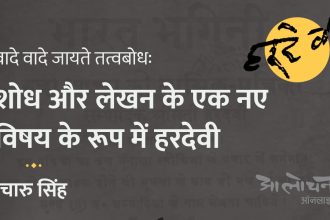अस्पताल मृत्यु से बना था। मृत्यु की ऊँची-ऊँची दीवारों में मृत्यु की खिड़कियाँ और दरवाज़े थे, मृत्यु का एक लंबा गलियारा, डॉक्टरों और नर्सों के कमरे, सीढ़ियाँ और तहख़ाने, मृत्यु की बेंचें, कुर्सियाँ, बिस्तर, हर बिस्तर तक मृत्यु पहुँचाते पाइप और नलियाँ, और नलकों से टप-टप टपकती मृत्यु। मृत्यु के बड़े गेट के अन्दर मृत्यु के छोटे गेट को खिसकाकर अन्दर क़दम रखो तो रिसेप्शन पर एक ऊबी हुई मृत्यु स्वागत करती थी और कोने में बड़े-बड़े डस्टबिन नज़र आते थे, पिछले दिन की बासी, मैली-कुचैली मृत्युओं से भरे हुए। उनके ढेर बिखरे होते थे। अलस्सुबह मृत्यु बुहारी, धोयी जा रही होती थी, नालियों में बहती नज़र आती थी। धड़कते दिल से मृत्यु की धूल से गुज़रता, मृत्यु के चमकते, चिकने फ़र्श पर एक-एक क़दम रखता, मृत्यु के गलियारे से होता हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ता मैं दूसरी मंज़िल पर आता था। वहाँ दिन-भर के शोरगुल से पहले, मरीज़ों और डॉक्टरों के आने और खिड़कियाँ खुलने, ओपीडी शुरू होने से पहले वह सुबह का एक छोटा, ख़ामोश वक़्फ़ा होता था। अगर वह सोमवार का दिन हुआ तो पहला काम होता था बाथरूम जाकर चेहरे से सफ़र की थकान और धुएँ और धूल के निशान मिटाना और तेज़ चल रही साँसों को क़ाबू करना, फिर…
इतना कहकर देवेन्द्र कुछ देर के लिए ख़ामोश हो गया। वह मेरे बचपन का दोस्त है। पिछले साल साउथ के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर वापस आया था और शहर के दूसरे छोर, दो-तीन घंटे की दूरी, पर एक उपनगर के अस्पताल में इंटर्नशिप पूरी की थी। जहाँ वह अस्पताल था, वह एक औद्योगिक इलाक़ा था जहाँ मीलों तक फैली बहुत सारी छोटी-बड़ी, क़ानूनी और ग़ैरक़ानूनी फ़ैक्टरियाँ थीं। अब उसे आगे की पढ़ाई, एम डी इन पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों की बीमारियों का विशेषज्ञ बनने के लिए वहीं वापस जाना था। वह नया-नया डॉक्टर है, बेशक पूरा नहीं, अभी डाक्टरी का छात्र ही—लेकिन उसके लिए ‘डॉक्टर’ संबोधन अभी तक मेरी ज़ुबान पर नहीं चढ़ा।
आदतन उसे नाम से ही बुलाता हूँ या कभी-कभी मज़ाक़ में कहता हूँ, डॉक्टर जिवागो। यह जिस दिन उसे साउथ के लिए उड़ना था, उससे पिछली शाम की बात है। हम दोनों उस रेलवे कॉलोनी के पार्क की एक बेंच पर बैठे थे, जहाँ उसके बड़े भाई और भाभी रहते हैं, जंक्शन से जुड़ी। माता-पिता बचपन में ही चले गए थे, उसके बाद वही उसके सब कुछ हैं। भाई, जो उससे दस बरस बड़े हैं, इसी जंक्शन पर बुकिंग क्लर्क हैं और भाभी शहर के किसी स्कूल में टीचर। उनकी अकेली बेटी मीनल पिछले ही साल…
—सोमवार को? और बाक़ी दिन? मैंने कहा।
—सोमवार बाक़ी दिनों से अलग एक ख़ास दिन होता था न। उसने कहा।—बाक़ी दिनों में तो वहीं रहता था, हॉस्पिटल से थोड़ी दूर एक किराए के कमरे में। इतनी दूर रोज़ तीन घंटे का सफ़र तय करके यहाँ से जाना, फिर शाम को उतना ही सफ़र तय कर वापस आना मुश्किल था इसलिए वीकली अप-डाउन करता था। कभी-कभी नाईट ड्यूटी भी लग जाती थी और कभी-कभी दिन-रात, चौबीस घंटे बिजी रहना होता था। हर सैटरडे यहाँ आ जाता था भाभी के हाथ का खाना खाने, मीनल की बातें सुनने। इतवार यहाँ बिताने के बाद सोमवार की सुबह यहीं से चलता था, ट्रेन से। उस दिन…नींद बहुत जल्दी खुल जाती थी। सुबह से ही दिल धड़कने लगता था, यह सोचकर कि आज…। उस दिन कुछ ख़ास होता था। बाक़ी दिनों में भी उसी के बारे में सोचता रहता था, इंतज़ार करता था।
—क्या? मैंने कहा।
—एक ख़ास चीज़, ख़ास लम्हा जो…
—इस तरह तो कुछ समझ पाना मुश्किल है। मैंने कहा।
देवेन्द्र ख़ामोश होकर कुछ सोचने लगा था, इसलिए मैंने कुरेदा नहीं। पार्क के बीच जमा बरसाती पानी में पड़ोस के गाँव ‘पसौंडा’ के या शायद क़रीब के झुग्गियों वाले ‘खोड़ा’ इलाक़े के कुछ आवारा बच्चे शोर मचाते हुए खेल रहे थे। कुछ झुंड बनाकर बैठे थे, किसी चर्चा में मशग़ूल। दो सबसे छोटे जो थे, मुश्किल से चार-पाँच साल के, नंगधड़ंग, बदमाश—उनका अलग खेल जारी था, पार्क की दीवार पर धार मारने, कुछ टेढ़ा-मेढ़ा लिखने का। वे दिन-भर गलियों में, सड़कों पर रद्दी काग़ज़ों जैसे उड़ते, डोलते, फड़फड़ाते रहते थे, कभी-कभी कुछ देर सुस्ताने के लिए कॉलोनी की एक टूटी दीवार के रास्ते पार्क में चले आते थे। आवारागर्द, बीड़ीबाज़, कुछ कचरा बीनने वाले भी। चौकीदार चीख़ते हुए उन्हें पकड़ता, भगाता रहता था।
कुछ देर उन्हें यूँ ही देखने के बाद उसने अपने आप कहना शुरू किया—आठ अगस्त की रात जो हुआ, उसके बाद वह हॉस्पिटल ख़ूब बदनाम है लेकिन जब मैंने इंटर्नशिप शुरू की तब कोई नहीं जानता था। न वो हॉस्पिटल, न वो जगह। मैं ही कहाँ जानता था। भाई-भाभी की ज़िद थी कि एमबीबीएस इतनी दूर के कॉलेज से किया है और आगे की पढ़ाई के लिए फिर दूर जाना होगा। इंटर्नशिप यहीं किसी हॉस्पिटल में करो, चाहे अनपेड ही सही। वह जगह जो है, कहने को इसी शहर का एक उपनगर है लेकिन ट्रेन से तीन-चार घंटे लगते हैं। एक छोटा-सा शहर, मैला-कुचैला, धूल से ढँका, धूप में झुलसा हुआ। उस क़स्बे का अपना अलग रेलवे स्टेशन है, कोई ‘हाल्ट’। मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना था इसलिए कि इस शहर से चलने वाली अधिकतर गाड़ियाँ वहाँ रुके बिना गुज़र जाती हैं। वैसे भी इस तरह के छोटे स्टेशन किसे याद रहते हैं? देखो, फिर भूल रहा हूँ उसका नाम, लेकिन उसकी एक ख़ास पहचान, उसका ‘पता’, अभी तक याद है…
वह एक पल के लिए ख़ामोश हो गया।
—पता? मैंने कहा।
—हाँ। उसने कहा। —और वह है…‘कट कट कटाक’ और इसके बाद काफ़ी देर तक मंद पड़ती आवाज़ …‘कटाक…कटाक…कटाक…’।
—इसका क्या मतलब? मैंने कहा।
—बताता हूँ। उसने कहा। —अलस्सुबह चलती है वह लोकल रेलगाड़ी, ईएमयू, इसी जंक्शन से वहाँ के लिए। सर्दियों के दिनों में मुँह-अँधेरे ही। हर सोमवार सुबह मुझे वही गाड़ी पकड़नी होती थी। वह स्टेशन के आख़िरी प्लेटफ़ॉर्म से चलती थी। सुबह के नीम अँधेरे में कोहरे-भरे रास्तों से निकलकर मफलरों और कम्बलों, स्वेटरों, शालों में लिपटे, भाप उड़ाते डेली पैसेंजर्स ओस से भीगे प्लेटफ़ॉर्म पर अपने क़दमों से गीले निशान बनाते हुए आते थे और सिकुड़करसीटों पर बैठ जाते थे, धीमे-धीमे ठिठुरते हुए। रात-भर खुले में खड़ी रही ट्रेन के हत्थे बर्फ़ की तरह ठंडे होते थे। कोहरा इतना गाढ़ा होता था कि डिब्बों के भीतर तक चला आता था। एक लंबी मगर भर्राई सीटी के साथ रेलगाड़ी चलती थी और थोड़ी देर के बाद शहर के बीचोंबीच एक बरसाती नदी, नदी क्या, उसकी लाश या क़ब्र—के पुल से गुज़रती थी गड़म गड़म और धड़म धड़म…तब तक मुझे नींद आ जाती थी और बहुत देर के बाद इंजन के लाइन बदलने की एक ऊँची, बुलंद आवाज़ से टूटती थी—‘कट क्ड़क कटाक’—फिर जब एक-एक डिब्बा, एक-एक पहिया उस पॉइंट से गुज़रता था तो देर तक यही आवाज़ आती थी, धीरे-धीरे मंद पड़ती हुई…कटाक…कटाक…कटाक। कभी सुनी है वह आवाज़…रोयें खड़े कर देने वाला ‘रेलवे म्यूज़िक’? जो उसे पहली बार सुने, उसे वह डरावना भी लग सकता है। शायद वहाँ लाइनों के बीच गैप कुछ ज़्यादा था, पहले से आख़िरी डिब्बे तक गाड़ी थरथरा जाती थी जैसे तेज़ हवाओं में तालाब या पोखर का पानी काँपता है।
वही था वह रेलवे का स्टेशन और वह आवाज़ उस क़स्बे का ‘पता’। गाड़ी एक लंबा गोल मोड़ लेकर धीमी पड़ती रफ़्तार में बहुत सारी मालगाड़ियों के बीच से गुज़रती हुई, जो लगता था कि हमेशा से वहाँ खड़ी हैं, हमेशा खड़ी रहेंगी—उस सारे ज़माने से छुपे छोटे से अनजान स्टेशन पर चुपचाप खड़ी हो जाती थी।
—छुपा हुआ क्यों? मैंने कहा।
—वह जगह जो है। उसने बताया। —रेलवे का डिवीज़नल हेडक्वार्टर है और वह रेलवे का अपना ‘पर्सनल’ स्टेशन। पटरियों की एक ओर रेलवे का बड़ा दफ़्तर और कॉलोनी, दूसरी तरफ़ इंडस्ट्रियल इलाक़ा…बहुत सारी छोटी-बड़ी फ़ैक्टरियाँ, मज़दूरों की बस्तियाँ, दुकानें, खोखे, होटल, एक छोटा-सा बाज़ार और वो अस्पताल। सबकुछ धूप में जला, काला। वह लोकल गाड़ी भी एक तरह से रेलवे की ‘पर्सनल’ थी, ख़ास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए जिन्हें रेलवे कॉलोनी में मकान नहीं मिल सका था।
शहर में किराये पर रहते हुए वे रोज़ तीन घंटे का सफ़र तय करके डीआरएम ऑफ़िस या उससे जुड़ी वर्कशॉप, लोको शेड, कंट्रोल रूम या किसी और दफ़्तर में ड्यूटी करने आते और शाम को फिर उतना ही लंबा सफ़र तय कर वापस जाते थे। लेकिन हर सोमवार उस गाड़ी में एक अतिरिक्त यात्री हुआ करता था, शायद अकेला शख़्स जो रेलवे का कर्मचारी नहीं था, तुम्हारा दोस्त।
—ख़ैर, ट्रेन से उस जगह पहुँचने के बाद, जिसका ‘पता’ था वह ‘रेलवे म्यूज़िक’…फिर क्या होता था?—एक गोलाई में गाड़ी रेंगती रहती थी, बहुत धीमी रफ़्तार में। खिड़की के बाहर सब सपने जैसा लगता था, एक काला सफ़ेद सपना। हर चीज़ पर कालिख की परत होती थी जैसे किसी फ़ोटो का नेगेटिव होता है, वैसे। बाक़ी यात्री प्लेटफ़ॉर्म पर उतरते थे, सिर्फ़ मैं अकेला ट्रेन की दूसरी तरफ़ सावधानी से सीढ़ियाँ उतरता झाड़ियों के और वहाँ बेतरतीब फैले औद्योगिक कचरे के बीच। एक लंबी पगडंडी, बहुत सारी सीढ़ियों, पुराने सामान, फ़र्नीचर के कंकाल, काग़ज़ों, प्लास्टिक, अवशिष्ट रसायनों, लोहे के टुकड़ों, सीलन-भरे गोदामों के बाद एक मैदान आता था जहाँ उस समय एक मटमैली, दाग़दार सुबह होती थी और मरता हुआ पतला, पीला चाँद…जैसे किसी बच्चे की आधी चूसी खट्टी-मीठी गोली। मैदान के बाद एक पुलिस चौकी थी और उसके पीछे वह चारमंज़िला इमारत जो मेरे सफ़र का गंतव्य हुआ करती थी, अस्पताल।
—वही अस्पताल जो मृत्यु से बना था, मौत के दरवाज़े खिड़कियाँ थीं और न जाने क्या-क्या? मैंने कहा।—देखो, तुम्हें बचपन से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम डॉक्टर बनने भले ही जा रहे हो, अन्दर से तुम एक पोएट हो या कलाकार। जैसे ‘डा. जिवागो’ था, कुछ-कुछ वैसे। फिर भी, कविता को अलग रखकर, एक सीधी-सादी आम भाषा में बताओगे ऐसा सोचने की वजह?
मेरी बात सुनकर वह मुझे काफ़ी देर अजीब निगाहों से देखता रहा। चेहरे पर मायूसी की एक झाईं उतर आई।
—या तो तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है या तुम किसी और दुनिया में रहते हो। उसने कहा। —तुम्हें याद नहीं कि पिछले साल कितने बच्चे मरे थे, किन-किन बीमारियों से—डेंगू, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, मलेरिया, ऑक्सीजन की कमी, नकसीर फूटना, नजला, हिचकी, बुख़ार, बेउम्मीदी। वे साल भर मरते रहे, रोज़ ख़बरें आती रहीं। बच्चों ने जैसे ज़िद ठान ली थी मरने की, चुपचाप। हमेशा मरते हैं, लेकिन पिछले साल तो उन्होंने हद कर दी। कल के पैदा हुओं से लेकर दस, बारह, पंद्रह साल तक के। मीनल भी तो पंद्रह साल की थी।…हर साल वे गर्मियों में शुरू करते हैं, मगर पिछले साल मार्च से ही शुरू हो गए, फिर सारी गर्मियों, सारी बरसात मरते रहे, हर महीने पिछले से ज़्यादा…और आठ अगस्त की उस काली रात को तो…। उसके बाद डायरेक्टर गिरफ़्तारी के डर से कुछ दिन फ़रार भी रहा, अग्रिम जमानत का इंतजाम करके ही सामने आया। सिर्फ़ यहीं नहीं, पूरे प्रदेश में, सारे देश में मरे थे, अख़बारों में आया था। इतने लेख छपे थे। हमारे अस्पताल के डायरेक्टर का बयान भी कि बच्चों का क्या है, वे तो मरते ही रहते हैं और गर्मियो में ज़्यादा मरते हैं। इसमें नई बात क्या है? इस तरह ख़बरें छापना अस्पताल को बदनाम करने के लिए दुश्मनों की साजिश है।…बहुत सारे तो मेरी ही आँखों के सामने मरे, नींद में या गोद में, कोई देर तक तितली की तरह फड़फड़ाते हुए और कोई एक ही हिचकी में अचानक। एक तो ऐसा था कि मरने के बाद भी मुस्कराते हुए नर्म होंठों से अँगूठा चूसता रहा, बदमाश। अपने पारले-जी के पैकेट, निप्पल, दूध की बोतलें, टाफ़ियाँ और लॉलीपॉप, काजल की डिबियाएँ, झुनझुने, गुड़ियाएँ…हर क़दम पर पीं-पीं बजते, जलते-बुझते जूते और ग्राइप वाटर और मुग़ली घुट्टी पाँच सौ पचपन की शीशियाँ (अ हा, मीठी मीठी )…सब कुछ पछाड़ खाती माँओं, दादियों और बुआओं के पास छोड़कर वे अचानक मरते थे जैसे…बहुत उतावली हो मरने की। उसके बाद…
—लगता है तुम्हारे भीतर डॉ. जिवागो की आत्मा जाग रही है। मैंने कहा। —तुम्हारे बताने का तरीक़ा…। ख़ैर, शुरू से बताओ। जब सोमवार को सुबह हॉस्पिटल पहुँचते थे, उसके बाद…
—सब दिन एक जैसे ही गुज़रते थे। उसने कहा।
—वक़्त की ज़ीरोक्स मशीन में एक जैसे छपते थे, एक दूसरे की कॉपी। सोमवार भी अलग नहीं होता था, बस एक ख़ास चीज़ को छोड़कर। लेकिन पहले हॉस्पिटल का आर्किटेक्चर…चार मंज़िलें थीं यह तो बता चुका हूँ। ‘चाइल्डकेयर डिपार्टमेंट’, जहाँ मुझे ड्यूटी दी गई थी, दूसरी मंज़िल पर था। बायीं तरफ़ मैटरनिटी वार्ड था जिसे हिन्दी में तुम कहोगे ‘जच्चा बच्चा विभाग’, और दायीं तरफ़ ओपीडी और स्त्री रोगों, प्रसूति रोगों और बाल रोगों के डॉक्टरों के कमरे। गायनाकालाजिस्ट्स, ओब्स्ट्रैटीशियंस और पीडियाट्रीशियंस। वार्ड के एक हिस्से में नवजात शिशु, कुछ घंटों से लेकर दो-चार दिन तक के—अपनी दुबली, कमज़ोर माँओं के संग बिस्तरों में या क़रीब झूल रहे पालनों में सोये रहते थे। वे इलाक़े की गारमेंट या प्लास्टिक, पॉलिथीन या मोटर पार्ट्स वग़ैरह बनाने वाली छोटी फैक्टरियों की मज़दूरनियाँ या मज़दूरों की पत्नियाँ होती थीं, हद से हद उनके सुपरवाइज़रों की—या दुकानदार, टेम्पो चालक, ढाबे चलाने वाले, मोटर मैकेनिक, इस तरह के लोग। सरकारी अस्पताल वहाँ से बहुत दूर था, इस वजह से। वहाँ दो बड़ी फ़ैक्टरियाँ भी थीं, एक साइकिलें बनाने वाली और एक बच्चों के खिलौने। मालिकान या मैनेजमेंट के लोग वहाँ नहीं आते थे। दूसरे हिस्से में दूसरे मरीज़ों के बेड्स थे…यानी कुछ बड़े बच्चे, पंद्रह साल तक के।
—मैटरनिटी वार्ड में बच्चे ख़ूब पैदा होते होंगे?
—हर रात कोई न कोई नन्हीं जान दुनिया में आती थी। उसने कहा। —कभी-कभी वे रात-भर आती रहती थीं, एक के बाद एक, जैसे उन्होंने पहले से आपस में, किसी सीक्रेट मीटिंग में, दिन और तारीख़ तय कर ली हो। उस रात औरतें चीख़ती रहती थीं, ख़ून लगातार बहता था। डॉ. सरिता वर्मा या डॉ. राजेश्वरी ग़ैरोला जो भी उस रात ड्यूटी पर हों, और कभी-कभी दोनों, नर्सों के झुंड के साथ यहाँ से वहाँ भागती रहती थीं। बच्चे ख़ून की नदी पार कर आते थे, ख़ून में लथपथ पहला डगमगाता पाँव दुनिया में रखते थे। कुछ बच्चे ख़ामोश होते थे या गुमसुम, उन्हें तमाचा मार कर रुलाया जाता था।
—ख़ूब भीड़ रहती होगी वहाँ। मैंने कहा। —और शोर…
—दिन के समय ओपीडी वाला हिस्सा खचाखच भरा रहता था। शोर भी रहता था। वार्ड में नवजात शिशु हमेशा नींद में होते थे, एक eternal नींद। दिन में किसी समय आहिस्ता से दरवाज़ा खिसकाकर वार्ड में घुसता था तो देखता था एक क़तार में हथेलियों के बराबर बहुत सारी छुई-मुई जानें, हौले से उठते-गिरते उनके सीने। बाक़ी बच्चे आपस में फुसफुसाकर या इशारों में कुछ बातें करते नज़र आते थे, मुझे देखकर चुप हो जाते थे। कभी-कभी कोई नवजात शिशु भी ध्यान से उनकी बातें सुनता नज़र आता था या छत पर आँखें गड़ाए कुछ सोचता हुआ। यहाँ तक कि बीच-बीच में हँस भी पड़ता था।
—क्यों नहीं, ऐसे नज़ारे डॉक्टर जिवागो नहीं देखेगा तो भला और कौन? मैंने कहा। — अच्छा यह बताओ, क्या बच्चों की बीमारियाँ…बड़ों से अलग होती हैं?
—बड़ों की जितनी बीमारियाँ होती हैं, टी.बी, नकसीर या दमा या कैंसर—वे सारी बच्चों को हो सकती हैं, मगर कुछ बच्चों की भी होती हैं अपनी ख़ास बीमारियाँ…खाँसी, दस्त, उलटी और पेटदर्द से लेकर मीज़ल्स, मम्प्स, कन्ज़क्टीवाइटिस, और भी तमाम। उनकी नाज़ुक खाल से पपड़ियाँ उतरने लगती हैं, सारा जिस्म जख़्मों से भर जाता है, हड्डियाँ चाक की तरह भुरभुरी हो जाती हैं। साँस की नली सूजकर सँकरी हो जाती है, उसके बाद एक-एक साँस जैसे मौत से मिला उधार होती है और पता नहीं चलता कि कौन-सी आख़िरी होगी। एक आख़िरी, हत्यारी हिचकी के रूप में सारा उधार एक ही बार वसूल लिया जाता है, मय सूद। बहरहाल, मैं बता रहा था, वहाँ दूसरी मंज़िल पर वार्ड और ओपीडी के बीच वेटिंग एरिया था और वहीं मेरी कुर्सी मेज़। वह एक सँकरी सी जगह थी, जहाँ…
—आर्किटेक्चर हो गया चलो। मैंने अधीर होकर कहा।—तुम्हारे ज़िम्मे जो काम थे, ड्यूटीज़…उनके बारे में…।
—ड्यूटीज़….मरीज़ों का टेम्परेचर और बीपी और वेट चेक करना, उनके पर्चों पर लिखना। मैं डॉक्टर नहीं, ‘इंटर्न’ था यार यानी डाक्टरी का स्टूडेंट, ट्रेनी। उनके ज़िम्मे ऐसे ही काम आते हैं। बच्चों के पेट दबाकर देखना, आँखें, जबान चेक करना। एक्सरे प्लेट्स और रिपोर्ट्स पर नज़र मारना।
किसी बहुत कमज़ोर दिखते बच्चे की माँ को डाँट देना… इसे ठीक से खाना नहीं देतीं क्या? वह सहमकर उसे गोद में छुपा लेती थी। कुछ बच्चे जन्म से ही बीमारियाँ साथ लाते हैं, नजला, पीलिया, एनीमिया। ऐसे बच्चों के पास जाकर पल्स, टेम्प्रेचर चेक करना, कुछ पूछना। ड्रिप, कैन्यूला लगाना, घावों की ड्रेसिंग करना। ऑक्सीजन दी जा रही हो तो उसका प्रेशर चेक करना। डॉक्टर्स जब वार्ड में राउंड लेने जाएँ तो उनके साथ चलते हुए ऑब्ज़र्व करना, सुनना, सवाल पूछना…। उनकी झिड़कियाँ खाना। सर्जरी में मदद करना, ऑपरेशन के बाद स्टिचिज लगाना, मगर उस छोटे अस्पताल में इसके मौक़े कम आते थे। मुझे तो सीनियर डॉक्टरों के इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फ़ाइल करने होते थे, ट्रेन रिज़र्वेशन भी। लेकिन इन सब कामों के अलावा एक काम और होता था…
—सिलसिलेवार बताओ। मैंने कहा।—वह बात अभी तक नहीं आई जिसकी वजह से…
—हर रोज़ सुबह मैं सबसे पहले पहुँचने वालों में से होता था। अपनी सीट पर बैठने से भी पहले जो सबसे पहला काम होता था वह था वार्ड का एक सरसरी राउंड लेना, ड्यूटी पर मौजूद नर्स या नर्सों से बात करना। बहुत हलके हाथों से दरवाज़ा खिसकाकर भीतर क़दम रखता था। बच्चे सोये हुए होते थे लेकिन कुछ उस समय भी किसी बेड या बेंच पर धीमी आवाज़ में कुछ डिस्कस करते दिखते थे। वे ग़मगीन लगते थे, अपनी उम्र से बहुत बड़े। कोने के पार्टीशन में नर्स फ़ाइलों और दवाइयों के बीच ऊँघती नज़र आती थी, या बार-बार घड़ी देखते हुए सामान समेट रही होती थी। ‘गुड मार्निंग डॉक्टर’ वह कहती थी, अक्सर बिना निगाह उठाए, थकी-सी आवाज़ में। सुबह की मद्धिम रौशनी में वार्ड में सब-कुछ ठीक वैसा ही होता था जैसा पिछली शाम…वही मरीज़, चेहरे, सीलन, धूल। लेकिन ग़ौर से देखो तो सब कुछ नहीं। अक्सर कोई एक कम होता था। एक बिस्तर ख़ाली होता था। मैं धड़कते दिल से नर्स के क्यूबिकल में जाकर पूछता था, सिस्टर वह फलाने नंबर बेड वाला…और वह मोबाइल में नज़रें गड़ाए जल्दी से कहती थी…वह, और ऊपर की ओर इशारा करती थी।
उसके बाद थोड़े बहुत हेरफेर के साथ हर बार तक़रीबन कुछ ऐसा होता था। क्या हुआ? मैं स्तब्ध होकर कहता था।—वह ऊपर चला गया।—आपका मतलब? कल रात, वह बताती थी।—उस समय डॉक्टर ग्रोवर ड्यूटी पर थे। वह मर गया? मैं कहता था।—कैसे? वह तो चार साल का…। मीज़ल्स, वह कहती थी या वाइरल फीवर या डायरिया, डिहाइड्रेशन या मम्प्स या पेट का दर्द।—मीज़ल्स यानी खसरा? मैं कहता था।—क्या खसरे से कोई मरता है, वह भी हॉस्पिटल में, डॉक्टरों के सामने? वह मर गया ज…जैसे, मैं हकलाने लगता था—जैसे…कोई काँच का गिलास टूटा हो और उसका मलबा…मैं कुछ कह ही रहा होता था कि वह बीच में ही कहती थी—नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर ग्रोवर…। ‘ऐसी की तैसी में गए डॉक्टर ग्रोवर।’ एक बार मैं फट पड़ा, सारे मरीज़ मुड़कर हमारी तरफ़ देखने लगे।—‘आप किसलिए हो यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ।’ नर्स सहमकर ख़ामोश हो गई लेकिन उसी समय, कुछ ही पलों में, सुनता हूँ, बाहर से, कहीं क़रीब से एक ख़ट ख़ट बढ़ी आती है। पलटकर देखा तो दरवाज़े पर एक पथरीले चेहरे वाली अधेड़ नर्स खड़ी थी। —बिहैव योरसेल्फ़ डॉक्टर…यू ऑलवेज क्रिएट न्यूसेंस। उस दिन भी आपने ऐसे ही सीन क्रिएट किया था। मैंने डायरेक्टर से या अपनी यूनियन में शिकायत कर दी न तो आपकी डॉक्टरी धरी रह जाएगी।
मैं उसका चेहरा देखता रहा, अवाक्। मेरे भीतर कुछ रुँधने लगा, आँखों के सामने कुछ धुंध जैसा…। चुपचाप सिर झुकाए बाहर चला आया, मन ही मन कहता हुआ…सॉरी मैडम, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। आप बहुत सीनियर हैं और मैं तो अभी…। लेकिन…लेकिन…आप सोचो मैडम…वह जो मर गया, वह कल तक…अभी कुछ घंटों पहले एक धड़कती हुई जान था। आपने ‘स्टेथो’ लगाकर उसकी धड़कन सुनी थी, वह अभी तक सुनाई देती होगी। उसके कूल्हे पर इंजेक्शन लगाया होगा तो अभी तक वह छुअन आपके हाथों में होगी। वह कैसे इस तरह…और आप…
—मैं समझ गया। मैंने कहा। —ऐसा ही कुछ अंदाज़ा था मुझे।
—क्या मतलब? उसने कहा।
—ये जो ‘डॉक्टर जिवागो’ क़िस्म के लोग होते हैं। मैंने कहा। —एक ख़ास तरह के ‘नाज़ुकमिज़ाज’, ‘निरीह’, ‘कातर’, ‘विकल’, कमज़ोर दिल वाले ‘संवेदनशील’ लोग…मौतों और लाशों के सामने काँपने लगते हैं। आँखों के सामने अँधेरा छाने लगता है। दिल ऐसे धड़कते हैं जैसे…। वे ‘शव’ शब्द से ख़ौफ़ खाते हैं और ख़ून बहता देख लें तो उनकी अपनी नसों में ख़ून जमने लगता है। ऐसे लोग डॉक्टरी के पेशे में…।
—ग़लत समझा है डियर तुमने। उसने उदास स्वर में कहा। मज़ाक़ बनाना चाहते हो तो बेशक बनाओ लेकिन…कुछ और है जो मुझे परेशान कर रहा है। उसके बारे में सोचते हुए सिर चकराने लगता है। उसके मायने भी साफ़ नहीं।
—‘डॉ. जिवागो’ क़िस्म के लोग…मैंने कहा। —बहुत कुछ ऐसा देख सुन लेते हैं जो होती ही नहीं। सिर्फ़ उनके मन की छाया होती हैं। फिर भी बताओ क्या चीज़ है। और वह ख़ास काम भी जो तुम्हारे ज़िम्मे था।
—वह काम…उसने कहा।—एक फ़ॉर्म भरना होता था।
—कैसा फ़ॉर्म?
—किसी मरीज़ की मौत होने पर…फ़ॉर्म नंबर फोर-ए, नियम सात के अंतर्गत…‘मेडिकल सर्टिफ़िकेट ऑफ़ कॉज ऑफ़ डेथ’। ‘आई हियरबाई सर्टिफाई दैट द डिसीज्ड…’।
नाम, उम्र, पता, माता-पित़ा का नाम, मरने का समय, मरने की जगह, मरने का कारण। फ़ॉर्म भरकर डॉक्टर के दस्तख़त कराने होते थे। हफ़्ते-भर ये फ़ॉर्म मेरे पास एक फ़ाइल में जमा होते रहते थे, चार, आठ या दस। एक बार तो पूरे सोलह हो गए थे। आख़िरी काम होता था हफ़्ते-भर के फ़ार्मों पर वहाँ के सबसे बड़े बॉस यानी मेडिकल डायरेक्टर की घुग्घी बिठवाना जो केवल सोमवार को आता था।
—और बाक़ी दिनों में?
—उन दिनों शायद दूसरे हॉस्पिटल्स। मैंने सुना था कि कई हॉस्पिटल्स थे जहाँ वह इसी तरह…।
—डेथ सर्टिफ़िकेट…उसका क्या होता था? और डॉक्टर के साइन करने के बाद डायरेक्टर की घुग्घी क्यों…?
—क़ानून है कि हर जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखा जाए। डॉक्टर के सर्टिफ़िकेट के आधार पर रजिस्ट्रार का दफ़्तर फाइनल मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करता है। बच्चों का बर्थ सर्टिफ़िकेट और बूढ़ों का डेथ सर्टिफ़िकेट, यहाँ तक तो समझ में आता था, लेकिन बच्चों का, शिशुओं का डेथ सर्टिफ़िकेट, वह मेरे लिए एक पहेली था। मैं सोचता था कि उसकी ज़रूरत क्यों होती होगी। फिर भी रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी होता था…उन घोर अभागे मामलों में भी जहाँ जन्म और मृत्यु का प्रमाणपत्र एक ही होता था…फ़ॉर्म नंबर थ्री, नियम बारह के तहत। कुछ भी हो, रिकॉर्ड दुरुस्त रहने चाहिए।…मैं अपनी मेज़ पर होता था, इर्द-गिर्द बच्चों से घिरा हुआ। उनकी सुई जैसी निगाहें जिस्म को आर-पार भेदती महसूस होती थीं। उनसे नज़रें चुराते हुए जब मैं उम्र के कॉलम में भरता था वन मंथ या वन वीक या कुछ घंटे…हाथ काँपते थे। बच्चों के नाम लिखता था डिंपल, डॉली, मुन्नू या un-named…उन सबके चेहरे सामने आ जाते थे। ‘मरने का कारण’ मैं डॉक्टर के भरने के लिए ख़ाली छोड़ देता था। अगला काम होता था हॉस्पिटल की भीड़ में उस डॉक्टर की तलाश…डॉक्टर ग्रोवर या डॉक्टर मेहंदीरत्ता या…। डॉक्टर मेहंदीरत्ता हमेशा जल्दी में होता था, सीढ़ियों पर या बरामदे में तेज़ रफ़्तार चलते हुए कहता था—एह की ए?
सर, यह फ़ॉर्म। मैं साथ-साथ चलते हुए कहता था।
केहड़ा फ़ॉर्म?
सर, फ़ॉर्म नंबर फ़ोर-ए। और यह कॉलम भी सर…।
केहड़ा कॉलम?
सर, यह…मैं ‘मरने का कारण’ पर उँगली रखते हुए कहता था।
यार तू वी कमाल कर्दा ऐ, ऐ ते सिस्टर दस्सेगी न? फ़ाइल इच वेख के। इन्ने मरदे ने, मैन्नु कीवें याद रयेगा? तूं वी यार…
वह तेज़ी से चलता हुआ कहीं ग़ायब हो जाता था और मैं वह काँपता हुआ काग़ज़ थामे वहीं गलियारे में खड़ा रहता था। लोना खाई छत या दीवार से मौत की एक पपड़ी या लोंदा मेरे सिर पर गिरता था, धप। अगले दिन मुझे डॉक्टर को फिर पकड़ना होता था, उसके कमरे में या गलियारे में या किसी वार्ड में। एक बार जब वह पकड़ में आया तो मैंने जल्दी से कहा…लेकिन सर एमबीबीएस में हमें पढ़ाया गया था कि इस बीमारी का वायरस बहुत पहले… की कैणा चाऊँदा ए, पुत्तर? उसने ऊबे भाव से कहा। सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने हकलाते हुए कहा। —लेकिन…ये बच्चे कुछ कहना चाहते हैं।
कौन?
सर…ये…। मैंने हाथों में पकड़े फ़ॉर्म उसके सामने रख दिए।
वह बहुत देर तक मुझे देखता रहा, अजीब निगाहों से। फिर उसने कहा—पुत्तर, एक गल दस्नी सी, तूं बुरा ते नईं मन्नेगा न?
नहीं सर, कहिये क्या बात है?
यार तेरी पिठ दे पिच्छे…लोकी जाणदा ए, की कैंदे ने? ल्यो जी, आ गया पग्लैट डॉक्टर। यार तू बेकार दे पंगे न लित्ता कर। डॉक्टर बनणा चाऊँदा ए के नईं? तेरे पेरेंट्स…
—और सोमवार को क्या होता था? मैंने कहा।
—सोमवार? बता चुका हूँ, उस दिन डायरेक्टर से सर्टिफ़िकेट्स पर साप्ताहिक घुग्घी लगवानी होती थी। तुमने पूछा था कि डॉक्टर के दस्तख़त के बाद डायरेक्टर की घुग्घी की क्या ज़रूरत थी? उसने ही यह नियम बनाया था कि हॉस्पिटल से कोई भी डेथ सर्टिफ़िकेट जारी हो तो उसकी जानकारी में, उसे दिखाकर। शायद वह तसल्ली करना चाहता होगा कि किसी मामले में कोई क़ानूनी पचड़ा न हो। वह साठ के पास पहुँचा एक भारी बदन और सूजे चेहरे और मोटे पपोटों वाला अधेड़ था। एक ही मुद्रा में अपनी टेबल पर बैठा मिलता था, फ़ाइलों और काग़ज़ों से घिरा। उसके चेहरे पर हमेशा खीझ रहती थी। —येस? वह मोटे चश्मे के पीछे से देखता था। इंटर्नशिप के पहले दिन मैंने उसे ही रिपोर्ट किया था, फिर भी वह मुझे भूल जाता था। हर बार मुझे नए सिरे से अपने बारे में बताना होता था, सर, डॉ. देवेन्द्र, डूइंग इंटर्नशिप।
—वह ख़ुद भी एक डॉक्टर था?
—हुआ करता था कभी लेकिन अब नहीं। पता चला कि वह बहुत पहले एक आई सर्जन था। उसी इलाक़े में उसका एक क्लीनिक था छोटा-सा। फिर उसकी अपनी आँखें ख़राब होती गईं, चश्मा मोटा, और मोटा होता गया। और भी न जाने कौन-कौन सी बीमारियाँ। उससे प्रैक्टिस छूट गई और सर्जरी करना तो बिलकुल नामुमकिन। फिर उसने अपनी फ्रैटर्निटी के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक हेल्थकेयर कंपनी की शुरुआत की। वह धीरे-धीरे बड़ी होती गई। क्लीनिक पहले अस्पताल बना, फिर बढ़ते-बढ़ते कई अस्पताल। अब वह सिर्फ़ डायरेक्टर था…कंपनी का एक बड़ा शेयर होल्डर। एक तरह से हॉस्पिटल का आधा या चौथाई मालिक। वह मोटे चश्मे के पीछे से सवालिया निगाहों से देखता था। मैं चुपचाप वे फ़ॉर्म्स उसके सामने रख देता था और धड़कते दिल से इंतज़ार करता था।
—किस चीज़ का इंतज़ार?
—उसी लम्हे का जिसका पूरे हफ़्ते इंतज़ार करता था।
जिसका हर समय ख़याल बना रहता था। वह लम्हा धीरे-धीरे क़रीब सरकता आता था और मैं…। बात यह है कि… कैसे कहूँ? शायद यह अजीब लगे लेकिन…मुझ पर यह उत्सुकता हावी रहने लगी थी कि एक साथ कितने फ़ॉर्म्स सामने होने पर उसके चेहरे पर कोई तकलीफ़ उभरेगी। कोई शिकन, सलवट नज़र आएगी। कुछ कहेगा, हाथ काँपेंगे। अभी तक जितने भी फ़ॉर्म्स रहे हों, दो-चार या आठ या दस, उसका चेहरा एक-सा सपाट रहता था। फ़ॉर्म्स हर हफ़्ते बढ़ते जाते थे मगर वह एक जैसे ऊबे भाव से घुग्घी बिठा देता था। मैं सोचने लगा था कि क्या वह जानता था कि वे मृत्यु प्रमाणपत्र थे…डेथ सर्टिफ़िकेट्स? क्या वह ‘मरने’ का मतलब जानता था? जब वह उड़ती-सी निगाहों से मुझे देखते हुए फ़ॉर्म्स वापस थमाता था तो टेबल से उठाकर मोहर मुझे ख़ुद लगानी होती थी।
—तो यह थी प्रॉब्लम हमारे डॉ. जिवागो की। मैंने कहा।
—आगे?
—एक बार, सिर्फ़ एक बार उसने मेरे चेहरे पर कुछ देखा और सीने पर लगी पट्टी से मेरा नाम पढ़ते हुए कहा, बैठो।
मैं उसके सामने की कुर्सी पर बैठ गया, चुपचाप उसे ताकते हुए।
क्या कोई परेशानी है? उसने कहीं जमा पानी से उठते बुलबुलों जैसी बुड़-बुड़ आवाज़ में कहा।
नहीं तो। मैंने कहा। क्योंकि और कुछ सूझा नहीं।
तुम्हारे चेहरे से लगता है कि…। वह कुछ कहते-कहते रुक गया।
सर, इतने बच्चे मर रहे हैं। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा।
तो? उसने कहा।
मैं ख़ामोश रहा।
अख़बार तो कुछ भी छाप देते हैं। मैंने ज़िले के और सारे स्टेट के हॉस्पिटल्स के डाटा निकलवाए हैं। ज़िले के जितने हॉस्पिटल्स हैं, ‘उनकी मौतों’ से ‘हमारी मौतें’ कम हैं। और स्टेट का मरने का जो एवरेज आता है, उससे भी…
सर, मेरा मतलब यह नहीं था कि यहाँ दूसरे हॉस्पिटल्स से ज़्यादा…
तो क्या प्रॉब्लम है?
सर, बच्चों का मरना, इतनी तादाद में…
वो तो मरेंगे ही। यह हॉस्पिटल है।
जी…
फिर?
वो सब मेरी नींद में लौटकर आते हैं सर, मैं कहना चाहता था। अपनी बड़ी-बड़ी गोल आँखों से घूरते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। फ़िज़ूल था यह, मैं जानता था कि वह क्या कहेगा। किसी निद्रा रोग विशेषज्ञ से मिलो यानी सोम्नोलोजिस्ट। वह बहुत सारी मशीनों, तारों, ट्यूबों और जलती-बुझती लाइटों के बीच सुला देगा और तुम्हारी नींद की, सपनों की जाँच करेगा। या ऐसा ही नाज़ुक कलेजा है तो डाक्टरी छोड़कर शायरी पकड़ो। या शुरू में सबको ऐसा लगता है मगर फिर आदत हो जाती है। डॉक्टर और ख़ून और मौतें, यह एक शाश्वत तिकड़ी है। ऐसा ही कुछ। वह फिर अपने काग़ज़ों में व्यस्त हो गया। सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे उसका सूजा, फूला, फटा-सा चेहरा याद आता रहा, उसकी बुड़-बुड़ आवाज़ कानों में पड़ती रही। मैं इस ख़याल से काँप गया कि क्या वही था मेरा भविष्य और भाग्य और आगे का जीवन…वे सारे मृत्यु प्रमाणपत्र फिसलकर गिर पड़े, उड़ते हुए सीढ़ियों पर और गलियारे में यहाँ-वहाँ फैल गए। मेरे भीतर न ताक़त की एक भी बूँद बाक़ी थी, न उछाह का कोई क़तरा। हताश और रुआँसा, यूँ ही सीढ़ियों पर बैठा रहा।
सुनसान गलियारे में नीम रोशनी थी। उसके आख़िरी छोर पर खिड़की के परे बादल थे, बहुत पुराने, बचपन जैसे बादल। मुझे लगा जैसे उन बादलों में से एक गुच्छा उतरकर भीतर चला आया, बरसते हुए धीरे-धीरे क़रीब आता रहा। काफ़ी पास आने पर मैंने देखा, वह नर्स की सफ़ेद, चुस्त पोशाक में एक अधेड़ सिस्टर थी, शायद साउथ के किसी इलाक़े की। बिखरे काग़ज़ों को देखकर उसने अपनी चमकीली आँखों और उजली मुस्कान से मुझे दूर से ही आश्वस्त किया और धीरज से एक-एक काग़ज़ जमा कर मेरे पास ले आई। पता नहीं वह कौन थी और कहाँ से आई थी, लेकिन…उसकी आँखों में कुछ था कि उनमें देखते हुए मेरे भीतर का सारा भय एक ही पल में भाप बनकर उड़ गया। यही नहीं, यह भी लगा, साफ़-साफ़, कि समूचे अस्पताल में अगर कोई था जिसकी मौजूदगी में मैं निर्भय हो सकता था तो वह वही थी, सिर्फ़ वही। जब उसने पास आकर काग़ज़ मेरी ओर बढाए, मैं जान-बूझकर निगाहें झुकाए बैठा रहा। मैं एक हमदर्दी भरे ‘टच’ के लिए तरस रहा था—और मन ही मन कहा भी, छुओ मुझे सिस्टर, बस एक छोटी-सी छुअन। उसने मेरे कन्धों पर हाथ रखा और उसी अ-विकार स्मित के साथ धीमी आवाज़ में कहा, टेक केयर ब्रदर। काग़ज़ थमाकर वह अपने रास्ते पर चली गई। मैं दूर तक उसे देखता रहा जो न जाने कहाँ से आई और मौत के उस सूने गलियारे में मुझे ज़िन्दगी की एक घूँट… नहीं, ‘लार्ज पैग’—पिला गई, बिना जाने ही। मन ही मन शुक्रिया कहते हुए मैंने उसे चुस्कियों में पिया, देर तक। बाद में मैं पूरी इंटर्नशिप के दौरान उसे ढूँढ़ता रहा लेकिन वह नज़र नहीं आई।
दिन की आख़िरी बात और बताता हूँ। शाम को लौटने के समय तक अँधेरा हो जाता था। कमरे वापस चलने के लिए पार्किंग से अपना सेकंड हैंड स्कूटर निकालता था जो ऊँची भड़भड़ के साथ चलता था और अक्सर दम तोड़ देता था। पार्किंग के गेट पर ही वे मुझे घेर लेते थे, अपने नन्हें अँगूठे लहराते हुए लिफ़्ट माँगते थे। मैं दूर से ही पहचान लेता था…वही बच्चे जिनके सर्टिफ़िकेट्स उस दिन बने होते थे। कुछ स्कूटर पर सवार हो जाते थे, कुछ मेरे कन्धों पर। देर हो जाए तो मैं रास्ते में एक ढाबे से लंच बँधवाता था या ब्रेड ऑमलेट से काम चलाता था। उन्हीं के साथ रात का खाना खाता था, फिर बिस्तर में उन्हीं के संग सो जाता था। हम गप्पें मारते थे। वे एल्फाबेट्स और राइम्स और जोक्स सुनाते थे। लेकिन…कितना ही ज़ोर देकर पूछो इतनी जल्दी जाने की वजह…वे सफ़ाई से गच्चा दे जाते थे। बस यही एक बात थी जो वे एक ज़िद्दी तरीक़े से अपने दिलों में छिपाए रखते थे, नटखट, चालाक, बदमाश।
कुछ शोर होने से हमारा ध्यान भंग हुआ। चौकीदार जो अभी तक ग़ायब था, उन आवारा बच्चों को पार्क के बाहर भगा रहा था, चिल्लाते हुए, स्साले बदमाश, फिर नज़र आए तो…। जब दुबारा ख़ामोशी लौटी तो देवेन्द्र ने आगे कहना शुरू किया—सारी बातें कुछ तफ़सील से इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें अन्दाज़ हो कि जब उसका…मीनल का फ़ोन आया, मैं कैसे हालात में था। दिन-भर और कभी-कभी रातों में भी, दवाइयों और अल्कोहल की गंध के बीच, यही सब देखते-समझते, नोट्स लेते सीनियर्स के इर्द-गिर्द रहना उन दिनों मेरी दिनचर्या थी। दिन उनकी झिड़कियाँ सुनते बीतते थे और रातें मरे हुए बच्चों की बातें और कराहें और बुदबुदाहटें। ऐसे में जब उसका फ़ोन आया…।
एक बार नहीं, दो-तीन बार आया था फ़ोन, मगर मैं अपनी इंटर्नशिप में गले-गले तक डूबा था। एक-एक मिनट का टोटा था। सुबह उठते ही अपने खड़खड़िया स्कूटर पर अपना छोटा सफ़ेद कोट और स्टेथो लेकर हॉस्पिटल भागता था। वहीं कैंटीन में कुछ उल्टा-सीधा खा लेता था। दिन देखते ही देखते पता नहीं कहाँ चला जाता था। रात बहुत देर से लौटता था, बस दो-चार घंटे की नींद लेने, और वह नींद भी…। कुत्ते भौंकते हुए पीछा करते थे। शोर मचाती एम्बुलेंसें आती रहती थीं। मेन गेट से लगातार स्ट्रेचर आते रहते थे और पीछे के गेट से लाशें निकलती थीं, एक के बाद एक। अचानक बहुत सारे लोगों की एक साथ रुलाई का शोर उठता था और किसी बच्चे को इंजेक्शन देते मेरे हाथ काँप जाते थे। मरीज़ों की बात समझने के लिए एक-एक लफ़्ज़ ध्यान से सुनना होता था, बार-बार रिपीट करवाते हुए। वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी, फ़ोन साफ़ सुनने के लिए एकदम बाहर जाओ। जब पहली बार फ़ोन आया तो शोरगुल के बीच बस इतना सुनाई दिया…अच्छा नहीं लगता, उसी समय सीनियर चीख़ने लगा, किधर ध्यान है मिस्टर? अगली रात उसका फ़ोन फिर आया जब मैं अपने कमरे में था। मैं उस समय अपनी टूटी-फूटी नींद में, एक सपने में था। मैं एक गलियारे से गुज़र रहा था जहाँ एक क़तार में सफ़ेद कपड़ों से ढँके बहुत सारे मृतक शरीर थे। कुछ तो इतने छोटे थे जैसे…स्कूली बस्ते। कुछ के पैर, सिर्फ़ पैर, कपड़ों के बाहर निकले नज़र आते थे और उनके अँगूठों में लटके टैग्स। बच्चो, मैं सपने में ही मन ही मन कहता हूँ—यह कोई मरने की उम्र है? कहाँ से पकड़ ली यह अजीब-सी ज़िद? चुपचाप चले जाते हो, बिना कुछ कहे। हमें बताओ इतनी जल्दी जाने की वजह, वह नहीं जो मैं फ़ॉर्म नंबर फोर-ए में भरता हूँ, एनसेफेलैटिस और टाइफाइड और मलेरिया…ये सब नहीं, असली वजह…। क़तार में जो सबसे पहला है उसका चेहरा हवा के झोंके से ज़रा-सा उघड़ता है। दूर एक पहचानी, डूबती-सी आवाज़ सुनाई देती है…चाचा, मन नहीं लगता। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं जल्दी से पास जाकर देखता हूँ…स्कूल ड्रेस में वह मीनल है, हमारी लख़्ते-जिगर, आँखें मूँदे हुए। एक चीख़ के साथ नींद खुल गई। दिल इतना तेज़ धड़क रहा था कि…। मैं उठकर बैठ गया, खुली आँखों से कमरे का घुप अन्धकार पीता रहा, पता नहीं कितनी देर।
फिर नींद आ गई। कैसा ही दहशतनाक हो सपना, नींद आ ही जाती है, बेशक कुछ टूटी-फूटी। जैसे…कितना ही बड़ा दुःख हो, जल्दी या कुछ देर से भूख लगती ही है और कितनी ही शर्म आए, रोटी स्वाद भी देती है। सुबह कुछ देर से नींद खुली। मैंने देखा कि मोबाइल में पिछली रात की उसकी कॉल दर्ज थी। मिस्ड कॉल नहीं, पूरी कॉल। रात तीन बजकर चालीस मिनट, जब घड़ियाँ बाँहें फैला देती हैं। क्या उसने सपने में नहीं, सचमुच फ़ोन पर कुछ कहा था? मुझे कुछ भी याद नहीं आया। शायद वह कुछ कहती रही लेकिन मैं अपनी नींद में डूबा रहा। मैंने सुना नहीं। उसने हाथ बढ़ाया था लेकिन मैंने थामा नहीं। उसे फ़ौरन फ़ोन करने का ख़याल आया मगर वह उसके स्कूल का वक़्त था। ठीक बीस मिनट के बाद भाई का वह मनहूस फ़ोन आया।
देवेन्द्र ने आगे कहा : न पैसे थे मेरे पास, न होश ठिकाने थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भाई ने टूटते हुए शब्दों में जो बताया, मेरे भीतर उतरा ही नहीं। उस समय यह भी नहीं कह सका कि मैं पहुँच रहा हूँ, और बाद में उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ़ आता रहा। वहाँ से यहाँ जाने वाली पहली गाड़ी शाम को थी और उस दूर दराज़ के इंडस्ट्रियल एरिया में टैक्सी मिलना मुश्किल था। पैसों का इंतज़ाम करने में भी काफ़ी वक़्त गया, एक दूसरे इंटर्न से उधार लेने पड़े। हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ अहाते में ‘ऑक्सी-एयर’ वालों का एक ट्रक खड़ा नज़र आया। वे बेसमेंट में ऑक्सीजन के सिलिंडर रिप्लेस करने आए थे। बहुत सारे मास्क लगाए मज़दूर, कुछ तो डबल मास्क लगाए, उन बड़े-बड़े सिलिंडर्स को फ़ुर्ती से लुढ़काते हुए बेसमेंट में ले जा रहे थे, फिर भी उन्हें अपना काम पूरा करने में दोपहर हो गई। ‘ऑक्सी-एयर’ के ट्रक ने लिफ़्ट दी मगर आधे रास्ते तक ही। उसके आगे भी टैक्सी फ़ौरन नहीं मिली। यहाँ तक आने में बहुत लंबा वक़्त लगा, पूरा दिन और आधी रात। मैं उस समय टैक्सी में, ट्रैफ़िक के बीच था जब जले हुए काग़ज़ों जैसी घुप अँधेरी रात उतरी—सोचता हुआ कि उन्होंने शाम तक मेरा इंतज़ार किया होगा लेकिन अब वह राख के ढेर में बदली जा रही होगी। आधी रात से ऊपर का वक़्त रहा होगा जब यहाँ पहुँचा।
देवेन्द्र ने आगे कहा : कॉलोनी के गेट से घर तक लड़खड़ाते हुए चल रहा था जैसे रास्ता भूल गया था। वही मनहूस सड़क थी जिस पर वह सुबह के समय, जैसे हर रोज़ निकलती थी, वैसे ही, अपनी स्कूल ड्रेस में घर से चली होगी लेकिन आगे जाकर बाहर का रास्ता लेने की जगह, जब इंजन की पहली सीटी सुनाई दी, स्टेशन की ओर मुड़ गई। बरसात रही होगी, उसने एक छतरी ले ली होगी। वही पानी अभी तक गड़हों में जमा था जिसमें चाँद खोया सा, गुमसुम, बीच-बीच में झाँक जाता था। एक अपाहिज बीमार कुत्ता डगमगाया हुआ साथ चल रहा था, भगाने पर भी लौट आता था। पूरा एकांत मिलता तो शायद मैं रो पड़ता या चिल्लाता—लेकिन नहीं, रोना नहीं था, कुछ भी हो। घर तक पहुँचते-पहुँचते मैं हाँफने लगा। वह बाक़ी मकानों की तरह अँधेरे में डूबा था। उसे देखते हुए यह सोचना नामुमकिन था कि उस घर की अकेली लाडली बिटिया…उसी दिन…। बत्ती काफ़ी देर के बाद जली। दरवाज़ा भाभी ने खोला, पीछे भाई नज़र आए। घर के भीतर क़दम रखने पर एक असह्य ख़ालीपन महसूस हुआ, दीवारों, छत और फ़र्नीचर, हर चीज़ से रिसता हुआ।
कैसे ज़र्द थे दोनों के चेहरे, और उन पर कितनी उम्र लदी थी। मैं सोचता आया था कि जब वे सामने होंगे तो सँभालना मुश्किल होगा, हम साथ-साथ रोएँगे। लेकिन कोई रुलाई नहीं उमड़ी, न किसी ने कुछ कहा। एक दूसरे की आँखों में और चेहरे की लकीरें देखते हुए हम बस बैठे रहे चुपचाप। जैसे यह अपने आप तय हो गया था कि हमें रोना नहीं था, कुछ भी हो। हमें रुलाई को भीतर भींच लेना था। नहीं, हमारे आँसू नहीं सूख गए थे, न रोने में हमें कोई शर्म थी। एक दूसरे के साथ रोना छाती से कुछ बोझ हल्का ही करता…लेकिन…लेकिन…यह कहीं ‘होनी’ को, उसकी अटलता को स्वीकार करना होता, उस बदज़ात के आगे सर झुकाने जैसा जो हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस आई थी। मौत नाम की चुड़ैल जो सामने बैठी थी, घूरे जाती थी। न रोना उसे बेमानी, बेपानी करने की तरकीब रही होगी।
—भूख लगी है? सूखे गले से भाभी ने इतना ही कहा।
—नहीं। मैंने कुछ खा लिया था। मैंने कहा।
फिर भी भाभी उठी और कुछ लाने किचन में चली गई।
मैं बैठक से जुड़े मीनल के कमरे में जाकर, बत्ती जलाकर यूँ ही खड़ा रहा। वह वहीं बैठकर अपनी पढ़ाई करती, सोचती, कल्पनाएँ करती थी। कविताएँ भी लिखती थी। मैं उसकी चीज़ों को अवाक् देखता रहा और मेरे भीतर कुछ रुधिर सरीखा बूँद-बूँद बहता रहा। वह रात ऐसे ही गुज़र गई।
आने वाले तीन-चार दिन, ख़ाली, ख़ामोश और कहीं अटके हुए, बहुत धीमे-धीमे बीते। दिन बहुत लंबे थे लेकिन रातें उनसे भी ज़्यादा। हम एक दूसरे के सामने थे लेकिन कुछ भी कहने को नहीं था। जैसे हमारी याददाश्त चली गई थी या गले ज़ख़्मी थे—या हम एक हारी हुई सेना के सिपाही थे, एक दूसरे से मुँह छुपाते हुए। हर साँस सीने को खुरचते हुए उतरती थी, इस तरह जैसे यह कोई गुनाह था, भद्दा और भयानक, कि हम अब भी ज़िन्दा थे और साबुत सलामत। कभी-कभी घर के सन्नाटे में कहीं दूर भाभी की दबी सुबकियाँ सुनाई देती थीं। कोई हिलता नहीं था इसलिए कि सब फ़िज़ूल था—तसल्ली देने वाले शब्द, प्रार्थनाएँ, अध्यात्म, भगवान। वे उसका कमरा भीतर से बंद कर चटाई पर पालथी मारे उसकी तस्वीर के सामने बैठी होंगी, आँखें मूँदे उसे याद करती, अपनी ही किसी टूटी-फूटी प्रार्थना में निमग्न। वहाँ एक दिया दिन-रात जलता था। पहले दिन वे उसकी चीज़ें…नोटबुक, रजिस्टर, डायरियाँ, उनका एक-एक पन्ना खोलकर कुछ खोजने की कोशिश करती रहीं। लैपटॉप में भी एक-एक फ़ाइल और फोल्डर, और उसका मोबाइल भी। कहीं कोई इशारा, कोई बात जिसमें उस सवाल का कोई जवाब हो जो हर घड़ी आँखों में घूरता था। कुछ पता, कोई भेद। अब भी वे कमरा बंद कर रोज़ कुछ ढूँढ़ने की कोशिश करती थीं, ख़ास तौर पर उन किताबों, कॉपियों में जिन पर धूल और बारिश के निशान थे, पटरियों के किनारे से बटोरकर लाई गईं थीं, स्ट्रेचर पर, उसके सिरहाने। कुछ फट भी गई थीं। डायरियों में उसकी बहुत सारी कविताएँ थी, हिंदी और अँग्रेजी में, जिन्हें पढ़ते हुए उनकी साँसें रुँध जाती थीं। वे छिपकर रोती थीं।
तीन-चार दिनों के बाद आया वह लम्हा जिसे आना ही था। कब तक हम उसे स्थगित रखते या मुँह छिपाते? वह शाम का वक़्त था, खिड़कियों के पीछे अँधेरा गाढ़ा हो रहा था। हमने चाय पीकर प्याले रख दिए थे और बुतों की तरह ख़ामोश बैठे थे।
—पोस्ट मार्टेम? मुझसे यह अनायास कहा गया, बहुत धीमी आवाज़ में।
भाई और भाभी ने निगाहें उठाकर, हत-चकित होकर मुझे देखा। पहले लगा कि वे मेरी बात समझे नहीं।
—मेरा मतलब…मैंने कहा।
—ले गए थे। भाई ने कहा।—वहीं पटरियों से सीधे। बॉडी बहुत देर से, शाम तक मिली।
—ऑटोप्सी की रिपोर्ट?
—वह…पुलिस के रिकॉर्ड में होगी। भाई ने कहा।
मुझे पता था कि पोस्टमार्टेम हैंडबुक के चैप्टर 8, सेक्शन 501 (ऑटोप्सी प्रोटोकॉल) के तहत एक एप्लीकेशन देकर उस रिपोर्ट की कॉपी हासिल की जा सकती थी। लेकिन इससे क्या होगा? फ़ॉर्म फ़ोर-ए में किसी बीमारी का ज़िक्र होता था, इस रिपोर्ट में अंदरूनी चोटों और फ़्रैक्चर्स और रक्तस्राव का। असली वजह वहाँ भी नदारद होती थी, यहाँ भी। असली हत्यारा हमेशा अँधेरे में छुपा रहता था। यह सोचकर मैं ख़ामोश हो गया, निरर्थक महसूस करता हुआ। बाहर अब झींगुरों, कीड़ों के द्वारा कुतरी जाती घुप अँधेरी रात थी। हर पल इतना धीमे बीतता था जैसे वह वक़्त की एक बूँद या बिंदु नहीं, अपने आप में पूरा वक़्त हो। एक निस्सीम प्रकल्प।
—क्या बात रही होगी? मैंने शब्दों को गले में धकेलते हुए कहा।
— …
—मेरा मतलब, उस समय उसके मन में…
—यह कहना बहुत मुश्किल है। भाभी ने कहा। उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई गला घोंट रहा हो।
—उसने कुछ भी नहीं कहा? पिछली रात या…
—नहीं। न कोई पर्ची या चिट्ठी। भाई ने अपने आप से ही कहा।
—उसके मन में जो बात थी, अपने साथ ही ले गई। भाभी ने कहा।
—उसके फ्रेंड्स…?
—वो सब भी सदमे में हैं। उसके मोबाइल में जितने नंबर हैं, मैंने सबसे बात की।
—मोबाइल वह घर छोड़ गई थी? मैंने पूछा।
—हाँ। भाभी ने कहा।
हम तीनों बहुत देर तक ख़ामोश रहे।
—सबने यही कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे कोई संकेत मिलता। मैं बुरी से बुरी बात सुनने को तैयार थी। यह तक पूछा कि कोई पर्सनल बात…जो वह हमें बता न सकी हो। कोई अच्छा लगने लगा हो और उसने…इस उम्र में होता है न? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी दूर दूर तक। हर चीज़ में हिस्सा लेती थी, हँसती-बोलती थी।
—तो फिर…कुछ…
—न उसे डिप्रेशन या ऐसा कुछ था। पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, हर टेस्ट में अच्छे नंबर लाती थी। जो खाने का मन होता था, बनवाती थी। फ़ेसबुक पर हमेशा की तरह पिक्चर्स वग़ैरह पोस्ट करती थी, कविताएँ भी…
—फिर भी कोई बात तो थी जो उसे भीतर ही भीतर…।
जिसकी वजह से…
—ऐसा क्या रहा होगा? भाभी ने कहा।
—यह जान सकना बहुत मुश्किल है। भाई ने कहा।
बातों के एक गोल घेरे में घूमते हुए हम वहीं आ गए थे जहाँ शुरू में थे। हम ख़ामोश बैठे रहे, ख़ाली-सा महसूस करते हुए। उतनी पास से दोनों के थके, उद्विग्न चेहरे और बालों की सफ़ेदी देखते हुए महसूस हुआ कि उसके जाने के बाद जो गुज़रे थे वे केवल कुछ दिन नहीं थे। एक साथ अनेक साल गुज़र गए थे या एक पूरा ज़माना। मुझे यह सोचकर डर लगा कि मैं आइने में देखूँ तो वहाँ भी शायद मैं नहीं, कोई और नज़र आएगा।
—वह बहुत सोचती थी। भाभी कुछ याद करते हुए कहने लगीं।
—सोचते-सोचते थक जाती थी। कभी किसी झिरी से उसे कहीं गुम, ख़ामोश देखती थी तो डर लगता था। तब वह चौदह-पंद्रह साल की नहीं, बहुत बड़ी लगती थी, कहीं बहुत दूर। जैसे उसके नन्हें से सीने पर कितना बोझ था। मैंने एक बार उसका सिर सहलाते हुए कहा कि बेटा, यू आर अ स्माल चाइल्ड, वही रहो न। इतना सोचने की ज़रूरत क्या है? सोचने के लिए हम लोग हैं, तुम्हें बड़े होने की क्या जल्दी है? वह मुस्कराई मगर इस तरह जैसे दिलासा दे रही हो। जैसे उसे कुछ भयानक या दर्दनाक पता है मगर हम बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। जैसे वह मेरी बेटी नहीं थी, मदर थी।
—उसने मुझे फ़ोन किया था। मैंने अटकते हुए कहा।
—उसकी पिछली रात, तीन बजकर चालीस मिनट। मगर मैंने सुना ही नहीं। शायद डूबते हुए आख़िरी पलों में उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया था, मगर…
—उसके पिछली रात? भाभी ने कहा।
—हाँ। मैंने सर झुकाकर कहा।—पता नहीं वह क्या कहना चाहती थी।
बहुत देर तक एक स्तब्ध ख़ामोशी छाई रही।
—वह अपने इर्द-गिर्द कुछ देखती थी जो हमें नज़र नहीं आता था। भाभी ने बहुत देर के बाद कहा।—हम अंधे थे, नाक़ाबिल थे। हम नालायक माँ-बाप थे। वरना उसका देखा हुआ नहीं तो उसका ‘देखना’ तो देख सकते थे। वह कोई आम देखना नहीं था। वह बातें करते-करते चुप हो जाती थी, वह चुप्पी भी कोई आम चुप्पी नहीं थी। काश…
उनका गला रुँध गया, उन्होंने एक डूबती-सी आवाज़ में कहा—मैंने अपनी ही बच्ची को ध्यान से…कुछ और ध्यान से देखा होता। उसकी बातें सुनी होतीं। जैसे एक बार, पता नहीं किस सिलसिले में उसने कहा…पारिस्थितिकीय विनाश…मगर रुक गई।
—क्या कहा…पार…? मैंने कहा।
—‘ईकोलोजिकल डिस्ट्रक्शन’। और कृत्रिम चेतना यानी आर्टिफिशियल कांशसनेस और डिजिटल डिक्टेटरशिप…। उसकी किताबें…
—किताबों के बारे में क्या…? मैंने पूछा।
—उसकी किताबें पलटती रहती हूँ। कल ही देखा, उसकी सिविक्स…नागरिक शास्त्र की किताब में ‘संविधान’ चैप्टर में जहाँ-जहाँ ‘जस्टिस’ लिखा था, उसने काट दिया था और एक जगह ‘लोकतंत्र’ से पहले हाथ से लिखा था…‘अन्यायों का…’।
भाभी ने जो कहा, वह मैंने स्तब्ध भाव से सुना। भाई भी, जो चुपचाप सुन रहे थे, बेचैन हो गए, यहाँ तक कि पसीने से उनका माथा भीग गया। यह सब इतना हैरत भरा था, अनबूझ, अजीबोग़रीब…मेरी कल्पना से भी परे, कि मुझे कुछ डर सरीखा…। अब हमेशा के लिए इस सवाल से बिंधा रहूँगा, एक चाक़ू की तरह घोंपता हुआ सवाल—कि हमारी ‘नन्हीं मुन्नी गुड़िया’ ने अपने भीतर क्या छुपा रखा था। उसके ज़ेहन में कैसे ख़याल रगड़ खाते थे, ख़ून में कैसे उबाल उठते थे। वह इतनी बड़ी कब हुई और क्या जानती और सोचती थी और उस आख़िरी रात उसने क्या सोचा था, जिसके बाद…।
देवेन्द्र ने कहा : भला यह सब यक़ीन करने लायक था? मैंने भी न किया होता। लेकिन…कुछ याद आया और मेरा सर चकराने लगा। याद आया, अस्पताल में, दूसरे फ़्लोर पर, जच्चा-बच्चा वार्ड में, जहाँ मेरी ड्यूटी थी, ऐसा ही कुछ चलता था दिन-रात। बच्चे दबे स्वरों या इशारों में गंभीर चर्चाएँ करते थे, कभी-कभी बहसें भी। चुपके से दरवाज़ा खोलकर वार्ड में घुसता था तो कभी-कभी कुछ शब्द या वाक्य, बातचीत के टुकड़े कानों में पड़ते थे। एक बार मुझे ‘बेइंसाफ़ी’ या शायद ‘बेबसी’ सुनाई दिया था…लेकिन उसे भ्रम समझकर भुला दिया। वे बड़ों की मौजूदगी में चुप हो जाते थे। यकायक भान हुआ कि बच्चे…जितने भी बच्चे हैं, जहाँ भी…बड़े हो चुके हैं। वे बहुत चालाक हैं, बच्चा होने का नाटक करते हैं सिर्फ़। अब न कहीं कोई बच्चा है न बचपन। सिर्फ़ तुम्हारा दिल रखने, भुलावा देने के लिए वे ज़िद करते, मचलते नज़र आते हैं मगर मन ही मन तुम पर, तुम्हारी बातों पर हँसते हैं। वे सब कुछ जानते-सोचते और कल्पनाएँ करते हैं। तुम्हारी नज़रों और ख़यालों और तसव्वुर से भी परे उनकी अलग बस्ती है या बस्तियाँ या शहर, बहुत सारे शहर। शायद एक पूरा मुल्क।
कुछ दिन ऐसे ही बीते, हालाँकि उन दिनों में कुछ भी ‘बीतता’ नहीं था। सब अपनी जगह अटल था—दिनों का निचाट सूनापन, भाई की ख़ाली आँखें और भाभी का सबसे छुपकर ख़ामोशी से रोना। फिर एक दिन भाई ने कहा—वापस कब जाना है?
—कहाँ? मैंने कहा।
—इंटर्नशिप पूरी करने। अब काफ़ी दिन हो गए। कुछ भी हो, जीवन…
—मैं कहीं नहीं जाना चाहता।
—क्या मतलब?
—कोई दूसरा काम कर लूँगा। मुझे रेलवे में कोई नौकरी दिलवा दीजिये। कोई भी छोटी-मोटी।
—रेलवे में? जैसे मैं तो एक मामूली बुकिंग क्लर्क नहीं, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन हूँ, क्यों? उन्होंने कहा।—लेकिन इस तरह सोचने की वजह?
—ऐसी की तैसी में गई डॉक्टरी। नहीं बनना मुझे।
—लेकिन क्यों?
इसलिए कि…मैं कहना चाहता था—बच्चों ने यह नया शगल पकड़ लिया है, मरना। रोज़-रोज़ मरते जाते हैं, बिना कुछ कहे। उन्होंने ज़िद ठान ली है। डॉक्टर का यही काम रह गया है कि उनके जाने के बाद डेथ सर्टिफ़िकेट बनाता रहे, भरसक कोशिश करते हुए कि उसके हाथ न काँपें—और बाद में रातों में, सपनों में…। मगर अब, मीनल के जाने के बाद, मैं कंधे पर इतने सारे मृतक लेकर नहीं चल सकता। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन। मैं यह सिलसिला यहीं रोक देना चाहता हूँ।
लेकिन यह सब मैंने कहा नहीं, सिर्फ़ सोचा था। मन की एक बहक या लहर जो उठने के साथ ही कहीं गुम हो जाती है। वक़्त ऐसा है कि कोई भी ग़म हो, कैसा ही हादसा गुज़रे, ज़िन्दगी बस दो-चार दिन की मोहलत देती है और फिर उसके तकाजे चोंच मारने लगते हैं। मुझे छुट्टी लिए हफ़्ता-भर हो चुका था। अगले दिन फिर सुबह लोकल रेलगाड़ी, ईएमयू पकड़ने के लिए मैं जंक्शन के आख़िरी प्लेटफ़ॉर्म पर था। वही हत्यारी गाड़ी जिसने उस मनहूस दिन मीनल को…और शायद इंजन भी वही जिसने पहले ही धक्के में उसे एक किनारे फेंक दिया था। वही जाने पहचाने बर्फ जैसे ठंडे हत्थे थे और ठिठुरते हुए सहयात्री। उस दिन ट्रेन चलने से पहले ही मैं ऊपर वाली बर्थ पर जा लेटा और फिर लंबी सीटी से ‘गड़म गड़म’ और फिर ‘कट कट…कटाक…कटाक’ तक का सफ़र एक बेहोशी जैसी, तन्द्रा जैसी हालत में पूरा किया। ट्रेन के रुकने पर कोई मुझे हिलाकर न जगाता तो न जाने कब तक सोया रहता। डिब्बे के पिछले, अधखुले दरवाज़े से धीरे-धीरे एक-एक सीढ़ी पर पाँव रखते हुए झाड़ियों और कचरे के बीच उतरना जैसे किसी सपने से सच्चाई तक का सफ़र पूरा करना था। उसी समय याद आया कि वह सोमवार का दिन था।
कुछ देर के बाद मैं उसी अस्पताल के सामने था जो मृत्यु से बना था। बड़े गटे के अन्दर छोटे गेट को खिसकाकर भीतर आया और सुबह की धूप में लॉन के किनारे, सड़क पर चलता हुआ रिसेप्शन पर पहुँचा जहाँ बड़ी-बड़ी आँखों वाली एक मौत…ऊबी हुई मौत अकेली बैठी थी, एक डिज़ाइनदार मास्क लगाए। मास्क के पीछे से ही उसने एक किटकिटाती-सी आवाज़ में ‘गुड मॉर्निंग’ कहा लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज़ कर मौत के गलियारे से गुज़रता हुआ सीधे दूसरी मंज़िल पर चला आया। मुझे जल्दी थी क्योंकि नर्स से हफ़्ते-भर की मौतों का हिसाब लेना था और डायरेक्टर के आने से पहले उनके सर्टिफ़िकेट्स बना लेने थे। वहाँ पहुँचकर हर सोमवार की तरह पहले बाथरूम गया जहाँ आईने में देखने पर एक कमज़ोर, बहुत पीला चेहरा नज़र आया। वही थकान और हलकी हरारत महसूस हुई, बुख़ार की शुरुआत। धीरे-धीरे चलता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा और दराज़ की तलाशी ली, शायद भूले-भटके क्रोसिन या कोई और गोली नज़र आए। मुझे यह देखकर हैरानी हुई, तसल्ली भी, कि छुट्टी के दौरान मेरी जगह जिस दूसरे इंटर्न को लगाया गया होगा, उसने अपने फ़र्ज़ में कोताही नहीं की थी। मेरी दराज़ में करीने से सारे सर्टिफ़िकेट्स मौजूद थे, मरने वालों का इलाज़ कर रहे डॉक्टरों के दस्तख़त समेत। सारे कॉलम सफ़ाई से भरे हुए थे…नाम, उम्र, माता-पिता, मरने का कारण। सिर्फ़ आख़िरी काम, डायरेक्टर की घुग्घी बिठवाना, वह मेरे ज़िम्मे था और उसके बाद मोहर लगाना। मैंने उन्हें गिना। उनकी संख्या, बता चुका हूँ कि हर हफ़्ते बढ़ जाती थी। उस बार भी वे पिछले हफ़्ते से चार ज़्यादा थे, कुल अठारह। हर बार की तरह उनके बबलू, बॉबी, बेबी जैसे नाम थे और उम्रें दो से दस के बीच। ‘मरने का कारण’ के नीचे वही मनगढ़ंत बातें लिखी थीं—मीज़ल्स, मम्प्स, ये, वो। वे हर बार की तरह बिना कुछ कहे, एक अनबूझ ख़ामोशी का निप्पल चूसते हुए चले गए थे। अपने दिल की बातें और अपनी बस्तियाँ और शहर, उनके पुल और सड़कें और नक़्शे वे अपने साथ ले गए थे, मीनल की तरह। उनमें से कुछ ने आसान वाक्य लिखना, ‘म…म…’ बोलना शुरू ही किया होगा और कुछ ने वह भी नहीं। उन्होंने इतनी जल्दी यह कौन-सी ज़ुबान सीख ली थी, ज़िन्दगी और मौत के हर्फों में लिखी, जिसमें वे कोई बात, एक ही बात बार-बार दोहराते थे, मगर न कोई सुनता था, न समझ सकता था?
अस्पताल में वह रोज़ जैसा ही व्यस्त दिन था। वक़्त तेज़ी से बीत रहा था मगर एक लड़खड़ाती चाल में। धीरे-धीरे बढ़ते बुख़ार में दूसरी मंज़िल से देखता रहा एक के पीछे एक एम्बुलेंसों, ऑटो रिक्शों, ई-रिक्शों, टेम्पों, स्ट्रेचरों, यहाँ तक कि साइकिलों, हाथगाड़ियों में भी, मरीज़ों का आते रहना, पीछे के गेट से लाशें निकलना। मास्क पहने लोग बदहवास इधर से उधर भागते हुए। झगड़े, चिल्लाहटें, बीच-बीच में रोने की आवाज़ें। सब कुछ पर एक पीलेपन की झिल्ली, जो शायद बुख़ार का असर रहा होगा। हर चीज़ पर एक अनिष्ट का, बदनसीबी का साया था, सब कुछ अशुभ, अशोभन था, बुनियादी रूप से ग़लत और बेहद भयास्पद। ऐसा लगा जैसे दुनिया की बुनियाद हिल गई है और सब कुछ फिर से अपने तत्वों में बिखर जाने वाला है। इन सबके बीच मुझे उस लम्हे का, हर सोमवार को आनेवाले ख़ास लम्हे का ख़याल बना हुआ था। वह क़रीब आते-आते आ ही गया आख़िरकार, आँखों के ठीक सामने। उस समय दोपहर के तक़रीबन तीन बजे थे जब मैंने दराज से वे सर्टिफ़िकेट्स निकाले और उठ खड़ा हुआ। बुख़ार काफ़ी रहा होगा क्योंकि पल-भर के लिए आँखों के सामने अँधेरा घिर आया।
डायरेक्टर का कमरा चौथे फ़्लोर पर था। हर बार मैं सीढ़ियों से जाता था लेकिन उस दिन लिफ़्ट ली, बुख़ार के कारण। लिफ़्ट में एहतियातन फ़ॉर्म्स को एक बार गिन लिया। डायरेक्टर के कमरे के बाहर एक सिक्योरिटी वाला कुर्सी पर बैठा था। मुझे देखकर वह मास्क समेत मुस्तैदी से खड़ा हो गया, सिर झुकाए।
—यस? आँखों का भूतपूर्व सर्जन मोटे चश्मे के पीछे से घूर रहा था।
—डॉ. देवेन्द्र, डूइंग इंटर्नशिप। मैंने कहा। वह हमेशा भूल जाता था।
—व्हाट डू यू वांट?
—दीज़ फ़ॉर्म्स, सर। मैंने जल्दी से कहा।—फोर-ए।
—प्लीज सिट डाउन। उसने कहा। वह उस समय किसी और फ़ाइल में कुछ पढ़ रहा था। मैं खचाखच भरी मेज़ पर उसके सामने बैठा था, उसके हाथों…सिर्फ़ हाथों पर एकटक निगाह टिकाए। इन्हीं हाथों से वह कभी आँखों के बहुत महीन, नाज़ुक ऑपरेशन करता होगा लेकिन वे अब सूखे और सख़्त थे, बेजान। पहली बार मेरा ध्यान इस बात पर गया कि उसकी उँगलियाँ बदसूरत, मोटी, सूजी हुई थीं और हर एक पर कोई न कोई नगीना जड़ा था, दो हीरे और शायद मोती, नीलम, पुखराज।
मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। वे कुल अठारह काग़ज़ थे, उस समय तक सबसे ज़्यादा। हर बार की तरह मुझे वही बात कुचल रही थी कि क्या यह भी उसके लिए सिर्फ़ एक संख्या होगी, एक आँकड़ा…रत्नजड़ित उँगलियों से एक दफ़्तरी, मशीनी घुग्घी की हक़दार? यह मैं जानता था कि वह विचलित या परेशान होने के परे था, फिर भी…मैंने अपने आप से कहा—फिर भी एक ही हफ़्ते में अठारह और एक, उन्नीस बच्चों की मौत पर शायद वह…। अठारह के ऊपर एक वह जो मरने के बाद भी मेरे कानों में कहे जाती थी…चाचा, मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम मृत बच्चों का अपमान नहीं कर सकते डायरेक्टर, वह भी बार-बार, मैंने अपने मन में कहा। मैं क्या चाहता था? कुछ नहीं, सिर्फ़ उसके माथे पर या आँखों में एक शिकन, सिकुड़न देखना चाहता था, उसके दस्तख़त करते हाथों में ज़रा-सी सिहरन, चाहे पल भर की। उसके दिल की तली में कहीं बची थोड़ी-सी नमी का सबूत। उसके रंग-बिरंगे रत्नों और पथरीले हाथों को देखते हुए मेरे भीतर लगातार कुछ दुहरा रहा था, एक सिहरन, कँपकँपी, ज़रा-सी जुम्बिश। ‘इंसानी’ जुम्बिश, मशीनी हरकत नहीं। मैंने देखा कि उसने बेध्यानी में हाथ बढ़ाकर वे काग़ज़ उठाए, उन्हें देखकर बुदबुदाया…बच्चों के पास मरने के अलावा कोई काम है? और इसके बाद कुछ अस्फुट गाली सरीखा। उस घड़ी, एकाएक…
बताना मुश्किल है कि क्या हुआ। जैसे भीतर कोई चाक़ू खुला था, खटाक। कुछ पलों के बाद, जिनकी स्मृति मुझे साफ़ नहीं, वही सिक्यूरिटी वाला मेरी गर्दन दबोचे मुझे दरवाज़े की तरफ़ धकेल रहा था और मैं इतने दिनों के दबे रोने के, हिचकियों के बीच चिल्ला रहा था…इतने बच्चे मार दिए, और कितने मारेगा हरामी? मैंने उसे हत्यारा भी कहा, मर्डरर। मेरी आवाज़ दूर तक गई होगी।
इसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं फालतू डिटेल्स छोड़ दूँगा। डायरेक्टर मुझे अस्पताल से बाहर निकालने पर आमादा था लेकिन डॉ. मेहँदीरत्ता, वही…वे मेरे काम आए। वही उसके कमरे में उसके पास बैठकर देर तक समझाते रहे…सर जी, पहले शांत करो अपने को, लो पानी पियो। यह लड़का…नातजुर्बेकार है, बेवकूफ़ है। लेकिन उसकी इंटर्नशिप पूरी होने वाली है। उसके कैरियर का सवाल है सर जी। “मैं ते जी, एहनू समझा समझा के मर गया कि यार तू बेकार पंगे न लित्ता कर”। लेकिन उसके घर में अभी एक ट्रेजेडी हुई है, इस वजह से…। “छड्डो जी, तुसी बड़प्पन दिखाओ ते एह गल्ल ते मिट्टी पाओ”। डायरेक्टर मुश्किल से इस शर्त पर राज़ी हुआ कि मैं उसे भूलकर भी अपना चेहरा न दिखाऊँ, साथ ही बाक़ी दिनों के लिए उसने मेरी नाइट ड्यूटी लगा दी। मेरा बकाया पेमेंट रोक लिया वह अलग।
मैं देवेन्द्र की बातें चुपचाप सुन रहा था। अब पार्क ख़ाली था।
—लेकिन वह बात अभी तक नहीं आई जो…। मैंने कहा —वही बतानी है अब…आख़िरी बात। उसने कहा।
—वह उसी रात की बात है।
—तुम्हारा मतलब है…?
—हाँ, अगस्त की आठ तारीख़। जब एक ही रात में चवालीस बच्चे…। ज़मीन से आसमान तक यही ख़बर छाई हुई थी।
—हाँ, हर चैनल, हर अख़बार में…मैंने कहा।—उसे कोई कैसे भूल सकता है?
—तमाम रातों के बीच वह कुछ अधिक काली, अँधेरी रात थी। उस रात लगता है सब बच्चों ने मिलकर ठान लिया था कि…। कुल चवालीस थे वे, चालीस के ऊपर चार—और उस्ताद खिलाड़ियों की तरह सबको सफ़ाई से छकाते रहे, थका-थका कर चूर कर दिया। सारी रात उन्होंने आँख-मिचौली खेली और जितने भी बड़े लोग थे, बदहवास और दिग्भ्रमित दौड़ते-भागते रहे, यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे, एक से दूसरे फ़्लोर। जैसे सफ़ेद लबादों में प्रेतात्माएँ नाच रही हों। उनकी हालत देखकर बच्चे, चार दिनों से लेकर दस साल तक के, चुपके-चुपके तकियों में मुँह छिपाए हँसते रहे हों तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। पता नहीं उन्होंने कब आपस में तय कर लिया था कि…। जो भी हो, उस रात उन्होंने सारे हिसाब चुकता कर लिये।
—कैसे हिसाब? मैंने कहा।
—दोस्तों की बेक़द्री के…उसने कहा। मौतों की बेक़द्री कहो या ज़िन्दगी की, एक ही बात है।
—…
—सारी रात तेज़ हवाएँ अस्पताल की खिड़कियाँ पीटती रहीं, उनकी डरावनी खड़-खड़, भागते बूटों की ख़ट-ख़ट और तेज़ रफ़्तार में आती-जाती गाड़ियों का मिला-जुला शोर दूर तक सुनाई देता रहा। रात आठ बजे से शुरू हुआ सिलसिला और उसके बाद वे एक के बाद एक जाने लगे, सिर्फ़ सेकंड फ़्लोर पर नहीं, सारे अस्पताल में। सारे डॉक्टरों और नर्सों और स्टाफ़ को बुला लिया गया था। आधी रात को डायरेक्टर भी दौड़ता आया, बदहवास। जब एक-एक अंक बढ़ती गिनती चवालीस पर जाकर रुकी, सुबह हो चुकी थी। उस समय सबकी हालत यह थी, डायरेक्टर, डॉक्टरों और नर्सों के साथ सिक्यूरिटी वालों, लिफ़्टमैन, ड्राइवरों और चपरासियों समेत—जैसे छूने भर से वे ढेर बनकर गिर पड़ेंगे। वे डायरेक्टर के कमरे में और बाहर वेटिंग एरिया में ख़ाली, थकी, डरी हुई आँखों से एक-दूसरे को ताकते बैठे रहे। डायरेक्टर ने मेज़ पर सर रखकर आँखें मूँद लीं। वे अस्त-व्यस्त थे, चेहरों पर स्याही पुती थी। आसपास के कुत्ते हवाओं में न जाने क्या सूँघते एक-एक कर अहाते में आ खड़े हुए। थोड़ी देर मरघट जैसी ख़ामोशी छाई रही। कुछ ही देर में सारी दुनिया एक आँधी की तरह टूट पड़ने वाली थी, उन्हें सैकड़ों सवालों के जवाब देने थे।
—उस रात…तुम…? मैंने कहा।
—मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं तो सिर्फ़ एक इंटर्न था यार, मेरे ज़िम्मे जो काम आया वह था जाने वाले बच्चों के नाम पतों वग़ैरह की लिस्ट बनाना। सारे रिकार्ड दुरुस्त रहने चाहिए न। डायरेक्टर ने मुझे अपने सामने आने से मना किया था मगर उस रात मजबूरी थी। सुबह की शुरुआती रोशनी में वह अपने कमरे में खिड़की के नीचे एक बुत की तरह बैठा था, इंसान का नहीं, किसी प्रेत का बुत—जब मैंने ख़ामोशी से वह लिस्ट उसके सामने रखी। उसकी किसी ख़ामोश बाँबी जैसी, मिट्टी के ढूह जैसी प्रेत-काया में बहुत देर के बाद हरकत हुई, वह लिस्ट उठाकर साफ़ देखने के लिए धीरे-धीरे आँखों के, मोटे चश्मे के पास लाया। मेरी निगाह फिर उसके हाथों और उँगलियों पर चली गई। उसके हाथों की कँपकँपी में हीरे, मोती, नीलम और पुखराज ख़ौफ़ में हिलते-डुलते…नाचते नज़र आए, इतने अरसे में पहली बार। उसी समय दूर पटरियों पर सुबह की लोकल रेलगाड़ी का वही डरावना ‘रेलवे म्यूज़िक’ सुनाई दिया …कट कट … कटाक…कटाक…कटाक।
काफ़ी देर हो चुकी थी। झुटपुटा घिरने से याद आया कि मुझे घर लौटना है। हम सुनसान पार्क से बाहर आकर उसके घर की ओर चलने लगे। मैं दोपहर में उनसे मिलने आया था। घर में भाभी की सूनी आँखें थीं, एक जमी हुई ख़ामोशी थी। देवेन्द्र उनके सामने सब कुछ दोहराने से बचना चाहता होगा इसलिए कुछ देर के बाद मुझे घर के पास उस पार्क में ले आया। मेरी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी थी। फ़ुटपाथ पर गड़हों में अभी तक बरसात का पानी जमा था, क़रीब से गुज़रती रेलगाड़ियों के कम्पन से बेचैन, बीच-बीच में काँपता हुआ। सर्दी भी बढ़ गई थी।
—एम. डी. पीडियाट्रिक्स में ही क्यों? मैंने रास्ते में चलते हुए पूछा।
—बच्चों को बचाना है न। उसने कहा। —जितने मुमकिन हों। वे मरते जा रहे हैं, इतनी तादाद में। …लेकिन…लेकिन इसके साथ…यह सुराग पाने के लिए भी कि वे अपने नन्हें दिलों में क्या-क्या छिपाए रहते हैं। यह मरने का शगल उन्होंने कहाँ से पकड़ लिया…इसका मतलब…। शायद कभी कोई अंदाज़ मिले कि हमारी मीनल के मन में…उस आख़िरी रात को…
हम चुप्पी के बीच चलते रहे। मैं बहुत देर से ख़ामोश सुन रहा था, एक भी शब्द कहे बिना, अपने भीतर वे सारी बातें स्थगित करते हुए जो मुझे डॉ. जिवागो से कहनी थीं। बोरिस पास्तरनाक के कथानायक की तरह वे यानी डॉ. जिवागो की बिरादरी के लोग बेहद संवेदनशील, पारे की तरह विचलित होते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ़ एक बात है। असली बात यह है कि, गोकि वे इसी दुनिया के होते हैं, उनके दिमाग़ में दुनिया का नक़्शा अलग होता है। वे बाहरी, ऊपरी चीज़ों में नहीं उलझते, सीधे सार-तत्व तक जा पहुँचते हैं। ऊपर से ठंडे दिखते हैं लेकिन जोश और आग से भरे होते हैं और उनकी आत्माएँ…तमाम नदों-नदियों को पीकर भी अतृप्त, उत्तेजित समुद्रों जैसी उनकी आत्माएँ…बोरिस के ही दोस्त मयाकोवस्की के शब्दों में कहूँ तो…अपनी लहरों के पंजों पर सवार होकर ऊँचे, ऊँचे, और ऊँचे उठती हुई जैसे चाँद को चूम आना चाहती हैं। लेकिन हर चीज़ में संगति और मायने और आपसी संबंध देखने, नतीजे निकालने की जल्दीबाजी में वे ऐसा भी कुछ देख या सुन सकते हैं जिनका वजूद नहीं होता। जो सिर्फ़ उनके बेचैन मन की छाया होती हैं। जैसे…उसकी यह बात कि अब न कहीं कोई बच्चा है न बचपन। बच्चे बड़े हो चुके हैं और सब कुछ जानते-सोचते हैं, लेकिन इतने चालाक हैं कि बड़ों से यह सब छिपाए रखते हैं। या यह कि बच्चों का इस तरह मरना…यह उनकी कोई अबूझ जुबान है…मृत्यु-जुबान—न जाने क्या कहने की कोशिश जो किसी और तरीक़े से नहीं कही जा सकती। या यही कि उस साल आठ अगस्त की रात को बच्चों ने मिलकर किसी बेक़द्री का बदला लिया था या कोई हिसाब चुकाया था। असल में तो यह एक मामूली, बेशक अफ़सोसजनक, बात थी जो अख़बारों में आ चुकी है, कि उस रात बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मारे गए थे। दिन में ऑक्सीजन सिलिंडर रिप्लेस किए जाने थे मगर सिलिंडर्स लेकर ट्रक पहुँचा ही नहीं। डायरेक्टर ने किसी बात पर, जैसे देवेन्द्र का बकाया रोका था, वैसे ही ‘ऑक्सी-एयर’ वालों का पेमेंट रोक लिया था और उन्होंने…।
लेकिन ये बातें मैंने उस शाम देवेन्द्र से नहीं कहीं। उसे अगले दिन के सफ़र की तैयारी करनी थी और मुझे भी घर लौटना था। मैंने सोचा कि एक-दो महीने के बाद जब यहाँ उसका पहला चक्कर लगेगा, तब कहूँगा। उस रात विदा लेते हुए मैंने उसे सिर्फ़ आगे की पढ़ाई के लिए शुभकामनाएँ दीं और कहा—‘फिर मिलेंगे दोस्त, बाय’।
[काफ़ी देर के बाद पसौंडा या खोड़ा इलाक़े के आवारा बच्चे जिन्हें चौकीदार ने भगा दिया था, पार्क की टूटी दीवार के रास्ते फिर भीतर चले आए। शाम के धुँधलके में केवल उनकी छायाएँ दिखाई देती थीं। वे आठ या दस रहे होंगे और उनकी उम्रें चार-पाँच से दस या बारह साल तक। उनके कपड़े फटे पुराने थे और उनमें से दो ने कंधों पर बड़े-बड़े थैले उठा रखे थे। गीली नम ज़मीन उनके पैरों तले धँसी जाती थी। वे क्यारियों के बीच कच्ची ईंटों के रास्ते पर चलते हुए उसी बेंच पर पहुँचे जहाँ कुछ देर पहले देवेन्द्र और उसका दोस्त बैठे थे। कुछ बेंच पर बैठ गए और बाक़ी क़रीब ही सूखी घास पर।
—यहाँ कुछ ठीक है। बाक़ी तो हर जगह गीला है। किसी ने कहा।
—रात बरसात भी तो इतनी हुई। दूसरी आवाज़ आई।
वे कुछ देर ख़ामोश बैठे रहे, इधर-उधर देखकर तसल्ली करते हुए कि चौकीदार या कोई और आसपास नहीं है।
बच्चों में जो सबसे बड़ा था, मुश्किल से दस साल का, उसने ज़मीन पर बैठे दो छोटे बच्चों को कान पकड़ कर खड़ा किया। वे केवल जाँघियों में थे।
—क्यों बे, दीवार पर धार से क्या लिख रहा था? बड़े बच्चे ने एक से कहा।
—कुछ भी नहीं। नंगे बदमाश ने अपने कान सहलाते हुए जवाब दिया।
—सब देख रहा था मैं।—बड़े लड़के ने कुछ ग़ुस्से से कहा।—‘नए सिरे से’ … यही न? और ऐसा ही कुछ लिखकर जवाब दे रहा था तेरा ये दोस्त। गनीमत है किसी ने देखा नहीं। पुराने ज़माने के बच्चों जैसी हरकतें…तुम्हें यह सब करने से मना किया था न?
—सॉरी, ग़लती हो गई। अब नहीं करेंगे। दूसरे लड़के ने कहा।
—हमें अपनी बातें बड़ों से छुपानी पड़ती हैं न। वे इसी दुनिया में बड़े हुए हैं, इसी के आदी हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। बातें ही नहीं, अपना ग़ुस्सा भी, सब कुछ। उस समय तक जब यह दुनिया फिर से बनाई जाएगी। बड़े लड़के ने कहा।—लेकिन उसके पहले हमें धीरज से, ध्यान से हर चीज़, सब कुछ समझना होगा साफ़-साफ़।
—जाने दो यार। बेंच पर बैठे दूसरे लड़के ने मुलायम आवाज़ में कहा।—ये ग्रुप में नए शामिल हुए हैं न। ये रूल्स नहीं जानते।
—तो सारी बातें फिर से ठूँसो इनके दिमाग़ में अच्छी तरह। इन्हें पता होना चाहिए कि वो बच्चे जो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, घरों में रहते हैं, हमारा काम उनसे कहीं मुश्किल है। वे लोग सह नहीं पाते…सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे। बहरहाल, हम लोगों के लिए क्या कोई स्कूल है या किताबें या इन्टरनेट? कचरा बीनने वाले हैं हम। लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करके कूड़े में फेंक देते हैं, उनको बीनकर, बेचकर हमारी रोटी चलती है। इसी तरह वे जो शब्द इस्तेमाल करके कूड़े में फेंक देते हैं, फटे पुराने काग़ज़, लिफ़ाफ़े, पुड़ियाएँ, अख़बारों के टुकड़े—उन्हें बीनकर हम ज्ञान हासिल करते हैं। उसे आपस में बाँट लेते हैं। शब्द ही नहीं, कभी-कभी पूरे वाक्य भी। देर से ही सही, हम भी सब कुछ जान और समझ लेते हैं।
—आज हमें किस चीज़ के बारे में जानना है? दूसरे ने कहा।
—आज का सब्जेक्ट था…‘डिटेंशन सेंटर’। उनके बारे में ढूँढ़ने और पढ़कर आने की, बताने की ज़िम्मेदारी किसकी थी ?
झुंड में सबसे पीछे ज़मीन पर बैठा एक सात-आठ साल का लड़का खड़ा हुआ और धीमी आवाज़ में, जो बहुत दूर न जाए, ग्रुप को संबोधित करते हुए कहने लगा—ये ‘डिटेंशन सेंटर’ जो हैं…ये नई चीज़ नहीं, न पहली बार…]
[आलोचना सहस्त्राब्दी अंक-66 में प्रकाशित]