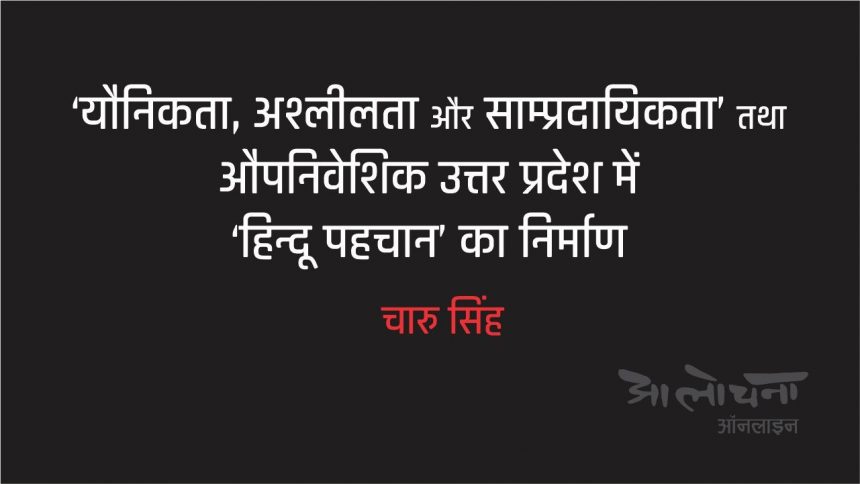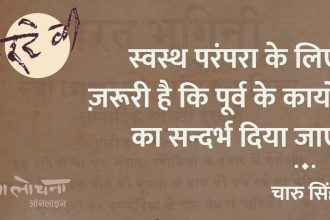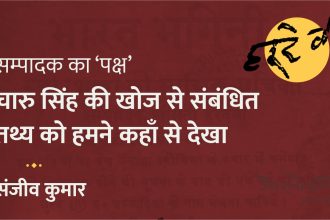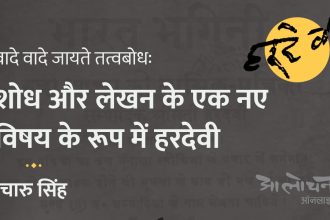“दरअसल ‘स्वच्छ’ और ‘अश्लील’ के आधार पर साहित्य का विभाजन पूरी तरह से एक निरर्थक कोशिश है। इसका हिन्दुस्तान की साहित्यिक परम्पराओं से कोई लेना-देना नहीं था। खोजने से भी यहाँ गुरुकुल की ब्रह्मचर्य पुस्तिकाओं के अलावा ऐसी रचना नहीं मिलेगी जिसमें शृंगारिक प्रसंगों या दैहिक सौन्दर्य का उल्लेख ‘अश्लील’ या वर्जित समझा जाता रहा हो। यहाँ तक कि कोकशास्त्र, जिसे लेखिका बाज़ार की माँग से पैदा हुई कोई नई रचना समझ रही हैं वह भी कई शताब्दियों से भारतीय पाठकों के बीच स्वीकृत रहा है। इसी तरह लोक-शैलियों में वर्णित कामुक उद्गारों को रीतिकाल की कविता की नक़ल समझ लेना, उपनिवेश-पूर्व लोकमानस में यौन-विषयों की सहज स्वीकृति की उपेक्षा करना होगा। साथ ही भारत-भारती जैसी कुछ गिनी-चुनी रचनाओं को ‘उच्च’ साहित्य का पैमाना मान लेना, किसी प्रामाणिक निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है।”
चारु गुप्ता की किताब स्त्रीत्व से हिन्दुत्व तक : औपनिवेशिक भारत में यौनिकता और साम्प्रदायिकता, उन इतिहास पुस्तकों में से है, जिसमें औपनिवेशिक भारत के इतिहास लेखन के केन्द्र में हिन्दी भाषी समाज को रखने की कोशिश की गई है। मूल रूप से अँग्रेज़ी में लिखी गई इस किताब को, लेखिका ने कुछ सम्पादन के साथ हिन्दी में उतारा है। इस किताब के ज़रिये चारु गुप्ता ने ‘हिन्दी में—या किसी भी देशी भाषा में—इतिहास लेखन कैसे किया जाए?’—इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। इस दृष्टि से भी यह किताब हिन्दी के पाठकों के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाती है, जिस पर देर से ही सही चर्चा करना बेहद ज़रूरी है।
यह किताब यद्यपि हिन्दी के पाठकों के लिए नई नहीं है, लेकिन बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिवेश में एक बार फिर से पढ़े जाने की माँग करती है। हिन्दी के अभिलेखीय स्रोतों, साहित्यिक पुस्तकों, लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पत्र-पत्रिकाओं तथा बड़े पैमाने पर हिन्दी भाषा में छप रही प्रचार पुस्तकों को आधार बनाते हुए लेखिका ने औपनिवेशिक उत्तर प्रदेश में हिन्दू ‘पितृसत्ता के पुनर्गठन’ तथा ‘एकरूपी हिन्दू पहचान’ के निर्माण पर प्रकाश डाला है। वे लिखती हैं, “इस किताब के अध्याय तथाकथित दो अलग मुद्दों—उत्तर भारत के औपनिवेशिक दौर में पितृसत्ता के पुनर्गठन और उसी दौर में हिन्दू संगठनों, विचारकों और उनकी विचारधारा के आक्रामक रूपों के उदय—को एक साथ लाती है। अध्याय यह भी दर्शाते हैं कि किस प्रकार यौनिकता, अश्लीलता और लैंगिकता के सवाल हिन्दू सांस्कृतिक और राजनैतिक पहचान के बलपूर्वक आग्रह के साथ जुड़े थे।”2
हिन्दी में अमूमन जिस कालखंड को ‘हिन्दी नवजागरण’ कहा जाता है, उस वक़्त ‘हिन्दू प्रचारकों (Hindu publicists) की उग्र साम्प्रदायिक गतिविधियाँ संयुक्त प्रान्त में क्या शक्ल ले रही थीं, यही इस किताब की विषयवस्तु है। ‘हिन्दू प्रचारक’ इस किताब के केन्द्रीय चरित्र हैं और उन्हीं के लेखन को इस किताब का आधार बनाया गया है।3 ‘हिन्दू प्रचारक’ कोई सीमित या अलग-थलग जमात नहीं थे, “वे कोई एकरंगी जमात या आवाज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे” बल्कि बहुत से अलग-अलग वर्गों से आते थे और “एक दूसरे के साथ अस्पष्ट सम्बन्धों में बँधे हुए थे। वे मुख्य रूप से मध्यवर्गीय थे, लेकिन वहाँ तक सीमित नहीं थे।” लेखिका ने ‘हिन्दू प्रचारकों’ की इस जमात में हिन्दी लेखकों से लेकर हिन्दू महासभा, आर्यसमाज या कांग्रेस-सदस्य जैसे परस्पर भिन्न और विरोधी समूहों को शामिल माना है।4 जिन्होंने “अपने ऊपर बहुसंख्यक हिन्दू जनता के सामान्य हितों को मुखरित करने की ज़िम्मेदारी ओढ़ रखी थी।” वे लिखती हैं, “इस किताब में हिन्दू प्रचारकों की आवाज़ केन्द्र-बिन्दु है…इन लेखों में मैंने हिन्दू प्रचारक/प्रचारवादी शब्दावली का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जिन्होंने सचेतन/अचेतन रूप से सार्वजनिक और जन मीडिया का उपयोग करके एक ख़ास तरह के ‘हिन्दू नज़रिए’ का प्रचार-प्रसार किया।…इनमें से कई आर्यसमाज से प्रभावित या उसके सदस्य थे। वे उपदेशक और प्रचारक थे। वे भिन्न-भिन्न प्रकार के सुधारवादियों और पुनरुत्थानवादियों-सनातनधर्मी, हिन्दू महासभा कार्यकर्ता, हिन्दी लेखक, कांग्रेस सदस्य, जाति सभाओं के प्रवक्ता—की जमात से आते थे। कई दूसरी पंगत के सुधारवादी और अनगढ़ लेखक थे, और एक दूसरे के साथ अस्पष्ट सम्बन्धों से बँधे हुए थे।”5
यही इस किताब का प्रस्थान बिन्दु है जहाँ ‘हिन्दी लेखकों’ तथा ‘हिन्दू प्रचारकों’ की घुली-मिली या अतिव्यापी पहचान को प्रस्थान-बिन्दु बनाते हुए बीसवीं सदी पूर्वार्द्ध के हिन्दी-लेखन के ज़रिये की जा रही हिन्दूवादी राजनीति की पड़ताल की गई है। ‘औपनिवेशिक भारत में यौनिकता, अश्लीलता और साम्प्रदायिकता’ पर केन्द्रित इस किताब की प्रमुख स्थापनाएँ यह हैं—
किताब के पहले हिस्से में हिन्दू पितृसत्ता के उभार को दर्शाया गया है। लेखिका मानती हैं कि स्त्री यौनिकता पर नियंत्रण के लिए ‘हिन्दू प्रचारकों’ ने जिनमें हिन्दी के साहित्यिक लेखक भी शुमार थे, ‘अभिजात्य’ या ‘उच्च’ साहित्यिक लेखन के ज़रिये शृंगारिक विषयों का निषेध और ब्रह्मचर्य का महिमामंडन करना शुरू किया। जिससे हिन्दी के साहित्यिक जगत में ‘अश्लीलता’ को लेकर एक विवाद ने जन्म लिया। जहाँ एक ओर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, रामचन्द्र शुक्ल तथा महावीर ‘प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखक शृंगारिक विषयों तथा यौन-प्रसंगों को हिन्दी साहित्य से सर्वथा बाहर रखना चाहते थे। वहीं हिन्दी के पाठकों की पढ़ने की आदतें बाज़ार में कामुक साहित्य की माँग को प्रस्तुत करती थीं जिससे मुनाफ़े की चाह में कामुक तथा ‘अर्ध-पोर्नोग्राफ़िक’ किताबें छपती और बिकती रहीं। इसी समय स्त्रियों के घरेलू दायरे में भी हस्तक्षेप किया गया और न सिर्फ़ ‘अश्लील महिला गीतों’ और होली जैसे त्योहारों में महिलाओं की बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी पर लगाम कसी गई; बल्कि एक क़दम आगे बढ़कर हिन्दूवादी प्रचारकों ने स्त्री-शिक्षा का एक नया मॉडल भी प्रस्तुत किया। स्त्री-शिक्षा का यह नया मॉडल स्त्रियों को आदर्श पत्नी और माँ की भूमिकाओं में प्रशिक्षित करना तथा स्त्रियों की यौन-आकांक्षाओं तथा अभिव्यक्तियों को भी नियंत्रित करना चाह रहा था। हिन्दी के लेखकों ने घर के भीतर और बाहर स्त्री के रहन-सहन पहनावे तथा सम्बन्धियों से बात-व्यवहार आदि ‘दैनंदिन जीवन’ के हर कोने में दख़लन्दाजी शुरू कर दी। इस तरह एक नियंत्रित स्त्री-यौनिकता के आधार पर ‘एकरूपी हिन्दू पहचान’ के निर्माण की कोशिशें शुरू हुईं। लेखिका का मानना है कि हिन्दू महिलाओं की अनियंत्रित यौनिकता तथा उस पर मँडराने वाला ‘मुस्लिम पुरुष’ का ख़तरा जातिगत मतभेदों को भुलाकर हिन्दू पुरुषों को एकजुट करने में सफल रहा। जिसे शुद्धि तथा संगठन आन्दोलन तथा अपहरण सम्बन्धी दंगों में ‘निम्न जातीय’ पुरुषों की बतौर हिन्दू भागीदारी से समझा जा सकता है।
किताब का दूसरा हिस्सा मुस्लिम पुरुषों को ‘अन्य’ या पराया बना देने की हिन्दूवादी प्रक्रिया पर केन्द्रित है। किताब के इस हिस्से में दिखाया गया है कि किस तरह मुस्लिम पुरुषों के हाथों एक हिन्दू महिला के तथाकथित बलात्कार या अपहरण की ख़बरें उड़ाकर ‘हिन्दू प्रचारक’ मुसलमानों को कामुक, व्यभिचारी और बलात्कारी के रूप में स्टीरियोटाइप करने की कोशिशें किया करते थे। इसी तरह हिन्दी के कई बड़े साहित्यकारों ने साहित्य या इतिहास पुस्तकें लिखकर मुसलमानों को कामुक या बलात्कारी के रूप में चित्रित करने की एक परम्परा शुरू की। इसके लिए ग़ाज़ी मियाँ जैसे लोकप्रिय मुसलमान संतों को भी निशाना बनाया गया तथा इन संतों को हिन्दू महिलाओं के बलात्कारी के रूप में चित्रित करते हुए हिन्दू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच वैमनस्य पर आधारित एक विभाजक रेखा खींचने की कोशिश की गई। हिन्दू महिलाओं के लिए ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए गए जिनमें मुस्लिम पुरुषों से रोज़मर्रा के जीवन में किसी भी तरह का व्यवहार रखने की मनाही थी। महिलाओं को अब मुसलमान दुकानदारों से सामान नहीं ख़रीदना था, न ही मुस्लिम चूड़ीहारों से चूड़ियाँ पहननी थीं। साम्प्रदायिकता तथा यौनिकता का यह हिन्दूवादी विमर्श विधवाओं के गर्भ से भी जुड़ गया। इस दौर का हिन्दूवादी प्रचार साहित्य, जिसमें लेखिका के अनुसार विभिन्न हिन्दी अख़बार तथा पुस्तक-पत्रिकाएँ शामिल थीं, हिन्दुओं की घटती संख्या तथा मुसलमानों की बढ़ती संख्या पर लगातार चिन्ता प्रदर्शित करते रहते थे। हिन्दुओं की इस कम होती संख्या का कारण विधवा-विवाह निषेध की प्रथा को माना गया और कहा गया कि हिन्दू विधवाएँ, जिनकी यौन-आकांक्षाएँ अनियंत्रित हैं, मुस्लिम पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं और मुस्लिमों की सन्तति को अपने गर्भ से जन्म देती हैं, जिससे मुसलमानों की संख्या बढ़ती है और हिन्दुओं की संख्या घटती जाती है। इस तरह अपनी किताब में लेखिका ने उस दौर के हिन्दूवादी विमर्शों तथा स्त्रियों पर बढ़ते पितृसत्तात्मक शिकंजे की ओर पाठकों का ध्यान खींचा है। वे मानती हैं कि हिन्दू पहचान के निर्माण की यह प्रक्रिया काफ़ी हद तक सफल रही लेकिन इसमें भीतर से दरार भी मौजूद थी और यह दरार हिन्दू महिलाओं की तरफ़ से डाली जा रही थी। हिन्दू महिलाएँ हिन्दुवादी पितृसत्ता को यह चुनौती प्रतिबन्धित ‘अश्लील साहित्य’ को पढ़कर भी दे रही थीं और धर्मान्तरण, सहपलायन, अन्तरधर्मीय विवाह, रोमांस, प्रेम और सेक्स के ज़रिये भी।
चारु गुप्ता की यह किताब औपनिवेशिक दौर के हिन्दी लेखन में स्त्री-यौनिकता को लेकर बढ़ रहे भय और उसे नियंत्रित करने की छटपटाहट को रेखांकित करने में सफल रही है। यह किताब उस दौर के हिन्दू प्रचार साहित्य से जुड़े कई रोचक तथ्यों को सामने रखती है और अपने तईं ‘औपनिवेशिक उत्तर भारत’ के हिन्दी प्रकाशन जगत की एक तस्वीर पेश करती है। विभिन्न जाति-संगठनों तथा धार्मिक सभाओं की बैठकों, बहसों तथा उनके साहित्य से रूबरू कराने के साथ ही यह किताब ‘चाँद’, ‘माधुरी’, ‘विशाल भारत’ जैसी हिन्दी की महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं तथा ‘भारत जीवन’, ‘अभ्युदय’, ‘प्रयाग समाचार’ तथा ‘वर्तमान’ जैसे पत्रों के ज़रिये हो रही हिन्दू साम्प्रदायिक गोलबन्दी की ओर भी हमारा ध्यान खींचने में सफल रही है। लेखिका यह भी दिखलाने में सफल रही हैं कि हिन्दू साम्प्रदायिकता और पितृसत्ता के बीच एक ‘चोली-दामन का रिश्ता’ था।
हिन्दी के वर्तमान अकादमिक संसार में रामचन्द्र शुक्ल की किताब ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ एक ख़ास जगह रखती है। इस किताब की पितृसत्तात्मक बनावट की ओर भी लेखिका ने हमारा ध्यान खींचा है। वे मानती हैं कि अपनी किताब में शुक्ल जी शृंगारिक साहित्य को बहुत ही हेय दृष्टि से देख रहे थे। लेखिका ने ठीक ही इंगित किया है कि शुक्ल जी का, “रीतिकालीन कवियों पर आक्रमण पौरुष के सवाल से भी गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। रामचन्द्र शुक्ल ने इस कविता की रचना को सीधे मध्यकाल और मुग़लकाल में पौरुष के पतन के साथ जोड़ा।”6 हालाँकि, लेखिका ने रामचन्द्र शुक्ल की पुस्तक के ज़रिये उस दौर के हिन्दी साहित्यिक परिदृश्य को समझ लेना चाहा है, जो इस शोध की सबसे गम्भीर भूल है। यहीं से लेखिका हिन्दी अकादमिक जगत के भीतर व्याप्त कुछ रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों का शिकार होती चली गई हैं। प्राथमिक स्रोतों की जगह हिन्दी की आलोचना पुस्तकों पर निर्भरता लेखिका को एक के बाद एक कई ग़लत निष्कर्षों की ओर ले गई है। शुक्ल जी की किताब के आधार पर बीसवीं सदी-पूर्वार्द्ध के हिन्दी साहित्यिक जगत में जिस तथाकथित ‘अश्लीलता विवाद’ की लेखिका ने कल्पना कर ली है, दरअसल वह बहुत दूर तक खींचा गया तर्क है जिस पर तफ़सील से बात करने की ज़रूरत है।
‘अश्लीलता विवाद’ इस पुस्तक की केन्द्रीय अव-धारणाओं में से एक है जिस पर लेखिका ने अपनी किताब के पाँच अध्यायों की रूपरेखा बनाई है।7 उनका मानना है, “उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हिन्दी साहित्य में अश्लीलता और यौन-रूपकों को लेकर विवाद”8 चला था जिसने हिन्दी की साहित्यिक दुनिया के दो ‘समानान्तर’9 हिस्से कर दिए। एक को लेखिका ‘उच्च साहित्य’ का नाम देती हैं और इसे हिन्दी के साहित्यिक ‘अाभिजात्य’ से जोड़ती हैं। दूसरे को वे ‘निम्न’ या ‘साहित्य का बाज़ारू और लोकप्रिय स्वरूप’10 कहती हैं और उसे “लोकप्रिय रुचि और पढ़ने की आदतों’11 से जोड़ती हैं। यहाँ ‘उच्च’ और ‘निम्न’ साहित्य के विभाजन का आधार लेखिका ने ‘अश्लीलता’ को बनाया है। ‘अश्लीलता’ क्या है?—इसे परिभाषित नहीं किया गया है। न ही ‘उच्च’ या ‘निम्न’ साहित्य की कोई परिभाषा दी गई है। ‘उच्च’ साहित्य के उदाहरण के रूप में लेखिका ने ‘सरस्वती’ जैसी पत्रिकाओं तथा हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त तथा सुमित्रानन्दन पंत को रखा है। शेष उस दौर में छपनेवाली प्रायः सभी साहित्यिक तथा लोक-शैलियों, उपन्यास आदि को ‘निम्न’ या ‘अश्लील’ की श्रेणी में रखा गया है।
हालाँकि, लेखिका ने ‘उच्च’ साहित्य को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन ‘बाज़ारू’ साहित्य में वे जिन विधाओं को शामिल करती हैं, उससे सम्भवतः पाठक किसी ‘उच्च’ साहित्य की कल्पना करने में सफल हो सकें। जो ‘उच्च’ साहित्य में शामिल नहीं है, अर्थात लेखिका के शब्दों में ‘कामुक’ और ‘अर्धपोर्नोग्राफ़िक’ विषयों पर केन्द्रित निम्न साहित्य है, उसमें ‘कोकशास्त्र’ जैसी ‘सेक्स टीकाएँ’ भी शामिल हैं और कजरी, फाग, होरी, लावनी जैसी लोक- शैलियाँ भी; रीतिकालीन कविता (जिन्हें लेखिका ने ‘ब्रजभाषा के कामुक गीत’ कहा है) भी शामिल है और देवकीनन्दन खत्री या किशोरीलाल गोस्वामी जैसे साहित्यकारों द्वारा लिखे गए ‘रोमांटिक नॉवल’ और ‘थ्रिलर’ को भी इसी ‘कामोत्तेजक साहित्य की श्रेणी में रखा गया है।12 यहाँ नौटंकी, संगीत या लोकगीतों की सस्ते दामों पर छपनेवाली छोटी-छोटी पुस्तिकाओं को भी अश्लील या लोकप्रिय साहित्य में शुमार किया गया है और ‘शृंगारशतक’ जैसे रीति-ग्रंथों को भी। इस तरह जो किताब ‘अश्लीलता’ की अवधारणा पर सवाल खड़ा करने के लिए लिखी गई थी, उसने ख़ुद ही हिन्दी के लगभग समस्त साहित्य को ‘अश्लील’ और ‘अर्धपोर्नोग्राफ़िक’ ठहरा दिया है।
लेखिका ने ‘अश्लीलता’ के इसी तर्क के सहारे ‘औपनिवेशिक उत्तर प्रदेश’ के शुरुआती हिन्दी पाठकों की पढ़ने की आदतों पर भी धारणा बना ली है। उनका मानना है कि लोगों की पढ़ने की आदतें अश्लील सामग्री को एक माल के रूप में उपलब्ध कराने का दबाव डालती थीं और “कामुक उपभोक्तावाद उत्तर प्रदेश के प्रकाशन जगत में आए भारी उछाल का हिस्सा बन गया। इस प्रवृत्ति के चलते ‘स्वच्छ’ साहित्य के वर्चस्व पर चोट लगती रहती थी।”13 वे यह भी मानती हैं कि, “ ‘उच्च’ स्वच्छ साहित्य के पाठक कम ही थे”14। इस तरह लेखिका ‘उच्च’ और निम्न के मध्य हिन्दी साहित्य को विभाजित करते हुए “हिन्दी साहित्य की जटिल और आपसी संघर्ष-भरी ज़मीन” की अवधारणा पेश करती हैं। जहाँ ‘स्वच्छ’ और ‘अश्लील’; ये दोनों तरह की रचनाएँ दरअसल ‘साहित्यिक उत्पादन’ के दो अलग-अलग रूप थे। इस “साहित्यिक उत्पादन के पीछे भाँति-भाँति की अपेक्षाओं, प्रेरणाओं और सन्दर्भों का हाथ था”15 ये नतीजे लेखिका ने किन आँकड़ों तथा तथ्यों के आधार पर निकाले हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता।
दरअसल ‘स्वच्छ’ और ‘अश्लील’ के आधार पर साहित्य का विभाजन पूरी तरह से एक निरर्थक कोशिश है। इसका हिन्दुस्तान की साहित्यिक परम्पराओं से कोई लेना-देना नहीं था। खोजने से भी यहाँ गुरुकुल की ब्रह्मचर्य पुस्तिकाओं के आलावा ऐसी रचना नहीं मिलेगी जिसमें शृंगारिक प्रसंगों या दैहिक सौन्दर्य का उल्लेख ‘अश्लील’ या वर्जित समझा जाता रहा हो। यहाँ तक कि ‘कोकशास्त्र, जिसे लेखिका बाज़ार की माँग से पैदा हुई कोई नई रचना समझ रही हैं16 वह भी कई शताब्दियों से भारतीय पाठकों के बीच स्वीकृत रहा है। इसी तरह लोक-शैलियों में वर्णित कामुक उद्गारों को रीतिकाल की कविता की नक़ल17 समझ लेना, उपनिवेश-पूर्व लोकमानस में यौन-विषयों की सहज स्वीकृति की उपेक्षा करना होगा। साथ ही ‘भारत-भारती’ जैसी कुछ गिनी-चुनी रचनाओं को ‘उच्च’ साहित्य का पैमाना मान लेना, किसी प्रामाणिक निष्कर्ष की ओर नहीं ले जाता है।
इस प्रसंग में दूसरा महत्त्वपूर्ण सवाल साहित्यिक परम्पराओं की उपेक्षा को लेकर है। जैसा कि भूमिका में कहा गया है कि यह किताब सत्तर प्रतिशत से भी अधिक हिन्दी के स्रोतों पर आधारित है। और जिस अधिकार से किताब में हिन्दी की साहित्यिक दुनिया पर बात की गई है, ऐसे में लेखिका से साहित्यिक परम्पराओं की सामान्य जानकारी रखने की अपेक्षा करना लाजमी है। रामचन्द्र शुक्ल की ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, रामविलास शर्मा की ‘महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण’ तथा महावीरप्रसाद द्विवेदी के एक लेख, जिसमें उन्होंने रीतिकालीन नायिका भेद का उपहास किया है; सन्दर्भ-सूची में उल्लिखित बस यही तीन स्रोत हैं जिनके आधार पर उस दौर के हिन्दी साहित्यिक जगत में किसी अश्लीलता विरोधी आन्दोलन की कल्पना कर ली गई है। हिन्दी लेखन में ब्रह्मचर्य का महिमामंडन तथा शृंगारिक विषयों का विरोध दिखलाने के लिए ‘हिन्दी साहित्य’ के जिन प्रमाणों को पेश किया गया है, वे हैं—गुरुकुल कांगड़ी से निकलनेवाला ‘गुरुकुल समाचार’ अख़बार, किन्हीं गणेशदत्त शर्मा गौड़ ‘इंद्र’ का ‘स्वप्न दोष रक्षक’, किन्हीं गुरुदास जी महाराज की उपदेश पुस्तिका ‘ब्रह्मचारी बनो’ तथा सूर्य्यबली सिंह नाम के किसी सज्जन की पुस्तिका ‘ब्रह्मचर्य की महिमा’। अगर केवल मैथिलीशरण गुप्त के ‘ब्रह्मचर्य का अभाव’ को पर्याप्त माना जाए, तभी हम कह सकते हैं कि हिन्दी साहित्यिक जगत में कथित ब्रह्मचर्यवाद छा गया था। अन्यथा उस दौर का साहित्य जिसमें छायावादी कविता तथा लम्बा-चौड़ा कथा साहित्य मौजूद था, वहाँ केवल दो-एक लेखों-किताबों के आधार पर किसी ‘नायिका संहार’ की कल्पना कर लेना अतिशयोक्ति ही होगी। साहित्यिक परम्पराओं की उपेक्षा तब और कचोटती है जब लेखिका बिना किसी ज़िम्मेदारी के न सिर्फ़ हिन्दी, बल्कि संस्कृत और फ़ारसी की साहित्यिक परम्पराओं पर भी लापरवाही-भरी टिप्पणी करती चली गई हैं। संस्कृत साहित्य की उन्मुक्त शृंगारिक परम्पराओं की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए संस्कृत साहित्य में शृंगारिक या ‘कामुक’ प्रसंगों की स्वीकृति केवल ‘उपासना की स्थापित परम्परा’ के भीतर ही सीमित मान लेती हैं, जिसका प्रमाण उनके अनुसार ‘गीत गोविन्द’ है।18 वे भूल रही हैं कि संस्कृत साहित्य में शृंगार कभी भी ‘उपासना’ या भक्ति का मोहताज नहीं रहा है। ‘राधा-कन्हाई’ की भक्ति तो रीति कविता में भी महज़ ‘बहाना’ ही थी। इसी तरह ‘सस्ती क़िस्म की कविताओं’ और ‘रूमानियत से भरे’ ‘निम्न’ साहित्य को हिन्दी में फ़ारसी के रास्ते आया बतलाना भी ठीक नहीं है।19 रीतिकाल के विषय में जानते हुए भी, इसे अनदेखा कर देती हैं और ‘हिन्दी में कामुक विषयों की अस्वीकृति’ के किसी लम्बे इतिहास की कल्पना कर लेती हैं।20 भ्रमरगीत परम्परा में उद्धव को कौन नहीं जानता? गोपियों को प्रेम का मार्ग छोड़ने और योग धारण करने का उपदेश देनेवाले उद्धव की गोपियाँ कितनी लानत-मलानत किया करती थीं! लेखिका उद्धव के ‘शृंगार विरोधी’ के रूप में रूढ़ चरित्र को भी इसकी परम्परा में नहीं देखतीं। उद्धव के इस परम्परागत शृंगार विरोधी चरित्र को बीसवीं सदी की कथित ‘अश्लीलता विरोधी’ मुहिम का हिस्सा समझ लेती हैं।21 कहना न होगा यह ‘घासलेटी साहित्य’ सम्बन्धी छोटे से विवाद को बहुत दूर तक खींचने की कोशिश में हुआ है।
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी और दुलारेलाल भार्गव को शृंगार-विरोधी के रूप में रूढ़ करना इस किताब की एक अन्य प्रमुख स्थापना है।22 लेखिका ने जिस तरह इन तीन लेखकों की छवि ‘अश्लीलता विवाद’ के झंडाबरदारों की बना दी है, वह छवि केवल इस पुस्तक में ही सिमटकर नहीं रह गई। सुधीश पचौरी ने अपने लेख ‘रीतिकाल में फूको विचरण’23 के भीतर चारु गुप्ता के इन निष्कर्षों को जगह देते हुए रीतिकाल सम्बन्धी एक नई बहस शुरू की, जिसे दूसरे लोगों ने भी ज्यों-का-त्यों अपना लिया और यह चल निकला कि महावीरप्रसाद द्विवेदी के सिर ‘नायिका हत्या’ का दोष है।24 न तो सुधीश पचौरी ने, न ही दूसरे लोगों ने चारु गुप्ता द्वारा उल्लिखित इन तथ्यों की जाँच करना ज़रूरी समझा। बहरहाल, बस एक बार उस दौर के प्राथमिक स्रोतों को पलटकर देखा जाए तो वे एक दूसरी ही कहानी कहते नज़र आते हैं। सबसे पहले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की ही बात करें, जिन्हें लेखिका “शृंगार रस की कविता पर सबसे गम्भीर हमला (करनेवाले) हिन्दी लेखकों के प्रभावशाली तबके”25 का अगुआ मानती हैं। जिन्होंने लेखिका के अनुसार, “इस कविता को स्त्री के शरीर पर केन्द्रित अश्लीलता का दोषी क़रार दिया” 26। चारु गुप्ता का दावा है, “इस प्रक्रिया की शुरुआत उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में स्वयं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने की, हालाँकि वह ख़ुद को इस क़िस्म की पद्य रचना से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाए।”27 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को शृंगार विरोधी सिद्ध करने के लिए लेखिका ने उनकी रचनाओं से उदाहरण देना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि वसुधा डालमिया की किताब में कहे गए कुछ वाक्यों का वास्तविक सन्दर्भ समझे बिना यह निष्कर्ष दे डाला, कि भारतेन्दु शृंगारिक कविता के विरोधी थे। वसुधा डालमिया के इस कथन का सन्दर्भ भी चारु गुप्ता ने अपनी हिन्दी-किताब में नहीं दिया है। ‘स्त्रीत्व से हिन्दुत्व तक’ के अंग्रेज़ी संस्करण में इसका सन्दर्भ वसुधा डालमिया की किताब का पृष्ठ 247 दिया गया है।28 वसुधा डालमिया की किताब के पृष्ठ 247 को देखने पर यह पता चला कि वसुधा ने कहीं भी नहीं लिखा कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने “इस कविता को स्त्री के शरीर पर केन्द्रित अश्लीलता का दोषी क़रार दिया” अथवा शृंगारिक कविता का विरोध किया। दरअसल, अपनी किताब के इस अध्याय में वे भारतेन्दु द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई ‘बालाबोधिनी’ पत्रिका के विषय में लिख रही थीं। यहाँ वे दिखला रही थीं कि सामान्य तौर पर ब्रजभाषा की शृंगारिक कविताओं को पसन्द करनेवाले भारतेन्दु, किस तरह महिलाओं की पत्रिका ‘बालाबोधिनी’ में इसे सेंसर कर रहे थे। वे लिखती हैं—
…स्त्री पत्रिकाएँ पुरुषों द्वारा सम्पादित भी होती थीं और उनमें लेख भी ज़्यादा उन्हीं के होते थे। पुरुष सम्पादकत्व के कारण ही, सम्भवतः, इनमें प्रस्तुत की जानेवाली विषय-वस्तु चरम नियंत्रित, यहाँ तक की सेंसरित होती थी। यह बालाबोधिनी की, और साथ में उस दौर की दूसरी स्त्री-पत्रिकाओं की एक केन्द्रीय विशेषता है…सेंसरशिप किस तरह की है, यह इसी से समझा जा सकता है कि भारतेन्दु की अन्य पत्रिकाओं में बहुत बड़े पैमाने पर छपनेवाली ब्रजभाषा की कविताएँ यहाँ बिलकुल नदारद हैं, जिसके पीछे वजह यही थी कि उन्हें कामोद्दीपक माना जाता। इससे क्या कि उनके ऊपर भक्ति का आवरण पड़ा हुआ था। इस रूप में भी वे कम ख़तरनाक नहीं थीं। शृंगार का वर्णन, भक्ति के छद्म वेश में भी साझा करने लायक़ अनुभव न था। ऐसी कविताएँ किसी स्त्री को अपने पति से इतर भी सोचने को विवश कर सकती हैं।
स्पष्ट है, शृंगारिक कविता केवल स्त्रियों के लिए वर्जित थी ‘सहृदय’ समाज के लिए इसका होना भारतेन्दु कितना ज़रूरी समझते थे, इसे ख़ुद उनकी रचनाएँ देखकर समझा जा सकता है। यही बात महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित पत्रिका सरस्वती या दुलारेलाल भार्गव द्वारा सम्पादित पत्रिका माधुरी के विषय में भी लागू होती है। भले ही द्विवेदी जी ने एकाध लेख लिखकर ‘नायिका भेद’ वाली कविता का उपहास किया लेकिन वे कहीं से भी अश्लीलता विरोधी किसी मुहिम के सरगना नहीं थे। इसके प्रमाण के लिए उनकी पत्रिका ‘सरस्वती’ के अंक पलटकर देखे जा सकते हैं जिनमें ‘शृंगारिक रचनाएँ’ भी थीं और अर्धनग्न नायिकाओं के ‘कामुक’ चित्र भी। इसी तरह दुलारेलाल भार्गव के कुछ वाक्यों के सहारे यह समझना कि वे ‘अपने अंग-अंग को खोले हुए बाज़ारू औरतों’ की तस्वीरों या ‘इन चित्रों के नीचे अश्लील दोहे और कविताओं के प्रकाशन’ का विरोध कर रहे थे, किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जाएगा। क्योंकि प्राथमिक स्रोतों को छानते हुए जब आप दुलारेलाल भार्गव की सुप्रसिद्ध चित्रशाला के चित्रों को पलटेंगे या उनके द्वारा सम्पादित पत्रिका के कंटेंट पर नज़र डालेंगे तो पाएँगे कि ‘अपने अंग-अंग को खोले हुए’ औरतों की तस्वीरें इन दोनों जगह बेशुमार हैं और तथाकथित अश्लील दोहे भी। ऐसे में अश्लीलता विवाद का यह समस्त प्रसंग इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों के इस्तेमाल से जुड़ी एक दूसरी लापरवाही की ओर हमारा ध्यान खींचता है। यह है साहित्यिक निबन्धों तथा रचनाओं में अभिव्यक्त विचारों अथवा कल्पनाओं को एक ऐतिहासिक तथ्य मान लेने की भूल। इसके अलावा द्वितीयक स्रोतों पर निर्भरता भी इसकी एक बड़ी वजह है।
ब्रह्मचर्य पर लिखी जानेवाली किताबों तथा ‘गुरुकुल समाचार’ को ‘उच्च’ साहित्यिक मूल्यों का प्रतिनिधि मानकर उनके बरक्स ‘सुहागरात’ या ‘कोकशास्त्र’ सम्बन्धी पुस्तकों और कामोद्दीपकों के इश्तेहारों को रखना और इसके आधार पर हिन्दी जगत में उभर रहे किसी ‘विरोधाभास’ को देखना भी ठीक नहीं है। ब्रह्मचर्य और शृंगार दोनों पर केन्द्रित पुस्तकें अभिलेखागारों में मौजूद हैं। इन्हें लेखिका ने ‘हिन्दू प्रचार साहित्य’ के दो विरोधाभासी तत्त्व बताया है। लेकिन क्या इन्हें ब्राह्मणवादी दर्शन में बताए गए जीवन के चार सोपानों के बतौर देखना अधिक कारगर न होगा? जहाँ छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य पर ज़ोर है और गृहस्थ जीवन में उन्मुक्त कामोपभोग की छूट। दरअसल ‘हिन्दू प्रचारक’ इन अलग-अलग पुस्तकों में हिन्दू जीवन-दर्शन के इन्हीं चार सोपानों में से किसी एक की बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर आर्यसमाजी ‘गुरुकुल कांगड़ी’ अपने छात्रों के लिए ब्रह्मचर्य पर ही ज़ोर देता। या दूसरे सनातनी संगठन ख़ास तौर पर युवकों को सम्बोधित करनेवाली ब्रह्मचर्य आधारित किताबें छापते। क्या केवल इन पुस्तिकाओं या गुरुकुल समाचार के आधार पर किसी व्यापक वीर्य-रक्षक मुहिम की कल्पना करना ठीक होगा? गुरुकुल और इसके बाहर की दुनिया के बीच यौनिकता, अश्लीलता या शृंगारिकता को लेकर कितनी बड़ी दरार थी, इसे समझना हो तो गुरुकुल के ही छात्र रहे यशपाल की रचना ‘सिंहावलोकन’ एक बेहतरीन दस्तावेज़ है। ऐसे में गुरुकुल को हिन्दी लेखन के ‘अाभिजात्य धड़े’ का प्रतिनिधि मान लेना सर्वथा भ्रामक है। इसी तरह ‘ब्रह्मचर्य’ और ‘कामोपभोग’ को हिन्दू प्रचारकों के किसी ‘विरोधाभास’ के रूप में देखना भी कारगर नहीं है। हालाँकि पच्चीस वर्षों तक ब्रह्मचर्य और उसके बाद ही गृहस्थ जीवन की बातें, बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखक बार-बार दोहराया करते थे। ऐसा करने के पीछे उनका मक़सद बाल-विवाह विरोधी एक वातावरण तैयार करना था। लेकिन इन बातों का असर समाज पर कितना हुआ, कहा नहीं जा सकता।
जहाँ तक ‘अश्लीलता’ के विरोध का प्रश्न है, यह केवल स्त्रियों तक सीमित था। सामग्रियों को लेकर ज़्यादातर विरोध स्त्रियों को केन्द्र में रखकर किया गया था। चाहे वह महिलाओं के मनोरंजन की देशज शैलियों का नियंत्रण हो, उनके द्वारा विवाह में गाई जानेवाली गारियों का विरोध, या मेलों-त्योहारों को ‘अश्लील’ बताकर महिलाओं को उनसे दूर रखने की कोशिश—‘अश्लीलता’ से जुड़ी सभी चिन्ताओं के केन्द्र में केवल महिलाएँ थीं। इसी किताब में दिए गए ‘गुरुकुल समाचार’ के एक लेख को देखें, जिसमें ‘अश्लीलता’ को लेकर सारी चिन्ता केवल महिलाओं और बच्चों तक सीमित है, पुरुषों के लिए यह सामग्री कहीं से भी ‘अश्लील’ या वर्जित नहीं मानी गई है,
कामोत्तेजक चित्त में विकार उत्पन्न करनेवाले विज्ञापनों को पढ़कर कुल कामिनी गण सिर नीचा कर लेती हैं, छोटी उम्र की कन्याएँ, बालक पढ़कर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह रात का मज़ा क्या है? हट्टा, कट्टा, पट्ठा कैसे बन जाना होता है, वीर्य गाढ़ा होकर दही का थक्का कैसे जमता है, यह अपूर्व पदार्थ क्या है? कोई यह तो नियम है नहीं कि इन अख़बारों को कुल कामिनी गण न पढ़ें, बालक-बालिका उधर दृष्टि न दें। वर्ण-पत्र पढ़ने को सभी का जी चाहता है पर उनमें अमृत के स्थान में विष भरा है, वे क्या जान सकते हैं…अब पाठक गण उन कौतुकवर्धक विज्ञापनों में उन दवाओं के नाम पढ़ें और देखें कैसे विलासिता के रस से भरे हुए हैं। रति विलास, कामिनी विलास, मदन विलास, काम विलास, मदन मंजरी, मदन संजीवनी, धातु संजीवनी, नपुंसक संजीवनी, सुन्दरी संजीवनी, मदन वटी, कामदेव वटी, कनक प्रभा, वन्धेज, सुख करक वन्धेज, शक्ति तैल, ब्रह्म शक्ति, धातु पुष्ट, पुष्ट राज आदि। यह तो थोड़े से पत्रों से ही चुने गए हैं।…
स्वार्थी कामी गण इन्द्रियों के दास बन इन्द्रियों के दासों को यहाँ तक प्रलोभन देते हैं कि दो-दो घंटे थकावट न होगी। स्त्रियों के लटके हुए कुच गेंद से कठोर हो जाएँगे…एक ओर शिक्षा का प्रवाह बह रहा है। गुरुकुल और ऋषिकुल खुल रहे हैं। ब्रह्मचर्य के पालन के उपाय किए जा रहे हैं…उधर संसार में इस प्रकार के अश्लील विज्ञापन छाप और बाँटकर देश का नाश कर रहे हैं…हमारी समझ में तो ऐसे अख़बारों को माँगने को कौन कहे, हाथ से भी नहीं छूना चाहिए, विशेष कर स्त्रियों के हाथ में तो जाना ही नहीं चाहिए।
ऐसे में लेखिका का यह कहना—“अश्लीलता के आक्षेप केवल लैंगिक विभाजनों से बँधे हुए नहीं थे…चिन्ता के केन्द्र में ‘अश्लीलता’ का ही मुद्दा था”30—बहुत ठीक नहीं लगता।
यह किताब हिन्दू साम्प्रदायिकता के उभार—‘अश्लीलता विवाद’ तथा लैंगिक संहिताओं के सुदृढ़ीकरण में हिन्दी लेखकों की भूमिका पर तो बात करती है लेकिन, औपनिवेशिक प्रभुओं के रूप में ब्रिटिश सत्ता की भूमिका को सिरे से ख़ारिज कर देती है। ‘अश्लीलता विवाद’ या नवीन लैंगिक संहिताओं के निर्माण में ब्रिटिश सरकार की भूमिका को नकारते हुए लेखिका ने स्पष्ट कर दिया है—
औपनिवेशिक भारत के बारे में कई अध्ययनों ने औपनिवेशिक शासन और शासकों की प्रभुत्वशाली भूमिका पर ज़ोर दिया है। उनके अनुसार उपनिवेश बनाए गए लोगों की ख़ुद की आवाज़ दब गई थी और वे कोई पहल करने के बजाए केवल प्रशासकों की आवाज़ पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। लेकिन यह ग़ौरतलब है कि अंग्रेज़ शासकों की अवाज़ ख़ुद भी अन्दर से विभाजित थी और वे सब मिलकर केवल एक ही बोली नहीं बोल रहे थे। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात है कि भारतीय लोगों की अपनी एक पहल थी, जो केवल एक प्रतिक्रिया नहीं थी।…एक अन्य बात मैं कहना चाहती हूँ—कई विचारक यह मानते हैं कि औपनिवेशिक काल के पूर्ववर्ती काल में लैंगिक, यौनिक और नैतिक संहिताओं में अधिक लचीलापन था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता।
लेकिन चारु गुप्ता का यह शोध ही इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह पूर्ववर्ती काल में लैंगिक, यौनिक और नैतिक संहिताओं में अधिक लचीलापन था, जिसे औपनिवेशिक दौर में ‘हिन्दू प्रचारकों’ ने पूरी तरह ख़त्म करने की मुहिम छेड़ दी। क्या ‘हिन्दू प्रचारकों’ की इस मुहिम पर ही यह किताब केन्द्रित नहीं है? हालाँकि लेखिका ने ‘विक्टोरियन नैतिकता’ के तर्क को सिरे से नकार दिया है और अश्लीलता या लैंगिकता से जुड़े हर विवाद को देशज विचारों की देन माना है। लेकिन किताब में पेश किए गए सन्दर्भ तथा घटनाएँ ‘अश्लीलता’ सम्बन्धी औपनिवेशिक निर्मिति की ओर इशारा करती हैं—“भारत में अश्लीलता को लेकर सबसे शुरुआती क़ानून उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशकों में सामने आए। भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 और 294 को ख़ासतौर से किसी भी प्रकार की अश्लीलता का निषेध करने के लिए संहिताबद्ध किया गया था।”32 इससे पहले के भारतीय शासकों के लिए ‘अश्लीलता’ जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी, जिसे रोकने के लिए किसी तरह की क़ानूनी संहिताएँ बनाई जातीं। नवलकिशोर प्रेस जैसे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन संस्थानों, जिन्होंने बड़े पैमाने पर रीतिग्रंथों को प्रकाशित और संरक्षित करने का बीड़ा उठाया, उन पर ‘अश्लीलता’ के आरोप में छापे डालना क्या औपनिवेशिक पहल को नहीं दर्शाता? क्या क़ानून बनाकर शृंगारिक साहित्य का लेखन और प्रकाशन को ख़त्म करने की सरकारी कोशिश पर बात नहीं की जानी चाहिए? इसके अलावा ‘बुढ़वा मंगल’ जैसे मेलों, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएँ भागीदारी करती थीं, उसमें महिलाओं की उपस्थिति को ‘अश्लील’ क़रार देकर उसका उपहास करना और उस पर रोक लगाना; क्या यह ‘अश्लीलता’ की आयातित अवधारणा की ओर इशारा नहीं करते? किताब में उद्धृत, ‘उत्तर प्रदेश’(पश्चिमोत्तर प्रान्त) के शिक्षा-निदेशक एम. कैम्पसन या फिर 1873 में ‘संयुक्त प्रान्त’ (पश्चिमोत्तर प्रान्त) के अधिकारी सी.ए. इलियट आदि के द्वारा की गई टिप्पणियाँ, जिनमें इन रचनाओं को ‘अश्लील तुकबन्दियाँ’ या ‘बेहद घटिया और अश्लील श्रेणी’ का क़रार दिया है, उनकी भूमिका को किस तरह देखा जाए? ग्रियर्सन द्वारा 1925 में लिखा गया ‘गोपनीय पत्र’ किस ओर इशारा करता है?
यह किताब ही बताती है कि ब्रिटिश सरकार ने “आदेश जारी कर दिया कि रेलवे प्लेटफ़ार्म पर ऐसा ‘आपत्तिजनक’ साहित्य नहीं बेचा जाएगा। कामुक किताबों, पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, पोस्टकार्डों और तस्वीरों को ज़ब्त किया जाने लगा और ‘अश्लीलता’ के आरोप में छापेख़ानों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं की धर-पकड़ होने लगी। भ्रष्ट और यौन विषयक सामग्री की तलाश में अक्सर किताबों की दुकानों पर छापे पड़ने लगे। 1870 में जोसेफीन बटलर द्वारा स्थापित की गई एसोसिएशन फ़ॉर मोरल एंड सोशल हाइजीन की भारतीय शाखा अपने केन्द्रीय संगठनकर्ता मैलीसैंट शेफ़र्ड के माध्यम से अश्लीलता के ख़िलाफ़ एक तीखी मुहिम छेड़े हुए थी। इन धर्मयोद्धाओं ने यौनिकता और सेक्स सम्बन्धी अभिव्यक्तियों पर लगाम कसी। उनकी कार्रवाइयाँ अक्सर यौन केन्द्रित किताबों, परचों और पत्रिकाओं पर सेंसरशिप का रूप ले लेती थीं।”33
ऐसे में यह दिखाने का प्रयास कि औपनिवेशिक सरकार हिन्दुस्तानी ‘अाभिजात्य’ की माँग पर यह सब कर रही थी, ठीक नहीं लगता। यह इसलिए भी ठीक नहीं लगता क्योंकि यही देशी अाभिजात्य, जो ख़ुद ही शृंगारिक रचनाएँ लिख रहा था और शृंगारिक कवियों को संरक्षण दे रहा था, क्या बिना किसी बाहरी दबाव के इनका विरोध करने पर आमादा हो गया? यह मानना ग़लत न होगा कि नवीन पीढ़ी के अंग्रेज़ी में शिक्षित रामचन्द्र शुक्ल जैसे कुछ विद्वान ‘अश्लीलता’ सम्बन्धी इस यूरोपीय अवधारणा के असर में थे। लेकिन हिन्दी की पूर्ववर्ती साहित्यिक परम्परा से इन विचारों का कोई तालमेल नहीं था। कुछेक हिन्दी लेखक जो ‘अश्लीलता’ के कारण हिन्दू पतन की अंग्रेज़ी मान्यता को दोहरा रहे थे, यह उनकी अपनी मौलिक प्रस्थापना भी नहीं थी। इसे अंग्रेज़ों के सम्मुख ख़ुद को शर्मिंदा महसूस कर रहे भारतीयों द्वारा ‘आत्मसुधार’ का प्रयास समझना अधिक कारगर होगा। ‘अश्लीलता’ जैसी अवधारणा में भरोसा कर रहे थोड़े से भारतीयों के बरक्स बहुत बड़ी संख्या उन लेखकों, पाठकों तथा प्रकाशकों की थी, जो ‘अश्लीलता’ की इस विक्टोरियन अवधारणा के असर में नहीं थे और सरकार की नज़रों से छिप-छिपाकर भी शृंगारिक ग्रंथ लिख, पढ़ और छाप रहे थे। साथ ही ‘अश्लीलता’ सम्बन्धी इन अंग्रेज़ी क़ानूनों को प्रेस एक्ट के ज़रिये देशी भाषाओं के प्रकाशनों पर लगाम कसने की एक कोशिश के बतौर भी देखना चाहिए। ग़ौरतलब है कि उपनिवेश विरोधी सरगर्मियाँ और ‘अश्लीलता’ सम्बन्धी सरकारी आक्षेप साथ-साथ लय पकड़ रहे थे।
एक अन्य सवाल इस पूरी किताब से स्त्रियों को बाहर रखने को लेकर है। जो उस दौर के हिन्दी सार्वजनिक जगत में एक अच्छी ख़ासी संख्या में शरीक हो चुकी थीं। उन पर बात न कर के महिलाओं की तरफ़ से पितृसत्ता को दी गई चुनौती को केवल “पलायन, धर्मान्तरण, रोमांस, प्रेम और सेक्स”34 या “मज़े ले-लेकर कामुक कथाएँ, जासूसी उपन्यास, प्रेम कहानियाँ, नाटक, स्वाँग, नौटंकियाँ, और गाने की किताबें”35 पढ़ने तक सीमित मान लेना; क्या औपनिवेशिक हिन्दी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पितृसत्ता को दी गई चुनौती को बहुत कम करके आँकना नहीं है? दरअसल, ये स्त्रियाँ केवल देह या सेक्स के स्तर पर ही चुनौती नहीं दे रही थीं, उनकी अपनी एक सार्वजनिक उपस्थिति भी थी। जिस दौर में ‘हिन्दू प्रचारक’ सार्वजनिक जगत में पितृसत्तात्मक विचारों का प्रचार-प्रसार कर रहे थे, ठीक उसी समय इसी सार्वजनिक दुनिया में महिलाएँ भी मौजूद थीं और अपनी बातें रख रहीं थीं। वे केवल कामोद्दीपक साहित्य नहीं पढ़ रहीं थीं, बल्कि विश्वविद्यालयों और दफ़्तरों में भी पहुँच रही थीं। पत्रिकाओं के सम्पादन, लेखन-सृजन, अध्ययन-अध्यापन और बहुत से दूसरे पेशों से भी जुड़ रही थीं।36 और इन मंचों से कई बार पितृसत्तात्मक नियम-क़ायदों को लताड़ भी लगा रही थीं। वे आन्दोलनों में शरीक हो रही थीं, सड़कों पर उतर रही थीं, कांग्रेस या आर्यसमाज की प्रचारिका थीं, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग कर रही थीं और जेलों को भर रही थीं। वे ऐसी बहुत-सी दूसरी गतिविधियों में शामिल थीं जिनसे ‘हिन्दू पितृसत्ता’ द्वारा प्रचारित की जा रही ‘घरेलू’ स्त्री की छवि को चुनौती मिल रही थी। क्या इन महिलाओं की उपेक्षा करके ‘हिन्दू पहचान’, पितृसत्ता और यौनिकता के आपसी सम्बन्धों को समझा जा सकता है?
यहाँ कुछ सवाल इतिहास लेखन पद्धति को लेकर भी हैं। किताब की भूमिका में लेखिका सवाल करती हैं कि “हिन्दी में—या किसी भी देशी भाषा में—इतिहास लेखन कैसे किया जाए?” ऐसे में किसी भी पाठक को इस किताब से गुज़रते हुए हिन्दी में इतिहास लेखन के किसी बेहतरीन नमूने का इन्तज़ार रहता है। उस वक़्त यह किताब ख़ासी निराश करती है। वह भी तब जब पाठक इसी किताब के 2001 में छपे अंग्रेज़ी संस्करण से गुज़र चुका हो। न सिर्फ़ अंग्रेज़ी की किताब के कई महत्त्वपूर्ण हिस्सों को इस किताब से बाहर रखा गया है बल्कि अंग्रेज़ी किताब में दी गई लम्बी-लम्बी सैद्धान्तिक चर्चाओं तथा क़रीब नब्बे फ़ीसदी सन्दर्भों को हिन्दी संस्करण में छाँट दिया गया है। क्या यह हिन्दी पाठकों को लेकर लापरवाही का मामला है? अथवा हिन्दी में इतिहास लेखन कैसा हो इसका कोई उत्तर? भाषा को साहित्यिक बनाने की कोशिश में भाषा सम्बन्धी कुछ ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि किताब कई जगह अबूझ बन गई है। जो हिन्दी में पढ़ने के आदी किसी पाठक के लिए ख़ासी मुश्किल पैदा कर देती है। नतीजन, बहुत से महत्त्वपूर्ण प्रसंगों में सम्प्रेषण बाधित होता है और लेखिका दरअसल कहना क्या चाह रही हैं, इसे समझने के लिए अंग्रेज़ी की किताब का सहारा लेना पड़ता है। बेहतर यही होता कि भाषा सम्बन्धी इन अनगढ़ प्रयोगों के बजाय सामान्य बोलचाल की भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता।
कुछेक सीमाओं के बावजूद यह एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें औपनिवेशिक दौर के हिन्दी-लेखन में घुसपैठ कर रहे साम्प्रदायिक विचारों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। किस तरह महिला और साम्प्रदायिकता का आपसी सम्बन्ध केवल दंगों तक सीमित न रखकर, औरतों के रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा बनाया जा रहा था, यह इस किताब की एक महत्त्वपूर्ण स्थापना है। किताब के इस हिन्दी संस्करण में अंग्रेज़ी की किताब से अलग जोड़ा गया अध्याय ‘तब और अब : निरन्तरता और बदलाव’ जिसमें ‘लव-जिहाद’ सम्बन्धी वर्तमान साम्प्रदायिक प्रचार की ऐतिहासिक जड़ें दिखाई गई हैं, हिन्दुवादी प्रचारतंत्र के तौर-तरीक़ों में एक निरंतरता को चिह्नित करता है। इस तरह यह किताब हिन्दी में छपनेवाली हिन्दू प्रचार साहित्य को समझने के लिए एक नवीन अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है। हालाँकि हिन्दू प्रचार साहित्य के उपांग के तौर पर ‘हिन्दी साहित्य’ को रखने से कुछ मुश्किलें ज़रूर खड़ी होती हैं। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या साहित्य प्रचार का ही एक उपकरण है? यह सच है कि साहित्यकार जनमत पर एक प्रभावशाली असर रखते हैं, लेकिन इससे क्या साहित्य की भूमिका प्रचार-सामग्री की हो जाती है? क्या इस आधार पर ‘हिन्दी लेखकों’ को ‘हिन्दू प्रचारकों’ की जमात में शामिल मान लेना उचित होगा? इससे जुड़ा हुआ ही एक दूसरा सवाल यह है कि क्या ‘औपनिवेशिक उत्तर प्रदेश’ (संयुक्त प्रान्त) की सार्वजनिक दुनिया इतनी एकल थी कि उसे केवल ‘हिन्दू प्रचारक’ जैसी किसी इकहरी जमात में हदबन्द कर दिया जाए? क्या हिन्दी में साम्प्रदायिक एकता का पक्षधर कोई लेखक-साहित्यकार नहीं था? क्या दयानन्द और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को एक ही जमात ‘हिन्दू प्रचारक’ के दायरे में रख देना, अथवा कांग्रेस और हिन्दू महासभा को एक ही ‘हिन्दू प्रचारक’ समूह का सदस्य मान लेना ऐतिहासिक जटिलताओं की अनदेखी करना न होगा? हिन्दू प्रचारकों के लेखन तक सीमित रहने से यह किताब उस दौर की एक अधूरी-सी तस्वीर ही पेश कर पाती है जबकि हिन्दी सार्वजनिक जगत में दूसरी भी आवाज़ें थीं, जो हिन्दू प्रचारकों की नफ़रत भरी संकीर्ण आवाज़ों से अधिक सुनी जाती थीं। हिन्दी की दुनिया में प्रेमचन्द जैसे लेखक बिलकुल अकेले नहीं थे, उनके साथ अनगिनत पाठकों की वह संख्या थी, जो हिन्दू प्रचारकों की बनिस्बत इन साहित्यकारों के अधिक सुने जाने का प्रमाण देती थी। सबसे बढ़कर क्या महात्मा गांधी के पंथनिरपेक्ष ‘हिन्दू’ विचारों का हिन्दी क्षेत्र में कुछ भी प्रभाव था? इस पर किताब में कहीं भी बात नहीं की गई है। बेहतर होता कि यौनिकता, अश्लीलता और साम्प्रदायिकता से जुड़े इन मुद्दों पर लेखिका केवल हिन्दू-संगठनों की गतिविधियों तक सीमित न रहतीं बल्कि महिला लेखकों और दूसरे बड़े साहित्यकारों तथा धर्मनिरपेक्ष संगठनों के साहित्य को भी इस बहस में जगह देतीं। ‘हिन्दू साम्प्रदायिकता’ सम्बन्धी यह अध्ययन इससे अधिक प्रामाणिक बन पाता। बावजूद इसके यह किताब कई महत्त्वपूर्ण जानकारियों को अपने में समेटे हुए है और औपनिवेशिक दौर की हिन्दूवादी सरगर्मियों तथा प्रचार तंत्र को समझने के लिए एक बहुमूल्य सन्दर्भ उपलब्ध कराती है। यह सन्दर्भ बहुत से नए सवालों और शोध की नई दिशाओं की ओर इशारा करते हैं।
(‘आलोचना’ सहस्त्राब्दी अंक-61 में प्रकाशित चारु सिंह का लेख। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में शोधार्थी हैं। वह जेंडर, साहित्येतिहास और समसामयिक विषयों पर लिखती हैं। संपर्क का माध्यम : [email protected])