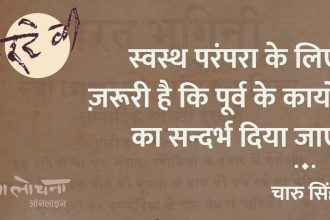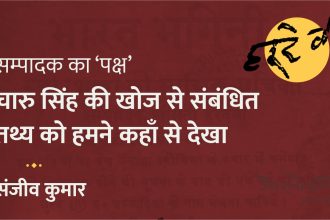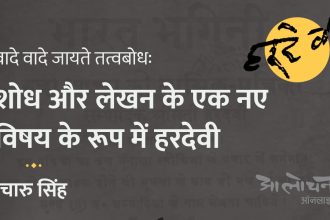इंडियन एक्सप्रेस (18 नवंबर, 2024) में सुहास पलसीकर लिखते हैं : ‘हमारे लोकतंत्र के साथ जो गड़बड़ी है, बुलडोज़र उसका एक अभिलक्षण है। अदालत ने आख़िरकार भौतिक बुलडोज़र पर ग़ौर फ़रमाया है और इसके ग़ैर-क़ानूनी इस्तेमाल को रोकने की कोशिश की है। लेकिन अवधारणा और विचारधारा के स्तर पर बुलडोज़र अभी भी हैं और अदालत उन्हें लेकर शायद ही कुछ कर पायेगी।’ ऐसे बुलडोज़रों के बारे में लगभग दो साल पहले प्रकाशित आलोचना अंक-68 का यह संपादकीय पढ़ा जा सकता है। क्या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ‘अवधारणा और विचारधारा के स्तर पर’ कार्यरत इन बुलडोज़रों का भी कुछ बिगाड़ पाएगा?
…
पूरा आर्यावर्त बुलडोज़रों से पटा पड़ा है। और क्यों न हो? अतिक्रमण की इंतिहा जो हो गई है!
जो जगह मनुस्मृति के लिए सुरक्षित थी, उसे कोई 72 साल पहले एक दलित की देख-रेख में बने भारतीय संविधान ने अतिक्रमित कर लिया। जो जगह आस्था को मिलनी चाहिए थी, उसे तर्क-बुद्धि और वैज्ञानिक मिज़ाज ने अतिक्रमित कर रखा है। जहाँ सिर्फ़ पुरुषों को होना चाहिए था, वहाँ स्त्रियों के अतिक्रमण, और जहाँ सिर्फ़ सवर्ण होने चाहिए थे, वहाँ दलित-बहुजनों के अतिक्रमण से कौन नावाक़िफ़ है! इन सबसे पुराना जो अतिक्रमण है, जिसने एक विशुद्ध/ग़ैर-मिलावटी संस्कृति को गंगा-जमुनी बना डाला, उसके बारे में कहना ही क्या! साहित्य और कलाओं में प्रगतिशीलता, प्रयोगशीलता और आलोचनात्मक चेतना का अतिक्रमण तो ख़तरे के निशान से ऊपर चल ही रहा है; पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालयों में हिन्दू-विरोधी और राष्ट्रविरोधी विचारों के अतिक्रमण की भी वही स्थिति है! और भाषा? हमारी हिन्दी में जहाँ सिर्फ़ देवभाषा के शब्दों को जगह मिलनी थी, वहाँ मलेच्छ शब्दों के अतिक्रमण के उदाहरण ढूँढ़ने के लिए आपको दूर भी नहीं जाना होगा। वे इसी अनुच्छेद में पूरी ठसक के साथ मौजूद हैं!
इन तमाम क़िस्म के अतिक्रमणों से निपटने के लिए असंख्य बुलडोज़र रात-दिन काम में लगे हुए हैं। काम चल तो बहुत पहले से रहा है, पर तब बुलडोज़रों की संख्या इतनी ज़्यादा न थी। उनके चालक भी, अपनी यथेष्ट निर्ममता के बावजूद, इतने कुशल नहीं थे। अब बात अलग है। अब बुलडोज़रों की फूलती-फलती आबादी को विश्वास है कि इन सभी अतिक्रमणों को नेस्तनाबूद करना मुश्किल भले ही हो, नामुमकिन नहीं है।
हाल ही में ऐसा एक बुलडोज़र वडोदरा के महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी के ललित कला संकाय में समय से पहले जा धमका। वह उस कला-प्रदर्शनी को उजाड़ने गया था जो अभी लगी ही नहीं थी। एबीवीपी के जत्थे के रूप में पहुँचे उस बुलडोज़र को पता चला था कि वहाँ कुछ ऐसी कलाकृतियों को प्रदर्शनी में शामिल किया गया है जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर उसकी भावनाएँ ऑलरेडी आहत हो चुकी हैं। उनमें से एक शृंखला देवी-देवताओं के उन कट-आउट्स की थी जो स्त्रियों के ख़िलाफ़ हुए अपराधों की अख़बारी ख़बरों से बनाए गए थे। अफ़सोस, बुलडोज़र को पता चला कि अभी तो प्रदर्शनी को जनता के लिए खोला भी नहीं गया है और उसके लिए आई प्रविष्टियों के चयन का काम चल रहा है। 2007 में इसी तरह बुलडोज़र की कृपा होने के बाद यह नियम बना था कि सालाना प्रदर्शनी से पहले कलाकृतियों की जाँच होगी और संभावित आपत्तिजनक कलाकृतियों को शामिल नहीं किया जाएगा। फिलवक़्त वही काम जारी था।
लेकिन पहले के बुलडोज़रीय कारनामों का महत्त्व धूमिल न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय ने एक नौ-सदस्यीय तथ्यान्वेषी कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी ने आनन-फानन में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी जिसके आधार पर घटना के महज़ छह दिनों बाद हुई सिंडिकेट की बैठक में उस ‘आपत्तिजनक’ कलाकृति को बनानेवाले विद्यार्थी कुंदन यादव को विश्वविद्यालय से बर्ख़ास्त कर दिया गया और उसके शिक्षक, सुपरवाइज़र, संकाय के डीन आदि को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इस घटना से बुलडोज़रों के महत्त्व का पता चलता है। इसी महत्त्व के कारण तो कई बार बाहर से बुलडोज़र भेजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती; विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं उस किरदार में आ जाते हैं। (वैसे हो सकता है, बात उलट हो। प्रशासनिक अमला बुलडोज़र का किरदार निभाने में लगा है या बुलडोज़र ही प्रशासनिक अमले की भूमिका में हैं, कहना मुश्किल है।) शारदा यूनिवर्सिटी ने मामूली-सी शिकायत पर उस शिक्षक को निलंबित करने में कोई देरी नहीं की जिसने राजनीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र में यह सवाल पूछा था: “क्या आप फ़ासीवाद/नाज़ीवाद और हिन्दू दक्षिणपंथ (हिन्दुत्व) के बीच कुछ समानताएँ देखते हैं? तर्कसहित विश्लेषण करें।” उस शिक्षक की ग़लती यह थी कि वह पढ़ा-लिखा था और उसे पता था कि—(1) हिन्दुत्व का मतलब हिन्दू धर्म नहीं है, जैसा कि स्वयं इस शब्द के आविष्कर्ता सावरकर साहब ने बता रखा है, और (2) हिन्दुत्व और फ़ासीवाद/नाज़ीवाद के बीच राजनीतिवैज्ञानिकों ने अनेक समानताएँ चिह्नित की हैं, स्वयं गुरु गोलवलकर का हिटलरीय जाति-शुद्धि-अभियान के प्रति प्रेम और आरएसएस की स्थापना के पीछे हिटलर और मुसोलिनी के कृत्यों की प्रेरणा जगज़ाहिर है, जिनसे परिचित होने की उम्मीद राजनीतिविज्ञान के विद्यार्थी से की जाती है।
पढ़े-लिखे होने के इस अपराध की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए! शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने सज़ा देकर साबित किया कि पढ़ाई-लिखाई जैसे अपराध में उनकी कोई मिलीभगत नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है : ‘विश्वविद्यालय बिरादरी ऐसे किसी विचार के पूरी तरह से ख़िलाफ़ है जो हमारी राष्ट्रीय प्रकृति (ईथाॅस) में निहित महान राष्ट्रीय पहचान और समावेशी संस्कृति को विरूपित करता है।’ इस बयान से पता चलता है कि हिन्दुत्व के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन की राय स्वयं हिन्दुत्ववादी है। ऐसा प्रशासन असिस्टेन्ट प्रोफ़ेसर श्री वक़स फ़ारूक़ कुट्टी को अविलंब निलंबित करे, यह बिल्कुल स्वाभाविक था। विडंबना बस यह है कि प्रश्न को अवैध मानकर जो कार्रवाई की गई, उससे प्रश्न की वैधता ही साबित होती है! ग़रज़ कि हिन्दुत्व और फ़ासीवाद/नाज़ीवाद के बीच समानता तलाशने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। एक ऐसा सवाल, जिसमें तर्कसहित विश्लेषण की माँग के कारण यह निहित है कि विद्यार्थी तार्किक विधि से समानता की बात को ख़ारिज भी कर सकता है, अगर उस प्रशासन के लिए इस हद तक नाक़ाबिले-बर्दाश्त है, तो फ़ासीवाद और किसे कहते हैं!
लखनऊ विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफ़ेसर रविकांत को तलाशते हुए जो बुलडोज़र पहुँचा था, उसकी शिकायत यह थी कि प्रोफ़ेसर ने एक यूट्यूब चैनल की बहस में ज्ञानवापी मुद्दे पर कुछ ऐसी बातें क्यों रखीं जो बुलडोज़र को नापसंद हैं। प्रोफ़ेसर रविकांत ने पट्टाभि सीतारमैया के हवाले से एक बात कही थी, उसे प्रोफ़ेसर की राय बताकर बुलडोज़र लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में तोड़फोड़ मचाने लगा और साथ में ‘देश के गद्दारों को गोली मारो सा.. को’ का आह्वान भी करता रहा। ‘गद्दारों’ का तुक ‘सारों’ से मिलता है, पर रलयोर-परिवर्तन के नियम का लाभ उठाते हुए ‘सारों’ के ‘रों’ की जगह ‘लों’ का प्रयोग किया गया। यह इम्प्रोवाइज़ेशन अब नया नहीं रह गया है; गत आठ (अब दस) सालों में इस नारे को भड़भड़ाते बुलडोज़र असंख्य बार देखे गए हैं और कई बार तो उनका संचालन राष्ट्रीय स्तर के बुलडोज़र चालकों के हाथ में रहा है।
वस्तुत:, ‘गोली मारो’ आज का मानक बुलडोज़र गान है। और यह गान तब तक प्रासंगिक बना रहेगा जब तक अतिक्रमण रहेंगे… नहीं, माफ़ कीजिएगा, जब तक बुलडोज़र रहेंगे। यह गान सम्पूर्ण आर्यावर्त में गूँज रहा है। कान बंद करके इसे अनसुना करने की कोशिश बेमानी है। और अनसुना करें भी क्यों? अगर आप देश के गद्दार नहीं हैं तो यह सुन-सुनकर आपको ख़ुश ही होना चाहिए! आपको ख़ुश होना पड़ेगा!
ख़ुश न होना ‘देश के गद्दार’ होने का सबूत माना जाएगा।
अगर आप लेखक हैं तो इस बुलडोज़र युग की प्रशस्ति में लेख, कविताएँ, कहानियाँ लिखिए। अगर आप गायक हैं तो इसकी विरुदावली गाइए। अगर फ़िल्मकार और चित्रकार हैं तो इसके मोहक दृश्य उकेरिए।
और अगर इनमें से कुछ नहीं हैं तो आप सबसे अधिक उपयोगी हैं; सीधा बुलडोज़र बन जाइए। फिर ‘देश के गद्दार’ आर. चेतन क्रांति आपको ‘वे’ में शुमार करते हैं तो करें—‘चीखदार पीकदार चैनलों की टी.आर.पी. बढ़ाने, सिरकटे एंकरों के कबंध-नृत्य में ढोल बजाने, खाली पंडाल भरने, तालियाँ पीटने, धूम मचाने, धर्म का राज्य स्थापित करने’ के लिए बुलाए जानेवाले ‘वे’। कवि को कराहने दीजिए :
वे अजीब थे
नहीं, शायद बेढंगे
नहीं, डरावने
न, सिर्फ़ अहमक
नहीं, अनपढ़
नहीं, पैदाइशी हत्यारे
नहीं, भटके हुए थे वे
नहीं, वे बस किसी के शिकार थे
हाँ, शायद किसी के हथियार
वे पहेली हो गए थे
समझ में नहीं आता था
कि वे कब कहाँ और कैसे बने
क्यों हैं वे, कौन हैं, क्या हैं
आरोपित दाम्पत्य की ऊब का विस्फोट?
वैवाहिक बलात्कारों की ज़हरीली फसल?
स्वार्थ को धर्म और धर्म को स्वार्थ बना चुके
पाखंडी समाज का मानव-कचरा?
ऊँच-नीच के लती देश की थू थू था था?
या असहाय माता-पिता की लाचारियाँ दुश्वारियाँ बदकारियाँ?
या कुछ भी नहीं
बस मांस-पिंड
जो यूँ ही गर्भ से छिटककर
धरती पर आ पड़े
और बस बड़े होते रहे
और फिर कुछ
अतीतजीवी
हास्यास्पद
लेकिन चतुर जनों के हाथ लग गए।
इन बुलडोज़रों की शिनाख़्त करनेवाले सबसे आला बुद्धिजीवियों में से एक, प्रो. एजाज़ अहमद इसी साल (2022) मार्च महीने में नहीं रहे। 2015 में वे भारत छोड़ चुके थे, क्योंकि हर पाँच साल पर वीज़ा का नवीकरण कराने की तकलीफ़देह अनिश्चितता मोदी सरकार के गठन के बाद से और मारक हो चली थी। हारकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफोर्निया, इरविन में चांसलर्स प्रोफ़ेसर का पद स्वीकार कर लिया और भारी मन से भारत को अलविदा कह दिया। किसे पता था कि सात साल बाद वे इस दुनिया को ही अलविदा कह जाएँगे!
एजाज़ साहब ने एडवर्ड सईद, सलमान रश्दी, फ़्रेडरिक जेमसन, देरीदा जैसे दिग्गजों की जाँच-परख करते हुए जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल की, उसकी तुलना में सांप्रदायिक प्रश्न पर उनकी अन्तर्दृष्टियों की चर्चा कम हुई है। बुलडोज़र प्रसंग में उनका 2013 का आलेख, ‘कॉम्युनलिज़्म : चेन्जिंग फ़ॉर्म्स एण्ड फ़ॉर्च्यून्स’ (पी सुंदरैया की जन्मशती पर हैदराबाद में आयोजित सेमीनार में प्रस्तुत पर्चा; THE MARXIST, XXIX, अप्रैल-जून 2013) विशेष रूप से ध्यान देने लायक़ है। नव-उदारवाद और सांप्रदायिक फ़ासीवाद के बीच के रिश्ते पर वामपंथी बुद्धिजीवियों ने काफ़ी विचार किया है और मुख्य बल इस बात पर रहा है कि हिन्दुत्व के मुद्दे नव-उदारवादी दौर में पूँजीवाद के अनिवार्य संकट, जो जनता की क्रयशक्ति और कुल माँग में आई कमी के कारण असमाधेय हैं, की ओर से जनता का ध्यान बँटाने के काम आते हैं, जहाँ राष्ट्र के भीतर एक ‘अन्य’ की गढ़ंत और उसका दानवीकरण आर्थिक मुद्दों को दरकिनार करने का साधन बनता है।
एजाज़ अहमद ने अपने व्याख्यान में इस रिश्ते के एक और पहलू की ओर हमारा ध्यान खींचा है जो 2013 के बाद के नौ वर्षों में अधिकाधिक प्रासंगिक होता गया है। वे इस रिश्ते को नव-उदारवाद, जिसे वे दूसरे शब्दों में उग्र-पूँजीवाद कहते हैं, के दौर में बेरोज़गारों की बहुत बड़ी फ़ौज और उसके कारण बने निम्न वेतन-स्तर से जोड़कर देखते हैं। यह ऐसे हालात तैयार करता है जहाँ सांप्रदायिक ताक़तों को बड़ी आसानी से अपने स्टॉर्म ट्रूपर्स, अपनी विराट लफंगी पैदल सेना के सिपाही हासिल होते हैं। आलेख का यह अंश एजाज़ अहमद के विश्लेषण की उस विलक्षणता का उदाहरण है जो उन्हें दूसरे चिंतकों से अलग करती है और जिसे बुलडोज़रो की चर्चा करते हुए हमें अवश्य याद रखना चाहिए :
भारतीय सांप्रदायिकता की पूरी संरचना में—वह संघ की हो, मुसलमानों की या शिव सेना की—बड़े पैमाने पर लंपट सर्वहारा और लंपटीकृत निम्न पूँजीपति वर्ग से आए स्टॉर्म ट्रूपर्स इतनी अहम भूमिका इसलिए निभाते हैं कि यही भारतीय पूँजीवाद की, ख़ासकर उसके नव-उदारवादी दौर में, संरचनात्मक विशेषता है। बेरोज़गारों की फ़ौज उन कामगारों के मुक़ाबले बहुत बड़ी है जिन्हें कोई स्थिर रोज़गार मिल पाता है, और यह एक ऐसी स्थिति निर्मित करता है जिसमें, अन्य रुग्ण लक्षणों के अलावा, तनख़्वाह इतनी कम है कि एक समुचित सर्वहारा संस्कृति का निर्वाह बहुत मुश्किल है और ख़ुद सर्वहारा के भीतर से बहुतेरे लंपटीकरण की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे आंशिक रूप से पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर श्रम और वेतन के आधार पर जीवन-निर्वाह करते हैं, लेकिन पूरक के तौर पर चतुराई/हेरा-फेरी, और कई बार तो अपराध, के ज़रिए भी कमाई करते हैं। और भी बदतर यह कि बेरोज़गारों की फ़ौज इतनी विराट, इतनी स्थायी है कि उनमें से अनगिनत लोग काम की तलाश ही छोड़ देते हैं, उस व्यवस्था से ही बाहर छिटक जाते हैं जिसे क़ायदे से पूँजीवादी व्यवस्था कहा जाता है, किसी ऐसे श्रम में नहीं लगते जो अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है, उस छद्म अर्थतन्त्र की आपराधिक दुनिया में पहुँच जाते हैं जो वास्तविक अर्थतन्त्र के समानांतर चलता है और किसी नियम के अधीन नहीं होता, यहाँ तक कि शोषण के नियम के भी, और जहाँ एक दाँव से दूसरे दाँव के बीच साधारण आजीविका से लेकर अकूत दौलत तक या एक औचक मौत तक कुछ भी कमाया जा सकता है। उत्पादक श्रमिक का स्थिर जीवन उसे अपने काम को लेकर एक आत्मसम्मान, या कम-से-कम पाँव तले की ज़मीन मुहैया करता है, लेकिन उत्पादकता का अभाव, इस बोध का अभाव कि वह कौन है, उसे आत्मसम्मान से वंचित कर देता है। वह आत्मसम्मान दुबारा किसी भी तरह से अर्जित किया जाना ज़रूरी है, भले ही वह दूसरों को नुक़सान पहुँचा कर हो, अपराध के द्वारा हो, या उस कथित ‘अन-अपराध’ के द्वारा जो स्वयं सांप्रदायिकता है, अपनी तमाम हिंसाओं के साथ। मूल्य-उत्पादक श्रमिक का जीवन उसके जैसे ही काम करनेवालों के समुदाय में जिया जाता है, लेकिन लंपट सर्वहारा का जीवन अपनी प्रकृति से ही ऐसा होता है कि वह श्रम की साझा परिस्थितियों से निकलनेवाले किसी समुदाय की रचना नहीं करता। वह हमेशा ऐसे समूहों में काम करता है जो अनिश्चित और परिवर्तनशील होते हैं और आकस्मिकताओं, जिनका सामना इस आधे-अधूरे वर्ग के व्यक्ति हमेशा करते हैं, के दबाव में पुनराविष्कृत होने की अनवरत आवश्यकता से घिरे होते हैं। वर्गीय जुड़ाव से वंचित होने के कारण उनमें जाति और धर्म सरीखे सामुदायिक जुड़ाव का प्रलोभन पैदा होता है—ऐसा जुड़ाव जो श्रमिक समुदाय के ठोस जुड़ाव के मुक़ाबले अधिक अमूर्त है। सांप्रदायिक राजनीति में भर्ती उन्हें एक वास्तविक समुदाय से जुड़ाव का बोध देती है, भले ही वह बोध झूठा हो। इस प्रक्रिया में हाव-भाव की वह आक्रामकता जो लंपट जीवन में जीवित-भर रहने के लिए ज़रूरी होती है, बड़ी आसानी से संगठित हिंसा के सांप्रदायिक/फ़ासीवादी प्रकारों में रूपांतरित हो जाती है।
रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस निकालते हुए जयकारों को जंग की ललकार में तब्दील कर देनेवाली, कला-प्रदर्शनियों को उजाड़नेवाली, लेखकों-बुद्धिजी गद्दार बताकर गोली मारने का आह्वान करनेवाली, और बहाने ढूँढ़कर बस्तियों की बस्तियाँ फूँक देनेवाली उपद्रवी सेनाओं पर नज़र डालिए—आप एजाज़ साहब की अंतर्दृष्टि के क़ायल होंगे। सांप्रदायिक फ़ासीवाद की बढ़त के साथ उग्र-पूँजीवाद के इस सूक्ष्म रिश्ते को पहचानने के कारण ही उनका मानना था कि सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ संघर्ष धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में चलाया जानेवाला विचारधारात्मक संघर्ष भर नहीं है, वह ख़ुद पूँजीवाद के ख़िलाफ चलनेवाले संघर्ष का हिस्सा है। वे ज़ोर देकर कहते हैं कि कॉम्युनलिज़्म का असली, टिकाऊ विकल्प खुद कॉम्युनिज़्म, या आपको बेहतर लगे तो सोशलिज़्म है, सेकुलरिज़्म या नेशललिज़्म नहीं, विचारधारात्मक हलके में वे जितने भी मददगार साबित हों।
ऐसे बुद्धिजीवी के न रहने से हमारी दुनिया थोड़ी और विपन्न हुई है, थोड़ी और निस्तेज।
[आलोचना सहस्त्राब्दी अंक-68 का संपादकीय]