साल 1911। इसी साल दो बच्चे पैदा हुए, आगे चलकर जिन्होंने अपनी शायरी से उर्दू अदब में खूब हंगामा बरपा किया। एक को फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के नाम से तो दूसरे को मजाज़ के नाम से जाना गया। मजाज़ शायरी की दुनिया में तब आये जब हक़ीक़तपसंदी और तरक्क़ीपसंदी का बोलबाला था, तरक्क़ीपसन्द तहरीक बाक़ायदा एक आन्दोलन की शक्ल अख़्तियार कर चुकी थी। मजाज़ रुदौली (बाराबंकी) में 19 अक्टूबर 1911 में पैदा हुए। इन्होंने शुरुआती पढ़ाई यहाँ की, इसके बाद आगरा आ गए। पहले तो मजाज़ इंजीनियर बनना चाहते थे, इस लिहाज़ से वो साइंस पढ़ने लगे थे। लेकिन शायरी का चस्का लग गया और फ़ेल होते रहे। बहरहाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बी.ए. किया।
मजाज़ ने ग़ज़ल और नज़्म के साथ रुबाइयाँ भी लिखीं लेकिन मजाज़ को नज़्मों से ही ख़ास शोहरत मिली। उर्दू शायरी में उनका योगदान ज़्यादा नज़्म के मैदान में ही है। “आवारा”, “रेल और रात”, “नौजवान ख़ातून से”, “लखनऊ” इत्यादि उनकी मशहूर नज़्में हैं। एक ज़माने में मजाज़ की मशहूर नज़्म “आवारा” साहिर लुधियानवी की नज़्म “ताजमहल” और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म “मुझ से पहली-सी मोहब्बत मिरी महबूब न माँग” से ज़्यादा मक़बूल थी।
मजाज़ को अपनी ज़िन्दगी के शुरुआती दौर में ही रातभर जागते रहने की आदत पड़ गई। इस आदत के कारण मिले लक़ब को उनके नाम की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। वह सफ़िया और हमीदा के जगन भैया बन गए। घर के प्यार का तमाम ख़ज़ाना मजाज़ पर ही लुटा दिया जाता था। हमीदा सालिम लिखती हैं कि अगर मजाज़ की मासूमियत और पुरख़ुलूस शख़्सियत ना होती तो पक्का हम भाई-बहन उन पर लुटाए जाने वाली मोहब्बत की हसद में ख़ूब लड़ाइयाँ करते फिरते। बचपन से ही मजाज़ को वह फ़न हासिल था कि जिस बैठक में शिरकत करते उसके केन्द्र बिन्दु वही हो जाते। रुदौली से उनका लगाव बदस्तूर बना रहा बल्कि वह इतना ज़्यादा था कि उनके घर के पास जब रुदौली से एक बेहद ख़ूबसूरत दुल्हन आई तो मजाज़ उस पर फ़िदा हो गए। इस क़दर फ़िदा हुए कि अपनी छोटी बहन का नाम उसी के नाम पर हमीदा रख दिया। हमीदा बताती हैं कि उम्र के शुरुआती दौर से ही उनकी शख़्सियत के दो रुख़ रहे हैं। हुस्न से दिलचस्पी और ड्राइंग से लगाव के साथ-साथ जोड़-घटाव और गुणा-भाग में महारत भी थी। मज़ाज उछल-कूद के साथ-साथ तीमारदारी का भी फ़न रखते थे। इसका असल उदाहरण देखने को मिलता है जब मजाज़ अपनी छोटी बहन हमीदा की पढ़ाई के मसले पर संजीदा हो गए और सारा ज़िम्मा अपने हाथ में ले लिया।
वालिद के आगरा तबादले के साथ-साथ मजाज़ की क़िस्मत भी बदलने वाली थी। हींग मंडी में पड़ोसी भी मिले तो फ़ानी बदायूँनी। इंजीनियरिंग के लिए गणित की तिकड़म लगाते-लगाते ज़िन्दगी ने कुछ ऐसी तिकड़म लगाई कि शायरी का जगत “जगन” के लिए बाँहें फैलाए तैयार खड़ा था। इंटर पास हुई तो आ पहुँचे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और साइंस के फंदे से आज़ाद होकर यह जहाज़ का पंछी अदब के जहाज़ पर आ बैठा। मजाज़ के ख़ुद के ये अश’आर उनकी अलीगढ़ में इब्तेदाई ज़िन्दगी की अक़्कासी करते हैं—
ये मेरी दुनिया, ये मेरी हस्ती
नगमा ताराज़ी, सहबा परस्ती
शायर की दुनिया, शायर की हस्ती
या नाला-ए-ग़म या शोरे मस्ती
यहाँ मजाज़ को मुईन अहसन जज़्बी, अख़्तर रायपुरी, सिब्ते हसन जैसे लोगों की संगत मिली। मजाज़ दोस्ती निभाने का हुनर बख़ूबी जानते थे लिहाज़ा हर एक दोस्त के जीवन के किसी भी बड़े काम में मजाज़ की शमूलियत होती ही थी। हमीदा अख़्तर रायपुरी ने ‘हमसफ़र‘ में अनोखे बाराती नाम से जो बाब लिखा है उसमें मजाज़ का नाम भी सरे-फेहरिस्त है। कमाल अहमद सिद्दीक़ी का मानना है कि मजाज़ ने शायरी के फ़न के नुक्ते अहसन मारहवी और फ़ानी बदायूँनी से सीखे पर उसे सही दिशा अख़्तर रायपुरी ने दी। खुद अख़्तर रायपुरी अपनी किताब गर्दे राह में लिखते हैं कि शाम को अक्सर वे और मजाज़ टहलने निकल जाते थे और अख़्तर अपने सीमित इल्म से (जो मजाज़ के लिए ग़ौरतलब था) उन्हें आगाह कराते रहते थे। सालभर ये सिलसिला चला और फिर उन्होंने देखा कि अब मजाज़ पुराने अंदाज़ की नज़्म लिखना छोड़ चुके हैं। उस वक़्त की मजाज़ की शायरी को लेकर मुशीर उल हसन ने बताया है कि एक ज़माने में आफ़ताब हॉस्टल मजाज़ की शायरी से सरशार रहा करता था।
बी.ए. करने के बाद एम.ए. उर्दू कर रहे मजाज़ का अभी पहला ही साल चल रहा था कि उन्हें ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में सरकारी पर्चे “आवाज़” के एडिटर की नौकरी मिल गई। सालभर ही गुज़रा था कि रेडियो स्टेशन की कमान पतरस बुखारी के हाथों में आ गई। हमीदा और अली सरदार जाफ़री दोनों ही के लेखों से यह मालूम होता है कि उनके वक़्त में पंजाबी और ग़ैर-पंजाबी की सियासत रेडियो स्टेशन में शुरू हो चुकी थी। आग़ा अशरफ़ और मजाज़ ग़ैर-पंजाबी होने के कारण रोज़ाना कुछ ना कुछ मुश्किल झेलते ही थे और आख़िरकार रेडियो स्टेशन के भीतर की सियासत ने मजाज़ को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रेडियो स्टेशन की दिक़्क़तों की तरफ़ इशारा देवेंद्र सत्यार्थी ने भी किया है। इस पर अधिक जानकारी के लिए बलराज मेनरा का देवेंद्र सत्यार्थी पर लिखा मज़मून “देवेंद्र सत्यार्थी के साथ एक दिन” देखें। दिल्ली छोड़ते हुए मजाज़ ने अपनी नज़्म “दिल्ली से वापसी” में अपने ताक़तवर होकर लौटने का ऐलान किया है—
सर से पा तक एक ख़ूनी राग बनकर आऊँगा
लालाज़ारे रंगो बू में आग बनकर आऊँगा
1936 में ही मजाज़ ने अपनी नज़्म “नज़रे अलीगढ़” लिखी जिसके आख़िर में उन्होंने लिखा कि—
इस गुलकदे पीराना में फिर आग भड़कने वाली है
फिर अब्र गरजने वाले हैं फिर बर्क़ कड़कने वाली है
यह एक हलचल की तरफ़ इशारा था और साथ ही यूनिवर्सिटी के भीतर से एक इंक़लाब बुलन्द करने की ललकार भी। अफ़सोस! ऐसा हो ना सका। उनकी बहन हमीदा ख़ुद लिखती हैं कि काश अलीगढ़ के नौजवान मजाज़ की उम्मीदों पर खरे उतर पाते! मजाज़ को कभी दकियानूसी रिवायत पसन्द ही नहीं आईं। वो किसी भी खाँचे में फिट हो जाना बुरा मानते थे। अलीगढ़ की रिवायत से वाक़िफ़ लोग जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में बोलते वक़्त टोपी की क्या अहमियत है मगर मजाज़ को इन सब से कोई लगाव नहीं था। अली सरदार जाफ़री बताते हैं कि अलीगढ़ की रिवायत के ख़िलाफ़ नंगे सर तरन्नुम में शेर पढ़ते हुए मजाज़ के अश’आर पर हॉल तालियों से गूँज रहा था। ये मजाज़ की मक़बूलियत का भी एक नमूना है। जब खालिदा अदीब खानम अलीगढ़ आईं तब यूनिवर्सिटी यूनियन में मजाज़ ने अपनी नज़्म से उनका इस्तिक़बाल किया। उर्दू न समझ सकने वाली खालिदा अदीब ने उनके तरन्नुम से मुतास्सिर होकर 5-10 मिनट तक उर्दू और मजाज़ की तारीफ़ की। मजाज़ की मक़बूलियत तो लड़कियों में भी काफ़ी थी। इस हद तक थी कि इस्मत चुगताई लिखती हैं कि गर्ल्स कॉलेज में लड़कियाँ उसके नाम के कुर्रे निकालती थीं और ख़ुश होती थीं।
मजाज़ जो लाखों दिलों की धड़कन थे और जिनके हज़ारों लोग दीवाने थे वह ख़ुद जिसके दीवाने हुए वह लड़की बदक़िस्मती से शादीशुदा निकली। राष्ट्रीय आन्दोलन के एक कद्दावर ख़ानदान की बहू से न तो इश्क़ लड़ाने की हिमाकत की जा सकती थी और न ही उसे पा सकने का ख़्वाब तामीर हो सकता था। मजाज़ की ज़िन्दगी में शायद ‘इब्तिदा–ए इश्क़ से बेमेहर’ ही रहना लिखा था। इसी कैफ़ियत के आलम में मजाज़ ने अपनी मशहूर नज़्म “आवारा” तख़लीक़ की। ग़म में भी शायर का अपना ग़म नहीं बल्कि ज़माने का ग़म और ग़ुस्सा झलकता है। रूमानियत में इंक़लाब का बेजोड़ मिलन होता है और क़ागज़ पर उतरती हैं यह पंक्तियाँ—
लेके इक चंगेज़ के हाथों से ख़ंजर तोड़ दूँ
ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूँ
औरत और मर्द के फ़र्क़ को मजाज़ ने ज़िन्दगी के साथ-साथ शायरी में भी मिटा दिया है। जब तरक्क़ीपसन्द तहरीक़ के भी कई शायरों ने औरतों को इंक़लाब के काबिल न माना उस वक़्त भी मजाज़ का इंक़लाब दोनों को साथ लेकर ही चल रहा था। मिसाल के लिए ये अश’आर देखें—
आओ मिलकर इंक़लाब-ए-ताज़ातर पैदा करें
दहर पर इस तरह छा जाएँ कि सब देखा करें
इस दौर में सात शायरों का एक ग्रुप था जिनमें से सबका आज शायरी में अलग मुक़ाम है। उनमें जज़्बी, नून मीम राशिद, जाँनिसार अख्तर, मख़दूम, मजाज़, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और अली सरदार जाफ़री शामिल थे। जोश मलीहाबादी की शायरी ने धूम मचा रखी थी, एजीटेशनल शायरी अपने उफ़ुक़ पर थी। इसी बीच मजाज़ अपनी रूमानी-इंक़लाबी शायरी के साथ शायरी की दुनिया में दाख़िल हुए तो हाथोंहाथ लिए गए। मजाज़ फ़ानी बदायूँनी से मुतास्सिर रहे थे और अख़्तर शीरानी को उर्दू अदब का बड़ा शायर मानते थे। लेकिन मजाज़ की शायरी में फ़ानी बदायूँनी की तरह अपनी ख़ुद की ज़िन्दगी का मातम नहीं है, न ही अख़्तर शीरानी जैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ रोमांस। उसकी शायरी में फ़न भी है और समाज की फ़िक्र भी। इसीलिए तो वो कहता है—
तेरे माथे पे यह आँचल बहुत ही ख़ूब है लेकिन।
तू इस आँचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने मजाज़ को इंक़लाब का ढिंढोरची नहीं बल्कि इंक़लाब का मुगन्नी कहा था। एक आलोचक ने तो उसे उर्दू अदब का कीट्स तक कहा है। वो फ़ैक्ट्री, कारख़ाने में काम करने वाले मज़दूरों का शायर था। बहुत पहले ही उसने मज़दूरों के ख़राब हालात के कारणों की निशानदेही कर ली थी और उसे अपनी नज़्म “सरमायेदारी” में दर्ज कर लिया था। यूँ—
कलेजा फुँक रहा है और जबाँ कहने से आरी है
बताऊँ क्या तुम्हें क्या चीज यह सरमाएदारी है।
यह वह आँधी है जिसकी रौ में मुफ़लिस का नशेमन है,
यह वह बिजली है जिसकी ज़द में हर दहकाँ का खरमन है।
यह अपने हाथ में तहजीब का फ़ानूस लेती है,
मगर मज़दूर के तन से लहू तक चूस लेती है।
मजाज़ को मज़ाहिया फ़लक पर भी एक चमचमाता इम्तियाज़ हासिल था। इसे वो अक्सर बहस-मुबाहिसों में दोस्तों के बीच गर्मा-गर्मी के आसार देख कर माहौल का तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही एक मौक़े पर मजाज़ ने मामला बिगड़ते देख जज़्बी से बेसाख़्ता पूछ लिया कि यार! तुम्हारे हाथ की खुजली का क्या हाल है? जज़्बी ने कहा जाने कितने मरहम इस्तेमाल कर चुका हूँ, कम हो जाती है, जाती नहीं है। मजाज़ ने कहा परेशान न हो कोढ़ है, कोढ़! एक ठहाका लगा और माहौल की ख़ुशगवारी लौट आई। एक समाजी तब्दीली का हामी मजाज़ का दोस्त फ़रमाने लगा कि सोचता हूँ किसी बेवा से शादी कर लूँ। जिस पर मजाज़ ने कहा यार फ़िक्र न करो! तुम जिससे भी शादी करोगे जल्द ही बेवा हो जाएगी।
मजाज़ को शायद सबसे बेहतरीन ढंग से जिसने समझा है वह है— मोहम्मद हसन जिन्होंने मजाज़ की ज़िन्दगी से मुतास्सिर होकर ‘ऐ ग़म-ए-दिल ऐ वहशत-ए-दिल’ नॉवेल लिखा। ‘बोल अरी ओ धरती बोल’ कैसे जन्मी होगी इसे समझाते हुए वह बताते हैं कि एक बार एक अंग्रेज़ अफ़सर मजाज़ के पहलवान नुमा दोस्त चक से भिड़ गया। जैसे-जैसे चक उस अंग्रेज़ अफ़सर को लात और घूँसे रसीद करते जाते मजाज़ जोश में आकर ‘बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डावाँ-डोल’ गाते जाते थे।
फ़ातमी साहब ने मजाज़ पर लिखी अपनी किताब (मजाज़ : शख़्सियत और फ़न) में उनका दूसरी जंग-ए-अज़ीम को लेकर एक भाषण उद्धृत किया है जिसमें वो साम्राज्यवादी ताक़तों और फ़ासिज़्म के सख़्त ख़िलाफ़ बयान देते हैं।
अपनी काबिलियत के दम पर मजाज़ इश्तिराकियत (समाजवाद) और सियासी ख़यालात से वाबस्ता थे। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड उनके वालिद जो लखनऊ के न्यू हैदराबाद में रहते थे मजाज़ भी अब उन्हीं के साथ रहने लगे थे। अली सरदार जाफ़री बहस-मुबाहिसों की दुनिया के औराक़-ए-मुसव्विर थे और मजाज़ जंग के इस तौर से बेनियाज़। सज्जाद ज़हीर ‘रौशनाई’ में लिखते हैं कि हम सब उस वक़्त मजाज़ की हर नज़्म को तरक्क़ीपसन्द तख़लीक़ (रचनाओं) में एक तारीख़ी मुकाम समझते थे लिहाज़ा जब हयातुल्लाह अंसारी ने उनकी नज़्म के सिलसिले में बताया तो सभी सुनने के लिए राज़ी हो गए। मजाज़ की मक़बूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ़िरंगी महल के हयातुल्लाह अंसारी और एक और नौजवान रज़ा अंसारी भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने मजाज़ की नज़्म “अँधेरी रात का मुसाफ़िर” को किसी जश्न की महफ़िल जैसा माहौल दिया था। जितनी कम उम्र में मजाज़ को शोहरत मिली बहुत कम शायरों नसीब हुई। उसको चाहने वाले बहुत थे, बावजूद इसके वो तनहा महसूस करता रहा। अपने को रेज़ा-रेज़ा मारता रहा। शराबनोशी की लत लग गयी और शराब का नशा उस पर इस क़दर तारी हुआ कि उसे राँची के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। वहाँ से ठीक होकर तो आया लेकिन शराब नहीं छूटी। जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गयी तो मजाज़ इससे बहुत आहत हुए थे। उसने गांधी को इंसानी दुखों का चारासाज़ कहा—
हिन्दू चला गया, न मुसलमां चला गया।
इंसां की जुस्तजू में इक इंसां चला गया।।
शारिब रुदौलवी मजाज़ की कॉफी हाउस में जगह को लेकर लिखते हैं। (कॉफ़ी का इंक़लाब में क्या हिस्सा हो सकता है इसे ले कर क्रिस्टिन विक्टोरिया मजिस्ट्रेली प्लाइस ने अपनी किताब ‘ब्रूइंग रेजिस्टेंस : इंडियन कॉफ़ी हाउस ऐंड इमरजेंसी इन पोस्ट कोलोनियल इंडिया’ में लिखा है) यूँ तो सभी की मेज़ें तक़सीम थीं मगर मजाज़ के आते ही सब तरतीब बदल जाती थी। कुछ देर एहतेशाम हुसैन और डॉक्टर आलम के साथ बैठकर अपनी मेज पर आते तो उनके इर्द-गिर्द एक दायरा बन जाता था जो देर रात तक वैसे ही रहता था। मजाज़ के जिन आवारा दोस्तों की बात सरदार जाफ़री ने लिखी है उनमें अचल सिंह, सदासरण मिश्र और हजीला शामिल थे। ये लोग अक्सर मजाज़ को अपने साथ ले जाते थे और ताड़ी पिला देते थे जो उनके लिए किसी ज़हर से कम न थी। माँ तो फिर माँ होती है। उस दौर में जब लोग मजाज़ से मिलने से कतराते थे और जब मजाज़ का कोई ठौर-ठिकाना न रहता था तब भी वो उनका खाना, सिगरेट और माचिस की डिब्बी और कुछ पैसे उनके बाहर वाले कमरे में रख जाती थीं। मजाज़ बेखुदी की हालत में भी आए तो भूखा न सोए और उसे घर छोड़ जाने वाले रिक्शेवाले अपनी मेहनत की कमाई ले जाएँ। मजाज़ जब ज़्यादा नशे में होते तो घर न जाते बल्कि हनुमान सेतु पार कर शारिब रुदौलवी के लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही रह जाते। ऐसा इसलिए कि वो नशे की हालत में कभी भी माँ-बाप के सामने नहीं आना चाहते थे। पीने के बाद भी वह कभी इज़्ज़त के ख़याल से ला-इल्म नहीं होते थे।
अली सरदार जाफ़री कहते हैं कि मजाज़ मुझसे शराब के लिए 5 रुपये माँगता था मगर शारिब रुदौलवी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह सब उनकी शराबनोशी की इंतेहा समझाने के लिए बढ़ा-चढ़ा कर लिखी गई बातें हैं और असल में मजाज़ ने कभी किसी से 1 रुपया तक न माँगा। अगर उनके पास रुपए होते थे तो वह कॉफ़ी के पैसे भी खुद ही अदा करते थे। इस तरह उन्होंने नशे की हालत में भी कभी कोई स्तरहीन या ओछी बात नहीं की। कमाल अहमद सिद्दीक़ी के मुताबिक़ मजाज़ मुनाफ़िकों को छोड़कर सभी का लिहाज़ करते थे। शारिब मजाज़ की कहानी ख़त्म होने की दास्तान कुछ यूँ सुनाते हैं— “3 दिसंबर से लखनऊ में अपने ढंग का पहला स्टूडेंट्स उर्दू कन्वेंशन था। कन्वेंशन की इंतज़ामिया कमेटी की चेयरमैन (आलिया इमाम) और जनरल सेक्रेट्री मैं (शारिब) था। मेरे साथ आरिफ़ नकवी, जकी शीराज़ी, शकेब रिज़्वी, इब्नेहसन, हैदर अब्बास, ख्वाजा राइक, हफ़ीज़ नौमानी और न जाने कितने नौजवान थे। साहिर पास ही एक होटल में रुके थे और उन्होंने मजाज़ से दिन में न पीने का वादा ले रखा था और उन्हें उनके आवारा दोस्तों से बचाने के लिए साथ ही रख रहे थे। मगर एक चूक हुई, थोड़ी आँख बची और ऐसी बची कि मजाज़ फिर आँख न खोल सके। “मजाज़ के एक दोस्त शाइर जलाल मलीहाबादी और एक साहब जो पहलवान की उर्फियत रखते थे बैठे थे। उन्होंने मजाज़ को देखकर आवाज़ दी, मजाज़ उस वक़्त भी ख़ासे सुरूर में थे लेकिन उन दोनों की आवाज़ सुनकर वह बेतहाशा रिक्शे की तरफ दौड़े और मेरे रोक सकने से पहले उस में बैठ कर निकल गए।” उन्होंने एक ताड़ीखाने की छत पर मजाज़ को अकेले छोड़ दिया और दिसंबर की सर्दी किसी दीमक की तरह हज़ारों लोगों के महबूब शायर के पहले से घायल जिस्म को खा गई। कोई उन्हें बलरामपुर अस्पताल ले गया मगर अब कुछ हो न सकता था। आख़िर मजाज़ ‘जाता हूँ जाता हूँ’ की पंक्तियों को साकार कर वाकई इस फ़ानी दुनिया से चले गए।
शारिब उस पूरे माहौल को कुछ ऐसे सामने लाते हैं— “नियाज़ हैदर का यह आलम था कि आँसुओं से चेहरा तर था और जनाज़े के एक पाए को इस तरह पकड़ रखा था कि किसी को बदलने नहीं देते थे। मैंने इस वक़्त किसी अदीब या शाइर के जनाज़े में न इतना बड़ा मज्मा देखा था, न ज़नाज़े के साथ इस तरह सड़क पर लोगों को आँसू बहाते देखा था।” आज का वक़्त ऐसा है कि शहर की रातों में नाशाद और नाकारा फिरने पर मजबूर किए गए मजाज़ की शायरी में हिस्सा लेने तो बहुत से लोग आते हैं मगर उन्हें अपनाता कोई नहीं है। न तब अपनाया था न अब अपनाते हैं और तो और जिस यूनिवर्सिटी को उसका तराना मजाज़ ने दिया वो तक उनसे दूरी इख़्तियार किए हुए है।
सिब्ते हसन मजाज़ के वालिद को लिखे खत में मजाज़ की शख़्सियत को जुज़ करते हैं— “मजाज़ सरापा मुहब्बत था। किसी की ज़ात को उसने नुक़सान नहीं पहुँचाया, बजुज़ अपने ज़ात के। बहुत हुआ तो मज़ाक उड़ा दिया, फिक़रे कस दिये, दिल की भड़ास निकल गयी। शिराओं की दुर्बलता के बावजूद उसमें धैर्य रखने और जी को मारने की ताक़त भी बहुत ज़्यादा थी।”
अली सरदार जाफ़री के ये अल्फ़ाज़ मजाज़ से उनकी मुहब्बत और सही मायने में मजाज़ की ख़िराज-ए-अक़ीदत दर्शाते हैं— “मजाज़ मेरे सामने है, उसके फ़िकरे तीरों की तरह बरस रहे हैं, उसकी हलकी-सी मासूम मुस्कराहट और बेपनाह ख़ुलूस और दोस्ती मुझे घेरे हुए है। बाईस साल की सैकड़ों रातें और सैकड़ों दिन हर तरफ़ से हुजूम कर रहे हैं, रातों के दिल में टूटे हुए पैमाने और छलकी हुई शराब है, दोनों के होंठ प्यास से सूखे हुए हैं, मायूसियाँ और मजबूरियाँ नौजवानी के अज़ायम पर हँस रही हैं, मगर नौजवानी की तरंग सबको रौंदती हुई आगे बढ़ रही है। मंसूबे बन रहे, किताबें छप रही हैं, रिसाले निकल रहे हैं, कांफ्रेंसों और मुशायरों पर धावे बोले जा रहे हैं। कभी मजाज़ नज़्म सुना रहा है और उसके तरन्नुम के जादू से बच्चे अपना खेल भूल गए हैं, कभी उसकी आवाज़ रेशम के डोरे की तरह टूटी जा रही है। कलकत्ते की शाम है और मजाज़ रो रहा है। बंबई की एक शाम है और मजाज़ नाच रहा है। लखनऊ की बरसात का अँधेरा है और मजाज़ भीगता हुआ चला जा रहा है। कोई सियासी जलसा है और मजाज़ बेइंतहा संजीदा है। कोई मुशायरा या अदबी जलसा है और मजाज़ बहका जा रहा है। रेडियो पर उसका नाम पुकारा गया है और वह सिर्फ़ हँस रहा है। वह अपने हज़ारों रंग-रूप में मेरे सामने है। वह शमशीर, जाम और साज़ का इम्तजाज था। कभी शमशीर बरहना हो जाती थी तो साँस और जाम भी काँप जाते थे, कभी जाम छलक उठता था, तो शमशीर भी डूब जाती थी। और आज की रात, 5 दिसंबर 1955 की रात जो हज़ारों रातों की आख़िरी रात है, मजाज़ ख़ुद डूबा हुआ है। मौत की गहरी नदी में शमशीऱ, साज़ और जाम तैर रहे हैं, और मजाज़ डूबा हुआ है, हमेशा के लिए ख़ामोश। अब वह कभी नहीं बहकेगा। मौत उसे कितने दिन से बुला रही थी, कहीं दूर आसमानों से आवाज़ दे रही थी, और वह भी कितने दिन से मौत की तरफ़ बढ़ रहा था—
ज़ईफ़ी महफ़िले इशरत में ख़िरकापोश आती है,
जवानी जब भी आती है कफ़न-बर-दोश आती है।
यह लेख अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दो युवा अध्येताओं— विष्णु प्रभाकर (डॉक्टोरल कैंडिडेट, हिन्दी विभाग) और भावुक (डॉक्टोरल कैंडिडेट, इतिहास विभाग) ने लिखा है।




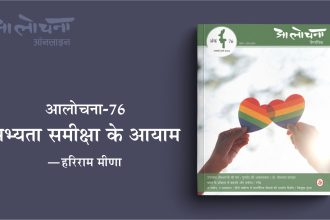

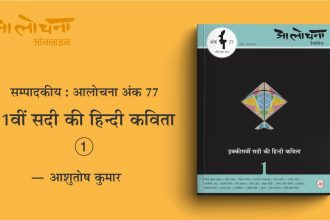
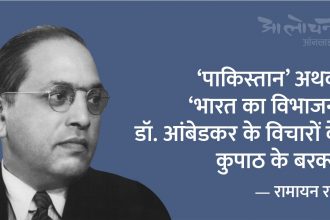

बहोत ख़ूब, विष्णु और भावुक… पढ़कर मज़ा आ गया।
उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के लेख पढ़ने को मिलेगा।
शुभकामनाएं..
मज़ाज को सम्पूर्णता में समझने का प्रयास यह आलेख करता है।
दोनों युवा अध्येता को बहुत बहुत बधाई।