चारु सिंह के आलेख के एक हिस्से पर प्रो. रमण सिन्हा के जवाब को ससम्मान हमने 12 जुलाई (अद्यतनीकृत 14 जुलाई) को इस पोर्टल पर लगाया था। चूँकि उनका जवाबी लेख मुख्यतः चारु सिंह के तर्कों पर केंद्रित था, बतौर सम्पादक मुझे चारु सिंह तक उस जवाब को पहुँचाने से ज़्यादा कोई भूमिका नहीं निभानी थी। लेकिन इस बीच फ़ेसबुक पर सक्रिय एकाधिक शोधार्थियों ने किंचित बाध्यकारी तरीक़े से इस ओर ध्यान दिलाया कि प्रो. रमण सिन्हा ने आख़िरी पैराग्राफ में सम्पादक के दायित्व की बात की है और मुझे उस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। ज़ाहिर है, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि उनके जवाबी लेख की मुख्य आपत्तियों पर प्रत्युत्तर पहले प्रकाशित हो और मुझ पर की गयी टिप्पणी के संबंध में स्पष्टीकरण उसके बाद आए, लेकिन अब लगता है कि मुझ पर की गयी टिप्पणी उतने भी गौण महत्त्व की नहीं है। लिहाज़ा, प्रस्तुत है सम्पादक का ‘पक्ष’:
प्रो. सिन्हा ने लिखा है―
सम्पादक को यह तो अधिकार है कि वह अपनी पत्रिका में क्या छापे और क्या न छापे, उसे पक्ष भी चुनने का अधिकार है लेकिन क्या उसे यह अधिकार है कि जब वह पक्ष चुन रहा है तब प्रतिपक्ष को बगैर सुने, बगैर पढ़े, बिना जाने अपने सम्पादकीय में एक पक्ष विशेष के लेख की संस्तुति करे?
आलोचना के सम्पादक श्री संजीव कुमार, डॉ. चारू सिंह के लेख और उनके मतों को ब्रह्मवाक्य मानकर उद्धृत करते हैं और सम्पादकीय में लिखते हैं—
“1882 ई. में छपी ‘एक अज्ञात हिन्दू औरत’ की पुस्तक सीमंतनी उपदेश से हिन्दी की समकालीन दुनिया का परिचय डॉ. धर्मवीर ने कराया जिनके सम्पादन में मूल संस्करण के आधार पर इसका दूसरा संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ था। इस क्रांतिकारी पाठ को हाथों-हाथ लिया गया, लेकिन वह अज्ञात हिन्दू औरत हिन्दी की दुनिया में शोधार्थी चारु सिंह के लेख ‘अज्ञात हिन्दू स्त्री कैसे बनती है? (आलोचना, अप्रेल-जून 2016) के प्रकाशन से पहले प्राय: अज्ञात ही रही। कुछ साधार और कुछ निराधार अनुमान लगाने के प्रयास चलते रहे। मसलन, स्वयं डॉ. धर्मवीर ने दो अलग-अलग तरह के अनुमान लगाए, पर उनके पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाए। वीर भारत तलवार रस्साकशी में यहाँ तक तो आते हैं कि लाहौर की कई ख़ूबसूरत इमारतों के वास्तुकार कन्हैया लाल की बाल-विधवा बेटी हरदेई, जिसने ‘इंग्लैण्ड में पढ़ने आए इलाहाबाद-लखनऊ के भावी बैरिस्टर रोशनलाल से प्रेम-विवाह किया था और विवाह के बाद अज्ञात हिन्दू औरत होने की वैचारिक दृष्टि से प्रबल संभावना है, लेकिन यह मानकर इस अनुमान को आगे नहीं ले जाते कि 1882 में ऐसी किताब लिखने के लिहाज से हरदेई की उम्र बहुत कम रही होगी’। अंतत: अपने शोध के आधार पर चारु सिंह को ही ‘अज्ञात हिन्दू औरत’ की हरदेवी के रूप में पहचान करने और उनके बौद्धिक एवं सामाजिक कार्यों को व्यवस्थित रूप में आलेखबद्ध करने का श्रेय जाता है।” (आलोचना अंक-78, पृष्ठ VIII-IX)
कमाल है कि इस सम्पादकीय में उन लोगों का जिक्र तो किया गया है जिन्होंने अनुमान किया, कयास लगाए पर ‘जो सबूत नहीं दे पाए’, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं जिसने सबूत पेश किया और जिसका स्वागत व्यापक हिन्दी समाज ने किया, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? या तो उन्होंने मेरा लेख—अंगरेजी या हिन्दी, किसी भाषा में—नहीं पढ़ा या पढ़कर भी अनदेखी करने की कोशिश की, दोनों ही स्थितियों में पाठक उनसे आज नहीं तो कल जरूर पूछेंगे कि क्या सम्पादक का यही धर्म होता है?
यह अच्छी बात है कि प्रो. रमण सिन्हा ने मेरे सम्पादकीय का अंश भी उद्धृत कर दिया है। उसे पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि यहाँ ‘अज्ञात हिन्दू औरत’ की हरदेवी के रूप में सर्वप्रथम पहचान करने का श्रेय चारु सिंह को दिया गया है। बाद के उद्विकासों का इसमें, उचित ही, उल्लेख नहीं है। जब सम्पादक 2016 के चारु सिंह के लेख से पहले ‘अज्ञात हिन्दू औरत’ के अज्ञात ही रहने की बात कर रहा है–और इस चर्चा का सन्दर्भ यह है कि जिस शोधार्थी के प्रयास से वह हिन्दू स्त्री अज्ञात नहीं रही, उसका आलेख इस अंक में शाया हुआ है–तो सम्पादक को और चीज़ों की चर्चा क्यों करनी चाहिए?
प्रो. सिन्हा का कहना है कि मैंने उनके तद्भव वाले आलेख का संज्ञान क्यों नहीं लिया? कारण स्पष्ट है। यह 2023 का आलेख है, जबकि मैं उस काम का ज़िक्र कर रहा था जो उक्त शोधार्थी 2016 और 2020 में ‘आलोचना’ पत्रिका के माध्यम से कर चुकी थी। पहले किसने किया, यह बात जब आएगी तो बाद के प्रकाशन वर्ष वाली चीज़ों का हवाला सम्पादक क्यों देगा?
अब जहाँ तक इसका सवाल है कि चारु सिंह के 2016 वाले लेख को सीमंतनी उपदेश की लेखिका के रूप में हरदेवी की पहचान करने का श्रेय दिया जाए या नहीं, तो यह श्रेय स्वयं प्रो. रमण सिन्हा 2019 में उन्हें दे चुके हैं। उसी वर्ष चंद्रावती लखनपाल की किताब ‘मदर इंडिया का जवाब’ रमण जी की भूमिका के साथ अनन्य प्रकाशन से प्रकाशित हुई। इसकी भूमिका में उन्होंने हरदेवी के बारे में लिखा, “लंदन यात्रा (1888) और लंदन जुबली (1889) जैसे यात्रा-संस्मरण, हुक्मदेवी (1892) शीर्षक उपन्यास, कुछ कविताएँ, लेख और सीमंतनी उपदेश जैसी पुस्तक की तेजस्वी रचनाकार ने भारत भगिनी (1889-1906) पत्रिका के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का जैसा काम किया, वह हिन्दी क्षेत्र के लिए अनन्य ही कहा जाएगा।” इसमें सीमंतनी उपदेश पर सुपरस्क्रिप्ट में 7 लगाकर 7 नंबर पाद-टिप्पणी में चारु सिंह के 2016 वाले लेख के विवरण दिये थे। ग़रज़ कि उस समय उनका मानना था कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका के रूप में हरदेवी का नाम इसी लेख के आधार पर लिया जा रहा है। (देखिए, श्रीमती चंद्रावती लखनपाल एम. ए., मदर-इंडिया का जवाब, भूमिका एवं प्रस्तुति : रमण सिन्हा, 2019, अनन्य प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ. 4)।
तो अब बताइए कि अगर मैं भी रमण जी की 2019 वाली बात को मानता हूँ तो क्या ग़लत करता हूँ? पहली बार किसने यह खोज की, इस तथ्य को बदलना होगा तो 2016 से पीछे जाना होगा, न कि आगे। मतलब यह कि 2016 से पहले का कोई आलेख हरदेवी की इस भूमिका की पहचान करता मिल जाए तो निश्चित रूप से हमें चारु सिंह के लेख को श्रेय देना बंद करना होगा, पर 2023 का कोई लेख यह काम करे तो चारु सिंह को श्रेय मिलना किस तर्क से बंद किया जाए?
समस्या यह है कि अपने प्रतिवाद में रमण जी यह कहते हैं कि चारु सिंह ने अपने पुराने आलेख में अज्ञात हिंदू स्त्री के हरदेवी होने का केवल अनुमान लगाया है, इसे प्रमाणित नहीं किया है। लेकिन 2019 की उपरोक्त भूमिका में उन्होंने स्वयं उनके कार्य को प्रमाण की तरह उद्धृत किया है ! ठीक यही बात चारु सिंह ने अपने ताज़ा आलेख में कही भी है। अब पाठक स्वयं सोचें कि रमण जी का यह प्रतिवाद चारु सिंह के दावे का खंडन किस तरह करता है।
2016 : आलोचना 58 में चारु सिंह का आलेख ‘‘अज्ञात’ हिन्दू स्त्री कैसे बनती है?’
2019 : चंद्रावती लखनपाल की किताब मदर-इंडिया का जवाब की रमण सिन्हा लिखित भूमिका
2023 : तद्भव 47 में रमण सिन्हा का आलेख ‘हरदेवी : उन्नीसवीं सदी की एक विस्मृत नायिका’
सम्पादक को उसका दायित्व बताने वाले हर दूसरे दिन उससे टकराते हैं। पर ऐसा बताने वालों को अपने सुझावों का भी समुचित संपादन करना आना चाहिए। रमण जी की बात मानें तो “सम्पादक को यह…अधिकार है कि वह अपनी पत्रिका में क्या छापे और क्या न छापे”; लेकिन मैं इस अधिकार के दुरुपयोग का पक्षधर नहीं हूँ। मेरी समझ तो यह है कि नहीं छापने का तर्क छापने के तर्क जितना ही संतुलित और स्पष्ट होना ज़रूरी है। सम्पादक लेखक का पक्ष नहीं चुनता, सामने जो प्रकाशन के लिए आयी हुई सामग्री होती है, उसका पक्ष चुनता है। जब तर्क और तथ्य अपनी बात साफ़ बोल रहे थे तो और किसकी सुनते? रमण जी ने कैसे समझ लिया कि “प्रतिपक्ष को…बगैर पढ़े, बिना जाने अपने सम्पादकीय में एक पक्ष विशेष के लेख की संस्तुति” की गयी?
प्रो. रमण सिन्हा अच्छे अध्येता हैं। न होते तो हमने आलोचना में उन्हें बार-बार छापा न होता। दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका यह जवाबी लेख ख़ासा कमज़ोर निकला। इसके अनेक अंतर्विरोध तो, हरदेवी का विशेषज्ञ न होने के बावजूद, मुझे स्पष्ट दिख रहे हैं। लेकिन उन्हें सामने लाना उस शोधार्थी का काम है जिसको लेख का बड़ा हिस्सा संबोधित है।


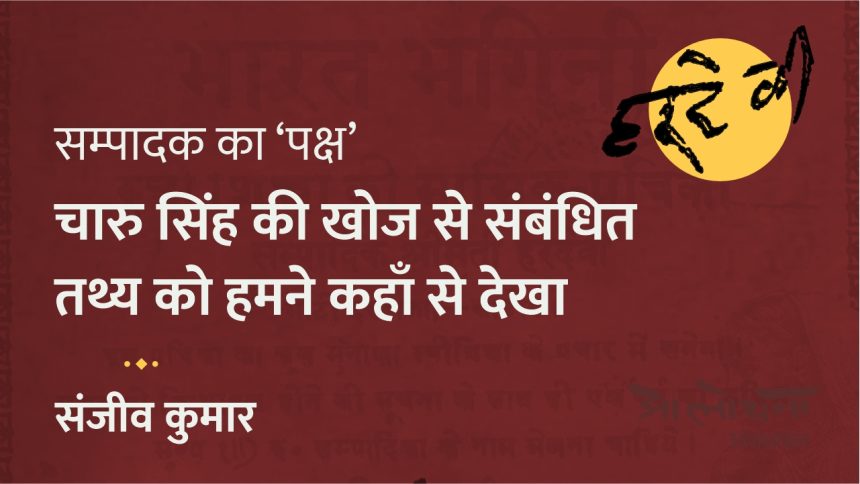
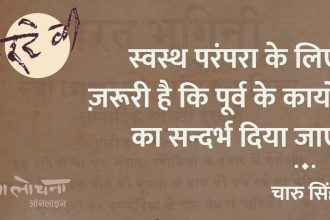

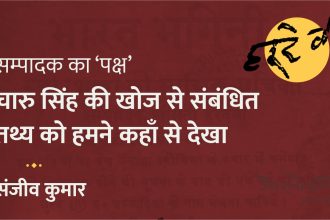

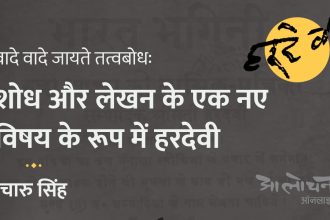

कहाँ से देखा ?
संपादक प्रायः दो तरह के होते हैं —-एक जो अपनी संपादकीय चूक और भूल को स्वीकार करते हैं और इस प्रक्रिया में परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं और दूसरे प्रकार के संपादक वे होते हैं जो अपनी भूल को स्वीकार करने के बजाय,सत्य से आँखें मिलाए बगैर दाएं बाएं करते हुए अपनी गलतियों को अंतिम सांस तक सही ठहराने की कोशिश करते हैं और परिणामतः निरंतर अप्रामाणिक होते चले जाते हैं । आलोचना संपादक श्री संजीव कुमार दूसरी श्रेणी में आते हैं ।
संपादक महोदय ने अपनी सफाई में कहा है:“ प्रो. सिन्हा का कहना है कि मैंने उनके तद्भव वाले आलेख का संज्ञान क्यों नहीं लिया? कारण स्पष्ट है। यह 2023 का आलेख है, जबकि मैं उस काम का जिक्र कर रहा था जो उक्त शोधार्थी 2016 और 2020 में ‘आलोचना’ पत्रिका के माध्यम से कर चुकी थी। पहले किसने किया, यह बात जब आएगी तो बाद के प्रकाशन वर्ष वाली चीज़ों का हवाला सम्पादक क्यों देगा?” मेरा कहना है कि वह इसलिए देगा क्योंकि वह यह बात जून 2025 में कर रहा है और वह लेखिका के 2016 और 2020 के कामों का नहीं बल्कि उसके एक नए लेख को प्रस्तुत करते हुए, उसका समग्र मूल्यांकन करते हुए इस प्रकार का निर्णय सुना रहा है : “अंतत: अपने शोध के आधार पर चारु सिंह को ही ‘अज्ञात हिन्दू औरत’ की हरदेवी के रूप में पहचान करने और उनके बौद्धिक एवं सामाजिक कार्यों को व्यवस्थित रूप में आलेखबद्ध करने का श्रेय जाता है।” इसी को कहते हैं सत्य से आँखें चुराकर दाएं-बाएं करना ।
जहां तक सीमंतनी उपदेश की लेखिका के रूप में हरदेवी की पहचान का सवाल है, वह मैंने अपने पिछले प्रतिवाद में स्पष्ट कर दिया था कि मुझसे पहले किसी के पास प्रमाण नहीं थे, मेरे पास भी 2022 के पहले नहीं थे इसलिए 2019 में चंद्रावती लखनपाल की पुस्तकों की भूमिका में पाठकों को मैंने चारु सिंह के ‘अनुमान’ को जानने के लिए उनके लेख का विवरण दिया था ,मैंने कहीं भी उसमें सीमंतनी उपदेश की लेखिका के रूप में हरदेवी की पहचान प्रमाणित करने का श्रेय चारु सिंह को नहीं दिया है. इसलिए संपादक महोदय का यह कहना भ्रामक है कि “ 2019 की उपरोक्त भूमिका में उन्होंने स्वयं उनके कार्य को प्रमाण की तरह उद्धृत किया है !” यह गलतबयानी है, जो फिर उनके एक पक्ष विशेष के साथ गठजोड़ की ओर संकेत करती है ।
इस समूचे प्रसंग में संपादक की भूमिका संदिग्ध इसलिए भी जान पड़ती है क्योंकि आरंभ से ही वे एक पक्ष के समर्थक और पक्षधर के रूप में सामने आते हैं, देखिए यह ज्ञापन :”चारु सिंह ने ‘आलोचना’ अंक-78 में प्रकाशित अपने लंबे शोध आलेख के इस हिस्से में हरदेवी संबंधी अपने काम को बिना श्रेय दिये हथियाए जाने के जो विवरण दिए हैं, उन पर हिन्दी संसार को तत्काल ग़ौर करने की ज़रूरत है।” न्यायमूर्ति संजीव कुमार प्रतिवादी को सुने बगैर यह जो अभूतपूर्व फैसला सुनाते हैं और तत्काल इसे सोशल मीडिया और आलोचना ऑनलाइन पर साझा करते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ? पाठक जानते हैं कि आलोचना पत्रिका के इतिहास में ऐसी तत्परता अब तक कभी किसी लेख के लिए नहीं देखी गई, क्या यह उनकी संपादकीय निष्पक्षता का प्रमाण है?
“अनुमान –अगर वह तर्क/न्याय के नियमों के अनुसार हो–प्रमाण ही माना गया है। सिर्फ़ प्रत्यक्ष को प्रमाण तो एकमात्र चार्वाक के यहाँ माना गया है।” – संजीव
सर, लगता है संजीव जी पर एयूडी, देशिक की संगोष्ठी का खासा प्रभाव पड़ा है, मार्क्सवादी शोध पद्धति और वैचारिकी में प्रत्यक्ष और द्वन्द्व पर जो जोर है, उसे छोड़कर अब वह अनुमान पर भरोसा करने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस और कंक्लुजन में उन्हें अब बस हाइपोथेसिस भर से मतलब लगता दिख रहा है। कंक्लुजन पर पहुंचने के लिए जो शोध प्रविधि अपनाई जाती है, बस वही किसी काम की नहीं। लगता है अभिमन्यु की तरह संजीव जी भी शोध प्रविधि वाला अन्तिम व्याख्यान सुनने के ऐन पहले सो गये थे। मार्च, 2023 में देशिक की संगोष्ठी में 2013 में शिमला में हुई कॉन्फ्रेंस में दिए गए अपने वक्तव्य पर अफसोस जताते हुए जैसे उसका ठीकरा संजीव जी ने अभय जी पर फोड़ा था, उम्मीद करती हूं कि आगे आने वाली किसी अन्य संगोष्ठी में वे ऐसे ही अपने इस हालिया ज्ञानोदय का ठीकरा किसी अन्य के माथे पर फोड़ेंगे।
माफ़ कीजिएगा, अनुमान नामक प्रमाण के विषय में आपकी जानकारी अधूरी है। ‘सभी कौवे काले होते हैं’ – यह अनुमान का ही उदाहरण है।
माफ करिए महोदय, मेरी जानकारी अनुमान के बारे में भी अधूरी है और मार्क्सवाद तो मैं जानती नहीं ! लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे न्याय दर्शन आदि का आधार लेकर पश्चिमी तरीके की शोध पद्धति विशेष कर मार्क्सवादी, को कैसे विकसित कर रहे हैं आप ? यह जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। इस तरह की किसी सैद्धांतिकी का विकास आलोचना के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान होगा जो आप जैसा महारथी ही कर सकता है। लेकिन कम से कम हम अज्ञानियों को भी इसके बारे में कुछ जानने का मौका दें ! क्या आप द्वारा प्रस्तावित इस नई सैद्धांतिकी में शोध में शोध पद्धति की जगह अनुमान आधारित निष्कर्ष निकाले जाएंगे? यह वास्तव में बड़ा रोचक है, कृपया बताएं।
माफ़ कीजिएगा, आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि आप कितनी बेसिरपैर की बातें कर रही हैं। ज्ञान-मीमांसा (इपिस्टमालजी) के मामले में भारतीय और अभारतीय का विरोधी द्विचर जिस तरह आप खड़ा कर रही हैं, वैसा किसी और विद्वान ने शायद ही खड़ा किया हो! लिहाज़ा, उसका कोई निदान ढूँढ़ने का दुस्साहस नहीं करूँगा।
अलबत्ता, बेपर की उड़ाने वाली इस हिकमत के सामने बस ‘देशिक’ वाले अपने लिखित व्याख्यान का एक अंश रखना चाहता हूँ, जिससे पाठकों को पता चले कि आप शिमला वाले मेरे व्याख्यान के बारे में मेरी ही बाद की राय को कैसे मिसकोट कर रही हैं। मेरे व्याख्यान का अंश है:
“मार्क्सवादियों की उस बहस को इस प्रसंग में दुबारा याद करते हुए मैं यह स्वीकार करूँ कि शिमला के व्याख्यान में मैंने हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना में ठीक-ठीक जिस तरह दो लाइनों का संघर्ष देखा था, वह बहुत दुरुस्त नहीं था। अव्वल तो वहाँ सभी मसलों पर दो लाइनों की टकराहट देखते हुए उनका प्रतिनिधित्व करनेवालों को संसक्त/कोहेसिव समूहों के रूप में देखा गया था, जो कि ग़लत था। दूसरे, वहाँ मतभेद रखनेवालों की अपनी-अपनी शक्तियों और सीमाओं को देखने के बजाए सफेद-स्याह तरीक़े से यह साबित करने का उत्साह ज़्यादा था कि अल्पमत में जानेवाले आलोचक-विचारक, जिन्हें चंद्रबली सिंह ने ‘प्रगतिशील आंदोलन के झाड़-झंखाड़’ कहा, अगर झाड़-झंखाड़ थे तो इस अर्थ में कि वे कँटीले और असुविधाजनक थे और प्रदत्त संस्कारों के साथ प्रगति के विचार का तालमेल बिठाने में बाधक। यह बात चुनिंदा विचारों के बारे में सही हो सकती है, विचारकों के बारे में नहीं। जैसे ही आप विचारकों को आगे करते हैं, आपकी जवाबदेही बनती है कि अपने हिसाब से उन्हें टुकड़ों में देखने के बजाए पूरा-पूरा देखें जो कि मैंने नहीं देखा, न सिर्फ़ अपने वक्तव्य में बल्कि उस वक्तव्य की तैयारी के दौरान भी। देखा होता तो मुझे पता होता कि नायक की ट्रैजिक शहादत वाले जिस नैरेटिव स्ट्रक्चर में मैं फँस रहा हूँ (शिवदान सिंह चौहान का बहिर्गमन, रांगेय राघव की घोर उपेक्षा आदि), उसमें गहरी फाँकें हैं।
“इसके बावजूद, अपने इस निचोड़ से मुझे कोई असंतोष नहीं है कि रामविलास शर्मा से मामूली असहमतियाँ रखते हुए भी लंबे समय तक हिंदी की प्रगतिशील-जनवादी धारा का बड़ा हिस्सा ज़्यादातर मसलों पर उनका अनुयायी रहा है और इसका कारण है उनका वह आख्यान जो अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपने राष्ट्र के प्रति गौरव-भावना को जगाने/सहलाने में सक्षम है तथा क्रांतिकारी शब्दावली के बावजूद ढेर सारे सामाजिक-नैतिक सवालों पर एक राष्ट्रवादी-सवर्ण-हिन्दू-पुरुष मन के लिए ज़्यादा असुविधाजनक नहीं है। उस आख्यान के अलग-अलग पक्षों को जो भी वैचारिक चुनौतियाँ मिलीं, उन्हें दोहराने, सराहने या विकसित करनेवाले आलोचक मार्क्सवादियों के बीच प्रायः अल्पमत में रहे।”
शोधप्रज्ञ भी दो तरह के होते हैं : एक, जो अपनी भूल चूक स्वीकार करते हैं और आगे सुधार करते हैं। दूसरे, जो सप्रमाण कही गई बात को भी नकार कर अपनी भूल पर कायम रहते हैं। आप इस दूसरी श्रेणी में बने रहना चाहते हैं तो ख़ुशी से रहिए! लोग तर्कसम्मत पक्ष खुद चुन लेंगे।
रही बात आलोचना की तत्परता की, तो यह आरोप लगानेवाले बताएं कि ‘आलोचना’ के इतिहास में आलोचना ऑनलाइन जैसी चीज कभी थी क्या? कितनी हास्यास्पद बात है!
हाँ, आलोचना (यहाँ पत्रिका की बात नहीं हो रही) के इतिहास में यह ढूँढ़ना थोड़ा मुश्किल है कि एक आलोचक किसी को ग्रंथ के रचनाकार के रूप में उल्लिखित करे, उसके लिए सन्दर्भ भी दे, और बाद में यह कहे कि उस समय जानकारी प्रामाणिक नहीं थी। बिना प्रामाणिक जानकारी के आप ऐसा उल्लेख कर जाते हैं, यह बता कर आपने आगे के लिए सावधान कर दिया। शुक्रिया!
प्रमाण बनाम अनुमान का जो द्विचर आप शुरू से प्रयोग करते आये हैं, वह भी अद्भुत है। पूरा भारतीय न्याय दर्शन प्रमाण के तीन भेदों पर कायम है: प्रत्यक्ष, अनुमान, और शब्द प्रमाण। अनुमान–अगर वह तर्क/न्याय के नियमों के अनुसार हो–प्रमाण ही माना गया है। सिर्फ़ प्रत्यक्ष को प्रमाण तो एकमात्र चार्वाक के यहाँ माना गया है।
खैर, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। चारु सिंह का प्रत्युत्तर बहुत सारे जाले साफ़ कर देगा।
पाठक को समझते देर नहीं लगेगी कि बात जब से आलोचना ऑन लाइन हुई है,तभी की हो रही थी और यह हास्यास्पद है कि संपादक महोदय इसे नहीं समझ पा रहे हैं ! यह आपने नहीं बताया कि किस ग्रंथ या रचनाकार का मैंने उल्लेख किया,संदर्भ दिया और ‘बाद में कहा कि उस समय जानकारी प्रामाणिक नहीं थी’ ऐसा कहते हुए मुझे आपने आगे के लिए सावधान कर दिया कि कोई मेरे सामने ही चारु सिंह की तरह मेरे कहे को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता है ,मेरा आग्रह है कि मैंने जो कहा है उसे दुबारा पढ़ने का कष्ट कीजिए,
न्याय दर्शन में प्रमाण के तीन नहीं चार भेद माने गए हैं :प्रत्यक्ष,उपमान,अनुमान और शब्द .गौतम के अनुसार शब्द प्रमाण आप्तोपदेश होता है, और मैंने सीमांतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी हैं,वह गौतम के अनुसार दृष्टार्थ शब्द-प्रमाण का उदाहरण माना जाएगा । यह अद्भुत है कि आप एक ओर संपादकीय में ‘सबूत’ का मापदंड लाते हैं और दूसरी ओर अनुमान को भी प्रमाण मानने का आग्रह करते हैं !
अब यह भी बताने की जरूरत है कि मैं ‘सीमंतनी उपदेश’ ग्रंथ और हरदेवी रचनाकार की बात कर रहा हूँ जिनका उल्लेख आपने अपनी उक्त भूमिका में बिना किसी किन्तु परन्तु के किया था। हद है!
कहां से देखा? में मैंने स्पष्ट कर दिया है,फिर से पढ़िए।