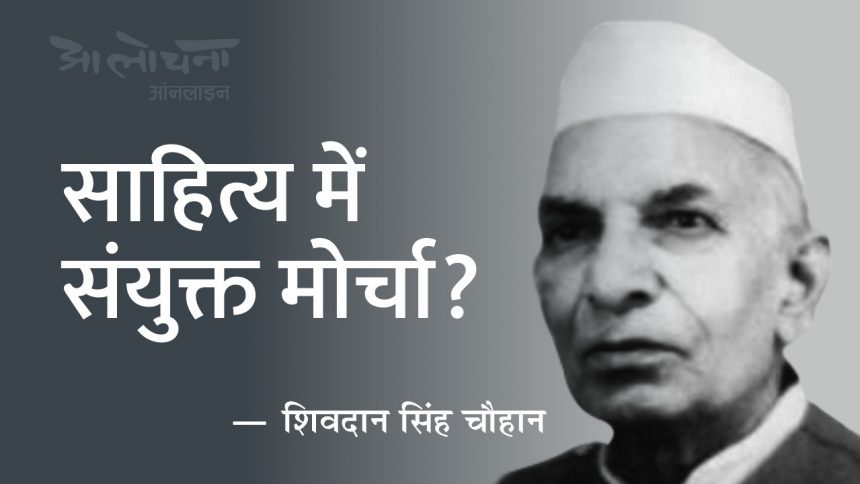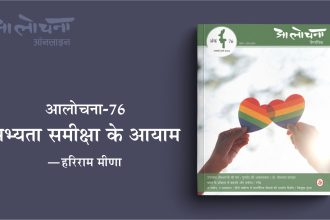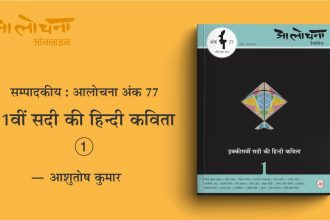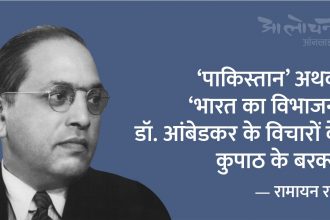सहयोगी ‘हंस’, ‘नया साहित्य’, ‘नई चेतना’ और कई दूसरी पत्र-पत्रिकाओं में इधर कुछ महीनों से ‘साहित्य में संयुक्त मोर्चा’ बनाने के प्रश्न पर बहस चल रही है। अनेक लेखको ने, जो प्रगतिशील लेखक संघ से सम्बद्ध हैं या जो संकीर्ण मतवादियों का दौर-दौरा होने से पहले उसमें थे, इस बहस में भाग लिया है। प्रस्तावित संयुक्त मोर्चे का क्या आधार हो, क्या उद्देश्य हो, क्या कार्यक्रम हो और कौन उसका नेतृत्व करे— इन सब प्रश्नों पर प्रत्येक लेखक ने अपनी-अपनी सूझ-बूझ के अनुसार सविस्तार सुझाव दिये हैं। वस्तुत: प्रत्येक लेखक ने कुछ हेर-फेर करके एक-सी बातें ही दुहराई हैं, या कहें कि मूलत: सबकी तर्क-प्रणाली और प्रवृत्ति एक ही पूर्व-निर्धारित विचार-वृत्त के भीतर आँख पर पट्टी बाँधकर चक्कर काटते रहने की रही है। अपने देश की विशिष्ट परिस्थितियों का विश्लेषण करके वर्तमान गतिरोध को तोड़ने और आगे बढ़ने के लिए एक सही नीति और कार्यक्रम बनाने का काम जिस वस्तुनिष्ठ चिन्तन और रचनात्मक प्रयत्न की माँग करता है, उसका इस बहस में बहुत बड़ी सीमा तक अभाव रहा है। इस बहस का अभी तक अन्त नहीं दिखाई देता, यद्यपि न ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ का गतिरोध टूट रहा है, न हम विशेष आगे ही बढ़ पाये हैं। हाँ, एक गोल परिधि के भीतर चक्कर काटते जाने से गति का भ्रम अवश्य पैदा हो गया है।
इस बहस का सूत्रपात एक विचित्र ढंग से हुआ। कई वर्षों से ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ में ‘कुत्सित समाज-शास्त्रियों’ का बोल बाला रहा है। इस अमार्क्सीय, जन-विरोधी प्रवृत्ति की “विनाशकारी आलोचना लेखकों को अपने अस्त्र डालने पर बाधित करती थी। यह किसी लेखक का सम्पूर्ण कृतित्व न परखकर इधर-उधर से अपनी सुविधा के उद्धरण बटोरकर उसके विरुद्ध ‘केस’ बनाने में दत्तचित थी। और यह उद्धरण तोड़े-मरोड़े जाते थे…” (श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, नया साहित्य, सितम्बर 1951, पृष्ठ 75)। कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन मंत्री बी० टी० रणदिवे की अवसरवादी नीति का परदाफाश होते ही, साहित्य क्षेत्र के संकीर्ण-मतवादियों के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई। सौभाग्य से उन्हीं दिनों ‘अखिल चीन लेखक और कलाकार संघ’ के अधिवेशन में सभापति पद से दिया गया प्रसिद्ध चीनी लेखक और नेता कुओ० मो० जो का वह भाषण, जिसमें उन्होंने तीस वर्ष से चले आने वाले चीन के लेखकों और कलाकारों के विशाल संयुक्त माेर्च को और अधिक व्यापक आधार पर संगठित करके विशालतर बनाने की माँग की थी, हमारे इन अवसरवादियों के हाथ लग गया—जैसे अन्धे के हाथ बटेर लग गई हो। ‘भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ’ की प्रारम्भिक जनवादी परम्पराओं, जन-सेवा और साहित्य-निर्माण के उच्चादर्शों का लगातार कृतघ्नतापूर्वक तिरस्कार करते आने वाले ये दोस्त एकाएक चोला बदलकर ‘संयुक्त मोर्चावादी’ बन गए, और उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में चीन और भारत के परिस्थिति भेद का विश्लेषण करने या स्वयं अपनी गलतियों की ईमानदारी से जाँच-परख करने की जरूरत नहीं समझी। एक सच्चे अवसरवादी की तरह, जो हवा का रुख बदलते ही अपना रुख भी बदल देता है, उन्होंने अपने कृतित्व के स्मारक भारत के जनवादी लेखकों की एकता के खंडहर पर खड़े होकर ‘साहित्य में संयुक्त मोर्चे’ की पताका फहरा दी। यदि वह भाषण उनके हाथ न लगा होता तो अपने दयनीय अस्तित्व की रक्षा के लिए वह और कौन-सा प्रपंच न रचते, यह नहीं कहा जा सकता।
कुओ० मो० जो के अनुसार जो व्यापक संयुक्त मोर्चा तीस वर्ष के संयुक्त कार्य और सम्मिलित संघर्ष और उससे उत्पन्न चीनी लेखकों की पारस्परिक सद्भावना और एकता का स्वाभाविक परिणाम होना था, उसे रामविलास शर्मा ने तीन-चार वर्षों तक नियमित रूप से प्रगतिशील लेखक आन्दोलन की नहीं पर कुठार चलाने और देश की साहित्यिक शक्तियों में फूट और वैमनस्य की चौड़ी खाई खोदने के बाद हठात् एक अनिवार्य आरम्भ-बिन्दु के रूप में पेश कर दिया और इस प्रकार अपनी और अपने कुत्सित समाज-शास्त्रीय जन-द्रोही गुट की संस्कृति-विरोधी करतूतों पर परदा डालने की चेष्टा की। उनकी इस अवसरवादी कलाबाजी पर ध्यान न देकर भी यदि हिन्दी के कुछ लेखकों ने इस विचार का स्वागत किया है और अधिकांश लेखक परस्पर के आदान-प्रदान, विचार-विनिमय और सक्रिय सहयोग के लिए उत्सुक हैं, और उसके सूत्र काट दिये जाने पर विक्षुब्ध रहे हैं, तो यह उनके उत्कट देश-प्रेम, मुक्ति-भावना और मूलत: प्रगतिशील दृष्टिकोण का ही प्रमाण है। इसका श्रेय संकीर्ण मतवादियों की अवसरवादी कलाबाजी को नहीं दिया जा सकता। और न इससे यह सिद्ध होता है कि तुरन्त ‘साहित्य में संयुक्त मोर्चा’ बना लेने का नारा और उस पर चलाई जाने वाली बहस ही परिस्थिति के आग्रह से उत्पन्न है और उसका औचित्य है। कुत्सित समाज-शास्त्रियों को यदि किसी बात का श्रेय दिया जा सकता है तो केवल इसका कि वह इस बहस की संकीर्ण सीमाएँ निर्धारित करने में सफल हुए हैं।
वस्तुत: यह बहस अनेक ‘कुत्सित समाज-शास्त्रियों’ के साहित्यिक अस्तित्व का एक मात्र सहारा और बहाना बन गई है। ‘संयुक्त मोर्चे’ का उच्च स्वर से मंत्रोच्चार करके आज भी वह आलोचना और रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उसी संकीर्ण मतवादी समझ या नासमझी का परिचय देते जाते हैं, जिसने साहित्य-जगत् में इतनी भयंकर फूट डाली थी। इसलिए यह बहस भारतीय जनता के प्रति अपने साहित्यिक कर्तव्यों से जी चुराने और मूल प्रश्नों को टालने का साधन बनती जा रही है।
‘साहित्य में संयुक्त मोर्चा’ पुस्तक में श्री अमृतराय ने बड़ी ईमानदारी और सूझ-बूझ से पिछले दौर की त्रुटियों की आलोचना की है, लेकिन अपने विवेचन के तर्क-संगत परिणामों को वे भी स्वीकार नहीं कर पाये और ‘साहित्य में संयुक्त मोर्चे’ को, जो संगठन क्षेत्र में हमारा ‘लक्ष्य’ हो सकता है, उन्होंने भी एक प्रकार से आरम्भ-बिन्दु ही मान लिया है। संकीर्णतावादी दौर की तबाहकारियों से उत्पन्न परिस्थिति चाहे जितनी अवांछित हो, है तो वह ठोस वस्तु-स्थिति ही। उसको बिना बदले और अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा किये, दोनों के अन्तराल की कठिन, दुर्गम राह को पार किये ही केवल छलाँग मारकर लक्ष्य तक पहुँच जाने की नीति निश्चय ही संकीर्ण मतवादी नीति का ही बदला हुआ रूप है। यह एक मरीचिका के पीछे दौड़कर गुमराह होना और दूसरों को गुमराह करना है।
मेरा विचार है कि ‘साहित्य में संयुक्त मोर्चा’ केवल कुछ दोस्तों के कृत्रिम उत्साह प्रदर्शन और खयाली पुलाव पकाने से नहीं बनेगा, न वस्तुस्थिति से आँखें मींचकर हथेली पर सरसों जमाने वाली उतावली से ही, और न उस समय तक जब तक कि प्रगतिवादी आन्दोलन से (चाहे वह राजनीतिक हो या साहित्यिक) अमार्क्सीय, संस्कृति-विरोधी कुत्सित समाज-शास्त्रीयता की संकीर्ण मतवादी और अबुद्धिवादी प्रवृत्ति और विचारधारा का पूरी तरह उन्मूलन नहीं कर दिया जाता, और वस्तुस्थिति का सही-सही जायजा लेकर एक ठोस जनवादी कार्य-नीति नहीं बनाई जाती या जब तक मार्क्सवादी लेखक ईमानदारी और सच्ची लगन से जनता के प्रति अपने साहित्यिक दायित्वों को पूरा नहीं करते। इसलिए हमें विचार के स्वनिर्मित बाड़ों में से निकलकर वस्तुस्थिति से आँखें मिलानी चाहिए और भेड़-चाल और तोता-रटन्त छोड़कर जनता की सेवा में रचनात्मक रीति से लग जाना चाहिए।
वस्तुत: प्रगतिशील लेखक आन्दोलन और मार्क्सवादी लेखकों के सम्मुख आज कौन-से प्रश्न हैं, कौन-से कार्य है और वह उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं, इस संबन्ध में मैं यहाँ सहयोगी ‘नई चेतना’ के सम्पादक श्री लक्ष्मीकान्त का वह पत्र जो उन्होंने मेरे निबन्ध ‘मानव-आत्मा के शिल्पियों से’ पढ़कर मुझे लिखा था और उसका जो उत्तर मैंने काश्मीर से 31 जनवरी 1951 को भेजा था, ज्यों-का-त्यों प्रकाशित कर रहा हूँ। इस उत्तर में मैंने जो सुझाव दिये थे वे हमें आज भी एक वस्तुदर्शी की तरह सोचने के लिए विवश करने में सक्षम हैं।
उनका पत्र इस प्रकार था—
बीकानेर, 25 जनवरी 1951
प्रिय साथी चौहान जी,
आपने अपने निबन्ध ‘मानव-आत्मा के शिल्पियों से’ में प्रगतिशील लेखक संघ को पुन: एक व्यापक जनवादी आधार पर संगठित करने के लिए भारत के तमाम लेखकों से अपील की है। ‘नई चेतना’ का सम्पादक-मंडल इस अपील का स्वागत करता है। परन्तु हमें इस सम्बन्ध में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयाँ नजर आती हैं। आपके लेख से भी स्पष्ट है कि ‘संकीर्णतावाद’ से भारत के जनवादी लेखकों की एकता पर कुठाराबात हुआ है, और विशेषकर ‘कुत्सित समाज-शास्त्रीयता के समर्थक साथियों’ के व्यवहार से अनेक प्रतिष्ठित लेखक ‘क्षुब्ध’ हैं और ‘अपमानित’ महसूस करते हैं। लेकिन आपने इस स्थिति की ओर संकेत नहीं किया है कि परिणामत: अधिकांश लेखकों की यह निश्चित धारणा बन गई है कि “प्रगतिशील लेखक संघ: हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का साहित्यिक मोर्चा है और वहाँ मार्क्सवादी लेखक ही सम्मानित होते हैं, चाहे वे अत्यन्त साधारण लेखक ही क्यों न हों; और दूसरे बड़े-से-बड़े लेखकों की बात पर यथोचित ध्यान भी नहीं दिया जाता। पार्टी की जब जो नीति होती है, प्रगतिशील लेखक संघ की नीति भी तब त्यों ही बदल जानी पड़ती है। वस्तुत: प्रगतिशील लेखक संघ साहित्य-निर्माण के प्रश्नों को छोड़कर पार्टी का प्रचार-केन्द्र बन गया है।”
यह धारणा काफ़ी गहरी और व्यापक है, और बिलकुल निराधार भी नहीं है। हम स्वयं चाहते हैं कि यह धारणा निर्मूल हो जाय और प्रगतिशील लेखक संघ सच्चे अर्थों में तमाम जनवादी लेखकों का संयुक्त मोर्चा बन जाय, परन्तु व्यवहारत: क्या यह सम्भव हो सकेगा और कैसे? यदि एक क्षण के लिए मान लें कि ऐसा न हो सके तो उस दशा में क्या करना उचित होगा, और प्रगतिशील लेखक संघ का क्या कार्यक्रम रहना आवश्यक होगा ? सम्भवत: आप हम से सहमत होंगे कि व्यावहारिक दृष्टि से इन सारे प्रश्नों का औचित्य है और इनका स्पष्ट उत्तर भी अत्यन्त जरूरी है।
इसलिए ‘नई चेतना’ का सम्पादक मंडल आपसे इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आग्रही है।
लक्ष्मीकान्त
‘नई चेतना’— सम्पादक-मंडल
इस पत्र का उत्तर मैंने यह दिया था—
प्रिय साथी लक्ष्मीकान्त जी,
श्रीनगर-काश्मीर 31-01-51
‘नई चेतना’ सम्पादक मण्डल की ओर से आपने प्रगतिशील लेखक संघ के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में अनेक संगत प्रश्न उठाये हैं। अपने निबन्ध में इन व्यावहारिक प्रश्नों का समाधान उपस्थित करना मेरा उद्देश्य नहीं था। अपनी अपील के द्वारा एक ऐसा अनुकूल वातावरण पैदा करना ही मुझे अभिप्रेत था जिसमें भारत के तमाम लेखक सद्भावना-पूर्वक एक-साथ बैठकर व्यावहारिक प्रश्नों पर विचार करते और अपने दायित्व की गम्भीरता का अनुभव करके कोई सामान्य कार्यक्रम बनाते। इसी कारण मैंने बुनियादी प्रश्नों तक ही अपने को सीमित रखा और व्यावहारिक प्रश्नों के समाधान की ओर केवल दिशा-संकेत ही किया। अब चूँकि निबन्ध प्रकाशित होने के पूर्व ही आपने कुछ जरूरी प्रश्न उठा दिये हैं, तो यह अच्छा होगा कि लेख के साथ इन प्रश्नों का उत्तर भी प्रकाशित करें।
प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में आपने अन्य लेखकों की जिस ‘धारणा’ का उल्लेख किया है, वह निस्सन्देह निराधार नहीं है और मैं उससे अपरिचित नहीं हूँ। यह बात किसी समय कोरी ‘धारणा’ थी, लेकिन आज अगर प्रगतिशील लेखक संघ की ओर देखें तो यह एक ‘हकीकत’ है। इसलिए अपना निबन्ध लिखते समय मुझे इस वस्तुस्थिति का पूरा अहसास था— पिछले आठ-दस वर्ष से है, जब यह एक ‘धारणा’ का रूप धारण कर रही थी। यही कारण है कि सन् 1942 में जब हमारा देश संकटापन्न था और आसन्न ‘फासिस्ट आक्रमण’ के विरुद्ध भारत के लेखकों को संगठित करने का प्रश्न उठा तो हमने संकीर्णमतवादियों की तरह इस बात का दुराग्रह नहीं किया कि संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए एक व्यापक आधार पर तमाम लेखकों को प्रगतिशील लेखक संघ में ही सम्मिलित हो जाना चाहिए। ऐसा करना गलत होता, क्योंकि अनेक लेखक इसके लिए तैयार न थे, यद्यपि फ़ासिस्ट विरोधी संयुक्त मोर्चे के वे समर्थक थे। इसलिए एक वस्तुदर्शी की हैसियत से हमें इस ‘धारणा’ के प्रारम्भिक रूप को भी स्वीकार करना पड़ा, यद्यपि उस समय प्रगतिशील लेखक संघ में मार्क्सवादियों के अतिरिक्त और विचारों तथा दार्शनिक दृष्टिकोणों के लेखक भी सम्मिलित थे, और जो सम्मिलित नहीं थे वे भी उसके साथ पूरी तरह सहयोग करते थे, और हम उनके साथ सहयोग करते थे। फलत: दिल्ली में ‘भारतीय लेखक कॉन्फ्रेन्स’ का अधिवेशन बुलाने के लिए हमने प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, कृष्णचन्द्र, उपेन्द्रनाथ ‘अश्क’ आदि की पूरी मदद की। विचार था कि लेखकों के अन्य संगठनों की तरह प्रगतिशील लेखक संघ भी इस नये व्यापक संगठन में एक इकाई की तरह सम्मिलित होगा। इसी प्रकार सन् 1947 के प्रारम्भ में जैनेन्द्र कुमार ने जब पुन: तमाम लेखकों को एक ऐसे ही व्यापक संगठन में लाकर एकता के सूत्र में बाँधने का विचार प्रकट किया तो प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से मैंने न केवल उसका स्वागत किया, बल्कि उनके साथ पूरा सहयोग करके प्रस्तावित संगठन की प्रारम्भिक रूपरेखा भी तैयार की। इस दिशा में अभी हमारे प्रयत्न जारी ही थे कि दिल्ली में फ़साद शुरू हो गए, और देश के बँटवारे के साथ चारों ओर ऐसी अफरातफरी मची कि इस विचार को एक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना पड़ा। प्रगतिशील लेखक संघ के तत्कालीन प्रधानमन्त्री सज्जाद जहीर को जब मैंने इस बारे में सूचित किया तो उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी और प्रस्तावित ‘भारतीय साहित्यकार सम्मेलन’ में बाजाब्ता सम्मिलित होने का इरादा प्रकट किया। अगर दंगा-फ़साद न हुआ होता और यह नया संगठन स्थापित हो गया होता, तो संभवत: प्रगतिशीत लेखक संघ उस समय ही उसका एक महत्वपूर्ण अंग बन गया होता।
ये तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि जब वह ‘धारणा’ अधिकांश में निराधार ही थी, उस समय भी वह मार्क्सवादी लेखक, जो प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व कर रहे थे, दुराग्रही और संकीर्णमतवादी नहीं बने। अर्थात् उन्होंने कभी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया कि प्रगतिशील लेखक संघ से बाहर भी देश-भक्त जनवादी और प्रगतिशील लेखक हैं, और अगर वे किसी नये संगठन के अन्दर ही संगठित होने के आग्रही हैं, तो प्रगतिशील लेखक संघ को भी उस व्यापक संगठन में सामूहिक रूप से सम्मिलित होने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अत: आज जब भारतीय लेखकों को ‘शान्ति, स्वतन्त्रता और जनवाद’ के सिद्धान्तों की बुनियाद पर एकजुट करने का प्रश्न हमारे सामने हैं, तो निश्चय ही हम ‘संकीर्ण मतवादियों’ की तरह इस बात का दुराग्रह नहीं कर सकते कि ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ ही लेखकों का ‘संयुक्त मोर्चा’ बन सकता है, या उसे ही हमें ‘संयुक्त मोर्चा’ बनाना है। ऐसी नीति का व्यावहारिक परिणाम अधिक-से-अधिक यह निकलेगा कि ‘संकीर्णतावाद’ के दौर में जो मार्क्सवादी या उनके निकट हमदर्द लेखक प्रगतिशील लेखक संघ से हट गए थे या हटा दिये गए थे, उनको ही वापस लाया जा सकेगा; और भारतीय लेखकों का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा संभवत: प्रगतिशील लेखक संघ के अन्तर्गत किसी संयुक्त मोर्चे में सम्मिलित होने को तैयार न होगा, क्योंकि ‘कुत्सित समाज शास्त्रीयता’ के समर्थक साथियों की संकीर्ण नीति ने उक्त ‘धारणा’ को इस समय एक हकीकत बना दिया है, और उन्होंने इस बात का अनेक ढंगों से अनेक बार एलान भी किया है।
फिर मैंने अपने निबन्ध में प्रगतिशील लेखक संघ का व्यापक जनवादी आधार पर पुनर्संगठन करने के लिए तमाम लेखकों से क्यों अपील की? क्योंकि प्रारम्भ से ही मार्क्सवादी लेखक इस ‘धारणा’ के विरुद्ध संघर्ष करते आए हैं। प्रगतिशील लेखक संघ जब स्थापित हुआ था, उस समय भारत के अधिकांश मुक्तिकामी, प्रगतिचेता लेखक इसमें सम्मिलित हुए थे, और जो नहीं हुए थे उनको भी इसमें ले आने की संभावनाएँ थीं, क्योंकि हर विचार और पार्टी के लेखक इस बात पर सामान्यत: सहमत थे कि एक व्यापक आधार पर प्रगतिशील लेखक संघ को भारत के तमाम लेखकों का साम्राज्य-विरोधी संयुक्त मोर्चा बनाना जरूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले मार्क्सवादी लेखकों के सामने भी कभी इस सीमा का उल्लंघन करके प्रगतिशील लेखक संघ को पार्टी का प्रचार-केन्द्र बना देने का संकीर्ण स्वार्थ नहीं था। अंग्रेजी हुकुमत ने अपने विरुद्ध भारतीय लेखकों को एक होते देखकर हमारे बीच फूट डालने की गरज से सबसे पहले ‘स्टेट्समैन’ जैसे अखबारों द्वारा यह भ्रामक प्रचार शुरू करवाया कि प्रगतिशील लेखक संघ कम्युनिस्ट पार्टी का खुला प्लेटफार्म है, और इसे चलाने के लिए मास्को से सोना आता है! सन्देह पैदा करके एक गुलाम देश में फूट डाल देना आसान काम होता है। अनेक नौकरीपेशा लेखक प्रगतिशील लेखक संघ से अलग हो गए। इससे संघ के सरगर्म संगठनकर्ताओं में मार्क्सवादी लेखकों का बहुमत-सा दिखाई देने लगा और प्रत्यक्षत: ऐसी ‘धारणा’ के पैदा हो जाने की संभावना उत्पन्न हो गई। इधर राजनीतिक पार्टियों के आन्तरिक झगड़ों और साहित्य-जगत् में सक्रिय प्रतिक्रियावादी प्रभावों और दकियानूसी विचारों की पत्र-पत्रिकाओं ने भी इस ‘धारणा’ को बल पहुँचाने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। हम लगातार इस भ्रामक ‘धारणा’ के विरुद्ध संघर्ष करते रहे, जिसका ही परिणाम था कि यद्यपि अनेक श्रेष्ठ लेखक इस धारणा से प्रभावित होकर प्रगतिशील लेखक संघ में सम्मिलित होने से अपना दामन बचाते रहे, लेकिन उन्होंने असहयोग नहीं किया। जिन मित्रों को सन् 1941-42-43 के दिन याद हैं वे जानते हैं कि हिन्दी के अधिकांश लेखक पूरे उत्साह और हार्दिकता से ‘हंस’ के लिए लिखते थे, जो उस समय ‘प्रगतिशील आन्दोलन’ का मुख-पत्र बन गया था। मार्क्सवादी लेखकों की ओर से उनकी रचनाओं की तीव्र आलोचनाएँ भी होती थी, लेकिन इससे परस्पर के सौहार्द में फ़र्क़ न आता था, क्योंकि ये आलोचनाएँ यथासंभव गंभीर सैद्धान्तिक दृष्टि से ही की जाती थीं, उनमें एक उदात्त मार्क्सवादी नैतिकता का ओज और दीप्ति होती थी। उनका उद्देश्य किसी लेखक को खामख्वाह जलील करना नहीं होता था। हिन्दी में प्रगतिवादी या कहें कि मार्क्सवादी आलोचना की इस गौरवशाली परम्परा के निर्माण में एक आलोचक और ‘हंस’ के तत्कालीन सम्पादक की हैसियत से मेरा काफी हाथ रहा था, परन्तु यह एक खेदजनक बात है कि इस ऊँचे सैद्धान्तिक धरातल को कायम रखने के लिए मुझे जितनी सतर्कता दिखानी चाहिए थी, उतनी मैं न दिखा सका, जिसके फलस्वरूप शरत् तथा सोहनलाल द्विवेदी आदि के सम्बन्ध में डॉ० रामविलास की सिद्धान्त-हीन, रुचि-वैचित्र्यवादी और केवल एक निम्न कोटि का आनन्द पाने के लिए चटखारे ले लेकर पढ़ी जाने योग्य आलोचनाएँ भी मेरी अनुमति से ही ‘हंस’ में प्रकाशित होती रहीं, और इस प्रकार ‘कुत्सित समाज शास्त्रीयता’ का बीज बोया जाता रहा— यद्यपि दूसरी तरफ मैं इस हीन अ-मार्क्सवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध उस समय से ही चेतावनी भी देता रहा। लेकिन चूंकि यह प्रवृत्ति प्रगतिशील आन्दोलन की मुख्य विचारधारा नहीं थी, इसलिए तमाम लेखकों में परस्पर सहयोग की भावना पूर्ववत् बनी रही।
प्रगतिशील आन्दोलन पर उन दिनों विरोधियों की ओर से दो आक्षेप किये जाते थे। पहला आक्षेप यह था कि प्रगतिवादी लेखकों की रचनाओं में अश्लीलता और नग्नता का चित्रण होता है। यह आक्रमण एकदम निराधार भी नहीं था, क्योंकि ‘छायावाद’ की ‘अशरीरी’ कल्पना की ‘स्वाभाविक’(!) प्रतिक्रिया के बहाने कतिपय कम उन्नत भाव-चेतना के लेखकों ने ‘जीवन की यथार्थ और मांसल अभिव्यक्ति’ करने का नारा देकर अपनी कहानियों और कविताओं में पिछड़े, कुरूप और यथासम्भव अनैतिक जीवन का यथातथ्य, फोटोग्राफिक, प्रवृत्त-चित्रण करना शुरू कर दिया था, और इस प्रकार एक हीन रुचि की, कला-विहीन, भाव-शून्य प्रकृतवादी (Naturalistic) रचनाएँ, जो मूलत: Formalistic और प्रतिक्रियावादी होती हैं, प्रगतिशील साहित्य के नाम पर होने लगी थीं। दूसरा आक्षेप यह था कि प्रगतिवादी साहित्य को मात्र प्रोपेगेण्डा बना देना चाहते हैं। इस आक्षेप में भी आंशिक सत्य था, क्योंकि अधिकतर नये लेखक सस्ती ख्याति पाने की गरज से ही किसान और मजदूर के बारे में कविताएँ लिखने लगे थे, यद्यपि मजदूर-किसान के जीवन और उसकी समस्याओं से उनका कोई दूर का सम्बन्ध भी नहीं था, जिसके कारण अक्सर उनकी उद्बोधनात्मक कविताओं में सच्ची हार्दिक सहानुभूति के स्थान पर मध्यवर्गी कृपा भाव, अतिरंजित अलंकार-योजना द्वारा पैदा किया गया कृत्रिम ओज और व्यर्थ का शब्द-जाल होता था। रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में ये दोनों प्रवृत्तियाँ ‘कुत्सित समाज शास्त्रीयता’ की ही सजातीय थी, और धीरे-धीरे अपनी आन्तरिक एकता का अहसास करके सहज भाव से खिंचकर एक-दूसरे के निकट आ रही थीं। मार्क्सवादी आलोचकों ने इन आक्षेपों का उत्तर देते समय इन प्रवृत्तियों का भी विरोध किया, परन्तु उस समय तक हमारा अनुमान था कि सम्भवत: समय के साथ-साथ ये लेखक-आलोचक भी उन्नति करते जाएंगे, धीरे-धीरे हकीकत पसन्द लेखक बन जाएंगे, और उनकी रचनाओं में कला का परिमार्जन और ओज आ जाएगा। इसलिए जिस जागरूकता से मार्क्सवादी लेखकों को ‘कुत्सित समाज शास्त्रीयता’ के प्रारंभिक रूपों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए था, हमने नहीं किया। अन्तत: इस ढिलाई का परिणाम यह निकला कि प्रगतिशील लेखक संघ पर पूरी तरह छा करके ‘कुत्सित समाज शास्त्रीयता’ के समर्थकों ने हमारे आन्दोलन की उदात्त, जनवादी परम्पराओं को धूल में मिला दिया और प्रारम्भ में अन्य लेखकों की जिस ‘धारणा’ को साम्राजी प्रचार और दकियानूसियों के आक्षेपों ने मुख्यत: एक भ्रामक आधार दिया था, उस ‘धारणा’ को हमारे ‘संकीर्णतावादी कुत्सित समाज शास्त्री’ साथियों ने अपने ‘अमल’ और अपनी ‘रचनाओं’ से आज हक़ीक़त बना दिया है।
प्रारम्भ में प्रगतिशील लेखक संघ का व्यापक जनवादी आधार बनाये रखने के लिए मार्क्सवादी लेखकों ने विरोधियों के लांछनों और आक्षेपों और दोस्तों की कुत्सित साहित्य-चेष्टाओं के विरुद्ध और उनसे उत्पन्न इस ‘धारणा’ को निर्मूल करने के लिए जो संघर्ष किया था, उसकी उदात्त परम्परा के प्रभाव में पड़कर ही मैंने अपना सुझाव दिया। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि आम लेखकों को यदि यह सुझाव अमान्य हो तो हम उनके साथ मिलकर कोई नया संगठन बनाने की बात को गलत और आपत्तिजनक समझें और अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग ही पकाते जायें। फिर भी मेरा सुझाव अस्पष्ट और अनिश्चित प्रकार का है— उसका आधार एक उदात्त पूर्व परम्परा है और उसमें बीच के दौरे में ‘कुत्सित समाज-शास्त्रियों’ द्वारा पैदा की गई संकीर्ण, एकांगी परिस्थिति को नजरअन्दाज किया गया है। और यह गलत है। आपने इस संगत प्रश्न को उठाकर मुझे अपने सुझाव की असंगति पर विचार करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आभारी हूँ, और अब मैं इस सम्बन्ध में अपने सुझाव सविस्तार पेश करता हूँ।
प्रगतिशील लेखक-संघ के सीधे-टेढ़े विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दृष्टि में रखकर हमारे लिए अब यही उचित होगा कि हम इस वांछित अथवा अवांछित स्थिति को स्वीकार कर लें कि प्रगतिशील लेखक-संघ प्रधानत: कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले मार्क्सवादी (दुर्भाग्य से इस स्थान पर ‘कुत्सित समाज-शास्त्रीयता’ के समर्थकों को भी इस कोटि में ही रखने के लिए विवश हैं) लेखकों का संगठन है, और उसको पुन: तमाम जनवादी लेखकों का संयुक्त मोर्चा बनाने की संदिग्ध चेष्टा में जितना समय और श्रम का अपव्यय करना होगा, उसकी अपेक्षा यह काम ज्यादा सुगम होगा कि ‘शान्ति, स्वतंत्रता और जनवाद’ के सिद्धान्तों के आधार पर साहित्यकारों के अन्य संगठनों और श्रेष्ठ लेखकों का व्यक्तिगत सहयोग प्राप्त कर, सबकी सामान्य चेष्टा से एक ‘अखिल भारतीय जनवादी लेखक सम्मेलन’ स्थापित किया जाये, जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ, साहित्यकार-संसद् और दूसरी प्रान्तिक, स्थानिक और विभिन्न भाषाओं के लेखकों की संस्थाएँ विभिन्न इकाइयों के रूप में सम्मिलित हों और जो लेखक किसी साहित्य-संस्था से सम्बन्ध न रखते हों, वे व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हों। ‘भारतीय जनवादी लेखक सम्मेलन’ कैसे बुलाया जाये, जो संगठन बने उसके उद्देश्य क्या हों, विस्तृत कार्यक्रम क्या हो, विधान कैसा हो—आदि का निर्णय पहले से नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ इन प्रश्नों पर विचार करना अप्रासंगिक होगा।
ऐसे एक सामान्य संगठन की अतीव आवश्यकता है, इस बात से निस्सन्देह अधिकांश लेखक सहमत होंगे, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।
प्रगतिशील लेखक संघ को मार्क्सवादी लेखकों का संगठन स्वीकार कर लिया जाय तो फिर उसका अपना कार्यक्रम क्या हो? क्या वह कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार केन्द्र ही न बन जायगा? क्या फिर उसके पुनर्संगठन की आवश्यकता नहीं रह जाती? ये कतिपय प्रश्न अनिवार्यत: उठते हैं।
इस सम्बन्ध में हमारी पार्टी के अन्दर भी प्रारम्भ से ही काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। सत्र से पहले पुनर्संगठन के प्रश्न को लें। किसी भी सूरत में प्रगतिशील लेखक संघ का पुनर्संगठन जरूरी है। जब तक मार्क्सवादी लेखकों के अन्दर से ‘कुत्सित समाज-शास्त्रीयता’ की प्रवृत्ति को सदा के लिए निर्मूल नहीं कर दिया जाय, उस समय तक हमारे देश में ‘मार्क्सवाद’ की विचार-धारा विकास नहीं कर सकती, न भारत के जनवादी लेखकों में एकता पैदा करके उन्हें एक व्यापक संगठन में इकट्ठा ही किया जा सकता है। वस्तुत: एकता मार्क्सवादी लेखकों में भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी एकता का आधार ‘मार्क्सवाद’ ही हो सकता है, ‘कुत्सित समाज-शास्त्रीयता’ नहीं। पिछले पाँच-सात वर्षों में ‘कुत्सित समाज-शास्त्रीयता’ ने हमारे देश में मार्क्सवाद को जितनी क्षति पहुँचाई है, उसका अनुमान लगाना आसान काम नहीं है। मार्क्सवाद और साहित्य-कला से सम्बन्धित हर प्रश्न पर इस प्रवृत्ति ने ऐसा गड़बड़घोटाला किया है कि उसके दुष्प्रभावों को मिटाने में कई वर्ष और अथक परिश्रम लग जाएगा। इसलिए अगर ‘मार्क्सवादी’ विचारधारा को विकास और उन्नति करनी है, तो हमें अविलम्ब प्रगतिशील लेखक संघ का पुनर्संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि उसमें ‘कुल्लित समाज शास्त्रीयता’ की प्रवृत्ति के विरुद्ध सतर्क होकर अविराम संघर्ष करने की सुविधा प्रत्येक मार्क्सवादी लेखक को प्राप्त हो। इस प्रवृत्ति के समर्थकों के गिरोह या गुट के प्रति मोह और पक्षपात दिलाकर हम इस गिरोह का ही हित-साधन कर सकते हैं, जनता और मार्क्सवाद का नहीं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि प्रगतिशील लेखक संघ से इस गुट के लेखकों को निर्वासित कर दिया जाय, बल्कि यह कि उन्हें स्वयं अपनी कुत्सित प्रवृत्ति से संघर्ष करने और काम और अध्ययन द्वारा मार्क्सवाद को सही ढंग से सीख-समझकर सच्चे मार्क्सवादी लेखक बनने का पूरा अवसर देना चाहिए, और उन्हें दूषित वातावरण को और ज्यादा दूषित करने से वंचित कर देना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रगतिशील लेखक-संघ का मार्क्सवादी लेखकों की संस्था के रूप में नये सिरे से जनवादी आधार पर संगठन करने के लिए एक अधिवेशन जल्द-से-जल्द बुलाया जाय जिसमें प्रत्येक भाषा के उन तमाम मार्क्सवादी लेखकों को निमंत्रित किया जाय, जिनका सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, या जो उसके हमदर्द हैं। यहाँ निम्न चार बातों को दृष्टि में रखकर प्रगतिशील लेखक संघ का पुनर्संगठन किया जाय—
01. शान्ति, स्वतन्त्रता और जनवाद के लिए भारतीय साहित्यकारों और जनता के संघर्ष आन्दोलन को तेजतर करने के लिए अपनी साहित्यिक रचनाओं और संगठन कार्य द्वारा मार्क्सवादी लेखक क्या कर सकते हैं, और उन्हें कैसे, क्या करना चाहिए।
02. मार्क्सवादी साहित्य में ‘कुत्सित समाज शास्त्रीयता’ की प्रवृत्ति के विरुद्ध सजग संघर्ष करने के लिए कैसे-क्या करना चाहिए।
03. भारत में सही मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अपने देश के साहित्य और इतिहास की अपेक्षा आलोचना और समाज-विज्ञान के क्षेत्रों में श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ साहित्य-निर्माण के लिए कैसे-क्या करना चाहिए!
04. अपने देश की भाषाओं में मार्क्सवादी ‘क्लासिक’ ग्रन्थों और देशी-विदेशी भाषाओं के रचनात्मक साहित्य की महान् कृतियों और प्रगतिशील रचनाओं आदि के अनुवाद और प्रकाशन के लिए कैसे-क्या किया जाय।
अभी तक यह सारा महत्वपूर्ण कार्य अराजक रीति से ही चलता-चलाता आया है, और इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। हमारे देश की प्रत्येक भाषा में मार्क्सवादी लेखकों की काफ़ी बड़ी संख्या है इन लेखकों में मैं पत्रकारों को नहीं शामिल कर रहा, क्योंकि उनका कार्य साहित्य सृजन नहीं है। जो लेखक साथ ही पत्रकार भी हैं, उनकी बात अलग है। दरअसल यहाँ मेरे ध्यान में रचनात्मक साहित्य के निर्माताओं कवियों, उपन्यासकारों, नाटककारों, कहानी लेखकों, आलोचकों के अतिरिक्त समाज-शास्त्रियों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, मनोवैज्ञानिकों, पुरातत्ववेत्ताश्री नृ-शास्त्रविज्ञों, भूगोल शास्त्रियों आदि मानव-शास्त्रों, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी खोज और लेखन से भाग लेने वाले उन तमाम लेखकों की बड़ी संख्या भी है, जो पार्टी में हैं, या हमारे निकट हैं, और जिनको हमें भुला नहीं देना चाहिए। इन सब साथियों को एकत्र किया जाय तो निश्चय ही मार्क्सवादी लेखकों की काफ़ी बड़ी तादाद बन जाती है, और यदि एक सुविचारित और सुनिश्चित योजना के अन्तर्गत इन तमाम साथियों के साहित्यिक और रचनात्मक प्रयत्नों को संगठित किया जा सके, तो इसमें सन्देह नहीं कि थोड़े समय में ही भारत के मार्क्सवादी लेखक विचार-जगत् के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयात्मक भूमिका खेल सकेंगे, और देश के चिन्तन को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकेंगे।
यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर देना जरूरी है कि प्रगतिशील लेखक संघ को मार्क्सवादी लेखकों का संगठन बनाने का यह अर्थ नहीं है कि उसे कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार-केन्द्र बना दिया जाय। ऐसा करना गलत होगा। कम्युनिस्ट पार्टी से उसका गहरा सम्बन्ध होगा, यह तो निश्चित है; लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ को हर सूरत में एक साहित्यिक संस्था ही बना रहना चाहिए, पार्टी का प्रचार-केन्द्र नहीं। मैं जानता हूँ कि ऐसा कहने पर ‘कुत्सित समाज शास्त्रीयता’ के समर्थक साथियों को घोर आपत्ति होगी और वे किसी व्यक्तिवादी, मध्यवर्गी मनोवृत्ति से इस बात का सम्बन्ध जोड़ने के लिए दलीलें तलाश करेंगे और लेनिन-स्टालिन की कृतियों को आद्यन्त उलट-पलट डालेंगे। लेकिन हकीकतपसन्दी का यह तकाजा है कि जब हम किसी विषय पर सोचें तो उसके पूर्वापर सम्बन्धों पर भी निगाह रखें और अन्य घटनाओं, वस्तुओं और विषयों से जुड़ने वाले उसके सम्बन्ध-सूत्रों को भी ध्यान में रखें, ताकि हमारा सोचना एकांगी न हो जाय। पार्टी के अन्य दैनंदिक कार्यों में प्रगतिशील लेखक संघ किस प्रकार और किस सीमा तक सहयोग कर सकता है या उसे करना चाहिए, यह प्रगतिशील लेखक संघ के अपने कार्यक्रम के आधार पर ही विचारणीय विषय है, उससे अलग नहीं और पार्टी के साथ बैठकर यह विचार किया जाना उचित भी होगा। मार्क्सवादी लेखकों के पास अपने साहित्य-क्षेत्र का स्वयं इतना कार्य होगा या होना चाहिए कि संघ को पार्टी का प्रचार-केन्द्र बना देने का अर्थ होगा कि इन लेखकों की क्षमताओं का प्रयोग मार्क्सवाद, पार्टी और जनता के हित में जिस सीमा तक किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, उस सीमा तक न करके उनका अपव्यय कराया जाय। कुत्सित समाज-शास्त्रीय दृष्टिकोण के साथियों को यह बात इसलिए नापसन्द होगी कि उस समय साहित्य-रचना का काम बच्चों का खेल नहीं रह जायगा, और सस्ती ख्याति के मार्ग बन्द हो जाएंगे और उन्हें भी अपने कार्य को गम्भीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाना पड़ेगा। तब साहित्य-रचना एक कठोर जीवन साधना बन जायगी।
इसलिए मेरी निश्चित राय है कि पार्टी का प्रचार-केन्द्र प्रगतिशील लेखक संघ से अलग होना चाहिए। इस प्रचार-केन्द्र का संगठन कैसे और किस आधार पर किया जाय, इस पर कोई परामर्श देना विषयान्तर होगा। विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पार्टी के दैनिक और साप्ताहिक पत्रों में काम करने वाले पत्रकार और संवाददाता साथियों को अपना अलग संगठन बनाना चाहिए, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से (अर्थात् वैज्ञानिक दृष्टिकोण से) पत्रकार-कला की समस्याओं का हर पहलू से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के पत्रों को अधिक से अधिक जन-प्रिय और उच्चकोटि का कैसे बनाया जाय और पार्टी की सही नीति और कारकर्दगियों का श्रेष्ठ और प्रभावकारी ढंग से कैसे प्रचार और प्रकाशन किया जाय यह उनका मुख्य काम है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय पत्रकार संघ में प्रेस की स्वतन्त्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए किस प्रकार लड़ा जाय, ये कतिपय प्रश्न हैं जिनको ध्यान में रखकर पार्टी के पत्रकारों की संस्था को भारतीय पत्रकार संघ जैसे संगठन में सम्मिलित होना चाहिए। पार्टी के प्रचार केन्द्र मार्क्सवादी लेखकों या अन्य जनवादी लेखकों की रचनाओं का अपने प्रचार के लिए किस प्रकार उपयोग करेंगे, इसका निर्णय तो वे स्वयं ही किया करेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन रचनाओं का उपयोग अन्य जनवादी पार्टियों के प्रचार केन्द्र भी कर सकते हैं।
प्रगतिशील लेखक संघ का विस्तृत कार्यक्रम क्या हो, इस सम्बन्ध में तफसील से सुझाव देने का यह अवसर नहीं है। जिन चार बातों के आधार पर संघ का पुनर्संगठन जरूरी है उनको दृष्टि में रखकर कुछ मोटी-मोटी बातें ही स्पष्ट कर देना उचित होगा ।
01. ‘मानव-आत्मा के शिल्पियों से’ निबन्ध में भारत के तमाम लेखकों से जीवन-वास्तव को मूर्त, सम्पूर्ण और सक्रिय रूप से प्रतिबिम्बित करने और शान्ति, स्वतन्त्रता और जनवाद के महान् विचारों को अपनी कलाकृतियों द्वारा जन-जन की मूर्त भावना बनाने के लिए मैंने जो अपील की है, वह मार्क्सवादी साहित्यकारों पर भी समान रूप से लागू होती है। मार्क्सवादी लेखक भारतीय साहित्य की व्यापक जनवादी परम्परा के ही अंग हैं, उससे बाहर नहीं हैं। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा अन्य लेखकों की तरह इस परम्परा को उत्तरोत्तर विकसित करते जाना उनका भी कर्तव्य है— एक प्रकार से कुछ अधिक ही। जीवन-वास्तव को प्रतिबिम्बित करते समय मार्क्सवादी लेखकों को भी कला की सचाई का पालन करना है। उदाहरण के लिए, किसी घटना, आन्दोलन, प्रदर्शन या व्यक्ति या परिवार के जीवन का मूर्तसम्पूर्ण चित्रण करते समय यदि मार्क्सवादी साहित्यकार किसी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता का चरित्र भी पेश करता है, तो उसे इस पात्र को एक आदर्श, मर्यादापुरुषोत्तम चरित्र नहीं बना देना चाहिए। कम्युनिस्ट मजदूर या किसान पात्र निर्व्यक्त, निर्विकार प्राणी नहीं हैं— इस वर्ग समाज के ही प्राणी हैं। मैं तो कहूँगा कि मार्क्सवादी लेखकों को रचनात्मक दृष्टिकोण से अपने कम्युनिस्ट पात्रों की कमजोरियों और खामियों की भी तीव्र आलोचना करनी चाहिए। जहाँ कहीं किसी साथी में ‘लिबरलिज़्म’ की संकीर्ण प्रवृत्ति या ‘हुक्मराना’ अन्दाज पाये, जिससे जन-कार्य का अहित होता हो, तो उनका कर्तव्य है कि उसकी खामियों को रचनात्मक दृष्टिकोण से चित्रित करें, और इस प्रकार पार्टी के साथियों को बेहतर कम्युनिस्ट बनने की प्रेरणा दें। पार्टी का हित जनता के हित से भिन्न चीज नहीं है केवल इस बात को ध्यान में रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि वह हकीकतपसन्दो का दामन न छोड़ें। पार्टी का भी कर्तव्य है कि वह मार्क्सवादी लेखकों की रचनाओं में निहित सही आलोचनाओं पर पूरी संजीदगी से ग़ौर करे और उनका स्वागत और आदर करे। लेखक अगर ‘मानय-आत्मा के शिल्पी’ हैं, तो कम्युनिस्ट भी ‘मानवों’ की श्रेणी में ही आते हैं, ये कहीं आसमान में नहीं उद्भूत हुए, इस वर्ग-समाज में ही पैदा हुए और पले हैं। मार्क्सवाद ने जीवन को देखने-समझने और बदलने के लिए अमल करने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है, पर यह दृष्टिकोण जादू की लकड़ी नहीं है कि उसको छूते ही आदमी ‘सर्व-गुण-सम्पन्न’ बन जाता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि मावर्सवादी कवियों, कथाकारों और नाटककारों आदि का अन्य लेखकों के साथ मिलकर शान्ति, स्वतन्त्रता और जनवाद के संघर्ष में अधिकाधिक और श्रेष्ट कलात्मक साहित्य की रचना करना ही मुख्य काम है।
02. ‘कुत्सित समाज-शास्त्रीयता’ द्वारा पैदा की गई तबाही के कारण मार्क्सवादी आलोचकों का दायित्व आज बहुत बढ़ गया है। इस अबुद्धिवादी और अवसरवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष का तात्पर्य केवल यही है कि मार्क्सवादी आलोचना का निरन्तर विकास करके उसे अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक बनाया जाय। यह एक बहुत व्यापक संघर्ष है, क्योंकि आलोचना के प्रतिमानों, मूल्य-निरुपण के सिद्धान्तों आदि की स्थापना करना और उनके आधार पर प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य का मूल्यांकन करना आदि सारे काम इसके अन्तर्गत आते हैं। साथ ही मानव-विज्ञानों के अन्य क्षेत्रों में भी जो शास्त्रीय साहित्य पैदा हो रहा है, उसकी विस्तृत सिद्धान्तपूर्ण गम्भीर आलोचना करना भी नितान्त आवश्यक है। उदाहरण के लिए कोई इतिहास या वेदान्त दर्शन के सम्बन्ध में पुस्तक निकलती हैं, तो ऐसी पुस्तकों की चलताऊ या टकसाली आलोचना से काम नहीं चलेगा, न पूर्व धारणाओं के आधार पर लेखक या पुस्तक का नाम देखकर ही उसे रद्दी करार देने से काम चलेगा। इसी प्रकार तुलसीदास, कालिदास या शेक्सपियर आदि विश्व-साहित्य के महान् लेखक क्यों आज भी जन-कवि या जनता के हकीकी लेखक हैं, और हमेशा रहेंगे, उनकी कृतियों का मूल्य क्यों स्थायी या अमर है और जनता में उनकी कृतियों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाना क्यों जरूरी है— आदि प्रश्नों का भी मार्क्सवादी आलोचना को वैज्ञानिक उत्तर देना है। कुत्सित समाज-शास्त्रीय आलोचकों की तरह केवल ‘तुलसी तब हहाकरी’ जैसे दस-पाँच उद्धरणों के आधार पर तुलसीदास या किसी अन्य लेखक की महत्ता को सिद्ध करना व्यर्थ है— इस रीति से ही कथा-वाचक आज तक तुलसीदास को हर प्रकार की धर्मान्धता और प्रतिक्रिया का समर्थक सिद्ध करते आए हैं। इसलिए मार्क्सवादी आलोचना के सामने बहुत बड़ा काम है। प्रत्येक भाषा में मार्क्स-वादी आलोचकों ने इस दिशा में काफ़ी उपयोगी काम किया भी है, जिसे कुत्सित समाज-शास्त्रीयता की प्रवृत्ति ने झुठलाने या विस्मृत करने की कोशिश की है। ऐसे तमाम आलोचना-साहित्य की परीक्षा करके, उसके वैज्ञानिक अंश का सम्पादन और प्रकाशन जरूरी है। इसी प्रकार पिछले पन्द्रह वर्षों में मार्क्सवादी लेखकों ने जो श्रेष्ठ और मूल्यवान रचनात्मक साहित्य पैदा किया है, उसका संकलन और प्रकाशन भी जरूरी है, ताकि दोस्तों या विरोधियों की यह धारणा निर्मूल की जा सके कि मार्क्सवादी लेखक कलात्मक साहित्य की मर्यादाओं को भंग करके केवल एकांगी और भावहीन साहित्य ही रचते हैं।
03. इतिहास, दर्शन, समाज-शास्त्र आदि अन्य मानव-विज्ञानों की ओर अभी तक मार्क्सवादी लेखकों ने सामूहिक रूप से ध्यान नहीं दिया है। वस्तुत: हमें हर क्षेत्र में बच्चों से लेकर उच्च-से-उच्च शिक्षा-प्राप्त उद्बुद्ध पाठकों के लिए रचनात्मक और वैज्ञानिक साहित्य का निर्माण करना है। यह कार्य अन्य लेखकों और खोज करने वाले विद्वानों का ही नहीं है। प्रत्येक भाषा के मार्क्सवादी लेखकों को इस महत् कार्य में भाग लेकर न केवल तमाम कौमियतों की भाषाओं के विकास में सहायक होना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके साहित्य का भंडार भी भरना चाहिए और जन-शिक्षा के कार्य में आगे रहना चाहिए। मैंने ‘जनपदीय भाषाओं के प्रश्न’ पर अपनी रिपोर्ट में जनपदीय भाषाओं के अलग प्रगतिशील लेखक संघों की स्थापना का सुझाव पेश करते हुए उनके कार्यक्रम को तीन सूत्रों में व्यक्त किया था— अर्थात् कहा था कि ‘जन-माषा’, ‘जन-शिक्षा’ और ‘जन-साहित्य’ ही इन जनपदीय प्रगतिशील लेखक संघों का कार्यक्रम होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह सुझाव आज भी सर्वथा सही है। देश की तमाम कौमियतों की भाषाओं के मार्क्सवादियों को इस कार्यक्रम को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए।
04. इसी प्रकार भारतीय भाषाओं में विश्व-साहित्य और मार्क्सवादी साहित्य के अनुवाद का प्रश्न भी काफ़ी व्यापक है, और इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, देश की किस भाषा में शेक्सपीयर, बाल्जक, गेटे, ताल्स्तॉय, पुश्किन, गोर्की आदि की तमाम श्रेष्ठतम रचनाओं का प्रामाणिक अनुवाद हो चुका है? किस भाषा में मार्क्स, एञ्जिल्स, लेनिन, स्टालिन की तमाम कृतियों का प्रामाणिक अनुवाद हो गया है?
शान्ति, स्वतन्त्रता और जनवाद के संघर्ष को तेजतर करने के लिए ये सारे रचनात्मक कार्य जरूरी है। ज्ञान और चेतना की मशाल ही साहित्यकारों का सबसे बड़ा अस्त्र है; मार्क्सवादी लेखकों का कर्तव्य है कि इस मशाल को उठाकर ही जनता के बीच में जाएँ, कोरे सिद्धान्त-प्रचारक की हैसियत से नहीं। साहित्य-निर्माण उनकी जीवन-साधना बन जाना चाहिए।
इसीलिए प्रगतिशील लेखक संघ को मार्क्सवादी लेखकों की संस्था के रूप में नये सिरे से संगठित करना चाहिए, और सुचारु रूप से उसका कार्य-संचालन करने के लिए उसके अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं के एक ही विषय से सम्बन्ध रखने वाले लेखकों की विभिन्न परिषदों की स्थापना होनी चाहिए, और उन्हें बाकायदा एक विस्तृत योजना के अनुसार साहित्यिक कार्य करना चाहिए। अन्त में, प्रगतिशील लेखक संघ को ‘भारतीय जनवादी लेखक-सम्मेलन’ की स्थापना में पूरा भाग लेना चाहिए, और मार्क्सवादी लेखकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अन्य साहित्य संस्थाओं और साहित्यकारों के साथ अपने रिश्ते अटूट बनाने चाहिए उनके साथ पूरा सहयोग करके और अपने साहित्यिक कार्यों में उनका सहयोग प्राप्त करके।
रही लेखकों के आदर-सम्मान की बात। अगर कभी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इस बारे में कोताही बरती गई है, लेखकों की उपेक्षा की गई है या वक्त जरूरत पर ही किसी लेखक को सम्मानित किया गया है और काम निकल जाने पर उसकी बात भी नहीं पूछी गई, तो निश्चय ही कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी सजगता से इस व्यवहार को तर्क करना चाहिए, क्योंकि लेलकों या किसी भी क्षेत्र के निर्माताओं (मजदूर, किसान, दस्तकार कलाकर आदि के प्रति अवहेलनापूर्ण व्यवहार मूलत: पूँजीवादी समाज के वर्ग-सम्बन्धों और बुर्जुआ नैतिकता ही का आईनादार है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और मार्क्सवादी लेखकों को अपने उच्च नैतिक विचारों के अनुकूल ही जनवादी साहित्यकारों और उनकी रचनाओं का सहज भाव से आदर-सम्मान करना लाजिमी है। हम उनके विचारों और कृतियों की खुलकर सैद्धान्तिक आलोचना करें, पर मनुष्योचित सौजन्य और सहानुभूति को तर्क करके नहीं, संकीर्ण हितों की दृष्टि से नहीं, एकांगी भी नहीं कि बुराइयाँ ही देखें और अच्छाइयाँ नजरअन्दाज कर दें। सकल जनता के लिए मानव संस्कृति की सारी जिन्दा और जावेद मीरात का दावा करने वाले कला संस्कृति का निर्माण करने वाली प्रतिभाओं को मानव-द्रोहियों और प्रतिक्रियावादियों के हाथों में तोहफ़ा बनाकर भेंट देने की हिमाकत नहीं कर सकते—न प्राचीन लेखकों को और न वर्तमान लेखकों को ही। मार्क्सवादी लेखकों को विशेष रूप से याद रखना चाहिए कि एक ग्रियर्सन को साम्राज्यवादी और एक राहुल को प्रतिक्रयावादी घोषित करने में तो केवल जबान हिलानी पड़ती है, लेकिन मनुष्य की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए इन मनीषियों ने जितना काम किया है, उसका एक शतांश भी कर लेना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है— धारा-प्रवाह गालियाँ बकने या बड़े-बड़े शब्दों को बाजीगर के गोलों की तरह कंठ से निकालते जाने की अपार क्षमता होने पर भी। जिस प्रकार जीवन के अन्य कार्य-व्यापारों में, उसी प्रकार साहित्य की दुनिया में भी रचनात्मक कार्य और कृतित्व ही सम्मानित होता है, जबानबाजी का गुण नहीं। मार्क्सवाद भी यही सिखाता है।
[आलोचना प्रथम अंक, अक्टूबर 1951 में ‘प्रस्तुत प्रश्न’ के अंतर्गत प्रकाशित]