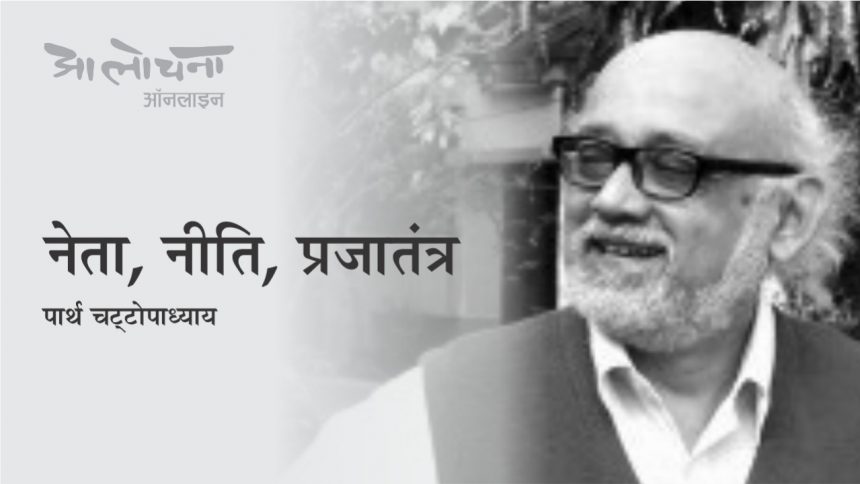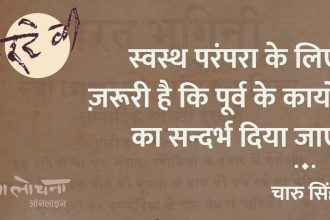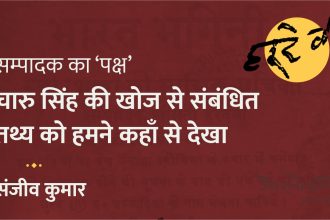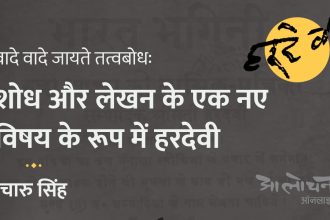भारत के आधुनिक राजनीति के इतिहास में सत्याग्रह की भूमिका को लेकर बहुत चर्चा हुई है। गांधी जी द्वारा संचालित आन्दोलन में ही यह अवधारणा विशिष्ट रूप से प्रकाशित हुई थी, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सामान्यतः सत्याग्रह कहने से जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियों को समझा जाता है वैसी बहुत-सी गतिविधियाँ व्यापक रूप से अन्य नाना प्रकार के आन्दोलनों के भीतर भी देखी गई हैं, यह भी हम जानते हैं। इतिहासविद् सुमित सरकार ने बताया है कि गांधी आन्दोलन से कई साल पहले बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन में इस्तेमाल किए गए राजनीतिक कौशलों में गांधी जी द्वारा वर्णित सत्याग्रह के पूर्व लक्षण सहज ही देखे जा सकते हैं। सिर्फ़ यही नहीं, सत्याग्रह का कौशल भारत के वामपंथी-समाजवादी आन्दोलन में भी बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। बहुत सरल ढंग से कहा जाए तो सत्याग्रह का अर्थ है अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करना, अन्यायपूर्ण कानूनों को न मानना, ऐसा करने पर यदि कोई सजा मिलती है तो उस सजा को स्वीकार करना और फिर प्रतिरोध करना। ठीक तरीके से संगठित होने पर सत्याग्रह जन-प्रतिरोध का आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन आम तौर पर इसमें हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता है। यह इस कारण कि हिंसक लड़ाई में संगठित राष्ट्र की शक्ति का पलड़ा बहुत, बहुत भारी होता है। दूसरी ओर निहत्थी जनता हजार सजा स्वीकार कर रही है लेकिन प्रतिरोध की राह नहीं छोड़ रही है। ऐसी स्थिति में आधुनिक राष्ट्र सबसे ज्यादा विपत्ति में होता है। राष्ट्र के कानून के प्रतिपक्ष के रूप में तब खड़ा हो जाता है सत्याग्रहियों का ‘सत्य’ जिसका मूल्य उनके लिए राष्ट्र के कानून की तुलना में बहुत ज्यादा है।
सत्याग्रहियों को अपना सत्य कहाँ से मिलता है? अर्थात्, वह कौन-सी ताकत है जिससे उनके मन में यह विश्वास दृढ़ होता है कि राष्ट्र का कानून अन्यायपूर्ण है और कानून से बड़ा भी कोई सत्य है जिसकी संगति में राष्ट्र का कानून नहीं है। इस प्रसंग में भारत की राजनीति में जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है, वह है ‘धर्म’। कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ ‘धर्म’ का तात्पर्य अंग्रेजी के ‘रिलीजन’ से नहीं है। धर्म याने कर्त्तव्य, कर्म, सत्कर्म; धर्म माने सामाजहितकारी नियम, धर्म माने सुनीति। धर्म की विधि का अर्थ किसी शासक द्वारा बनाए नियम नहीं, गोया वह नित्य, ध्रुव और चिर सत्य है।
उपनिवेशकालीन भारत में हिंसक-अहिंसक अनेक राजनीतिक आन्दोलनों में धर्म की इस भूमिका को लेकर पिछले बीस-पच्चीस सालों में बहुत चर्चा हुई है। अठारहवीं सदी के किसान विद्रोह से लेकर बीसवीं सदी के अहिंसक और सशस्त्र, हर तरह के आन्दोलन में ‘धर्म’ की भूमिका पर अनुसंधान किया गया है। राष्ट्र या सरकार के विरुद्ध प्रतिरोध जहाँ राजनीति का प्रधान उपादान है, खासतौर से हमारे समकालीन इतिहासकारों के लिए, वहाँ कानून की अवज्ञा करनेवाली जनता की चेतना में छिपा हुआ ‘धर्मबोध’ या ‘धर्म’ की भावना को लेकर हमारे मन में कौतूहल होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है।
दूसरी लक्षणीय बात है धर्मबोध से प्रेरित इन राजनीतिक आन्दोलनों के नेतृत्व का चरित्र। आदर्श नेता है त्यागी, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में निरुत्साही। राष्ट्र-शक्ति के विरोध के फलस्वरूप प्राप्त सजा का अधिकांश अपने सर पर लेकर दूसरों के सामने जो दृष्टांत स्थापित कर सके, वही है आदर्श नेता। गांधी जी ने अपने कल्पित आदर्श सत्याग्रही के बारे में कई बार कहा है कि देश की जनता यदि सत्य और अहिंसा के प्रति अपनी आस्था खो दे, तब भी सत्याग्रही को हर पल सत्य के मार्ग पर डटे रहना होगा। उसकी निष्ठा दिखेगी उसके आत्मत्याग में जो आम लोगों के लिए दृष्टांत होगी और उन्हें हिम्मत देगी। चरमतम आत्मत्याग है अन्यायपूर्ण शासन के विरोध में प्रतिवाद करते हुए मृत्यु का वरण करना। आत्मत्याग का यह आदर्श और उसकी चरम अभिव्यक्ति के रूप में शहीद होना, यह धारणा किसी भी तरह गांधीवादी आन्दोलनों तक ही सीमित नहीं थी। ये आदर्श भारत के आधुनिक राजनीतिक आन्दोलनों की अनेक धाराओं में आज तक व्याप्त हैं। अतः राजनीति की जिस विरासत को हम धर्मबोध से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे थे, नेतृत्व और आत्मत्याग के आदर्श को भी हम उसी विरासत की धारा में मूलतः धर्मबोध से प्रेरित मान सकते हैं।
आधुनिक राजनीति की एक और धारा की चर्चा इस प्रसंग में करूँगा जो धर्मबोध से प्रेरित नहीं है। सम्प्रति इस प्रसंग को दक्षिण भारत के दो सांस्कृतिक इतिहासकारों―वेलचेरू नारायण राव और संजय सुब्रमण्यम ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि बारहवीं से चौदहवीं सदी में आंध्र प्रदेश के काकतीय राजाओं के काल में तेलुगू भाषा में लिखी गई एक किस्म की रचनाएँ मिलती हैं जिन्हें नीति साहित्य कहा जाता है। इन नीति रचनाओं का एक पुराना संकलन भी मिलता है, जिसे सकल-नीति-सम्मतमु नाम से जाना जाता है। पंद्रहवीं सदी के इस संकलन से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय आंध्र प्रदेश के इलाके में नीति साहित्य काफी प्रचलित रहा है।
नीति रचनाओं के लेखक कभी स्वयं राजा हैं और कभी राज परिषद का कोई सदस्य। नीति साहित्य का प्रधान लक्षण है कि इसकी विषय-वस्तु में धर्म या मोक्ष की बातें सर्वथा अनुपस्थित है। केवल अर्थ और काम ही इसका विषय है। इतना ही नहीं, अर्थ और काम की खोज में सफल होने के लिए किसी ईश्वरीय या दैवी शक्ति के कृपापात्र होने की बात भी इसमें नहीं है। धर्म शास्त्र का प्रसंग भी कहीं उठाया नहीं गया है। सकल-नीति-सम्मतमु नामक संकलन में सत्रह नीति ग्रन्थों से लगभग एक हजार उद्धरण एकत्रित किए गए हैं। लेकिन एक भी उद्धरण धर्मशास्त्रों से नहीं है। नारायण राव और सुब्रमण्यम ने इसीलिए कहा है कि नीति साहित्य पूरी तरह से लौकिक रचना है। यथार्थ के सांसारिक जगत में सफलता प्राप्त करने के कला-कौशलों को लेकर इसका कारोबार है। धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र का अन्तर यहाँ सुस्पष्ट और प्रतिष्ठित है।
नीति साहित्य के प्राचीन सूत्र यदि ढूँढ़े जाएँ तो स्वाभाविक है कि महाभारत और अर्थशास्त्र की चर्चा भी होगी।
नृसिंह प्रसाद भादुड़ी ने अपनी पुस्तक दण्डनीति में इस पर विस्तृत चर्चा की है। महाभारत में राजनीति के लिए ‘नीति’ शब्द का ही प्रयोग हुआ है। महाभारत और अर्थशास्त्र का विषय है राजधर्म। लेकिन राजधर्म का मूल उद्देश्य है राजा का अर्थलाभ। महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें राजा की स्वार्थपूर्ति के लिए ऐसे-ऐसे उपाय किए गए हैं कि सुनकर शायद मेकियाविली को भी शर्म आ जाए। लेकिन समग्रता में महाभारत में ‘अर्थ’ की तुलना में ‘धर्म’ को ही उच्चतर स्थान दिया गया है― कम से कम हम इसी तरह महाभारत को पढ़ने के अभ्यस्त हैं। नृसिंह प्रसाद कहते हैं कि सिर्फ राजा का अर्थलाभ, अर्थात् राज्य का सफल शासन ही नहीं, बल्कि जो धर्म राजा का भी धारण करता है, वहीं आकांक्षित अर्थ है। वैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि राजधर्म का मूल उद्देश्य ही है अर्थलाभ। हालाँकि अर्थशास्त्र में यह भी उल्लेख है कि धर्म और अर्थ में विरोध उत्पन्न होने पर धर्म को ही मानना होगा। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि ऐसी चेतावनी का कोई विशेष तात्पर्य नहीं है क्योंकि तब तक अर्थशास्त्र एक स्वतन्त्र विद्या के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। इस स्वतन्त्रता का आधार ही था धर्म और अर्थ में स्पष्ट अन्तर।
मध्ययुगीन भारत में, खास तौर से दक्षिण भारत में, कौटिल्य तथा अर्थशास्त्र की अन्य रचनाएँ प्रचलित थीं, इसके अनेक प्रमाण हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के जिस पाठ को आज हम पढ़ते हैं वह बीसवीं सदी की शुरुआत में मैसूर में आविष्कृत हुआ था। ऐसा परिपूर्ण संस्करण मध्ययुग के पाठकों के पास नहीं था, इतना निश्चित है।
लेकिन अन्य अनेक अर्थशास्त्रीय रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से उद्धृतियाँ और चर्चा बहुत मिलती है। विजय नगर के सम्राटों के शासनकाल में ऐसी अनेक रचनाएँ मिलती हैं जिनमें कौटिल्य और अन्य अर्थशास्त्रियों के वक्तव्य उद्धृत और चर्चित हुए हैं। नारायण राव और सुब्रमण्यम के लेख में उल्लेखनीय है कि काकतीय या बाद के विजय नगर साम्राज्य में नीति साहित्य संस्कृत भाषा में नहीं लिखे जा रहे थे, बल्कि स्थानीय तेलुगू या कन्नड़ भाषा में लिखे जा रहे थे। यह तथ्य इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्त्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि भाषा के माध्यम से धर्मशास्त्र के पर्वत से विशाल आभिजात्य को एक तरफ हटाकर नीति शास्त्रकार विमर्श की अपनी जमीन तैयार कर रहे थे।
नारायण राव कहते हैं कि आंध्र, कर्णाटक और उड़ीसा में इन लेखकों को ‘करणम’ कहते थे। इनमें अधिकांश नियोगी ब्राह्मण या कायस्थ थे। सभी कमोबेश संस्कृत के जानकार थे। लेकिन स्मृति या धर्मशास्त्र के पंडित बिलकुल नहीं थे। उनके पाठक संस्कृत के पंडित होंगे, ऐसा वे सोचते भी नहीं थे। वे आम तौर पर छोटे राजा या जमींदार के मंत्री या सलाहकार के रूप में काम करते थे। उनकी रचनाएँ भी छोटे-छोटे राज्यों के संचालन के कौशलों से सम्बन्धित थीं। उनके पाठक थे राजा, जमींदार, सम्भ्रान्त राजपुरुष और व्यापक करणम समुदाय।
वस्तुतः नीति साहित्य का लक्ष्य पाठक समुदाय सिर्फ राजा या राजपुत्र ही नहीं थे, कोई भी महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति जो अर्थ, यश, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान प्राप्त करना चाहता था, नीतिग्रन्थों का पाठ कर सदुपदेश ले सकता था। किस तरह के उपदेश होते थे नीतिशास्त्र के इन ग्रन्थों में? कुछ उपदेश प्रत्याशित थे। जैसे ‘‘जिस राजा में हुकूमत की क्षमता नहीं है, जो शासन नहीं कर सकता है वह मानो चित्रपट का राजा है। जो उसके आदेशों का पालन नहीं करता वह उसका पुत्र ही क्यों न हो अगर राजा उसे दंडित न करे तो उसका शासन स्थायी नहीं होता।’’ या फिर ‘‘किसी राजा के राज में यदि तराजू और बाटों का नियमित परीक्षण नहीं किया जाता है तो उस राज्य में चोरों का ही राज होता है।’’ कुछ उपदेश तो बहुत आधुनिक लगते हैं। जैसे ‘‘राजा के द्वारा शुल्क बढ़ा देने से विदेशी पण्य के आयात के बन्द होने का डर रहता है’’ अथवा ‘‘राजा के दफ्तर में जो चिट्ठियाँ आती हैं उनमें से किसी को भी बिना पढ़े फेंकना नहीं चाहिए। चिट्ठी-पत्री के माध्यम से ही राजा जान पाते हैं कि उनके राज्य में कहाँ, क्या हो रहा है।’’ चौंकाने लायक उपदेश इस प्रकार है― ‘‘जो राजा अपने कर्मचारी के साथ सिर्फ बदसलूकी करता है, वह कैसे उनसे वफादारी की माँग कर सकता है!’’ अथवा ‘‘जो राजा धनी है, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, बाहुबल में अतुलनीय है, लेकिन मूर्ख है, उस राजा का कर्मचारी उसे छोड़ अन्यत्र काम ढूँढ़ेगा, इसमें क्या शक है!’’ अथवा ‘‘बुरे राजा के चारों ओर बुद्धिमान पार्षद होने से ही हमेशा फल अच्छा नहीं होता है। लेकिन बुरे परामर्शदाता हों तो अच्छे राजा के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाता है।’’ राजा के प्रति निष्ठा को लेकर ऐसे सतर्क उपदेश धर्मशास्त्र की पोथियों में कभी नहीं मिल सकते।
उत्तर या पश्चिम भारत में करणम समुदाय से तुलनीय थे ‘मुंशी’। मुंशी, खास तौर से मुगल काल में, उसी तरह स्थानीय प्रशासकों, राजाओं, जमींदारों और अन्य राजपुरुषों के परामर्शदाता होते थे और राजनीति व इतिहास की पुस्तकें लिखते थे। मुंशी मुस्लिम भी होते थे और गैर मुस्लिम भी। राजकाज संचालन की नीतियाँ और ऐतिहासिक घटनाओं के विवेचन की कसौटी इस्लामी शास्त्र या शरीया नहीं होती थी। बल्कि सियासत का पाठ लिया जाता था अख़लाक नाम से परिचित एक रचना से। सम्प्रति इतिहासकार मुजफ़्फ़र आलम ने मुगलकालीन भारत में अख़लाक साहित्य के प्रभाव पर विस्तृत चर्चा की है। अख़लाक साहित्य का जन्म हुआ था ईरान और मध्य एशिया के देशों में। उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में प्राक्-इस्लामी फारस की दीर्घ विरासत थी। साथ ही समकालीन वास्तविक घटना जिसका प्रभाव पड़ा, वह थी मंगोलों का सामरिक वर्चस्व। ऐसे संधिकाल में नासिर-अल-दीन-अल-तुसी जैसे प्रमुख लेखकों ने राजनीति की चर्चा में इस्लामी कानून या शरीया से पूर्णतः अलग हटकर प्रश्न उठाया, ‘‘सुलतान के राज में जब अधिक संख्या में प्रजावर्ग मुस्लिम धर्मावलम्बी नहीं है तब राज्य के शासन में सुनीति अवलम्बन का उपाय क्या है?’’ फारस से यह साहित्य आया हिन्दुस्तान में। यहाँ भी तुर्की-अफ़गान सुल्तान या मुगल बादशाह के सामने यही समस्या थी। हिन्दुस्तान में भी नए सिरे से अख़लाक साहित्य लिखा जाने लगा। इस साहित्य में मुद्दे की बात यही थी कि राष्ट्र की नीति का प्रधान उद्देश्य है विभिन्न प्रजा समुदायों में सहयोग, समझौता और शान्ति स्थापित करना। मुजफ़फ़र आलम ने कहा है कि अख़लाक साहित्य में कहीं भी काफ़िर, कुफ्र, जिम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आदर्श सुल्तान का प्रधान गुण था ‘अक्ल’ अर्थात् अच्छे विवेचन की क्षमता, धर्मज्ञान या धर्म के प्रति निष्ठा नहीं। सुल्तान में यदि ‘अक्ल’ है तो ‘आदिल’ या न्याय मिलता है। न्याय की प्रतिष्ठा से राज्य और सम्मिलित प्रजा वर्ग का मंगल होता है।
नारायण राव और उनके सहयोगी लेखकों का अनुमान है कि चौदहवीं से अठारहवीं सदी, यहाँ तक कि उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक भारत की विभिन्न आंचलिक भाषाओं में नीति साहित्य का विकास हुआ है। बांग्ला भाषा में ठीक इसी तरह के साहित्य की जानकारी मुझे नहीं है। ‘करणम’ या ‘मुंशी’ समुदाय के बहुत से लोगों ने बांग्ला में साहित्य की रचना की है। सत्रहवीं सदी में आराकन राजसभा के अलावल से अठारहवीं सदी के सबसे गण्यमान्य कवि भारतचन्द्र राय तक ली। लेकिन पद्य या गद्य में कहीं भी नीति साहित्य या राजनीतिक इतिहास का वर्णन ढूँढ़ना मुश्किल है। शायद एकमात्र अपवाद है 1751 में रचित गंगाराम का महाराष्ट्र पुराण। उनके बारे में जितनी जानकारी है उससे उन्हें करणम समुदाय के अन्तर्गत माना जा सकता है। अलीवर्दी खान के शासन-काल में गंगाराम पूर्वी बंगाल के किसी जमींदारी के कार्य से मुर्शीदाबाद आकर महाराष्ट्र के अश्वारोही सेना के हमले में फँस गए थे। मराठों के साथ अलीवर्दी के युद्ध का वास्तविक और आश्यर्चजनक वर्णन मिलता है महाराष्ट्र पुराण में। लेकिन इस तरह के एकाध दृष्टान्त से बंगाल में नीति साहित्य का विमर्श नहीं बन सकता है। बांग्ला भाषा में तो नहीं लेकिन फारसी में बंगाल के इलाके में इस तरह का बहुत-सा साहित्य अठारहवीं सदी में लिखा गया है। कुमुकुम चट्टोपाध्याय ने बंगाल-बिहार के ऐसे इतिहास रचयिताओं के बारे में लिखा है। मुगल साम्राज्य के पतन के युग में ये लेखक-प्रशासक राजपुरुष राज्य शासन की पद्धति में अपने-आपको पारंगत और विशेषज्ञ मानते थे। सुल्तान या नवाब यदि शासन के कार्यों में दक्ष न हो या ध्यान न दे तो दरबारी मुंशियों का कर्त्तव्य हो जाता है कि राष्ट्र के कामकाज का सुचारु संचालन करें। ऐसे विचार अठारहवीं सदी में लिखे गए अनेक फारसी इतिहास ग्रन्थों में देखे जा सकते हैं। मैं एक इतिहासकार के उदाहरण से पूर्व में वर्णित नीति साहित्य के साथ अठारहवीं सदी के तारीख-साहित्य की समानताएँ ढूँढ़ने का प्रयास करूँगा।
गुलाम हुसैन ताबताबई के सियार-अल-मुताखरिन के बारे में बहुत से लोग जानते हैं। अठारहवीं सदी के बंगाल में इतिहास के समकालीन देशीय विमर्श का सबसे विख्यात निदर्शन है यह विराट ग्रन्थ। गुलाम हुसैन स्वयं राजकर्मचारी थे। बंगाल-बिहार के विभिन्न शासक नवाबों के परामर्शदाता के रूप में उन्होंने कार्य भी किया था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज कम्पनी के साहबों के साथ भी उनका मेलजोल था। तत्कालीन राजनीति की विभिन्न घटनाओं, कूटनीति, साजिश और युद्ध में वे स्वयं उपस्थित थे। इस असाधारण पुस्तक पर बहुत-सी बातें की जा सकती हैं। वस्तुतः मेरा अपना मत है कि भारत के आधुनिक इतिहास की रचना के क्रमविकास में सियार-अल-मुताखरिन और उसके लेखक गुलाम हुसैन का वास्तविक मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ है। खैर, आज के परिप्रेक्ष्य में जिन बातों का उल्लेख जरूरी है, सिर्फ उन्हीं बातों को आपके सामने पेश करता हूँ।
सियार-अल-मुताखरिन की पृष्ठभूमि में है मुगल साम्राज्य का पतन। पूरी अठारहवीं सदी में एक के बाद एक नालायक, अक्षम और अनाचारी बादशाहों की शोभायात्रा नजर आती है। बादशाह जब शासन चलाने में अक्षम है तब प्रशासन कैसे चलेगा? देश और प्रजा की रक्षा कौन करेगा? ऐसी स्थिति में साम्राज्य का भविष्य गहरी अनिश्चितता में डोलने लगता है। सुशासन होगा या नहीं, मानो यह देशवासियों के भाग्य पर निर्भर हो। लेकिन इस तरह सब कुछ किस्मत पर भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। अनिश्चय पर थोड़ी-सी लगाम कसी जा सकती है यदि इतिहास विद्या, कूटनीतिक बुद्धि और समीक्षा का सहारा लिया जाए। बादशाह में यदि ये गुण न हों तो मुगल सरकार के योग्य प्रशासक-राजपुरुषों को ही यह जिम्मेदारी निभानी होगी। गुलाम हुसैन द्वारा वर्णित अठारहवीं सदी के इतिहास के श्रेष्ठ नायक हैं हुसैन अली खान, अलीवर्दी खान, शुजा-उद-दौला, शिताब राय। इनमें से कोई भी वंशगत अधिकार से शासक नहीं बने थे। लेकिन व्यक्तिगत योग्यता, मनोबल, साहस और राजनीतिक दक्षता के गुणों के कारण उन्होंने राष्ट्र और प्रजा की रक्षा के लिए शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। राज्य में यदि चरम अनिश्चय और अराजकता व्याप्त हो जाए तो अयोग्य राजा को हटाकर योग्य प्रशासक सत्ता पर काबिज हो सकते हैं―धर्म की नजर से यह अन्याय है लेकिन नीति की युक्ति से यह समर्थन योग्य है।
अलीवर्दी खान अपने मालिक सरफराज खान के खिलाफ़ विद्रोह कर युद्व में उन्हें मारकर नवाब बने थे। गुलाम हुसैन ने स्वीकार किया है कि धर्म की नजर से यह काम चरम गुनाह है। लेकिन इतिहास विद्या के अनुसार बतौर शासक सरफराज की कोई योग्यता नहीं थी और कुछ दिन यदि वे सत्ता पर रहते तो देश और प्रजा की अवर्णनीय दुर्दशा की स्थिति बनती। अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल की जनता ने जितनी सुख और सुविधा का भोग किया था, उसके पहले और बाद में उतना नहीं किया था। यहाँ ध्यान देने लायक है कि ‘धर्मबोध’ तुलनात्मक ढंग से पृथक् होने के बावजूद राजनीति में भी नीति बोध मौजूद है। गुलाम हुसैन ने इस पर काफी चर्चा की है। शासक की व्यक्तिगत नैतिकता होनी चाहिए। कयामत के डर से नहीं बल्कि इस लोक में राजनीतिक परिणामों के बारे में सोचकर ही शासक के लिए उचित है कि वह व्यक्तिगत जीवन में दुर्नीति का प्रवेश न होने दे। जो शासक निष्ठावान और सच्चरित्र के रूप में परिचित है, दुश्मन भी उसकी बदनामी नहीं कर सकता है। अनिश्चयता और विपत्ति के दिनों में बहुत से लोग ऐसे शासकों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अलीवर्दी की मौत के बाद बंगाल की राजनीतिक इमारत भरभरा कर गिर गई थी। गुलाम हुसैन के अनुसार इसका एक मुख्य कारण है अलीवर्दी के बेटी-दामाद की चारित्रिक कुख्याति जिसकी वजह से साजिश की आग एक बार जो जल उठी, उसे बुझाने के लिए लोग मिलना दूभर हो गए। अशान्ति सर्वत्र व्याप्त हो गई।
गुलाम हुसैन ने देखा था कि विश्वास, वचनबद्धता और ईमानदारी के बन्धन से निर्मित मुगल राजनीति की बहुत दिनों से प्रचलित नैतिकता का विन्यास टूट रहा है। दो सौ सालों में प्रतिष्ठित प्रथा या नियम पर भी निश्चित रूप से आस्था रखना सम्भव नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में नई नैतिकता की पहली शर्त ही है आत्मरक्षा। अपने आत्मीय, स्वजनों, धनसम्पदा और आश्रितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन आज जो किया जाएगा, भविष्य में उसका फल भी भोगना होगा। इसीलिए अपनी स्वार्थ रक्षा में भी दूरदर्शिता का प्रयोजन है। आज जिससे छल-कपट या विश्वासघात किया, भविष्य में वह बदला ले सकता है, यह याद रखना चाहिए। लेकिन फिर इसीलिए आत्मीयता और ईमानदारी पर भरोसा न कर शासक के लिए उचित है कि वह योग्य कर्मचारी नियुक्त करें। सियार-अल-मुताखरिन में एक आश्चर्यजनक अंश है जहाँ गुलाम हुसैन अपने वृद्ध पिता हिदायत अली को राजनीति की नई संज्ञा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हिदायत अली आजीवन मुगल दरबार के आमिर रहे हैं। प्लासी के पट परिवर्तन के बाद वे शाहजादा अली गौहर के परामर्शदाता हो गए थे। वही अली गौहर अपनी सेना लेकर इलाहाबाद से बंगाल की ओर बढ़ रहे थे। इधर गुलाम हुसैन तब पटना के शासक रामनारायण के दरबार में थे। रामनारायण अंग्रेजों के सहयोगी थे। गुलाम हुसैन को हिदायत अली के पास भेजा गया कि वे समझा-बुझाकर अंग्रेजों के साथ सन्धि के लिए अली गौहर को राजी कर लें। गुलाम हुसैन ने पिता को समझाया कि बादशाही फौज चरम दुर्दशा की स्थिति में है और उसके सेनापति नालायक हैं। सीधे युद्ध में अंग्रेजों का जीतना तय है। शाहजादे के लिए यही उचित होगा कि वे अंग्रेजों से सन्धि कर लें और अगर ऐसा नहीं होता है तो हिदायत अली के लिए यही उचित है कि वे कम से कम शाहजादे की नौकरी से इस्तीफा देकर अपने प्राण और धन-सम्पत्ति की रक्षा करें। वृद्ध हिदायत अली ने पुत्र की बातें नहीं मानी। उन्होंने कहा कि तैमूर खानदान में किसी ने आज तक किसी के साथ दगा नहीं की है। वे अपने मालिक के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। भारत में राजनीतिक पट-परिवर्तन के युग में दो पीढ़ियों का यह विरोध मात्र धर्म और नीति के मौलिक अन्तर को ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता है।
इतने भिन्न-भिन्न प्रकार के नीति साहित्य की उपस्थिति अठारहवीं सदी में होने के बावजूद उन्नीसवीं सदी में उसका क्या हुआ? मेरा मानना है कि औपनिवेशिक आधुनिकता की जो लहर अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ बहने लगी थी, उसी से अंकुरित हुआ था ‘धर्मबोध’ का नवजागण। नीतिशास्त्र एकदम से दब गया। धर्मबोध के पुनरुत्थान के अनेक कारण हैं। एक कारण तो है पूरी अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी में प्राच्य शासन पद्धति की यूरोप के पंडित-पर्यवेक्षकों द्वारा समालोचना। उनका मत था कि प्राच्य के शासक ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट, शातिर और अत्याचारी थे। उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं है और नीति में कोई स्थिरता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, शासकों की दुर्नीति फैल गई है प्राच्य समाज के सभी स्तर के लोगों में। कोई भी सच नहीं बोलता है। जरा से फायदे के लिए लोग किसी भी तरह के छल का सहारा लेते हैं। इनके धर्मशास्त्र में कितनी ही अच्छी बातें क्यों न हों, व्यावहारिक जीवन में बचपन से ही ये लोग दुर्नीति सीखते हैं। अंग्रेज प्रशासक और ईसाई मिशनरियों के प्रबल आक्रमण के सामने पड़कर भारत के आधुनिक समाज-सुधारक यह प्रमाणित करने में व्यस्त हो गए कि दुर्नीति के ये लांछन झूठे हैं। छल, चातुर्य और स्वार्थ-सिद्धि नहीं, सत्य और धर्म ही है भारतीय समाज व्यवस्था का आदि और अकृत्रिम आदर्श। दुर्नीति और मिथ्याचार यदि कहीं आ भी गया है तो वो नितांत एक विच्युति है और उसका संशोधन ही है आधुनिक धर्म सुधार का उद्देश्य। दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिश शासनकाल में आधुनिक राजनीति का क्षेत्र उन्नीसवीं सदी में जितना अधिक प्रसारित होने लगा उतना ही प्रधानता पाने लगा प्रजा का स्वत्व और प्रजा के अधिकार का प्रश्न। प्रश्न किया गया कि यदि प्रजा की सम्मति ही आधुनिक राष्ट्र की नैतिक बुनियाद है तो फिर विदेशी शासन न्यायसंगत कैसे हो सकता है? असली मुद्दा क्या है―त्रुटिहीन प्रशासन या न्यायोचित सार्वभौमिक सत्ता?
राष्ट्रवाद के युग में कैसे धर्म और नीति का सम्बन्ध नए सिरे से बना, यह दिखाने के लिए 1876 में प्रकाशित राष्ट्रनीति सम्बन्धी एक पुस्तक की चर्चा उदाहरणस्वरूप कर रहा हूँ। पुस्तक का नाम है व्यवहार दर्शन और लेखक हैं―आनन्दचन्द्र मित्र। शीर्षक के नीचे ही अंग्रेजी में लिखा है एन इंट्रोडक्शन टु दि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। पुस्तक पर अन्य प्रसंग में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। आनंदचन्द्र मयमनसिंह जिले में शिक्षक थे। ब्रह्म समाज के सदस्य और शिवनाथ शास्त्री के शिष्य समान थे। प्राचीन भारत के नीति साहित्य से आनंदचन्द्र अच्छी तरह वाकिफ थे। लेकिन आधुनिक यूरोप के आदर्श को सामने रखकर वे एक नए सिद्धांत की खोज में उतरे, जिसको उन्होंने साइंस ऑफ पॉलिटिक्स कहा और उसका बांग्ला नाम रखा व्यवहार दर्शन। साइंस को ढूँढ़ते हुए आनंदचन्द्र ने पाया कि ‘भारत में व्यवहार दर्शन नाम का कोई दर्शन नहीं है।’ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि साधारणतः भारत में दर्शन की चर्चा ही निष्प्रभ है। ‘‘सभी स्वीकार करेंगे कि भारतवर्षीय लोग जितने धर्मभीरु हैं, यहाँ के निवासियों में जितनी भक्ति है, और यहाँ का साहित्य जितना हृदयग्राही है, उतना और कहीं नहीं है। इससे यही प्रमाणित होता है कि विश्वास, भक्ति, स्नेह, वीरता और सौन्दर्यानुराग की वृत्तियाँ और उनका आधार हृदय भारतवासियों में अत्यन्त प्रबल है। यह हृदय-प्रवणता ही इस देश में दर्शनशास्त्र की समुचित चर्चा न होने का मूल कारण है।’’ अतः साइंस ऑफ पॉलिटिक्स भारत में ढूँढ़ना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीति की चर्चा ही नहीं थी। ‘भारत में व्यवहार दर्शन की चर्चा न होने के बावजूद राजनीति की उन्नति बहुत अच्छे ढंग से हुई थी।’ यहाँ आनंदचन्द्र की वर्णना में धर्म और नीति का अन्तर जैसे मिट गया है, इस पर ध्यान दें: ‘‘व्यवहार दर्शन का समुचित अनुशीलन न होने की वजह से इस देश में सभी विषय धर्मशास्त्र के अन्तर्गत रखे गए थे। भारतवर्ष में राजा साक्षात् धर्म का अवतार है। वास्तविक भारतवर्ष में राजा और प्रजा के कर्तव्यों को लेकर कुछ नीतिकथाओं का सृजन हुआ था, उन्हीं को कहता हूँ भारत की राजनीति। इन नीतियों में से बहुत-सी नीतियाँ व्यवहार दर्शन से प्रभावित और नियंत्रित नहीं हैं लेकिन फिर भी उनमें ऐसी गहराई और उच्च भाव हैं कि पाठ से आनंद जन्म लेता है एवं उसमें चिन्तनशीलता का भी विलक्षण परिचय है।’’ लेकिन यहाँ भी ‘धर्मभाव’ घुसकर सब मिट्टी में मिला रहा है। ‘‘उन सभी ग्रन्थों में राज्य शासन के विषय पर प्रत्येक प्रजा के अभिमत को बेकार कर राजा को ईश्वर मान पूजा करने का उपदेश देकर और ब्राह्मणादि श्रेष्ठ वर्णों का माहात्म्य घोषित कर उसके मूल पर ही कुठाराघात किया गया है।’’
दरअसल आनंदचन्द्र जिस राजनीति-दर्शन की खोज कर रहे थे, उसके मूल में था प्रजा का अधिकार। राष्ट्र की सार्वभौमिक सत्ता प्रजा के अधिकार की बुनियाद पर प्रतिष्ठित है, यह धारणा उन्हें आधुनिक यूरोप के दर्शन से प्राप्त हुई है। ‘‘यदि प्रजाशक्ति, अर्थात् साधारण जन के मत पर निर्भर होकर और प्रजा की सत्ता अर्थात् साधारण जन का मंगल बरकरार रखते हुए किसी राज्य का गठन होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, लेकिन मानना होगा कि व्यवहार दर्शन के अनुसार राज्य ही वास्तविक राज्य है। और ऐसी शासन-प्रणाली ही सर्वोत्कृष्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है।’’ वस्तुतः व्यवहार दर्शन या साइंस के अनुसार वास्तविक राज्य किसे कहते हैं, इस मामले में आनंदचन्द्र को कोई शक नहीं था। पराधीन भारतवासी होकर भी 1876 में उन्होंने बिना किसी दुविधा के परिभाषित किया― ‘‘समग्र प्रजाशक्ति जिससे आपस में सम्बन्धित होती है, जिसका आश्रय लेती है, जिसके द्वारा नियमित होती है, और जिसका अतिक्रम नहीं कर सकती है उसे राजा कहते हैं। आम प्रजा/समग्र शक्ति का प्रतिनिधि एक अथवा कतिपय राजा है।’’ इसके बाद की परिभाषा निश्चित है― ‘‘जिस समाज में राजशक्ति और प्रजाशक्ति सम्मिलित होकर कार्य करती है, उसे राज्य कहते हैं। समग्र प्रजाशक्ति सम्मिलित होकर राजशक्ति को बनाती है और उसी राजशक्ति के वशीभूत होकर स्वयं भी उसका बाध्य हो जाती है। राजशक्ति भी प्रजाशक्ति के ऐसे नियंत्रण में होती है कि किसी भी तरह प्रजाशक्ति की उपेक्षा कर कोई कार्य नहीं कर सकती है। जिस समाज में इस तरह कार्य सम्पन्न होता है वही राज्य है।’’ प्रजाशक्ति के वशीभूत होकर राजशक्ति कार्य कैसे करेगी? ‘‘अधिकांश का मत ही साधारण मत है और उस मतानुसार कार्य ही साधारण जन के मंगल का कार्य है।’’ आनंदचन्द्र ने यहाँ तक स्पष्ट किया कि दर्शन द्वारा अनुमोदित वास्तविक राज्य की राजशक्ति आदिकाल का राजा नहीं है बल्कि आधुनिक प्रजातन्त्र है। उन्होंने घोषणा की, ‘‘आजकल दिन-प्रतिदिन जिस तरह साधारण मत का प्रादुर्भाव हो रहा है, भरोसा किया जा सकता है कि जल्द ही सभी प्रतिष्ठित राज पद ध्वंस हो जाएँगे।’’ आधुनिक राजनीति में धर्म की भूमिका को लेकर आनंदचन्द्र का संदेह अत्यन्त गहरा है। ‘‘पित्त के सहयोग से आहार्य वस्तु पचकर रक्त की सहायता से शरीर को जीवित रखती है। उसी तरह धर्म के बिना राष्ट्रीय जीवन असम्भव है और व्यवहार दर्शन के अनुशीलन से धर्मोन्मत्तता और धर्मान्धता पर, जिससे समाज का हित होता है, नियंत्रण कर समाज को स्वाभाविक रखा जाता है।’’ आनंदचन्द्र जानते थे कि धर्मभाव की प्रबलता से एक तरह के उन्माद की सृष्टि की जा सकती है और उसकी ताकत से कोई राष्ट्र युद्ध जीत सकता है, या कोई बड़ी राष्ट्रीय सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन यह सफलता सामयिक ही है। ‘‘हम उसे राष्ट्रीय जीवन नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं राष्ट्रीय जीवन का विकार। रक्त की अधिकता से हिस्टीरिया होकर कोई व्यक्ति जैसे अकेले ही पाँच-छह जनों के समान बल प्रदर्शित करता है, वैसा ही वे भी करते हैं। लेकिन ऐसा बल बहुत समय तक नहीं टिका, और परिणाम अशुभ ही हुआ। मुसलमानों का दिग्विजय इसी का एक अच्छा प्रमाण है।’’ मुश्किल है कि धर्म की प्रबलता पर संशय होने के बावजूद नीति पर उनकी आस्था नहीं है। ‘‘भारतवर्षीय लोग इस वक्त सिर्फ स्वार्थ को लेकर व्यस्त हैं। पड़ोसी का सर्वनाश कर अपना पेट भरने के लिए कृतसंकल्प हैं। ऐसा होने के दो कारण हैं। एक धर्मज्ञान और दूसरे व्यवहार दर्शन चर्चा का अभाव।’’ आनंदचन्द्र को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। दरअसल आधुनिक राष्ट्रीय राजनीति के उन्मेष के काल में धर्म और नीति का स्वातंत्रय, या धर्म-भाव निरपेक्ष-नीति की यथार्थता निर्दिष्ट करना उनके लिए सम्भव नहीं था। जिस प्रजाशक्ति के उत्थान की उम्मीद से वे व्यवहार दर्शन का प्रसार चाह रहे थे, विदेशी साम्राज्य के साथ संग्राम कर राष्ट्रीय सार्वभौमिक सत्ता हासिल करने के अलावा उस प्रजाशक्ति के साथ राजशक्ति का मिलन सम्भव नहीं था। वह लड़ाई सार्वभौमिक सत्ता की लड़ाई है। उमसें धर्मभाव और आत्मत्याग का मूल्य कितना अधिक है, वह शुरू में ही कह चुका हूँ। दैनंदिन प्रशासन के जिस जटिल, विन्यस्त, छोटी-मोटी प्रक्रियाओं में नीतिशास्त्रा की आवाजाही है, राष्ट्रीय जन प्रतिरोधी संगठन के युग में उसका मूल्य बहुत ही कम था। इसीलिए बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन की शुरुआत में ही वंदेमातरम् पत्रिका घोषणा कर सकी थी― ‘‘आज का नया आन्दोलन खराब शासन के खिलाफ़ नहीं है। यह ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रतिवाद है। यह हुकूमत किस तरह इस्तेमाल हो रही हैदृअच्छी तरह से या बुरी तरह से, मंगल के उद्देश्य या अमंगल के उद्देश्य सेदृयह अति तुच्छ और अवांतर प्रश्न है।’’ प्रजाशक्ति/सार्वभौमिक सत्ता की लड़ाई तभी शुरू हो गई थी। धर्म और नीति के स्वातंत्रय की प्रतिष्ठा का मौका प्रायः था ही नहीं, ऐसा कहा जा सकता है।
मेरा मानना है कि यह स्थिति बरकरार रही 1975 से 1977 तक, आपातकाल के विरुद्ध आन्दोलन तक। 1980 के दशक तक बीसवीं सदी के भारत में राजनीतिक आन्दोलन का एक नक्शा तय था। उसमें मतादर्श के महत्त्व को लेकर गर्व था, साध्य और साधन की समानता पर बहस थी। नेताओं की लोकप्रियता का आधार थादृउनके त्याग के जीवन का वृत्तांत। पिछले बीस सालों में एक दूसरा नक्शा लोकतान्त्रिक राजनीति में बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। मैं कहूँगा, प्रजा की सत्ता जितनी ज्यादा सार्वभौमिक सत्ता की लड़ाई से प्रशासनिकता की दैनंदिन मोलभाव का विषय बनती जा रही है, उतना ही धर्म के स्थान पर नीति का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। पिछले दो सौ सालों तक जो दबा हुआ था, प्रादेशिक राजनीति के लोकतान्त्रिक मैदान में वह अब दम्भ के साथ विचरण कर रहा है। अब तक इस नई राजनीति का कोई शास्त्र तैयार नहीं हुआ है। लेकिन धर्मबोध न होने पर दृष्टांत के सहारे इस नए नीतिबोध के लक्षणों को दिखाने की कोशिश करूँगा।
आपातकाल से ही बात शुरू की जाए। आजादी के बाद के भारतीय राजनीतिक इतिहास के क्रम विकास में आपातकाल कई कारणों से एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। आम तौर पर आपातकाल से हम समझते हैं इंदिरा गांधी की तानाशाही, संवैधानिक और लोकतान्त्रिाक व्यवस्था की आवाज को दबाना, विरोधी दल के नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, संजय गांधी का बीस सूत्राीय (या छह सूत्रीय) कार्यक्रम, नसबंदी और दिल्ली में बस्तियों का विस्थापन। और समझते हैं 1977 का चुनाव जिसमें अविश्वसनीय ढंग से भारत के मतदाताओं ने केवल अपने मतों की ताकत से अप्रतिहत क्षमता की अधिकारी इंदिरा कांग्रेस को सत्ता से हटाया था। राष्ट्रशक्ति का अत्याचार और जनता का प्रतिरोध―यही है आपातकाल की प्रचलित कहानी। मुझे खुद याद है, धर्मयुद्ध, कौरव-पांडवों की लड़ाई, आदि बातें तब इंदिरा विरोधी राजनीतिज्ञों से हमेशा सुनने को मिलती थीं। वे ये बातें कपटता से कह रहे थे, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। हमारे लिए आपातकाल एक असाधारण व्यतिक्रमी घटना है। लेकिन उस डेढ़ साल में भी अनगिनत लोगों ने अपने दैनंदिन जीवन का निर्वाह किया था। यहाँ तक कि जिन्हें हम आपातकाल के पीड़ित लोग मानते हैं, यानी दिल्ली की झुग्गी- झोंपड़ी के रहवासी, उनका भी रोजमर्रा का एक जीवन था सन् 1975 या 1976 में। वे कोई राजनीतिक नायक नहीं थे। उनमें से अधिकांश तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं थे। उनके लिए आपातकाल का क्या तात्पर्य है? इस मुद्दे पर एक शोध ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है, मानवशास्त्री एमा टारलो ने जिसे लिखा है। उन्होंने आपातकाल के बीस-बाइस साल बाद पीड़ित व्यक्तियों से पूछा था कि उनके लिए आपातकाल का क्या अर्थ है? उत्तर चौंकाने लायक है।
दिल्ली में यमुनापार स्थित वेलकम कॉलोनी एक सरकारी आवास परियोजना है। आपातकाल में विस्थापित लोगों को यहाँ जमीन दी गई थी। सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है कि एक बहुत बड़े हिस्से को नसबंदी प्रमाण पत्र के विनिमय पर जमीन दी गई थी। परंतु नियमानुसार झुग्गी-झोपड़ी से सरकार द्वारा विस्थापित होने पर ही किसी को इस कॉलोनी में जमीन पाने का अधिकार था। लेकिन दस्तावेज में दिख रहा है कि बहुत से जमीन मालिक विस्थापित नहीं थे। किसी विस्थापित व्यक्ति के नाम से, उसके कागज दिखाकर, उन्हें जमीन मिली है। अर्थात् विस्थापन का प्रमाण जो सरकारी कागज का टुकड़ा है, वह भी बिकने लायक है और उसका एक विनिमय मूल्य है। विस्थापित व्यक्ति को हरजाने के रूप में सरकारी आवासन परियोजना में एक टुकड़ा जमीन मिला है, लेकिन उस टुकड़े के उपयुक्त इस्तेमाल की क्षमता भी उसमें नहीं है। इसीलिए विस्थापन का प्रमाण-पत्र किसी को बेचकर फिर वह लौट गया है किसी झुग्गी-झोंपड़ी में। जिसने यह प्रमाण-पत्र खरीदा, वह भी एक गरीब बस्ती निवासी ही है। उसने सरकारी कर्मचारी को दस्तूर के मुताबिक खुश करके दूसरे के नाम से शुल्क जमा कर जमीन को प्राप्त किया। इसके ऊपर है नसबंदी का प्रमाण पत्र। आपातकाल में इसके विनिमय में भी जमीन मिलती थी। या तो खुद स्टरिलाइजेशन ऑपरेशन कराने पर या किसी दूसरे को प्रेरित करने पर प्रमाण पत्र मिलता था। ये प्रमाण पत्र भी बड़े पैमाने पर बेचे और खरीदे गए, इसके भी प्रमाण हैं।
आश्चर्य की बात है कि यमुनापार कॉलोनी के बहुत से रहवासियों के लिए आपातकाल की स्मृति अत्याचार की स्मृति नहीं है। उल्टे शासन व्यवस्था और बाजार के साथ उनके दैनंदिन मुकाबले में कुछ अद्भुत मौकापरस्ती की स्मृतियाँ हैं। एक महिला ने जैसे कहा, ‘‘उस समय मैंने ऑपरेशन करा लिया था। उसी से सरकारी दफ्तर में सफाई कर्मचारी की पक्की नौकरी मिल गई है। आजकल तो ऑपरेशन कराओ तो सिर्फ एक घड़ी या इलेक्ट्रिक पंखा देते हैं, इसीलिए कोई ऑपरेशन नहीं कराता है।’’ एमा टारलो ने अपने शोध में एक विस्मयकारी महिला को खोज निकाला है। यह महिला अपनी झोंपड़ी से विस्थापित होकर अस्वस्थ पति को लेकर वेलकम कॉलोनी के परिचित के यहाँ पनाह लेती है। कुछ दिनों बाद उस मकान-मालिक से उसका विवाह हुआ, ऐसा शपथ-पत्र पेश कर मकान अपने नाम लिखवा लेती है। कुछ दिन बाद देखा जाता है कि मकान के असली मालिक सड़क पर थे और पनाह लेने वाली महिला मकान मालकिन बन चुकी थी। यह महिला कॉलोनी के प्रशासनिक नियम कानून के दायरे से अपने स्वार्थ सिद्धि के मौके निकालने में सिद्धहस्त हो चुकी थी। इस मामले में वह दूसरों को सलाह भी देती थी। कहने की जरूरत नहीं, पारिश्रमिक लेकर!
आप कह सकते हैं कि इसके साथ राजनीति का क्या सम्बन्ध है? ऐसे किस्से तो किसी भी समय, किसी भी देश में किसी भी राजनीतिक परिवेश में मिल सकते हैं। इससे आपातकाल की राजनीति समझने में हमें क्या सहयोग मिल रहा है? उत्तर देते हुए कहूँगा कि महिला की यह कहानी राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों के साथ गरीब शहरवासी लोगों के दैनंदिन जीवन के गहरे सम्पर्क की सूचक है। और यह भारतीय राष्ट्र के इतिहास में नया है। कई लोगों को याद होगा कि सबऑल्टर्न स्टडीज के शुरुआती दौर में औपनिवेशिक काल में किसान विद्रोह के तारतम्य में अनेक इतिहासकारों ने दर्शाया था कि कृषक चेतना में राष्ट्र बहुत दूर की चीज है। मैजिस्ट्रेट, अदालत, थाना, अस्पताल आदि से किसान कोई सम्बन्ध न रखने की स्थिति में ही खुश रहते थे। उसी तरह शहर के गरीब मजदूरों का भी राष्ट्र के साथ सम्पर्क आम तौर पर दूर का था। सम्पर्क यदि हुआ भी तो मात्र सामयिक हुआ। इसीलिए दीपेश चक्रवर्ती ने बीसवीं सदी के शुरुआती दौर में औद्योगिक श्रमिक चेतना को भी मुख्यतः कृषक चेतना के आधार पर ही देखना चाहा था। आजादी के बाद विकासमूलक कार्य प्रारम्भ हो गए थे लेकिन 1970 के दशक के पूर्व बृहत्तर जन समुदाय तक सरकारी परियोजनाओं के माध्यम से निर्दिष्ट प्रशासनिक उपाय द्वारा अवसर और सुविधाएँ पहुँचाने के कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इंदिरा गांधी की ‘गरीबी हटाओ’ आदि परियोजनाओं से यह कार्य शुरू होता है। मैं कहूँगा, आपातकाल का बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रशासनिकता के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। इसीलिए वेलकम कॉलोनी के बाशिंदों के साथ आपातकालीन प्रशासन की रोजमर्रा की लेन-देन की कहानी मुझे बेहद तत्त्वपूर्ण लगती है। पिछले बीस-पच्चीस सालों में हुए व्यापक और गहरे प्रशासनिक कार्यों के फलस्वरूप उद्भूत नई राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में मैंने अन्यत्र विस्तृत चर्चा की है। उसे नए सिरे से यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद दिलाने लायक दो बातें सिर्फ आपके सामने रखूँगा।
एक, प्रशासनिक कार्यों के कानून के मुताबिक कौन-सा कार्य वैध है और कौन-सा कार्य अवैध, यह अन्तर अस्पष्ट हो गया है। झुग्गी-झोंपड़ी के रहवासियों के रहने का स्थान ही अवैध है। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी से विस्थापित हुआ और उसे विस्थापन का सरकारी प्रमाण पत्र मिला वैसे ही पूर्ण वैधता के साथ उसे ‘अवैध- दखलदार’ का तमगा मिल गया। अब इस तमगे को बेचा, खरीदा जा सकता है। लग सकता है कि यह खरीद-फरोख़्त अवैध है। लेकिन प्रशासन ‘वैध तमगे’ वाले अवैध मालिक को स्वीकृति प्रदान करने को राजी हो सकता है। इसके पक्ष में उत्कृष्ट प्रशासनिक युक्ति है। जैसे, यदि प्राप्त जमीन पर विस्थापित लोगों की मकान बनाने की क्षमता नहीं है तो वे जमीन किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं। अर्थात्, कॉलोनी की जमीन में कालाबाजारी शुरू। इसके प्रशासनिक झमेले बहुत ज्यादा हैं। इससे ज्यादा अच्छा यह स्वीकार कर लेना है कि वैध प्राप्तकर्ताओं में जो जमीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, वे अपने विस्थापन का प्रमाण-पत्र ही बेच दें। इसमें कोई नुकसान नहीं है। जमीन उन्हीं के हाथों रहेगी जो उस पर मकान बना सकते हैं। इसके बाद किसे वैध कहेंगे और किसे अवैध? प्रशासनिकता की युक्ति के ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएँगे।
दूसरी बात है, प्रशासनिकता की युक्ति से क्या स्वेच्छा से है और कौन सा जबरदस्ती, इसकी मीमांसा करना अत्यन्त जटिल है। सामान्यतः हम जानते हैं कि प्रशासनिकता का नियम है कि पारितोषिक और जुर्माने के जरिए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास करो, जबरदस्ती मत करो। इसी युक्ति से विस्थापित कोई व्यक्ति यदि बदले में सरकारी जमीन का दखल करता है, तो सरकारी परिभाषा में यह हो जाता है स्वेच्छा से पुनर्वास। कह सकते हैं कि विस्थापन तो जबरदस्ती हुआ था। बिलकुल ठीक। लेकिन विस्थापन से पहले वह था ‘अवैध दखलदार’। विस्थापन के बाद जमीन पाकर वही हो गया ‘वैध मालिक’। तो फिर विस्थापन को अत्याचार कहा जाएगा क्या? वेलकम कॉलोनी के बहुत से रहवासियों ने बुलडोजर से अपनी झुग्गी-झोंपड़ी के ध्वंस की मार्मिक कहानी का विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन जिन्होंने जमीन पाकर घर बनाया है उन्होंने बेहिचक सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है क्योंकि वे आज वैध आवास के मालिक हैं। नसबंदी के बारे में भी यही कहा जा सकता है। वहाँ भी पारितोषिक और जुर्माने का नियम था। जिस दिहाड़ी मजदूर ने सरकारी नौकरी के लोभ में नसबंदी कराई, क्या उसने अपनी विचार बुद्धि से नफे-नुकसान का हिसाब लगाकर स्वेच्छा से निर्णय लिया, या उस पर जबरदस्ती की गई? कहना मुश्किल इसीलिए है कि क्योंकि जिनकी पसंद-नापसंद का क्षेत्र इतना सीमित है कि उनके निर्णय के पीछे परिस्थितियों का अन्यायपूर्ण दबाव है कि नहीं, इसकी विवेचना कठिन है।
बृहत्तर राजनीतिक इतिहास में आपातकाल के तात्पर्य पर बहुत लिखा गया है, मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है। उस इतिहास में आपातकाल एक रोज की घटना नहीं, असाधारण घटना है। आपातकाल के विरुद्ध प्रतिरोध और उसके परिणाम में इंदिरा कांग्रेस की हार की कहानी में धर्मयुद्ध का स्पर्श होगा ही। इस इतिहास के सभी पात्र नायक हैं अथवा खलनायक। यहाँ तक कि नामहीन, अवयवहीन जन समुदाय, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है भारत की मतदाता जनता, वह तो महानायक है। लेकिन राष्ट्रीय जीवन की असाधारण घटना से हटकर व्यक्तिगत जीवन के वास्तविक रोजनामचे पर उतर आने से, मेरा कहना है, एक दूसरी प्रक्रिया की खोज होती है। वह प्रक्रिया है भारतीय राष्ट्र के प्रशासनिकता (सरकारियत) के विस्तार की प्रक्रिया। इस इतिहास में आपातकाल कोई व्यतिक्रम नहीं है। अथवा और सावधानी से कहा जाए तो व्यतिक्रम सिर्फ इस मामले में है कि पारितोषिक और जुर्माने के सुविन्यस्त, लचीली व्यवस्था के माध्यम से, संवैधानिक ढाँचे को अक्षत रखते हुए पुलिस सेना की जबरदस्ती के बिना कैसे प्रशासनिक कार्यक्रम को वास्तव रूप दिया जा सके, आपातकाल के अनुभव ने उसकी सीमाएँ निर्दिष्ट कर दी थीं। बस्तियों के विस्थापन और नसबंदी से जो घोटाले हुए उनसे प्रशासन ने शिक्षा ली। कौन-सा प्रशासनिक कौशल कार्यकारी है, और कौन सा नहीं, इस पर और सूक्ष्म, और सुचिंतित प्रक्रिया आविष्कृत हुई। आज के भारतवर्ष के प्रशासक एक आवाज में कहेंगे, आपातकाल फिर कभी भी लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन बस्तियों का विस्थापन बन्द नहीं हुआ है और परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी जारी है, सिर्फ कौशलों में अन्तर आया है।
वेलकम कॉलोनी के बारे में एक और बात कहना जरूरी है। यहाँ के लगभग सभी रहवासियों को आपातकाल की जोर-जबरदस्ती की याद है। बहुत से भुक्तभोगी भी हैं। लेकिन उनसे बात कर एमा टारलो ने पाया कि इंदिरा गांधी उनके लिए प्रायः देवता के समतुल्य हैं। हम जानते हैं कि 1980 के बाद से लगातार दिल्ली के यमुनापार कॉलोनी के रहवासी कांग्रेस के समर्थक रहे हैं। इंदिरा के तानाशाह कुशासन के जो शिकार हैं, वही कैसे इंदिरा के निष्ठावान भक्त हो जाते हैं? उनसे पूछो तो कहते हैं कि ‘‘आपातकाल में अत्याचार जरूर हुआ था। लेकिन वह सब किया था सरकारी अधिकारी और निचले स्तर के कांग्रेसी गुंडों ने। इसके लिए इंदिरा गांधी को दोष देने से क्या लाभ? इंदिरा गांधी ने गरीबों के लिए जो किया, देश के लिए जो किया, उसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है उनका बलिदान, वे देवता हैं।’’ समझा जा सकता है, लोकमानस में इंदिरा गांधी की छवि को रोजमर्रा के प्रशासनिक क्षेत्र से बहुत ऊपर उठाकर एक पौराणिक जगत में स्थापित किया गया है। वे रोज की जिंदगी की नीति से ऊपर हैं। वे अब ‘धर्म’ की प्रतीक हैं।
नृसिंह प्रसाद भादुड़ी की पुस्तक दंडनीति की चर्चा मैंने पहले की है। उन्होंने एक और बात हमें याद दिलाई है। ‘नीति’ और ‘नेता’ दोनों ही शब्दों की उत्पत्ति है ‘नी’ धातु से जिसका अर्थ है ‘खींचकर ले जाना’। अर्थात् लक्ष्य की ओर वह खींचकर ले जाए, वही नेता है और जिस विद्या की सहायता से जो खींचकर ले जाए वही नीति है। निर्दिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना ही प्रशासनिकता की राजनीति है। इसीलिए इस राजनीति में जो नेता है, उनका ‘धर्मज्ञान’ भले ही न हो, नीतिविद्या में उन्हें दक्ष होना ही होगा। मैं कहूँगा पिछले बीस-पच्चीस सालों में भारत की लोकतान्त्रिाक राजनीति में जो नए नेता दिख रहे हैं, वे नीतिविद्या में पारंगत हैं। उनसे ‘धर्मबोध’ की उम्मीद निरर्थक है। स्वतन्त्रता संग्राम या वामपंथी आन्दोलन के विगत युग के नेताओं से तुलना करने पर आज के नेता स्वार्थी, मौकापरस्त, लोभी और भोगी नजर आते हैं। राजनीति के निचले स्तर के ऐसे स्थानीय नेताओं को हम दलाल, बिचौलिया, टाउट आदि नामों से अलंकृत करते हैं। लेकिन आम जनता को जब अपने दैनिक जीवन में प्रशासनिक पद्धति से जूझना होता है, तब वे ऐसे नेताओं के पास जाएगी ही, इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वही नेता जब काम नहीं करा पाता है तो उसे छोड़ दूसरे को नेता बनाया जाएगा, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है।
एक और प्रसंग है जिस पर कभी और विस्तार से चर्चा की जरूरत है। ‘धर्मबोध’ प्रेरित राजनीति में अस्त्र उठाने और बल प्रयोग की भूमिका बहुत बड़ी है। आधुनिक जगत में सभी युद्धों के पीछे किसी ईमानदार, न्यायोचित और मंगलकामी उद्देश्य की घोषणा की गई है। अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का सशस्त्र संग्राम आज भी अनेक लोगों को न्यायोचित लगता है। भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में इस मुद्दे पर बहुत वाद-विवाद हुआ है। उन्नीसवीं-बीसवीं सदी में जैसे बार-बार भगवद्गीता से उद्धरण दिए जाते थे अंग्रेज शासन के खिलाफ धर्मयुद्ध को न्यायोचित ठहराने के लिए। यहाँ तक कि गांधी द्वारा संचालित अहिंसक सत्याग्रह में बलप्रयोग की भूमिका नहीं थी, ऐसा सोचना गलत होगा। अहिंसक सत्याग्रही के कानून तोड़ने का मुख्य उद्देश्य ही था राष्ट्र शक्ति की हिंसा को अपने शरीर में वहन करना। वस्तुतः राष्ट्र को हिंसा का सहारा लेने के लिए आमंत्रित करना। राष्ट्र जब बल प्रयोग के लिए राजी नहीं होता था तब सत्याग्रही का चरम अस्त्र था आमरण अनशन, अर्थात् अपने शरीर पर स्वयं बल प्रयोग करना और राष्ट्र को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना। धर्मबोध प्रेरित राजनीति के साथ बल प्रयोग का सम्बन्ध मेरे मत से अविच्छिन्न है।
‘धर्म’ छोड़ ‘नीति’ के जगत में आएँ तो देखेंगे कि यहाँ भी हिंसा की भूमिका है। लेकिन ‘नीति’ के लिए मुख्यतः विचारणीय है उपयोगिता और कार्यकारिता। उतना ही बलप्रयोग नीतिसम्मत है जो इच्छित लक्ष्य तक पहुँचाने में कारगर हो। इसी नीति के आधार पर आधुनिक युद्धविद्या में है प्रिसिजन बॉम्बिंग का प्रकरण जिसका उद्देश्य है आस-पास कोई नुकसान न पहुँचाते हुए, कौलेटेरल डैमेज को कम से कम रखते हुए लक्ष्य वस्तु पर हमला करना। आज के भारत में प्रजाशक्ति का जो नया ज्वार उठा है उसमें भी नियंत्रित बलप्रयोग हमेशा ही हो रहा है। कई बार बलप्रयोग राष्ट्रीय तन्त्र के खिलाफ है तो कई बार राष्ट्रशक्ति के पक्ष में भी है। राष्ट्रीय तन्त्र से मुकाबला करने के लिए अनेक जन समुदाय हिंसा का सहारा अक्सर लेते हैं। हिसाब ऐसा है कि एक दफा हिंसा-अराजकता होने पर राष्ट्र शक्ति चेतेगी और प्रशासनिक व्यवस्था की नेकनजर में मुद्दे आएँगे। उत्तर-पूर्व भारत के कई इलाकों में प्रतिरोध का यही नक्शा पिछले तीन दशक से दिख रहा है। कितना बल प्रयोग कारगर है, कितना होने से ज्यादती होगी, इसका भी कोई निर्दिष्ट नियम नहीं है। साम्प्रदायिक दंगे अनेक बार योजनाबद्ध ढंग से शुरू किए जाते हैं या दंगा शुरू होने पर पुलिस या सेना से तभी नहीं रोका जाता है, कुछ समय तक चलने दिया जाता है। निर्णय लेने का यह तरीका भी योजनाबद्व होता है, यह हम जानते हैं। कभी-कभी योजनाबद्ध हिंसा का तात्कालिक लाभ मिलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह नीतिसम्मत नहीं था, ज्यादती हो गई थी। जैसे गुजरात में मुस्लिम संहार के बाद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता। लेकिन आज सुनते हैं मुश्किल में पड़कर नरेन्द्र मोदी भी कह रहे है कि वह कार्य ठीक नहीं था, ज्यादती हो गई थी। अन्यत्र देखेंगे कि बल प्रयोग से बल प्रयोग की भंगिमा ही ज्यादा कारगर है। टॉमस ब्लोम हानसेन ने मुम्बई में शिवसेना पर शोध करते हुए पाया है कि शिव सैनिक अपनी राजनीति के अंग के रूप में जितना खून-खराबा और तोड़-फोड़ करते हैं उससे कहीं ज्यादा बलप्रयोग का दिखावा करते हैं, डराते हैं। एक तरह के नाटकीय प्रदर्शन से ही उनका उद्देश्य सध जाता है। उनकी युक्ति के अनुसार बलप्रयोग की भंगिमा ही नीतिसम्मत है। असली हिंसा होने से वह हो जाएगा सुनीति का गलत प्रयोग। लेकिन मैंने पहले ही कहा है, राजशक्ति और प्रजाशक्ति के बीच खींचतान की नई राजनीति में हिंसा की भूमिका पर विस्तारित चिन्तन, शोध और चर्चा की जरूरत है। यह कार्य अभी तक ठीक से शुरू नहीं हुआ है।
मैंने आनंदचन्द्र मित्र की संज्ञा उधार लेकर अनेक बार ‘प्रजाशक्ति’ और ‘राजशक्ति’ की बातें की हैं। फिर से याद दिला दूँ ‘प्रजाशक्ति’ का उद्भव होता है प्रजा के स्वत्व और अधिकार बोध से, और वह कारगर होता है प्रजा की मंगल कामना की इच्छा से। राजशक्ति है प्रजामंडल के प्रतिनिधि के रूप में जो राजकर्म का संचालन करते हैं, वे लोग। पिछले बीस-पच्चीस सालों में भारत की राजनीति में विभिन्न आकारों और विभिन्न स्तरों पर प्रजाशक्ति का क्रम विकास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रजाशक्ति के साथ राजशक्ति का मिलन नहीं हुआ है। उसका प्रमाण है राष्ट्र, प्रशासन, अफसर और राजनीति के प्रति व्यापक रूप से श्रद्वा न होना। एक के बाद एक हुए शोध से पता चलता है कि शहर और गाँवों के अधिकांश लोग प्रशासन की अक्षमता, सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रतिनिधियों के कपटाचार को लेकर मुखर हैं। कह सकते हैं कि राजशक्ति के प्रति मोहभंग आज सार्वजनिक है। लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं है कि प्रशासन से सेवाएँ प्राप्त करने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। बल्कि इसका उल्टा ही सत्य है। प्रजा का अधिकार बोध जितना प्रबल हो रहा है, उतना ही प्रशासन से सेवाएँ प्राप्त करने की माँग भी बढ़ रही है, सेवाएँ हासिल करने के नए कौशल भी खोजे जा रहे हैं। प्रजाशक्ति के उत्थान के इस क्षेत्र को मैं कह रहा हूँ ‘नीति’ का क्षेत्र। ‘नीति’ के सूत्र से ही उसे समझा जा सकता है। मुश्किल यह है कि हम लोग जो राजशक्ति की दुनिया में रहते हैं, प्रजाशक्ति के इस उत्थान को गहरे संदेह की नजर से देखते हैं और जितना संदेह बढ़ रहा है उतना ही हम ‘धर्मबोध’ की शरण में जा रहे हैं। नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे कहते हैं कि विस्थापित लोगों को पुनर्वास देने का मतलब है पॉकेटमार को पुरस्कृत करना! यह ‘धर्मशास्त्र’ की बात है, ‘नीतिशास्त्र’ की नहीं। ‘धर्म’ और ‘नीति’ का अन्तर एक समय हम जानते थे। अब भूलना चाहते हैं क्योंकि एक समय जो लोग सिर्फ प्रजा थे, वे भी आजकल राजनीति सीखने लगे हैं। मुझे इस पर कोई सन्देह नहीं है कि राजशक्ति और प्रजाशक्ति की खींचतान ही आगामी दिनों में भारतीय लोकतन्त्रा का भविष्य निर्धारित करेगी।
प्रस्तुत लेख का अनुवाद तरुण गुहा नियोगी ने किया है। वे कवि, अनुवादक है और वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा कार्यरत है।
(अप्रैल, 2005 को कोलकाता महाबोधि सोसाइटी में दिए गए सप्तम बुद्धदेव स्मृति व्याख्यान पर आधारित; आलोचना सहस्त्राब्दी अंक-54, जनतंत्र का जायजा-1 विशेषांक में प्रकाशित)