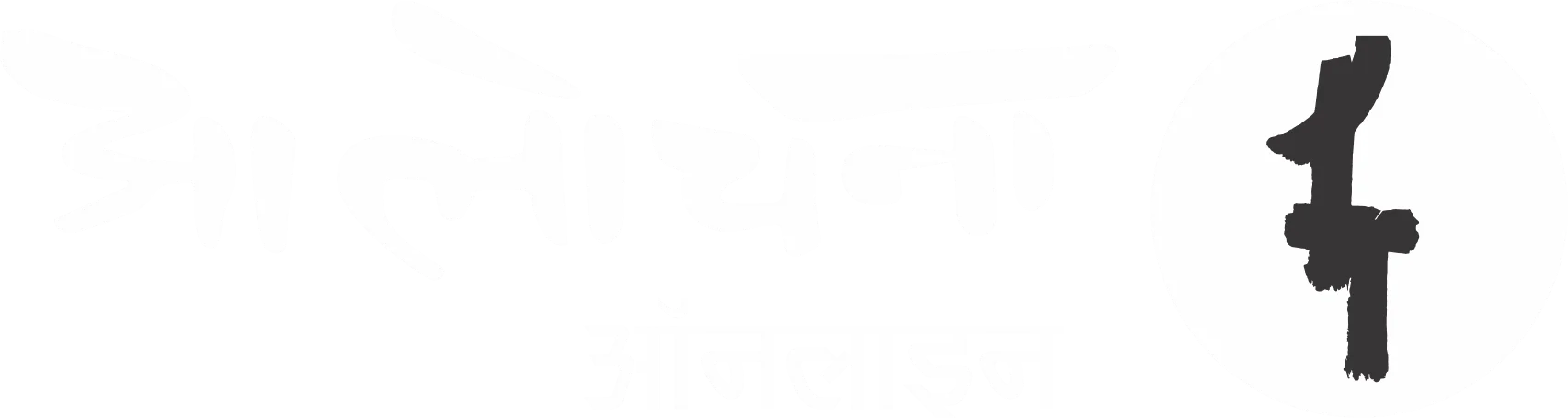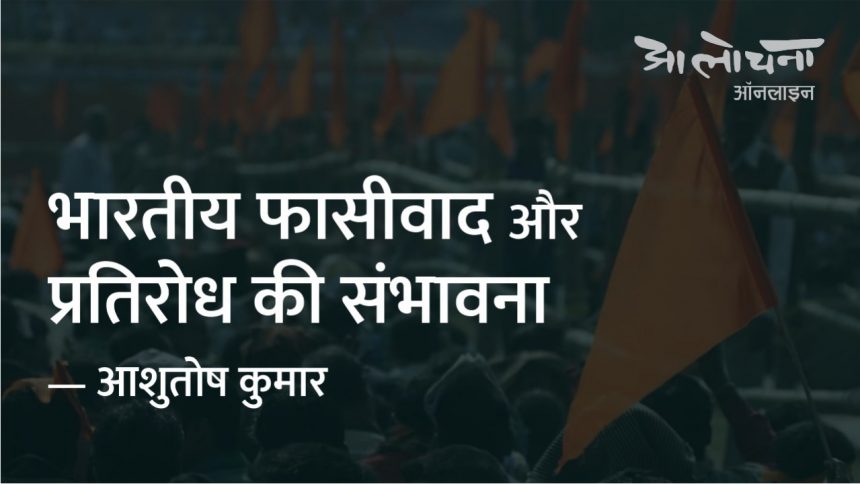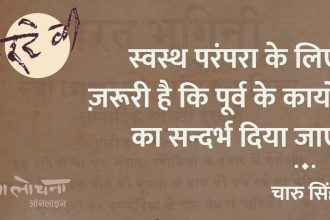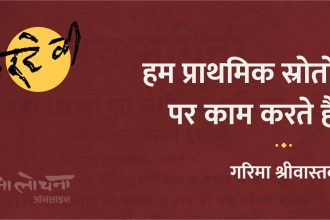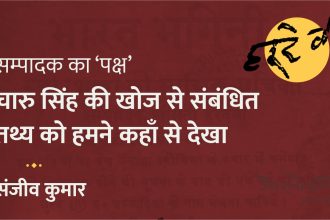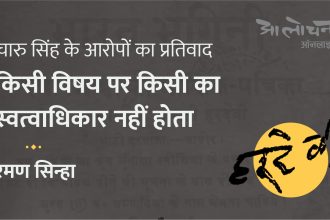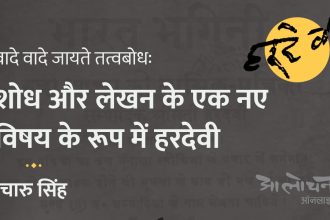क्या भारत की वर्तमान परिस्थिति को फासीवाद के रूप में चिन्हित किया जा सकता है? अथवा क्या इसे केवल साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण, धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवाद की राजनीति के रूप में देखा जाना चाहिए? यह सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके जवाब पर इस परिस्थिति से मुकाबला करने की रणनीति निर्भर करती है।
अगर यह फासीवाद है तो इसके उद्भव और वर्तमान शक्ति-सम्पन्नता के आधारभूत कारण क्या है? क्या यह केवल वैश्विक वित्तीय पूँजीवाद के संकट की अभिव्यक्ति है, जैसा कि प्रभात पटनायक जैसे अर्थशास्त्री समझते हैं?
क्या भारतीय फासीवाद जैसी किसी अवधारणा के बारे में सोचा जा सकता है? या यह सिर्फ़ एक वैश्विक प्रवृत्ति है?
अगर यह फासीवाद नहीं है तो क्या यह पश्चिम और पश्चिमपरस्त राजनेताओं और बौद्धिकों द्वारा अन्यायपूर्ण ढंग से दबाए गए हिंदू राष्ट्रवाद का उभार है, जैसा कि के. भट्टाचार्जी जैसे सावरकरी टिप्पणीकार दावा करते हैं?
क्या यह संघ के भीतर बढ़ते हुए लोकतंत्रीकरण के चलते उसकी पहल पर वंचित-उत्पीड़ित जन समुदाय द्वारा किया गया सत्ता-परिवर्तन हैं, जिसने कुलीन वर्गों की कीमत पर अकुलीनों को शक्तिशाली बनाया है? जैसा कि अभय कुमार दुबे और बद्री नारायण जैसे सामाजिक लेखक संकेत करते हैं?
इतिहासकार रामचन्द्र गुहा सरीखे कुछ बुद्धिजीवियों के मन में यह संशय रहता आया है कि भारत के मौजूदा निजाम और उसके द्वारा पैदा किए गए सामाजिक-राजनीतिक संकट को फासीवाद कहा जा सकता है या नहीं। वामपंथी दायरों में भी एक मत यह है कि भारत की वर्तमान सत्ता-संस्कृति को अधिनायकवादी या सर्वसत्तावादी तो कहा जा सकता है, लेकिन फासीवादी नहीं। इस मत के अनुसार, भारत में अभी भी लोकतांत्रिक संस्थाएँ काम कर रही हैं, वे पूरी तरह खत्म नहीं हो गई हैं। नागरिक समाज के सामने अभी भी बेहतर को चुनने का विकल्प मौजूद है, विपक्ष की चुनौती खुद को उसके सामने भरोसेमंद तरीके से बेहतर विकल्प के रूप में पेश करने भर की है।
दूसरा मत इस बात पर जोर देता है कि फासीवाद भारत में भले ही अभी भी अपने निकृष्टतम रूप में प्रगट न हुआ हो, लेकिन लगातार आगे बढ़ रहा है और देश की लोकतांत्रिक शक्तियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है। वामपंथी दायरों के भीतर से ही उभरने वाला एक मत यह है कि भारत में सर्वसत्तावाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष चलाने के लिए यह जरूरी है कि फासीवाद और ‘सर्वहारा की तानाशाही’ की कम्युनिस्ट अवधारणा की समान रूप से और एक साथ निंदा की जाए। यह मत इन दोनों अवधारणाओं को सर्वसत्तावाद के रूप में चिह्नित करता है और इसके विरुद्ध ‘उदारवादी लोकतंत्र’ को बेहतर विकल्प के रूप में पेश करता है। हालाँकि अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में यह ‘समाजवादी लोकतंत्र’ को ही मान्यता देता है।
इन सभी मतों को हमने भारत की दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों, माकपा और भाकपा माले, की अंदरूनी बहसों के रूप में उभरते हुए देखा है।
बुद्धिजीवियों का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान संकट को आज भी केवल साम्प्रदायिकता की समस्या के रूप में देखता है। यह तबका इस बात पर जोर देता है कि इस समस्या को हल करने के लिए हिंदू और मुस्लिम साम्प्रदायिकताओं के विरुद्ध एक साथ और समान रूप से संघर्ष चलाने की जरूरत है। कहना न होगा कि जिस समय हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा और हिंदूकृत राज्य मशीनरी अल्पसंख्यक नागरिक आबादी के रूप में मुस्लिम समुदाय के गैरीकरण, हाशियाकरण और न्यूनीकरण के अभियान लगातार चला रही हो, उस समय ‘हर तरह की साम्प्रदायिकता’ की निंदा का यह विमर्श हिंदूकृत राजसत्ता को वैधता देने के सिवा कुछ और नहीं करता।
इधर सर्वोच्च न्यायालय ने एक के बाद एक कई फ़ैसलों में नागरिक आज़ादियों के खिलाफ़ राजकीय दमन के अधिकार को मान्यता देकर ऐसे भोले संदेहों को निर्मूल करने की कोशिश की है। ये आज़ादियाँ कठिन संघर्ष और अनगिनत बलिदानों से हासिल की गई थीं।
हमने अयोध्या मामले में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले हिंदूवादी फासीवादी नेताओं को दोषी ठहराने से इनकार कर दिया। यह मानते हुए भी कि मस्जिद का विध्वंस घोर आपराधिक कृत्य था और वहाँ किसी राम मन्दिर के होने के कोई सबूत नहीं हैं, कोर्ट ने उन्हीं अपराधियों को उनकी क़ब्जाई जमीन मन्दिर बनाने के लिए दे दी। दूसरी तरफ़ इसी कोर्ट ने धारा 370 और नागरिकता क़ानूनों के मुद्दों पर जनता की व्यापक अपीलों के बावजूद सरकार की असंवैधानिक कार्रवाइयों पर रोक नहीं लगाई।
जकिया जाफ़री मामले में जनसंहार पीड़िता की जाँच कराने की माँग को ठुकराते हुए कोर्ट ने उलटे उनकी सहयोगी याचिकाकार तीस्ता सीतलवाड़ के ख़िलाफ़ सरकार को पुलिस कार्रवाई करने का अधिकार बिन माँगे दे दिया। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के जनसंहार की जाँच की याचिका देने वाले हिमांशु कुमार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भारी जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर गिरफ्तारी का आदेश है। गांधीवादी हिमांशु कुमार ने इस अन्यायपूर्ण जुर्माने को अदा करने से इनकार कर दिया है।
यह सच है कि फेक न्यूज के ख़िलाफ़ अभियान चलाने वाले पत्रकार मुहम्मद जुबैर की अवैध गिरफ्तारी जैसे एकाध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुरूप फ़ैसला दिया है। लेकिन ऐसे मामले अपवाद होते जा रहे हैं और सरकारपरस्ती के तहत लिये जा रहे फैसले आम।
भीमा कोरेगाँव हिंसा मामले में भिड़े और एकबोटे जैसे असली दंगाई खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि दलित अधिकारों के लिए काम करने वाले आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा जैसे लब्धप्रतिष्ठ लेखक-कर्मकर्ता बनावटी सबूतों के आधार पर यूएपीए के तहत सालों से जेल में बंद हैं।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ सरकारी लठैत की तरह काम कर रहे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को बिना आरोप बताए किसी के भी घर छापा मारने और उसे गिरफ़्तार करने के अधिकार की पुष्टि कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि ईडी धन शोधन के मामलों की जाँच करने की जगह अपने असीमित दमनकारी अधिकारों का उपयोग विपक्षी सरकारों को ध्वस्त करने और असहमत आवाज़ों को चुप करने के लिए कर रही है।
पिछले कुछ सालों में पनामा पेपर से लेकर पंडोरा पेपर्स तक भ्रष्टाचार से हासिल की गई अकल्पनीय धनराशि को विदेशों में खपाने, बैंकों से भारी मात्रा में अवैध कर्ज लेकर विदेश भाग जाने के मामले एक के बाद एक सामने आते गए हैं। इन घोटालों में सत्ता-संपन्न वर्गों से जुड़े हजारों बड़े-बड़े नाम सामने आए हैं। स्विस बैंकों में हिंदुस्तानियों के द्वारा जमा किया गया काला धन 14 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है—30 हजार 500 करोड़। इन सभी मामलों में अपराधियों के ख़िलाफ़ कोई गंभीर क़दम नहीं उठाए गए हैं। स्पष्ट है कि सरकार भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की जगह उसे प्रोत्साहित करने में लगी हुई है।
इसका सबसे बड़ा सबूत गोपनीय इलेक्टॉरल बॉन्ड्स के जरिये बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा दिए जा रहे गुप्त चंदे की व्यवस्था को बनाए रखना है। सभी जानते हैं कि इस गुप्त चंदे का भारतीय चुनावों में कितना बड़ा दखल है।
फासीवाद का सबसे बड़ा लक्षण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के एक गठबंधन के रूप में काम करने की प्रवृत्ति है। लोकतंत्र में इन तीनों के अलगाव और इनकी स्वायत्तता पर इसलिए जोर दिया जाता है कि कोई एक समूह राजसत्ता का दुरुपयोग न कर सके। तीनों निकाय एक दूसरे पर नजर रखने और एक दूसरे को नियंत्रित करने का कार्य करें। इस व्यवस्था के बिना एक व्यक्ति और एक गुट की निरंकुश तानाशाही से बचना नामुमकिन है।
अयोध्या विवाद से लेकर गुलबर्ग सोसाइटी जनसंहार और छतीसगढ़ जनसंहार तक के मामलों में हमने सुप्रीम कोर्ट को संविधान-प्रदत्त नागरिक अधिकारों और न्याय की अवधारणा के विरुद्ध राज्य के बहुमतवादी फ़ैसलों के पक्ष में खड़े होते देखा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धन-शोधन निवारण अधिनियम के अन्यायपूर्ण प्रावधानों के ख़िलाफ़ दी गई याचिका पर राज्य के पक्ष में फ़ैसला दिया है। सीएए और धारा 370 के निर्मूलीकरण जैसे मामलों में चुप्पी साधकर भी उसने नागरिक अधिकारों के विरुद्ध राजकीय निरंकुशता का समर्थन किया है।
नाजी जर्मनी में ग्लाइसेशतुंग या समेकन के नाजी क़ानूनों के जरिये इसी तरह राज्य के सभी निकायों को संकेंद्रित और एकात्म बनाया था। हिटलर की तरह मुसोलिनी ने भी ‘राष्ट्र-राज्य सर्वोपरि’ के सिद्धांत के तहत न्यायपालिका को पालतू बनाने का काम किया था। भारत में भी हमने गृहमंत्री अमित शाह को सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देते देखा है। कहना न होगा कि भारत में भी संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका के बड़े हिस्से पर कार्यपालिका के साथ मिलकर समेकित रूप से काम करने के आरोप तेज हुए हैं।
भारत में फासीवाद के सभी जाने-पहचाने लक्षण प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति की तानाशाही और व्यक्ति-पूजा का व्यापक प्रचार। मुख्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के विरुद्ध नफ़रत, हिंसा और अपमान का अटूट सिलसिला। अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ अधिकतम हिंसा के पक्ष में जनता के व्यापक हिस्सों का जुनून। विपक्ष की बढ़ती हुई असहायता। स्वतंत्र आवाजों का क्रूर दमन। दमन के क़ानूनी और गैरकानूनी रूपों का विस्तार। मजदूरों और किसानों के अधिकारों में जबरदस्त कटौती। आदिवासियों, दलितों और स्त्रियों के सम्मान के संघर्षों का पीछे ढकेला जाना। शिक्षा पर भगवा नियंत्रण। छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का विलोपन। फासीवादी प्रचार के लिए साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा और दीगर कला-विधाओं के नियंत्रण और विरूपण को राज्य की ओर से दिया जा रहा संरक्षण और प्रोत्साहन।
देश-काल के अनुसार फासीवाद अनेक रूप ग्रहण करता रहा है। मुसोलिनी का फासीवाद हिटलर का नाजीवाद, ट्रंप का ट्रंपवाद या पुतिन का पुतिनवाद बिल्कुल एक ही जैसी परिघटनाएँ नहीं हैं, लेकिन इनमें कुछ बुनियादी और आत्यंतिक समानताएँ मौजूद हैं। इन्हीं समानताओं के आधार पर फासीवाद की पहचान की जा सकती है।
फासीवाद पहचान-मूलक भावनात्मक राष्ट्रवाद का एक ऐसा संस्करण है, जो बाहरी और भीतरी ‘शत्रुओं’ की शिनाख्त पर जोर देता है और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत और हिंसा से भरे हुए जन-उन्मादी अभियानों से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह नागरिकों में राष्ट्र के प्रति शर्त रहित समर्पण की भावना जगाता है, उनसे राष्ट्रहित में आधुनिक नागरिक अधिकारों के परित्याग की माँग करता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य मशीनरी की हिंसक शक्ति के अतिरिक्त गैर-राज्य मिलिशिया के संगठित समूहों का उपयोग करता है। जाहिर है यह एक ऐसा निजाम है जो अंतत: राष्ट्र, राज्य और नागरिक तीनों के लिए विनाशकारी साबित होता है।
भारतीय फासीवाद की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। ये विशेषताएँ भारत की अपनी परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ एक विशाल महादेश है, जहाँ यूरोप के छोटे देशों में फले-फूले फासीवादी-नाजीवादी प्रयोग का टिक पाना असंभव था। यूरोप में फासीवाद के प्रयोग मुख्यत: एक व्यक्ति-महानायक को केंद्र में रखकर चले। मसीहा के रूप में महानायक की स्थापना वहाँ के फ़ासी-नाजी निजामों की बुनियाद थी। भारत में भी फासीवादी राजनीति महानायक का इस्तेमाल करती है, लेकिन वह हमेशा मातृ-संगठन के नियंत्रण में रहता है। इसलिए एक महानायक के विफल होने पर उसे दूसरे से विस्थापित किया जा सकता है।
वास्तव में इस विशाल महादेश की समाज-राजनीति को एक सर्वोच्च व्यक्ति-केंद्र नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसा नियंत्रण क़ायम करना किसी ऐसे ही संगठन के बस की बात है, जिसकी शाखाएँ हर गाँव-शहर-बस्ती में, हर गली-कूचे में फैली हुई हों। जो अपने आप में स्वायत्त इकाइयों की तरह काम करती हों, लेकिन जो संगठन के दृश्य-अदृश्य आंतरिक नेतृत्व के फ़ैसलों, प्रचार-अभियानों, सांस्कृतिक राजनैतिक रणनीतियों और तात्कालिक कार्यक्रमों को मशीनी कुशलता और तत्परता के साथ लागू कर सकती हों। भारत में संघ ने महानायक से पहले ऐसे संगठन के निर्माण पर जोर दिया, कि जिसकी जमीनी ताक़त से आज वह महानायकों को प्रक्षेपित और नियंत्रित कर सकने की स्थिति में है।
संघ जिस तरह वैयक्तिक नायकत्व और सांगठनिक सर्वोच्चता को एक साथ साध लेता है, उसी तरह अपनी हजारों इकाइयों, समूहों, मंचों और संस्थाओं की सापेक्षिक स्वायत्तता और कठोर सांगठनिक नियंत्रण को भी। वह उसी तरह बहुत तरह के वैचारिक राजनीतिक नवाचार और हिंदुत्व की अपनी कोर-विचारधारा की कट्टरता को भी एक साथ साथ लेता है। यह विचारधारा राजनीति के हिंदूकरण और हिंदुओं के सैन्यीकरण की सावरकर-प्रणीत विचारधारा है।
कोर-कट्टरता और बाहरी लचीलेपन के इस विरुद्ध सामंजस्य ने भारतीय फासीवाद को एक लम्बी कालावधि में, बदलते हुए अनेक अच्छे-बुरे दौरों में टिके रहने और आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की है। ध्यान से देखने पर साफ़ हो जाता है कि ये सारी विशेषताएँ हिंदू वर्ण-जाति व्यवस्था की वे विशेषताएँ हैं, जिनके सहारे ये व्यवस्था हजारों सालों से बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों के बीच ख़ुद को बचाए रखने में ही नहीं, अधिकाधिक मजबूत बनाते जाने में भी सफल हुई है।
भारतीय फासीवाद दुनिया का सबसे दीर्घकालीन राजनैतिक अभियान है। यह अभियान व्यवस्थित रूप से सन् 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के साथ शुरू होकर अनेक अवस्थाओं से गुजरता हुआ आज तक चल रहा है। संघ की संकल्पना में इतालवी फासीवाद और जर्मन नाजीवाद की प्रेरणाओं और प्रभावों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। विश्वयुद्ध के साथ इन दोनों प्रयोगों का उदय और अस्त बहुत तेज गति से हुआ। भारत में संघ की राजनीति लगभग 100 वर्षों के समय अंतराल में धीमे-धीमे फलती-फूलती रही है।
अब जाकर वह एक ऐसी स्थिति में है जब यह कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति और समाजनीति के नियंत्रणकारी और निर्णायक निकायों पर उसका प्रभुत्व लगभग उसकी इच्छा-अनुसार क़ायम हो चुका है। यह बदलाव धीमी गति से भारतीय समाज-राजनीति की समूची संरचना को बाहर से बहुत बदले बगैर उसकी अंतर्वस्तु को भीतर से बदलते हुए किया गया है। यह बदलाव ऐसे हैं जिन्हें अनकिया करने के लिए उतने ही दीर्घकालीन और सतत उद्यम की जरूरत होगी। इसलिए किसी को यह मुग़ालता नहीं होना चाहिए कि केंद्र की सरकार बदल जाने भर से भारतीय फासीवाद को शिकस्त दी जा सकेगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सैनिक या सैनिक तरीक़ों से सीधे राजनेता पर क़ब्ज़ा करने की किसी तात्कालिक परियोजना के बजाय शुरू से ही भारतीय राजनीति के स्वरूप को बदलने और भारतीय नागरिक समाज की चेतना को अपनी कल्पना के अनुसार पुनर्निर्मित करने पर जोर दिया है।
प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध विविधताओं से भरे विस्तृत भूभाग वाले किसी विशाल देश में सहजीवन, सद्भाव, मेल-जोल, साझापन, सहभागिता, नवोन्मेष और विविधता के सम्मान जैसे गुण सहज ही विकसित हो जाते हैं। संघ की स्थापना के समय भारत का राष्ट्रीय आंदोलन इन्हीं सामाजिक मूल्यों के साथ विकसित हो रहा था।
लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के आधुनिक विचारों ने इन मूल्यों को और अधिक मजबूत और चमकीला बना दिया था। इन विचारों के बढ़ते प्रसार ने भारत की परंपरागत वर्णाश्रमी ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक सत्ता-संरचना के ध्वजधारियों को गहरी चिंता में डाल दिया था। संघ और हिंदू महासभा के संस्थापकों और उन्नायकों का सीधा संबंध इन्हीं तत्वों का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करने वाली मराठी पेशवाई की परंपरा से था। वे भारत में एक ऐसे राष्ट्रवाद को स्थापित करने के लिए बेचैन थे, जिसके जरिये स्वाधीनता संग्राम के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी मूल्यों को संघ द्वारा पोषित मूल्यों से विस्थापित किया जा सके।
संघ धर्मनिरपेक्षता की जगह धर्म सापेक्षता, लोकतंत्र की जगह वर्णाश्रम संस्कार तथा समाजवाद की जगह अंध-राष्ट्रवाद को स्थापित करने की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मुहिम चलाता रहा है। संघ धर्मनिरपेक्षता की निंदा उसे छद्म बताकर करता है। स्यूडो-सेकुलर होना संघ की बोली में भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी गाली है।
वैसे तो वह पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग यह जताने के लिए भी करता है कि उसे सेकुलरिज्म की आधुनिक अवधारणा से कोई बुनियादी समस्या नहीं है, और कि भारत में धर्म-राज्य की स्थापना करना उसका लक्ष्य नहीं है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथनिरपेक्षता शब्द का चुनाव करने से यह स्पष्ट है कि संघ राजनीति में धर्म की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करता है। एक बार इसे स्वीकार कर लिया जाए तो बताने की जरूरत ना होगी कि भारतीय राजनीति में यह केंद्रीय भूमिका किस धर्म की होगी।
सावरकर की हिंदुत्व की थीसिस को ध्यान में रखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह वही धर्म है जो भारतीय महाकाव्यों के माध्यम से एक संस्कार के रूप में भारत के प्रभुत्वशाली वर्ग के जनमानस में उपस्थित है। इस संस्कार का सबसे प्रचलित नाम वर्णाश्रम है। सच है कि सावरकर से लेकर मोहन भागवत तक हिंदुओं में जाति-पाँति की बुराई के ख़िलाफ़ अभियान चलाने की बात करते रहे हैं, लेकिन यह अभियान प्रायोजित सहभोजों तक ही सीमित है।
सावरकर हिंदुत्व में लिख चुके हैं कि वर्णाश्रम ही वह संस्कार है जिसने अनेक ऐतिहासिक चुनौतियों के सामने हिंदू समाज की रक्षा की है। इसी रचना में उन्होंने यह भी कहा है कि एक राजनीतिक हिंदू की सबसे बड़ी पहचान उसका वह हिंदू संस्कार है जो उसे भारतीय आर्ष ग्रंथों से मिलता है। यहाँ अलग से यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह संस्कार वर्णाश्रम के सिवा कुछ और नहीं है।
वर्णाश्रम संस्कार समानता और लोकतंत्र के किसी भी आधुनिक विचार के खिलाफ़ है। यह संस्कार बड़े और छोटे के भेदभाव को सम्मान की नज़र से देखने और स्त्री-पुरुष के बीच के स्वाभाविक और सांस्कारिक विभेद को बनाए रखने में है। सावरकर और संघ हिंदू-एकजुटता और हिंदुओं के सैन्यीकरण की जरूरत के तहत जाति-पाँति को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन वे उस संस्कार को मिटाने की बात सोच भी नहीं सकते, जिसे वर्णाश्रम कहते हैं।
यह वही संस्कार है, जो भारतीय आर्ष ग्रंथों, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि का मुख्य प्रतिपाद्य है। इस वर्णाश्रम संस्कार की ध्वजा उठाए हुए ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान, रामनाथ कोविंद जैसे दलित और द्रौपदी मुर्मू जैसे आदिवासी संघ द्वारा सम्मानित और प्रतिष्ठित किए जाते हैं। इसी वर्णाश्रम संस्कार के ख़िलाफ़ संघर्ष छेड़ने के कारण उमर खालिद, आनंद तेलतुंबडे, स्टेन स्वामी, पांडु नरोटे और जी. एन. साईंबाबा जैसे लोग राज्य की अधिकतम बर्बरता झेलने के लिए विवश किए जाते हैं।
जहाँ तक समाजवाद की बात है, इसे सभी आधुनिक नागरिक समाजों में सामाजिक राजनीति के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। पूँजीवादी देशों में भी लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा में समाजवाद की कल्पना मौजूद रही है। इसके ठीक विपरीत फासीवाद, नाजीवाद और हिंदू राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएँ सबसे ज्यादा इस बात पर जोर देती हैं कि ‘राष्ट्र’ के हित के समक्ष नागरिक को अपने सभी अधिकारों और हितों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यावहारिक स्तर पर इसका अर्थ होता है कि आम श्रमजीवी जनता को देश के छोटे-से मलाईखोर शासक वर्ग के हितों के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए।
100 सालों में संघ की सफलता इस बात में है कि उसने भारतीय समाज में इन प्रतिगामी मूल्यों के लिए जनमत के एक अच्छे-खासे हिस्से को तैयार कर लिया है। भारत में जाति-व्यवस्था और वर्णाश्रम के रूप में यह सभी मूल्य हजारों वर्षों से जनमानस के किसी न किसी कोने में मौजूद रहे हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के अग्रधावकों ने केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं छेड़ी थी। गांधी, नेहरू, भगत सिंह और आम्बेडकर ने अपने-अपने तरीक़ों से भारतीय जन की सांस्कारिक आज़ादी की लड़ाई भी छेड़ी थी। इसीलिए उन्होंने लगातार वर्णाश्रम के परंपरागत मूल्यों की जगह आधुनिक नागरिक मूल्यों को स्थापित करने पर जोर दिया था।
ये आधुनिक मूल्य भारत की सनातन परंपरा में एक गंभीर विक्षेप की तरह हैं। संघ ने कुल इतना किया है कि इस विक्षेप को निरस्त कर पुराने सनातन संस्कारों को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की है। फिर भी उसे इस काम में 100 साल लगे हैं तो मानना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रधावकों ने भारतीय समाज को रूपांतरित करने में कितनी दूर तक सफलता हासिल कर ली थी!
अभी भी कुछ लोग भारत में फासीवादी निज़ाम से सिर्फ़ इसलिए इनकार करते हैं कि इस देश में गैस चैंबर स्थापित नहीं किए गए हैं। उन्हें समझना चाहिए कि भारतीय फासीवाद ने फासीवाद के अतीत से बहुत कुछ सीखा है। उसने समझ लिया है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में भौतिक गैस चैंबर से कहीं अधिक असरदार और स्थायी व्यवस्था है देश के भीतर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक गैस चैम्बरों का विस्तार।
लगभग समूचे देश को एक ऐसे सांस्कृतिक गैस चैंबर में बदल दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति और एक विचारधारा की गुलामी से इनकार करने वाले स्वतंत्रचेता जन अपने जीवित होने का कोई मतलब ही ना निकाल सकें।
यूरोप की लोकतांत्रिक परम्पराओं के कारण फासीवादी राज्य की स्थापना के लिए क़ानूनी बदलावों की जरूरत थी। भारत में ‘भक्ति-परम्परा’ की जड़ें बहुत गहरी हैं। शर्तहीन-समर्पण का संस्कार प्रबल रहा है। क्या यह भी एक कारण है कि भारत में यूएपीए और अफ्स्पा जैसे कुछ विशेष क़ानूनों के अलावा व्यापक क़ानूनी बदलावों की जरूरत नहीं पड़ी है?
फासीवाद की मुख्य जीवनी शक्ति नफ़रत की भावना है। हमारे देश में वर्ण-व्यवस्था और जाति-प्रथा के कारण अपने ही जैसे दूसरे मनुष्यों से तीव्र नफ़रत का संस्कार हजारों वर्षों से फलता-फूलता रहा है। वोट तंत्र ने इस नफ़रत को उसकी चरम सीमा तक पहुँचा दिया है। क्या भारतीय फासीवाद नफ़रत के इस चारों ओर फैले खौलते हुए समंदर से उपजे घन-घमंड के रूप में ख़ुद को जनमानस में स्थापित कर चुका है?
लेकिन यह समय उदास होने या निराशा में डूब जाने का नहीं है।
जैसे फासीवाद ने अपने इतिहास से सीखा है, वैसे ही प्रतिरोध की शक्तियों को भी अतीत के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। फासीवाद केवल अल्पसंख्यकों को नहीं, कमोबेश सभी नागरिकों को पीड़ित और तबाह करता है। भले ही भक्तजन ख़ुद अपनी बर्बादी को न देख सकें।
आज एक ऐसे प्रबल सांस्कृतिक-सामाजिक आंदोलन की जरूरत है, जो जनसाधारण को उनकी अपनी ही यातना और हमारे देश के ऊपर टूट रही महा-विपत्ति के बारे में जागरूक कर सके, जो एक तरफ़ तो लोगों को उनके वास्तविक दुखों के प्रति सचेत कर सके और दूसरी तरफ़ उन्हें राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महान प्रयत्न के साथ एकजुट कर सके।
एक ऐसे महान राष्ट्र के सपने को जीवित करने की जरूरत है जो बुद्ध, कबीर, अंदाल, मीरा, मोइनुद्दीन चिश्ती, आंबेडकर, पेरियार, गांधी, भगत सिंह, प्रेमचंद और फ़ैज़ अहमद फ़ैज के सत्य, न्याय, क्रांति और प्रीति के आदर्शों से स्पन्दित हो। निरंकुश निजीकरण पर रोक तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों के संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना यह सपना पूरा नहीं हो सकता।
(आलोचना सहस्त्राब्दी अंक-69, अप्रैल-जून 2022 में प्रकाशित संपादकीय)