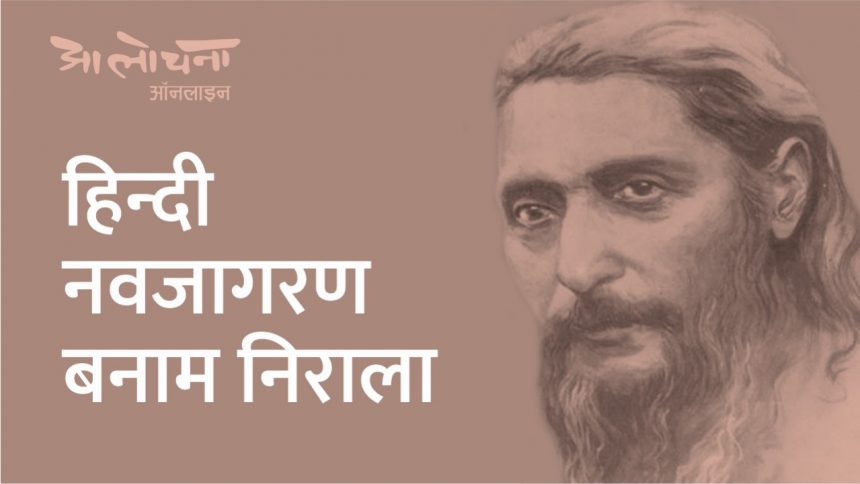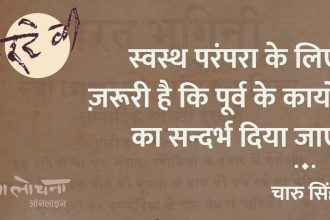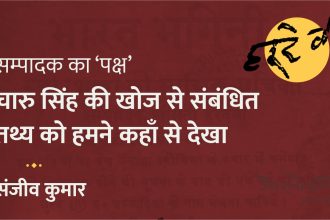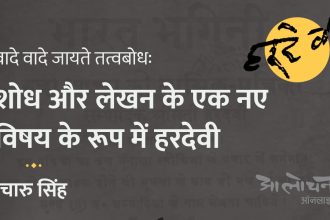1929 के अपने एक लेख में निराला शंकराचार्य को शूद्र विरोधी कहने पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते हैं। उस पंक्ति के आधार पर उन्हें ब्राह्मणवादी करार दिया जा सकता है। इसी तरह 1946 में प्रकाशित संग्रह ‘वेला’ की कविता ‘जल्द-जल्द पैर बढ़ाओ’ के आधार पर उन्हें ब्राह्मणवाद का विरोधी और मार्क्सवादी भी बताया जा सकता है। ‘राम की शक्तिपूजा’ कविता के आधार पर हिन्दूवादी संगठन निराला को हिन्दूवादी ठहराते हैं और कुछ दलित आलोचक भी ऐसा करते हैं। दोनों ही इस कविता के हिन्दूवादी पाठ पर सहमत हैं। इसी कविता के आधार पर कुछ आलोचक निराला को गांधीवादी बताते हैं।
ऐसे सभी आलोचक निराला को किसी एक पंक्ति या किसी एक पल में कीलित करके देखने की मेटाफ़िजिकल पद्धति के प्रभाव में हैं। निराला के गंभीर अध्येता दुर्गा सिंह ने इस लेख में दिखाया है कि निराला के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों का तर्कसंगत आकलन करने के लिए उनकी यात्रा को ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक ढंग से विश्लेषित करने की जरूरत है। निराला की वैचारिक यात्रा कथित ‘हिन्दी नवजागरण’ के दायरे में शुरू होती है, लेकिन क्रमश: वे इससे टकराते हैं और इसे पार कर भारतीय समाज की आधुनिक विवेक से प्रेरित कल्पना तक पहुँचते हैं। निराला की परम्परा को समझने के लिए इस लेख को ध्यान से देखना जरूरी हैं।
दुर्गा सिंह ‘निराला का कथा साहित्य’ के लेखक हैं, जो निराला के मूल्यांकन की परम्परा में एक मौलिक हस्तक्षेप है।
हिन्दी के बौद्धिक जगत में निराला एक बार फिर से चर्चा में हैं। निराला पुरस्कार के बहाने शुरु हुई चर्चा निराला पर विमर्श तक पहुँच गयी। कोई उन्हें प्रतिगामी तो कोई ब्राह्मणवादी करार देने लगा। उन पर हिन्दूवादी होने के भी आरोप हैं।
निराला को ‘बसन्त का अग्रदूत’ भी कहा गया है। बसन्त नवीनता का सूचक है। निराला की कविताओं में ‘नव-नव’ आया भी बहुत है। निराला का साहित्य ही उसके लिए प्रमाण देता है। निराला के लिए महाप्राण विशेषण भी प्रयोग किया गया। यह भी उनकी कविता के व्याकरण से ही निकला है।
निराला और प्रेमचंद, दो लेखक-रचनाकार ऐसे हैं, जिन्होंने हिन्दी नवजागरण की अंतर्वस्तु को बदल दिया। उसे नये जमाने के मेल में खड़ा किया। लेकिन यह सब धीरे-धीरे हुआ। दोनों ने परम्परा से प्राप्त वस्तु और विचार को लगातार विवेक की कसौटी पर रखा।
विवेक की कसौटी कबीर समेत समूचे सन्त साहित्य के पास थी। इसीलिए कुछ आलोचक निराला में कबीर जैसा आभास पाते हैं। इस विवेक को पाने की निराला की खुद की यात्रा को ‘स्वामी सारदानन्द महाराज और मैं’ में पढ़ा जा सकता है।
निराला समाज और राजनीति में देशी और वैश्विक स्तर पर हुए परिवर्तनों से खुद को जोड़ते हैं और खुद भी बदलते हैं। निराला के साहित्य की अंतर्वस्तु में भी बदलाव इसी के सापेक्ष है। जो इस बात को नहीं समझेगा, वह निराला के अधूरे सत्य का साक्षात्कार करेगा।
रचना और विचार के स्तर पर निराला के विकास के प्राय: तीन चरण दिखते हैं। पहला, बंगाल से आना, हिन्दी भाषा सीखना। इसी क्रम में, ज्यादातर, प्राचीन धार्मिक, दार्शनिक साहित्य से परिचित होना। दूसरा, अवध के किसान आन्दोलन व राजनीति के सम्पर्क में आना। तीसरा, परिवर्तनकामी सामाजिक-राजनीतिक विचारों के सम्पर्क में आना।
वेदान्तिक साम्य का प्रभाव
पहला चरण 1930-32 तक माना जा सकता है। इस समय निराला भारतीय समाज के वर्णवादी विभाजन, स्तरीकरण और भेदभाव आदि के समाधान की दृष्टि से शंकर के वेदान्तिक साम्य के दर्शन से गहरे प्रभावित हैं। शंकर के वेदान्तिक साम्य के दर्शन को सन्त साहित्य के उदय के पीछे एक प्रमुख तत्व माना जाता है। उस समय इस दर्शन ने जाति-पाँति के बन्धन ढीले किये, ऐसा माना जाता है।
निराला भी वेदान्तिक साम्य को वर्णवादी विभाजन और जाति-पाँति के समाधान के रूप में देखते हैं। विवेकानंद का वेदान्त दर्शन और वर्णों और जातियों की उनकी नवीन अवधारणा का निराला पर गहरा असर पड़ता है। जैसे विवेकानंद का यह कहना कि गुलाम देश में सभी शूद्र हैं।
इसी दृष्टि से निराला वर्ण-व्यवस्था के विषय में पहला लेख लिखते हैं, ‘वर्णाश्रम-धर्म की वर्तमान स्थिति।’ 1929 ई. का यह लेख ‘चाबुक’ में संकलित है और ‘माधुरी’ दिसम्बर में छपा है।
इस लेख में निराला तर्क देते हैं कि द्विजत्व चिरन्तन नहीं होता। जो उसे चिरन्तन मानते हैं, वे ‘कठहुज्जती’ करते हैं। ‘उत्थान और पतन का विवर्तन’ द्विज जातियों पर भी लागू होता है। इसलिए ‘वर्ण-व्यवस्था की रक्षा’ के प्रयासों को वे सार्थक नहीं मानते।
दोनों बातें वर्णवादी या सनातन धर्म के रक्षकों के गले उतरने वाली नहीं थीं। इन विचारों के चलते इस समाज में वे तिरस्कृत होते हैं। उनकी कविता में इस तिरस्कार की मार्मिक अनुगूँजें हैं तो कथा साहित्य में गहरी व्यंग्योक्तियाँ हैं। इस विचार के बावजूद वेदान्तिक साम्य के दर्शन का आग्रह निराला में है। लेकिन आधुनिक विवेकवादी विचारों ने दरवाजे की सांकल खटखटानी शुरू कर दी है।
वेदान्तिक साम्य के इसी प्रभाव में निराला जाति-पाँति तोड़क मण्डल के मंत्री सन्तराम की आलोचना करते हैं।
“इधर माधुरी में वर्ण व्यवस्था पर जितने लेख निकले हैं, उनमें से कोई भी लेख ऐसा नहीं, जो विवर्तित समय की मौलिकता या नवीन युग का यथार्थ तत्व समझाता हुआ वर्ण-व्यवस्था की एक विचार पुष्ट व्याख्या कर रहा हो। सब-के-सब अपनी ही धुन में लीन, अपने ही अधिकार के प्रतिपादन में नियोजित हो रहे हैं। शूद्रों के प्रति केवल सहानुभूति प्रदर्शन कर देने से ब्राह्मण-धर्म की कर्तव्यपरता समाप्त नहीं हो जाती, न ‘जाति-पाँति तोड़क मंडल’ के मंत्री संतरामजी के करार देने से इधर दो हजार वर्ष के अन्दर का संसार का सर्वश्रेष्ठ विद्वान महा-मेधावी त्यागीश्वर शंकर शूद्रों के यथार्थ शत्रु सिद्ध हो सकते हैं। शूद्रों के प्रति उनके अनुशासन कठोर से कठोर होने पर भी अपने समय की मर्यादा से दृढ़ संबद्ध हैं।”
निराला यहाँ नवीन समय के यथार्थ तत्व के सापेक्ष वर्ण व्यवस्था की व्याख्या की बात करते हैं, लेकिन शंकर के वर्ण व्यवस्था के कठोर से कठोर अनुशासन को समय की मर्यादा से दृढ़ संबद्ध भी बताते हैं।
अभी निराला के यहाँ भी वही अन्तर्विरोध दिखाई देते हैं, जो ‘हिन्दी नवजागरण’ में प्रबल थे। जो राष्ट्रीय आन्दोलन में भी थे।
उस दौर में भारतीयता की अवधारणा को प्राय: संस्कृत के धर्मशास्त्रों और वैष्णव केन्द्रित हिन्दू दर्शन से संबद्ध किया जा रहा था। इस पर पूरबवादी नज़रिए का असर भी था। औपनिवेशिक सत्ता भी साम्प्रदायिक विभाजन पैदा करने हेतु भारतीयता की मनगढंत झूठी अवधारणा का पोषण करती थी, जो हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष पर आधारित थी।
निराला इस से प्रभावित होते हैं लेकिन इसके प्रभाव से निकलते भी हैं।
निराला बांग्ला नवजागरण से भी संबद्ध थे। इसलिए उनमें वर्ण व्यवस्था की पुरातन नैतिकता की तीखी आलोचना भी साथ-साथ मिलती है। वर्ण-व्यवस्था को उदारता के साथ न्यायोचित ठहराने की नवजागरण की प्रवृत्ति से निराला क्रमश: भिन्न होते जाते हैं।
इसी लेख में वे लिखते हैं कि ‘जायते वर्णसंकर’ के प्रमाण से वर्ण-व्यवस्था की सार्थकता नहीं दीख पड़ती। लेकिन संतरामजी के ‘जाति-पाँति तोड़क मंडल’ की आवश्यकता को भी नकारते हैं। कहते हैं, जाति-पाँति तोड़क मंडल की जगह जाति-पाँति योजक मंडल की जरूरत है। तोड़ ही हिन्दोस्तान को तोड़ रहा है, जबकि जरूरत जोड़ने की है।
बाद के एक लेख में निराला संतरामजी के प्रयास को ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन के सामाजिक सुधार के साथ रखकर देखते हैं। लेकिन अभी इस लेख में शंकर को शूद्र विरोधी बताने के कारण उनसे सहज नहीं हैं। शंकर के वेदान्तिक साम्य में उनका विश्वास अभी प्रबल है।
जाति भेद के दंश और वर्ण व्यवस्था की मार से पीड़ित जातियों से निराला का गहरा सम्पर्क अब तक नहीं हुआ था। जब होता है तब वे अपनी समझ की सीमा जान-समझ जाते हैं।
1929 में यह लेख लिखते समय निराला वेदान्तिक साम्य के विचार से इस कदर प्रभावित थे कि उसे सभी विचारों और वादों से श्रेष्ठ बताते हैं। वे लिखते हैं,
“भारतवर्ष को मुक्ति की ओर ले जाने वाले आज तक जितने भी विचार देखने में आए हैं, वे राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक किसी भी दिशा में झुकाए गए हाें, वेदान्तिक विचार की समता नहीं कर सकते।… कोई वाद ऐसा नहीं, जो जाति, देश या समाज को पूर्ण स्वतंत्रता तक पहुंचा सके—जहाँ किसी प्रकार का विरोध न हो। भारतवर्ष की समाज-शृंखला उसी वेदान्तिक धातु से मजबूत की गयी है।”
इसी में आगे निराला लिखते हैं कि अगर कोई ‘वेदान्त को नहीं मानता तो वह भारतीय कहलाने का दावा नहीं कर सकता।’
वेदान्त संबन्धी निराला के इस विचार को निरपेक्ष मान लेने से निराला को समझने में दिक्कत होगी। निराला बंगाल से हिन्दी में आए थे। निराला के ऊपर विवेकानंद का प्रभाव बहुत था। उनके दो लेखों के शीर्षक हैं, ‘वेदान्त केशरी स्वामी विवेकानंद’ व ‘वेदान्त केसरी स्वामी विवेकानंद और भारत।’ पहला लेख ‘समन्वय:’, मासिक, कोलकाता में, फरवरी-मार्च 1928 ई. में छपा है और दूसरा ‘हंस’, मासिक, काशी स्वदेशांक, अक्टूबर-नवंबर 1932 ईस्वी में।
विवेकानंद द्वारा वेदान्त की जो व्याख्या की गयी, शूद्र की जो व्याख्या और अवधारणा प्रस्तुत की गयी, वर्ण धर्म और हिन्दू धर्म के पाखंड की जो आलोचनाएँ उनके द्वारा की गयी, इन लेखों में निराला उन से प्रभावित दिखाई देते हैं।
विवेकानंद का प्रभाव राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व पर भी था। विवेकानंद की व्याख्या से हिन्दूवादियों ने भी हिन्दू धर्म को श्रेष्ठ मानने के प्रमाण जुटाये।
निराला ने भी विवेकानंद से वेदान्त को श्रेष्ठ मानने के प्रमाण पाए लेकिन उनके सन्दर्भ अलग थे। निराला विवेकानंद की सीमा जानते हैं। लिखते हैं कि विवेकानंद के विचार ज्ञान के स्तर पर अधिक हैं, व्यवहार के स्तर पर कम। फिर भी निराला मानते हैं कि विवेकानंद के विचारों ने सामाजिक सुधार और नवीन सामाजिक संगठन के निर्माण में योग दिया। ठीक यही राय शंकर के वेदान्तिक साम्य को लेकर भी है। ज्ञान क्षेत्र में ही सही, वेदान्तिक दर्शन में प्रस्तुत साम्य के विचार से वे प्रभावित थे, क्योंकि इसमें सभी जातियों को भक्ति का समान अवसर दिया गया था। इसे निराला जाति-भेद के समाधान के रूप में देखते थे। मजेदार यह है, कि निराला खुद भी यह मानते हैं कि शंकर ने बौद्ध धर्म के निचली जातियों पर बढ़ते प्रभाव को रोकने और वैष्णव धर्म को पुन: स्थापित करने के लिए ऐसा किया।
निराला का वेदान्तिक झुकाव जाति भेद को समाप्त करने के लक्ष्य से ज्यादा प्रेरित है। इस लेख के आखिर में वे लिखते हैं,
“वृद्ध भारत की वृद्ध जातियों की जगह धीरे-धीरे नवीन भारत की नवीन जातियों का शुभागमन हो, इसके लिए प्रकृति ने वायुमंडल तैयार कर दिया है। यदि प्राचीन ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियाँ उनके उठने में सहायक न होंगी तो जातीय समर में अवश्य ही उन्हें नीचा देखना होगा।… इन्हीं की अजेय शक्ति भविष्य में भारत को स्वतंत्र करेगी।”
इसी बात को वे अपने अगले लेख ‘वर्तमान हिन्दू समाज’ में आगे बढ़ाते हैं। इस लेख में निराला नई सभ्यता के अनुकूल सामाजिक-सांस्कृतिक विचार के अन्तर्गत ब्रह्म समाज का विस्तार से जिक्र करते हैं। वह मानते हैं कि ब्रह्म समाज में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं था। ब्रह्म समाज ने एक स्तर पर नई सभ्यता के अनुकूल सामाजिक साम्य स्थापित करने में मदद की। इस क्रम में वे विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के कार्यों को गिनाते हैं। इसमें सभी जातियों को समान अधिकार मिले थे। रामकृष्ण के जन्म के अवसर पर विवेकानंद सभी जातियों को एक ही पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाने को आमंत्रित करते हैं।
निराला लिखते हैं कि वहाँ वर्ण भेद नहीं है। जात-पात का झमेला नहीं मानते। यहाँ पुन: निराला ‘जाति-पाँति तोड़क मंडल’ का इसी क्रम में जिक्र करते हैं। लेकिन इसमें वे संतरामजी के प्रति उदार हैं। वे लिखते हैं,
“आज जाति-पाँति तोड़क मंडल को स्थूल रूप से भी जाति-पाँति की आवश्यकता नहीं देख पड़ती। संतरामजी की पुरअसर बातें निष्पक्ष पाठकों के हृदय में पूरी सहानुभूति पैदा कर रही हैं। अन्त्यजों की शिक्षा-दीक्षा तथा अधिकारों की वृद्धि भी क्रमश: होती जा रही है। महात्माजी ने भी अन्त्यजों के लिए बहुत कुछ कहा है।”
इसके बाद फिर से वे विवेकानंद को उनके इस कथन से याद करते हैं,
“ऐ भारत के उच्च वर्ण वालों, तुम्हें देखता हूँ, तो जान पड़ता है, चित्रशाला में तस्वीरें देख रहा हूँ। तुम लोग छायामूर्तियों की तरह विलीन हो जाओ, अपने उत्तराधिकारियों को (शूद्रों को) अपनी तमाम विभूतियाँ दे दो, नया भारत जग पड़े।”
नवीन मानव धर्म
असवर्ण विवाह को लेकर पिछले लेख में जो असहमति निराला ने प्रकट की थी, उसमें भी बदले हुए विचार दिखते हैं। निराला लेख के आखिर में लिखते हैं,
“वर्तमान सामाजिक स्थिति पूर्ण मात्रा में उदार न होने पर भी विवाह आदि में जो उल्लंघन कहीं-कहीं देखने को मिलते हैं, वे भविष्य के ही शुभचिन्ह प्रकट कर रहे हैं। संसार की प्रगति से भारत की घनिष्ठता जितनी ही बढ़ेगी, स्वतंत्रता का ब्राह्म रूप जितना ही विकसित होगा, असवर्ण विवाह का प्रचलन भी उतना ही होता जाएगा।… वर्ण समीकरण की इस स्थिति का ज्ञान विद्या के द्वारा ही यहाँ के लोगों को हो सकता है। इसके साथ ही साथ नवीन भारत का रूप संगठित होता जाएगा, और यही समाज की सबसे मजबूत शृंखला होगी।”
1931 ई. की टिप्पणी ‘हमारे समाज का भविष्य रूप’ में निराला लिखते हैं,
“आज ब्राह्मण-विचार, पुरानी परिपाटी जितने अंशों में यहाँ है, देश उतने ही अंशों में पराधीन है, और नवीन मानव धर्म जितने अंशों में, उतने ही अंशों में देश स्वतंत्रता-प्रेमी।”
नवीन मानव धर्म अर्थात जिसमें जाति भेद न हो। आगे वे लिखते हैं,
“स्वतंत्रता किसी ख़ास जाति या खास मनुष्य के लिए नहीं होती। यदि कोई भंगी शिक्षा के उच्च शिखर पर पहुँचे, और यथार्थ शिक्षा अर्जित करे, तो क्या उसके लिए भंगी-शब्द का प्रयोग ही रह जाएगा?… वह कौन सी वृत्ति है, जो योग्य को योग्य नहीं समझती? अपनी महामूर्खता, महानीचता को केवल जन्मगत अधिकार के दावे पर दबा रखती है? इसी का नाश करना है। किसी मनुष्य का नहीं। तब जाति आप मर जाएगी। फिर मिठाई बेचकर राजाराम मिश्र किसी आर्ट्स के मास्टर नाई को डाँट नहीं सकते। रही बात संस्कृति की, सो नाई एम.ए. होकर संस्कृत नहीं हुआ और मिश्रजी मिठाई बेचते हुए सुसंस्कृत हैं, इससे बड़ी मूर्खता दूसरी हो नहीं सकती।”
निराला नवीन सामाजिक संगठन को इसी रूप में देखते हैं, अर्थात शूद्र अगर कर्म से श्रेष्ठ है, तो वह शूद्र नहीं और ब्राह्मण अगर कर्म से च्युत है, तो वह ब्राह्मण के रूप में प्राप्त सामाजिक अधिकार का हकदार नहीं।
निराला की यह बात रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा बार-बार हर अवस्था में ब्राह्मण को पूज्य बताने के विपरीत है। निराला ने एक टिप्पणी ही ‘अधिकार समस्या’ शीर्षक से लिखी है। यह ‘सुधा’, अर्धमासिक, लखनऊ में 1 दिसम्बर 1933 को छपी है। इसमें वे लिखते हैं,
“अधिकारवाद भारत में महाभारत के समय से प्रबल होने लगा था, और भारत के वर्णाश्रम-धर्म के भीतरी अधिकार भी तभी से और अधिक दृढ़ होकर वर्णाधिकारों के शासन में जड़ जमा रहे थे। बौद्धयुग इन्हीं भावनाओं का विरोधकाल है। पर तब तक चूँकि देश का शासन देश ही में था, इसलिए कर्मकाण्ड के अधिकारी शासक तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था की रक्षा के लिए तत्पर रहे थे। हम पहले लिख चुके हैं, संस्कृत साहित्य में पुराणयुग का प्राबल्य इसका फल है। व्यास, कालिदास, श्रीहर्ष तक में इसी वर्णाश्रमधारा की पुष्टि मिलती है।”
संस्कृत साहित्य के बारे में यह कहने का साहस रखने वाले निराला अनूठे हिन्दी लेखक है। पूरा हिन्दी नवजागरण संस्कृत साहित्य के वर्णधर्म की रक्षा वाले पक्ष पर बोलता ही नहीं।
निराला आगे जो लिखते हैं, वह उनके चिन्तन की केन्द्रीय बात है:
“पर अब वह समय नहीं रहा। अब प्रकृति ने वर्णाश्रम-धर्म के सुविशाल स्तम्भों को तोड़ते-तोड़ते पूर्ण रूप से चूर्ण कर दिया है।… अब कोई मूर्ख ही इसका अस्तित्व स्वीकार करेगा।”
निराला बार-बार लिखते हैं, कि ऊपर के वर्ण एक सुप्तावस्था में हैं, जो नवीन सभ्यता की बजाय पुरातन सभ्यता को बनाये रखने के भ्रम में हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में वह शक्ति नहीं कि वह किसी नवीन सामाजिक संगठन का निर्माण कर सके। अब वर्णाश्रम धर्म ‘अपने घरों में सोते हुओं के स्वप्नों के सदृश’ ‘पहले की जागृति के संस्कार-रूप, छायादेह मात्र रह गया’ है। ‘दूसरी जागृति में वह भ्रम ही साबित होगा।’
इसी में आगे लिखते हैं,
“जिस तरह एक ओर प्रकृति वर्णाश्रम-धर्म को तोड़ रही थी, उसी तरह दूसरी ओर वह शूद्र-शक्ति के अभ्युत्थान की तैयारी कर रही थी। अधिकार-भोग पर मनुष्य-मात्र का बराबर दावा है। जो यह समझता है, हम बड़े हैं, हम छोटे न होंगे, उसे मनुष्य कहलाने में बड़ी देर है। जो यह समझता है, बड़ा छोटा और छोटा बड़ा हो सकता है, उसे यह मानने में भी कोई आपत्ति न होगी कि शूद्र भी कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सकते हैं। शूद्रों के इसी अधिकार पर भारत का भविष्य जातीय संगठन अवलम्बित है।… यही साम्य स्थिति की वर्तमान उद्भावना कहती है।”
नवीन सामाजिक संगठन सम्बन्धी अपने इन्हीं विचारों के सन्दर्भ में निराला राजनीतिक यथार्थ को भी जाँचते हैं। वहाँ भी निराला अन्य हिन्दी लेखकों से भिन्न हैं। पृथक निर्वाचन को लेकर निराला की टिप्पणी ध्यान देने की है। वे लिखते हैं,
“सरकार ने राजनीति की यह बड़ी टेढ़ी मार दी है। यहीं इसी अछूत समस्या के पास हिन्दुओं की तमाम प्राचीन कमजोरियाँ एकत्र हैं।… यह पृथक-निर्वाचन समस्या जब से खड़ी हुई तमाम राजनीति का रुख ही बदल गया। पर यह अच्छा ही हुआ। अब सुधार ठीक जड़ पर पहुंचा है।”
यह टिप्पणी ‘हिन्दुओं का जातीय संगठन’ शीर्षक से 1932 नवंबर में ‘सुधा’ की सम्पादकीय में छपी है।
महात्मा गांधी के अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए निराला अपनी दो टिप्पणियों; ‘महात्माजी और हरिजन’, (‘सुधा’ अर्द्धमासिक, लखनऊ, 16 अगस्त 1933) तथा ‘सनातन धर्म और अछूत’ (वही 16 नवंबर 1933) में अपील करते हैं: ‘इससे सहानुभूति ही नहीं-इसकी सिद्धि के लिए जहाँ तक हो, मदद करें…।’
निराला ने ‘समाज और मनुष्य’, ‘सामाजिक व्यवस्था’ समेत कई अन्य टिप्पणियों में स्वाधीनता आन्दोलन और भावी आधुनिक, नवीन राष्ट्र निर्माण के सन्दर्भ से जाति और वर्ण पर विचार किया है। जितने सन्दर्भ दिए गये, वे 1933 तक के हैं।
1933 की ही एक टिप्पणी ‘राजनीति के लिए सामाजिक योग्यता’ में निराला की भाषा का अन्दाज बहुत कुछ बयाँ करता है,
“हम बहुत पहले से कह रहे हैं, समाज का आमूल परिवर्तन जरूरी है।… वैश्य-शक्ति, राज-शक्ति, ब्राह्मण-शक्ति तीनों योरप को गयीं। हम इस बात को न समझकर, ब्राह्मण बनकर, भारतीय संस्कृति के एकच्छत्र सम्राट होकर भाइयों पर खोखली भारतीयता का रोब गाँठते रहें। अब उस भारतीयता से कैसा फल पैदा हुआ, वह सामने है, चखिए।”
आगे लिखते हैं,
“जो ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी वर्णोच्चता का ढोंग भी नहीं छोड़ सकते, अपने ही घर के अन्त्यजों को अधिकार नहीं दे सकते, भारतीयता के अंधेरे में प्रकाश देखने के आदी हैं, वे बिना दिये हुए कुछ पाने का विचार कैसे रखते हैं? उनकी सामाजिक नीचता ‘समाज’ शब्द को, उन्नतिशीलता के अर्थ को कैसे पुष्ट कर सकती है? हमारी राजनीतिक दुर्बलता यहीं पर है। यहीं से हमें समाज-जातीय समाज-भारतीय समाज की नींव डालनी है। उसी की मजबूती हमारे राष्ट्र की दृढ़ता है।”
निराला राजनीतिक संघर्ष के लिए नवीन सामाजिक योग्यता की बात करते हैं। समाज के आमूल परिवर्तन की बात करते हैं। इसी में वे लिखते हैं,
“जो समाज पुराना, हारा हुआ है, वह कितनी भी प्राचीन विभूतियों से युक्त हो, वह नवीन युग के लिए मृत है। उसी से पहले हमें लड़ना था, लड़कर परास्त करना था। परास्त कर नये समाज को सजीव और बहुजनोंवाला बनाना था। तब हम राष्ट्र का पहला सोपान तय करते। इसी समाज से राष्ट्र को बल मिलता। यही समाज राष्ट्र का समाज है। जो लोग यह तर्क उपस्थित करते हैं, कि इस तरह भष्टाचार पैदा होगा (सामाजिक भ्रष्टाचार, जोर मेरा), वे मूर्ख हैं, फिर कहिए, हम फिर कहते हैं, वे मूर्ख हैं। अगर आप नहीं जानते, तो विश्वास कीजिए, वे मूर्ख हैं। जो मनुष्य देश के सभी मनुष्यों को अपने बराबर समझता है, वह अगर भ्रष्टाचार फैलाता है, तो मनुष्य की उच्चता का, सदाचार का कोई प्रमाण नहीं।”
सामाजिक समता, समानता के विचार को आज कुछ लोग सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन मानते हैं। कौन लोग हैं, जो आजादी के बाद संविधान में शामिल सामाजिक बराबरी के विचार से अपार घृणा करते हैं? कौन लोग हैं, जो आज भी भारतीयता को पतित, मनुष्यविरोधी वर्णवादी मूल्यों, सनातनी मूल्यों आदि से परिभाषित कर रहे हैं? इसे याद कर लेने पर निराला कहाँ खड़े हैं, इसे सहज समझा जा सकता है। ऐसे लोग 1930 के दशक में भी पूरे जोर, दमखम से, सक्रिय थे। निराला उनसे मुखातिब थे।
निराला इसी टिप्पणी में आगे लिखते हैं,
“इसलिए तोड़कर फेंक दीजिए जनेऊ, जिसकी आज कोई उपयोगिता नहीं, जो बड़प्पन का भ्रम पैदा करता है, और समस्वर से कहिए कि आप उतनी ही मर्यादा रखते है, जितनी आपका नीच-से-नीच पड़ोसी, चमार या भंगी रखता है। तभी आप महामनुष्य हैं। … एक समाज आपको च्युत करेगा, तो आपको दूसरा समाज मिलेगा। उसी समाज से आप साबित कर सकेंगे, आप समाज से नहीं बढ़े, समाज आपसे बढ़ा है। यहीं से राष्ट्र की वृद्धि है, शक्ति है, उत्थान है, गति है। सब सुधार, सारी शिक्षा, कुल वैमनस्य का प्रतिरोध यही है। आज का सच्चा भारतीय यही है।”
यह टिप्पणी है 1933 ई. की। 16 अगस्त, ‘सुधा’ अर्द्धमासिक, लखनऊ।
व्यक्तित्वान्तरण
इसके बाद निराला का वैचारिक लेखन कम होने लगता है। रचनात्मक गद्य साहित्य अधिक सामने आता है। जाति एवं वर्ण संबन्धी उनके विचार यहाँ और स्पष्ट होकर आए हैं।
‘देवी’, ‘चतुरी चमार’, ‘कुल्ली भाट’, ‘सुकुल की बीवी’ इस सन्दर्भ से महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। निराला वेदान्तिक दर्शन से आगे इन रचनाओं में जाते हैं।
‘सुकुल की बीवी’ कहानी में एक कट्टर हिन्दू ब्राह्मण युवक के व्यक्तित्वान्तरण और मुस्लिम पृष्ठभूमि की युवती से विवाह करने के प्रसंग तथा ‘कुल्ली भाट’ में कुल्ली के अछूतों के लिए खोले स्कूल में जाने के बाद नैरेटर या कथावाचक के आत्मस्वीकार से कोई गुजरे तो उसे निराला के बदले विचार को समझने में संकट नहीं होगा। यहाँ वर्ण और जाति भेद के अलावा धार्मिक भेद के विरुद्ध निराला मनुष्यता और बराबरी का संसार रचते हैं।
‘सुकुल की बीवी’ निराला की चर्चित कहानी है। यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ‘सुधा’ में 1937 ईस्वी में छपी। इसी नाम से निराला की कहानियों का एक संकलन भी छपा था। इस कहानी का समय ‘कुल्ली भाट’ और ‘बिल्लेसुर बकरिहा’ के छपने के आसपास ही है।
उस समय तक निराला सांस्कृतिक, सामाजिक और सियासी मसलों पर एक निर्णायक और परिवर्तित विचार तक पहुँच रहे थे। मसलन वर्णवाद, जाति, हिन्दू-मुस्लिम आदि समस्याओं को अपनी रचनाओं में नये बोध या आधुनिक प्रगतिशील बोध के साथ प्रस्तुत कर रहे थे। ‘सुकुल की बीवी’ कहानी की अन्तर्वस्तु में यह सब है। इस कहानी में निराला कहानी-वाचक भी हैं और कहानी के पात्र भी।
कहानी यह है कि निराला के स्कूल के मित्र सुकुल पड़ोस में रहने वाली ग्रेजुएट छात्रा से प्रेम कर बैठते हैं। बाद को उसके साथ रहने लगते हैं लेकिन दोनों के विवाह में एक दिक्कत है। सुकुल की प्रेमिका, बाद में बीवी, ब्राह्मण स्त्री के पेट से पैदा हुई है लेकिन पली-बढ़ी है मुसलमान के घर में। सुकुल चाहते हैं, कि निराला उसे अपनी बहन बनाकर यह विवाह सम्पन्न कराएँ। निराला ऐसा ही करते हैं और सुकुल का विवाह करवाते हैं।
मुख्य कथा बस इतनी है। लेकिन, इतनी सी कथा में हिन्दी समाज का यथार्थ, स्त्री की समाज में, परिवार में हैसियत और इसी बहाने 1930 के दशक में हिन्दू-मुसलमान समस्या का अन्तर्गुंथन निराला करते हैं। और, इन्हीं के बीच से सुकुल, कुँवर और खुद निराला का व्यक्तित्वान्तरण सामने आता है।
सुकुल स्कूल के दिनों में चोटीधारी ब्राह्मण युवक थे। साथ ही, हिन्दूवादी संस्कृति और विचार के मुख्य प्रवक्ता हैं, लेकिन यही सुकुल बाद में खुद के जीवन के विकास में एक आधुनिक प्रगतिशील मनुष्य और व्यक्ति बनकर उभरते हैं। कुँवर पैदा होती है जरूर ब्राह्मण स्त्री के पेट से, लेकिन वह है पूरी तरह से मुस्लिम रीति-रिवाज, परम्परा और संस्कृत में पली हुई। बाद में वह भी प्रेम में होकर बदलती है। सुकुल के मातृविहीन बच्चे को पालती है और एक आधुनिक स्त्री के रूप में उभरती है।
लेकिन यह आधुनिकता नयी नागरिकता के साथ है। निराला दोनों को उनकी धार्मिक पहचान से बाहर निकालकर नयी पहचान देते हैं। यह पहचान आधुनिक, स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष है। इस कहानी में निराला स्वयं भी हैं और हिन्दूवाद से अलग उनका स्पष्ट पक्ष है।
निराला ने सुकुल के स्कूल के जीवन प्रसंग को भी व्यंग्य का हिस्सा बनाकर इस पर ही चोट की है। पुरातनपंथियों और हिन्दूवाद की ही खिल्ली उड़ाई है।
“सुकुल का परिचय आवश्यक है। सुकुल मेरे स्कूल के दोस्त हैं, साथ पढ़े। उन लड़कों में थे जिनका यह सिद्धान्त होता है, कि सिर कट जाए चोटी न कटे। सुकुल-जैसे चोटी के एकान्त उपासकों से चोटी की आध्यात्मिक व्याख्या कई बार सुनी थी, पर सग्रन्थि बालों के बल्ब में आध्यात्मिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश न मुझे कभी दीख पड़ा, न मेरी समझ में आया। फलत: सुकुल की और मेरी अलग-अलग टोलियाँ हुई। उनकी टोली में वे हिन्दू लड़के थे, जो अपने को धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ समझते थे, मेरी में वे लड़के, जो मित्र को धर्म से बड़ा मानते हैं, अत: हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान सभी।”
अगर कोई, निराला को हिन्दूवादी मानता है, तो उसे ‘सुकुल की बीवी’ कहानी पढ़नी चाहिए।
इसी तरह ‘कुल्ली भाट’ है। कुल्ली भी मुसलमान स्त्री से विवाह करते हैं और दलित बच्चों के लिए विद्यालय खोलते हैं। इन दोनों रचनाओं में निराला के जाति, धर्म सम्बन्धी विचार हैं। इन रचनाओं के विचार-तत्व ब्राह्मणवाद और हिन्दूवाद के विपरीत हैं। वेदान्तिक साम्य का विचार भी पीछे छूट जाता है।
इस सन्दर्भ से ‘कुल्ली भाट’ से एक प्रसंग का उद्धरण देखा जा सकता है, “तीसरे दिन कुल्ली आये। बड़े आदर से ले गये। देखा, गड़हे के किनारे, ऊँची जगह पर, मकान के सामने एक चौकोर जगह है। कुछ पेड़ हैं। गड़हे के चारों ओर के पेड़ लहरा रहे हैं। कुल्ली के कुटीनुमा बँगले के सामने टाट बिछा है। उस पर अछूत लड़के श्रद्धा की मूर्ति बने बैठे हैं। आँखों से निर्मल रश्मि निकल रही है। कुल्ली आनन्द की मूर्ति साक्षात आचार्य। काफ़ी लड़के। मुझे देखकर सम्मान प्रदर्शन करते हुए नत सिर अपने-अपने पाठ में रत हैं। बिल्कुल प्राचीन तपोवन का दृश्य। इनके कुछ अभिभावक भी आये हैं। दोने में फूल लिए हुए मुझे भेंट करने के लिए। इनकी ओर कभी किसी ने नहीं देखा। यह पुश्त-दर-पुश्त से सम्मान देकर नतमस्तक ही संसार से चले गये हैं। संसार की सभ्यता के इतिहास में इनका स्थान नहीं। यह नहीं कह सकते हमारे पूर्वज कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणाद थे; रामायण, महाभारत इनकी कृतियाँ हैं; अर्थशास्त्र, कामसूत्र इन्होंने लिखे हैं; अशोक, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज उनके वंश के हैं। फिर भी ये थे और हैं।”
“अधिक न सोच सका। मालूम दिया, जो कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं; जो कुछ किया है, व्यर्थ है; जो कुछ सोचा है, स्वप्न। कुल्ली धन्य है। वह मनुष्य है, इतने जम्बूकों में वह सिंह है। वह अधिक पढ़ा-लिखा नहीं; लेकिन अधिक पढ़ा-लिखा कोई उससे बड़ा नहीं। उसने जो कुछ किया है, सत्य समझ कर। मुख-मुख पर इसकी छाप लगी हुई है। ये इतने दीन दूसरे के द्वार पर क्यों नहीं देख पड़ते? मैं बार-बार आँसू रोक रहा था।”
“इसी समय बिना स्तव के, बिना मंत्र के, बिना वाद्य, बिना गीत के, बिना बनाव, बिना सिंगारवाले वे चमार, पासी, धोबी और कोरी दोने में फूल लिए हुए मेरे सामने आ-आकर रखने लगे। मारे डर के हाथ पर नहीं दे रहे थे कि कहीं छू जाने पर मुझे नहाना होगा। इतने नत। इतना अधम बनाया है मेरे समाज ने उन्हें।”
“कुल्ली ने उन्हें समझाया है, मैं उनका आदमी हूँ, उनकी भलाई चाहता हूँ। उन्हें उसी निगाह से देखता हूँ, जिससे दूसरे को। उन्हें इतना ही आनन्दविह्वल किए हुए है। बिना वाणी की वह वाणी, बिना शिक्षा की वह संस्कृति, प्राण का पर्दा-पर्दा पार कर गयी। लज्जा से मैं वहीं गड़ गया। वह दृष्टि इतनी साफ़ है कि सबकुछ देखती-समझती है। वहाँ चालाकी नहीं चलती। ओफ्! कितना मोह है। मैं ईश्वर, सौन्दर्य, वैभव और विलास का कवि हूँ!— फिर क्रांतिकारी!!”
“संयत होकर मैंने कहा, ‘आप लोग अपना-अपना दोना मेरे हाथ में दीजिए, और मुझे उसी तरह भेंटिए, जैसे मेरे भाई भेंटते हैं।’ बुलाने के साथ मुस्कुराकर वे बढ़े। वे हर बात में मेरे समकक्ष हैं, जानते हैं। घृणा से दूर हैं। वह भेद मिटते ही आदमी-आदमी मन और आत्मा से मिले, शरीर की बाधा न रही।”
“इस रोज मैं और कुछ नहीं कर सका, देखकर चला आया, कुछ लड़कों से कुछ पूछकर।”
यह लंबा उद्धरण इसलिए, कि समाज, साहित्य, शिल्प, संवेदना, भाषा आदि के तो उच्च दर्शन इसमें होते ही हैं, लेकिन इसमें एक और बात दिखती है; जो एक रचनाकार और मनुष्य दोनों स्तरों पर निराला के बनने से जुड़ी है। बाहर से भीतर और भीतर से बाहर आवाजाही का ऐसा साहस परले ही दिखा पाए हैं हिन्दी रचना संसार में। आत्मा को पिघला देना और फिर उसे नये ढाँचे-साँचे में ढालने की प्रक्रिया इसमें दिखती है। इसे ही लोक में आत्मा को छीलना कहते हैं। इसी में ऊँचे उठते जाने और अकेले होते जाने के खतरे थे, जो निराला ने उठाये/पाये।
एक-एक पैराग्राफ, एक-एक पंक्ति, एक-एक शब्द पर ध्यान दें और 1940 ई. के बाद लिखी उनकी ‘कुकुरमुता’, ‘अणिमा’, ‘बेला’ और ‘नये पत्ते’ की कविताओं की बदली वस्तु और संवेदना, काव्य-भाव की भंगिमा, तेवर को परखें तो ‘कुल्ली भाट’ के भू-चिन्ह होने वाली बात और स्पष्ट हो जाएगी।
तुलसीदास और कबीर
निराला जब तक साहित्य के माध्यम से हिन्दी समाज की संस्कृति को जाँचते हैं, तब तक वे तुलसीदास और शंकर के वेदान्त दर्शन को मुख्य मान-मूल्य बनाते हैं, लेकिन जब वे हिन्दी समाज से व्यावहारिक मेल-जोल में उतरते हैं, तो खुद को बदलते हैं। 1930-32 के बाद का निराला का विकास आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष दिशा में है।
जिस तुलसीदास को निराला ने एक तरह से हिन्दी जाति का मान-मूल्य बनाया था, अब हिन्दी समाज के पिछड़े मूल्यों की संस्कृति के निर्माण में उस तुलसीदास के रामायण को जिम्मेदार बताते हैं।
‘देवी’ कहानी में वे कहते हैं कि ‘हिन्दुओं के मँजे स्वभाव को गोस्वामी तुलसीदासजी ने और माँज दिया है।’ यह कहानी 1934 की है। निराला के इस व्यंग्य का अभिप्राय इसी कहानी में पहले आए इस अनुच्छेद से स्पष्ट हो जाता है:
“चार किताबों की रूह छानकर एक किताब लिख दूँगा। ‘सीता’, ‘सावित्री’, ‘दमयन्ती’ आदि की पावन कथाएँ आँखें मूँदकर लिख सकता हूँ। तब बीवी के हाथ ‘सीता’ और ‘सावित्री’ आदि देकर बग़ल में ‘चौरासी आसन’ दबानेवाले दिल से नाराज न होंगे। उनकी इस भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश करके ही बिगड़ा हूँ। अब जरूर संभलूँगा। राम, श्याम जो-जो थे पूजने-पुजाने वाले सब बड़े आदमी थे। बगैर बड़प्पन के तारीफ़ कैसी? बिना राजा हुए राजर्षि होने की गुंजाइश नहीं, न ब्राह्मण हुए बगैर बह्मार्षि होने की है। वैश्यर्षि या शूद्रर्षि कोई था, इतिहास नहीं; शास्त्रों में भी प्रमाण नहीं; अर्थात् नहीं हो सकता। बात यह कि बड़प्पन चाहिए। बड़ा राज्य, बड़ा ऐश्ववर्य, बड़े पोथे, तोप-तलवार गोले-बारूद, बन्दूक किर्च रेल तार, जंगी जहाज टारपेडो, माइन-सबमेरीन-गैस, पल्टन-पुलिस, अट्टालिका-उपवन आदि-आदि सब बड़े-बड़े इतने कि वहाँ तक आँख नहीं फैलती, इसलिए कि छोटे समझें वे कितने छोटे हैं। चन्द्र, सूर्य, वरुण, कुबेर, यम, जयन्त, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक बाक़ायदा बाहिसाब ईश्वर के यहाँ भी छोटे से बड़े तक मेल मिला हुआ है।”
इसी तरह 1935 का एक लेख है, ‘हिन्दी में तर्कवाद’। इसमें वे लिखते हैं,
“हमारा साहित्य इस सिद्धान्त से बहुत पीछे है। इसीलिए हमारे यहाँ तरह-तरह की बुराइयाँ हैं, तरह-तरह की रूढ़ियाँ स्थान पाये हुए हैं। तरह-तरह के प्रचार, जो यथार्थ मनुष्यता के विरोधी हैं, चलते जा रहे हैं। साहित्य में हम खड़ी बोली के रूप में भी बहुत कुछ वैसे ही हैं, जैसे पहले थे। हमारे अधिकांश जन तीरधनुष लेकर राक्षसों का नाश करते हैं…। धर्म, शिखा-सूत्र आदि की सैकड़ों रूढ़ियाँ हैं, जिनसे वास्तव में देश, साहित्य तथा भावना को क्षति पहुँचती है।” (‘सुधा’, मासिक, लखनऊ)
अर्थात् 1930 ई. के बाद निराला के चिन्तन और विचार में एक बदलाव दृष्टिगोचर होने लगता है। हिन्दी समाज और जाति को लेकर वे एक निराशा में भी जाते हैं। ‘राम की शक्तिपूजा’ में इसकी झलक है। ‘अन्याय जिधर है उधर शक्ति’ की घोषणा करने वाले राम तुलसीदास के राम नहीं हैं। राम के मोहभंग में निराला का मोहभंग भी शामिल है। यह मोहभंग उन्हें शक्ति की मौलिक कल्पना की ओर ले जाता है। तुलसीदास भले ही वर्णाश्रम के रक्षक रहे हों, निराला के तुलसीदास इसकी विडंबना को पहचानते हैं।
वे शेष-श्वास, पशु, मूक-भाष,
पाते प्रहार अब हताश्वास;
सोचते कभी, आजन्म ग्रास द्विजगण के
होना ही उनका धर्म परम,
वे वर्णाधम, रे द्विज उत्तम,
वे चरण-चरण बस, वर्णाश्रम-रक्षण के!
यह मोहभंग सरोज स्मृति में इस स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुँचता है कि ब्राह्मण संस्कृति की विषय वेलि में विष ही फलित होना है।
निराला हिन्दी जातीयता की खोज में तुलसीदास के पास बार-बार जाते हैं, यह हिन्दी नवजागरण की अन्तर्वस्तु और उसकी मुख्य दिशा के मेल में है, लेकिन ‘राम की शक्तिपूजा’ में उनकी दिशा भिन्न है।
तुलसीदास और ‘वैदान्तिक साम्य’ के दर्शन पर वे जो लेख लिखते हैं, वे सभी प्राय: 1920-22 के हैं। अर्थात् हिन्दी जाति से परिचय का बिलकुल प्रारम्भिक समय।
मसलन, ‘तुलसीकृत रामायण में अद्वैत तत्व’ (सितम्बर-अक्टूबर, 1922, ‘समन्वय’, कलकत्ता), ‘ज्ञान और भक्ति पर गोस्वामी तुलसीदास’ (मई-जून, 1923, ‘समन्वय’, कलकत्ता), ‘तुलसीकृत रामायण का आदर्श’ (अगस्त 1923, ‘माधुरी’, लखनऊ)। इसके बाद ‘विज्ञान और गोस्वामी तुलसीदास’ (अगस्त-सितम्बर, 1927, ‘समन्वय’, कलकत्ता), ‘दो महाकवि, गोस्वामी तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ (मार्च-अप्रैल, 1929, ‘मतवाला’ साप्ताहिक, कलकत्ता), ‘तुलसीकृत रामायण की व्यापकता’ (1930, ‘सुधा’, लखनऊ), ‘तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ’ (1931, ‘सुधा’)।
इसके बाद का कोई लेख नहीं है।इन लेखों में निराला बांग्ला जातीय साहित्य के बराबर हिन्दी जातीयता में साहित्यिक श्रेष्ठता की तलाश करते हुए तुलसीदास के पास जाते हैं। इसीलिए बार-बार वे तुलसीदास और रवीन्द्रनाथ टैगोर की तुलना करते हैं।
लेकिन जब वे साहित्य के इलाके से बाहर निकल कर हिन्दी समाज की व्यावहारिक दुनिया में प्रवेश करते हैं तब तुलसी-साहित्य के सांस्कृतिक प्रभाव को समाज के आधुनिक निर्माण के विपरीत पाते हैं।
तुलसीदास के रामायण का आदर्श बताने-गाने वाले समाज में सबसे अधिक जाति-भेद के पूजक और मानवीय करुणा से हीन हैं। दूसरे, दलित जातियों में वे कबीर-साहित्य का व्यापक असर देखते हैं। ‘चतुरी चमार’ कहानी में इसका प्रसंग है। यह कहानी 1934 की है।
हिन्दी नवजागरण में पुराणों, वेदों, उपनिषदों के ज्ञान, विचार को धो-पोंछ कर समकालीन बनाने और उसे ही भारतीय या जातीय बताने की एक आम धारणा थी। जिसे औपनिवेशिक सत्ता-संस्कृति ने गौरवपूर्ण बताया उसे ही लपक लेने का चलन था। निराला उससे अलग अपने तर्क-विवेक से चलते हैं। वे प्राचीन जातीय साहित्य को आधुनिक सन्दर्भ में आलोच्य बनाना चाहते हैं।
जून, 1933, ‘सुधा’ में छपे लेख, ‘साहित्य और जनता’ में निराला हिन्दी समाज और साहित्यिक दोनों की इस स्थिति पर लिखते हैं,
“हमारे निन्नानबे फ़ीसदी साहित्यिकों को और सौ फीसदी जनता को भगवान् श्रीरामचन्द्र पर, उनके जन्म-कर्मादि पर, पूरा-पूरा विश्वास है। अत: आज यदि राम के विरोध में कोई प्रासंगिक बात की जाय, तो जनता उसे सुनने को तैयार नहीं; साहित्यिकों में केवल सुनने का धैर्य है, मत बदलने की शक्ति नहीं।”
निराला साहित्य को मत बदलने की शक्ति से युक्त देखना चाहते हैं, लेकिन हिन्दी के निन्नानबे फ़ीसदी साहित्यिकों में यह शक्ति नहीं। आगे वे लिखते हैं,
“यह अवश्य ही युगों की संचित साहित्यशक्ति का ही दौर्बल्य है। इससे जनता को कुछ हासिल हुआ, तत्व के भीतर से यह साबित नहीं होता। किसी महान भक्त से ही पूछिए, अग्नि से यज्ञ-हवि कैसे पैदा होती है, जानकीजी ऋषियों के खून से भरे घड़े से, जमीन से, कैसे निकलती हैं, महावीरजी लंका से एक ही रात में उत्तराखण्ड जाकर, सजीवन-मूरिवाला पहाड़ लेकर, रात ही-भर में लंका कैसे लौट आते हैं, तो आपको युक्तिपूर्ण, सन्तोषप्रद उत्तर कदापि प्राप्त न होगा।”
इससे यह भी पता चलता है कि तार्किकता निराला के चिन्तन का प्राणतत्व है। तार्किकता ने ही दुनिया में तमाम पुनर्जागरण नवजागरण आदि को जन्म दिया। लेकिन हिन्दी नवजागरण में वह है ही नहीं। यह नवजागरण ज्यादातर भाषागत रूप और शैली तक ही सीमित रहा!
आगे वे लिखते हैं,
“भारत में प्रचलित, भारतीय नाम से प्रसिद्ध आर्य-सभ्यता की उज्ज्वल श्री से मण्डित जो कुछ प्राप्त होगा, उसका अधिकांश इसी प्रकार शिरश्चरणहीन, अदृष्ट, काल्पनिक जन्तुविशेष ज्ञात होगा, जहाँ मानवीय दृष्टि की गति नहीं।”
निराला उस समय यह सब भारतीयता या भारतीय संस्कृति की हिन्दूवादी प्रस्थापनाओं के सापेक्ष लिख रहे थे। आज सत्ता पर वही तत्व काबिज हैं, जो ‘शिरश्चरणहीन’ और ‘अदृष्ट’ हैं तथा जिन्होंने हिन्दी समाज को ऐसी ही संस्कृति से ढंक दिया है।
हिन्दी धारावाहिक, सिनेमा, साहित्य में आज फिर से शिरश्चरणहीन और अदृष्ट बातों का बोलबाला है। आज कोई हिन्दी समाज की इस गति को देखकर निराला के साहित्य, चिन्तन को देखे तो उसका महत्व जान सकता है और यह भी कि निराला हिन्दी की जातीय पहचान को किन आधारों पर खड़ा करना चाह रहे थे।
निराला इसी में आगे लिखते हैं, कि इन्हीं ‘बुराइयों का दूरीकरण देश का, साहित्य का सच्चा उद्धार है।’
एक अन्य लेख, ‘साहित्य का विकास’ में वे लिखते हैं,
“हमारे साहित्यिकों का ज्ञान किसी धातु के बने बर्तन की तरह जड़ है, जो अपना गढ़ा हुआ स्वरूप बदल नहीं सकता।” (‘सुधा’, मासिक, लखनऊ, 1932)
जैसे-जैसे निराला हिन्दी समाज से परिचित होते हैं, वैसे-वैसे उनके सोच-विचार और धारणा में बदलाव होता है। सबसे बढ़कर निराला बंगाल के नवजागरण की विरासत लेकर आते हैं।
निराला जिस समय बंगाल से वापस आते हैं, तब तक वहाँ नवजागरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर का सांस्कृतिक वैचारिक व्यक्तित्व वैश्विक महत्ता प्राप्त कर चुका था। इसका प्रभाव कला, साहित्य, समाज, राजनीति सब पर पड़ रहा था।
बंगाल और हिन्दी समाज के भीतर के सांस्कृतिक अन्तर या नवजागरण की अन्तर्वस्तु के अन्तर का एक प्रतीकात्मक प्रकरण कबीर को लेकर पाया जा सकता है।
प्राय: राष्ट्रीयताओं में नवजागरण की सांस्कृतिक थाती संत साहित्य है। बंगाल में इसी प्रक्रिया में कबीर को खोजा जा चुका था। हिन्दी में कबीर को लेकर हिचक है। कारण है कबीर की वर्णवाद के प्रति आक्रामकता।
1920 ई. के बाद हिन्दी का जो लघु बौद्धिक तबका बन रहा था, उसमें कबीर को लेकर एक भय है और तुलसीदास को लेकर एक मोह है। खुद निराला एक लेख में लिखते हैं, कि जिस कबीर से रवीन्द्रनाथ प्रभाव ग्रहण करते हैं, उसी कबीर को लेकर हिन्दी में आदर नहीं है। ‘साहित्य का विकास’ लेख में निराला लिखते हैं,
“कबीर एक ऐसे ऊँचे विचारवाले साहित्यिक हमारी हिन्दी में हैं, जिनका जोड़ संसार में दुर्लभ है। क्या कहीं एक अपढ़ मनुष्य इतना बड़ा ज्ञानी कवि हुआ है? हिन्दी साहित्य का ज्ञान-काण्ड यदि कबीर के साहित्य को कहें, तो अत्युक्ति न होगी। पर हिन्दी में ही कबीर का जैसा आदर होना चाहिए, नहीं हुआ। बंगाल में कबीर से बढ़कर हिन्दी का दूसरा कवि नहीं समझा जाता।… रवीन्द्रनाथ जैसे महाकवि कबीर की प्रतिभा पर मुग्ध हैं।”
1920 ई. तक हिन्दी नवजागरण की अन्तर्वस्तु में जो कुछ भी था, वह मूल्य और नैतिकता के स्तर पर वर्णवाद से मुक्त नहीं था। इसीलिए कबीर का आदर नहीं। फिर इस हिन्दी साहित्य या नवजागरण की अन्तर्वस्तु क्या है, इस पर निराला लिखते हैं,
“हमारी हिन्दी में अभी छन्दों के हस्व-दीर्घ की मात्राएँ गिनी जा रही हैं। भारतीयता, शालीनता और ‘पन’ के विचार से साहित्यिकों को फुरसत नहीं मिल रही।… देश ही में एक तरफ़ तमाम विश्व की भिन्न जातीय संस्कृति (Culture) अपने साहित्य में मिलाने की कोशिश हुई और हो रही है और हमारे यहाँ अभी साहित्यिक ‘भाषा कैसी होनी चाहिए’ प्रश्न नहीं हल कर सके।”
अर्थात् हिन्दी नवजागरण में जो साहित्य रचा जा रहा था, उसमें अपने समय के मनुष्य की कोई छवि, छाया या प्रतिबिम्ब नहीं था। उसमें ‘साहित्यिक विशालता, उदारता, स्वातन्त्र्य’ का अभाव है। वे लिखते हैं,
“हमारी हिन्दी को ऐसी ही भावना से युक्त साहित्यिकों की आवश्यकता है। सत्य की रक्षा के लिए साहित्यिक अपने प्राणों का बलिदान कर दे। सत्य वही है, जो मनुष्य- मात्र में है। ज्ञान में हिन्दू, मुसलमान नहीं।… हिन्दी में बहुत करना है, बहुत पड़ा है, बहुत पीछे हैं हम।” (‘साहित्य का विकास’, दिसम्बर 1932, ‘सुधा’, लखनऊ)
इसीलिए हिन्दी नवजागरण को निराला भिन्न भूमि पर ले जाते हैं। वर्णवाद, जाति-भेद, ऊँच-नीच को चुनौती देते हैं, आलोच्य बनाते हैं। यहाँ से वे हिन्दी की नयी, आधुनिक जातीय पहचान बनाना चाहते हैं।
निराला इस विचार तक पहुँचते हैं, कि आधुनिक समय में हमें नये मनुष्य को गढ़ना होगा। इस मनुष्य को साहित्य में स्थापित करना होगा। इस नये मनुष्य को बनाने के लिए, नये सांस्कृतिक मूल्य स्थापित करने होंगे। इन मूल्यों में मानवीय तत्व हों, साम्य हो, साथ ही, विश्व मानवतावाद की उपलब्धियाँ भी शामिल हों।
अपने इस विचार के चलते निराला वेदान्त दर्शन और तुलसीदास के प्रस्थान बिन्दु से 1938-40 तक एक मोड़ लेने लगते हैं। इस दौरान वे हिन्दी के साहित्य की दुनिया से बाहर निकल कर वास्तविक हिन्दी समाज में, इसके जन के बीच में चलने-फिरने, उठने-बैठने लगते हैं।
ये वास्तविक जन निराला को बदलने लगते हैं। निराला का कथा साहित्य ऐसे जन, समाज और ऐसे मनुष्यों से क्रमश: भरता जाता है। हिन्दी की जातीय पहचान को बनाने के विचार का आधार तत्व व्यवहार में आने पर बदलने लगता है। और खुद निराला बदलते हैं।
1938 ईस्वी के बाद का निराला का साहित्य इसका प्रमाण है अर्थात् व्यवहार से विचार बदलता है या जिस विचार को लेकर वे समाज के उपेक्षित, वंचित, दीन-हीन, छोटे लोगों को साहित्य में रचते हैं, वे सभी निराला के विचार को बदल देते हैं।
‘कुल्ली भाट’ का विद्यालय प्रसंग हो या ‘देवी’ कहानी की अन्तर्वस्तु, निराला के इस बदलाव के चिह्न को देखा-पाया जा सकता है। ‘कुकुरमुत्ता’ की कविताओं को कोई देखे और उसमें अन्तर्भुक्त आक्रामकता, उसके तेवर, तेज को कोई जाँचे तो वह इस बदलाव को समझ सकता है।
हिन्दी जातीयता को हिन्दू जातीय पहचान से अलग आधुनिक तत्व चिन्तन और विचार से जोड़ने की दिशा में निराला का यह प्रयास ऐतिहासिक है!
[दुर्गा सिंह से [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सऐप नंबर: 9451870000]