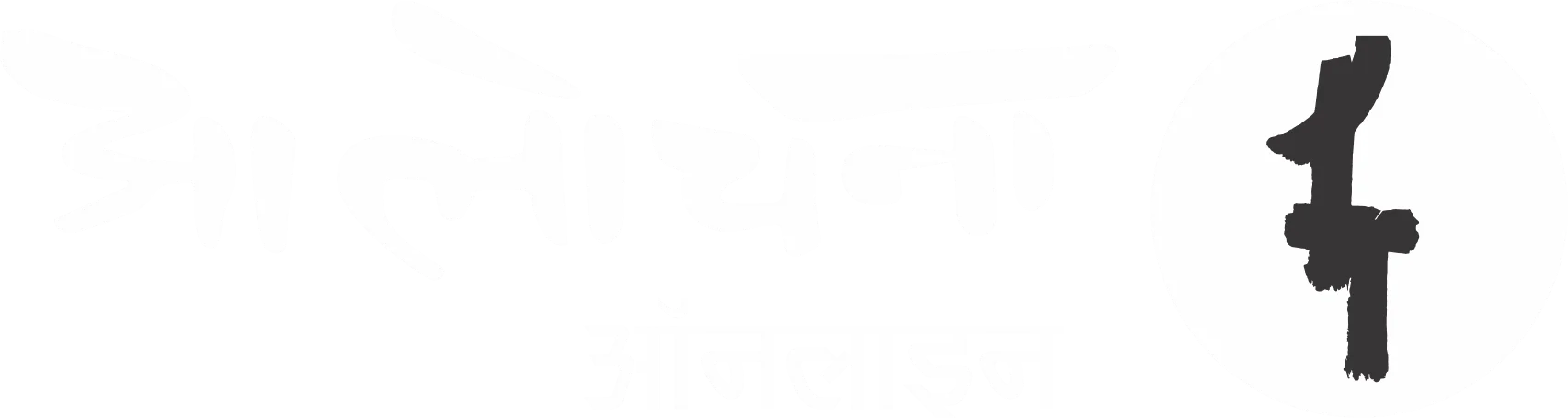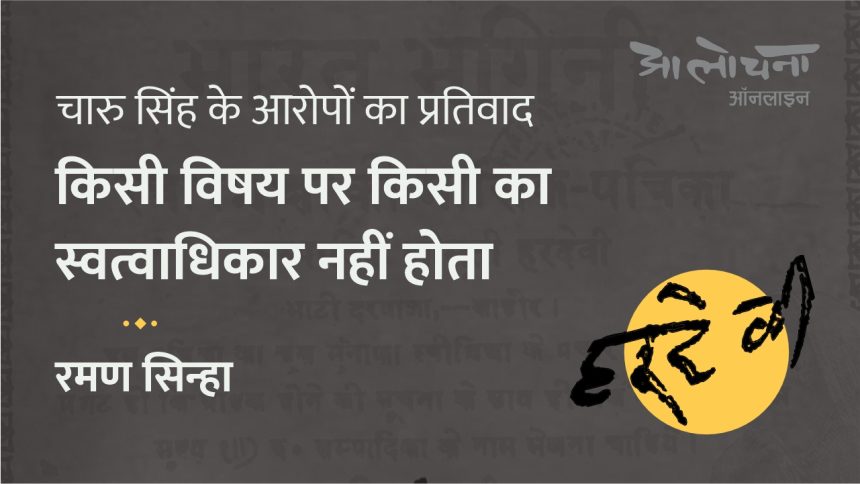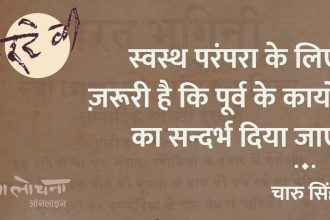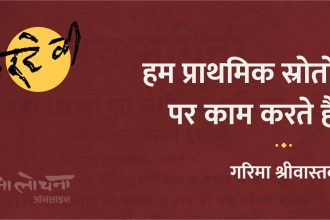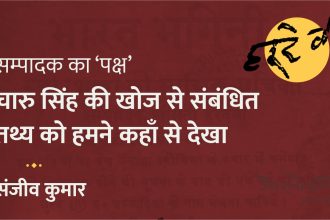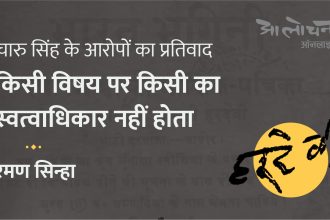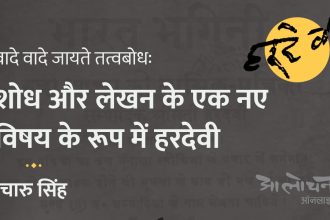वाद-विवाद और संवाद से ही आलोचना विकसित होती है। चारु सिंह के आलेख के जिस हिस्से को हमने ऑनलाइन साझा किया था, उसका जवाब प्रो. रमण सिन्हा ने भेजा है। हम उनके जवाब को अविकल प्रकाशित कर रहे हैं। आलोचना इस बहस में आए सभी उत्तरों, प्रत्युत्तरों, प्रति-प्रत्युत्तरों को जगह देने के लिए कृतसंकल्प है, बशर्ते उनमें आवश्यक शालीनता का अतिक्रमण न हुआ हो।
_ _ _ _
आलोचना अंक-78 (जुलाई-सितम्बर 2024) में प्रकाशित डॉ. चारु सिंह के लेख ‘अभिलेख, आलोचना, इतिहास और हरदेवी का जीवन’ में मेरे एक लेख ‘Hardevi : A Forgotten Heroine of Nineteenth Century’ पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं:
अगर प्रोफ़ेसर सिन्हा के इस लेख को एक शोध के रूप में देखें तो इसके दो दावे हैं:
- “इसकी भाषा शैली और पद्धति दर्शाती है कि यह हरदेवी को अकादमिक जगत में पहली बार प्रस्तुत कर रहा है और प्राथमिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए उन्नीसवीं सदी के एक महत्वपूर्ण लेकिन इतिहास में उपेक्षित व्यक्तित्व के रूप में हरदेवी के जीवन की पहली बार पुनर्रचना कर रहा है।”
- “सीमंतनी उपदेश और स्त्री विलाप की अज्ञात रचनाकार के रूप में हरदेवी की पहचान कर रहा है” और फिर आगे उन्होंने लिखा कि “फॉरगॉटन हीरोइन लेख के उपरोक्त दोनों ही दावे निराधार हैं। यह दोनों काम हरदेवी संबंधी मेरे उपरोक्त शोधालेख और मेरा पीएच. डी. शोध प्रबंध (जिसके परीक्षक खुद प्रोफ़ेसर सिन्हा ही थे) कई वर्ष पहले कर चुके थे। एक लेख के रूप में ‘फॉरगॉटन हीरोइन’ का ढाँचा, सूचनाएँ, बहुत से निष्कर्ष, प्रस्तुतीकरण और यहाँ तक कि इसका शीर्षक हूबहू ‘अज्ञात हिन्दू स्त्री कैसे बनती है?’ का अंगरेजी अनुवाद है।” (आलोचना अंक-78, पृष्ठ 55-56)
पहली बात तो यह है कि दुनिया के किस व्याकरण के अनुसार ‘अज्ञात हिन्दू स्त्री कैसे बनती है?’ का अंगरेजी अनुवाद ‘फॉरगॉटन हीरोइन ऑफ़ नाइनटीन्थ सेंचुरी’ ठहराया जा सकता है, मैं नहीं जानता। मैं तो यह भी नहीं जानता कि डॉ. चारु सिंह अनुवाद के अलावा स्टाइलिस्टक्स और लिंग्विस्टिक्स की भी ज्ञाता हैं और वे इस क्षेत्र में इतनी सिद्धस्त हो चुकी हैं कि किसी अंगरेजी लेख की तुलना किसी हिन्दी लेख की भाषा शैली और पद्धति की विवेचना किए बगैर, मैं यहाँ लेख की अंतर्वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, इस निष्कर्ष पर पहुँच सकती हैं?
मैं यह भी नहीं जानता कि जब मेरा यह लेख तद्भव–47 (जुलाई-2023, पृष्ठ 257-280) में पहले से ही हिन्दी में प्रकाशित है फिर इस अंगरेजी लेख को आधार बनाने का क्या औचित्य हो सकता है? मैं ऐसा भी नहीं मान सकता कि तद्भव ऐसी पत्रिका है जो अल्पख्यात है और जिसे लोग न जानते हों। आखिर माजरा क्या है? पूरा लेख पढने पर पता चलता है कि यह मेरे चरित्र हनन की उनकी परियोजना की रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है—हिन्दी भाषी पाठक के सामने झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में इससे बड़ी सहूलियत मिल जाती है, भाषा जितना कहती है उससे अधिक छुपाने का साधन भी बन जाती है लेकिन हिन्दी के पाठक जिन्होंने मेरे इस लेख को पढ़ा होगा, डॉ.चारु सिंह के इस बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोप को तुरन्त भाप लेंगे, यही नहीं उनके और भी जितने आरोप हैं उसका प्रत्याख्यान स्वयं मेरा वह लेख कर रहा है, मुझे कुछ अतिरिक्त कहने की जरूरत भी नहीं है।
जहाँ तक दूसरे दावे का सवाल है तो मैं अपने पाठकों से कहना चाहता हूँ कि मेरा यह दावा सही है कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी हैं, यह सबसे पहले मैंने ही अकाट्य प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया। इससे पहले सिर्फ़ अनुमान और कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि सीमतंनी उपदेश पर बतौर लेखिका ‘एक अज्ञात हिंदू औरत’ छपा हुआ था।
मैं कई वर्षों से प्रारंभिक दौर के रचनाकारों पर शोध करता रहा हूँ, इसी की एक कड़ी के रूप में गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में 27 दिसंबर, 2022 को भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुमनाम महिला स्वतंत्रता सेनानियों के उत्सव में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में पहली बार मैंने एक प्रामाणिक दस्तावेज़ के आधार पर यह प्रमाणित किया था कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी हैं।
यहाँ डॉक्टर धर्मवीर या चारू सिंह की तरह कयास नहीं लगाया गया था बल्कि एक दस्तावेज़ के आधार पर यह स्थापना की थी। वह दस्तावेज़ था—द इंडियन मैगजीन के जुलाई 1889 के अंक में हरदेवी की पुस्तक ‘तालीम-ए-तीफ्लां (किंडरगार्टन): बाल शिक्षा या शिक्षण का खजाना’ नामक पुस्तक की एक समीक्षा जिसमें समीक्षक लिखता है—
“तालीम-ए-तीफ्लां (किंडरगार्टन): बाल शिक्षा या शिक्षण का खजाना; श्रीमती हरदेवी, सुपुत्री राय बहादुर कन्हैया लाल, ओरिएंटल प्रेस, लाहौर, 1889 : इस पुस्तक की लेखिका भारत में स्त्री शिक्षा के प्रति अपने गहन सरोकारों को बेबाकी से रखने के लिए दृढसंकल्प जान पड़ती है। इनकी पूर्व लिखित पुस्तकें—‘सीमंतनी संगीत’, ‘विधवा अश्रु’, ‘सीमंतनी उपदेश’, ‘लंदन जुबली’ और ‘लंदन यात्रा’ सुचिंतित पुस्तकें हैं जो भारतीय स्त्रियों को जगाने और जागरूक बनाने के उदेश्य से लिखी गई हैं।” (द इंडियन मैगजीन, जुलाई 1889, पृष्ठ 316)
इसके पहले इस दस्तावेज को किसी ने न देखा था और न सुना था। इस तथ्य को हिन्दी समाज ने पहचाना और प्रखर आलोचक रवि भूषण ने समालोचन पर ‘लेखन और दृष्टि का स्त्री अध्याय’ नामक लेख में रेखांकित किया:
“डॉ. धर्मवीर ने सीमतंनी उपदेश की खोज की और उसकी लेखिका ‘एक अज्ञात हिन्दू औरत’ को माना। सीमंतनी उपदेश (1883) के पहले स्त्री-विलाप (1881) की लेखिका भी ‘एक विधवा स्त्री’ ही थी। उनके नाम की किसी को जानकारी नहीं थी। गंभीर अध्येता और हिन्दी आलोचक रमण सिन्हा ने पहली बार दुर्लभ दस्तावेजों के आधार पर गोविन्द वल्लभ पंत संस्थान द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी (27-28 दिसम्बर, 2022) में यह प्रमाणित किया कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी ही हैं। उन्होंने उनके द्वारा रचित ‘सीमंतनी संगीत’ का भी उल्लेख किया है, जो अनुपलब्ध है। हरदेवी रचनावली रमण सिन्हा ने सम्पादित कर ली है, जो शीघ्र प्रकाश्य है।”
इसी प्रकार हरदेवी की यात्रा (2023) पुस्तक को संपादित करते हुए प्रोफ़ेसर गरिमा श्रीवास्तव ने पुस्तक की भूमिका में दर्ज किया:
“हाल ही में गोविन्दवल्लभ पन्त सामाजिक संस्थान में प्रोफ़ेसर रमण सिन्हा ने भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक दुर्लभ दस्तावेज़ का हवाला देते हुए बताया कि हरदेवी ही सीमंतनी उपदेश की रचनाकार हैं। इस दस्तावेज़ के मिल जाने से यह पुष्ट हो गया कि सीमंतनी उपदेश की ‘एक अज्ञात हिन्दू औरत’ दरअसल श्रीमती हरदेवी ही थी।”
लेकिन चारु सिंह के लेख का यह अंश देखिए:
“हरदेवी सीमंतनी उपदेश की लेखिका हैं, 2016 के मेरे शोध के इस निष्कर्ष को एक नए प्रमाण से पुष्ट करने के लिए उन्होंने इंडियन मैगजीन में प्रकाशित सूचना को उद्धृत किया जिसमें साफ़ लिखा हुआ था कि हरदेवी ही इस किताब की लेखिका हैं। यह एक ज़रूरी उदाहरण था और इस पत्रिका की सूचना मेरे पिछले लेख में भी दी गयी थी। संभवत: हिन्दी की दुनिया में पहली बार कोई इंडियन मैगज़ीन की बात कर रहा था। 2016 के हरदेवी की जीवनी संबंधी लेख तक यह अंक मैं देख न सकी थी और इतनी ख़ास सूचना मुझसे छूट गयी। यह मिल जाती तो छह-सात पन्नों के तर्कों की वह शृंखला जिनके सहारे मैं हरदेवी को सीमंतनी उपदेश की लेखिका सिद्ध कर रही थी, वह काम एक पैराग्राफ में उद्धरण देकर हो जाता।” (आलोचना अंक-78, पृष्ठ 56)
इनकी यह तर्क-प्रणाली उस दृष्टांत-कथा की याद दिलाता है जिसमें एक गोताखोर सागर के उस रत्न पर दावा ठोंकता है जिस सागर में वह कभी नहीं उतरा था लेकिन अपने दावे में वह कहता है कि कम से कम सागर का नाम तो वह जानता है! क्या चारु सिंह को शोध निष्कर्ष और शोध-प्रस्ताव का भेद भी नहीं मालूम है! अनुमान और प्रमाण को एक मानते हुए 2016 के अपने जिस लेख का वह हवाला दे रही हैं उसमें प्रस्ताव है, अनुमान है, तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित कोई निष्कर्ष नहीं है। आगे की पंक्ति दिलचस्प है। वह लिखती हैं—
“2016 के मेरे शोध के इस निष्कर्ष को एक नए प्रमाण से पुष्ट करने के लिए उन्होंने इंडियन मैगज़ीन में प्रकाशित सूचना को उद्धृत किया जिसमें साफ़ लिखा हुआ था कि हरदेवी ही इस किताब की लेखिका हैं।”
अब बताइए, अगर शोध से निष्कर्ष निकल ही चुका है तो फिर नए प्रमाण की जरूरत कहाँ रही और फिर नए प्रमाण का क्या मतलब, किसी ने कोई पुराना प्रमाण भी दिया था क्या? और जब आपको यह मालूम ही था कि सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी हैं तो अनुमान किस चीज़ की लगा रही थीं और फिर यह अफ़सोस क्यों जाहिर कर रही थीं कि “2016 के हरदेवी की जीवनी संबंधी लेख तक यह अंक मैं देख न सकी थी और इतनी ख़ास सूचना मुझसे छूट गयी। यह मिल जाती तो छह-सात पन्नों के तर्कों की वह श्रृंखला जिनके सहारे मैं हरदेवी को सीमंतनी उपदेश की लेखिका सिद्ध कर रही थी, वह काम एक पैराग्राफ़ में उद्धरण देकर हो जाता।” इसे कहते हैं शब्दों की आड़ में छिपने की कोशिश करना लेकिन झूठ ऐसा कि लाख चाहने पर भी सत्य के सामने अपने को बेनकाब होने से न रोक पाना! इसे आलोचना नहीं कहते हैं, और यह पोलेमिक्स भी नहीं है, यह वकालत है—और खराब किस्म की वकालत है—जिसमें सच और झूठ का कोई अर्थ नहीं होता, मुकदमा जीत लेना ही जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है।
मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सभी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, शोध गंगा पर उनका और अन्य शोधार्थियों का शोध प्रबंध भी शायद होगा (और अगर न हो तो रखवा देना चाहिए), इंटरनेट पर हरदेवी पर उनके लेख और मेरे अंगरेजी और हिन्दी के लेख तो हैं ही, पाठक स्वयं तय करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या लेकिन मैं डॉ. चारु सिंह से यह अनुरोध जरूर करूँगा कि मुझ पर प्लेजरिज्म और फेब्रिकेशन का आरोप लगाने के पहले उनको पाठकों को यह अवश्य बताना चाहिए कि निम्नलिखित बातें जो मेरे लेख में हैं, उसके पहले उनके या किसी और शोधार्थी के किस लेख या किस शोध प्रबंध में हैं:
- अनुमान के बजाय प्रमाण के आधार पर सीमंतनी उपदेश की लेखिका हरदेवी हैं।
- महान सुधारक गोपाल गणेश अगरकर (1856-1895) के हवाले से एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में हरदेवी का उल्लेख।
- महात्मा गांधी द्वारा हरदेवी का उल्लेख।
- प्रथम स्त्री इतिहासकार मानी जाने वाली बन्दारू अच्चामम्बा (1874-1904) के उल्लेखनीय भारतीय स्त्रियों की जीवन-माला अबला सच्चरित्र रत्नमाला (1901) में हरदेवी का उल्लेख।
- सच्चिदानंद सिन्हा के ‘रिकलेक्शन एंड रिमिन्सेस ऑफ़ अ लॉन्ग लाइफ़’ और सच्चिदानंद सिन्हा कॉम्मेमोरेशन वोल्यूम के हवाले से सच्चिदानंद सिन्हा, राधिका देवी और हरदेवी का प्रसंग।
- निहाल सिंह के हवाले से रोशनलाल और हरदेवी का प्रेम-प्रसंग।
- सक्सेना रोशनलाल और भटनागर हरदेवी से सम्बंधित अंतरजातीय विवाद।
- खुशवक्त राय के हवाले से हरदेवी के लन्दन स्वागत का आँखों देखा हाल।
- कवि रूप में हरदेवी की पहचान।
- बिपिन चन्द्र पॉल के हवाले से पिता और भाई के साथ हरदेवी का सम्बन्ध।
- सीमतंनी संगीत की लेखिका के रूप में हरदेवी का उल्लेख।
- हरदेवी की मृत्यु वर्ष 1826 है यह तय होना।
यह सूची और भी लम्बी हो सकती है जिसे मैं अपने पाठकों पर छोड़ता हूँ। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि किसी विषय पर किसी का स्वत्वाधिकार नहीं होता—एक ही विषय पर हजारों शोध होते हैं, होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे और यह भी सच है कि विषय जितना अचर्चित होगा उससे सम्बंधित सामग्री भी उसी अनुपात में सीमित होगी; ऐसे में अचर्चित विषय पर शोध कर रहे व्यक्तियों की शोध-सामग्री के एक-समान होने की संभावना बढ़ जाती है; उन्हीं स्रोतों पर सभी शोधार्थियों को लौटना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कोई यह दावा नहीं कर सकता कि चूंकि इस स्रोत का पहले मैंने उपयोग किया इसलिए इस पर मेरा एकाधिकार है अगर कोई दूसरा उसका उपयोग करता है, भले ही उसको उस स्रोत की जानकारी जिससे मिली हो, उसका वह उल्लेख न करे (यह भी संभव है कि उसे उस सामग्री की जानकारी किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई हो), यह प्लेजरिज्म नहीं है।
चारु सिंह के दो लेखों के बाद मेरा लेख छपा; यह संभव है कि इन तीनों की स्रोत सामग्री काफ़ी मिलती-जुलती हो उसी प्रकार उनके इस तीसरे लेख की स्रोत सामग्री में जो बढ़ोतरी हुई है उसका अधिकाँश हिस्सा पहले-पहल मेरे लेख में उल्लिखित है लेकिन इस आधार पर डॉ. चारु सिंह पर प्लेजिरिज्म का आरोप नहीं लग जाता।
अब उन आरोपों की चर्चा करूँगा जो मुकदमा जीत लेने के उदेश्य से एक सुचिंतित योजना के तहत मुझ पर लगाए गए हैं, यहाँ मैं उन प्रसंगों को नहीं उठाउँगा जिसका सम्बन्ध व्याख्या से है, क्योंकि मैं यह मानकर चलता हूँ कि तथ्य तो पवित्र होते हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए लेकिन उस तथ्य की अनेक प्रकार की व्याख्याएँ संभव हैं, यह हम सब जानते हैं । यह तो संभव है कि आप किसी तथ्य के सहारे किसी निष्कर्ष तक पहुँचे और दूसरा उसी तथ्य से किसी दूसरे निष्कर्ष की और बढ़े; लेकिन आप अपने निष्कर्ष के अनुसार तथ्य को तोड़ने मरोड़ने का काम करें, यह गलत है और इससे भी अधिक गलत बात यह है कि स्वयं ऐसा करते हुए अपने प्रतिपक्ष पर ठीक यही आरोप मढ़ दें। एक जगह पर डॉ. चारु सिंह लिखती हैं—
“प्रोफ़ेसर सिन्हा हरदेवी के बारे में अपनी स्थापना देते हैं : उनके (हरदेवी के) जीवन और लेखन में किसी भी प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद-विरोधी दृष्टिकोण को खोजना कठिन है (It’s difficult to find any direct anti-colonial stance in her life and letters)। हरदेवी के लेखन में अंगरेजी शासन या उपनिवेशवाद का कोई विरोध खोजने में उन्हें हो रही कठिनाई का कारण यह है कि प्रोफ़ेसर सिन्हा ने हरदेवी का लिखा (या कहें कि प्राथमिक स्रोत) बस उतना ही पढ़ा है जितना वह आलोचना में प्रकाशित मेरे लेखों में उद्धरणों की सूरत में मौजूद था।” (आलोचना अंक-78, पृष्ठ 64-65)
इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी पर तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा लेकिन मेरे जिस उद्धरण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है, उस पर मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने लिखा था—
“भारत, विशेषकर लाहौर के सार्वजनिक जीवन में हरदेवी की सक्रियता ताउम्र रही। राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक मुद्दों को ज्यादा अहमियत देने के कारण उनमें स्पष्टत: औपनिवेशिकता विरोधी चेतना की अभिव्यंजना का अभाव है, बल्कि कहीं-कहीं ब्रिटिश शासन व रानी विक्टोरिया का गुण-गान ही है लेकिन ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि हरदेवी क्रांतिकारियों की सहायता करती थीं। यही नहीं बल्कि आपराधिक खुफ़िया विभाग के एक रिपोर्ट में गैब स्त्रियों के पंजाब में अति सक्रिय होने की बात कही गयी थी तो उसमें सरला देवी और हरदेवी का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय बताया गया था।” (तद्भव-47, पृष्ठ 265)
चूंकि उन्होंने अंगरेजी लेख का उद्धरण दिया है इसलिए वह उद्धरण भी फुटनोट में दे रहा हूँ।*
इस लेख को पढ़ते ही आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि पाठक का सामना किसी ऐसे चतुर-सुजान वकील की कार्यशैली से हो रहा है जिसे तथ्य को तोड़ने मरोड़ने, क्षत-विक्षत करने में रत्ती भर गुरेज नहीं है; इसके बावजूद वह जिस बात को सिद्ध करना चाहता है, वह नहीं कर पाता कि आखिर उसके उद्धरण और उनके निष्कर्ष में क्या सम्बन्ध है? पूरे लेख में इसी शैली को अपनाया गया है जिसमें निष्कर्ष पहले निकाल लिया जाता है फिर उदाहरण को फिट करने की कवायद शुरू की जाती है; अगर वह मनमाफ़िक नहीं उतरा तो उसका अंग-भंग निश्चित है। क्या यह किसी परियोजना के तहत किया जा रहा है? आइए इस शैली के एक और नमूने का जायका लें, वह लिखती हैं—
“फॉरगॉटन हीरोइन लेख में हरदेवी संबंधी सूचनाओं को करीब पंद्रह पन्नों में समेटते हुए किस तरह उनका एक जीवन रचा गया हैं और इसमें यह कितना सफल रहा है या विफल, उसकी सीमाएँ क्या हैं इसे आगे देखते हैं। कई बार लगता है कि यह सीमाएँ एक पूर्व-प्रकाशित लेख का ढाँचा हूँ-ब-हू इस्तेमाल करने के कारण भी हैं और इस ढाँचे में तमाम अंतर्विरोधी सूचनाओं और व्याख्याओं को बिना किसी सैद्धांतिक फ्रेम के इस तरह एक-दूसरे के साथ जोड़कर इस्तेमाल करने से भी। इस पद्धति का परिणाम है कि पूरा लेख आधी दूरी तक एक कहानी को कहता है और फिर उसी कहानी को एकदम विपरीत सूचनाओं से काटकर ध्वस्त कर देता है।”
इसका पहला उदाहरण सेवाराम का प्रसंग है। फॉरगॉटन हीरोइन कन्हैयालाल की मृत्यु पर अखबार में छपी सूचना का संकलन करते हुए यह बताता है कि कैसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर हरदेवी और उनके भाई सेवाराम को भारत लौटना पड़ा। इसके बाद यह लेख बिपिन चन्द्र पाल के संस्मरण में मौजूद एक दूसरी सूचना का जिक्र भी ‘तथ्य’ की तरह करता है और इसके सहारे यह स्थापना देता है कि देश लौटकर जब हरदेवी और रोशनलाल की शादी हुई, तो वह शादी दरअसल हरदेवी के भाई सेवाराम ने कराई थी जिसके लिए पिता और पुत्र के संबंधों में कड़वाहट आ गयी। यह दोनों बातें फॉरगॉटन हीरोइन को कैसे एक साथ संभव लगती है, समझना मुश्किल है। (आलोचना अंक-78, पृष्ठ 58) अब बताइए यह समझना कैसे मुश्किल है? पिता से मनमुटाव होने के बावजूद, क्या आज भी कोई चाहे कितनी भी नाराज़ क्यों न हो, मृत्यु की ख़बर सुनकर नहीं आती है और वह तो ज़माना संयुक्त परिवार और निकट सामुदायिक जीवन का था? यहाँ भी वही दिक्कत है स्थापना कुछ, उदाहरण कुछ, निष्कर्ष कुछ!
मेरे लेख की शोध पद्धति और निष्कर्षों को जिन पाँच उदाहरणों से विश्लेषण करने की घोषणा डॉ. चारु सिंह करती हैं उसमें पहले और अंतिम की पद्धति हमलोग देख चुके हैं; बीच के तीन उदाहरण भी इसी किस्म के हैं। उनका दूसरा उदाहरण मेरे लेख में निहाल सिंह के लेख के इस्तेमाल को लेकर है, वह कहती हैं—
“प्रोफ़ेसर सिन्हा ने जब अपने लेख ‘फॉरगॉटन हीरोइन’ में निहाल सिंह के लेख से सूचनाएँ उद्धृत कीं तब तलवार जी के इतिहास बोध से उलट राह चुनी और ‘This is fact that’ (यह एक तथ्य है कि…) पदबंध का उपयोग करते हुए उसकी सूचनाओं को अपने लेख में पिरोते गए। यह भी न सोचा कि निहाल सिंह तब जन्मे भी नहीं थे, जब का वे किस्सा लिख रहे थे। ध्यान रहे कि वे इतिहासकार भी नहीं थे, राजनीतिक रूप से सक्रिय एक लेखक और पत्रकार थे।” (आलोचना अंक-78, पृष्ठ 59)
अगर तर्क की यह पद्धति स्वीकार कर लें तो हरदेवी पर डॉ. चारु सिंह के काम को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे भी हरदेवी की समकालीन तो हैं नहीं, वे इतिहासकार भी नहीं हैं और तो और वे राजनीतिक रूप से सक्रिय एक लेखक और पत्रकार भी नहीं हैं!
‘इतिहासकार को सिर्फ़ समकालीन इतिहास ही लिखना चाहिए’, थूकिदीदिस (c. 460 – c. 400 ई.पू.) की यह मान्यता असंगत होने की हद तक बहुत पुरानी पड़ चुकी है, यह हम सब जानते हैं। चौथा उदाहरण तो अकादमिक अनैतिकता और अशालीनता की सारी हदें लाँघ गया है, डॉ. चारु सिंह लिखती हैं—
“यह चौथा उदाहरण एक शोध के रूप में ‘फॉरगॉटन हीरोइन’ की हरदेवी के जीवन और उन्नीसवीं सदी के हिन्दी लोकवृत्त संबंधी सतही समझ को दर्शाता है। जिसका कारण ‘फॉरगॉटन हीरोइन’ द्वारा हर उस सूचना को जो उसे इंटरनेट पर, या दूसरे शोधार्थियों के यहाँ मिली जल्दबाजी में अपने लेख में में भरते चले जाना है—यह देखे बिना कि कहीं वह अपनी ही कही बातों को काट तो नहीं रही है। यह प्रसंग डॉ. धर्मवीर के निष्कर्षों के साथ मेरे उपरोक्त शोध की स्थापनाओं को मिलाने से पैदा हुई अंतर्विरोधी व्याख्या का है जिसे लेख में ‘धर्मवीर–सिंह विवाद’ कहा गया है। ‘फॉरगॉटन हीरोइन’ की कल्पना ने यह तीसरा तथ्य रचा है। यहाँ कहना आवश्यक है कि डॉ. धर्मवीर वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2014 की फरवरी में सीमंतनी उपदेश संबंधी लेख प्रकाशित होते ही फ़ोन करके बात की थी और मेरा मनोबल बढ़ाया था। यह न भी होता तो भी अपने शोध से वे आदरणीय हैं। अपने से पहले के किसी शोधार्थी के निष्कर्षों को गलत पाना और अपने शोध में उसका उल्लेख कर देना विवाद नहीं संवाद कहलाता है। यह संवाद आप तब तक नहीं करते जब आप बिना सन्दर्भ दिए पिछले शोध के निष्कर्षों का अपने नाम से इस्तेमाल करने की नीयत रखते हैं।” (आलोचना अंक-78, पृष्ठ 63)
पीएच. डी. शोध प्रबंध के परीक्षक होने की बात लिखकर उन्होंने जो पहले संकेत किया था, उसका यहाँ खुलासा कर दिया गया गया है; डॉ. चारु सिंह की किस कल्पना ने और किस नीयत से ‘धर्मवीर–सिंह विवाद’ रचा है, वह भी स्पष्ट हो जाता है, मेरे दोनों लेख शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाइए कहीं आपको ‘धर्मवीर–सिंह विवाद’ नहीं मिलेगा और जो मिलेगा वह यह अंश है—What could be the reason for hiding her name? There is a long debate around this question in Hindi literary world. (Dharmaveer 1999:38-40; Singh 2016:15-44)
स्त्री विलाप और सीमंतनी उपदेश में हरदेवी ने अपना नाम क्यों नहीं दिया, इस प्रश्न पर विचार करते हुए मैंने लिखा कि इस प्रश्न पर हिन्दी की साहित्यिक दुनिया में विवाद रहा है और इससे परिचित होने के लिए कोष्ठक में शिकागो शैली में डॉ. धर्मवीर और चारु सिंह की पुस्तक का हवाला दिया है—क्या यह ‘धर्मवीर–सिंह विवाद’ है? पहले तो मैंने चारू सिंह की अंगरेजी भाषा की जानकारी की सीमा समझा लेकिन पूरे लेख या इस अंश के तेवर और तंज को देखते हुए यह समझने में देर नहीं हुई कि यह महज मेरे चरित्र-हनन की कुत्सित परियोजना का एक हिस्सा है।
किसी के बारे में आप की धारणा तो हो सकती है लेकिन क्या बिना किसी प्रमाण के किसी पर प्लेजरिज्म (साहित्यिक चोरी) का आरोप लगा सकते हैं? मैं डॉ. चारु सिंह से यह निवेदन करता हूँ कि या तो वे प्रमाण दें या अपने शब्द वापस लें नहीं तो मानहानि के लिए क़ानून का दरवाजा खटखटाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस तरह के बेबुनियाद आरोप और फ्रॉड मेरी बर्दाश्त की सीमा से बाहर है।
प्रसंगवश यहाँ थोड़ा ठहरकर पत्रिका के सम्पादक की भूमिका पर भी विचार करने की गुजारिश करता हूँ। सम्पादक को यह तो अधिकार है कि वह अपनी पत्रिका में क्या छापे और क्या न छापे, उसे पक्ष भी चुनने का अधिकार है लेकिन क्या उसे यह अधिकार है कि जब वह पक्ष चुन रहा है तब प्रतिपक्ष को बगैर सुने, बगैर पढ़े, बिना जाने अपने सम्पादकीय में एक पक्ष विशेष के लेख की संस्तुति करे?
आलोचना के सम्पादक श्री संजीव कुमार, डॉ. चारू सिंह के लेख और उनके मतों को ब्रह्मवाक्य मानकर उद्धृत करते हैं और सम्पादकीय में लिखते हैं—
“1882 ई. में छपी ‘एक अज्ञात हिन्दू औरत’ की पुस्तक सीमंतनी उपदेश से हिन्दी की समकालीन दुनिया का परिचय डॉ. धर्मवीर ने कराया जिनके सम्पादन में मूल संस्करण के आधार पर इसका दूसरा संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ था। इस क्रांतिकारी पाठ को हाथों-हाथ लिया गया, लेकिन वह अज्ञात हिन्दू औरत हिन्दी की दुनिया में शोधार्थी चारु सिंह के लेख ‘अज्ञात हिन्दू स्त्री कैसे बनती है? (आलोचना, अप्रेल-जून 2016) के प्रकाशन से पहले प्राय: अज्ञात ही रही। कुछ साधार और कुछ निराधार अनुमान लगाने के प्रयास चलते रहे। मसलन, स्वयं डॉ. धर्मवीर ने दो अलग-अलग तरह के अनुमान लगाए, पर उनके पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाए। वीर भारत तलवार रस्साकशी में यहाँ तक तो आते हैं कि लाहौर की कई ख़ूबसूरत इमारतों के वास्तुकार कन्हैया लाल की बाल-विधवा बेटी हरदेई, जिसने ‘इंग्लैण्ड में पढ़ने आए इलाहाबाद-लखनऊ के भावी बैरिस्टर रोशनलाल से प्रेम-विवाह किया था और विवाह के बाद अज्ञात हिन्दू औरत होने की वैचारिक दृष्टि से प्रबल संभावना है, लेकिन यह मानकर इस अनुमान को आगे नहीं ले जाते कि 1882 में ऐसी किताब लिखने के लिहाज से हरदेई की उम्र बहुत कम रही होगी’। अंतत: अपने शोध के आधार पर चारु सिंह को ही ‘अज्ञात हिन्दू औरत’ की हरदेवी के रूप में पहचान करने और उनके बौद्धिक एवं सामाजिक कार्यों को व्यवस्थित रूप में आलेखबद्ध करने का श्रेय जाता है।” (आलोचना अंक-78, पृष्ठ VIII-IX)
कमाल है कि इस सम्पादकीय में उन लोगों का जिक्र तो किया गया है जिन्होंने अनुमान किया, कयास लगाए पर ‘जो सबूत नहीं दे पाए’, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं जिसने सबूत पेश किया और जिसका स्वागत व्यापक हिन्दी समाज ने किया, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? या तो उन्होंने मेरा लेख—अंगरेजी या हिन्दी, किसी भाषा में—नहीं पढ़ा या पढ़कर भी अनदेखी करने की कोशिश की**, दोनों ही स्थितियों में पाठक उनसे आज नहीं तो कल जरूर पूछेंगे कि क्या सम्पादक का यही धर्म होता है?
_ _ _ _
* Hardevi’s activism in the public sphere was lifelong. Since she was more inclined to social issues than political, it is difficult to find any direct anti-colonial stance in her life and letters—rather at some places there is admiration for British rule and Queen Victoria, but there is also evidence when “She arranged meetings and collected funds for the purpose of assisting anarchists under trial”. (Kaur 1968:98) and the Criminal Intelligence Department, reported in 1908 about women’s ‘increasing interests in politics’ when “Sarla Devi and Hardevi were the most prominent women leaders of this time. They organized secret associations, collected funds for revolutionary under trial prisoners and arranged meetings to inculcate the national spirit amongst the women and youth of the region” (Singh 1989:248). 1889:167). (Link to article)
** यहाँ यह याद दिलाना जरूरी है कि जिस तद्भव-47 (जुलाई 2023) में मेरा लेख—’हरदेवी : उन्नीसवीं सदी की एक विस्मृत नायिका’ प्रकाशित हुआ था, उसी में आलोचना सम्पादक संजीव कुमार का भी एक लेख छपा था!