आलोचना पत्रिका का एक विज्ञापन जून 2025 में आता है जिसमें एक शोध आलेख की चर्चा है। अंक-78 में 50 पन्ने का लेख है, ऐसी सूचना पाठकों को दी जाती है। लेख आलोचना पत्रिका के ऑनलाइन ब्लॉग पर भी प्रकाशित होता है, जिसका शीर्षक है—‘वादे वादे जायते तत्वबोध:— शोध और लेखन के एक नए विषय के रूप में हरदेवी’। इस पर टिप्पणी करते हुए सम्पादक ने लिखा है—“चारू सिंह ने आलोचना अंक-78 में प्रकाशित अपने लंबे शोध आलेख के इस हिस्से में हरदेवी संबंधी अपने काम को बिना श्रेय दिये हथियाए जाने के जो विवरण दिए हैं, उनपर हिन्दी संसार को तत्काल ग़ौर करने की ज़रूरत है।” (आलोचना ऑनलाइन, 8 जुलाई 2025)
सम्पादकीय टिप्पणी से स्पष्ट है कि शिवदान सिंह चौहान, नंददुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह जैसे महान साहित्यकार-सम्पादकों की सम्पादकीय मर्यादा की धज्जियाँ उड़ाते हुए कैसे वर्तमान सम्पादक ने सत्य का दूसरा पहलू जाने-समझे बगैर अपना दुराग्रहपूर्ण फैसला सुना दिया है। यह जीवन के हर क्षेत्र में हुए पतन की तरह ही सम्पादकीय मर्यादा के पतन की इंतिहा का नमूना है। संभव है कि खुद को सम्पादकाचार्य समझने का भ्रम पाले सज्जन द्वारा इस तल्ख़ सच्चाई को उजागर करनेवाली मेरी टिप्पणी को भी ‘सम्पादित’ कर दिया जाए। इसलिए हिन्दी के प्रबुद्ध पाठकों के सूचनार्थ हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं।
इस कथित शोध-आलेख में हरदेवी विषयक मेरे आलेख पर निम्नलिखित आधारविहीन आरोप लगाए गए हैं:
- इसमें मूल शोध का सन्दर्भ देने की अकादमिक नैतिकता और शिष्टाचार को पूरी तरह तिलांजलि दे दी गई है।
- यह वास्तव में हरदेवी की कुछ किताबों का पुनर्प्रकाशन है जिसमें उपरोक्त शोधों से प्राप्त निष्कर्षों को दोहराते हुए पाठकों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है कि यह भूमिका या आलेख ही हरदेवी को पहली बार सामने रख रहा है।
- वास्तव में यह किताब हरदेवी संबंधी शोध में कोई भी योगदान देने में सक्षम नहीं है अतः इसे शोध कहना उचित नहीं होगा।
- इस किताब में सीमन्तनी उपदेश की लेखिका के रूप में प्रमाणित करने का श्रेय जिनको दिया गया है, वह ग़लत है।
आरोपों के उत्तर :
1. यह मानी हुई बात है कि जब शोध के प्राथमिक स्रोत उपलब्ध होते हैं तब द्वितीयक स्रोत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्रोत सामग्री पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, एक ही स्रोत के आधार पर कई व्याख्याएँ हो सकती हैं, होती हैं। हरदेवी के बारे में जो तथ्य उपलब्ध हैं (मसलन, उनके पिता का नाम रायबहादुर कन्हैयालाल था आदि), वे पब्लिक डोमेन में न जाने कब से उपलब्ध है। अब इस तरह के जीवनीपरक तथ्यों के लिए किसी को श्रेय देने की बात कहाँ से आ जाती है? यह बचकानी बात है। आगरे में ताजमहल है, क्या इसे कहने के लिए भी किसी को श्रेय देना होगा?
2. मेरे द्वारा सम्पादित ‘हरदेवी की यात्रा’ (सेतु प्रकाशन, दिल्ली) के अंतिम पैराग्राफ़ में कहा गया है—“प्रस्तुत पुस्तक श्रीमती हरदेवी के यात्रा वृत्तांत के संकलन और पुनर्प्रस्तुतीकरण का प्रयास है, इस कार्य में जिन मित्रों और छात्रों का सहयोग मिला उसके लिए मैं आभारी हूँ”—इस कथन से यह कहीं भी स्थापित करने की कोशिश नहीं की जा रही कि हरदेवी पर मेरा कॉपीराइट या स्वत्वाधिकार है या पहली बार इनकी खोज मैंने की है। जब हम इंटेंशन की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि इस तरह के संकलन या सम्पादन की क्या आवश्यकता है? पुस्तक की भूमिका में इसका ज़िक्र इन शब्दों में है—“प्राक् आधुनिक और आधुनिक स्त्री रचनाकारों के बारे में तथ्य एकत्र करना, उनके लिखे हुए को प्रकाशित करना, इतिहास में स्त्री-रचना की अप्राप्य और उपेक्षित धारा की विलुप्त कड़ियों को जोड़ना … विशेषकर स्त्री रचनात्मकता के बहुत से पहलू अभी भी उपेक्षित और अनछुए ही रह गये हैं।” (हरदेवी की यात्रा, सेतु प्रकाशन, पृष्ठ 53)
इस दिशा में मैं पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही हूँ। इस क्रम में ‘नवजागरण और स्त्री शृंखला की पुस्तकें’, ‘वामा शिक्षक’ का पुनर्प्रकाशन, नवजागरणकालीन रचनाकारों के योगदान को सामने लाने के लिए लाला श्रीनिवासदास और किशोरीलाल गोस्वामी पर भी मैंने लिखा-पढ़ा है।
3. ‘हरदेवी की यात्रा’ पुस्तक की भूमिका और सम्पादन का उद्देश्य हरदेवी द्वारा लिखे गए दो यात्रा वृत्तांतों ‘लंदन यात्रा’ और ‘लंदन जुबली’ को विस्मृत और अल्पज्ञात टेक्स्ट के रूप में पहचान कर शोधार्थियों और पाठकों के सामने लाना था। इससे पहले मुझे या मेरे किसी छात्र या मित्र को ‘लंदन यात्रा’ या ‘लंदन जुबली’ की प्रति नहीं मिल सकी थी। ‘लंदन जुबली’ आरोपकर्ता के पास भी नहीं थी। (ऐसा उन्होंने ख़ुद लिखा है। पता नहीं फिर कैसे रचनावली पूरी होती?) मैंने सारी सामग्री लंदन की लाइब्रेरी से ली जिसके पर्याप्त प्रमाण मेरे पास हैं। आरोपकर्ता को तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि सेतु प्रकाशन से छपी पुस्तक में ‘लंदन जुबली’ पुनर्प्रकाशित हुई जिससे उनको सामग्री मिल गयी।
4. हरदेवी के बारे में रमण सिन्हा ने अपने लेख में लिखा कि हरदेवी के जीवन के बारे में हमें छिटपुट जानकारियाँ ही मिलती हैं। उन्होंने अपने संस्मरणों ‘लंदन यात्रा और ‘लंदन जुबली’ में भी बहुत कम बताया है… 1901 के एक दस्तावेज़ में उन्हें 42 वर्ष का बताया गया है। उनके लेख में फुटनोट संख्या 6 में ‘भारत भगिनी’ के सर्कुलेशन का ब्यौरा देते हुए ‘द पंजाब प्रेस’ में 1901 के एक नार्मन जेरल्ड बैरियर, पॉल वेल्स, अंक 14 ऑफ़ ओकेज़नल पेपर्स: साउथ एशिया सीरीज, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी एशियन स्टडीज सेंटर, प्रकाशक रिसर्च कमेटी ऑफ़ पंजाब, 1970 लिखा गया है: “प्रोपराइटर : श्रीमती हरदेवी, कायस्थ, एज 42, डॉटर ऑफ़ द लेट राय बहादुर कन्हैयालाल।” डॉ.सिन्हा ने जिन तथ्यों का हवाला दिया है उनमें एक भी सेकेंडरी सोर्स नहीं है। इसलिए उनके स्रोत को उद्धृत करना मुझे विवेकसम्मत प्रतीत हुआ।
हरदेवी से संबंधित चर्चा वीरभारत तलवार की ‘रस्साकशी’ के अध्याय ‘धर्म और समाज’ (प्रथम संस्करण, सारांश प्रकाशन, पृष्ठ 223-235) में विस्तार से हुई है। इसमें उन्होंने हरदेवी को ‘सीमंतनी उपदेश’ की लेखिका के रूप में पहचानने की बात की, लेकिन यह उनका अंदाज़ा था। इसके लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि डॉ. तलवार की दृष्टि में उनकी उम्र 1882 में इतनी कम थी कि वे ‘सीमंतनी उपदेश’ जैसी परिपक्व कृति लिख पातीं, इसमें सन्देह है। संभवत: तब तक उनके पास ठोस सन्दर्भ मौजूद नहीं थे। लेकिन रमण सिन्हा ने अपने लेख में फुटनोट संख्या 25 (द इण्डियन मैगज़ीन, जुलाई 1889, पृष्ठ15-44) के हवाले से लिखा कि इस दस्तावेज़ के मिल जाने के बाद सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रही कि इसकी लेखिका कौन थी।
जब यह तथ्य प्रस्तुत कर दिया गया तो मुझे किसी अन्य के ‘अनुमान’ की जगह डॉ. सिन्हा के ‘प्रमाण’ को श्रेय देना उचित लगा जो मैंने ‘हरदेवी की यात्रा’ में किया।
शोधकार्य एक सतत प्रक्रिया है। यदि स्रोतों पर ध्यान दिया जाये तो ‘सीमंतनी उपदेश’ की चर्चा अपनी भूमिका में डॉ. धर्मवीर ने पहली बार व्यवस्थित ढंग से की, उन्होंने ही सूसी थारू और के. ललिता के हवाले से लिखा कि इसकी लेखिका अज्ञात है, इसी भूमिका में 7 अगस्त, 1881 की सुबोध पत्रिका के हवाले से अज्ञात लेखिका के लेख के माध्यम से कायस्थ जाति के बारे में लिखते हुए वे दर्ज़ करते हैं कि—“हिंदुओं में चार मुख्य जातियाँ हैं और मैं कायस्थ जाति में पैदा हुई थी जो क्रम में हिंदुओं की तीसरी जाति है तथा अपनी विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार करने में बेहद कठोर है।” (सीमन्तनी उपदेश, भूमिका एवं सम्पादन डॉ. धर्मवीर) क्या इसी सूत्र से आरोपकर्ता के अतिरिक्त किसी और की खोज का प्रस्थान बिंदु यह भूमिका नहीं हो सकती।
सम्पादित पुस्तक की भूमिका पर बचकाना आरोप लगाया गया है कि इसमें कोई नई बात नहीं कही गई। यह आरोपकर्ता की निजी राय हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हिन्दी पाठकों को पहली बार उत्तर भारत के किसी स्त्री की विदेश यात्रा का विवरण पढ़ने को मिला। मेरे लेख में कोई बात या नई बात है कि नहीं, इसके विषय में सबके अपने विचार, आग्रह, पूर्वग्रह और दुराग्रह हो सकते हैं। लेकिन ऐसे विषयों पर भविष्य में शोध करने के लिए इच्छुक शोधार्थी ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं किसी निजी यश की लालसा की बजाय उन्हीं के लिए परिश्रम करती रही हूँ।
कालिदास ने ‘मैं’ शैली में ‘रघुवंश’ में यश-लिप्सा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो लिखा है उससे आरोपकर्ता को सबक लेना चाहिए:
मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्।
प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः॥
‘हरदेवी की यात्रा’ के अलावा ऐसा बहुत कुछ है जो मेरे अकादमिक परिश्रम का प्रमाण है। हरदेवी को शोधार्थियों के लिए सुलभ बना देने से अगर किसी को कोई कठनाई है तो सहानुभूति के अलावा उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती।
रमण सिन्हा के लेख में फुटनोट संख्या 36 में सच्चिदानंद सिन्हा के ‘कायस्थ समाचार’ के 1902 अप्रैल अंक का जिक्र है (पृष्ठ संख्या 436 से 437)। इसकी चर्चा ‘हरदेवी की यात्रा’ में भी है। ऐसे में जब प्राथमिक स्रोत उपलब्ध था तो यहाँ किसी और का सन्दर्भ देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, कभी भी स्रोत पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है। इसमें चारू सिंह के योगदान को या शोध को कम करके आँकना या अकादमिक साजिश देखना आरोपकर्ता का दृष्टिदोष है, क्योंकि ‘हरदेवी की यात्रा’ की भूमिका में पृष्ठ संख्या 15 पर ही डॉ. चारु सिंह का बड़ा उद्धरण दिया गया है जिसमें उनकी प्रशंसा करते हुए उनका योगदान स्वीकार किया गया है। दूसरे शब्दों में किसी के शोध को कमतर आँकने के उद्देश्य से ‘हरदेवी की यात्रा’ पुस्तक सम्पादित नहीं की गई। एक ही रचनाकार की कई रचनावलियाँ एकाधिक विद्वान सम्पादित करते रहे हैं। यदि डॉ. रमण सिन्हा या डॉ. चारु सिंह ‘हरदेवी रचनावली’ को प्रकाश में लाने के लिए कृतसंकल्प हैं तो यह शोध अध्येताओं और पाठकों के लिए स्वागतयोग्य कदम होगा।
इस पूरे प्रसंग में ‘आलोचना-78’ के सम्पादक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। ‘आलोचना’ में प्रकाशित सामग्री को ऑनलाइन लाकर अपने फेसबुक पेज पर साझा करना और फेसबुक पर जाली अकाउंट से अनर्गल प्रलाप करते हुए मानहानि करनेवाले और फेक आईडी के माध्यम से ट्रोलिंग करनेवाले की गैर-क़ानूनी हरकत को सम्पादक संजीव कुमार द्वारा अपनी फेसबुक वॉल पर लगातार दो-तीन दिनों तक अतिसक्रिय होने देना और अनाप शनाप अपलोड करने देना कहाँ तक न्यायोचित है?
गौरतलब है कि आलोचना-सम्पादक द्वारा इस प्रकरण को अपने फेसबुक पेज पर साझा करने से आलोचना पत्रिका में इस विषय पर हो सकने वाली संभावित स्वस्थ अकादमिक बहस की सारी गुंजाइश खत्म हो गयी और फेसबुक पर उन फेसबुक के नायक छुटभैयों को भी बिना जाने समझे टिप्पणी करके कीचड़ उछालने का मौक़ा मिल गया जिन्होंने ज़िन्दगी में कोई शोध-पत्र लिखने का कभी कष्ट नहीं उठाया है।
दिलचस्प है कि गौतम बुद्ध का चित्र लगाकर ग़ैरक़ानूनी तरीके से जाली फेसबुक अकाउंट खोलने और दो-तीन दिनों तक आलोचना-सम्पादक के फेसबुक पेज पर आरोप-प्रत्यारोप का ‘कूड़ा-कचरा’ अपलोड करके अकाउंट मिटा देने वाले वाले ‘रामबाबू सिन्हा’ का फेसबुक पर एक ही मित्र था, जिसका ख़ुलासा समय आने पर किया जाएगा। इसके सारे प्रमाण मौजूद हैं और इस गैर-क़ानूनी आपराधिक हरकत के डिजिटल फुटप्रिंट की शिनाख़्त करवाई जा रही है।

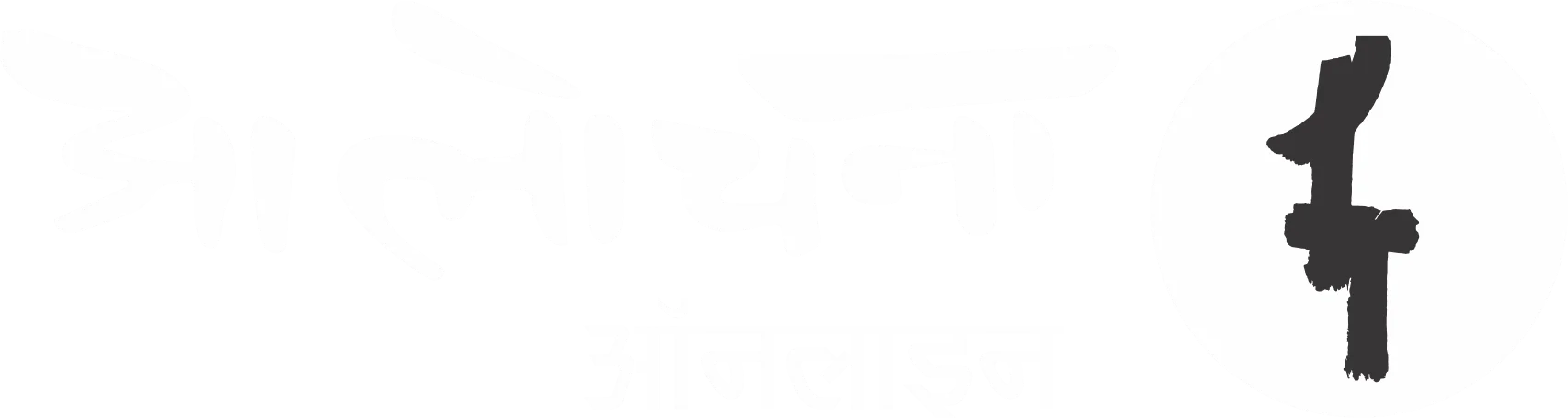
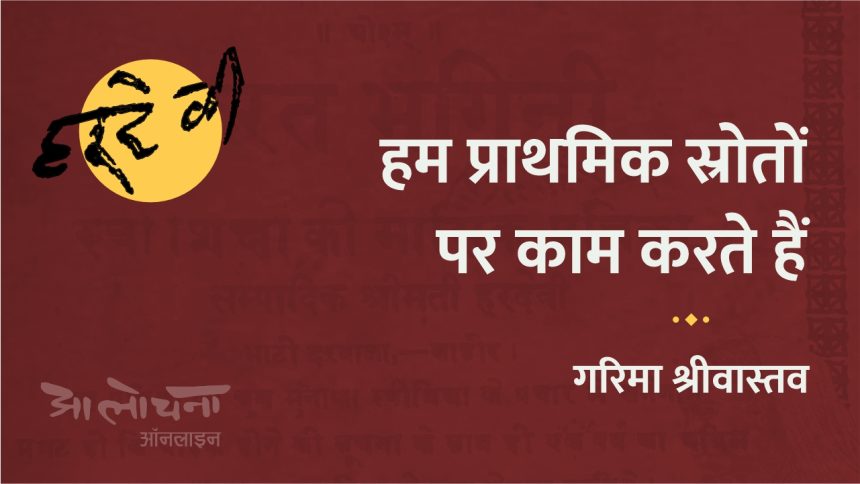
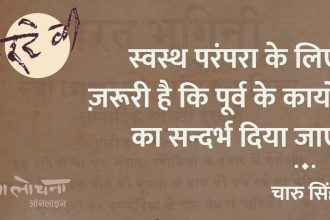
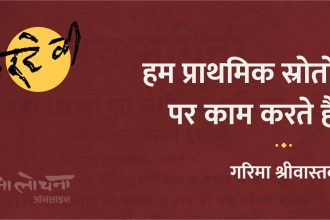
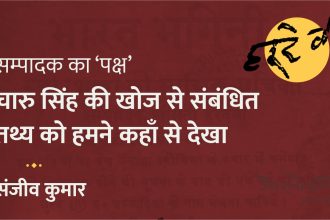
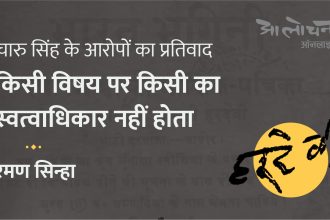
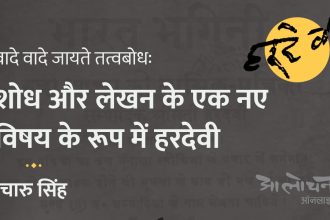

बहुत बढ़िया जवाब.