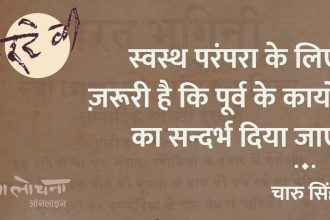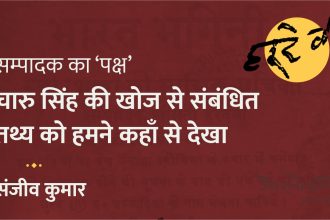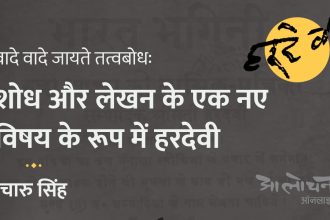विभाजन के प्रचलित आख्यानों पर सवाल उठाता आशुतोष कुमार का यह लेख भारत विभाजन को समझने की नई अंतर्दृष्टि मुहैया कराता है। कुछ व्यक्तियों और घटनाओं को विभाजन का जिम्मेदार ठहराने की आम प्रवृत्ति के उलट यह आलेख उपनिवेशन, औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा और भारतीय समाज की ऐतिहासिक बनावट में निहित अंतर्विरोधों की पड़ताल करता है। यह विभाजन और उसकी अब तक जारी परिणतियों को समझने की एक ऐसी सुसंगत और सुव्यवस्थित कोशिश है, जिसने इस विषय के अध्येताओं का भरपूर ध्यान आकर्षित किया है। यह आलेख आशुतोष कुमार और संजीव कुमार के संपादन में निकले आलोचना के पहले अंक (जनवरी-मार्च 2019; सहस्त्राब्दी अंक-59) का संपादकीय था। दोनों के संपादन में निकले आलोचना के पहले दो अंक ‘विभाजन के 70 साल’ पर केंद्रित थे।
एहसासे-ज़ियाँ
कराची के एक मुशायरे में हबीब जालिब अपना कलाम पढ़ रहे थे। दसियों हज़ार की भीड़ थी। गर्मी बहुत थी। समंदर क़रीब होने के चलते उमस भी। लोग हाथपंखों और रूमालों से कुछ हवा पैदा करते मुशायरे का आनंद ले रहे थे। जालिब ने अपनी मशहूर ग़ज़ल पढ़नी शुरू की:
सरे मिंबर वो ख़्वाबों का महल तामीर करते हैं
इलाजे-गम नहीं करते फ़क़त तक़रीर करते हैं।
पाकिस्तान के हाकिमों पर यह एक तीखा व्यंग्य था। लोग गर्मी भूलने लगे। तभी एक अप्रत्याशित शे’र पढ़ा गया:
हँसीं आँखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर
मैं हैराँ हूँ वो ज़िक्रे-वादिए-कश्मीर करते हैं!
तालियों की गड़गड़ाहट से शामियाना गूँज उठा। तालियों की यह गूँज आश्चर्यजनक थी, क्योंकि यह समझा जाता है कि पाकिस्तान की जनता कश्मीर को लेकर अत्यंत भावुक है। कश्मीर पाकिस्तान की सियासत की धुरी है। पाकिस्तान की राजनीति में चमकने के लिए कश्मीर पर ज़्यादा से ज़्यादा उग्रता दिखाना ज़रूरी समझा जाता है। इस शे’र में पाकिस्तानी सियासत के इसी पाखंड की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थीं। फिर भी इस शे’र को बेहद पसन्द किया गया।
हसीं आँखों और मीठे गीतों वाली ‘बुलबुलों’ के जिस चमन हिन्दोस्तान को खो देने की पीड़ा इस शे’र में है, उसकी भरपाई धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से भी नहीं हो सकती, अगर किसी तरह मिल भी जाए। यह उस अद्भुत देश को खो देने का अहसास है जो सारे जहाँ से अच्छा है, और जिसकी हस्ती, बकौल इक़बाल, दुनिया के मिटाए मिटाई नहीं जा सकी।
यूनान, मिस्र और रोम जैसी महान हस्तियाँ मिट गईं, मगर हिन्दोस्तान नहीं। ज़ाहिर है, इक़बाल पराधीन भारत के मुकाबले यूरोपीय सभ्यता के सभी महान उत्थानों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। यूनान नाम का देश और रोम नाम का शहर धरती पर आज भी मौजूद हैं। इक़बाल के ज़माने में भी भारत से बेहतर हालत में ही रहे होंगे। लेकिन उनकी प्राचीन सभ्यताओं की निरन्तरता मौजूद नहीं है।
अल्लामा का इशारा इसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता कि हिन्दोस्तान की तहज़ीबी निरन्तरता आज भी क़ायम है। शायद यही चीज़ इक़बाल की नज़र में इस देश को सारे जहाँ से अच्छा बनाती थी। लेकिन क्या सचमुच यह कोई अच्छी चीज़ थी?
दो सदियों की बेमिसाल लोकप्रियता के बावजूद तराना-ए-हिंद के आख़िरी शे’र पर कम ध्यान दिया गया है, जबकि यह सबसे काव्यात्मक और रहस्यमय शे’र है:
‘इक़बाल’ कोई महरम, अपना नहीं जहाँ में,
मालूम क्या किसी को, दर्द-ए-निहाँ हमारा।
यह हमारे किस छुपे हुए दर्द का इशारा है, जिसे समझने वाला जहाँ में कोई नहीं?
हबीब जालिब के शे’र में इक़बाल के उसी देश के खो जाने का दर्द है, जिसने वहाँ मौजूद हज़ारों श्रोताओं को एक साथ उद्वेलित कर दिया।
‘आलोचना’ का यह अंक (विभाजन के सत्तर साल, आलोचना के अंक 59 और 60; 2019) विभाजन से उपजे इस विराट क्षति-बोध यानी एहसासे-ज़ियाँ या ‘सेंस ऑफ़ लॉस’ के बारे में है।
इस एहसासे-ज़ियाँ का ज़िक्र करने से बचा जाता है। भारत की आज़ादी या पाकिस्तान के निर्माण के जश्न में इसे गुम कर देने की कोशिश की जाती है। यह कोशिश कामयाब नहीं हुई, क्योंकि साहित्य और कलाओं ने इस क्षति-बोध को खो जाने नहीं दिया। कविता ने, उपन्यास ने, संगीत ने, चित्रकला ने, नाटक ने, सिनेमा ने, सोशल मीडिया ने इसे सहेजा। सम्हालकर रखा। इसका सामना करने और इसे समझने के तरीके खोजे। और यह सब अनेक तरीकों से, अनेक रूपों में किया। यह काम आज भी लगातार जारी है। ‘आलोचना’ के दो अंकों में विभाजन के इसी क्षति-बोध को रेखांकित करने की कोशिश है।
बेशक इस काम के लिए इतिहास की गलियों में ताक-झाँक करनी पड़ती है। लेकिन इतिहास का ज़ोर विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उद्घाटित करने पर है। उन तात्कालिक कारकों की पहचान करने पर है, जिन्हें इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सके। अक्सर यह डिबेट जिन्ना, नेहरू, पटेल और माउंटबेटन के इर्दगिर्द घूमती रह जाती है, या मृतकों और विस्थापितों की संख्या तय करने में जुट जाती है। ये सारे काम ज़रूरी हैं, लेकिन साहित्य और कलाओं का काम इनसे आगे का है। उन गहनतर सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं को उद्घाटित करने का है, जिन तक इतिहास और समाज-विज्ञान के उपकरणों की पहुँच नहीं है। जहाँ जाने के लिए एक कवि की अंतर्दृष्टि चाहिए।
पिछले कुछ समय से इतिहास की शास्त्रीय सीमाओं के पार जाने की एक कोशिश मौखिक इतिहास के रूप में सामने आई है। इनके द्वारा जारी ढेर सारी ऐसी कहानियाँ सामने आई हैं, जो अब तक ‘ख़ामोशी के उस पार’ पड़ी हुई थीं। यह उर्वशी बुटालिया की 2002 में छपी एक चर्चित किताब का नाम है। ऐसी बहुत-सी कोशिशों ने उस ओढ़ी हुई ख़ामोशी को तोड़ने और कहीं गहरे दफ़ना दिये गए अनकहे दर्द को उजागर करने का काम किया है। ये मौखिक इतिहास-कथाएँ आँकड़ों में कैद यातनाओं को उद्घाटित करने का ज़रूरी काम करती हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीस-बाइस साल के युवाओं ने एक कमाल का काम किया है। उन्होंने मिलकर ‘बोलती खिड़की’ नाम का फेसबुक पेज बनाया है, जिससे विभाजन की बिछड़ी हज़ारों कहानियाँ आपस में बात कर रही हैं। इन मर्मस्पर्शी कहानियों को पढ़ना शुरू कीजिए। आप समझ जाएँगे कि विभाजन केवल नक़्शे पर है, केवल सरहदों पर है। दिलों में न कोई विभाजन था, न कोई है। यह वही एहसासे-ज़ियाँ है, जो सरहद के दोनों तरफ दिलों को दर्द के एक तार से जोड़ रहा है।
विभाजन की युगव्यापी पीड़ा जिस शिद्दत से उर्दू कविता में उभरकर आई, उस तरह किसी और ज़बान में नहीं। शायद उर्दू ने ही सबसे अधिक सहा है, और इसीलिए सबसे अधिक कहा है। कहानी में भी, कविता में भी। उर्दू के विश्वप्रसिद्ध अफ़सानानिगार और शायर बुनियादी रूप से विभाजन के क्षति-बोध के छायाकार हैं। ये छायाएँ अनेक रूप बदलकर आती हैं। सआदत हसन मंटो, इस्मत चुग़ताई, कृश्नचंदर, कुर्तुल ऐन हैदर, इब्ने इंशा, अब्दुल्ला हुसैन और इन्तज़ार हुसैन जैसे गद्य-लेखकों में वह सामने से दिखाई देती है। फ़ैज़, जोश, नासिर काज़मी और अख़्तर शीरानी जैसे शायरों के यहाँ कविता के स्वभाव के अनुरूप मनुष्यता के और बहुत सारे दुखों के साथ घुल-मिलकर आती है। जॉन एलिया की यह ग़ज़ल एक उदाहरण है। यह एक ऐसी ग़ज़ल है, जिसके आँसू दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर कहीं धधकते रहते हैं।
हम तो जैसे वहाँ के थे ही नहीं
बे-अमाँ थे अमाँ के थे ही नहीं
हम कि हैं तेरी दास्ताँ यकसर
हम तिरी दास्ताँ के थे ही नहीं
उनको आँधी में ही बिखरना था
बाल-ओ-पर आशियाँ के थे ही नहीं
अब हमारा मकान किसका है
हम तो अपने मकाँ के थे ही नहीं
हो तिरी ख़ाक़-ए-आस्ताँ पे सलाम
हम तिरे आस्ताँ के थे ही नहीं
हमने रंजिश में ये नहीं सोचा
कुछ सुख़न तो ज़बाँ के थे ही नहीं
दिल ने डाला था दरमियाँ जिनको
लोग वो दरमियाँ के थे ही नहीं
उस गली ने ये सुन के सब्र किया
जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं
नासिर काज़मी की समूची शायरी उसी एहसासे-ज़ियाँ को सम्बोधित है जो विभाजन की देन था। अपनी एक मशहूर ग़ज़ल में वे कहते हैं― ‘कुछ तो एहसासे-ज़ियाँ था पहले’। उसी में आगे फरमाते हैं :
डेरे डाले हैं बगूलों ने जहाँ
उस तरफ चश्म-ए-रवाँ था पहले
अब वो दरिया न वो बस्ती न वो लोग
क्या ख़बर कौन कहाँ था पहले
उर्दू शायरी को उदासी के आदाब सिखाने वाले नासिर काज़मी जिस खो गए चश्मे-रवां, दरिया और बस्ती को खोज रहे हैं, उसी की खोज कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने महा-आख्यान ‘आग का दरिया’ में की है। उसी के गुम होने की कहानी अब्दुल्ला हुसैन ‘उदास नस्लें’ में कहते हैं। सन इकहत्तर की लड़ाई की पृष्ठभूमि में उसी ‘बस्ती’ की तलाश इन्तज़ार हुसैन को भी रहती है। यशपाल ‘झूठा सच’ में उसी की बर्बादी की दास्ताँ लिखते हैं। भीष्म साहनी ‘तमस’ में उसी के ऊपर मँडलातीं चीलों का पीछा करते हैं।
फ़ैज़ ने अपनी मशहूर नज़्म ‘सुब्हे-आज़ादी’ में इस क्षति को कुछ अलग ढंग से देखा।
उनके लिए वह अतीत के किसी स्वर्णद्वीप की क्षति न होकर भविष्य के स्वप्नलोक की क्षति थी। उस उजली सुबह की क्षति थी, जिसे आना था, लेकिन जो अभी नहीं आई। आई एक शबगज़ीदा सहर, जिसकी नाउम्मीदी ख़ून के धब्बों की शक्ल में इकहत्तर की जंग के बाद इस शे’र में प्रकट हुई:
कब नज़र में आएगी बेदाग सब्जे की बहार
ख़ून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद
जो बात फ़ैज़ साहेब ने ‘सुब्हे-आज़ादी’ में इशारों में कही, उसे इंकलाबी शायर जोश मलीहाबादी ने अपनी नज़्म ‘मातमे आज़ादी’ में साफ़-साफ़ बयान कर दिया। यह भी बता दिया कि इस मातम के लिए पहला श्रेय किसको मिलना चाहिए।
शाखें हुईं दो-नीम जो ठंडी हवा चली
गुम हो गई शमीम जो बादे-शबा चली
अंग्रेज़ ने वो चाल बा-ज़ोरो-ज़फा चली
बरपा हुई बरात के घर में चला-चली
अपना गला खरोशे-तरन्नुम से फट गया
तलवार से बचा तो रगे-गुल से कट गया
विभाजन के बाद हिंद-पाक खित्ते में मेहदी हसन और ग़ुलाम अली जैसे दो महान ग़ज़ल गायकों का उभरना एक परिघटना है। दोनों गायकों ने जैसे ग़ज़ल गायकी का पुनराविष्कार किया और उसे अभूतपूर्व लोकप्रियता दिलाई। मेहदी हसन की आवाज़ में जो एक ख़ास तरह का दर्द है, क्या है वो? बहुत ठहरा हुआ-सा, सांद्र, सदियों की उदास अनुगूँजें समाए, जमीनी।
अबकि हम बिछड़े तो शायद कभी ख़्वाबों में मिलें…।
क्या यह बँटवारे का दर्द नहीं है?
जो मेहदी हसन की जीवन-कथा जानते हैं, उन्हें मालूम है कि उनका मन जोधपुर ज़िले के अपने जन्म-ग्राम लूणा के लिए किस कदर तड़पता था।
पटियाला घराने के गायक ग़ुलाम अली के गुरु बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहेब विभाजन के बाद अपने जन्म-ग्राम कसूर (लाहौर) जाकर भी जल्दी ही स्थायी रूप से रहने के लिए भारत लौट आए थे। अपनी गायकी से नासिर काज़मी की ग़ज़लों को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता गुलाम अली ने दिलाई। वे उस पार के इलाके के रहने वाले थे, लेकिन एहसासे-ज़ियाँ के दर्द का रिश्ता किसी इलाके से नहीं, एक तहज़ीब से है। यह दर्द छलकता है, जब गुलाम अली उदासी में डूबे हुए स्वर में गाते हैं :
भरी दुनिया में जी नहीं लगता
जाने किस चीज़ की कमी है अभी।
उपनिवेश और देश
कुछ सवाल यहाँ लाज़िमी हैं।
क्या सचमुच ‘भारतीय सभ्यता’ जैसी कोई चीज़ थी? अनगिनत जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों में विभाजित इस देश में क्या सचमुच कोई ऐसी बात थी, जो इसकी एक साझा पहचान बनाती हो?
क्या भारतीय सभ्यता की ‘निरन्तरता’ जाति, धर्म, जेंडर और वर्ग जैसी श्रेणियों पर आधारित शोषण के एक ख़ूबसूरत बारीक मकड़जाल का ही दूसरा नाम नहीं है? फिर इस भारतीय सभ्यता के घायल हो जाने और भारत के विभाजित हो जाने पर किस ‘क्षति’ का बोध हमारे कवियों लेखकों को होता रहा है?
क्या ‘भारतीय सभ्यता’ एक मिथक मात्र नहीं है, जिसे कथित राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान, ख़ास तौर पर, हिन्दू भद्रवर्गीय बुद्धिजीवियों के द्वारा गढ़ा गया था, ताकि उपनिवेश-विरोधी आन्दोलन के शामियाने में अपने लिए स्वायत्तता माँग रहे अल्पसंख्यक और दलित समुदायों को हाशिए तक महदूद रखा जा सके?
भारत, भारतवर्ष, हिंद, हिन्दोस्तान या इंडिया जैसी प्राचीन संज्ञाएँ किसी एक सुपरिचित सभ्यता की ओर संकेत करती हैं या अनेक सभ्यता-संस्कृतियों के एक ढीले-ढाले समूह की तरफ?
राष्ट्र या नेशन आधुनिक अर्थ में, बकौल एंडरसन, आख़िरकार एक परिकल्पित समुदाय ही तो है। क्या भारतीय राष्ट्रीयता की अवधारणा ऐसी ही एक इकाई के रूप में विकसित हुईं थी? या शुरू से ही अनेक राष्ट्रीयताओं के समुच्चय के रूप में?
एंडरसन मानते हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्र का उदय औद्योगिक क्रान्ति, जनभाषाओं के प्रेस के प्रसार और प्रिंट पूँजीवाद के विकास के साथ हुआ। यूरोप में भाषा आधारित राष्ट्रीयताओं के संगठन का यह बड़ा कारण है। भारत में यह प्रक्रिया भिन्न ढंग से घटित हुई।
जनभाषा प्रेस के प्रसार के साथ भाषिक जातीयताओं का विकास हुआ, लेकिन उसी के साथ एक वृहत्तर भारतीय राष्ट्रीयता की परिकल्पना भी चलती रही। बंगाली जातीयता की चेतना से प्रेरित गीत ‘वंदे मातरम’ की अखिल भारतीय लोकप्रियता इस सचाई का एक रोचक उदाहरण है। स्वाधीनता-संग्राम की पूरी अवधि में किसी भी भाषिक-जातीय समूह ने स्वयं को स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में कल्पित नहीं किया। रवीन्द्रनाथ, अल्लामा इक़बाल और प्रेमचन्द से लेकर सुब्रह्मण्यम भारती तक की ‘राष्ट्र की कल्पना’ में समूचा भारत शामिल होता है। आखिर क्यों?
शायद ही कोई इस सच्चाई से इनकार करता हो कि अनगिनत भाषाओं, बोलियों, जातियों, धर्मो और संस्कृतियों के होते हुए भी भारत के बहुतेरे लोग अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से खुद को भारतवासी या हिंदुस्तानी के रूप में देखने लगे थे। बाकी दुनिया भी उन्हें बहुत प्राचीन काल से उन्हें हिंदी, हिंदू या इंडियन कह कर बुलाती आई थी। ये सभी शब्द सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किए गए फिर धीरे-धीरे समूचे भरत खंड के लिए।
बेशक सभी भारतवासियों की भारत की कल्पना एक जैसी नहीं थी। संपन्न और विपन्न वर्गों की कल्पना का भारत एक जैसा हो भी नहीं सकता था। मालिकों का भारत अलग था और आदिवासियों, दलितों और वंचितों का भारत अलग। लेकिन भारत की कल्पना तब भी थी जब आधुनिक राष्ट्र या भारतीय राष्ट्र की कल्पना नहीं थी।
हिन्दी-पट्टी यानी ‘सूबा हिन्दुस्तान’ की हिन्दुस्तानी बोली दो स्वतन्त्र भाषाओं―उर्दू और हिन्दी―के रूप में आगे बढ़ी। इन दो भाषाओं का उत्थान एक स्तर पर बहुत सहज और स्वस्थ ढंग से हुआ। लेकिन एक दूसरे स्तर पर उसने साम्प्रदायिक रूप ले लिया।
एक ही व्यक्ति भारतेंदु के नाम से हिन्दी में और रसा के नाम से उर्दू में लिख सकता था, और दोनों जगह स्वीकृत हो सकता था। इंशा अल्ला ख़ाँ हिन्दी और उर्दू में एक साथ अपनी स्वतन्त्र पहचान बना सकते थे। प्रेमचन्द हिन्दी और उर्दू, दोनों के महानतम अफ़सानानिगार तस्लीम किए जा सकते थे। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा और कुछ हद तक छायावादी कवि भी उर्दूदाँ जमात के बीच पढ़े और सराहे जा सकते थे। मीर, ग़ालिब और फ़ैज़ जैसे इंक़लाबी शायर हिन्दी के पाठकों के बीच उतने ही मक़बूल हो सकते थे। ये सभी उदाहरण दोनों की सहज सह-उपस्थिति के हैं।
लेकिन हिन्दी और उर्दू क्रमशः हिन्दू और मुसलमान की नई बनती राजनीतिक पहचानों से जुड़ गईं। कुछ लोग यहाँ तक मानते हैं कि हिन्दी और उर्दू के सम्प्रदायीकरण ने ही देश के विभाजन की भूमिका बनाई। यह एक तरह की प्रयोजनमूलक या टेलिअलॉजिकल व्याख्या है। न तो सावरकर हिन्दी-भाषी थे, न जिन्ना उर्दू-भाषी। दोनों ने क्रमशः हिन्दी और उर्दू को अपने साम्प्रदायिक राजनीतिक अभियान की धुरी बनाया। हिन्दी और उर्दू के किसी बड़े लेखक ने ऐसा नहीं किया।
निराला पर हिन्दू राजनीतिक अस्मिता का जितना प्रभाव है, उतना ही इक़बाल पर मुस्लिम राजनीतिक पहचान का। निराला को जितना हिन्दू अतीत का अभिमान है, उतना ही इक़बाल को मुस्लिम इतिहास का। लेकिन दोनों न तो साम्प्रदायिक हैं और न ही द्विराष्ट्रवादी!
हिन्दू और मुसलमान की धार्मिक पहचानें राजनीतिक पहचानों में कैसे बदलती गईं? इस प्रक्रिया में औपनिवेशिक राज्य की भूमिका क्या थी? क्या यह भूमिका ‘फूट डालो और राज करो’ की उस बहुचर्चित रणनीति तक सीमित थी, जिसके उदाहरणों के रूप में बंग-भंग से लेकर कैबिनेट मिशन तक की बातें सामने रखी जाती हैं?
शायद उससे कहीं अधिक प्रभावशाली थी, औपनिवेशिक ज्ञान-निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय अतीत की हिन्दू काल और मुस्लिम काल के रूप में पुनर्रचना। इसे सबसे पहले जेम्स मिल के ‘हिस्ट्री ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया’ में सूत्रबद्ध किया गया। हिन्दू और मुस्लिम ‘गौरव’ की सारी प्रेरणाओं का स्रोत औपनिवेशिक इतिहास लेखन ही है।
इस इतिहास लेखन ने मध्यकाल के भारतीय इतिहासबोध को बदल दिया। इसने हिन्दू और मुसलमान को दो शत्रु सेनाओं के रूप में एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। इनके बीच समय-समय पर संधि-वार्ताएँ तो हो सकती थीं, लेकिन पूर्ण शांति कभी नहीं। इस इतिहास बोध में मध्यकाल मुसलमान सेना के हाथों हिन्दू सेना की पराजय का काल था। सो इस ऐतिहासिक पराजय का हिसाब बराबर करना हिन्दू गौरव की स्थापना का आवश्यक कार्यभार है। इसी तरह मुस्लिम स्वर्ण युग की वापसी मुस्लिम गौरव की स्थापना के लिए।
यह बोध हाली से लेकर इक़बाल तक को और मैथिलीशरण गुप्त से लेकर निराला तक को उद्वेलित तो करता है, हमेशा समन्वय पर जोर देने वाली भारतीय बुद्धि को विस्थापित नहीं कर पाता। लेकिन आगे चलकर यही साम्प्रदायिक इतिहास बोध व भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का आधारभूत सिद्धान्त बन जाता है। आज के भारत का मन्दिर-मस्जिद विवाद इसी सिद्धान्त की एक परिणति है।

इस विकृत बोध को अनेकानेक तरीकों से जनसाधारण पर थोपने के यत्न किये गए। लेकिन यह विभाजित इतिहासबोध जन-स्मृति को पूरी तरह विस्थापित न कर सका। विभाजन के एक दशक बाद आई फ़िल्म ‘मुग़ले आज़म’ उपमहाद्वीप की सफलतम फ़िल्मों में गिनी जाती है। इस फ़िल्म की विपुल लोकप्रियता आज तक बनी हुई है। यह भारतीय अतीत की उस जन-स्मृति का जीवंत प्रमाण है, जिसमें मुगल आख्यान हर भारतीय घर की कहानी का हिस्सा है। फ़िल्म ‘मुग़ले आज़म’ विभाजन की राजनीति का कलात्मक प्रतिकार भी थी।
हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य का सारा ठीकरा उपनिवेश के माथे पर ही नहीं फोड़ा जा सकता। इस वैमनस्य का एक देसी स्रोत था। भारतीय जाति-व्यवस्था।
लेकिन इस्लाम की वैचारिक उपस्थिति और मुसलमानों की भौतिक निकटता जाति-व्यवस्था के सामने एक जीवंत चुनौती की तरह उभरती हैं।
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन ‘मुसलमानों’ द्वारा पराजित ‘हिन्दुओं’ की कातर प्रार्थना के रूप में दिखाई देता है। हिन्दू-मुसलमान संघर्ष को मध्यकाल के मुख्य द्वंद्व के रूप में रेखांकित करना भारतीय इतिहास लेखन की औपनिवेशिक पद्धति को हिन्दी साहित्य के इतिहास पर लागू करना है। इसका प्रभाव ‘दूसरी परम्परा की खोज’ करने वाले आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर भी है।
वे भक्ति आन्दोलन को इस्लाम की चुनौती के समक्ष हिन्दू कोंसिलिडेशन की कोशिश के रूप में देखते हैं। अपनी पुस्तक ‘कबीर’ में साफ़-साफ़ कहते हैं कि इस्लाम भारतीय जाति-व्यवस्था को मिली पहली गम्भीर चुनौती थी, जिसने हिन्दू समाज को झकझोर दिया था।
मुसलमान के प्रति सवर्ण हिन्दू की असहजता का कारण यह है कि उसने भारत में प्रवेश करने वाले अन्य जातीय समुदायों की तरह हिन्दू जाति-व्यवस्था में खुद को समाहित नहीं किया। लेकिन मध्यकाल के किसी हिन्दू आचार्य या कवि ने इस चुनौती का उल्लेख नहीं किया। यह असहजता निश्चय ही उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के लेखकों की खोज है।
सवर्ण हिन्दू की यह असहजता सवर्ण (अशरफ़) मुसलमान के मन में हिन्दू वर्चस्व के भय में रूपान्तरित हो जाती है। जिन्ना का कथन कि अगर हिन्दुओं के हाथ में सत्ता आई तो वे मुसलमानों को हमेशा के लिए शूद्र बना देंगे, इसी भय की अभिव्यक्ति है। यह भय वास्तविक है कि जातिवादी सवर्ण हिन्दू मुसलमान को म्लेच्छ समझते हैं। सहयोग और बराबरी की बातें तभी तक हैं जब तक वे सत्ता से वंचित हैं।
भारत की हिन्दू-मुस्लिम समस्या एक स्तर पर सवर्ण हिन्दुओं और अशरफ़ मुसलमानों के बीच की सत्ता-प्रतियोगिता थी, जिसे राष्ट्रीय समस्या का रूप दे दिया गया।
दर्दे-निहाँ हमारा
1876 के आसपास रचे गए और 1882 में ‘आनन्द मठ’ उपन्यास में शामिल कर प्रकाशित किये गए गीत ‘वंदे मातरम’ में भारतमाता की परिकल्पना देवी के रूप में की गई थी। इस देवी की छवि बंगाल में प्रचलित दुर्गा या शक्ति से मिलती-जुलती है। उपन्यास में भारतमाता को बंदिनी बनाने वाले आततायी अंग्रेज़ नहीं, मुसलमान ज़मींदार दिखाए गए थे! इन दो कारणों से इस गीत को कुछ मुसलमानों के बीच अस्वीकार्य समझा जाता रहा है।
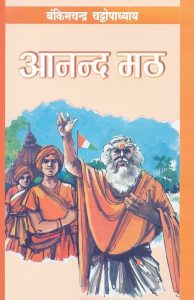
लेखक ने स्वयं इस तथ्य का उल्लेख किया है कि यह उपन्यास संन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जो बंगाल में अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुआ था। उपन्यास में अंग्रेज़ों को निशाना न बनाने का कारण इसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता कि सरकारी नौकर होने के नाते लेखक अंग्रेज़ी राज पर सीधा हमला करने से बचना चाहता हो।
उपन्यास का समूचा तेवर राजनीतिक है। धार्मिक या साम्प्रदायिक नहीं। उपन्यास और गीत की प्रचंड लोकप्रियता का कारण है: शक्ति की मौलिक कल्पना। बंगालियों की कल्पना में दुर्गा की जगह भारतमाता को बिठा देना असली सांस्कृतिक क्रान्ति थी। यह मुस्लिम-विरोधी न थी। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि इसमें भारतमाता की सात करोड़ सन्तानों को उनकी शक्ति के स्रोत के रूप में चित्रित किया गया है। उस समय बंगाल की समूची जनसंख्या सात करोड़ के आसपास थी। इसमें हिन्दू-मुसलमान, दोनों शामिल थे। ‘वंदे मातरम’ राजनीतिक सन्देश और राष्ट्रीय काव्य के रूप में बहुत समय तक हिन्दुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय रहा।
कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि देवता की तरह देश की वन्दना करना मूर्तिपूजा का एक रूप है। कुछ मुसलमान इस कारण भी इस गीत से परहेज करते हैं। उधर देशभक्ति का मतलब ‘हिंदुत्व’ समझने वाले कहते हैं कि ‘वंदे मातरम’ ही देशभक्ति की असली कसौटी है। आख़िर इसी एक कसौटी पर कतिपय मुसलमानों की देशभक्ति को संदिग्ध ठहराया जा सकता है! साम्प्रदायिक विचारधारा अपनी बड़ाई से नहीं, दूसरे की बुराई से पहचानी जाती है।
इसी ज़बरदस्ती के कारण मुस्लिम लीग को यह कहने का मौका मिलता था कि ‘वंदे मातरम’ के बहाने मुसलमानों पर हिन्दू मान्यताएँ थोपी जा रही हैं। सन सैंतीस के बाद बनी कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों ने कहीं-कहीं स्कूलों और सरकारी दफ़्तरों में ‘वंदे मातरम’ का गायन शुरू किया था। लीग इसे कांग्रेस सरकार के हिन्दू सरकार होने का एक और सबूत मानती थी। लेकिन लीग के ध्यान में यह नहीं था कि उनके प्रेरणा-पुरुष और अध्यक्ष रह चुके मुहम्मद इक़बाल भी देश की मिट्टी की वन्दना देवता के रूप में कर चुके थे:
पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है
ख़ाके-वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है
1879 में सर सैयद अहमद ख़ान की प्रेरणा से रचा गया मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ‘मुसद्दस’ प्रकाशित हुआ, जो भारतीय मुसलमानों के नवजागरण का आधारभूत ग्रन्थ बन गया। यह ग्रन्थ भारत की चिन्ताओं के बारे में न होकर दुनिया में इस्लाम के उत्कर्ष और पराभव के बारे में था। भारत में मुसलमानों की दुरवस्था को इस विश्वव्यापी मुस्लिम पराभव की एक कड़ी के रूप में देखा गया। घोषित रूप से मुस्लिम काव्य होने के बावज़ूद ग़ैर-मुस्लिमों ख़ासकर हिन्दुओं पर इसका गहरा असर था। दिलचस्प है यह देखना कि किस तरह लोगों ने ‘मुसद्दस’ के धार्मिक-साम्प्रदायिक कथ्य की उपेक्षा करते हुए राष्ट्रीय और जातीय जागरण के उसके सन्देश को पहचाना और अपनाया।
1912 में लिखा गया और 1914 में प्रकाशित ‘भारत-भारती’ ‘मुसद्दस’ से प्रत्यक्षत: प्रेरित था। राष्ट्रकवि कहे गए मैथिलीशरण गुप्त ने इस रचना में ठीक ‘मुसद्दस’ की तर्ज़ पर हिन्दुओं के पराभव की कथा लिखी और उन्हें जगाने की भरपूर कोशिश की। राष्ट्रकवि ने अपने काव्य की भूमिका में स्वयं इस तथ्य का उल्लेख किया है। हाली के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। इस रचना पर अंग्रेज़ इतिहासकारों के बनाए इतिहास-बोध का किंचित असर है। मुस्लिम राजत्वकाल की भरपूर निंदा है। लेकिन इस्लाम या मुसलमान का विरोध नहीं है। मुसलमानों के योगदान को स्वीकार किया गया है। अकबर की तो अलग से भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है।
‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा’ यानी ‘तराना-ए-हिंद’ की रचना इक़बाल ने सन 1905 में की थी। इस रचना में ‘हिन्दी’ शब्द हिन्दुस्तानियों के लिए आया है, जिनके मज़हब उनको आपस में बैर रखना नहीं सिखाते थे।
लेकिन कुछ ही समय बाद, 1908 के आसपास इक़बाल ने ही ‘तराना-ए-मिल्ली’ लिखा, जिसमें कहा गया था:
चीनो अरब हमारा, हिन्दोस्ताँ हमारा
मुस्लिम हैं हम वतन है, सारा जहाँ हमारा।
कहते हैं, यह राष्ट्रवादी इक़बाल के इस्लामवादी हो जाने का घोषणापत्र था।
बाद में, सन 1958 में, एक फ़िल्म आई, ‘फिर सुबह होगी’। इस फ़िल्म में साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा, जिसे ‘तराना-ए-हिंद’ और ‘तराना-ए-मिल्ली’―दोनों की यथार्थवादी पैरोडी कह सकते हैं। दोनों तरानों से ली गई कुछ लाइनें इसमें शामिल हैं:
चीन ओ अरब हमारा, हिन्दोस्ताँ हमारा
रहने को घर नहीं है, सारा जहाँ हमारा
चीन ओ अरब हमारा…
खोली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गईं हैं
सड़कों पे घूमता है, अब कारवाँ हमारा
जेबें हैं अपनी ख़ाली, क्यों देता वरना गाली
वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा
चीन ओ अरब हमारा…
29 दिसम्बर 1930 को इलाहाबाद में आल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन में सर मुहम्मद इक़बाल ने वह प्रसिद्ध अध्यक्षीय भाषण दिया जिसे पाकिस्तान की परिकल्पना का बीज-वक्तव्य समझा जाता है। इसी भाषण में पहली बार यह धारणा पेश की गई कि पश्चिमोत्तर के मुस्लिमबहुल प्रान्तों को मिलाकर एक स्वशासित राज्य का निर्माण करना कम से कम पश्चिमोत्तर के मुसलमानों की अन्तिम नियति है।
इसी बिना पर कहा जाता है कि पाकिस्तान इक़बाल का स्वप्न था, जिसे जिन्ना ने साकार किया।
1930 के लीग अधिवेशन में इक़बाल द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण को फिर से देख लिया जाए तो इतिहास के कुछ भरम दूर हो सकते हैं।
इस अच्छे-खासे दार्शनिक भाषण में इक़बाल सबसे पहले इस्लाम और राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं। कहते हैं यूरोप का प्रान्तिक (टेरिटोरियल) राष्ट्रवाद एक खंडित चेतना है। यह ईसाई द्वैतवाद की उपज है। यह इस्लाम की अद्वैत दृष्टि और अखंड मानवीय चेतना के विरुद्ध है। राष्ट्र जमीन का टुकड़ा नहीं, एक तरह की ‘नैतिक चेतना’ है। वे लगातार यूरोपीय ईसाई नज़रिए और इस्लाम के बीच के कंट्रास्ट को रेखांकित करते हैं। इस प्रसंग में वे हिन्दू या भारतीय नज़रिए का उल्लेख नहीं करते। लेकिन अखंड मानवीय चेतना, अद्वैत और नैतिक चेतना के रूप में राष्ट्र की उनकी ये व्याख्याएं महर्षि अरविन्द, महात्मा गांधी और गुरुदेव की धारणाओं की संगति में हैं। यहाँ निराला के इस वाक्य को याद किया जा सकता है, ‘दीन इस्लाम अद्वैत की रौशनी लेकर फैला।’
प्रान्तिक या टेरिटोरियल राष्ट्रवाद के खंडन का यह मतलब नहीं कि इक़बाल के भारत-प्रेम में कोई कमी आ गई है। वे अपने भाषण की शुरुआत में एक आश्चर्यजनक बात कहते हैं:
‘ऐसा कहने में सचमुच कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत दुनिया का एकमात्रा देश है, जहाँ एक जन-निर्मात्राी शक्ति के रूप में इस्लाम ने श्रेष्ठतम कार्य किया है।’
(Indeed it is not an exaggeration to say that India is perhaps the only country in the world where Islam, as a people-building force, has worked at its best)
इक़बाल के सामने अरब देश भी हैं, फ़ारस भी है, तुर्की भी है, अफ़ग़ानिस्तान भी है। लेकिन इस्लाम उनके लेखे अपने श्रेष्ठतम रूप में प्रस्फुटित हुआ भारत में! भाषण के अन्त में वे यह भी साफ कर देते हैं कि भारत के भीतर एक एकीकृत मुस्लिम राज्य की ज़रूरत इसलिए है कि भारतीय इस्लाम को अरबी साम्राज्यवाद के ठप्पे से बचाया जा सके। (‘…an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian Imperialism was forced to give it…’)
यानी 1905 में ‘सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा’ लिखने वाले इक़बाल 1930 में भी वही सोचते हैं। यह मिथ्या प्रचार है कि इक़बाल बदल गए, भारत-प्रेमी की जगह पाकिस्तान-परस्त हो गए। इस भाषण में इक़बाल ने मुसलमानों के किसी स्वतन्त्र देश का विचार पेश नहीं किया था। ‘भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत’ की बात कही थी। मूल विचार यह था कि पश्चिमोत्तर के मुस्लिम-बहुल प्रान्तों को एक संयुक्त प्रान्त या राज्य के रूप में पुनर्गठित करना चाहिए। इक़बाल ने बंगाल का ज़िक्र नहीं किया था।
भारत के भीतर एकीकृत मुस्लिम राज्य की ज़रूरत क्या थी? भारत धीरे-धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था। डर यह था कि आज़ाद भारत में संख्या बल के कारण हिन्दुओं का राजनीतिक वर्चस्व कायम हो जाएगा। इससे मुसलमानों की अपनी संस्कृति, उनका सामाजिक संगठन और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी ख़तरे में पड़ सकती है। मुसलमानों का भारत के भीतर अपना एक विशाल राज्य होगा, जहाँ वे बहुमत में होंगे, तो निर्द्वन्द्व भाव से अपने लिए अनुकूल जीवन-शैली का निर्माण कर सकेंगे।
लोकतान्त्रिक भारत में बहुसंख्यक हिन्दुओं का वर्चस्व होगा, यह भय पाकिस्तान के समूचे आन्दोलन की जड़ था। क्या यह भय काल्पनिक था? इस भय के पीछे थी, ‘हिन्दू’ और ‘मुसलमान’ की राजनीतिक पहचानों के निर्माण की प्रक्रिया। अंग्रेज़ों के आने के पहले ये महज धार्मिक और साम्प्रदायिक पहचानें थीं। 1857 के बाद हिन्दू और मुसलमान राजनीतिक श्रेणियों में ढलने लगे थे। ‘द्विराष्ट्रवाद’ का सिद्धान्त इसी प्रक्रिया की परिणति थी, जिसे 1937 में सावरकर ने और 1940 में जिन्ना ने सूत्रबद्ध किया। इक़बाल के सन तीस के भाषण पर इस विचार की कोई छाया नहीं थी।
इस भाषण में इक़बाल यूरोपीय ढंग के एकात्म राष्ट्रवाद का खंडन करते हुए भारतीय राष्ट्रीयता की मौलिक कल्पना पेश करते हैं:
“इसलिए भारतीय राष्ट्र की एकता अनेक के निषेध में नहीं बल्कि परस्पर सामंजस्य और सहयोग में ढूँढ़नी चाहिए….अगर भारत में सहयोग का कोई असरदार सिद्धान्त तलाश लिया गया तो वह इस प्राचीन भूमि में शांति और पारस्परिक कल्याण-भाव को सम्भव करेगा, ऐसी प्राचीन भूमि जिसने लम्बे समय तक यातना सही है, अपने लोगों की किसी अन्तर्निहित अक्षमता के कारण उतना नहीं जितना इतिहास-परिसर में अपनी अवस्थिति के कारण। और वह सहयोग का सिद्धान्त, लगे हाथ एशिया की समग्र राजनीतिक समस्या को भी हल करेगा।”
(The unity of an Indian nation, therefore, must be sought not in the negation, but in the mutual harmony and cooperation, of the many…If an effective principle of cooperation is discovered in India, it will bring peace and mutual goodwill to this ancient land which has suffered so long, more because of her situation in historic space than because of any inherent incapacity of her people. And it will at the same time solve the entire political problem of Asia.’)
इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे इक़बाल ‘सारे जहाँ से अच्छा’ की अपनी व्याख्या पेश कर रहे हों। समझा रहे हों कि सारे जहाँ से अच्छे हिन्दोस्तान की प्राचीन भूमि का ‘दर्दे-निहाँ’―अलक्षित वेदना―क्या है।
इतिहास परिसर की अवस्थिति का संकेत स्पष्ट है। भारत के उपनिवेशन की ऐतिहासिक त्रासदी। इस त्रासदी से लड़ने का एक ही तरीका है: सामंजस्य और सहयोग।
भारत में संस्कृतियों, भाषाओं, परम्पराओं, जातियों, धर्मों और आस्थाओं की इतनी बहुलता है, और हर इकाई अपनी स्वकीयता को लेकर इतनी आग्रही है कि उन सबकी उन्नति, और सबके साथ भारतीय समग्र की उन्नति केवल पारस्परिक सामंजस्य और सहयोग से ही सम्भव है। विविधता में छुपी हुई किसी एकता की नेहरू जी की खोज से उतनी नहीं, जितनी ‘अनेक के इक़बाल सम्मत सामंजस्य और सहयोग’ से। सामंजस्य और सहयोग को एक शब्द में कहना हो तो समन्वय कह सकते हैं।
भारत में कभी श्रद्धा का कोई एक वर्चस्वमान केन्द्र नहीं रहा। एकेश्वरवाद अपनी जगह, देवी-देवताओं की अनन्त कतार अपनी जगह। तौफ़ीक़ अपनी जगह, पीरों-फ़कीरों की बहार अपनी जगह।
भारत की राष्ट्रीयता यूरोप की तरह एकात्म नहीं हो सकती, इसे बहुलात्म होना होगा। यह बहुलात्मता हमेशा से भारतीय जीवन शैली की एक मूलभूत विशेषता रही है। इक़बाल कहते हैं कि स्वयं हिन्दू जनसमुदाय बहुलात्म है। यह कोई एक परम्परा नहीं, अनेक परम्पराओं का समन्वय है।
भारतीय मेधा जब कभी बहुलात्म समन्वय की दिशा में सक्रिय होती है, महानताओं की सृष्टि करती है। इसी समन्वय से हिन्दुस्तानी संगीत की रचना हुई है, जो लगभग हज़ार वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर और भीतर संगीत-पिपासु आत्माओं को तृप्त करती आ रही है। अमीर खुसरो का युग-प्रवर्तक व्यक्तित्व इसी समन्वय की उपज है। कव्वाली उनके अनेक आविष्कारों में एक है, जो भारतीय संस्कृति की ख़ास पहचान है। कव्वाली के स्वर ही नहीं, भाव भी समन्वय के राग से उपजते हैं। मुगलों की चित्रकला से एम.एफ. हुसैन तक की कला परम्परा में इस समन्वय के अनोखे रंग हैं। ताजमहल की वास्तुकला इसी समन्वय से बना एक विश्व-आश्चर्य है। स्वयं हमारी हिन्दी-उर्दू जबां, जिसके हिन्दवी, रेख़्ता, दकनी, गूजरी और हिन्दुस्तानी जैसे नाम-रूप भी अनेक हैं, इसी समन्वय की देन है।
जब एकल वर्चस्व की कोई ज़िद इस बहुलात्मता को दबाने की कोशिश करती है, विघटन और विनाश के रास्ते खुलने लगते हैं। क्या समन्वय और वर्चस्व के दो उपक्रमों के बीच निरन्तर जारी यह कशमकश ही भारत की वह अलक्षित वेदना है, दर्दे-निहाँ है, जिसकी ओर ‘तराना-ए-हिंद’ में इशारा किया गया है?
इक़बाल ने इस भाषण में इस भारतीय कल्पना के जिन दो महान स्वप्नदर्शियों का उल्लेख किया है, वे हैं, कबीर और अकबर। यहीं यह दुःख भी प्रकट किया है कि हम उस स्वप्न को पूरी तरह साकार न कर सके।
यह अकारण नहीं है कि इक़बाल ने कबीर का नाम लिया। तुलसीदास का नहीं। जबकि समन्वय की चेष्टा का लोकनायक तो तुलसीदास को कहा गया है। कबीर तो सबको डाँटने-फटकारने वाले माने जाते हैं। हमारे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तो साफ कहते थे कि हिन्दुओं और मुसलमानों के हृदयों को जोड़ने का काम कबीर से नहीं सधा।
लेकिन कबीर और तुलसीदास की समन्वय-चेष्टा में एक बहुत बड़ा फर्क है। तुलसी का समन्वय पदानुक्रम पर आधारित है, कबीर का बराबरी पर। टिकाऊ समन्वय बराबरी के आधार पर ही हो सकता है। कबीर जिस सहजता से अल्लाह और राम दोनों के नाम ले सकते हैं, तुलसीदास नहीं। तुलसी का समन्वय वर्चस्व की एक व्यवस्था पर आधारित है। सही मायने में, वह समन्वय नहीं, प्रतिपालन यानी ‘पैट्रनाइज़िंग’ है।
युग की विडम्बना यह है कि एक तरफ गांधीजी हैं, दूसरी तरफ अल्लामा इक़बाल। दोनों ही समन्वय के महान स्वप्नद्रष्टा। वे आपस में ही समन्वय कायम नहीं कर सके! यह भारतीय इतिहास की एक ऐसी गुत्थी है, जिसे हल किए बिना भारतीय उपमहाद्वीप की भविष्य-यात्रा शुरू नहीं हो सकती। विभाजन इस गुत्थी के अनसुलझे रह जाने का परिणाम था। और जब तक यह गुत्थी नहीं सुलझती, हम विभाजन के निरन्तर जारी विनाश-चक्र से मुक्त नहीं हो सकते।
इक़बाल अपने समन्वय-स्वप्न की पूर्ति के लिए भारत में ख़ास तरह के संघीय गणराज्य की कल्पना करते है, जिसमें एक एकीकृत मुस्लिम-बहुल प्रान्त भी होना चाहिए। इस कल्पना की व्यावहारिक झलक कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में दिखाई देती है। इस प्रस्ताव में मुस्लिम-बहुल राज्य दो हो जाते हैं, तीसरा शेष भारत है। इन तीनों का एक परिसंघ बनना है, जिसमें केन्द्र की शक्तियाँ रक्षा, विदेश नीति और संचार तक सीमित रहनी हैं। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान के लिए आन्दोलन करने वाली मुस्लिम लीग तो राजी हो जाती है, लेकिन कांग्रेस सहमति देने के बावजूद दुविधा से मुक्त नहीं हो पाती। दुविधा कुछ और नहीं, केन्द्रीयता और संघीयता के दो सिद्धान्तों की है। कांग्रेस अन्ततः दुर्बल केन्द्र के लिए तैयार नहीं हो पाती। वह समन्वय ज़रूर चाहती है, लेकिन केन्द्रीय सत्ता की कमज़ोरी नहीं। क्या इसका अर्थ यह है कि वह बहुलात्म संघीय समन्वय के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी? क्या उसका झुकाव प्रतिपालक समन्वय की तरफ बना रहा।
इतिहास के कुछ अनुत्तरित प्रश्न अल्लामा इक़बाल के लिए भी हैं। यह कैसे हुआ कि पाँच सदियों तक मुसलमान शासकों के वर्चस्व के बावजूद भारत के अधिसंख्य मुसलमान भीषण गरीबी और जहालत की ज़िन्दगी जीने के लिए अभिशप्त बने रहे? इन ग़रीब मुसलमानों के लिए भविष्य के एकीकृत मुस्लिम-बहुल प्रान्त में मुस्लिम लीग की क्या योजना थी? जिन किसानों की बदहाली पर खुद इक़बाल साहेब का बयान यह था कि जिस खेत से दहकाँ को मयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर गोश-ए-गंदुम को जला दो, उनके लिए इस लम्बे दार्शनिक राजनीतिक भाषण में दो शब्द भी क्यों नहीं थे? क्या भारत में लोक-निर्मात्री शक्ति के रूप में इस्लाम की सर्वश्रेष्ठ भूमिका नवाबों और ज़मींदारों के निर्माण और शोषित अवाम पर उनके शिकंजे को मज़बूत बनाने में देखी जा रही थी?
बराबरी का सन्देश देने वाले इस्लाम ने भारत में अपनी एक स्वतन्त्र वर्ण-व्यवस्था बना ली थी। निचली जातियों के मुसलमानों को, जिनकी संख्या अशरफ़ की तुलना में कई गुना ज़्यादा थी, एकीकृत मुस्लिम-बहुल प्रान्त में क्या हासिल होने वाला था? क्या मुस्लिम बहुमत वाले उस विशाल प्रदेश में सैय्यद और अंसारी बराबर हो जाने वाले थे? लेकिन इक़बाल ने अपने उस ऐतिहासिक भाषण में इन बड़े बुनियादी सवालों को छुआ तक नहीं।
संघीयता का सिद्धान्त अच्छा है, लेकिन आधुनिक भारत धार्मिक-साम्प्रदायिक समूहों का संघ क्यों बने? अगर पश्चिमोत्तर सरहदी प्रान्त के पठान पंजाबी मुसलमानों की तुलना में बंगाली हिन्दुओं से अधिक निकटता महसूस करते हों तो उन्हें एक पंजाबी वर्चस्व वाले मुस्लिम-बहुल प्रान्त में रहने के लिए क्यों बाध्य किया जाए? कैबिनेट मिशन के अनिवार्य समूहीकरण के प्रस्ताव के विरोध के पीछे कांग्रेस का यही सवाल था।
इक़बाल अगर सामने होते तो इनमें से कुछ सवालों के जवाब दे सकते थे। जैसे सन तैंतीस में पंडित नेहरू को दिया था। वे कहते कि भारत के आठ करोड़ मुसलमान अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ न्यूनतम संवैधानिक उपाय चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस बात की संवैधानिक गारंटी की जाए कि लोकतान्त्रिक भारत में एक विराट अल्पसंखयक समुदाय के रूप में उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के बराबर अवसर मिलेंगे। इसमें किंचित भी कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस का हिन्दू नेतृत्व इन्हें लागू करने की जगह टालमटोल करता क्यों दिखाई दे रहा है?
इक़बाल कहते कि कांग्रेस नेतृत्व वर्णाश्रमी विचारधारा से मुक्त नहीं है। जब वे अपने समुदाय के लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकते, तो उनसे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे मुसलमानों के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे? जब सत्ता से वंचित होते हुए वे अपनी जाति-पहचानों और अपने धार्मिक प्रतीकों पर ज़ोर देते हैं, तो सत्ता मिल जाने के बाद वे ऐसा नहीं करेंगे, इसकी उम्मीद कैसे की जाए?
जब स्वघोषित हिन्दू नेतागण देश-भर में ‘शुद्धि अभियान’ के नाम पर मुसलमानों की घर-वापसी का अभियान चलाने में जुटे हुए हों, और इन नेताओं की कांग्रेस में भी आवाजाही लगी रहती हो, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद ये लोग मुसलमानों के साथ म्लेच्छों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे?
जब वे अपने स्वराज को भी ‘राम राज्य’ के रूप में परिभाषित करते हैं, तब यह यकीन किस बिना पर हो कि वे अपने राज्य की चाभियाँ किसी राम मन्दिर में नहीं छोड़ आएँगे? यह कैसे कहा जा सकता है कि जिन राम और कृष्ण जैसे देवताओं के लिए मुसलमानों ने हिन्दुओं से भी बेहतर गीत रचे और गाए हों, उन्हें एक दिन उनके समक्ष शत्रुतापूर्ण चुनौती की तरह पेश नहीं कर दिया जाएगा?
इक़बाल कहते कि अगर बहुसंख्यक हिन्दुओं ने अपने को एक राजनीतिक श्रेणी के रूप में संगठित करने के उत्तेजक अभियान न चलाए होते तो मुसलमानों के मन में उनके वर्चस्व का भय पैदा ही नहीं होता। अगर हिन्दुओं ने भारतीय राष्ट्रीयता को हिन्दू रंग देने की कोशिश न की होती तो शायद मुसलमानों को यह फिक्र न होती कि इसमें उनका रंग कहाँ है! वे कहते कि अल्पसंख्यक के मन में बहुसंख्यक का भय स्वाभाविक और तर्कसंगत है, जिसे दूर करने की ज़िम्मेदारी बहुसंख्यक की है, और इसका विलोम सम्भव नहीं।
आज अगर इक़बाल होते, तब तो उनके पास कहने को और भी बहुत कुछ होता। उनके हाथ में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट होती। उनके पास आज़ादी के बाद हुए दंगों का इतिहास होता। उनके पास अख़लाक़ और जुनैद की सत्य-कथाएँ होतीं। बल्कि आज अगर वे होते तो कहते कि तुम पूछ किस मुँह से रहे हो मियाँ!
पलटकर आप भी पूछ सकते थे कि वैसे मुसलमानों के नाम पर बने दुनिया के पहले मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों के क्या हाल हैं!
पाकिस्तान प्रस्ताव?
1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को ‘पाकिस्तान प्रस्ताव’ कहा जाता है। इस प्रस्ताव में भी पाकिस्तान का नाम नहीं था। कहा यह गया था कि मुस्लिम लीग को ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था मंजूर नहीं होगी, जिसमें पश्चिमोत्तर और पूर्व के मुस्लिम-बहुल इलाकों को स्वतन्त्र ‘राज्यों’ के रूप में पुनर्गठित न किया गया हो। इस प्रस्ताव में भी यह बिलकुल स्पष्ट नहीं था कि ये राज्य भारत के बाहर ही होंगे। मुस्लिम लीग ने अपने रिकॉर्ड में इसे ‘लाहौर प्रस्ताव’ के नाम से दर्ज किया है, पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से नहीं। शुरुआत में इसे पाकिस्तान-प्रस्ताव विरोधियों द्वारा कहा गया। मज़ाक उड़ाने के लिए। इसका अवमूल्यन करने के लिए। बाद में लीग ने इसे सगर्व अपना लिया, एक मुस्लिम यूटोपिया के रूप में पाकिस्तान की चर्चा के जड़ ज़माने के साथ।

इस अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भीषण में जिन्ना ने घोषित किया कि भारत के हिन्दू और मुसलमान दो स्वतन्त्र राष्ट्र हैं। दोनों नितान्त भिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं। दोनों की संस्कृति, इतिहास और जीवन-दृष्टियाँ भिन्न हैं। हज़ार वर्षों से एक साथ रहते हुए भी उन्होंने कोई समान जीवन-शैली विकसित नहीं की है। इसलिए उन्हें एक ही राज्य के अन्तर्गत इस तरह समायोजित करना कि बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व स्थायी हो जाए, सभी के लिए विनाशकारी होगा।
ये वही जिन्ना थे, जिन्होंने धर्म और राजनीति का घालमेल करने के लिए गांधीजी की अगुआई में चले ख़िलाफ़त आन्दोलन की आलोचना की थी!
पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में खुद मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने पहले ही इस भाषण में इस सिद्धान्त की धज्जियाँ उड़ा दीं। 11 अगस्त, 1947 के इस मशहूर भाषण में उन्होंने फ़रमाया कि अब जबकि पाकिस्तान बन गया है, हिन्दू और मुसलमान राजनीतिक अर्थों में हिन्दू और मुसलमान नहीं रह जाएँगे। पाकिस्तान मुस्लिमबहुल तो होगा, लेकिन इस्लामी राज्य नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा।
इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दू और मुसलमान तभी तक दो राष्ट्र थे, जब तक भारत एक था!
‘द सोल स्पोक्समैन: जिन्ना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फ़ॉर पाकिस्तान’ नामक पुस्तक में पाकिस्तानी इतिहासकार आएशा जलाल का तर्क है कि पाकिस्तान की माँग महज सौदेबाजी के लिए थी। जिन्ना का असली मकसद स्वतन्त्र भारत की लोकतान्त्रिक सत्ता-संरचना में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना था। यह सुनिश्चित करना था कि हिन्दू अपनी बहुसंख्या के आधार पर मुसलमानों को दूसरे दर्जे की नागरिकता में न ढकेल दें।
यही कारण था कि उन्होंने कैबिनेट मिशन के उस प्रस्ताव के लिए मुस्लिम लीग को राजी कर लिया था, जिसमें त्रिस्तरीय परिसंघ की कल्पना की गई थी। पूर्व और पश्चिम के मुस्लिमबहुल प्रान्तों और शेष हिन्दूबहुल प्रान्तों को लेकर तीन समूह बनाए जाने थे। केन्द्र के पास रक्षा, संचार और विदेश विभाग छोड़कर बाकी का बँटवारा समूहों और प्रान्तों के बीच होना था।
दस वर्षों के लिए निर्धारित समूहों के साथ प्रान्तों की सदस्यता अनिवार्य थी। उसके बाद प्रान्त अपनी सदस्यता पर पुनर्विचार कर सकते थे। यह व्यवस्था मुसलमानों के लिए उनके बहुमत वाले इलाकों में अधिकतम स्वायत्तता की गारंटी करती थी। भारत की एकता को बनाए रखते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यकों की चिन्ताओं को सुलझाने का यह सबसे बेहतर इन्तज़ाम था।
गांधीजी और जिन्ना दोनों ने साफ-साफ कबूल किया कि उस वक़्त के हालात में अंग्रेज़ों से इससे बेहतर कुछ पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लीग के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी, भीषण अन्दरूनी वाद-विवाद के बाद, भारी बहुमत से इसे मंजूर कर लिया। यह एक ऐसा क्षण था, जो टिका रह जाता तो भारतीय अवाम की सारी ज़द्दोज़हद और कुर्बानियों को सार्थकता मिल जाती। एशिया में एकजुट आज़ाद भारत का उदय होता तो मनुष्यता की नियति कुछ और होती। लेकिन नियति के साथ जो हमारा समझौता था, उसमें ये शर्त शामिल नहीं थी।

7 जुलाई को कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद 10 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस कांफ्रेंस में दिया गया नेहरू जी का वक्तव्य विभाजन और आज़ादी के इतिहास का सबसे विवादास्पद वक्तव्य साबित हुआ। नेहरू ने कहा कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को मंजूर कर संविधान-सभा में जाने के फैसले का यह मतलब नहीं कि कांग्रेस ने उसकी सम्पूर्ण योजना को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है।
यह एक रहस्य है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्पष्ट फैसले के बाद संशय उपजाने वाला यह वक्तव्य किस दबाव में और क्यों जारी किया गया। जो भी हो, इस बयान से कांग्रेस के भीतर और नेहरू के मन में चल रही भारी दुविधा जगजाहिर हो गई। इस वक्तव्य के बाद कांग्रेस के इरादों को संदिग्ध घोषित करते हुए लीग ने भी कैबिनेट मिशन के लिए अपनी मंजूरी वापिस ले ली। इसी के साथ आज़ाद भारत के एकजुट रहने की उम्मीद लगभग ख़त्म हो गई थी। हालाँकि कोशिशें अन्त-अन्त तक चलती रहीं।
विभाजन के दस्तावेजों को देखने से पता चलता है कि लीग और कांग्रेस के बीच सबसे बड़ी फाँस प्रान्तों के अनिवार्य समूहीकरण के बारे में थी। कांग्रेस को लगता था कि यह प्रान्तीय स्वायत्तता का निषेध है। प्रान्तों के पास अपना समूह चुनने का विकल्प होना चाहिए। उसे उम्मीद थी कि अब्दुल गफ़्फार ख़ान का उत्तर पश्चिम सरहदी प्रान्त किसी मुस्लिम समूह का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। असम से भी यही उम्मीद थी।
उधर लीग कांग्रेस से यह गारंटी चाहती थी कि अनिवार्य समूहीकरण से छेड़छाड़ न की जाए। उसे डर था कि प्रान्तीय स्वायत्तता का नारा मुस्लिम बहुमत के इलाकों में मुस्लिम स्वायत्तता को कमज़ोर करने के लिए लगाया जा रहा है।
समय की दूरी का लाभ उठाकर आज कोई कह सकता है कि अगर लीग ने स्वतन्त्र पाकिस्तान की माँग से पीछे हटने का साहस दिखाया तो कांग्रेस भी समूहीकरण के मुद्दे पर कुछ लचीलापन दिखा सकती थी। आख़िर दस साल बाद समूची व्यवस्था पर पुनर्विचार होना ही था। जो प्रान्त अपने समूह से अलग होना चाहते, दस साल बाद हो जाते। देश का बँटवारा तो न होता।
उन्माद के उस दौर के निकल जाने के बाद शायद विभाजन की बात टल ही जाती। आख़िर जिस कलकत्ते ने ‘सीधी कार्रवाई’ के दिन उस दौर का सबसे वीभत्स जनसंहार देखा था, वहीं एक साल बाद शान्ति के फूल खिल रहे थे। वह भी ऐन विभाजन के दिन, जब समूचे उत्तर भारत में हिंसा की आग तेज़ हो गई थी। जब सीधी कार्रवाई दिवस के और भी भयानक दुहराव की पूरी आशंका थी! इसी को ‘कलकत्ते का चमत्कार’ कहते हैं।
इस चमत्कार के प्रणेता महात्मा गांधी थे। और इस काम में उनके सहयोगी थे, बंगाल के ‘प्रधानमंत्री’ सुहरावर्दी। वही सुहरावर्दी, जिन्हें पिछले साल की हिंसा का सूत्रधार समझा जाता था। कलकत्ते में, और उसके बाद दिल्ली में, जो चमत्कार हुआ, वह राष्ट्रीय स्तर पर न होता, यह कौन कह सकता है!
कम-से-कम गांधीजी को यह उम्मीद थी। विभाजन को विफल करने का उनका यही तरीका था। दिल्ली में शान्ति-स्थापना के लिए किए गए मृत्युपर्यन्त उपवास के समापन के दिन उन्होंने पंजाब और फिर लाहौर जाने की घोषणा कर दी थी। अगर हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे को मारना बन्द कर देते, तो विभाजन अपने आप अप्रासंगिक हो जाता। दिलों का बँटवारा ख़त्म हो जाए तो नक़्शे पर कब तक टिका रहेगा! गांधीजी का बाकी मिशन यही था।
गांधी जी को मारी गई गोली उनके इसी मिशन पर चलाई गई थी! हत्यारी गोली के सिवा कोई और ताकत उन्हें रोक न सकती थी। गोली ने अपना काम किया। दिलों का बँटवारा ख़त्म करने का गांधीजी का मिशन वहीं रुक गया। विभाजन की राजनीति धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई।
विभाजन अवश्यंभावी नहीं था
भारत का विभाजन अवश्यम्भावी हरगिज नहीं था। लेकिन यह दो-एक वर्षों के साम्प्रदायिक उन्माद का नतीजा भी नहीं था। विभाजन की त्रासदी के बारे में केवल एक बात बिना किन्तु-परन्तु के कही जा सकती है। स्वाधीनता संग्राम के सभी नेतागण इस विषय में या तो गहरी दुविधा के या अन्तर्विरोधी विचारों के शिकार थे।
इस दुविधा की सबसे हैरतअंगेज झलक ‘फ्रीडम ऐट मिडनाइट’ के प्रसिद्ध लेखक लैरी कॉलिन्स और डोमिनिक लापियर द्वारा लिए गए लार्ड माउंटबेटन के एक इंटरव्यू से मिलती है। इस इंटरव्यू में माउंटबेटन ने विभाजन का ठीकरा सबसे ज़्यादा जिन्ना और फिर सरदार पटेल के माथे फोड़ने की कोशिश की है।
माउंटबेटन ने कहा है कि उन्होंने आख़िरी दम तक भारत को एक रखने के लिए जिन्ना को मनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आख़िर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर बना तो बँटवारा पंजाब और बंगाल का भी होगा। इन प्रान्तों के हिन्दूबहुल इलाके पाकिस्तान को नहीं दिए जा सकते। जिन्ना शुरुआत में इस ‘घुन खाए’ पाकिस्तान के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उन्हें बता दिया गया कि और कोई विकल्प नहीं है। माउंटबेटन कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, कांग्रेस को और सिखों को विभाजन की अपनी योजना के लिए राजी किया। सबके राजी हो जाने के बाद उन्होंने फिर जिन्ना से पूछा। लेकिन जिन्ना ने साफ मना कर दिया: ‘मुझे मुस्लिम लीग की कौंसिल में बात रखनी होगी। उनकी इजाज़त के बगै़र मैं हामी नहीं भर सकता। इसमें कम से कम एक हफ़्ता लगेगा।’
माउंटबेटन सकते में आ गए। पटेल, नेहरू और गांधी को विभाजन के लिए राजी करने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। बहुत दिमाग़ लड़ाया था। और जब हर कोई जिन्ना की माँग पर राजी हो गया था, यह शख़्स टालमटोल कर रहा था।
माउंटबेटन ने बहुत दबाव बनाया। ललचाया। डराया। धमकाया। आपको हद से हद कल सुबह आठ बजे तक का वक़्त मिल सकता है। अगर आपने देरी की, कांग्रेस नेता बिदक जाएँगे। फिर कभी आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा। पर जिन्ना टस से मस नहीं हुए। जो होना है, होने दीजिए। लेकिन इस तरह औचक कोई फैसला नहीं होगा। जो भी होगा एक उचित और वैध प्रक्रिया के तहत होगा।
आख़िर माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखा। कल एक मीटिंग होगी, जिसमें मैं सबको बताऊँगा कि कांग्रेस पार्टी और सिख समुदाय के लोग विभाजन की मेरी योजना के लिए राजी हो गए हैं। कल रात जिन्ना साहेब से भी मेरी बातचीत तफ़सील से हुई है। उन्हें भी लगता है कि यह एक पूर्ण स्वीकार्य योजना है। इतना कह कर मैं आपकी तरफ देखूँगा। आप बस अपना सर सहमति में हिला देना। आपको कुछ बोलना नहीं है। सिर्फ़ सर हिला देना है। अगर आपने इनकार में सर हिलाया, तो फिर पाकिस्तान को भूल जाना। और मेरी तरफ से चूल्हे भाड़ में जाना।
माउंटबेटन ने कहा कि ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने ऐसा तनाव नहीं महसूस किया था। कल इस जिद्दी इंसान का सर ऊपर-नीचे हिलेगा या दाएँ-बाएँ। उस सर की इतनी-सी हरकत से, बकौल माउंटबेटन, इस महादेश की किस्मत तय होनेवाली थी।
अगले दिन मीटिंग शुरू हुई। योजनानुसार सारी बातें कह चुकने के बाद आख़िरी वायसराय ने तयशुदा मौके पर जिन्ना की तरफ देखा। जिन्ना का चेहरा बिलकुल भावशून्य था। उनका सर हिला ज़रूर, लेकिन इस तरह कि न उसे सहमति कह सकते थे, न असहमति!
चूँकि यह स्पष्ट इनकार नहीं था, इसलिए इसे सहमति मान लिया गया। यों हिन्दुतान की नियति के साथ एक समझौता सम्पन्न हुआ!
माउंटबेटन का दावा है कि सर की इस अबूझ-सी हरकत ने करोड़ों हिन्दुस्तानियों-पाकिस्तानियों के सर पर अनंत काल के लिए विभाजन की त्रासदी का बोझ डाल दिया।
क्या इस विवरण के आधार पर माना जा सकता है कि वायसराय का यह दावा सही है कि विभाजन के लिए मुख्य रूप से जिन्ना ही ज़िम्मेदार थे?
कोई कुछ भी माने, लेकिन इस विवरण से खुद माउंटबेटन की भूमिका बहुत साफ हो जाती है। विभाजन के लिए सबको राजी करने का काम खुद वायसराय ने किया। इस काम में उन्होंने अपनी सारी शक्ति और मेधा, जितनी उनके पास थी, झोंक दी। इसी इंटरव्यू में वे अपनी इस प्रतिभा की प्रशंसा करने से भी नहीं चूकते। प्रतिभा से ज़्यादा उनके पास ‘राज’ का बल था। भारत के बँटवारे का मुख्य श्रेय उन्हें और उनके ब्रिटिश राज के सिवा किसी और को दिया जाए, यह इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी होगी।
आख़िरी वायसराय का एक ही मकसद था। भारत से निकल भागना, जितनी जल्दी हो सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने तो सत्ता-हस्तान्तरण के लिए 30 जून, 1948 तक समय तय किया था। इसे लगभग साल-भर पहले ही, 15 अगस्त 1947 तक, निपटा देने का फैसला पूरी तरह वायसराय का था।
विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक कमर टूट चुकी थी। लेकिन दो सदियों से ब्रिटिश साम्राज्य की ऊर्जा का अक्षय स्रोत भारत अचानक एक असह्य बोझ क्यों बन गया? इसलिए कि बग़ावतें समन्दर से सड़क तक फैल गई थीं। मुश्किल यह थी कि सेना, पुलिस, रेल और डाक जैसे साम्राज्य को थाम कर रखने वाले सभी मज़बूत स्तम्भ इस बग़ावत में शामिल हो गए थे। उन्हें सड़क पर मज़दूरों और नौजवानों का भरपूर सक्रिय समर्थन मिल रहा था। इसलिए इस विद्रोह को सँभालना असम्भव हो चुका था।
भलाई जल्दी-से-जल्दी भाग लेने में ही थी। सत्ता हस्तान्तरण के लिए कोई एकल केन्द्र मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो दो, तीन या सैकड़ों टुकड़े सही। बीस लाख दहशतनाक मौतें और दो करोड़ लोगों की बेघरबारी सही। आपराधिक औपनिवेशिक लापरवाही और क्रूरता की ऐसी दूसरी मिसाल खोजना मुश्किल है।
अगर भारत को ब्रिटिश मुकुट की प्रभाव-छाया में रहना मंजूर हो तो भले एकजुट रहे, लेकिन अगर उसके कम्युनिज़्म के रास्ते पर चल पड़ने का ख़तरा हो तो उसका टूट-फूट जाना ही अच्छा। युद्धोत्तर विश्व में सोवियत संघ की बगल में एक और शक्तिशाली समाजवादी देश कैसे सहन किया जा सकता था!
इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत से पलायन करते समय ब्रिटिश साम्राज्य ने हद दर्जे के स्वार्थीपन और अकल्पनीय क्षुद्रता का परिचय दिया। ब्रिटेन ने सब कुछ भारत का दोहन करके ही पाया था। वह औद्योगिक क्रान्ति, जो इंग्लैण्ड से शुरू हुई और जिसने पश्चिम को ‘विकास’ की चोटी पर पहुँचा दिया, भारत के उत्कृष्ट कपास की देन थी। इस कपास को खपाने के लिए ही सूती मिलों की खोज हुई। भारतीय किसानों के ख़ून-पसीने से चमक रही बर्तानवी सूती मिलों का मुकाबला करने के लिए ही गांधी जी ने अपने चरखे की खोज की थी।
लीग और कांग्रेस के समझौते में ऐसी भी कोई असम्भव बाधा नहीं थी। अगर कुछ और समय मिलता तो कामगारों, मज़दूरों और नौजवानों के आन्दोलनों के दबाव में उन्हें समझौता करना ही पड़ता। लेकिन इस सूरत में कांग्रेस और लीग के नवपूँजीवादी और सामन्ती तत्वों को राष्ट्रीय नेतृत्व में मज़दूरों-कामगारों को भी जगह देनी पड़ती। यही वह सम्भावना थी जिससे उपनिवेशियों के साथ-साथ कांग्रेस और लीग का नेतृत्व भी भयभीत था। पाकिस्तानी इतिहासकार लाल ख़ान ने अपनी पुस्तक ‘पार्टीशन, कैन इट बी अनडन?’ में इस थियरी को विस्तृत सबूतों और मज़बूत तर्कों के साथ पेश किया है।
साम्राज्य के थके हुए सिपाही हांगकांग से मिस्र तक बेहतर मुआवजे के लिए आन्दोलन और हड़ताल पर उतारू थे। इधर सन पैंतालीस के नवम्बर-दिसम्बर में भारत में आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों के ख़िलाफ़ लाल किले में चले कोर्ट मार्शल के मुकदमे ने समूचे उपमहाद्वीप को बग़ावत के जज़्बे से भर दिया था। ‘लाल किले से आई आवाज़: सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज’―यह नारा भारतीय युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुका था। संयोगवश कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे पहले तीन सेनानियों में एक हिन्दू था, एक सिख और एक मुसलमान। अगले दौर में कोर्ट मार्शल का सामना करने वालों में अब्दुल राशिद, सिंघारा सिंह, फतेह ख़ान और कैप्टन मुनव्वर ख़ान थे।
इन मुकदमों और उनके विरोध की गूँज देश में ही नहीं, दुनिया-भर में सुनाई पड़ी। इन्ही मुकदमों के दौरान यह सिद्धान्त स्थापित हुआ कि देश की आज़ादी के लिए लड़ना गु़लाम देशों के नागरिकों का वैध और ज़रूरी अधिकार है। आज़ादी, एकता और इंकलाब के इसी माहौल में फरवरी के आते-आते भारतीय नौसेना में बग़ावत फूट पड़ी। यही बग़ावत मुम्बई से शुरू हुई, लेकिन 48 घंटों के भीतर कलकत्ता, कराची, मद्रास, कोचीन और विशाखापत्तनम तक फैल गई। नौसैनिक जहाजों से यूनियन जैक उतार फेंका गया।

नौसैनिकों के इस अपूर्व विद्रोह में कई अनोखी बातें हुईं। कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर मुम्बई के मज़दूर और नौजवान हज़ारों की तादाद में नौसैनिकों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। नौसैनिकों ने जहाजों पर एक साथ तीन झंडे लहराए। कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। उन्होंने नौसैनिक एम. एस. ख़ान को अध्यक्ष और मदन सिंह को उपाध्यक्ष के रूप में चुना।
सरकार की दमनकारी कार्रवाई में मुम्बई की सड़कों पर मज़दूरों और सैनिकों का ख़ून साथ-साथ बहा। सिर्फ़ 22 और 23 फरवरी को शहीद होने वाले मज़दूरों और सैनिकों की संख्या 250 तक पहुँच गई। एम. एस. ख़ान ने एक यादगार भाषण में कहा: ‘हमारी हड़ताल हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक ऐतिहासिक घटना है। पहली बार एक समान उद्देश्य के लिए सैनिकों और नागरिकों का ख़ून एक साथ बहा है। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद!’
बग़ावतों का सिलसिला बढ़ता गया। मार्च-अप्रैल में देश-भर में पुलिसकर्मियों की व्यापक हड़तालें शुरू हो गईं। मई में उत्तर-पश्चिमी रेलवे के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। जुलाई में एक लाख डाक कर्मचारी हड़ताल पर थे। देश-भर में बग़ावतों, हड़तालों और विरोध-प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। इन बग़ावतों में कहीं कोई साम्प्रदायिक दरार नहीं थी। 1857 में जिस तरह हिन्दू-मुसलमान एक साथ लड़े थे, उसी तरह 1946 में भी एक साथ सड़कों पर थे।
इन बग़ावतों को संगठित करने और कर्मचारियों के समर्थन में किसानों और मज़दूरों को लामबंद करने में कम्युनिस्ट पार्टी की अग्रणी भूमिका थी। कांग्रेस और लीग के अग्रणी नेताओं ने इन आन्दोलनों का समर्थन करने से इंकार कर दिया।
विभाजन के प्रचलित आख्यानों में इस इतिहास को याद नहीं रखा जाता। इसे न अंग्रेज़ याद करना चाहते हैं, न भारत और पाकिस्तान के ‘राष्ट्रवादी’ इतिहासकार। न कांग्रेस याद रखना चाहती है, न मुस्लिम लीग। इस इतिहास को याद रखने पर यह थियरी भरभराकर गिर न जाएगी कि अंग्रेज़ी राज के आख़िरी वर्षों में हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के ख़ून के इस कदर प्यासे हो रहे थे कि बँटवारे को मंजूर करने के सिवा कोई चारा ही न था!
यह सच है कि विभाजन और उसके आगे-पीछे के वर्षों में साम्प्रदायिक हिंसा उन्माद और बर्बरता की सारी सीमाएँ पार कर गई। लेकिन नए शोध से पता चल रहा है कि इनमें अधिकतर मामले ऐसे नहीं थे, जिन्हें भीड़ की स्वतःस्फूर्त हिंसा के दायरे में रखा जा सके। अक्सर संगठित और प्रशिक्षित सशस्त्र समूह इन हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे। ये समूह सीधे तौर पर साम्प्रदायिक राजनीतिक पार्टियों और संगठनों से जुड़े हुए थे। उनके बगै़र यह हिंसा इतनी व्यापक और दीर्घजीवी न हो सकती थी।
एक दूसरा पहलू यह था कि ब्रिटिश सरकार हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सेना का उपयोग करने से बच रही थी। देश को विभाजन की आग में झोंक देने के बाद लोगों की जान-माल की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता नहीं रह गई थी। उन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र खुद सेना को साम्प्रदायिक तनाव से बचाने, सैनिक संसाधनों की रक्षा करने, टुकड़ियों का बँटवारा करने और उन्हें स्थानान्तरित करने की थी।
यह भी मालूम है कि साम्प्रदायिक पार्टियों और समूहों द्वारा अक्सर युद्ध से लौटे और घरों पर बेकार बैठे प्रशिक्षित सैनिकों की मदद भी ली गई। सन 1939 में हिन्दुस्तानियों से सलाह-मशविरा किए बगै़र भारत को युद्ध में झोंक देने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे।
इस अवसर का लाभ उठाते हुए बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सरहदी प्रान्त में मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा ने गठबन्धन सरकारें बनाईं। युद्ध में सरकार का भरपूर सहयोग किया। इस सहयोग का एक रूप सेना में भारी संख्या में अपने समर्थकों की भर्ती कराना भी था। सावरकर ने तो घोषित कर दिया था कि युद्ध हिन्दू लड़ाकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने का उत्तम अवसर है, जिसका लाभ उठाया जाना चाहिए। यह आह्वान सावरकर ने 25 मई, 1941 के अपने जन्मदिन-सन्देश में किया था। इसी सन्देश में उन्होंने ‘राजनीति के हिन्दूकरण’ और ‘हिन्दुओं के सैन्यीकरण’ का प्रसिद्ध नारा भी दिया था। मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा द्वारा लाखों की संख्या में भर्ती किए गए इन सैनिकों की विभाजन के दंगों में क्या भूमिका थी, इस पर विस्तृत शोध की आवश्यकता है।
सन् छियालीस के इन आन्दोलनों और जन-विद्रोहों में एक नए तरह की जुझारू राष्ट्रीयता, मज़बूत हिन्दू-मुस्लिम एकता, कामगार-नागरिक सहयोग और वास्तविक आज़ादी की आकांक्षा उभर कर सामने आई। इस समग्र परिदृश्य को ध्यान में रखे बगै़र सत्ता-हस्तान्तरण में अंग्रेज़ों के साथ-साथ कांग्रेस और लीग की उस ऐतिहासिक हड़बड़ी की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसने विभाजन को अपरिहार्य बना दिया था। यह सिर्फ़ ‘सत्ता का लालच’ नहीं था, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है। लगभग चौथाई सदी से जूझ रहे नेतागण क्या दो-चार साल और इन्तज़ार न कर सकते थे? असली डर नेतृत्व के मज़दूर वर्ग की तरफ खिसक जाने का था।
पटेल विभाजन के माउंटबेटन-प्रस्ताव पर राजी होने वाले पहले भारतीय नेता थे। वे इस प्रस्ताव की घोषणा के समय भी माउंटबेटन के साथ थे। 14 जून, 1947 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की उस बैठक की अध्यक्षता भी पटेल ने ही की थी जिसमें विभाजन की योजना को मंजूरी दी गई थी। माउंटबेटन पटेल की उपमा अखरोट से दिया करते थे, जिसका छिलका बहुत कठोर होता है, गरी मुलायम होती है।
यही सरदार पटेल पहले विभाजन को नामंजूर करने वाली कैबिनेट मिशन योजना के लिए भी सबसे अधिक उत्साहित थे। माना जाता है कि अंतरिम सरकार के गृहमंत्री के रूप में पटेल लीगी वित्तमंत्री लियाकत अली ख़ान की अड़ंगेबाज़ियों के कारण इस नतीजे पर पहुँच चुके थे कि कांग्रेस और लीग का मिल-जुलकर काम करना नामुमकिन है।
यह वक्तव्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उस बैठक में दिया गया था, जिसमें विभाजन के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी।
अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कहा: ‘यह बात हमें पसन्द हो या नापसन्द, लेकिन पंजाब और बंगाल में वास्तव में (de facto) पाकिस्तान मौजूद है। इस सूरत में मैं एक कानूनी (de jure) पाकिस्तान अधिक पसन्द करूँगा, जो लीग को अधिक ज़िम्मेदार बनाएगा। आज़ादी आ रही है। 75 से 80 प्रतिशत भारत हमारे पास है। इसे हम अपनी मेधा से मज़बूत बनाएँगे। लीग देश के बचे हुए हिस्से का विकास कर सकती है।’
यह देखना कम हैरतअंगेज नहीं है कि सरदार केवल पाकिस्तान के प्रस्ताव को ही नहीं, एक तरह से उसके पीछे की ‘टू नेशन थियरी’ को भी मंजूर करते लग रहे हैं। और भी हैरतअंगेज यह देखना है कि बँटवारे की बात इस तरह की जा रही है जैसे मातृभूमि नहीं, कोई जागीर बँट रही हो। हम अपने अस्सी फीसद को सँभालेंगे, बाकी का जो करना हो, लीग करे!
एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुल चार सौ सदस्य थे, जिनमें उस दिन की ऐतिहासिक मीटिंग में केवल 218 मौजूद थे। इनमें से 29 सदस्यों ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया। 30 सदस्यों ने ‘ऐब्स्टेन’ किया, और 159 ने प्रस्ताव का समर्थन किया। यानी कुल सदस्यों के केवल 40 प्रतिशत के समर्थन से देश बँट गया।
प्रस्ताव के समर्थन में महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के वोट भी थे, जिन्हें मनाने का काम, जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं, सरदार ने किया था। मौलाना खुद ‘ऐब्स्टेन’ करने वालों में थे, जबकि ख़ान अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान ने विरोध में वोट डाला था!
हज़ार वर्षों से एक साथ रहकर हिन्दुओं और मुसलमानों ने भारत में एक बहुआयामी बहुस्तरीय सभ्यता का निर्माण किया था। फिर भी सन चालीस में जिन्ना महसूस करने लगे थे कि हिन्दू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। सन सैंतालीस में सरदार पटेल भी ऐसा ही महसूस करने लगे थे। लेकिन मज़दूरों, किसानों और विद्रोही सिपाहियों ने ऐसा कभी महसूस नहीं किया।
ज़ाहिर है कि अगर कभी इस महाद्वीप की राजनीति पर मज़दूरों और किसानों का नेतृत्व कायम हुआ तो विभाजन की राजनीति और उसके ज्ञान-तन्त्र के अन्त की शुरुआत हो जाएगी।
वो सुबह कभी तो आएगी
आज विभाजन को याद करने का मतलब क्या है?
क्या दस से बीस लाख अनुमानित मौतों को याद करना? यह याद करना कि यह संख्या 1857 के महाविद्रोह के या वियतनाम युद्ध के दौरान हुई कुल मौतों के लगभग दोगुनी है? और फ़्रांसीसी क्रान्ति के दौरान हुई मौतों के लगभग बराबर है? क्या यह लगभग एक लाख महिलाओं के साथ हुए जघन्यतम यौन अत्याचारों को याद करना है?
क्या यह त्रिशूलों पर नचाए गए दुधमुँहे बच्चों और तलवारों से चीरे गए गर्भों को याद करना है? क्या यह लाशों से भरी रेलगाड़ियों को याद करना है? क्या यह सब कुछ गँवाकर देश-देशान्तर भटकते घायल, भूखे, असहाय लोगों के विराट काफ़िलों को याद करना है, जिनमें सबसे बड़े काफ़िले में लगभग चार लाख लोग शामिल थे?
क्या यह तीन भारत-पाकिस्तान युद्धों, कारगिल संघर्ष, बांग्लादेश युद्ध और सीमा पर लगातार जारी झड़पों को याद करना है? क्या यह कश्मीर की अन्तहीन समस्या और एक लाख से अधिक नागरिक-सैनिक मौतों को याद करना है? क्या यह बेरहम साम्प्रदायिक दंगों में हुई लाखों मौतों को याद करना है? क्या यह पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों के सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्मूलन को याद करना है?
क्या यह भारत के मुसलमान अल्पसंख्यकों के हाशियाकरण और कथित गोरक्षकों के आतंक को याद करना है? क्या यह इस बात को याद करना है कि विभाजन की सभ्यता-परिवर्तनकारी हिंसा में कमी आना तो दूर, यह निरन्तर और अधिक भीषण आयाम ग्रहण करती जा रही है?
क्या यह इस बात को याद करना है कि विभाजन की प्रक्रिया न केवल जारी है, बल्कि वह आगे और रफ़्तार पकड़ती जा रही है? और यह कि अगर इसे थामा न गया तो यह भारतीय सभ्यता के सम्पूर्ण विनाश से कम पर रुकने वाली नहीं है?
दरअसल, विभाजन को याद करने का मतलब इससे कहीं अधिक गहरा है। हम जिस क्षति और क्षति-बोध की बात कर रहे हैं, उसकी साफ पहचान भारत और पाकिस्तान के अतीत, वर्तमान और उसकी नियति से मिलती है।
भारत और पाकिस्तान दोनों विभाजन की आधी रात की सन्तानें हैं।
हम भारत के लोगों को यह खुशफहमी रहती आई है कि भारत की नियति कभी पाकिस्तान जैसी नहीं हो सकती। भारत उस भारतीय संस्कृति या हिन्दुस्तानी तहजीब का सीधा वारिस है। अलग होकर पाकिस्तान इस तहजीब से छिटक गया। इस अलगाव के सब दुष्परिणाम अकेले पाकिस्तान को झेलने हैं। आज का भारत मूल भारत है। इसकी सभ्यता और संस्कृति विभाजन के बावजूद अक्षुण्ण है। हमारे साथ कोई सभ्यतामूलक संकट नहीं है।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों और दशकों की घटनाओं ने इस विश्वास को गहरा झटका दिया है। धीरे-धीरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य में पाकिस्तानी सियासत का पसमंजर दिखाई देने लगा है। धर्म और राजनीति का वही घालमेल यहाँ भी बनने लगा है। वहाँ इस्लाम ख़तरे में रहता आया है, यहाँ हिंदुत्व संकट में पड़ गया है। वहाँ फौजी हुकूमतें काबिज रही हैं, यहाँ फौज अचानक राजनीति का केन्द्रबिन्दु बन चली है। आन्तरिक मामलों में भी सेना को खुली छूट देने का विचार न केवल स्वीकार कर लिया गया है, बल्कि वह सबसे लोकप्रिय शासन-सिद्धान्त बन गया है।
न्यायपालिका, चुनाव आयोग और दीगर संवैधानिक संस्थाओं की स्वतन्त्रता और स्वायत्तता पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। मीडिया के पालतूकरण के मामले में भारत पकिस्तान से आगे निकल चुका है। जिस तरह वहाँ ज्ञान-विज्ञान का इस्लामीकरण हुआ है, उसी तरह यहाँ भी शिक्षा और विज्ञान का हिन्दूकरण करने का प्रयत्न जारी है।
पाकिस्तान के बारे में एकमत से यह बात कही जाती है कि वह पहचान के संकट का शिकार देश है। बाहर के ही नहीं, पाकिस्तान के लेखक भी यही कहते हैं।
भारत के सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा होने के नाते पाकिस्तान की सांस्कृतिक पहचान भारतीय संस्कृति से भिन्न नहीं हो सकती। मगर यह बात पाकिस्तान के अस्तित्व के मूल तर्क के विपरीत है। मजबूरन पाकिस्तानी हुकूमत को इस्लामी पहचान का सहारा लेना पड़ा। जिन्ना के तसव्वुर के सेक्युलर पाकिस्तान को धीरे-धीरे इस्लामिक रिपब्लिक का चोला धारण करना पड़ा। यह इस्लामिक चोला आज पाकिस्तान में लोकतंत्र और सेक्युलर आधुनिकता की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है।
पहचान के इस सभ्यतामूलक संकट का गहरा साया भारत के ऊपर भी मँडराता रहा है, भले ही हम उसे देखने से इनकार करते रहे हों।
विभाजन का सम्भव होना ही भारत की प्रसिद्ध गंगा-जमुनी तहजीब और बहुलात्म संस्कृति पर प्रश्नचिह्न लगाने वाली घटना थी। भारतीय सभ्यता की बहुलात्मता का विध्वंस उसके सभी वारिसों की साझा क्षति है, किसी एक हिस्से की नहीं।
विभाजित भारत हमेशा इस प्रश्न से जूझता रहा है कि क्या अब भी वह अपनी साझा विरासत का दावा कर सकता है अथवा अब उसे मुस्लिम पाकिस्तान की तर्ज़ पर एक हिन्दू भारत हो जाना चाहिए? पिछले सत्तर वर्षों में भारतीय राजनीति इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती रही है।
पिछले कुछ दशकों में इस प्रश्न के पूर्वपक्ष को उत्तरपक्ष के सामने क्रमशः समर्पण करते देखा गया है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस से शुरू हुई यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के पूर्ण बहुमत और सत्तारोहण के साथ अपना एक चरण पूरा कर चुकी है।
लेकिन हिन्दू भारत का बनना मुस्लिम पाकिस्तान के बनने की तरह ही भारतीयता के मूल तर्क का अन्यथाकरण है। हिन्दू भारत का बनना कठिन तो है ही, अगर किसी तरह वो बन भी जाए तो उसे भारतीयता की विरासत का दावा उसी तरह छोड़ देना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा है।
भारतीयता की इस विरासत की क्षति का अर्थ है समन्वय और सहजीवन के सबसे अनूठे प्रयोग का अन्त। उस सृजनात्मक सभ्यतागत प्रक्रिया का अन्त जिसने भारतीय चमत्कार का निर्माण किया।
जैसे पाकिस्तान मुसलमान बन कर अस्मिता और अस्तित्व के अपने संकट को हल नहीं कर पाया, भारत भी हिन्दू बनकर नहीं कर पाएगा।
इस संकट से पार पाने का इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं कि विभाजन और उसकी ऐतिहासिक परिणतियों की तरफ से आँखें मूँद कर रखने की शुतुरमुर्गी चाल छोड़ी जाए। विभाजन के क्षतिबोध को याद किया जाए और क्षतिपूर्ति की दिशा में कदम उठाए जाएँ।
‘आलोचना’ का यह अंक इस दिशा में एक छोटी-सी कोशिश है।
इस अंक में प्रकाशित लेखों में दृष्टियों, सिद्धान्तों और विचारों की विविधता है। यहाँ सहमति की सुरम्यता की जगह असहमति की आकुलता अधिक मिलेगी। यह ‘विभाजन के सत्तर साल’ पर ‘आलोचना’ के दो अंकों की योजना का पहला अंक है।
‘आलोचना’ के इस अंक के साथ इस पत्रिका के सम्पादन की ज़िम्मेदारी संजीव कुमार को और मुझे संयुक्त रूप से दी गई है। प्रधान सम्पादक नामवर सिंह के निर्देशन में हम दोनों ‘आलोचना’ की परम्परा और संस्कृति का निर्वाह करने के कठिन काम में ‘आलोचना’ के सभी पाठकों और लेखकों के सहयोग और शुभेच्छा के तलबगार हैं।
(आलोचना के सहस्त्राब्दी अंक-59; जनवरी-मार्च 2019 में प्रकाशित आशुतोष कुमार का संपादकीय)