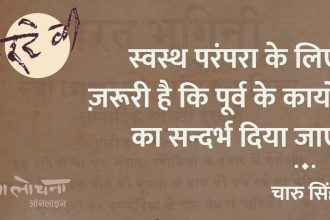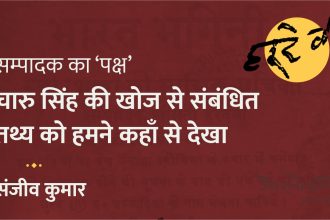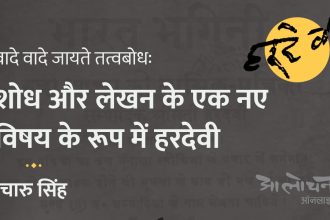हमारे साहित्य और जीवन की जिन सामयिक और स्थायी आवश्यकताओं ने ‘आलोचना’ का प्रकाशन अनिवार्य बना दिया उनका संक्षेप में निर्धारण यों किया जा सकता है :
आचार्य शुक्ल के पश्चात् हिन्दी-आलोचना ने अपने विकास और मनोविज्ञान का आधार लेकर ‘प्रतीकवाद’ की विचारधाराएँ साहित्यालोचन का दृष्टिकोण बनीं। परन्तु पिछले कई वर्षों से हिन्दी का आलोचना-साहित्य एक अवांछित गतिरोध की स्थिति में पड़कर मनमाने पथों पर भटकता रहा है।
प्रगतिवादी आलोचना ने अपने प्रारंभिक काल में हमारे साहित्यकारों को नई दृष्टि दी और उन्हें अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। आधुनिक हिन्दी साहित्य, विशेषकर छायावादी कविता का नए दृष्टिकोण से मूल्यांकन करते समय प्रगतिवादी आलोचना ने साहित्य के नए वैज्ञानिक मान-मूल्यों का निर्धारण करने की ओर प्रवृत्ति दिखाई और सामाजिक जीवन और संघर्ष के व्यापक प्रश्नों से साहित्य का सम्बन्ध कराने की चेष्टा में उसने अनेक प्रचलित शुद्ध कलावादी, असामाजिक और प्रगतिवादी प्रवृत्तियों और विचारधाराओं से संघर्ष भी किया। प्रगतिवादी आलोचना यदि इसी प्रकार अपने वैज्ञानिक और रचनात्मक पथ पर अग्रसर होती रहती तो सम्भवतः आज की-सी अराजकता न फैली होती। हमारा आलोचना-साहित्य अधिक सम्पूर्ण और उच्च कोटि का होता। अपने साहित्यिक इतिहास और आधुनिक साहित्य का समुचित मूल्यांकन करने के लिए हमने वैज्ञानिक मानदंडों की स्थापना करने में आशातीत सफलता पा ली होती। आज हमारा दृष्टिपथ अपेक्षया अधिक विस्तृत और व्यापक होता। हम अपने साहित्य की विशिष्ट प्राणवन्त परम्परा के उत्तराधिकार को सहेजे, साहित्य के माध्यम से जनसेवा के पथ पर आश्वस्त भाव से आगे बढ़ते होते, और जनजीवन के सामयिक वास्तव को सच्चाई और गहराई से प्रतिबिम्बित करनेवाले श्रेष्ठ कलात्मक साहित्य की रचना के लिए प्रेरणा-केन्द्र बन गए होते।
परन्तु हुआ यह कि प्रगतिवादी आलोचना के क्षेत्र में विकृत समाज-शास्त्रीयता का प्रतिपादन करनेवाली एक नकारात्मक संकीर्ण मतवादी प्रवृत्ति ने अपना अकांड तांडव रचकर ऐसी असैद्धान्तिक और अबुद्धिवादी आलोचना-पद्धति चलाई जिसके आतंक के सामने प्रेरणा और अनुभूति के स्रोत बन्द होने लगे, वस्तु-सत्य की संवेदनशील प्रतिभा के पौधे मुरझाने लगे और साहित्यालोचन के मानदंड इस स्वेच्छाचारी संकीर्ण दृष्टिकोण की वेदी पर बलिदान कर दिए गए इसके विपरीत मनोविज्ञान का आधार लेकर आलोचना क्षेत्र में जो विचारकोण बनाया गया वह अन्ततः साहित्य के सामाजिक प्रयोजनों और दायित्वों को त्यागकर केवल प्रतीकवादी प्रयोगों तक ही सीमित रह गया और साहित्य और समाज के आधारभूत प्रश्नों के प्रति उसकी अभिरुचि एकांगी और आनुषंगिक ही रही। इसके अतिरिक्त प्राचीन अलंकार-ग्रंथों की परिपाटी का अनुसरण करनेवाले आलोचक एक प्रकार से लकीर के फकीर ही बने रहे और उन्होंने आचार्य शुक्ल के समान आधुनिक चेतना और सामाजिक जीवन-वास्तव के अनुकूल उन सिद्धान्तों का नव-संस्कार करने की भी कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति नहीं दिखाई। यहाँ तक कि सत् साहित्य का मूल्यांकन करनेवाली ‘लोक-मंगल’ और ‘लोक रंजन’ की शास्त्रीय कसौटियाँ भी उनके निकट मात्र एक रूढ़, अमूर्त ‘विचार’ बनकर रह गई ऐसे काम्य आदर्श न रहीं जो प्रत्येक युग के सामयिक संघर्ष में जनता का हित-साधन करनेवाली सजग चेतना का ठोस आधार लेकर बदलते और विकास करते जाते हैं और स्वयं ऐतिहासिक सत्य के सारवाही विचारों का मूर्त-सजीव युग-रूप धारण करके साहित्य में मानव मूल्यों और जन-हितों के संरक्षक बनते हैं। आज के संघर्षपूर्ण संक्रान्ति युग में हमारे साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत् का यह गतिरोध तो हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता और प्रगति के मार्ग में और भी बाधा बना हुआ है।
आलोचना इस गतिरोध को तोड़ने का संकल्प लेकर जन्मी है।
साहित्य में पूर्ण मानव की प्रतिष्ठा
‘युगवाणी’ के एक गीत में कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने माँग की है :
आज मनुज को खोज निकालो।
जाति वर्ण संस्कृति समाज से
मूल व्यक्ति को फिर से चालो!
… … …
खंड मनुज को फिर से ढालो!
किन्तु यह एक खेदजनक स्थिति है कि प्रेमचन्द के बाद हिन्दी में जिस साहित्य की सृष्टि हुई है चाहे वह प्रगतिवादियों द्वारा रचा गया हो या प्रतीकवादियों, प्रयोगवादियों, छायावादियों और प्रकृतवादियों द्वारा उसमें हमारे असंख्य अन्तर्विरोधों से ग्रस्त वर्ग-समाज के संघर्षशील मानव के समग्र व्यक्तित्व का चित्रण नहीं हो पाया है। ऊपर से यह रचनाएँ किसी भी विचारधारा से अनुप्रेरित क्यों न हों, उनके अन्तर में एक दृष्टि-साम्य तो मिलता ही है कि उनमें ‘खंड मनुज को फिर से डालने’ या ‘मनुज को खोज निकालने’ की यथार्थवादी प्रवृत्ति का अभाव है। उनमें ऐसे समग्र मानव को ‘खोज निकालने की प्रवृत्ति और स्पर्धा का अभाव है जो हमारी गुलामी, सामन्ती और पूँजीवादी वर्ग-संबन्धों की क्रूरता, अनैतिकता, अन्याय, साम्प्रदायिक द्वेष, अशिक्षा, भुखमरी, चोर बाजारी, महामारी―मनुष्य के व्यक्तित्व को भौतिक और नैतिक अन्धकार में आवेष्टित करके खंड-खंड, विकृत और विकलांग बनानेवाली वर्तमान जीवन की समस्त आधि-व्याधि, दुःख-दैन्य, अनिश्चितता और दुर्निवार कठिनाइयों से पग-पग पर ठोकरें खाकर भी निराश और हताश नहीं है, जो संघर्षों से पराङ्मुख नहीं है, जो युग-पुरुष है, एक ‘टाइप’ है अर्थात् जो सम और विषम परिस्थितियों में पर्याय और सम्भाव्य, व्यष्टि और समष्टि की मार्मिक समन्विति का युगानुरूप जीवन्त प्रतिनिधि है।
प्रतीकवादी या प्रयोगवादी लेखक नए प्रयोगों नवीनता, उक्ति-वैचित्र्य और मनोवैज्ञानिकता के नाम पर साहित्य में मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व के पुनर्निर्माण की समस्या को तिलांजलि देकर उसे और भी एकांगी, असामाजिक और विकृत बनाने में दत्तचित्त रहे हैं और उनमें से कुछ अनेक सत्याभासों की आड़ लेकर साहित्यिक प्रतिक्रियावाद को प्रश्रय देते रहे हैं। इसके विपरीत यशपाल और अश्क़ आदि को छोड़कर अन्य प्रगतिवादी और समाज का यथातथ्य, फोटो-चित्र उपस्थित करनेवाले प्रकृतवादी या तो यथार्थवाद से पथ-भ्रष्ट होकर और अपने को प्रचार-साहित्य की संकीर्ण सीमाओं में बाँधकर सामयिक जीवन-वास्तव को अपने मनचाहे ढंग से ही देखने के आदी रहे हैं या इतिहास की सम्भावनाओं से उसका विच्छेद करके, केवल उसके वर्तमान कुत्सित रूप को ही निःसंग, निष्क्रिय दर्शक की भाँति देखते रहे हैं, अर्थात् जो उसके अन्धकार के ही चित्रकार हैं, इतिहास-क्षितिज पर उगते प्रगति-सूर्य की रश्मियों के नहीं। इस प्रकार यह दोनों प्रवृत्तियों भी मनुष्य के व्यक्तित्व के एकांगी और विकृत रूप को ही पेश करती आई हैं, उसके सम्पूर्ण, सक्रिय मूर्त वास्तविक रूप को नहीं। निस्सन्देह, साहित्य और संस्कृति को सर्व-जन-सुलभ बनानेवाले उत्पादन-साधनों (फिल्म, रेडियो, प्रेस) के उत्तरोत्तर विकास और हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के दबाव से, इस बीच, हमारे देश में साहित्यिक निर्माण में परिमाण-वृद्धि तो अवश्य हुई है, परन्तु महान और स्थायी मूल्य के साहित्य की रचना अपेक्षया बहुत कम हुई है। अन्य क्षेत्रों की ही तरह कला-साहित्य-संस्कृति के क्षेत्र में भी उसके प्रचार-साधनों के संचालकों का उद्देश्य मुनाफा कमाना ही है, जनता को संस्कृत बनाना नहीं, जिससे इस बीच जनता की कलाभिरुचि विकृत और सस्ती हुई है और अपवादों को छोड़कर साहित्य का सामान्य स्तर भी नीचा हुआ है।
ऐसे सर्वव्यापी संकट के समय ‘अज्ञेय’ की तरह इस ह्रास और गतिरोध को, लेखकों के सरकारी नौकरियों में चले जाने या राजनीतिक पार्टियों और विचारधाराओं से सम्बद्ध हो जाने के कारण बताकर हम एक आलोचक के दायित्व से छुटकारा नहीं पा लेना चाहते। हमारे देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों का यह स्वाभाविक परिणाम है कि हमारी राष्ट्रीय भाषाओं के अनेक लेखक और विद्वान सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों में लगेंगे ही, और जब तक भारतीय जनवादी क्रान्ति पूर्णतः सफल नहीं हो जाती, उस समय तक और उसके बाद भी, हमारे अधिकांश लेखक विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में से किसी-न-किसी को अपनाते ही जाएँगे, क्योंकि हमारे साहित्यकार ‘त्रिशंकु’ के वंशज नहीं हैं―सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक जीवन के संघर्ष और पुनर्निर्माण के कार्य से तटस्य ‘कला के लिए कला’-वादी नहीं हैं और सामाजिक दायित्वों को ठुकराकर व्यक्ति की काल्पनिक ‘स्वतन्त्रता’ की घोषणा करनेवाली अहम्मन्यता भी उनमें नहीं है। प्रतिभाएँ अगर मर रही हैं या नई प्रतिभाएँ जन्म नहीं ले रहीं तो इसका कारण केवल लेखकों का ‘सरकारीकरण’ या राजनीति में उनकी सक्रिय रुचि नहीं है। प्रतिभाओं का गला घोंटनेवाले कारणों को समझने के लिए वर्ग-समाज की शूर वास्तविकता की सजग जाँच करनी चाहिए, जिसमें रहकर और जिसके विरुद्ध अविराम संघर्ष करके ही प्रतिभाएँ आज तक उभरी हैं। सरकारी नौकरी में दाखिल होते ही एक ईमानदार और वस्तुनिष्ठ कलाकार के लिए इस संघर्ष का अन्त नहीं हो जाता (कठिनतर चाहे हो जाए)। और राजनीतिक चेतना तो उसे कहीं भी रहकर संघर्ष के लिए नया मनोदल और प्रेरणा ही दे सकती है।
इसी प्रकार शचीरानी गुर्टू की तरह आत्म-प्रवंचना में पड़कर विश्व-साहित्य के अनेक निर्माताओं जैसे ब्राउनिंग, शैली, राबर्ट वर्क्स, क्रिस्टिना रोजेटी, चेखव, मेरीडिय आदि का वर्तमान हिन्दी लेखकों के रूप में एक साथ और एक ही समय ‘पुनर्जन्म’ कराके हम एक आलोचक के दायित्व से छुटकारा नहीं पा लेना चाहते। क्योंकि हकीकत यह है कि इस समय विश्वजनीन प्रतिभाओं की बात तो दूर, पन्त, निराला, यशपाल और राहुल के अतिरिक्त हमारे साहित्य में ऐसी रचनाशील प्रतिभाएँ भी विरल ही हैं जिनका कृतित्व उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी―हमारे देश की अन्य प्रमुख भाषाओं के श्रेष्ठ लेखकों और कवियों के बराबर हो। जो प्रतिभाएँ अखिल भारतीय महत्ता पा गई हों, अर्थात् जिनकी रचनाओं के अन्य भाषाओं में केवल अनुवाद ही न हुए हों, बल्कि जिन्होंने रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरतचन्द्र, इकबाल और प्रेमचन्द की तरह देश की अन्यान्य भाषाओं के साहित्यों को समग्र रूप से प्रभावित किया हो, और उनमें नई साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रतिभाओं को जगाकर उन्हें अपनी प्रान्तीय सीमाओं से बाहर निकलने की प्रेरणा दी हो। ‘अज्ञेय’ की तरह हम निराश नहीं हैं, न संशय और भ्रम के बीज बोने के पक्ष में हैं, और न ही लेखकों को समाज के ‘त्रिशंकु’ बन जाने के लिए प्रोत्साहन देने के हक में हैं। यह साहित्यिक प्रतिक्रिया का मार्ग है।
साथ ही, हम शचीरानी गुर्टू की तरह शिशु-सुलभ विस्मय भावना से प्रत्येक लेखक को विश्व के किसी-न-किसी महान साहित्यकार का ‘अवतारी’ मानकर साहित्य के वर्तमान संकट और गतिरोध से आँख मींच लेने के पक्ष में भी नहीं हैं। यह आत्म-प्रवंचना का मार्ग है।
हिन्दी-साहित्य में इस समय जो भी रचनाएँ हैं या पैदा हो रही हैं―वह जीविकोपार्जन के लिए चाहे जहाँ काम करते हों, और चाहे जिस जनवादी विचारधारा या साहित्यिक आदर्श को मानने वाले हों, उनकी प्रतिभा चाहे जिस कोटि की हो―वही तो हमारे साहित्य की पूँजी हैं―हमारे साहित्य की धारा हैं। मुख्यतः उन्हें ही उन तमाम अवरोधों से लड़ते जाना है जो उनकी प्रतिमा को बेड़ियाँ पहनाते हैं। और साथ ही, उन्हें ही साहित्य में जीवन के वस्तु-सत्य को मूर्त, सम्पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित करने और मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण करने के लिए भगीरथ प्रयत्न करना है तभी हमारा साहित्य अपनी वर्तमान संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर एक विपुल शक्ति बन सकेगा। एक आलोचक की हैसियत से हम अपनी भाषा के सामयिक साहित्य का सही-सही मूल्यांकन करके, उसके स्थायी और अस्थायी मूल्यों और उसके सामाजिक उपलक्ष्यों का विवेचन करने तक ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मानते, बल्कि हम अपने साहित्यकारों में ऐसा मुक्तिकामी और मानववादी संकल्प जगाना भी अपना कर्तव्य समझते हैं जिससे वह अपनी व्यक्तिगत अक्षमताओं और समाजगत कठिनाइयों के बावजूद उस भगीरथ प्रयत्न में ईमानदारी से लग सकें जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है। इस पुनीत कार्य में हम उनके सखा और सहयोगी बनना चाहते हैं।
और इसीलिए आज हम विश्व-साहित्य के अध्ययन का प्रश्न विशेष रूप से उठा रहे हैं। विश्व साहित्य से हमारा तात्पर्य उन महान लेखकों की महाकृतियों (क्लासिक्स) से है जो चाहे जिस देश और काल की पैदावार क्यों न हों, पर जो आज भी अपना मूल्य रखती हैं और सदा अमर रहेंगी और चिरकाल तक मनुष्य जाति को अनुप्राणित करती जाएँगी।
इसमें सन्देह नहीं कि एक आलोचक की हैसियत से हमें इस सम्बन्ध में उठनेवाले अनेक प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर देना है। प्रत्येक देश की जनता को विश्व के अन्यान्य देशों का प्राचीन साहित्य एक सामान्य विरासत के रूप में मिला है। ये महान कृतियाँ उन विचारों पर आधारित हैं और उन वर्गों के प्रतिनिधियों ने उनकी सृष्टि की है जो या तो समाप्त हो गए हैं या जिन्हें हम अपने देश में समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी कृतियाँ आज भी जनता को सचेतन और जागृत बनाने के लिए क्यों मूल्यवान हैं? वह क्यों आज भी हमारे साहित्य की प्रेरणा बनती हैं? यह क्यों आज भी हमारे संकल्प को बल देती हैं, हमारी सौन्दर्य-भावना का परिष्कार करती हैं, उसे गहरा और मानवीय बनाती हैं? वह क्यों हमारी संवेदनशीलता को उभारती हैं और हमारी जिज्ञासा और विवेक को जगाती हैं? उनका साहित्य क्यों सही अर्थों में जन-साहित्य है? यह क्यों हमें आज भी आनन्द देती हैं और आगे चलकर एक वर्गहीन समाज में भी पाठकों को आनन्द देंगी? संक्षेप में इन प्रश्नों का उत्तर देकर ही हम अपने लेखकों और पाठकों के सामने विश्व-साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता का पूरा अहसास करा सकते हैं।
इसमें सन्देह नहीं कि महान लेखकों की रचनाओं में अपने-अपने काल की सामाजिक विचारधाराएँ व्यक्त हुई हैं और उनकी कृतियाँ अपने समय के ऐतिहासिक वास्तव से पूर्णतः सम्बद्ध हैं। लेकिन इन महान लेखकों को किसी शोषक वर्ग के खूँटे से बाँधकर जाँचना व्यर्थ होगा, क्योंकि उनकी रचनाओं में अपने समय का समग्र जीवन, तमाम वर्गों के अन्तःसम्बन्ध प्रतिबिंबित हुए हैं और इस प्रकार उस युग की मूल समस्याओं का उद्घाटन हुआ है। इसी कारण उनकी रचनाओं में शोषण-दोहन की विचारधाराओं के प्रति गहरे प्रतिवाद की मुखर ध्वनि है और आजादी और समानता की विचारधारा के प्रति गहरा मोह है। महान लेखक यथार्थवादी और अपने समय के आलोचक थे। वस्तुतः यह अपने काल के वर्ग-समाज के विद्रोही थे। इसलिए महान लेखक चाहे जिस काल में और चाहे जिस वर्ग में पैदा हुए हों, वह मूलतः मानववादी थे। उनकी महानता का यही रहस्य है कि उन्होंने ‘मनुष्य’ को ही प्रमाण और प्रतिमान माना, जिससे उनकी सहानुभूतियाँ मानव-मात्र तक प्रसरित हुईं―विश्वजनीन बनीं। आज जब वर्ग-समाज का अभिशाप इतना बढ़ गया है कि विराट नरमेधों के आयोजन से शोषक-वर्ग का मुनाफा सौ गुना बढ़ता है, जब जनता की मुसीबतों से उसकी तिजोरियों भरती हैं और जनता के रोदन-चीत्कार से समाज के उन कापालिकों का अट्टहास जगता है―ऐसे समय स्वयं मनुष्य का अध्ययन करना और उसके प्रति आदर-सम्मान का भाव जगाना एक महती आवश्यकता बन गया है। मनुष्य की नैतिक और शारीरिक सुन्दरता और विशिष्टता को और अन्य लोगों के साथ परस्पर सहयोग करके रहने की आवश्यकता को स्वीकार किए बिना आज कोई भी समाज-व्यवस्या प्रगतिशील और जनवादी होने का दावा नहीं कर सकती। शोषण-दोहन, ऊँच-नीच और हत्या कांडों पर जीवित रहनेवाली व्यवस्था अवश्य ही स्थायी नहीं हो सकती। साहित्य की प्राचीन महाकृतियों का यह सबसे बड़ा सन्देश है कि उनमें मानव की प्रतिष्ठा है।
और महाकृतियों के पात्रों के रूप में प्रतिष्ठित मानव खंडित व्यक्तित्व के एकांगी और विकृत मानव नहीं हैं। महाभारत के पात्रों के बारे में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है : “मूल कथानक में जितने भी चरित्र हैं वे अपने-आप में ही पूर्ण हैं। भीष्म-जैसा तेजस्वी और ज्ञानी, कर्ण-जैसा गम्भीर और वदान्य, द्रोण-जैसा योद्धा, बलराम-जैसा फक्कड़, कुन्ती और द्रौपदी-जैसी तेजोद्दप्त नारियाँ, गान्धारी-जैसी पति-परायणा, श्रीकृष्ण-जैसा उपस्थित-बुद्धि और गम्भीर तत्त्वदर्शी, युधिष्ठिर-जैसा सत्यपरायण, भीम-जैसा मस्तमौला, अर्जुन जैसा वीर, विदुर-जैसा नीतिज्ञ चरित्र अन्यत्र दुर्लभ है।” और आगे, “महाभारत का अदना-से-अदना चरित्र भी डरना नहीं जानता। किसी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं पड़ने पाती। पाठक महाभारत पढ़ते समय एक जादू-भरे अरण्य में प्रवेश करता है, जहाँ पग-पग पर विपत्ति है, पर भय नहीं है; जहाँ जीवन की चेष्टाएँ बार-बार असफलता की चट्टान पर टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं, पर चेष्टा करनेवाला हतोत्साह नहीं होता, गलती करनेवाला अपनी गलती पर गर्व करता है, प्रेम करनेवाला अपने प्रेम पर अभिमान करता है और घृणा करनेवाला अपनी घृणा का खुलकर प्रदर्शन करता है। यहाँ सरलता है, दर्प है, तेज है, वीर्य है, महाभारत की नारी अपने नारीत्व पर अभिमान करती है, पुरुष इस अभिमान की रक्षा के लिए अपने को मृत्यु के हाथ सौंप देता है।”
यही बात अन्य भारतीय और इतर भारतीय साहित्यों को महाकृतियों से सिद्ध है कि उनके अदना-से-अदना पात्र (हीरो) दुर्दमनीय साहस से जीवन की विषमताओं और विफलताओं का सामना करते हैं, अविचलित रहकर जीवन के समरांगण में जूझते जाते हैं, विपत्तियों को झेलते हैं, अपने बुद्धि-विवेक और बल से मार्ग की दुर्गम कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। उनकी इस अक्षय जीवट और वीरत्व भावना से हमें आज के कुंठापूर्ण जीवन में एक नई चेतना, नया आत्म-बल और नया ढाँढ़स मिलता है कि प्राचीन युगों में न्याय और नैतिक आदर्शों की स्थापना के लिए उन्हें जितने भयंकर तूफानों के बीच से गुजरना पड़ा था और जितनी वीरता दिखानी पड़ी थी, आज हमें सर्वदा के लिए शोषक-समाज की काल-रात्रि से बाहर निकलकर एक सच्चा मानवीय समाज स्थापित करने के लिए उससे कहीं ज्यादा भयानक तूफानों के बीच से गुजरना पड़ेगा और उनसे अधिक वीरता दिखानी होगी। इसके साथ ही इन संघों में मनुष्य ने जिन नैतिक आदर्शों और मानव-मूल्यों की स्थापना की है, यह जीवन की अन्ततः विजय और प्रगतिशीलता में हमारी आस्था उत्पन्न करते हैं। मानव जाति की जरूरतों और हितों की उपेक्षा करके स्वार्थवश सत्ता प्राप्त करने की चेष्टाएँ सामाजिक जीवन के स्खलन और ह्रास का कारण बनती है। मनुष्यों और देवताओं का असम्मान करने से सामाजिक जीवन विच्छिन्न होता है। बड़े-बड़े साम्राज्य और फलती-फूलती सभ्यताएँ नष्ट हो जाती हैं, यदि समाज के हित का तिरस्कार किया जाता है। यही पाप होता है। विश्व-साहित्य की महाकृतियों की यह सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा है, जो मानवता को आगे बढ़ने के लिए सतत उकसाती रहती है।
और फिर, विश्व-साहित्य की महाकृतियाँ हमारे भीतर मनुष्य-जीवन की ऐतिहासिक परम्परा की अनुभूति कराती हैं। सीता के विलाप, भरत के क्षोभ, लक्ष्मण के क्रोध का प्रसंग पढ़कर हमारे मन में जब वैसी ही सहानुभूत्ति और उद्वेलन होता है, जब हमें यह प्रतीत होता है कि आज हम जो कुछ अनुभव करते हैं, ऐसे ही अवसरों पर प्राचीन काल में अन्य लोगों ने भी अनुभव किया था, और उनका यह अनुभव विलक्षण सौन्दर्य और सूक्ष्म-भेदी सच्चाई के शब्दों में सर्वदा के लिए विजड़ित कर दिया गया है, तो हमें लगता है कि यह हमारी सबसे अधिक मूल्यवान सम्पत्ति है जो मनुष्य के ऐतिहासिक अतीत के साथ हमारी एकता और सम्बन्ध-सूत्रता का भाव जगाकर हमें सौन्दर्यानुभूति कराती है। विश्व हमें अपने वर्तमान गोचर जगत् से कहीं अधिक विशालतर लगने लगता है, साथ ही हम इस युगानुयुगीन विश्व के साथ अत्यधिक सामीप्य का भी अनुभव करते हैं। प्राचीन साहित्य इस प्रकार हमें अपने जीवन की क्षुद्रताओं और संकीर्णताओं से ऊपर उठने में सहायक होता है। और देश-काल की सीमाओं को तोड़कर हमें मनुष्य के समूचे विकास-क्रम की व्यापक धारा का साक्षात्कार कराता है।
ये कतिपय मानव-मूल्य हैं जो हमें विश्व-साहित्य की महान कृतियों के अध्ययन से सहज ही प्राप्त होते हैं, वे कृतियों और हमारी जनता में इस विश्व-संकट के समय शान्ति, आहा और जनवाद के संघर्ष में अन्ततः विजयी होने का विलास जगा सकती हैं, और हमारे साहित्यकारों को पूर्ण मानव-पहिले की सृष्टि करने में योग दे सकती हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विश्व की महान कृतियों ने मनुष्यों के दिमागों को गुलाम नहीं बनाया, उन्हें नया उत्साह और नई प्रेरणाएँ ही से है, क्योंकि महान कलाकार और उनकी कृतियाँ मूलतः कान्तिकारी होती हैं, विज्ञान की ही तरह कला भी मनुष्य की स्वतन्त्रता का अस्त्र है, विश्व-विख्यात मार्क्सवादी आलोचक जार्ज लूकाच के शब्दों में, अतीत के महान लेखकों ने “मानवीय विकास के महान युगों के सर्वांगीण और समुचित चित्र हमें दिए हैं और साथ ही वह आज मनुष्य के अखंडित व्यक्तित्व की पुनर्स्थापना करने के विचार-संघर्ष में हमारे लिए आलोक-दीप का भी काम देते हैं।” इसलिए यदि हमारे साहित्यकार अपने युग की चेतना लेकर विश्व के महान लेखकों की अनुपम कृतियों से सीखेंगे तो निश्चय ही वह आज के जीवन-वास्तव का अधिक व्यापक और मूर्त चित्रण कर पाएँगे और आए दिन के साहित्यिक फैशनों से अभिभूत होकर पथ-भ्रष्ट न होंगे।
अगर हम अपने समय की समस्याओं को हल करने में असफल रहे तो सम्भव है कि इस बार हम ही नहीं, बल्कि महायुद्ध की लपटों में विश्व-मानवता द्वारा अपने रक्त-स्वेद से बनाई हर चीज भस्म हो जाएगी। महाभारत के इतिहास की विश्वव्यापी पुनरावृत्ति समग्र मानव-जीवन, सभ्यता और संस्कृति के लिए भयंकर होगी। साहित्य की प्राचीन महाकृतियाँ जहाँ हमारा मनोरंजन करती हैं, हमारी चेतना का सीमा-विस्तार करती हैं, हमारी मानवता का विकास करती हैं, यहाँ वह हमारे अन्दर केवल यह भाव ही नहीं जगातीं कि मानव-मात्र एक है और उनका इतिहास देश-काल की अनेकरूपता के होते हुए भी प्रगति पथ पर एकोन्मुख हैं, बल्कि वह हमारे अन्दर कर्म की प्रेरणा भी जगाती हैं ताकि हम अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर संघर्ष-क्षेत्र में कूद पड़े और समय रहते हुए प्रतिक्रियावादी शक्तियों को विश्व की शान्ति भंग करने से रोक दें, ताकि हम, आप, संसार के सभी मनुष्य जीवित रह सकें, और अपनी बुद्धि और अपने श्रम से एक स्वतन्त्र, जनवादी समाज का निर्माण कर सकें। साहित्य में पूर्ण-मानव की प्रतिष्ठा का संघर्ष इस व्यापक जीवन-संघर्ष का ही महत्त्वपूर्ण अंग है।
(‘आलोचना’ के प्रथम अंक अक्तूबर, 1951 में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान का सम्पादकीय)