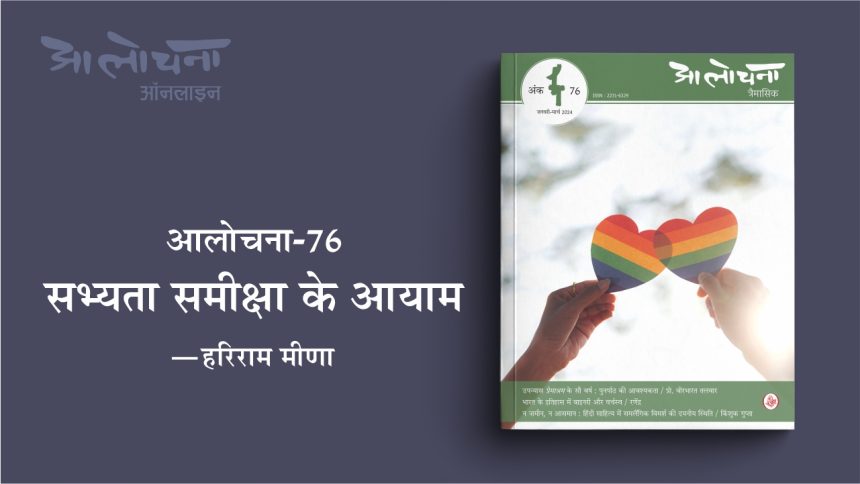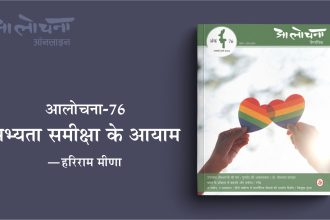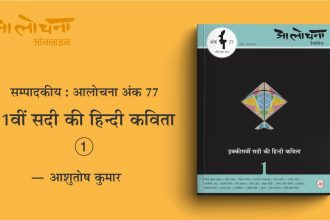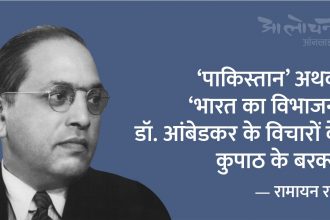राजकमल प्रकाशन की त्रैमासिक पत्रिका ‘आलोचना’ का 76वाँ अंक प्राप्त हुआ। साहित्यिक आयाजनों में बहुराष्ट्रिक निगमों के हस्तक्षेप के कारण तमाशाबाज़ी, कुलीन वर्चस्व और व्यावसायिकता की बढ़ती ख़तरनाक प्रवृत्ति को रेखांकित करने वाले आशुतोष जी के विचारोत्तेजक संपादकीय सहित इस अंक में सम्मिलित समस्त सामग्री अकादमिक रूचि की है, किंतु रणेंद्र का ‘भारत के इतिहास में बाईनरी और वर्चस्व’ एवं (डॉ०) पल्लव का ‘औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध ये ख़त’ लेखों की अपनी विशिष्ट एवं सामयिकता है।
पिछले एक दशक से सत्ता-वैचारिकी भारत की राष्ट्रीयता को कथित ‘हिंदू’ धर्म का जामा पहना कर जोर-शोर से इस प्रचार-प्रसार में लगी हुई है कि भारतीय संस्कृति एक-रेखीय है और इसका आद्यांत उस वैदिक वैचारिकी पर टिका हुआ है जिसे सनातन, ब्राह्मणवाद अथवा हिंदूवाद भी कहा जाने लगा है। यहाँ तक कि वैदिक सभ्यता से बहुत पहले विकसित और उससे सर्वथा भिन्न सिंधु घाटी सभ्यता को भी इसी का हिस्सा सिद्ध करने की जिद की जा रही है। रणेंद्र अपने लेख में इस वर्चस्ववाद का खंडन करते हैं और यह स्थापित करते हैं कि भारतीय संस्कृति की ‘संरचना सम्पूर्ण देश की विभिन्न परंपराओं के योग से बनी है जिसमें हर एक परंपरा ने अपने विकास में कई तरह के तत्वों (समूहों, केन्द्रों, संबंधों आदि) का उपयोग किया है।’ रणेंद्र का मत है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए हर्बर्ट होप रिज्ले व विलियम विल्सन हंटर जैसे विदेशी अध्येताओं ने गोरों की श्रेष्ठता के नस्लीय और उनसे प्रभावित जी. एस. घुर्ये व एम. एन. श्रीनिवास जैसे भारतीय विद्वानों ने आर्यों (एक तरह से यूरोपीय) व उनके उत्तराधिकारी ब्राह्मण वर्ग (व्यापक अर्थ में सवर्ण) की श्रेष्ठता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी वैचारिकी से भारतीय संस्कृति को लेकर रणेंद्र के अनुसार ‘महान/श्रेष्ठ बनाम लघु परंपरा की बाईनरी’ की अवधारणा हमारे सामने आती है।
ध्यातव्य है कि आर्य-वैदिक-ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक धारा के मूल में भारत के ख़ासकर देहाती एवं वनांचलों में निवास करने वाले और घूमंतू-अर्द्ध घूमंतू अवस्था में सदियों तक जीवनयापन करते रहे अनेकानेक लोक व आदिम मानव समूहों की सांस्कृतिक चेतना रही है। जोहन फ्रेडरिक ‘फ्रिटस’ स्टाल सहित मिल्टन सिंगर एवं मैककिम मैरियट जैसे अमरीकी मानववैज्ञानिकों ने भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा को दो चरणों यथा; ‘नियत विकासवादी या आदिम विकास’ और ‘विभिन्न सभ्यता-संस्कृतियों के विविधतापूर्ण मिलन’ के रूप में पहचानने का प्रयास किया है। इसी द्वितीय चरण के स्वरूप को कालांतर में वर्ण-श्रेष्ठता की मानसिकता के चलते भारतीय संस्कृति की ‘वृहत परंपरा’ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहा। सिंगर के अनुसार—‘वृहत परंपरा का मूल स्रोत असंख्य लघु परंपराएँ हैं जो भारतीय इतिहास एवं उसके भौगोलिक विस्तार में बड़े पैमाने में अंतर्निहित हैं।’
इसी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए इतिहासकार विजयनाथ का मानना है कि ‘गुप्तकाल और उत्तर गुप्तकाल में इस देश में पर-संस्कृति ग्रहण (acculturation) यानी सांस्कृतिक आदान-प्रदान की लंबी प्रक्रिया चली है।’ जब वैदिक ब्राह्मणों का संपर्क भारत के आदिम समुदायों सहित तत्कालीन समाज के यत्र-तत्र बिखरे व्रात्य, गण, पूग, श्रेणी, संघ, निगम, पण जैसे मानव समूहों से हुआ तो उन्होंने भारत के इस वृहत्तर समाज से बहुत कुछ ग्रहण किया। इस क्रम में मूल वैदिक मान्यताओं में संशोधन, परिवर्द्धन एवं परिवर्तन देखने को मिला। वैदिक रूद्र को शिव, भूमि की उर्वरता से संबंधित मातृशक्ति को शिव की पत्नी, गण-अधिपति गणेश को शिव-पार्वती का पुत्र, आदिम समुदायों के गणचिह्न हाथी को गणेश का शीश, पशुपालक व कृषि-कर्म से जुड़े कृष्ण व बलराम जैसे आदिम नायकों, हनुमान जैसे जनजातीय नायकों को रामभक्त का रूप दिया जाने लगा। यहाँ तक कि आदिम समुदायों के मत्स्य, कूर्म, वराह एवं नरसिंह जैसे गणचिह्नों व मिथकों की पौराणिक प्रस्तुतियाँ विष्णु के अवतारों के रूप में होने लगी। वैदिक धर्म में मंदिर और मूर्ति-पूजा के संदर्भ नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज में प्रचलित गणचिह्न एवं पूर्वजों से संबंधित पूज्य-स्थलों के प्रभाव में मंदिर-निर्माण, मूर्ति-पूजा एवं पुजारी-पुरोहित परंपरा का आरंभ होता चला गया।
यदि भारत को एक राष्ट्र के रूप में व्याख्यायित किया जाता है तो उसका केंद्रीय भाव सांस्कृतिक बहुलता है, न कि एकरेखीय कोई सांस्कृतिक ढाँचा। रणेंद्र इस विचार पर जोर देते हैं कि ‘अनेकता में एकता या किसी और नारे के नाम पर उनकी (विविध संस्कृति-परंपराओं) विविधता, विशिष्टता, बहुलता और बहुरंगी इंद्रधनुषी सौंदर्य को नष्ट नहीं होने दिया जा सकता। इसलिए हमारे देश की प्रकृति के अनुरूप ‘अनेकता और एकता’ ज्यादा बेहतर और बहुलतावादी अवधारणा है। भारतविद् गुंथर डी० सोंतहाईमर के इस मत से रणेंद्र पूरी तरह सहमत होते हैं कि ‘जनजातीय संस्कृतियों के रूप में छोटे-छोटे समुदायों की परंपराओं का संरक्षण एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय परिघटना है। हर परंपरा, व्यक्ति और समुदाय की अपनी पहचान, अपनी अस्मिता बचाये और बनाये रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आधुनिक समय के उथलेपन में वे खो जाएँगी।’
भारतीय राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक परंपरा और मानस (psyche) को समझने के लिए रणेंद्र के इस शोधपूर्ण व श्रमसाध्य आलेख को पढ़ना आवश्यक है।
(डॉ०) पल्लव का ‘औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के विरुद्ध ये ख़त’ लेख की अपनी विशिष्ट एवं सामयिकता है। यह लेख बालमुकुन्द गुप्त उर्फ़ शिवशम्भु शर्मा द्वारा वायसराय लॉर्ड कर्ज़न को लिखे ‘चिट्ठे’ की वर्तमान प्रासंगिकता तक का भान हमें कराता है। ‘शिवशम्भु के चिट्ठे तथा चिट्ठे और ख़त’ पुस्तकाकार में सन् 1905 में प्रकाशित हुए। राष्ट्रीय नवजागरण काल के दौरान उन्होंने ‘अखबार-ए-चुनार’, ‘हिंदुस्तान’, ‘हिंदी बंगवासी’ और ‘भारत मित्र’ आदि महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया था। ‘शिवशंभु के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत’ के अलावा उनकी कृति ‘खेल तमाशा’ भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। गुप्त जी को हिंदी साहित्य में भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है।
भले ही बालमुकुंद गुप्त ने ‘शिवशम्भु शर्मा’ के छद्मनाम से ये ख़त लिखे थे, लेकिन फिर भी साम्राज्यवाद के उस दौर में इस कदर सत्ता से सवाल करना किसी दुस्साहस से कम नहीं था। अपने प्रत्येक पत्र के माध्यम से वे वायसराय को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं, यथा; ‘हिसाब कीजिये, नुमायशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन-सी कर चले हैं और भड़कबाज़ी के सिवाय ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है?’ बकौल पल्लव—‘गुप्त जी नुमायशी कामों और कर्तव्य में भेद करना जानते हैं। यह बात ही उन्हें महत्वपूर्ण बना देती है कि औपनिवेशिक काल में एक सामान्य व्यक्ति नागरिकता के आधुनिक बोध से संपन्न हो तथा वह अपने शासक से सवाल करना जानता हो। लोकतंत्र के इतने वर्षों बाद भी नागरिक बोध की कमी देखी जाती है और अपरिपक्व लोकतंत्र कहकर दुनिया में मजाक भी किया जाता है। उसी देश में औपनिवेशिक दासता के दिनों में शिवशम्भु शर्मा अपने शासक से पूछता है—‘आप बारंबार अपने दो अति तुमतराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं। एक विक्टोरिया-मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर ज़रा विचारिये तो ये दोनों काम ‘शो’ हुए या ‘ड्यूटी’?’
‘शो’ के रूप में सत्ता के तमाशा और लोकतंत्र में सत्ता की जन-प्रतिबद्धता का मुद्दा आज भी यथावत है। संसद के सेंगोल से लेकर मंदिर, प्रतिमा, जुमले, दिन में दस-दस दफ़ा वस्त्र-परिवर्तन, फ़ोटो-प्रियता, ताली-थाली बजवाने, मोमबत्ती-मोबाईल जलवाने, ब्लैक-आउट करवाने से लेकर कुम्भ के मेला तक की शो-बाज़ी और दूसरी तरफ़ बेरोजगारी, महँगाई, ग़रीबी, शिक्षा-स्वास्थ्य-पानी-बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं और भाईचारा एवं वैज्ञानिक दृष्टि के प्रति बेरुख़ी देश की जनता के प्रति कर्तव्यहीनता नहीं तो क्या? अपने ख़तों के माध्यम से ब्रितानी हुकूमत के दिनों भारत में वायसरायों की तैनाती की अवधि पाँच वर्ष होती थी। उसी तरह वर्तमान लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की कार्यावधि भी एक समय में पाँच साल की ही होती है। किसी कारण से यह कार्यकाल पूरा नहीं होना अथवा अगले चुनावों के बाद पुन: पदस्थापित होना अलग मसला है।
बालमुकुंद जी अपने ख़त में लिखते हैं—‘जिस पद पर आप आरूढ़ हुए, वह आपका मौरुसी नहीं…जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है, उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है…आडंबर से इस देश का शासन नहीं हो सकता। आडंबर का आदर इस देश की कंगाल जनता नहीं कर सकती…आपने अपनी समझ में बहुत कुछ किया; पर करने से अधिक कहने का आपका स्वभाव है…’ जब गुप्त जी लिखते हैं—‘माइ लॉर्ड! आप वक्तृता देने में बड़े दक्ष हैं’ तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री को लक्षित कर जनता की तरफ़ से एक सजग नागरिक का प्रतिरोध दर्ज़ करा रहे हों। यह बात आगे के इस उद्धरण से और भी स्पष्ट हो जाती है—‘क्या आप कह सकेंगे—अभागे भारत! मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा; पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश! जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जिम्मे न थी…’ आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माइ लॉर्ड में कहाँ?’
पल्लव के इस लेख से जानकारी मिलती है कि बालमुकुंद गुप्त जी ने शिवशम्भु शर्मा बनकर वायसराय कर्ज़न को जो ख़त लिखे, उनके अलावा कुछ चिट्ठे अन्य लोगों के नाम भी लिखे। ‘बंगाल के शासक रहे शाइस्ता खाँ के ख़त फुल्लर साहब उन्होंने लिखे जिनमें नवाबी जाने और अंग्रेजी हुकूमत के यथार्थ की तुलना है।’ पल्लव अपने इस लेख में संदर्भित शिवशम्भु के ख़तों की मार्फ़त एक बड़े लेखक के कालातीत महत्व और सत्ता के मनुष्य विरोधी चेहरे को बेनक़ाब करने के साहस को रेखांकित करते हैं। ‘शाइस्ता के बहाने यह कथन हर शासक के लिए चेतावनी ही तो है, ‘ख़्याल रखो कि दुनिया चंद रोज़ा है। आखिर सबको इस दुनिया से काम है, जिसमें हम हैं। सदा कोई रहा, न रहेगा। नेकनामी या बदनामी रह जावेगी।’
शिवशम्भु शर्मा के छद्मनाम से बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखे इन पत्रों के प्रकाशन के ठीक 120 वर्ष बाद हम उनपर चर्चा कर रहे हैं। बाईबल के अनुसार ‘संख्या 120 देह के युग के समाप्त होने और आत्मा के युग के आरंभ का प्रतीक है।’ भारतीय लोकतंत्र के विशेष संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वयस्क मताधिकारी नागरिकों की दैहिक गणना की भेड़चाल के स्थान पर सजग नागरिकों की आत्मा (चेतना) की आवाज़ पर जब तक अपने मताधिकार का उपयोग करने की क्षमता विकसित नहीं होगी, तब तक जनविरोधी राजसत्ता को सही राह पर नहीं लाया जा सकता।
भारत आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जिसमें सत्ता के खिलाफ़ तनिक भी आवाज़ उठाने वाले को राजद्रोह और फिर देशद्रोह का ‘पाप’ करने वाला वाला घोषित करने में देरी नहीं की जाती। ऐसे में राजसत्ता की तानाशाही पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दशा का एक मात्र विकल्प लोकतान्त्रिक-जनजागृति है। यह काम बालमुकुंद गुप्त जैसा साहसी लेखक, तल्ख़ व्यंगकार, निर्भीक पत्रकार और सचेत संपादक कर सकता है।
—हरि राम मीणा (जयपुर)