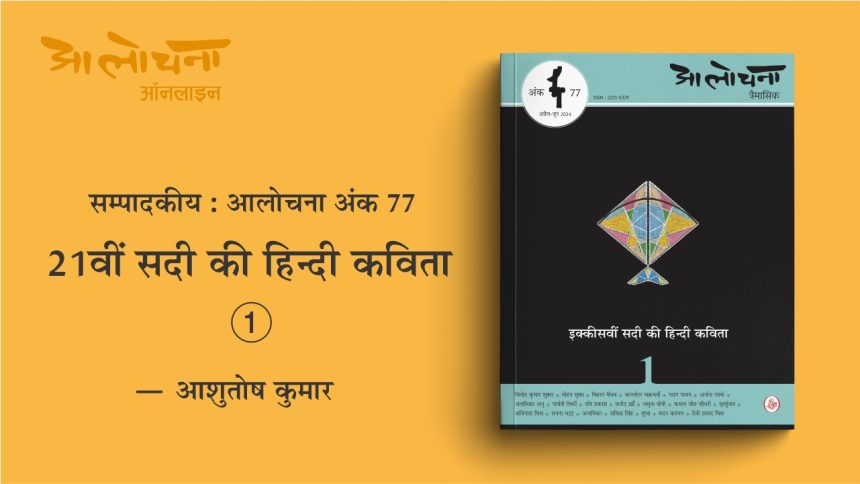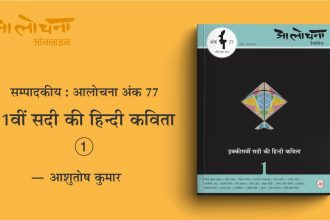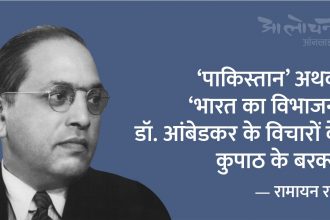आलोचना पत्रिका के कविता-अंक की योजना बने हुए साल-भर से अधिक समय हो गया। उस समय सोचा यह गया था कि इसे एक महीने के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। हमारे पास अनेक कवियों की स्वीकृत कविताएँ पहले से मौजूद थीं। हमने कुछ और कवियों से कविताओं के लिए अनुरोध किया। किसी को पंद्रह दिन का समय बताया गया, किसी को पाँच दिन का। लेकिन धीरे-धीरे कवियों और दिनों की संख्या बढ़ती चली गई। कविता अंक के साथ वही हुआ, जो कविता के साथ होता है। जब आप काग़ज़ पर कविता शुरू करते हैं, तब आपको कुछ पता नहीं होता कि आगे चलकर क्या होगा। कविता कहाँ ख़त्म होगी, कहीं होगी भी या नहीं। जल्दी ही यह बात स्पष्ट हो गई कि जैसे कविता के साथ कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, वैसे ही कविता-अंक के साथ भी न ज़बरदस्ती की जा सकती है, न उससे मुँह मोड़ा जा सकता है। उसके साथ मिलकर मनोयोग से काम करना होता है। कवि और कविता, दोनों एक-दूसरे को रचते बदलते हैं। दोनों पहले से नहीं जानते इस काम का अंजाम क्या होगा। कविता-अंक के साथ भी यही हुआ। कवियों से हमें जो सहयोग मिला, वह आश्चर्यजनक था। उन्होंने न केवल तत्परता से अपनी कविताएँ भेजीं, बल्कि अंक के प्रकाशन में होते जा रहे अनंत विलम्ब का भी कवि-संभव धैर्य के साथ सामना किया।
इक्कीसवीं सदी के संकट और कविता
इस अंक के लिए हमने एक ज़रूरी नया प्रयोग यह किया कि कविताओं के साथ हमने कवियों के वक्तव्य भी माँगे।
हमने कवियों से जानना चाहा कि आज लिखी जा रही हिन्दी कविता पहले की तुलना में आगे बढ़ी हुई जान पड़ती है, या ठहरी हुई। यह भी कि क्या उन्हें आज की हिन्दी कविता में कोई संकट दिखाई देता है। क्या उन्हें आज देश और दुनिया की परिस्थितियों में भी किसी तरह का कोई संकट दिखाई देता है? अगर हाँ तो क्या देश-दुनिया के इस संकट का हिन्दी कविता के वर्तमान परिदृश्य से भी कुछ रिश्ता है, चाहे यह परिदृश्य संकट का हो या सफलता का?
प्रश्नों के इस सूत्रीकरण में यह धारणा अन्तर्निहित है कि कविता अनिवार्यतः मनुष्यता के संकट के प्रति संबोधित होती है। अर्थात संकट का एहसास, उसे पहचानने और समझने की कोशिश और उसके प्रति एक रचनात्मक प्रतिक्रिया मूल कविकर्म है। कविता में ही नहीं, कला और उद्यम के बाक़ी क्षेत्रों में भी यही मनुष्य का बुनियादी रचनात्मक कर्म है।
मुक्तिबोध कहते थे कि कविता की मूल प्रेरणा कोई वास्तविक जीवन-समस्या होती है। कामायनी : एक पुनर्विचार में उन्होंने इस जीवन-समस्या को कवि के अन्तर और वाह्य के द्वंद्व के रूप में उपस्थित किया है।
‘संकट’ का अर्थ-संकेत इससे मिलता-जुलता किंतु अधिक व्यापक है। यह निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी। यूँ भी इक्कीसवीं सदी में निजी और वैयक्तिक का अर्थ उतना निजी नहीं रह गया है, जितना वह मुक्तिबोध के युग में रहा होगा। मुक्तिबोध मानते थे कि जीवन-समस्या का अनुभव ही श्रेष्ठ कविताओं में पूरी ‘सभ्यता समीक्षा’ संभव करता है।
आज न जीवन-समस्या की पहचान इतनी आसान रह गई है, न ही सभ्यता की कोई सरल समीक्षा। सभ्यता और समीक्षा जैसे पद ही समस्याग्रस्त हो चले हैं। यह वाल्टर वेन्यामिन की स्थापना है कि सभ्यता का इतिहास बर्बरता का इतिहास भी है। उत्तर-आधुनिकों ने दिखाया है कि मानव-सभ्यताओं का कोई एकल वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं होता। ताक़तवर लोग यह दिखाने के लिए इतिहास लिखते हैं कि उनकी ताक़त स्वाभाविक, तार्किक और इतिहास-सिद्ध है। इसलिए इतिहास के नए दावेदारों को हर बार मनुष्य का नया इतिहास लिखने की ज़रूरत पड़ती है।
हमारे समय में मानव जाति के संकट का एहसास व्यापक है। इसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आयाम हैं। पर्यावरण और अस्तित्व की चिंताएँ भी साथ जुड़ी हुई हैं। आज संकट-मुक्त कोई है तो वे हैं, दुनिया के अरबपति, जिनकी आबादी लगभग एक प्रतिशत है। हर संकट में उनकी संपदा बढ़ती जाती है।
पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि 20वीं सदी ने मानव जाति से कुछ बेहद आसान सवाल पूछे थे और उनके आसान जवाब ढूँढे थे।
जैसे एक सवाल यह था कि स्त्री के साथ होने वाले भेदभाव का अंत कैसे हो सकता है। जवाब यह पाया गया कि राजनीतिक और क़ानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक बदलाव के ज़रिये ऐसा किया जा सकता है।
21वीं सदी में आकर ये सारे जवाब संदिग्ध हो गए। सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भागीदारी कुछ बढ़ी ज़रूर लेकिन स्त्री बतौर एक श्रेणी पुरुष के वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में आज भी नहीं है। इस नियम के कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, वे नियम को सिद्ध करने के लिए ही होते हैं।
हमारे समय में स्त्री-विद्वेष, स्त्री-विरोधी हिंसा और और स्त्री-उत्पीड़न के ऐसे भयावह नए रूप सामने आए, जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रसार से पहले यह उम्मीद की गई थी कि वंचित उत्पीड़ित तबक़ों को नई शक्ति मिलेगी। लेकिन हुआ यह कि इनसे उत्पीड़न के व्यवसाय को नया अभूतपूर्व विस्तार मिला और उत्पीड़कों के हाथों में विराट शक्ति आ गई।
फिर यह भी समझ में आने लगा कि जेंडर भेदभाव का सवाल केवल स्त्री-पुरुष का सवाल नहीं है। जेंडर केवल दो नहीं हैं। उनकी पूरी रेंज है जिस पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता, क्योंकि स्त्री-पुरुष की बाइनरी या विपरीत युग्म को परम सत्य मान लिया गया है। यह बाइनरी कई तरह की सच्चाइयों पर पर्दा डाल देती है। न दुनिया की सारी स्त्रियाँ एक समान हैं, न पुरुष। शहर में रहने वाली अमीर ब्राह्मण स्त्री और गाँव में रहने वाली ग़रीब दलित स्त्री के सवाल एक जैसे नहीं हो सकते भले ही पितृसत्ता दोनों को अपना शिकार बनाती हो। पितृसत्ता के शिकार तो पुरुष भी हैं, लेकिन अलग तरह से।
वैज्ञानिक शिक्षा के विकास और पूँजीवादी उत्पादन के नए रूपों के प्रसार ने उत्पीड़न के पुराने साँचों को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि अनेक रूपों में और अधिक मज़बूत बना दिया। यह बात भी दिखाई देने लगी कि भेदभाव और अन्याय के सभी रूप एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे को बचाते हैं। इसका मतलब सवाल केवल स्त्री के साथ होने वाले भेदभाव का नहीं है बल्कि कहीं अधिक मूलगामी और जटिल है। जेंडर और पितृसत्ता के साथ वर्ग, रेस, जाति, राष्ट्रीयता, रंग, यौन अभिरुचि और तमाम दूसरे सवाल जुड़े हुए हैं। एक ही व्यक्ति अनेक श्रेणियों में उत्पीड़न का शिकार हो सकता है और यह भी हो सकता है कि जो किसी एक जगह उत्पीड़ित हो, वह कहीं और स्वयं उत्पीड़क बना हुआ हो।
बीसवीं सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट था शीतयुद्ध। शीतयुद्ध दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई तो था ही, यह दो विचारों और दो महास्वप्नों के बीच की प्रतियोगिता जैसा भी नज़र आता था।
शीतयुद्ध की महान बाइनरी ने मानवीय संकट की जटिलता, बहुस्तरीयता और बहुकोणीयता को छुपा लिया। इसने संकट को विपरीत युग्म के रूप में देखने की आदत को सार्वभौमिक बना दिया।
एक जटिल दुनिया सरल नज़र आने लगी। उसकी लड़ाइयाँ सीधी, सरल और समझ में आने लायक़ थीं।
अमेरिका बनाम सोवियत संघ, पूँजीवाद बनाम समाजवाद, पहली बनाम दूसरी दुनिया और इन्हीं दो में किसी एक की तरफ झुकी हुई तीसरी दुनिया, पूर्व बनाम पश्चिम, श्वेत बनाम अश्वेत, स्त्री बनाम पुरुष, सफ़ेद बनाम काला, सच बनाम झूठ, दिन बनाम रात, सही बनाम ग़लत। यही लड़ाइयाँ थीं और इनमें ग़लत के ऊपर सही की जीत केवल वक़्त की बात समझी जा रही थी।
सोवियत संघ के पतन ने इस परिप्रेक्ष्य को बदल दिया। यह बहस चलती रहेगी कि सोवियत संघ का पतन मुख्यतः उसके आंतरिक संकटों के कारण हुआ या बाहरी दबाव के कारण, लेकिन एक बात बहस से परे है। शीतयुद्ध ने हथियारों की जिस होड़ को जन्म दिया, वह अमरीकी पूँजीवाद के लिए मुँहमाँगा वरदान था, जबकि सोवियत समाजवाद के लिए एक अभिशाप।
अमेरिकी पूँजीवाद अपने हथियार उद्योग और हथियारों के व्यापार के सहारे अपने संकटों से उबरता रहा, जबकि सोवियत समाजवाद के भीतर हथियारों की इसी होड़ ने एक असमाधेय आर्थिक संकट पैदा कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट की सन् 94 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ 1980 से 90 के बीच दुनिया में अमेरिकी हथियारों का निर्यात दुगुना हो गया। आज हथियारों के निर्यात में संयुक्त राज्य अमरीका का हिस्सा 42 प्रतिशत से अधिक है।
सोवियत संघ का अंत वैश्विक पूँजीवाद की जीत थी। तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से सोवियत संघ का सहारा छिन गया। वे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी अमरीका-नियंत्रित संस्थाओं के आगे समर्पण करने को मजबूर हो गईं।
मार्क्स ने बताया था कि पूँजीवाद विश्व बाजार के निरंतर विस्तार के ज़रिये ही अपने आंतरिक संकट को हल कर सकता है, चाहे यह हल कितना ही अस्थायी हो। विश्व पूँजीवाद की सेवक इन संस्थाओं ने अपनी सशर्त सहायताओं के बदले विकासशील अर्थ-व्यवस्थाओं को विनियमन, निजीकरण और मुक्त बाज़ार की बढ़ावा देने वाली नीतियों को स्वीकार करने को विवश किया। इसे वाशिंगटन सर्वसम्मति कहते हैं, जिसे संरचनात्मक समायोजन का नाम देकर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। इसी परिघटना ने उस बहुआयामी राजनीतिक सांस्कृतिक प्रक्रिया को जन्म दिया जिसे भूमंडलीकरण कहा जाता है।
भूमंडलीकरण ने पूँजी का रुका हुआ रास्ता खोल दिया। खरबपतियों की संख्या और उनकी संपदा में बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ। पूँजी सस्ते श्रम की तलाश में दुनिया के ग़रीब हिस्सों की तरफ़ दौड़ी। आउटसोर्सिंग ने दुनिया-भर में कुशल श्रमिकों की हालत में कुछ सुधार किया तो अमीर और ग़रीब दोनों तरह के मुल्कों में बेरोज़गारी के नए महाद्वीप भी पैदा किए। इसी के साथ संरचनात्मक समायोजन के कारण सामाजिक सुरक्षाओं में हुई भारी कटौती ने असमानता की स्थिति को विकराल बना दिया।
2022 की वैश्विक असमानता रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले दो दशकों में दुनिया के अमीर और ग़रीब देशों के बीच असमानता की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है लेकिन देशों के भीतर की असमानता लगभग दोगुनी हो गई है। सन् 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत दुनिया के सबसे अधिक असमान देशों में है।
फ्रंटलाइन और एनडीटीवी की रिपोर्टों के मुताबिक़ भारत की एक प्रतिशत सबसे अमीर आबादी के पास देश की कुल संपदा का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, जबकि नीचे की 50 फ़ीसद आबादी के पास केवल 6.4 प्रतिशत। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स क्रैबट्री की 2018 की चर्चित पुस्तक में भारत की आर्थिक अवस्था को ‘बिलेनियर राज’ कहा गया है। किताब का नाम है : द बिलेनियर राज : ए जर्नी थ्रू इंडिया’ज न्यू गिल्डेड एज।
इधर सन् 2015 से 25 के बीच भारत में अरबपतियों की संख्या 70 से बढ़कर 284 हो गई है। भारत में ग़रीबी उन्मूलन के संदिग्ध दावों के बीच मुफ़्त अनाज की सरकारी सहायता पर निर्भर लोगों की संख्या 80 करोड़ से अधिक हो गई है।
सामाजिक सुरक्षाओं में लगातार होती कटौती और निजीकरण के निरंतर तेज़ होते चक्र के कारण लगातार हाशिए की ओर धकेली जा रही आबादियों का जीवन अतिभंगुर (Precarious) होता चला गया है।
संकट को विस्फोटक होने से बचाने के लिए मुफ़्त अनाज, मुफ़्त सेहत बीमा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की गारंटी की योजनाएँ चलानी पड़ रही हैं, बावजूद इसके कि 10 साल पहले ही मनरेगा को राष्ट्रीय विफलता का स्मारक घोषित किया जा चुका था। इन योजनाओं से अतिभंगुर जीवन जीने को अभिशप्त आबादियों को एक दिलासा तो मिलता है, लेकिन उनकी भंगुरता की स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं होता।
भूमंडलीकरण के कारण दुनिया के अमीरों की अमीरी में बेतहाशा इज़ाफ़ा हुआ लेकिन दूसरी तरफ़ ग़रीबों का जीवन उतना ही असुरक्षित होता चला गया। इस अंतर्विरोध ने दुनिया भर में पूँजीवाद के ख़िलाफ़ जन-आक्रोश पैदा किया जिसकी अभिव्यक्ति ‘ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट’ जैसे अनेक आंदोलनों में देखी गई। लेकिन इसके पहले कि यह आक्रोश एक संगठित राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकता, दुनिया-भर में दक्षिणपंथी फ़ासीवादी पार्टियों ने बड़ी चतुराई से उसे आप्रवासियों और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ मोड़ दिया।
नेशन फ़र्स्ट के नारे के सहारे इन पार्टियों ने एक तरफ़ तो ग़रीबों के ग़ुस्से से अमीरों को सुरक्षा प्रदान की तो दूसरी तरफ़ भ्रष्टाचार-नियंत्रण की जुमलेबाजी और संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों की पैरोकारी करते हुए ग़रीबों को हालात के सुधरने का सपना दिखाया। इससे विनियमन और निजीकरण के नृशंस अभियान को बेरोकटोक जारी रखना आसान हो गया। दक्षिणपंथी पार्टियों ने आक्रोश को भय के उन्माद में बदला और उसे आप्रवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ-साथ पिछली तीन सदियों के सारे प्रगतिशील आदर्शों के ख़िलाफ़ भी मोड़ दिया। ये आदर्श थे समानता, स्वतंत्रता, प्रेम, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय और मानवाधिकार के। जेंडर, रंग, नस्ल, जाति, धर्म, यौनिकता आदि के भेदभाव के उन्मूलन के।
इन आदर्शों की वकालत करने वालों के लिए अमेरिका में एक शब्द चलता था : ‘वोक’। वोक यानी सजग। ‘स्टे वोक’ हर तरह के ‘अन्याय’ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों का लोकप्रिय नारा था। सन् 2019 के बाद यही शब्द ‘वोक’ ऐसे लोगों का मज़ाक़ उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। भारत में भी हिंदुत्ववादी राजनीति के सुप्रीम संचालक ने देश के सामने मौजूद ख़तरे को चिह्नित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया।
‘वोक’ शब्द का यह अर्थ-विपर्यय बताता है कि 21वीं सदी में लोकप्रिय संस्कृति की धुरी दक्षिणपंथी फ़ासीवादी ताक़तों की ओर खिसक रही है।
आधुनिकता के महान आदर्शों की विफलता को महसूस करते हुए फूको और देरिदा जैसे उत्तर-आधुनिक चिंतकों ने ज्ञान और सत्य की राजनीति को समझने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दिखाया कि न कोई ज्ञान सार्वभौमिक है, न सत्य। ताक़तवर एजेंसियाँ ताक़त से अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए अनुकूल ज्ञान और सत्य का निर्माण करती हैं और उसे सार्वभौमिक घोषित कर देती हैं। इसलिए सत्य क्या है यह जानना उतना ज़रूरी नहीं है, जितना यह जानना कि सत्य किसका है। हर उस सत्य को चुनौती देना और विखंडित करना ज़रूरी है जो शक्तिशाली एजेंसियों और सत्ताओं के हितों की परवरिश करता है।
विडंबना यह है कि चतुर सयाने पूँजीवाद (लेट कैपिटलिज़्म) ने इन विचारों का भी अपने हितों की रक्षा के लिए भरपूर इस्तेमाल कर लिया।
उसने क्रांतिकारी विचारों और पूँजीवाद-विरोधी कला को भी उपभोक्ता वस्तुओं में बदल दिया। उसने आभासी सत्य को ही सत्य के रूप में बेचना शुरू कर दिया। उसने बदलाव की हर आकांक्षा और ‘अन्याय’ के हर एक विरोध को संदिग्ध बना देने की कोशिश की।
ऐसे संकट काल में बुद्धिजीवी, कवि और कलाकार के सामने दोहरी चुनौती आ खड़ी होती है। एक तो अपने काम को उपभोक्ता वस्तु में बदलने से बचाने की यानी अपने आप को सेलिब्रिटी सनसनी, पुरस्कार और अदबी नुमाइशों के पूँजीवादी बाज़ार में इस्तेमाल हो जाने से बचाने की। दूसरे सत्ताओं से ऐसे सवाल पूछते रहने की, जो उनकी ओर से चलाए जा रहे सत्यों की बखिया उधेड़ सकें।
कविता और कवि वक्तव्य
कहा जा सकता है कि कविता हमेशा किसी संकट की प्रतिक्रिया हो, यह क्यों ज़रूरी हो! वह जीवन के उल्लास और सौंदर्य की अभिव्यक्ति भी हो सकती है। हो सकती है, लेकिन अगर समाज में व्यापक संकट हो, तो उल्लास उसके बाहर नहीं हो सकता। उल्लास कहीं-न-कहीं संकट का सामना करने के रचनात्मक रूपों से ही प्रकट हो सकता है। अन्यथा वह एक विमूढ़ उल्लास है, जिसे जगत गति नहीं व्यापती।
ऐसे में कविता की शक्ति इसी बात पर निर्भर करती है कि वह मनुष्यता के संकट का सामना कितनी गहनता और रचनात्मकता के साथ कर पाती है। अगर नहीं कर पाती तो वह स्वयं संकट-ग्रस्त कही जा सकती है।
प्रश्न उपस्थित करते समय यह आशा नहीं की गई थी कि कविगण इस सूत्रीकरण से हमेशा सहमत होंगे। प्रश्न केवल उन्हें उकसाने के लिए थे। हुआ भी यही। सभी कवियों ने अलग-अलग ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर दिए। लेकिन इस बहाने हमें इस दौर के महत्त्वपूर्ण कवियों के चिंतन-पक्ष को जानने-समझने का मौक़ा मिला। हम इस बात के क़ायल नहीं थे कि कविता ही कवि का वक्तव्य है। या इस बात के कि कवि जो कुछ कहता है, कविता में कहता है। बेशक कविता में कहता है, लेकिन कविता सार्थक तब होती है, जब उसमें वह बात कही जाती है, जो कविता के बाहर नहीं कही जा सकती।
कवि के चिंतन-आलेख से ही इस बात को समझने की राह मिलती है कि आख़िर वह कौन-सी खोज है जो कवि को कविता के बीहड़ प्रदेश में उतरने के लिए बाध्य करती है। अगर वह कविता में भी लगभग वही कह रहा है, जो वह कविता के बाहर कह सकता है, तो उसे कविता की ख़ास ज़रूरत नहीं है। तब उसकी कविता ज़रूरी कविता नहीं है।
इसी बात को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर कवि के पास कविता के बाहर कहने के लिए कुछ ख़ास नहीं है, तो कविता में भी शायद वह वही कह रहा है, जो वह बाहर भी कह सकता था। चिंतन की मौलिकता के बिना कविता में मौलिकता की उम्मीद करना कविता को एक रहस्यमय प्रक्रिया बना देना है।
इस अंक में कवियों के चिंतन-आलेख या ‘वक्तव्य’ पर हमारा ज़ोर कविता को रहस्य के पर्यावरण से मुक्त करने के लिए है। कविता के किसी ‘रहस्यवादी पाठ’ की आशंका को कम करने के लिए है।
हम यह नहीं मानते कि कविता अपने लिखित पाठ में शेष हो जाती है। कविता अपने पाठकों और आलोचकों के साथ संवाद करते हुए बार-बार पुनर्जीवित होती है। कविता और पाठक के संवाद के पहले कवि के साथ पाठक का संवाद कविता की पाठ-प्रक्रिया को अराजकता से बचा सकता है।
हम यह भी मानते हैं कि कविता की पाठ-प्रक्रिया एक सामूहिक सामाजिक संवाद-प्रक्रिया है। ऐसे में कवि का ‘वक्तव्य’ इस समूची संवाद-प्रक्रिया को समृद्ध कर सकता है।
आप देखेंगे कि इस अंक के सभी सहभागी कवियों ने देश, दुनिया और हिन्दी कविता की वर्तमान परिस्थिति के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इन वक्तव्यों को बहुत कम संपादित किया गया है। अधिकांश कवियों ने हिन्दी कविता में अनुभव-क्षेत्रों की बढ़ती हुई विविधता की ओर ध्यान खींचा है। स्त्री, दलित, दलित स्त्री, आदिवासी, आदिवासी स्त्री, क्वीयर, श्रमिक विकलांग, वृद्ध, विज्ञान और तकनीकी तथा पर्यावरण जैसे अनुभव के नए क्षेत्र हिन्दी कविता से लगातार जुड़ रहे हैं।
हिन्दी कविता में इन क्षेत्रों से आनेवाले कवियों की संख्या कहीं कम कहीं ज़्यादा लगातार बढ़ रही है। इनमें से स्त्री, दलित और आदिवासी कविता ने मुख्यधारा के समानांतर नहीं उस के भीतर अपनी महत्वपूर्ण स्वायत्त पहचान स्थापित कर ली है। अर्थात हिन्दी कविता के महत्वपूर्ण नामों की चर्चा करते हुए अब कई स्त्री, आदिवासी और दलित कवियों को अलग श्रेणी में रखना बेतुका लगने लगा है। यह बात उन कवियों के बारे में भी कही जा रही है, जो स्वयं को सचेत रूप से स्त्री, दलित या आदिवासी चेतना से जोड़ते हैं, न कि उन कवियों को जो इन अनुभव-क्षेत्रों से होते हुए भी ऐसा नहीं करते।
इस अंक में ऐसे बहुत से कवियों को शामिल किया गया है। उनकी चेतना को उनकी कविताओं और वक्तव्यों से पहचाना जा सकता है। अलग से उनकी श्रेणिया नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि वे सभी हिन्दी कविता की मुख्य धारा हैं।
यह महत्त्वपूर्ण है कि सहभागी कवियों ने प्राय: अपनी और अपने समय की कविता के प्रति एक विवेकपूर्ण आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई है। उन्होंने जो नया किया है इसका उन्हें संतोष है लेकिन जो कुछ नहीं हो पाया है उसके लिए गहरा असंतोष भी है।
अधिकांश कवियों ने संकेत किया है कि प्रवृत्तियों की विविधता और व्यापकता के बावजूद प्रत्येक प्रवृत्ति के भीतर एक जैसे विषयों और एक जैसी संवेदना का दोहराव बहुत अधिक हो रहा है।
स्त्री और दलित कवियों को इस बात का एहसास है कि वर्तमान हिन्दी कविता की काव्य- भाषा इतनी परिष्कृत और स्थापित हो चुकी है कि उसे बदलना आसान नहीं है। वह इस बात को लेकर सचेत हैं कि काव्य-भाषा को बदले बिना कविता में नई संवेदना और नई चेतना संभव नहीं हो सकती। वे सचेत हैं कि पुरानी भाषा में नई बात कहने की कोशिश करते हुए अक्सर उस नई बात में पुरानी अर्थ-भंगिमाएँ बोलने लगती हैं।
पुरानी भाषा का विखंडन और नई भाषा का निर्माण हर ज़माने के नए कवि का संघर्ष होता है।
यह संघर्ष चल रहा है और इसमें किसको कितनी सफलता मिलती है इसी पर उसकी कविता की प्रासंगिकता निर्भर करती है। आगे हम यह रेखांकित करने की कोशिश करेंगे कि 21वीं सदी की नई हिन्दी कविता में किस तरह का नया रचनात्मक प्रयत्न दिखाई देता है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे 21वीं सदी की कविता-प्रक्रिया कहा जा सकता है?
हमने इस अंक में पीढ़ियों के बँटवारे से भी जान-बूझकर परहेज़ किया है। आप देखेंगे कि इस अंक में कवियों को जन्मतिथि या वरिष्ठता के क्रम में संकलित नहीं किया गया है।
हम यह समझते हैं कि इक्कीसवीं सदी की हिन्दी कविता में जो कुछ महत्त्वपूर्ण हो रहा है वह पीढ़ियों के दायरे को तोड़कर हो रहा है। जो कवि इन दायरों को नहीं तोड़ पा रहे हैं वे अपनी पूर्ववर्ती रचनाशीलता को दोहराने के लिए अभिशप्त हैं।
21वीं सदी की हिन्दी कविता के कूचे में जिन कवियों की आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही है वे वही हैं जो 21वीं सदी की कविता लिख रहे हैं। हमने यह कोशिश की है कि इस अंक में आपको 21वीं सदी की हिन्दी कविता का नया चेहरा दिखाई दे।
यहाँ दो बातें कहनी ज़रूरी हैं। एक तो यह कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस कविता अंक में 21वीं सदी के सभी महत्त्वपूर्ण कवियों को संयोजित कर लिया गया है। ऐसे बहुत-से कवियों की कविताएँ अभी तक हमें नहीं मिल पाई हैं जिनके बारे में हम सोचते थे कि उनका इस अंक में रहना बेहद ज़रूरी है। कविता अनुरोध पर नहीं लिखी जा सकती है, न समय-सीमा के भीतर तैयार की जा सकती है। इसलिए एक ही विशेषांक में सब कुछ समेट लेने के व्यामोह से मुक्त रहना ज़रूरी है।
यह भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो कविताएँ संकलित हैं उन सभी को 21वीं सदी की प्रतिनिधि कविता मान लिया जाए। हमने इतनी कोशिश ज़रूर की है कि इस अंक में वैसी कविताएँ न ली जाएँ जिनमें 21वीं सदी की कविता-प्रक्रिया का स्पर्श बहुत हल्का हो।
इक्कीसवीं सदी और हिन्दी कविता
21वीं सदी की विशिष्टता पर ध्यान देने के लिए पिछली सदी के आख़िरी दशकों की हिन्दी कविता में जो बदलाव आ रहे थे, उन पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। 80 के दशक के कवियों में नष्ट होते हुए जीवन को सहेज लेने और बचा लेने की एक तड़प थी। कविता में यह बार-बार सुनाई दे रहा था कि सब कुछ नष्ट हो रहा है और जो कुछ बचाया जा सके उसे बचा लेना चाहिए या कम से कम उसके बचे रहने की कामना करनी चाहिए।
आधुनिकता के महास्वप्न से रंजित पूरी दुनिया नष्ट होती हुई दिखाई देती थी। यहाँ तक कि कविता भी नष्ट हो रही थी और कवि भी।
मंगलेश डबराल की प्रसिद्ध कविता है : कवियों में बची रहे थोड़ी लज्जा।
बचा लेने की यह कामना बताती है कि मनुष्यता के साझा स्वप्न में इस दौर के कवियों की श्रद्धा अभी बची हुई थी, नष्ट नहीं हुई थी।
90 के दशक से हिन्दी कविता में अश्रद्धा, प्रश्नवाचकता और प्रतिरोध की आवाज़ तेज़ होती है। सन् 1988 में देवी प्रसाद मिश्र की कविता ‘प्रार्थना के शिल्प में नहीं’ के पुरस्कृत होने से इस बदलाव की साफ़ झलक मिलने लगती है। इसी समय के आसपास आई कात्यायनी की कविता ‘हॉकी खेलती लड़कियाँ’ भी इस बदलाव का एक प्रमुख उदाहरण है। ओमप्रकाश वाल्मीकि की चर्चित कविताएँ ‘ठाकुर का कुआँ’ और ‘तब तुम क्या करोगे’ का भी यही समय है। यहीं से हिन्दी कविता में विभिन्न उत्पीड़ित विमर्शों का मुखर समय शुरू होता है।
90 के आसपास हिन्दी कविता में हाशिए की आवाज़ों का प्रबल रूप से उभरकर आना सीधे-सीधे किसी उत्तर-आधुनिक सैद्धांतिकी से प्रेरित नहीं था।
1990 के अगस्त महीने में मंडल कमीशन की घोषणा और सितंबर महीने के आख़िर में आडवाणी की रथयात्रा इस वर्ष की सबसे उल्लेखनीय घटनाएँ तो थीं ही, भारतीय राजनीति के लिए भी एक पैराडाइम शिफ़्ट थीं।
आज़ादी के बाद भारतीय लोकतंत्र के लगातार विस्तार ने हाशिए पर पड़े सामाजिक समूहों के भीतर नई राजनीतिक आकांक्षाएँ जगा दी थीं। मंडल कमीशन की घोषणा सामाजिक न्याय की इन्हीं आकांक्षाओं को मुख्यधारा में जगह देने की एक गंभीर कोशिश थी।
मंडल कमीशन घोषित होते ही रथयात्रा की घोषणा एक प्रतिक्रांति थी।
आडवाणी की रथयात्रा कुछ समय से चल रही मंदिर आंदोलन की सुगबुगाहट को एक उदग्र दौर में ले गई। मंदिर आंदोलन हाशिए के सभी समूहों की न्याय, प्रगति और लोकतंत्र की माँग को रैडिकल हिंदुत्व के विस्फोट से पीछे धकेल देने का आंदोलन था। यह भारत में फ़ासीवाद की राजनीति का प्रक्षेपण-बिंदु था। इसका उद्देश्य सनातन हिंदुत्व के सामने सभी विद्रोही अस्मिताओं का समर्पण सुनिश्चित करना था।
इन विद्रोही अस्मिताओं में स्त्री,दलित, पिछड़े, आदिवासी और क्वीयर जैसी सभी श्रेणियाँ थीं, जिनको एक ख़ास तरह के राजनीतिक संस्कृतिकरण के ज़रिये सनातन हिंदुत्व की छत्रछाया में ले आना था।
इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं कि इसके बाद आने वाली हिन्दी कविता मुख्यतः हिंदूवादी फ़ासीवाद के विरुद्ध प्रतिरोध की कविता के रूप में उभरती है।
इस हद तक कि इस दौर में हिन्दी साहित्य के भीतर हमेशा चलने वाली जनवाद और कलावाद की बहस भी अगर अप्रासंगिक नहीं होती तो कम से कम चुप-सी लगा लेती है।
90 की रथयात्रा और 92 में हुए बाबरी मस्जिद के विध्वंस से जो संकट गहरा हुआ उसकी चरम परिणति सन् 2002 के गुजरात के दंगों में दिखाई देती है।
सन् 2002 जैसे भारतीय राजनीति के लिए वैसे ही हिन्दी कविता के लिए भी एक निर्णायक वर्ष है। यहाँ से हिन्दी कविता में एक ख़ास रचना-प्रक्रिया दिखाई देती है जिसे ऊपर 21वीं सदी की कविता-प्रक्रिया कहा गया है। इसे बिल्कुल नया तो नहीं कह सकते लेकिन इसमें बहुत कम संशय है कि यह धीरे-धीरे हिन्दी कविता का सबसे महत्त्वपूर्ण ढब बनता जा रहा है।
मंगलेश डबराल की कविता ‘गुजरात के मृतक का बयान’ में इस नई कविता-प्रक्रिया और नए ढब की ताक़त को आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस कविता में मंगलेश की ही पूर्ववर्ती कविताओं सरीखी प्रगीतात्मकता नहीं है। विस्थापन के अवसाद का वह परिचित राग और स्मृति का नॉस्टेल्जिया नहीं है।
इस कविता में द्वंद्वात्मकता ने प्रगीतात्मकता को विस्थापित कर दिया है। प्रगीतात्मक कविताओं में प्रायः संवेदना कोई एक गहरा क्षण, निजी या निजीकृत क्षण, अपना आवर्तन और विस्तार करता चलता है।
द्वंद्वात्मक कविताएँ भिन्न संवेदनाओं के सघन टकराव और निकट संवाद से निर्मित होती हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में द्वंद्व वाचक ‘मैं’ और संबोध्य ‘तुम’ के बीच नाटकीय ढंग से प्रगट होता है और समूची कविता की मार्मिकता में एक अप्रत्याशित आयाम जोड़ देता है।
…अब जबकि मैं महज़ एक मनुष्याकार हूँ एक मिटा हुआ चेहरा
एक मरा हुआ नाम तुम जो कुछ हैरत और कुछ ख़ौफ़ से मेरी और देखते हो
क्या पहचानने की कोशिश करते हो
क्या तुम मुझ में अपने किसी स्वजन को खोजते हो
किसी मित्र परिचित को या ख़ुद अपने को
अपने चेहरे में लौटते देखते हो किसी चेहरे को
यहाँ मैं और तुम के बीच एक द्वंद्वात्मक संवाद घटित होता है। ‘मैं’ अगर गुजरात का मृतक है तो ‘तुम’ वह समूचा नागरिक समाज, जिसकी आँखों के सामने वह समूची प्रक्रिया घटित हुई जिसकी परिणति गुजरात जनसंहार के रूप में हुई। इस कविता में कवि महज़ एक संवेदनशील दर्शक की तरह अपनी आँखों के सामने घटित हो रहे त्रासद दृश्य को चित्रित नहीं कर रहा है। वह इस त्रासदी के ‘दर्शक’ नागरिक और ‘विक्टिम’ मृतक को एक-दूसरे के सामने ला खड़ा करता है।
इसी द्वंद्वात्मकता से 21वीं सदी की हिन्दी कविता अपनी गतिशीलता प्राप्त करती है। हिंदूराष्ट्र-परियोजना के विक्टिम और इस परियोजना को एक दर्शक की तरह अपनी आँखों के सामने घटित होते देख रहे नागरिक समाज को आमने-सामने ला खड़ा करना जैसे हिन्दी कविता का नया कार्यभार है। यह प्रक्रिया दर्शक को प्रश्नकर्ता में बदल देती है।
कविता की यह द्वंद्वात्मकता बताती है कि कवि कविता में केवल अपने ही मन की बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह कविता में अपनी ही किसी जीवन-समस्या, भावनात्मक उलझन या संवेदनात्मक गुत्थी को खोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह अपने समय की व्यापक सच्चाई का साक्षात्कार करने के लिए उसमें निहित द्वंद्वों, पारस्परिक प्रतिक्रियाओं, संवादों, बहसों और संघर्षों में गहरे उतरने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे में मैं-तुम की यह शैली उसे सबसे कारगर लगती है।
21वीं सदी की हिन्दी कविता में एक नए ढंग से ‘मैं’ की वापसी हुई है। सत्तर, अस्सी और नब्बे के दशक तक हिन्दी कविता में ‘मैं’ लगातार धूमिल होता गया था। जब कभी वह दिखाई भी देता तब ‘हम’ का विस्तार लिये होता था। एक तरफ़ तो कवि के ऊपर अपनी निजी इयत्ता को किसी बड़ी सामाजिकता या सामूहिकता में समाहित कर लेने का दबाव दिखाई देता था तो दूसरी तरफ़ रचना में रचनाकार की भूमिका ही संदिग्ध होती जा रही थी।
रोलाँ बार्थ 1967 में ही लेखक की मृत्यु और पाठक की स्वायत्तता की घोषणा कर चुके थे। यह पाठ के ऊपर लेखक की तानाशाही के अंत की घोषणा थी। पाठ के आशय का निरूपण और निर्धारण लेखक का स्वत्वाधिकार नहीं है। पाठ एक जटिल सांस्कृतिक प्रक्रिया का उत्पाद है जिसकी परिणति पाठक तक पहुँचकर होती है। ऐसे में रचना के भीतर उत्तम पुरुष ‘मैं’ का पीछे हटते जाना तर्कसंगत लगता था।
चौथाई सदी के बीतते-बीतते महा-सिद्धान्तों और लघु-सिद्धांतों की बहस भी पीछे छूट चुकी है। फलक पर क़ब्ज़ा जमाए बैठी महान सच्चाइयाँ संदिग्ध होती जा रही हैं और अगोचर दुनियाएँ सामने आने के लिए बेचैन जान पड़ती हैं। सिर्फ़ एक चीज़ असंदिग्ध है: सत्ताओं और शक्तियों के मायावी खेल। पूँजी और सैन्य शक्ति के नृशंस गठबंधन का निरंकुश राज, जिसे किसी मूल्य, आदर्श या विचार का नाम लेकर लज्जित नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा राज है जो हिंसा के विक्षिप्त महोत्सव को अनंत समय तक फैला सकता है। जो हर नए जनसंहार को अगले बड़े जनसंहार का पूर्वाभ्यास बना सकता है। 20वीं सदी ने मानव प्रगति के नाम पर जो कुछ भी हासिल किया, उसे सब कुछ को हँसते हुए कुचल सकता है। जो अपने सिवा किसी और के लिए जवाबदेह नहीं है।
ऐसे में कविता का एक ही काम रह जाता है : सत्ताओं द्वारा पहने गए ‘सत्य’ के कवच को भेदकर उन्हें निरावृत कर देना, विखंडनीय बना देना। कविता यह काम वास्तविक मानव अनुभवों की विषमता से निकले सबसे मार्मिक सवाल उठाकर ही कर सकती है। 21वीं सदी की हिन्दी कविता यही करने की कोशिश करती है। वह बुनियादी तौर पर सत्ताओं को सवालों से घेरती छापामार कविता है।
ग़ौरतलब है कि पाठकों का संसार भी एकदम बदल गया है। पहले जो केवल विषय होते थे वे ही अब लेखक भी हैं और पाठक भी। वे सभी लोग अनेक तरह की सांस्कृतिक राजनीतिक प्रक्रियाओं की खींचतान के बीचो-बीच हैं। ऐसे में रचना और पाठ की प्रक्रिया की अंतिम परिणति जहाँ हो सके, वहाँ कोई जाना-पहचाना पाठक उपलब्ध नहीं है। ऐसी अस्थिर और संदिग्ध सच्चाइयों के बीच रचना के लिए भी किसी स्पष्ट वाचक के बिना अपनी अन्विति हासिल करना और बनाए रखना पहले से कठिन हुआ है। ऐसे में यह कोई हैरानी की बात नहीं कि हिन्दी कविता में वाचक ‘मैं’ का नए ढंग से उदय हुआ है। लेकिन वह अब एकालाप की मुद्रा में नहीं है। जहाँ ‘मैं’ है वहाँ उसके सामने उसका संबोध्य ‘तुम’ भी है, भले ही प्रत्यक्ष दिखाई न दे।
यह भी सच है कि इन्हीं अस्थिर और संदिग्ध सच्चाइयों के कारण 21वीं सदी में कविता पहले से अधिक ज़रूरी हुई है। ऐसी उलझती-बदलती सच्चाइयों के बीच समझ का रास्ता बना पाना व्याकरणसम्मत गद्य के वश की बात नहीं रह गई है। गद्य में पकड़ने की हर कोशिश उन्हें सीमित, सरलीकृत और विकृत कर सकती है। कविता के लिए भी अब कोई स्पष्ट, सरल और सुनिश्चित निष्कर्ष या कथ्य संभव नहीं रह गया।
व्याकरणसम्मत गद्य का काम है, जीवन की बढ़ती हुए अव्यवस्था के बीच व्यवस्था का निर्माण करना। कविता का काम है जीवन के अव्यवस्थित, अस्थिर, अन्तःसंघर्षी और विकासमान मर्म के साक्षात्कार में बाधा बन सकने वाली व्याकरणिक संरचनाओं को ध्वस्त कर देना। गद्य ‘सामान्यता’ का निर्माण करता है, कविता विक्षिप्ति का साक्षात्कार करती है।
ज़ाहिर है ऐसी कविता ख़ुद कविता की रूढ़ हो चुकी भाषा और शैली को सबसे पहले ध्वस्त करती है। ऐसी कविता कवितानुमा दिखने से बचती है। वह अधिक से अधिक आम बोलचाल के क़रीब जाने की कोशिश करती है। 21वीं सदी की कविता इससे भी आगे जाने की कोशिश करती है। वह कविता की ही नहीं, बोलचाल की भाषा में भी वर्चस्व की संरचनाओं को पहचानती है, उन्हें ध्वस्त करने का प्रयत्न करती है।
आज की श्रेष्ठ कविताएँ वे भी हैं जो अनुभव के घमासान से गुज़रती हुई प्रश्नों के एक खुले हुए मोड़ तक पहुँचने की कोशिश करती हैं, किसी उत्तर तक नहीं।
उनकी ताक़त इस बात में दिखाई देती है कि वे आपको बेचैन करने वाले गहरे सवालों के सामने छोड़ जाती हैं, और बच निकलने का रास्ता नहीं देतीं। ये प्रतिरोधी प्रश्नवाचक कविताएँ हैं।
अगर वह आपको किसी सैद्धांतिकी या विमर्श के ज़रिये सवालों के उस मोड़ तक ले जातीं तो वे सवाल भी ऐसे होते जिनके जवाब आसानी से उन्हीं सिद्धांत और विमर्शों में ढूँढे जा सकते। लेकिन ये कविताएँ अनुभवों के घमासान से, समय के द्वंद्वों के बीच से, आपको वहाँ तक ले जाती हैं, जहाँ आसानी से मिल जाने वाले जवाब नहीं मिल सकते।
जैसे ‘गुजरात के मृतक का बयान’ की यह पंक्ति :
मेरे जीवित होने का कोई बड़ा मक़सद नहीं था
लेकिन मुझे इस तरह मारा गया जैसे मुझे मारना कोई बड़ा मक़सद हो।
सन् 2002 में ही वीरेन डंगवाल का दूसरा संग्रह ‘दुष्चक्र में स्रष्टा’ प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में शीर्षक कविता समेत अनेक कविताएँ हैं जिनमें यही द्वंद्वात्मक प्रश्नानुभूति मौजूद है।
आख़िर यह किनके हाथों सौंप दिया है ईश्वर
तुमने अपना बड़ा कारोबार?
अपना कारख़ाना बंद करके
किस घोंसले में जा छिपे हो भगवान?
कौन-सा है आख़िर, वह सातवाँ आसमान?
हे, अरे, अबे, ओ करुणानिधान!!!
सन् 2002 के वातावरण का प्रभाव शीर्षक कविता समेत संग्रह की अनेक कविताओं पर साफ़ देखा जा सकता है। अन्यत्र प्रकाशित हुई ‘रामपुर बाग़ की प्रेम कहानी’ और ‘कटरी की रुकुमिनी’ जैसी उनकी कविताएँ भी इसी प्रतिरोधी प्रश्नवाचकता की कविताएँ हैं।
सन् 2007 में असद ज़ैदी की चर्चित कविता ‘1857 : सामान की तलाश’ प्रकाशित हो गई थी। सामान की तलाश शीर्षक से उनका संग्रह भी अगले साल छपकर आ गया। इस संग्रह की कविताओं और उसके बाद आने वाली उनकी कविताओं के बारे में भी प्रतिरोधी प्रश्नवाचकता देखी जा सकती है।
1857 के मृतक कहते हैं भूल जाओ हमारे सामंती नेताओं को
कि किन जागीरों की वापसी के लिए वे लड़ते थे
और हम उनके लिए कैसे मरते थे
कुछ अपनी बताओ
क्या अब दुनिया में कहीं भी नहीं है अन्याय
या तुम्हें ही नहीं सूझता उस का कोई उपाय।
21वीं सदी की इसी रचना-प्रक्रिया का एक सिलसिला कवि अमिताभ की 2014 के बाद के परिदृश्य में आई कविताओं में मिलता है।
इन कविताओं में 2014 और उसके बाद का समय बोलता है, हालाँकि यह वही दौर है जिसका आग़ाज़ 2002 में होता है। ‘समस्तीपुर’ नौ पंक्तियों की एक छोटी-सी कविता है लेकिन यह भी मैं और तुम की उसी द्वंद्वात्मक नाटकीयता और तीक्ष्ण प्रश्नानुभूति की कविता है। इस कविता में भी ‘मैं’ एक विक्टिम की तरह आता है, जिसका ‘समस्तीपुर’ ग़ायब हो गया है। इस कविता में जिसे संबोधित किया गया है, वह ‘तुम’ भी वही नागरिक समाज है, जो समस्तीपुर के ग़ायब होने को एक दर्शक की तरह देख रहा है।
कविता में ‘समस्तीपुर’ के ग़ायब होने की तकलीफ़ है। यह तकलीफ़ पाठक को और भी गहरे सवालों में छोड़ जाती है। ‘समस्तीपुर’ इस तरह ग़ायब हो जाता है कि लगता है वो कभी था भी या नहीं। ‘समस्तीपुर’ से वाचक का प्यार भी उसे भ्रम लगने लगता है। वाचक ‘मैं’ को लगता है कि यह सब एक ग़ायब हो गई लड़की के चक्कर में होता है। ‘समस्तीपुर’ उसी का मायाजाल था और उसी के साथ ग़ायब हो गया।
जगहें, चाहे वह कोई शहर हो या कोई देश, क्या केवल अपने भूगोल और इतिहास में होती हैं? या उन सपनों में होती हैं, जिनसे वहाँ के लोग प्यार करते हैं, जिनसे अपनी जगहों को पहचनाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि सपने ग़ायब हो जाएँ और उनसे जुड़े शहर और देश उसी तरह बचे रहें? वह लड़की क्यों ग़ायब हो गई? ‘समस्तीपुर’ क्यों ग़ायब हो गया?
चौथाई सदी बाद की हिन्दी कविता केवल साहित्य के बाहर की सत्ताओं से टकराती हो, ऐसा नहीं है। वह साहित्य और संस्कृति की पूरी परंपरा से टकराती है। शायद पहली बार हिन्दी कविता अपनी ही परंपरा के बारे में वे सारे असुविधाजनक सवाल पूछने लगी है, जिन्हें पहले कभी उठने ही नहीं दिया गया।
वह अपने समय से ठीक पहले की कविता और ख़ुद अपने समय की कविता को भी सवालों के घेरे में ला रही है।
इसी अंक में मोहन मुक्त अपने वक्तव्य में कहते हैं कि हिन्दी कविता पिछली सदी के अंत तक अपनी तमाम ‘जेनेटिक’ सीमाओं के बावजूद अपने समय के वर्चस्व की राजनीतिक श्रेणियाें के सामने इतनी निरीह कभी नहीं दिखी जितनी आज दिखती है। मोहन मुक्त समूची आधुनिक हिन्दी कविता की छानबीन करते हुए यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस निरीहता की जड़ें हिन्दी कविता की सांस्कृतिक परंपरा में मौजूद हैं।
प्रतिक्रियावादी राजनीति के नवीनतम दौर का मुक़ाबला करने के लिए जिस सांस्कृतिक आग की ज़रूरत है, हिन्दी कविता में उसकी कमी दिखाई देती है। यह कमी वर्चस्व की भाषा को विखंडित कर पाने में हिन्दी कविता की असहायता में दिखाई देती है। इस अंक में मोहन मुक्त की दो कविताएँ ऐसी भी हैं जो मंगलेश डबराल और वीरेन डंगवाल जैसे 21वीं सदी के सबसे ‘सचेत’ कवियों की प्रतिष्ठित कविताओं पर काव्यात्मक प्रश्न उठाती हैं। यह कविताएँ दिखाती हैं कि कवि की वर्ण-वर्ग-अवस्थिति उसकी प्रतिरोधी चेतना को इस हद तक सीमित कर सकती है कि हो सकता है कविता उसी ख़ेमे में पड़ी हुई मिल जाए जिसका विरोध करने के लिए उठी थी।
पाठक देखेंगे कि इस अंक के अधिकांश कवियों ने अपनी-अपनी तरह से अपने वक्तव्यों और कविताओं में इन्हीं चिताओं और सवालों को उठाया है।
इस अंक की कविताएँ
इस अंक में संकलित पहले कवि विनोद कुमार शुक्ल ने आज की हिन्दी कविता पर समुचित टिप्पणी की है कि कवि स्त्रियाँ हिन्दी कविता को आगे ले जा रही हैं। उन्होंने ठीक ही पहचाना है कि हिन्दी कविता के सभी इलाक़ों में स्त्रियों के अनुभव और उनकी अभिव्यक्ति ने नई काव्य-चेतना निर्मित की है।
इस अंक में संकलित उनकी अपनी कविताओं में भी 21वीं सदी की प्रतिरोधी चेतना का स्पर्श स्पष्ट देखा जा सकता है। विनोद कुमार शुक्ल की कविताएँ हमेशा से वैचारिक उद्वेलन पैदा करने वाली अनुभूतियों के अंकन के कारण जानी जाती रही हैं। इस अंक की कविताओं में वह अनुभूति अधिक सामाजिक और अधिक राजनीतिक हुई है। उसका विस्तार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से लेकर सीरिया और मध्य पूर्व के संघर्षों तक देखा जा सकता है।
इसी अंक में संकलित मोहन मुक्त की कविताओं में ‘मैं-तुम’ की द्वंद्वात्मकता और कविता की प्रतिरोधी प्रश्नवाचकता को एक नया विद्रोही तेवर लेते हुए देखा जा सकता है।
…तुम्हारी संस्कृति की हर बात जो तुम्हें जान से प्यारी है…
वो मेरे लिए जान का खतरा है..!
यह वर्चस्ववादी सवर्ण संस्कृति के विक्टिम दलित ‘मैं’ की तरफ़ से मुख्यधारा पर उठाया गया एक विचलित करनेवाला सवाल है।
इस अंक में विहाग वैभव की कविताएँ फूलों के बीच से भी गुज़रती हैं तो वे फूल सवाल की तरह खिल जाते हैं।
‘मैं-तुम’ की शैली का प्रतिरोधी तेवर उनकी दूसरी कविताओं में भी, जैसे कि ‘तत्त्व संवाद’ में पहचाना जा सकता है।
कल्लोल चक्रवर्ती ने यह चिंता ज़ाहिर की है कि भारतीय संकट के बरअक्स हिन्दी-इतर भाषाओं में चिंता और प्रतिरोध कहीं अधिक प्रबल दिखाई देता है। यह 21वीं सदी के हिन्दी कवि की चिंता है जो उनकी कविता ‘एक स्त्री रोती है नेपथ्य में’ विक्टिम स्त्री और नागरिक ‘तुम’ के बीच द्वंद्वात्मक संवाद के रूप में घटित होती है।
पराग पावन की प्रसिद्ध बेरोज़गार-शृंखला की कुछ कविताएँ इस अंक में संकलित हैं। इन कविताओं में व्यंग्य की धार के साथ विडंबना का उपयोग शब्दों के मारक हथियार की तरह किया गया है। यहाँ उनकी एक कविता ‘जंगली बबूल के तने’ पर है, जो पृथ्वी की उन असंख्य उपेक्षित संतानों को सेलिब्रेट करती है जो ‘पृथ्वी पर बिना तर्क ही पैदा होते रहे हैं’, लेकिन जिनका आसानी से शिकार नहीं किया जा सकता, भले ही इसकी आशंका हमेशा बनी रहती हो।
अर्चना लार्क की कविताएँ ‘संकोच के गहने से बँधी हुई’ स्त्री को बौखलाते हुए प्रश्नचिह्न की तरह पुनर्जीवित करती हैं।
अनामिका अनु की कविताओं में एक स्त्री बिस्तर पर बे-सिर मिलती है, जिस का सिर खोजी कुत्ते किताबों के बीच से ढूँढ़कर निकालते हैं! दोनों स्त्रियों की वर्ग-स्थितियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन पितृसत्ता लगभग एक ही तरह दोनों का शिकार करती है।
यह आश्चर्य किंचित सुखद लगता है कि आदिवासी स्त्री के अनुभव से उपजी पार्वती तिर्की की कविताओं में स्त्री पितृसत्ता की विक्टिम की तरह दिखाई नहीं देती, जिस तरह वह निर्मला पुतुल की कविताओं में दिखती है। यहाँ वह अपने पुरुष साथी संग सहियापन की भावना के साथ नाचती-गाती दिखाई देती है। यही सहियापन पार्वती को हिन्दी कविता में कम मिलता है। सहियापन जीवन है। वही हमले की ज़द में है। जंगल उसकी पहरेदारी करता है। पाहन उसे बचाने के लिए देव और दईत दोनों से संवाद करता है। इसीलिए जंगल की कविता उनके लेखे आज की सबसे राजनीतिक कविता है।
रवि प्रकाश की कविता में ‘मैं-तुम’ की द्वंद्वात्मकता अधिक जटिल रूप लेकर आती है। ‘मैं’ और ‘तुम’ दोनों ही विक्टिम हैं लेकिन अजनबी या शत्रु ख़ेमों में नज़र आते हैं। जबकि शत्रु कोई और है, जो पूरी तरह प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसे में हवा के रुख़ का बदलना ‘बसंत के मेरे शरीर की तरह जलने’ की संभावना पर निर्भर है।
फ़रीद ख़ान की कविता में गुजरात का मृतक मुसलमान के रूप में प्रकट होता है। यह देवी प्रसाद मिश्र की कविता का मिथकीय या ‘मिथीकृत’ मुसलमान नहीं है। वह तो मिथीकरण की हर कोशिश के ख़िलाफ़ एक उबलती हुई आह है।
जमुना बीनी की कविताएँ सरकार से सीधा सवाल करती हैं। विकास हमारे लिए है या हम विकास के लिए?
कमलजीत चौधरी की कविता ‘गलियों में चाक़ू लहराते लोग’ में भी ‘मैं और तुम’ की द्वंद्वात्मकता अलग ढंग से आती है। यहाँ भी दोनों ही विक्टिम हैं, लेकिन अपने साझा दुश्मन को चाक़ू लहराते लोगों के रूप में प्रत्यक्ष देखते हैं, जो ‘शब्दों के अर्थ नहीं, सिर्फ़ इतिहास को बदलना चाहते हैं।’ शायद इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ भी अधिक हैं।
मृत्युंजय की कविताएँ प्रमाण हैं कि वे छंद के शिल्प में प्रतिरोधी प्रश्नवाचकता के निर्माण में माहिर हो चले हैं। छंद की परंपरागत लय नए समय के विस्फोटक प्रश्नों से उलझती हुई विचार की सघन लहरें पैदा करती चलती है, पर उन्हें अराजक नहीं होने देती।
इस अंक में अविनाश मिश्र की कुछ ऐसी कविताएँ संकलित हैं जिन्हें आसानी से प्रेम कविताएँ कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी आसानियाँ मुश्किल पैदा करती हैं, क्योंकि प्रेम और प्रतिरोध एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते।
अन्य के लिए शुभ का सपना देखना और मंगल की कामना करना अगर प्रेम है तो यह प्रेम स्वतः अशुभ की आशंका और अमंगल के दुस्स्वप्न का प्रतिरोध भी है।
प्रेम जीवन की व्यथा है, इसीलिए काम्य है। यह एक ऐसी व्यथा है जिससे हम जीवन को जान पाते हैं। लेकिन समय के दूसरे हिस्से में न प्रेम है, न व्यथा।
यह हमें याद दिलाता है कि हमारा समय एक अंतर विभाजित समय है।
सपना भट्ट इस अंक की कविताओं में नश्वरता, मृत्यु और शोक की पृष्ठभूमि में प्रेम, प्रणय कामना और जीवन राग के शास्त्रीय द्वंद्व को स्त्री दृष्टि से पुननिर्मित करती हैं।
यही कारण है कि उनके यहाँ इस द्वंद्व की निष्पत्ति मोक्ष की चिंता, निर्वाण भाव या आस्तित्विक अवसाद में नहीं होती, जीवन-मृत्यु के तसलसुल के वत्सल स्वीकार में होती है।
अनामिका ने इस अंक की अपनी कविताओं में प्रेम को कविता का ककहरा बताया है और कविता को प्रेम की बारहखड़ी। लेकिन यह कोई आध्यात्मिक प्रेम नहीं है। यह जीवन में रमी हुई एक स्त्री का लौकिक प्रेम है, जो उस तक हमेशा एक सुदूर पुकार की तरह आता है, हमेशा पहुँच से परे बना रहता है, लेकिन उसके भीतर जीवन के रमन चमन की गूँज भर देता है।
सविता सिंह इस अंक की अपनी कविताओं में इंटर-सेक्शनैलिटि यानी अंतर-अनुभागीयता के स्त्री विमर्श का प्रामाणिक स्वर निर्मित करती हैं। वे मनुष्यों की दुनिया से परे पेड़-पौधों, जानवर और कीड़े-मकोड़ों तक उसका विस्तार करती हैं। यहाँ स्त्री हर तरह की निम्नता के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति में ही अपनी ख़ुद की मुक्ति की संभावना भी देखती है।
शुभा इसी अंतर-अनुभागीयता को भारतीय स्त्री के वास्तविक अनुभवों और संघर्षों में स्थापित करती हैं। इन कविताओं में फ़ासीवाद एक विचार की तरह नहीं बल्कि पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों पर बरसती लाठियों-गोलियाें और दिसंबर की सर्दियों में पानी की तोपों की शक्ल में प्रकट होता है और उनसे लड़ता हुआ शाहीन बाग़ देश-भर में फैल जाता है। माँएँ लहूलुहान लोकतंत्र के लिए इस तरह लड़ती हैं जैसे कि वह अपने मृत घायल या ग़ायब हो चुके बच्चों के लिए।
मदन कश्यप ने अपनी कविताओं में सिसिफस के प्राचीन यूनानी मिथक को पुनर्जीवित करते हुए इक्कीसवीं सदी में अतिभंगुर जीवन का अभिशाप झेल रहे बहिष्कृत जनसमुदाय को कविता के केंद्र में स्थापित किया है। इस नए सिसिफस का श्रम ही नहीं, अस्तित्व भी अभिशप्त है, लेकिन यह अभिशाप उसे स्वर्ग के देवताओं से नहीं, इसी दुनिया के विधाताओं से मिला है।
देवी प्रसाद मिश्र की कविताएँ एक लंबे समय से भारत में हिंदुत्ववादी फ़ासीवाद के इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की खोजबीन और ठोंक-पीट करती आई हैं। उनकी कविता अमूर्तनों और सामान्यीकरणों से बचते हुए सीधी मुठभेड़ करने की हामी है।
‘मैं-तुम’ की द्वंद्वात्मक शैली में प्रतिरोधी प्रश्नवाचकता निर्मित करने के लिए देवी प्रसाद उमर खालिद को एक शक्तिशाली काव्य-चरित्र के रूप में स्थापित करते हैं। उमर खालिद हमारे समय में हिंदुत्ववादी फ़ासीवाद के प्रतिरोध का सबसे प्रामाणिक चेहरा है। प्रतिरोध के अनेक जटिल सवालों की पहचान करने के लिए देवी प्रसाद इस चेहरे की काव्य-संभावनाओं की गहरी खोज करते हैं। इस अंक की उनकी कविताएँ इस खोज को आंतरिक संवाद के नए शिल्प में प्रामाणिक रूप से उपस्थित करती हैं।
हमने कविता के एक ही विशेषांक की योजना बनाई थी, लेकिन काटते-छाँटते भी यह विशेषांक इतना बड़ा हो गया कि इसे तीन अंकों में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले अंक के जारी होने के बाद शीघ्र ही दूसरे दो अंक भी जारी कर दिए जाएँगे।
उम्मीद है, 21वीं सदी की इन कविताओं की प्रतिरोधी प्रश्नवाचकता आपके ध्यान में जगह बना सकेगी।
[‘आलोचना’ कविता विशेषांक : 21वीं सदी की हिन्दी कविता-1 (अंक-77) का सम्पादकीय]