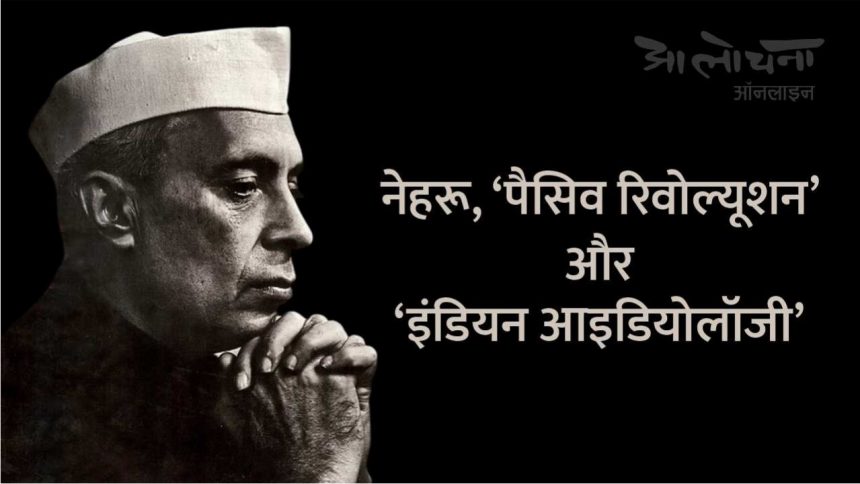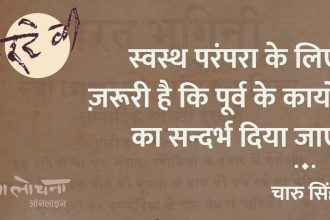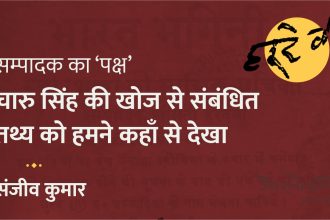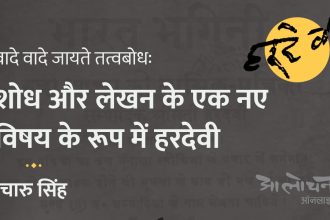नेहरू को समझने के विभिन्न आयाम रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख मार्क्सवादी स्कूल रहा है। यह लेख भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से नेहरू को समझने का प्रयास करता है। मार्क्सवादी स्कूल के अंदर भी ख़ास तौर पर दो तरह की अवधारणाएँ रही हैं जिसको ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ और ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ दृष्टिकोण कहा जा सकता है। यह लेख पार्थ चटर्जी के ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ और पैरी एंडरसन की ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ में किस तरह से नेहरू को समझा गया है, उसकी विवेचना करते हुए नेहरू की विचारधारा को उजागर करता है। जब नेहरू को मौजूदा हिंदुत्ववादी दौर में क़रीब-क़रीब ख़ारिज किया जा रहा है, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि यह देखा जाए कि नेहरू की राजनीतिक विचारधारा का सबसे प्रमुख आयाम क्या है और इन आयामों से नेहरू के दो प्रसिद्ध आलोचक किस तरह संबंध स्थापित करते हैं?
“पंडितों की सरकार में एकमात्र ग़ैर-ब्राह्मण व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू हैं।”
— बी.आर. आंबेडकर, 1950 (संदर्भ)
“नेहरू बंकिमचंद्र से कहीं कम व्यवस्थित लेखक थे…”
— पार्थ चटर्जी (संदर्भ)
“स्कॉलरशिप से भी ज़्यादा उनकी [नेहरू की] मनोवैज्ञानिक सीमा भी है—छल की क्षमता, जिसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम होने थे।”
— पैरी एंडरसन (संदर्भ)
प्रस्तावना
पार्थ चटर्जी ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ (शिथिल क्रांति) और पैरी एंडरसन ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ (भारतीय विचारधारा) के माध्यम से नेहरू का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। दोनों ही अपने अध्ययन को मार्क्सवाद के दायरे के अंदर रखते हैं। यह लेख ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ और ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ के संदर्भ में नेहरू को कैसे समझा गया है इस पर प्रकाश डालता है। इसके लिए यह विश्लेषण की एक पद्धति विकसित करता है। इस पद्धति के तीन महत्त्वपूर्ण अंग हैं— पहला, व्यक्ति-कर्म-मूल्य; दूसरा, राजनीतिक कर्म और राजनीतिक विचारधारा; और तीसरा, इतिहास की समझ। नेहरू को समझने में तीनों महत्त्वपूर्ण हैं। इसके बाद यह नेहरू के मुख्य आदर्श को उजागर करने का प्रयास करता है। ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ और ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ के संदर्भ में नेहरू को किस तरह समझा गया है, यह निरूपित करने के बाद आलेख इन दोनों फ्रेमवर्कों की पद्धति और उनमें नेहरू के मुख्य आदर्शों पर प्रकाश डालता है।
पद्धति का महत्त्व
किसी व्यक्ति को कैसे समझें? यह सवाल तब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आज़ाद भारत के शुरुआती दौर में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस क्रम में तीन बातों पर ग़ौर किया करना ज़रूरी है। पहला ‘व्यक्ति’ और उसके आदर्शों के निर्माण यानी ‘मूल्य-सृजन’ से संबंधित है। किसी भी तरह के विश्लेषण में ‘व्यक्ति’ का व्यक्तित्व और उसके ‘मूल्य-सृजन’ की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की वास्तविकता और भौतिकता को उसके मूल्य ही प्रतिबिंबित करते हैं। व्यक्ति, उसके कर्म और मूल्यों में कोई अंतर है तो उसके कारकों को बहुत ही सारगर्भित तरीक़े से बताने की ज़रूरत है। व्यक्ति-कर्म-मूल्य में एक को लेना और बाक़ी को छोड़ देना, वह भी बिना एक को दूसरे से जोड़े, काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है।
इसमें राजनीतिक कर्मकर्ता और राजनीतिक सिद्धांतकार का विभेद बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। राजनीतिक कर्म सार्वजनिक जीवन से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांतकार भी सार्वजनिक जीवन के बारे में लिखता है। राजनीतिक कर्मकर्ता की भी विचारधारा होती है जिसको ‘मूल्य’ कहा जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांतकार भी विचारधारा से प्रभावित होता है। राजनीतिक कर्मकर्ता बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है जिनमें उसकी ख़ुद के वास्तविक हस्तक्षेप की संभावना बहुत ही कम होती है। सैद्धांतीकरण के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांतकार अपने हस्तक्षेप को काफ़ी हद तक स्वतंत्र बनाए रख पाते हैं। उदाहरण के लिए एक धुर हिंदुत्ववादी राजनीतिक कर्मकर्ता भी ‘न्याय’ और ‘समावेशी समाज’ के मुहावरों को अपनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका इनमें विश्वास है। ये मुहावरे बहुत-सी परिस्थितियों की उपज हैं और परिस्थितियाँ एक हिंदुत्ववादी राजनीतिक कर्मकर्ता को भी ‘न्याय’ और ‘समावेशी समाज’―जैसी जुमलेबाज़ी का सहारा लेने को मजबूर कर देती हैं। हिंदुत्ववादी राजनीतिक सिद्धांतकार के सामने ‘न्याय’ और ‘समावेशी समाज’ बनाने की भाषा बोलने की ‘लोकतांत्रिक’ मजबूरियाँ नहीं होती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीतिक कर्मी के साथ-साथ हमें राजनीतिक सिद्धांतकार पर भी ध्यान देना चाहिए।
तीसरा आयाम ‘इतिहास की समझ’ से संबंधित है। बहुत सारे राजनीतिक कर्मी या राजनीतिक सिद्धांतकार भी इतिहासकार नहीं होते। इतिहास के बारे में समझ बनाना एक बात है और इतिहास की समझ होना दूसरी बात है। इतिहास की समझ बनाने में बहुत सारे कारक महत्त्वपूर्ण होते हैं। इनमें फौरी कारक और सहज ज्ञान की पद्धति महत्त्वपूर्ण हो जाती है। बहुत-से समाजों और व्यक्तियों ने विभिन्न परिस्थितियों में इस पद्धति को अपनाया है। उदाहरण के लिए, दुनिया-भर के उपनिवेश-विरोधी आंदोलनों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के रूबरू और भारत में जाति-विरोधी आंदोलनों ने ‘मिथकों’ के ख़िलाफ़ ‘जवाबी मिथक’ खड़े किए हैं। इनको इतिहास नहीं कहा जा सकता। इनको विखंडित (डीकंस्ट्रक्ट) किया जाए तो इनमें भविष्य के स्पष्ट संदेश (वर्तमान जैसी परिस्थितियों का नकार) भी दिखते हैं। इतिहास की समझ होना मुश्किल नहीं लेकिन यह एक संघर्षमय प्रयत्न है। इसके लिए मिथकों से बाहर जाते हुए यथार्थ को समझने की लगन होनी चाहिए। ई.एच. कार “इतिहास क्या है?” को इन शब्दों में परिभाषित करते हैं : “यह इतिहासकार और उसके तथ्यों के मध्य की सतत प्रक्रिया है, यह अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन वार्ता है।” इन तीनों बातों का ध्यान इस लेख में नेहरू को समझने में रखा जाएगा।
नेहरू : मूल्य, सिद्धांत और इतिहास
यह लेख तीन प्रस्थापना लेकर चलता है, एवं इन तीनों प्रस्थापनाओं के इर्द-गिर्द नेहरू का विश्लेषण करता है। इन तीनों प्रस्थापनाओं से पहले बी.आर. आंबेडकर की नेहरू पर टिप्पणी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यह टिप्पणी नेहरू को समझने की प्रक्रिया को और जटिल बना देती है। इन सभी को हम तीन प्रस्थापनाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहली प्रस्थापना “व्यक्ति-कर्म-मूल्य” से संबंधित है। चूँकि मूल्य ही व्यक्ति को प्रतिबिंबित करता है, लिहाज़ा यह प्रश्न पूछा जाना ज़रूरी हो जाता है कि नेहरू के मूल्य क्या थे। मेरा मानना है कि नेहरू का मूल्य “आधुनिकता” है। इसको नेहरू के धुर आलोचक समुदायवादी और पुनरुत्थानवादी भी मानते हैं और यही उनकी आलोचना का प्रमुख केंद्र है। (संदर्भ)
आधुनिकता को समझने से पहले यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि यूरोपीय पुनर्जागरण ने आधुनिकता को और आधुनिकता ने लोकतंत्र को जन्म दिया है। तीनों को एक साथ देखने की ज़रूरत है। पुनर्जागरण का सबसे बड़ा योगदान चर्च का प्रभुत्व ख़त्म करना था। इसमें “इंडिविजुअल” (व्यक्ति) महत्त्वपूर्ण था न कि दैवी शक्ति। “पुनर्जागरण ने ‘इंडिविजुअल’ को संपूर्णता के साथ जन्म दिया” जिसने आधुनिकता के आगमन को संभव बनाया। आधुनिकता का विमर्श बहुत ही समृद्ध रहा है जिसमें फ्रांसिस बेकन, गैलीलियो गलिलेई, रेने देकार्त, इमैनुएल कांट, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, नीत्शे, और हेबरमास का योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है।
आधुनिकता वास्तव में तत्त्वमीमांसा (मेटाफिज़िक्स) और ज्ञानमीमांसा (एपिस्टेमोलोजी) का मिलाप/कन्वर्जेंस है। आधुनिकता तत्त्वमीमांसा में “मैटर” (तत्त्व) पर ज़ोर देती है और ज्ञानमीमांसा से रीज़न (तर्क) को लेती है जो अनुभववाद (एंपिरिसिज्म) पर आधारित है। दूसरे शब्दों में आइडिया (भाव) को नकारते हुए भौतिकता पर ज़ोर दिया जाता है। यहाँ पर तर्क और अनुभवजन्य यथार्थ (empirical reality) का मिश्रण होता है।
आधुनिकता को आधुनिकीकरण से अलग करके देखना ज़रूरी है। आधुनिकता में अन्वेषण बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर किसी भी तरह की “मान्यता” की जगह नहीं होती है। आधुनिकता हर तरह की “शाश्वत” और “ग़ैर-आलोचनात्मक” प्रस्थापनाओं को ख़ारिज करती है। इसमें रूढ़िवाद, अंधविश्वास और दैविक आदेशों को सिरे से ख़ारिज कर दिया जाता है। इस तरह हर तरह के शोषण के ख़िलाफ़ आधुनिकता एक मुक्तिदायी माध्यम बन जाती है। आधुनिकता में “लगातार प्रश्न” किया जाता है। आधुनिकता एक पद्धति है, एक दृष्टिकोण है। इसमें सभी प्रक्रियाओं को द्वंद्ववाद और विज्ञान के माध्यम से समझा जाता है।
आधुनिकता और आधुनिकीकरण दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। कोई चाहे तो आधुनिकता को गले लगाए बिना भी आधुनिकीकरण को अपना सकता है। आधुनिकीकरण तकनीकीकरण के साथ-साथ इसके उत्पादों का उपभोग करने की परिघटना है। बहुत सारे समाजों में पुरातनपंथी भी आधुनिकीकरण को अपनाए प्रतीत होते हैं। ये वही लोग हैं जो खाप पंचायतों का भी नेतृत्व करते हैं।
लेकिन अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाक़ी है कि नेहरू में आधुनिकता के क्या प्रमाण हैं? नेहरू और आधुनिकता के संबंधों की विवेचना और सत्यापन अभी बाक़ी है। आधुनिकता को “समुदायवाद” और “पुनरुत्थानवाद” के विरोध के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आधुनिकता का दुनिया-भर में सबसे ज़्यादा विरोध “समुदायवादियों” और “पुनरुत्थानवादियों” ने ही किया है। आधुनिकता तथा पुनरुत्थानवाद और समुदायवाद दो ध्रुव हैं।
नेहरू पर हुए अध्ययन में उनकी राजनीतिक जीवनी की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण रही है। हालाँकि यह प्रश्न विचलित करता है कि इनमें आधुनिकता को क्यों कोई जगह नहीं मिली। नेहरू को कई तरीक़ों से समझा गया है। माइकल ब्रेचर नेहरू के माध्यम से भारतीय इतिहास और राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वपल्ली गोपाल उन्हें अंतरराष्ट्रीय विवेक के प्रवक़्ता के बतौर पेश करते हैं। जुडिथ ब्राउन उनकी जीवनी के माध्यम से भारतीय राजनीति को समझने की चेष्टा करते हैं। वहीं बेंजामिन ज़कारिया सामाजिक शक्तियों को समझने के लिए ऐतिहासिक जीवनी की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं।
अलग-अलग लेखकों ने नेहरू के विचारों के अलग-अलग पक्षों पर ज़ोर दिया है। नीरा चंढोक जहाँ अंतरराष्ट्रीयता और रेडिकल विश्वबंधुत्व के पक्ष पर बल देती हैं, वहीं रजनी कोठारी “स्थिरता” और “आम-सहमति” पर, एम.एल. दाँतवाला योजना आयोग और औद्योगीकरण पर, एच.के. मनमोहन सिंह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, वी.के.आर.वी. राव और पी.सी. जोशी मिश्रित अर्थव्यवस्था के पूँजीवादी दिशा में चले जाने पर, बी.आर. नायर बिचौलियों को कम आँकने पर और सब्यसाची भट्टाचार्य श्रमिक अधिकारों के संबंध में उनके विचारों पर। इसके अलावा नेहरू को समझने के लिए विद्वानों ने “उत्थान-पतन” और “लोकप्रिय-अलोकप्रिय-लोकप्रिय” की अवधारणाओं का भी इस्तेमाल किया है। कई विचारकों ने 1933-36 के कालखंड को नेहरू की विचारयात्रा का “मार्क्सवादी” चरण माना है। साथ ही, नेहरू के सबसे बड़े योगदानों में आस्था को ग़ैर-धार्मिक स्वरूप देना, “सेकुलर राज्य” का निर्माण करना, राज्य की तुलनात्मक स्वायत्तता को स्थापित करना माना गया है। इन सारे महत्त्वपूर्ण अध्ययनों में ‘आधुनिकता’ पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना दिया जाना चाहिए था।
लाहौर कांग्रेस (29 दिसंबर 1929, लाहौर) में नेहरू का अध्यक्षीय भाषण आधुनिकता के विमर्श के माध्यम से दुनिया में लगातार होनेवाले परिवर्तनों की बात करते हुए श्रम के महत्त्व को उजागर करता है और एक नई दुनिया के जन्म की बात करता है। “मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प” (द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकॉनोमिक प्रोग्राम, 1931) नेहरू की विचारयात्रा का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। इसे नेहरू ने लिखा था जिसे गांधी के थोड़े फेरबदल के बाद कराची कांग्रेस ने 1931 में अपनाया था। आधुनिकता के तीन महत्त्वपूर्ण अंगों (व्यक्ति, समाज और राज्य) को, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, इसमें काफ़ी प्रमुखता दी गई है। इसमें व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी गई है; धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर सार्वजनिक रोज़गार या व्यापार में पक्षपात करने की मनाही की गई है; और समाज से संबंधित अधिकारों में “संघ और संयोजन की स्वतंत्रता”, “भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता”, “सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन अंतरात्मा की स्वतंत्रता” और “धर्म को मानने और कर्म की स्वतंत्रता” को शामिल किया गया है। राज्य को अधिकार-संबंधी विमर्श (rights discourse) के ज़रिए धर्म से अलग किया गया है।
नेहरू का लखनऊ कांग्रेस का अध्यक्षीय भाषण (18 मई 1936) पूरी तरह समाजवाद का अनुमोदन करता है। नेहरू पूरे भाषण में आक्रामक तरीक़े से समाजवाद का पुरज़ोर समर्थन करते हैं। नेहरू कहते हैं कि वे आश्वस्त हैं कि दुनिया और भारत की समस्या के समाधान की कुंजी केवल समाजवाद में निहित है। समाजवाद का मतलब अस्पष्ट मानवीयता नहीं है। समाजवाद वैज्ञानिक और आर्थिक है। वे यह भी कहते हैं कि समाजवाद महज़ आर्थिक सिद्धांत नहीं है बल्कि उससे भी ज़्यादा कुछ है। यह जीवन का दर्शन है और इसके इसी रूप ने मुझे लुभाया है।37 नेहरू के लिए यह एक नई सभ्यता है। यह नई सभ्यता “व्यक्ति, समाज और राज्य” को “सामुदायिक मनुष्य, समुदाय और राज्य-धर्म” के स्थान पर स्थापित करती है। इसी संदर्भ में नेहरू का भाषण “ट्रिस्ट विद डेस्टिनी” (अगस्त 14-15, 1947) कई मायने में महत्त्वपूर्ण हो जाता है। नेहरू कहते हैं कि “वर्षों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को पूरी तरह न सही, लेकिन काफ़ी हद तक निभाएँ। आज रात बारह बजे, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। ऐसा क्षण, जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने को छोड़, नए की तरफ़ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है।”
नेहरू की तीन किताबों में आधुनिकता के प्रश्न को सारगर्भित तरीक़े से उठाया गया है। विश्व इतिहास की झलक (Glimpses of World History) (1934) में पुनर्जागरण को बहुत ही सकारात्मक तरीक़े से देखा गया है। पुनर्जागरण सीखने का पुनर्जन्म था। यह कला, विज्ञान और साहित्य एवं यूरोपीय देशों की भाषाओं के विकास का समय था। नेहरू कुस्तुंतुनिया के पतन को तारीख़ी घटना मानते हैं; इसे एक युग के अंत और नए युग की शुरुआत मानते हैं। यहाँ मध्य युग ख़त्म हो जाता है; 1000 वर्ष का अंधकार युग समाप्त होता है। यूरोप में स्पंदन है और नया जीवन और नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। इसको पुनर्जागरण यानी सीखने और कला के पुनर्जन्म की शुरुआत कहा जाता है। लोग लंबी नींद के बाद जागृत लग रहे हैं। यूनान के महान दिनों से प्रेरणा लेते दिख रहे हैं। चर्च ने मानव जीवन को हताशा और जंजीर से बाँध रखा था, मनुष्यता के सार को बंधक बना रखा था, उसके ख़िलाफ मानव-मन ने विद्रोह कर दिया है। सुंदरता के प्रति पुराना यूनानी प्रेम प्रकट हो रहा है, और यूरोप की चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला को नया जन्म मिला है।
नेहरू लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, रफाएल, कोपरनिकस और जिओरडानो ब्रूनो के योगदान का सगर्व वर्णन करते हैं। नेहरू चार्ल्स डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ़ स्पिसीज को सामाजिक तौर पर महत्त्वपूर्ण मानते हैं। नेहरू के अनुसार डार्विन की पुस्तक युगांतरकारी थी; इसने बहुत-ही बड़ा असर डाला और वैज्ञानिक कार्य से ज़्यादा इसने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद की। इसने जनमानस में एक युगांतरकारी चिंतनपरक उद्वेलन को जन्म दिया और डार्विन को प्रसिद्ध बना दिया।
एन ऑटोबायोग्राफी (1936) उनके राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों का केंद्र बिंदु है। यह आत्मकथा गांधी के साथ उनके संबंधों और नीतियों के मामले में असहमतियों को “मतभेद” मानती है, “मनभेद” नहीं। उनके आधुनिकतावादी राजनीतिक और सामाजिक मूल्य धार्मिक कट्टरवादियों पर हमला किए बिना स्थापित नहीं हो सकते। इस किताब में यही किया गया है। नेहरू का मानना था कि वास्तविक संघर्ष हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में नहीं है, बल्कि इन दोनों संस्कृतियों और आधुनिक सभ्यता की वैज्ञानिक संस्कृति के बीच है। नेहरू कहते हैं कि उन्हें कोई संदेह नहीं कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों का आधुनिक सभ्यता की मुख़ालफत का प्रयास असफल ही रहेगा और उन्हें उनकी इस असफलता से कोई खेद नहीं होगा। नेहरू के अनुसार उनका मुख्य लक्ष्य वर्ग-रहित समाज है, जहाँ पर आर्थिक न्याय और सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। जो कोई भी इसमें बाधा बने उसको हटाना ही होगा चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े।
नेहरू अपनी तीसरी और आख़िरी किताब भारत की खोज (Discovery of India, 1946) में “अतीत” को लेकर बहुत ही सजग हैं। वे कहते हैं कि भारत को अतीत के ज़्यादातर हिस्सों से संबंध तोड़ लेना चाहिए और उसे वर्तमान पर हावी होने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। नेहरू जाति-प्रथा पर जमकर वार करते हैं। जाति हिंदुओं के बीच ख़ासियत का प्रतीक और इसकी अभिव्यक्ति है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि जाति के मूल विचार को रखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद के हानिकारक विकास और नतीजों को हटाया जाना चाहिए। यह भी कि इसका आधार जन्म न होकर योग्यता होना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल अप्रासंगिक है बल्कि मुद्दे से भटकाता भी है।
ऐतिहासिक संदर्भ में जाति के विकास के अध्ययन के कुछ मूल्य हैं, लेकिन हम उस काल में वापस नहीं जा सकते। आज के सामाजिक संगठन में इसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर केवल योग्यता कसौटी है, और सबको समान अवसर उपलब्ध है, तो जाति सभी वर्तमान विशिष्टताओं को खो देती है और वास्तव में समाप्त हो जाती है। जाति ने न केवल अतीत में कुछ समूहों का दमन किया है, बल्कि बड़ी चतुराई से सैद्धांतिक और शैक्षिक सीख से वास्तविक जीवन और उसकी समस्याओं को अलग-थलग कर दिया। यह परंपरावाद पर आधारित एक अभिजात्य दृष्टिकोण था।
पुनर्जागरण के दौरान आधुनिकता ने ज्ञान-मीमांसा के साथ-साथ, “व्यक्ति”’, “समाज” और “राज्य” की संकल्पना पर भी गहरा असर डाला। (संदर्भ) सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 14वीं और 15वीं सदी के मानवतावादियों ने चिंतन के लिए वातावरण तैयार किया। अब व्यक्ति दैवी शक्ति का निमित्त मात्र नहीं रह गया। वह किसी पूर्व-निर्धारित/नियोजित प्रणाली का हिस्सा नहीं था। उसका स्थान स्थिर नहीं था। सीधे सरल शब्दों में, पुनर्जागरण से निकली आधुनिकता की रूपरेखा के अंतर्गत व्यक्ति अब अधिकारप्राप्त प्राणी बन गया। उसका अस्तित्व उसके कार्यों के उपरांत उसके अधिकारों से संबंधित था। इस तरह के व्यक्ति की कल्पना ने एक अलग तरह के समाज (समाज) को जन्म दिया। यह समाज पाँच कारणों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। पहला, समाज पूर्व-निर्धारित परिघटना नहीं है। दूसरा, चूँकि यह पूर्व-निर्धारित परिघटना नहीं है, इसलिए इसकी स्थिरता/जड़ता से इनकार किया जाता है। तीसरा, स्थिरता को नकारने से, सैद्धांतिक तौर पर, समाज पूरी तरह से भौतिक परिघटना बन जाता है। चौथा, समाज गतिशील संस्था है। पाँचवाँ, चूँकि समाज संस्था है, इसलिए इसमें लोग अंदर या बाहर रहने का निर्णय स्वयं लेते हैं। वास्तव में समाज आधुनिक परिघटना है, जहाँ से “पब्लिक”-जैसी संस्था का गठन होता है।
राज्य के संदर्भ में पुनर्जागरण-आधुनिकता के ढाँचे ने असीमित योगदान दिया है। इसके चलते राजनीतिक समुदाय-जैसी संकल्पना का उद्भव हुआ। यहाँ पर इसका योगदान राज्य (State) और धर्म के संदर्भ में और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। पुनर्जागरण-आधुनिकता के ढाँचे में लोग राजनीतिक संस्था के प्रस्थान-बिंदु होते हैं, और उसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर राज्य को धार्मिक नियंत्रण में रखने की संकल्पना को पूरी तरह से ख़ारिज कर दिया जाता है। धार्मिक योजना (theological schema) में राज्य के नियम, उसकी भूमिका और संबंध पूर्व-निर्धारित होते हैं। इसको और विस्तार से बताने की ज़रूरत है। धर्म एक “पूर्वसिद्ध” (a priori) संस्थान है। इसकी मुख्य “वैधता” स्थिर है। धर्म का विस्तार तो हो सकता है, लेकिन इसकी मुख्य वैधता का विस्तार होना नामुमकिन होता है। मुख्य वैधता का मतलब “शाश्वत मूल्य” के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है। ये शाश्वत मूल्य “पूर्वसिद्ध” होते हैं। समस्या तब आती है जब राज्य और धर्म को जोड़ दिया जाता है।
अगर हम राज्य को न्यूनतावादी दृष्टिकोण (minimalist standpoint) से भी देखें तो यह एक “क्रमिक विकासी संस्था”’ (evolutionary institution) है। क्रमिक विकासी संस्था का आशय यहाँ पर बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति का प्रतिबिंब होने से है। बुर्जुआ राज्य भी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को नकार नहीं सकता है। धर्म को राज्य से जोड़ने से इसकी प्रकृति में परिवर्तन आता है। शाश्वत मूल्य पूर्वसिद्ध होने से राज्य का क्रमिक विकासी स्वरूप बदल नहीं जाता। इसके दो त्वरित परिमाण होते हैं। पहला, शाश्वत मूल्य को बड़े स्तर पर वैधता मिलती है। दूसरे, जो इस शाश्वत मूल्य से संबंधित नहीं होते हैं (या किसी पूर्वसिद्ध शाश्वत मूल्य जैसे नहीं होते) उनको “बहिष्कृत” कर दिया जाता है। इस बहिष्करण को रोकने के लिए ही राज्य और धर्म का अलग-अलग होना ज़रूरी है।
इनके आठ प्रमाण नेहरू में मिलते हैं : पहला, नेहरू की आधुनिकता में व्यक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसका अस्तित्व सबसे पहले आता है। व्यक्ति को अधिकार दिए जाने की वकालत की जाती है, जिसे किसी भी क़ीमत पर वापस नहीं लिया जा सकता। दूसरा, नेहरू व्यक्ति को राजनीतिक श्रेणी मानते थे। कांग्रेस को उच्च वर्गों तक सीमित न रख आम जनता में ले जाने के प्रयत्न को उनकी एन ऑटोबायोग्राफी में देख सकते हैं। तीसरा, नेहरू व्यक्ति को किसी भी ख़ास दृष्टि (ख़ास तौर से जन्म पर आधारित) से देखने से मना करते थे, यह बहुत ही स्पष्ट है। यह उनके धर्म, जाति के विरोध से देखा जा सकता है। चौथा परंपरा से जुड़ा है। नेहरू परंपरा को अस्वीकार करते थे। इसके लिए वह “परंपरा” और “अतीत” में अंतर करते थे। परंपरा किसी भी वस्तु को बिना छानबीन के अपनाने का समर्थन करती है। इसमें आलोचनात्मक परीक्षण (critical examination) का अभाव दिखता है। हो सकता है कि अतीत में बहुत कुछ अच्छा हुआ हो, लेकिन परंपरा सोचने की प्रक्रिया को कुंद कर देती है। पाँचवाँ, नेहरू निरंतरता को इसलिए भी नकारते हैं, क्योंकि निरंतरता परंपरा को जन्म देती है। छठा, नेहरू राज्य और धर्म में अंतर करते हैं। यह बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि धर्म अधिकार-आधारित संस्था नहीं है। धर्म को राज्य के साथ लाने या जोड़ने का मतलब ही हुआ कि लोग अधिकारविहीन हो जाते हैं, क्योंकि धर्म के अंदर अधिकार आधारित विमर्श का होना नामुमकिन है। धर्म और राजनीति के संबंधों के बारे में नेहरू ने 17 मई 1928 के द बंबई क्रॉनिकल में लिखा था कि “भारत में तथाकथित धर्म आज जीवन के हर क्षेत्र—आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक—का अतिक्रमण कर रहा है और मैं इस पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूँ। इस अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर धर्म या धर्म-जैसी किसी और चीज़ का हस्तक्षेप भारत में जारी रहता है, तब इसे सिर्फ़ राजनीति से अलग करने का प्रश्न नहीं उठता, बल्कि जीवन से ही इसे अलग करना होगा।” सातवाँ, नेहरू अधिकार-आधारित संस्था की संकल्पना करते हैं। आठवाँ, नेहरू सार्वजनिक तर्क (public reasoning) को वैज्ञानिक मनोभाव (scientific temper) में बदल देने के लिए आग्रह करते हैं। सार्वजनिक तर्क से धर्म-आधारित राज्य ख़त्म हो जाता है। यह आधुनिकता व्यक्ति को अधिकार देती है, समाज को परंपरा से मुक्त कराती है, और अधिकार-आधारित राज्य की कल्पना करती है।
नेहरू के मूल्य और राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के बाद अब हम “कर्म” वाले प्रश्न पर आते हैं। आधुनिकता सिर्फ़ “विश्लेषणात्मक श्रेणी” (analytical category) नहीं है। यह बहुत हद तक कर्म से जुड़ी प्रक्रिया है। कर्म का पक्ष बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में यह पूछा ही जाना चाहिए कि क्या नेहरू “आधुनिकता” को इसके मुकाम पर पहुँचा पाए थे? इसके जवाब में यह कहना पड़ेगा कि नेहरू आधुनिकता को लेकर कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। अगर हम कांग्रेस का ही मूल्यांकन करें और नेहरू के विश्लेषण का सहारा लें, जैसा कि वह अपनी आत्मकथा में करते हैं, तो पाते हैं कि कांग्रेस में ही रूढ़िवादी लोग भरे हुए थे।55 कांग्रेस में रूढ़िवाद 1930 के दशक से ही मज़बूत हो चुका था।
जिन लोगों ने भी 1930 के दशक की कांग्रेस को देखा था और उस कांग्रेस में शामिल थे और वामपंथी झुकाव रखते थे, उन्होंने ख़ुद को संगठन से बाहर रखने की ज़रूरी क़वायद शुरू की। संगठन ने दक्षिणपंथ की तरफ़ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के अंदरूनी समूहों में अब कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी भी शामिल थी। यह एक दक्षिणपंथी पार्टी थी, जिसका झुकाव हिंदू हितवाद की तरफ़ ही था। मदनमोहन मालवीय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी समूह के लोग इसके कर्ता-धर्ता थे। कांग्रेस के बहुत-से सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य थे, जो निस्संदेह सांप्रदायिक (sectarian) संगठन था। कांग्रेस में बहुत सारे लोग दोहरी सदस्यता वाले भी थे और वे इस तरह के संगठनों के भी सदस्य थे।
सत्ता का विधिवत हस्तांतरण होने के कुछ दिनों तक, हिंदू दक्षिणपंथ और पूँजीवादी दक्षिणपंथ कांग्रेस के अंदर और बाहर भी था। यह भी सच है कि कुछ समय तक कांग्रेस के अंदर और बाहर के दक्षिणपंथियों ने एक-दूसरे को पहचाना नहीं था।
इस संदर्भ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (जो भारत के प्रथम शिक्षामंत्री बनने के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे) की महत्त्वपूर्ण किताब इंडिया विन्स फ्रीडम में वर्णित दो घटनाओं का ज़िक्र करना उचित होगा। “गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935” के बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी। इसके बावजूद बंबई और बिहार प्रांत के दो सबसे बड़े नेताओं (नरीमन और सईद महमूद) को, जो ग़ैर-हिंदू थे, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया।
ऊपर दिए गए विवरण यह बताते हैं कि नेहरू के समय दो तरह का विकास देखने को मिलता है। कांग्रेस क़रीब-क़रीब रूढ़िवादी दल में तब्दील हो चुकी थी, जिस पर दक्षिणपंथी हिंदूवादियों की पकड़ और मज़बूत हुई थी। इस संदर्भ में हिंदू कोड बिल का ज़िक्र करना उचित होगा। रेबा सोम का अध्ययन इस पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालता है। हिंदू कोड बिल न पास के होने की वजह से निराश आंबेडकर ने सितंबर 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। बाद में नेहरू ने इसको चार चरणों में पास करवाया : मई 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया; मई 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया गया; हिंदू दत्तक ग्रहण और अनुरक्षण अधिनियम दिसंबर 1956 में और जुलाई 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। इसको सोम “प्रतीकात्मक” कहती हैं जिसमें “सार” कम था। जिन लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया उनमें चार समूह प्रमुख थे : कांग्रेस के कट्टर रूढ़िवादी (वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी); कांग्रेस के हिंदू कट्टरपंथी (तत्कालीन डिप्टी-स्पीकर एम.ए. अय्यंगर); हिंदू महासभा और उसकी महिला इकाई (श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एन.सी. चटर्जी व अन्य लोगों ने हिंदू समाज की धार्मिक नींव के लिए ख़तरा बताते हुए बिल का विरोध किया); सिख समूह (सरदार मान और हुकुम सिंह ने हिंदुओं के दायरे में सिखों को लाने के चलते इसका विरोध किया); मुस्लिम समूह (बंगाल के नाज़िरुद्दीन अहमद को कांग्रेस के कट्टरपंथी समूह ने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया); और महिला सांसद (जिन्होंने इसके महत्व को तो माना लेकिन इसे नाकाफ़ी बताया)। हिंदू कोड बिल (1951) के पास न होने के लिए आंबेडकर ने प्रधानमंत्री के “वादे” और “अमल” में अंतर को ज़िम्मेदार ठहराया था। अकील बिलग्रामी भी नेहरू को कांग्रेस के अंदर सांप्रदायिक हिंदू तत्त्वों को नियंत्रित करने में विफल मानते हैं।
दूसरा, नेहरू लगातार 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे; यह समय आधुनिकता को और आगे ले जाने का था। प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए था परंपरावादी जकड़नशील शक्तियों को कमज़ोर करना। इसके विपरीत नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में इस तरह का कोई आंदोलन नहीं हुआ। यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रहते कोई भी उदारपंथी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आंदोलन नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सही है कि आधुनिकता बिना आंदोलन के आगे नहीं बढ़ सकती। इस संदर्भ में ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद का आकलन महत्त्वपूर्ण हो जाता है। नंबूदिरीपाद कहते हैं कि प्रधानमंत्री नेहरू और स्वतंत्रता आंदोलन के वामपंथी नेतृत्व के नेहरू में अंतर है। उन्होंने राज्य पर परिवर्तन लाने को लेकर ज़्यादा भरोसा किया।
अब हम तीसरे मुद्दे पर आते हैं जो इतिहास की समझ से संबंधित है। नेहरू की सबसे ज़्यादा आलोचना, इतिहास की समझ को लेकर, ख़ास तौर पर उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया को लेकर होती है। इतिहास के आते ही राष्ट्रवाद का भी प्रश्न आता है। अंशुमन मंडल का मानना है कि भारतीय राष्ट्रवाद हमेशा खुलेआम या छुपकर हिंदू रूपकों का सहारा लेता रहा है और इसलिए इसका सार धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इस मसले पर जावीद आलम महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हैं। आलम के अनुसार नेहरू “रेडिकल लिबरल” हैं, जब वे “राष्ट्र” (नेशन) के बारे में बात करते हैं, तो ख़ुद ही वह अपनी बौद्धिक पहचान से अलग नज़र आते हैं। आलम के अनुसार, निस्संदेह यह सच है कि राष्ट्र की उनकी अवधारणा में भविष्योन्मुख लक्ष्य (औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास, विज्ञान और वैज्ञानिकता, लोकतांत्रिक सामाजिक संबंध, धर्मनिरपेक्ष समाज, समाजवादी सामाजिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था इत्यादि) समाहित हैं। यही वजह है कि नेहरूवादी राष्ट्रवाद की भावना संकीर्ण राष्ट्रवाद की धारणा से मेल नहीं खाती है। उनका राष्ट्रवाद उदार और समावेशी है, और इसलिए वह साम्राज्यवाद-विरोध के बंधनों से परे जाता है। भारतीय राष्ट्र की उनकी मूल भावना, सामान्य रूप में राष्ट्रों की अवधारणा से बहुत अलग है। पर नेहरू अपने साथियों और पूर्ववर्तियों से अलग नहीं बल्कि उन्हीं की धुन में दिखाई देते हैं। वह उसी शृंखला की कड़ी के रूप में सामने आते हैं जो 1880 के दशक में सांस्कृतिक पुनरुद्धार के साथ शुरू हुई थी।
आलम के इस महत्त्वपूर्ण विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर नज़र डालें तो नेहरू भी “प्राचीनता की भावना से मुक्त” नहीं हो पाए थे। अलेक्स टिक्केल भी नेहरू में “आदिकाल के प्रति लगाव” (primordial rootedness) देखते हैं।68 लेकिन यहाँ पर हम फिर नेहरू को इतिहासकार के तौर पर समझने की भूल कर देते हैं। अगर नेहरू ने ख़ुद ही इतिहास की अपनी समझ को बहुत गंभीरता से लिया होता तो “समावेशी राष्ट्रवाद” की संकल्पना वे कर ही नहीं पाते। अगर हम डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया की विरचना (डीकंस्ट्रक्ट) करें तो कुछ बातें समझ में आ जाएँगी। इसको साम्राज्यवादी शक्तियों के बरअक्स “मिथ” के ख़िलाफ़ “जवाबी मिथ” खड़ा करने के तौर पर देखना चाहिए। इसको इतिहास नहीं कहा जा सकता। इसमें भविष्य के स्पष्ट संदेश भी दिखते हैं। जैसा कि सुदीप्त कविराज का मानना है कि इतिहास लेखन का उपक्रम भी इतिहास का ही एक हिस्सा है।
नेहरू, पैसिव रिवोल्यूशन और इंडियन आइडियोलॉजी
अंतोनियो ग्राम्शी ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें राज्य का सुधार अतीत से पूर्ण संबंध-विच्छेद की प्रक्रिया अपनाए बिना ही किया जाता है। ग्राम्शी के अनुसार, “पैसिव रिवोल्यूशन न सिर्फ़ इटली पर बल्कि हर उस देश पर लागू होता है, जो सिलसिलेवार सुधार या राष्ट्रीय युद्ध के माध्यम से रेडिकल-ज़ेकोबिन सरीखी राजनीतिक क्रांति को अपनाए बिना राज्य का आधुनिकीकरण करते हैं।” मोर्टन के अनुसार, “पैसिव रिवोल्यूशन दो भागों में विभाजित होनेवाले पोर्तमोंतो (सूटकेस) जैसा है जो पूँजीवाद के अंदर निरंतरता और परिवर्तन दोनों को दर्शाता है।” भारतीय संदर्भ में पार्थ चटर्जी ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ का प्रयोग करते हैं। पार्थ चटर्जी अपनी किताब Nationalist Thought and the Colonial World (राष्ट्रवादी सोच और औपनिवेशिक दुनिया) में नेहरू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उनकी इस किताब से कुछ महत्त्वपूर्ण अंशों को विस्तार से उद्धृत करूँगा। वे मानते हैं कि ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ वह पुनर्निर्माण (reconstruction) था जिसका विशेष मक़सद राष्ट्रवाद को राज्य की विचारधारा की परिधि के भीतर स्थापित करना था। औपनिवेशिक सामाजिक गठन के तहत भारतीय पूँजीपति वर्ग के समक्ष उपस्थित ऐतिहासिक अवरोधों के कारण इसका बौद्धिक-नैतिक नेतृत्व मज़बूती से नागरिक समाज में कभी ख़ुद को स्थापित नहीं कर पाया। ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इसकी क्रांति सिलसिलेवार या शिथिल यानी “पैसिव” ही होनी थी। भारत में ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ का विशिष्ट वैचारिक रूप अधिनायकवादी राज्य-नियंत्रित (etatisme) था, जिसके केंद्र में एक केंद्रीकृत और स्वायत्त राज्य की भूमिका प्रमुख थी। प्रगति और सामाजिक न्याय के विचारों के बीच एक विशेष राष्ट्रवादी गठबंधन के ज़रिए इसे वैधता प्रदान करने का प्रयास किया गया। नेहरू बंकिमचंद्र की तुलना में कम व्यवस्थित लेखक थे और उनके लेखन में बहुत ठोस तार्किकता नहीं थी जो गांधी में नैतिक प्रतिबद्धता के कारण दिखती है। उनकी दो प्रमुख किताबें, आत्मकथा और भारत की खोज कारावास की लंबी अवधि के दौरान लिखी गई थीं और मोटे तौर पर छिटपुट विचारों का जमावड़ा (रैमब्लिंग) हैं और इनमें अंतर्विरोध कूट-कूट कर भरा हुआ है। ख़ुद नेहरू के अनुसार, जब काग़ज़ की आपूर्ति ख़त्म हो गई तो किताबों का लिखना उन्होंने बंद कर दिया। चटर्जी राष्ट्रवाद के अंतिम वैचारिक पुनर्निर्माण का प्रमुखता से ज़िक्र करते हैं। यह एक विचारधारा है जिसका केंद्रीय सिद्धांत राज्य की स्वायत्तता है; सामाजिक न्याय की अवधारणा इसकी वैधता का सिद्धांत है।
पार्थ चटर्जी “इस” तर्क को आगे समझाते हैं : “सभी के लिए सामाजिक न्याय का प्रावधान इस पुराने ढाँचे के अंदर नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पुराना पड़ चुका है, अवनति का शिकार है और गतिशीलता खो चुका है। यह ज़रूरी है कि संस्थानों का नया ढाँचा तैयार किया जाए जो प्रगति या आधुनिकता की भावना को समाहित कर सके। बीसवीं सदी की शर्तों के अनुसार, प्रगति या आधुनिकता का मतलब आर्थिक क्षेत्र को प्राथमिकता देना है, क्योंकि केवल आर्थिक उत्पादन और वितरण की व्यवस्था के पुनर्गठन से ही पर्याप्त धन जुटाया जा सकता है ताकि सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।”
नेहरू के लिए वैज्ञानिक विधि का मतलब सामाजिक सवालों से ज़्यादा आर्थिक क्षेत्र को प्रधानता देने से रहा है। हर मामले में, तर्क इस प्रकार से थे : वर्तमान में अर्थव्यवस्था की सिर्फ़ एक ही ऐतिहासिक दिशा हो सकती है और वह है तेज़ी से औद्योगीकरण की दिशा। इसलिए परिपक्व राष्ट्रवाद के वैचारिक ढाँचे के भीतर आर्थिक विकास के रास्ते को स्पष्ट रूप से समाज और इतिहास की “वैज्ञानिक” समझ के साथ स्थापित किया गया था। आर्थिक विकास के इस रास्ते की तीन बुनियादी शर्तें थीं : भारी इंजीनियरिंग और मशीन-निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और बिजली उत्पादन।
नेहरू सरीखे राष्ट्रवादियों ने “आर्थिक प्रधानता”—जैसे उपयोगी सिद्धांत का प्रयोग करने के क्रम में मार्क्सवाद के तर्कवादी (रेशनलिस्ट) और समतावादी पक्ष को अपनाया लेकिन इसकी मुख्य राजनीति को छोड़ दिया। राष्ट्रवादी विचार द्वारा जो वैचारिक पुनर्निर्माण शुरू हुए उन्होंने एक स्वायत्त राष्ट्र-राज्य के विचार को सबसे ज़्यादा तरज़ीह दी। यह एक ऐसा राज्य है जो सबको समाहित करता है, लिंग, धर्म, जाति, धन या भाषा पर ध्यान दिए बिना सबको नागरिकता का बराबर अधिकार देता है। विशेष रूप से, इसको राष्ट्रीय एकजुटता की चेतना पर आधारित होना चाहिए जिसमें बड़े स्तर पर किसान सक्रिय राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हों।
किसान ग़रीब हैं, अनपढ़ हैं, कल्पनालोक में नहीं रहते और बिना ज़्यादा सोचे-समझे आवेश में आ जाते हैं। उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में लाने के लिए राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यक्रम को कृषि मुद्दों पर ज़ोर देने के साथ यह दिखाना पड़ेगा कि किस तरह सच्चे राष्ट्र-राज्य के गठन से कृषि समस्या का समुचित और तर्कसंगत समाधान संभव हो पाएगा। राजनीति के क्षेत्र का दो हिस्सों (अभिजातवर्गीय और सबाल्टर्न राजनीति) में बँट जाना परिपक्व राष्ट्रवादी सोच में भी परिलक्षित होता है। यह विभाजन तार्किकता और अतार्किकता, विज्ञान और आस्था तथा संगठन और स्वतःस्फूर्तता के बीच विभाजन को स्पष्ट मान्यता में दिखाई दिया। विशेषज्ञता पर ज़ोर देना राजकीय विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद की पुनर्व्याख्या का प्रमुख तत्त्व और उसकी ख़ासियत थी। ज़ाहिर है कि वैज्ञानिक रूप से नियोजित विकास का प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था का तेज़ी से औद्योगिकीकरण होता।
इस प्रकार समानता की ज़रूरत प्रगति के तर्क में समाहित थी और प्रगति का मतलब औद्योगीकरण था। औद्योगीकरण के लिए ज़रूरी था कि उन बाधाओं को दूर किया जाए जिन्होंने विशेष समूहों को नई आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी से रोक रखा था। लिहाज़ा औद्योगीकरण के लिए अवसर की समानता ज़रूरी थी। औद्योगीकरण और समानता के सार्वभौमिक सिद्धांत और वैश्विक मानक पहले से ही निर्धारित थे; उन मामलों में पसंदगी या नापसंदगी की कोई गुंजाइश नहीं थी। केवल विशिष्ट राष्ट्रीय पथ निर्धारित किया जाना बाक़ी था।
“यह अब एक आदर्शलोक (यूटोपिया) बन गया था, एक यथार्थवादी आदर्शलोक। पर यह आदर्शलोक घनघोर रूप से राज्य-केंद्रित था जहाँ सरकार के कामकाज को रोज़मर्रा की राजनीति के दलदल से बाहर निकालकर तर्कसंगत निर्णय-प्रक्रिया की पवित्रता का जामा पहना दिया गया। और यह निर्णय-प्रक्रिया आर्थिक प्रबंधन के विज्ञान की उन्नत परिचालन तकनीक से संचालित होनी थी।”83 राज्य की ज़ोर-जबरदस्ती अपने आप में राष्ट्र की प्रगति का एक तर्कसंगत साधन बन गई। राज्य को अपनी दमनकारी ताक़त का प्रयोग बिना किसी लाग-लपेट के सटीक रूप से करना था और इसका औचित्य उसके लक्ष्य में ही निहित था। राष्ट्रवाद मूर्त रूप ले चुका था; अब उसने एक राजकीय विचारधारा की शक्ल अख़्तियार कर ली और राष्ट्रीय जनजीवन को राजकीय जीवन में समो लिया। यह राजकीय विचारधारा तर्कसंगत और प्रगतिशील थी, और विवेक (रीज़न) की सार्वभौमिक सत्ता की विशिष्ट अभिव्यक्ति थी।
पैरी एंडरसन के अनुसार भारतीय विचारधारा (इंडियन आइडियोलॉजी), जिसे भारत की कल्पना (आइडिया ऑफ़ इंडिया) या भारत की एकता (यूनिटी ऑफ़ इंडिया) के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, छलावा मात्र है। यह विरोधाभासों से भरी है। असल में, यह एक हिंदू विचारधारा है। एंडरसन पार्थ चटर्जी की ही तर्ज़ पर “विभाजन और नेहरू” को साथ जोड़ते हैं। एंडरसन के अनुसार भारत की खाेज (Discovery of India), अगर हम इसकी पूर्ववर्ती “यूनिटी ऑफ़ इंडिया” की बात न भी करें तो, न केवल नेहरू में औपचारिक पांडित्य (स्कॉलरशिप) की कमी और मिथकों के प्रति उनके रूमानी लगाव को दिखाता है बल्कि इससे आगे भी जाता है; एक विद्वान के रूप में उनकी मनोवैज्ञानिक सीमाओं से भी ज़्यादा आत्म-छलावे की प्रवृत्ति, जिसके राजनीतिक परिणाम बेहद दूरगामी थे।85 एंडरसन के अनुसार जब गांधी आंबेडकर को ब्लैकमेल कर रहे थे तो नेहरू ने आंबेडकर का साथ नहीं दिया और जाति को “गौण मुद्दा” माना।
ज़ाहिर है जाति प्रथा की अपनी बुराइयाँ थीं जिन्हें गांधी ने भी स्वीकार किया था। पर नेहरू के मुताबिक़ भारत को इसके लिए शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है : “जाति सेवाओं और कार्यों के आधार पर बनी व्यवस्था थी। यह किसी आम रूढ़ि से मुक्त एक सर्व-समावेशी व्यवस्था थी और इसके तहत हर समूह को पूरी छूट हासिल थी।” गांधी के मुताबिक़ इतिहास ने प्रकृति में व्यवधान डाला। इसके सबूत अप्रासंगिक हैं। गांधी ने जो कुछ ख़ुद के लिए कहा, नेहरू ने उसे सब पर लागू कर दिया। नेहरू ने लिखा, “सत्य क्या है? मैं यक़ीनी तौर पर नहीं कह सकता। व्यक्ति के लिए सत्य वही है जिसे वह जानता-मानता और भरोसा करता हो।” ज्ञानमीमांसा की इस पद्धति से नेहरू जहाँ एक ओर जाति की स्वतंत्रता और समानता की बात कर सकते थे वहीं उसके ख़ात्मे की उम्मीद भी लगा सकते थे।
इसी तरह 1937 के प्रादेशिक चुनावों के बाद मुस्लिम लीग ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिली-जुली सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। पर नेहरू, जो उस वक़्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, का कहना था—“मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूँ कि हमारे और मुस्लिम लीग के बीच किसी भी तरह का समझौता या गठबंधन बहुत ही घातक होगा” और मुस्लिम लीग से कहा गया कि अगर वह चाहे तो कांग्रेस में शामिल हो सकती है। आंबेडकर उच्च जाति के हिंदुओं की इस मानसिकता का वर्णन एकाधिकारवादी मानसिकता के तौर पर करते हैं।
अपनी आत्मकथा में नेहरू ने 1935 में ही मुस्लिम राष्ट्र की किसी भी संभावना को ख़ारिज कर दिया था : “यह विचार राजनीतिक रूप से बेतुका और आर्थिक रूप से ऊटपटाँग है; यह शायद ही ग़ौर करने लायक है।” वर्ष 1938 में वह अमरीकी श्रोताओं को बताते हैं कि “भारत में कोई धार्मिक या सांस्कृतिक संघर्ष नहीं है। भारत की विलक्षण और मौलिक सच्चाई है सदियों से चली आ रही उसकी एकता।” सन् 1941 में वह अपने विचारों में किसी भी तरह के संशोधन से इनकार हुए कहते हैं कि “भारत को एक बनाए रखनेवाली शक्तियाँ काफी सुदृढ़ और अजेय हैं और किसी भी ऐसी अलगाववादी शक्ति की कल्पना असंभव है जो उसकी एकता को तोड़ सके।” हालाँकि यह सच होता दिख रहा था।
कांग्रेस ने संपत्ति कर के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोगी लियाकत अली ख़ाँ के प्रस्ताव को इसलिए अवरुद्ध कर दिया क्योंकि अधिकांश व्यवसायी हिंदू थे, इसलिए ऐसा करने का मतलब उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करना होगा। एंडरसन के अनुसार, लीग जहाँ विभाजन की बात कर रही थी, वहीं जिन्ना परिसंघ का सुझाव दे रहे थे और जब कांग्रेस राज्य-संघ की बात कर रही थी, नेहरू बँटवारे की तैयारी कर रहे थे। नेहरू का मानना था कि मुस्लिम लीग ज़मींदारों का एक प्रतिक्रियावादी गुट भर है जिसका कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस को हासिल अपार चुनावी समर्थन के आलोक में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। एंडरसन नेहरू को सीधे-सीधे बँटवारे के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं। “नेहरू एक दर्शक नहीं बल्कि परिणाम के वास्तुकार थे” और “विरासत को किसी भी क़ीमत पर हासिल” करना चाहते थे।
‘पैसिव रिवोल्यूशन’, ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ और आधुनिकता
नेहरू को समझने में चटर्जी-एंडरसन मॉडल दो तरह की ग़लतियाँ करता है। पहली ग़लती “मूल्य-राजनीतिक सिद्धांत-इतिहास” की समझ से संबंधित है। नेहरू के मूल्य पर ध्यान न देकर “व्यक्ति” और “कर्म” पर ज़ोर दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके कर्म को उसके मूल्यों को समझे बिना महत्त्वपूर्ण बना दिया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत की जगह राजनीतिक कर्म पर ज़ोर दिया जाता है। इतिहास को समझने में प्राथमिक भूल कर दी जाती है। दूसरी ग़लती अध्ययन-पद्धति से जुड़ी (methodological) है। पार्थ चटर्जी राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें इतिहास एक प्रक्रिया के तौर पर स्थगित हो जाता है और “अवधारणात्मक संवर्ग” (conceptual category) बन जाता है। लेकिन यह पद्धति नेहरू को यह अवसर नहीं देती है। नेहरू भी यही ग़लती कर रहे थे जब वह भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे। नेहरू का इतिहास वास्तव में इतिहास नहीं था। यह उसी तरह का इतिहास था जिस तरह का इतिहास चटर्जी ख़ुद गढ़ रहे हैं जो कि पूरी तरह अवधारणात्मक है। यही ग़लती पैरी एंडरसन भी करते हैं जब वे नेहरू के इतिहास को वास्तव में “इतिहास” मानकर उसे “पूरी तरह” ख़ारिज कर देते हैं। एंडरसन भारतीय राजनीति के अध्ययन (मेघनाद देसाई, रामचंद्र गुहा, प्रताप भानु मेहता, अमर्त्य सेन और सुनील खिलनानी) के ज़रिए नेहरू के इतिहास को समझने का प्रयत्न करते हैं।
पार्थ चटर्जी में ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ का आगमन नेहरू के दौर में होता है तो पैरी एंडरसन की नज़र में वह सीधे-सीधे भारत के विभाजन के लिए िज़म्मेदार हैं। चटर्जी के “अवधारणात्मक नेहरू” और एंडरसन के “राजनीतिक नेहरू” की समझ में बहुत सारी समस्याएँ हैं। दोनों के ही अध्ययन में राजनीतिक अर्थशास्त्री दृष्टिकोण का अभाव है। चटर्जी में जहाँ यह विमर्श आधुनिकता के ख़िलाफ़ मुड़ जाता है, वहीं एंडरसन नेहरू को सिर्फ़ राजनीतिक कर्मी में तब्दील कर देते है। दोनों में ही सबसे बड़ी समस्या नेहरू के माध्यम से मार्क्सवादी मूल्यों को नकारने की है। अगर नेहरू पर मार्क्सवाद के दुरुपयोग का आरोप लग सकता है तो यही आरोप चटर्जी और एंडरसन पर भी लगाया जा सकता है।
पार्थ चटर्जी नेहरू के अध्ययन के बहाने विज्ञान और आधुनिकता को पूरी तरह ख़ारिज कर देते हैं और इसे राज्यवादी विचारधारा का अंग बना देते हैं। यह सही नहीं है। औद्योगीकरण और आधुनिकता एक नहीं हैं। अगर नेहरू में “औद्योगीकरण” है, तो आधुनिकता भी है। लेकिन ये दोनों अलग-अलग हैं। आधुनिकता को “औद्योगीकरण” में समाहित करते हुए चटर्जी पूरी तरह समुदायवादी सिद्धांतकारों की तरफ़ मुड़ जाते हैं जहाँ पर “जाति” से ज़्यादा समस्या विज्ञान से है। चटर्जी की नेहरू की आलोचना “मार्क्सवादी” दृष्टि से शुरू होती है और निष्कर्ष में “समुदायवादी” के तौर पर ख़त्म होती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि नेहरू को पूरे अध्ययन में उनकी दो किताबों में समेट दिया जाता है। ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ के नाम पर मार्क्सवाद के मूल्यों को ही चटर्जी नकार देते हैं।
पैरी एंडरसन की सबसे बड़ी समस्या नेहरू को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक राजनीतिक कर्मी के तौर पर देखने की है। उनके साथ सबसे बड़ी दिक़्क़त यह है कि वे नेहरू के बारे में कोई भी राय सिर्फ़ उनके कथन के आधार पर बनाते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते। एंडरसन में नेहरू की इतिहास की समझ बहुत महत्त्वपूर्ण बनकर उभरती है। यहाँ परेशानी यह है कि वे राष्ट्रीय आंदोलनों में इतिहास को समझने की प्रक्रिया या पद्धति को ख़ारिज कर देते हैं। हर राष्ट्रीय आंदोलन बहुत सारा “इतिहास” उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ गढ़ता है। लिहाज़ा उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय संघर्षों के परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। एंडरसन अपने अध्ययन में साम्राज्यवाद और इसके ख़िलाफ़ चलनेवाले संघर्षों की असलियत को पूरी तरह भुला देते हैं। इस तर्क-प्रक्रिया में नेहरू मात्र एक राजनीतिक कर्मी बनकर रह जाते हैं जिसका हर कार्य मूलतः प्रतिकारी है। उदाहरण के लिए, नेहरू अगर धर्म के आधार पर राज्य के निर्माण की मुस्लिम लीग की माँग का विरोध कर रहे थे तो क्या वे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के आधार पर भी राज्य-निर्माण के ख़िलाफ़ नहीं थे? ऐसे प्रश्न एंडरसन में गौण हो जाते हैं। एंडरसन जिस तरह से मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति के विश्लेषण से ख़ुद को बचा लेते हैं वह सही नहीं है। एंडरसन अन्य मार्क्सवादी इतिहासकारों को भी कम तरजीह देते हैं। यहाँ मुस्लिम लीग के बारे में हमजा अल्वी का अध्ययन मुस्लिम लीग को वर्ग-विश्लेषण के जरिए समझता है जिसको एंडरसन के अध्ययन में कोई जगह नहीं मिलती है।
दोनों ही मार्क्सवादी विद्वान हिंदू दक्षिणपंथ के ख़िलाफ़ नेहरू के संघर्षों को कोई जगह नहीं देते और इस तरह से नेहरू के साथ-साथ उन मूल्यों के लिए संघर्षों के इतिहास को भी ख़त्म कर देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि चटर्जी जहाँ नेहरू में ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ को “आधुनिकता” के माध्यम से देखते हैं, वहीं एंडरसन नेहरू में “आधुनिकता” की अनुपस्थिति को ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ के आगमन के तौर पर देखते हैं। समस्या यह है कि दोनों परस्पर विरोधी मतों में से कोई एक ही सही होगा। पर मेरा मानना है कि दोनों ही ग़लत हैं। ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ और आधुनिकता साथ-साथ नहीं चल सकते। पैसिव रिवोल्यूशन/पूँजीवाद/सामंतवाद को आधुनिकता के साथ रखना ग़लत है। जहाँ पर भी आधुनिकता की बात होती है, एंडरसन नेहरू के विचार के विविध पहलुओं को नकार देते हैं।
आधुनिकता के बिना नेहरू को समझना बड़ी ग़लती है और यह ग़लती चटर्जी और एंडरसन दोनों ही करते हैं। पहले में आधुनिकता को खलनायक बनाकर नेहरू को ख़ारिज कर दिया जाता है, वहीं दूसरे में नेहरू में आधुनिकता खोजी ही नहीं जाती। जबकि आधुनिकता नेहरू के राजनीतिक सिद्धांत का बहुत महत्त्वपूर्ण पहलू बनकर सामने आती है। इसके तीन सबसे महत्त्वपूर्ण लक्षण (व्यक्ति, समाज और धर्मनिरपेक्ष राज्य) भारतीय समुदायवादी और पुनरुत्थानवादी विचारों के ख़िलाफ़ जाते हैं, जो आधुनिकता और विज्ञान को नकारते हैं।
भारतीय समुदायवादी जहाँ पर आधुनिकता को नकारते हैं वहीं पुनरुत्थानवादी दोनों को प्राचीन कहकर अपनाते हैं और इस तरह उसके सार को मार देते हैं। यहाँ पर तीन बातें प्रमुख हो जाती हैं : सामुदायिक मनुष्य, समुदाय और धर्म-आधारित राज्य। सामुदायिक मनुष्य के पास अधिकार नहीं होता है। जब कोई मनुष्य किसी समुदाय में जन्म लेता है तो उसका इस समुदाय से निकलना या किसी बाहरी व्यक्ति का किसी ख़ास समुदाय में समाहित होना मुश्किल हो जाता है। धर्म अगर राज्य के साथ है तो राज्य की सतत विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। मनुष्य हमारे समाज में सैद्धांतिक तौर पर “कर्मवादी” रहा है। यहाँ अभिप्राय मौजूदा कर्म से नहीं, बल्कि पिछले जन्म के कर्मों से है, जो वर्तमान परिस्थिति को प्रभावित या निश्चित करते हैं। शुक्रनीति (इसमें मनुष्य “सात्विक”, “राजसिक” और “तामसिक” गुणों में से किसी एक के साथ जन्म लेता है), मनुस्मृति (मनुष्य हमेशा से ही “संबंधित” (relational) होता है और उसका अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है), अर्थशास्त्र (मनुष्य राज्य के अंदर ही समाहित है) और गीता ने मनुष्य, समुदाय और राज-धर्म को बहुत हद तक प्रभावित किया है। इन चारों में व्यक्ति निमित्त मात्र है। गीता में कृष्ण के उपदेश के अनुसार, “तेरा कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं, इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूँ (कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि)। मनुष्य समुदाय का प्रारब्धिक वफ़ादार (destinated loyal) है और समुदाय धर्म-आधारित राज्य का।
इस तरह के सिद्धांतों के सहारे जिस मनुष्य का निर्माण होगा, उसके तीन प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला, इस सैद्धांतीकरण से मनुष्य भाग्यवादी (fatalist) होना शुरू हो जाता है। ऐसे में स्वयं कुछ करने की उसकी अभिलाषा पर प्रतिबंध लग जाता है या लगा दिया जाता है। दूसरा, इस मनुष्य के लिए हर परिस्थिति स्वाभाविक होगी। इस तरह स्वाभाविकता जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। तीसरा, व्यक्तिगत तार्किकता का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी तरह के सामुदायिक मनुष्य के “निर्माण” ने भारत में समाज की जगह समुदाय का निर्माण किया है। समाज और समुदाय में अंतर है। समाज का गठन परस्पर संबंध-निर्माण पर आधारित प्रक्रिया है, अर्थात यहाँ पर हम दूसरे लोगों के साथ अपने संबंधों को ख़ुद निर्धारित करते हैं, वे पूर्व-निर्धारित नहीं होते। जबकि समुदाय में लोग पहले से ही इसका हिस्सा होते हैं। समाज का विस्तार ज़्यादा व्यापक होता है। समाज आधुनिक जीवन के आगमन से संबंधित है, जबकि समुदाय “प्राचीन” संबंधों को दर्शाता है। समाज का स्वरूप विविध होता है जबकि समुदाय समरूप होता है।
अब हम व्यक्ति, समाज और राज्य की तरफ़ मुड़ते हैं। इन तीन विशिष्ट अवधारणाओं की हम तीन प्रभावी स्थानीय अवधारणाओं—मनुष्य, समुदाय और राज्य—से तुलना करते हैं। मनुष्य ऊपरी तौर पर व्यक्ति के क़रीब है, लेकिन यह दोनों काफ़ी हद तक एक-दूसरे से भिन्न हैं। सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति आंतरिक मूल्यों को दर्शाता है, जो बाहरी तौर पर दिखता है। इसलिए भारतीय संदर्भ में मनुष्य, व्यक्ति नहीं बन सका। व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होने के संदर्भ में देखा जा सकता है। व्यक्ति वास्तव में अधिकारप्राप्त मनुष्य है। मेरे अनुसार, अगर भारतीय दर्शन का गूढ़ अवलोकन करें, तो यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की तीन पहचानें हैं : कर्मवादी, भाग्यवादी और स्थितप्रज्ञ। कर्मवाद का तात्पर्य पहले से निर्धारित लक्ष्य से है जहाँ “इच्छा” का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। भाग्यवादी किसी भी घटना को पूर्व-निर्धारित मानेंगे और उनके लिए स्वैच्छिकता/एजेंसी का कोई मायने नहीं है। स्थितप्रज्ञ के लिए सारी घटनाएँ “सामान्य” हैं। समाज और समुदाय में भी गहरा अंतर है। समाज “ख़ुद” के द्वारा बनाया हुआ संस्थान है और यह सामूहिक रूप से बनता है। इसे छोड़ने और इसमें जुड़ने का रास्ता बहुत ही सुगम है। दूसरी तरफ़, हम देखें तो समुदाय की संरचना काफ़ी कठोर और स्थायी होती है। इसमें से निकलने का रास्ता बहुत ही मुश्किल या क़रीब-क़रीब न के बराबर है। ख़ास तौर पर भारतीय संदर्भ में समुदाय की सदस्यता जन्म पर आधारित है और मनुष्य की पहचान उससे जुड़ी है। इसके आंतरिक संबंध बहुत ही जटिल होते हैं और अस्मिता का प्रश्न जड़ हो जाता है। राज्य धर्म के साथ जुड़ा होता है जो पुनर्जागरण-आधुनिकता के “स्टेट” से अलग है। राज्य के साथ धर्म अपने आप जुड़ जाता है। राज-धर्म काफ़ी प्रचलित अवधारणा रही है। धर्म को बहुत तरह से व्याख्यायित किया गया है। इसको धारण के (“धारयति इति धर्म”) कर्तव्यपालन के साथ भी जोड़ा गया है। धारण या कर्तव्य की प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित कार्य से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए राज्य और धर्म को एक-दूसरे से अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
निष्कर्ष
अंतोनियो ग्राम्शी का ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ जहाँ शासक वर्ग की प्रकृति को दिखाते हुए आधुनिकता की अपील करता है, वहीं पार्थ चटर्जी में आधुनिकता ही “समस्या” बन जाती है। मार्क्स की “जर्मन आइडियोलॉजी” जहाँ हेगल के प्रभाव को चुनौती देने का रास्ता खोलते हुए “इतिहास की भौतिकवादी संकल्पना” प्रस्तुत करती है वहीं पैरी एंडरसन की ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ में सब कुछ “हिंदू आइडियोलॉजी” हो जाता है जिसमें वैकल्पिक संघर्ष और उसकी भौतिकवादी संकल्पना बेमानी हो जाती है। पद्धति के तौर पर जहाँ “जर्मन आइडियोलॉजी” “मैटर/मेटेरियलिज्म” पर ज़ोर देती है वहीं ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ में “आइडिया” महत्त्वपूर्ण बनकर उभरता है। दोनों विश्लेषणों (चटर्जी और एंडरसन) में वर्ग की राजनीति बेमानी हो जाती है, इसलिए ये अध्ययन नेहरू की आधुनिकता (व्यक्ति, समाज और धर्मनिरपेक्ष राज्य) और भारतीय समुदायवादी और पुनरुत्थानवादी (व्यक्ति, समुदाय और धर्म-परायण राज्य) का तुलनात्मक अध्ययन करने में विफल रहते हैं। विमर्शों की गहराई में न जाना और नेहरू को ‘पैसिव रिवोल्यूशन’ और ‘इंडियन आइडियोलॉजी’ तक सीमित कर देना न सिर्फ़ नेहरू के राजनीतिक सिद्धांत का ख़ात्मा है, बल्कि इतिहास के अभिन्न और विभिन्न मौक़ों पर भारतीय दक्षिणपंथ के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक लड़ाई को भी नकारना है। इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ख़ुद मार्क्सवादी मूल्यों पर ही है जिसको आंदोलन में न तब्दील करने के लिए नेहरू को अवश्य ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए।
[आलोचना सहस्त्राब्दी अंक-69 में प्रकाशित]