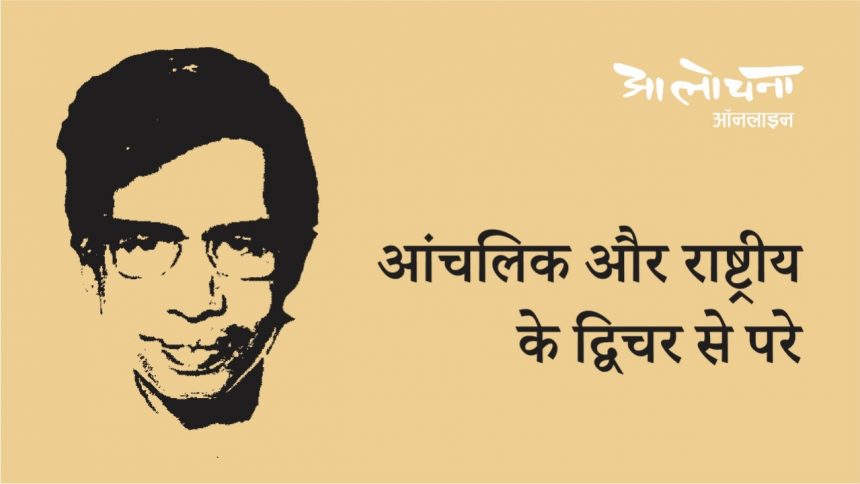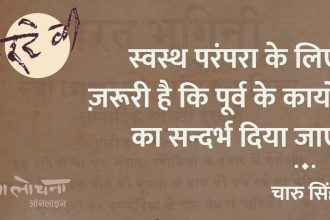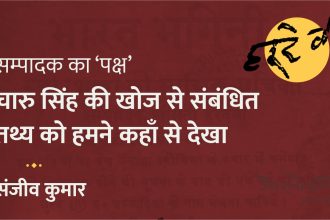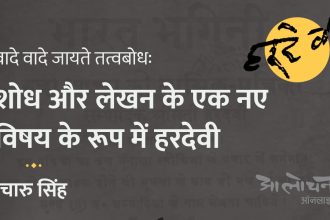अभी हम हिंदी के बेमिसाल कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु (4 मार्च 1921 – 11 अप्रैल 1977) के जन्मशती वर्ष की आख़िरी तिमाही में हैं।
देश का किसान इस हाड़तोड़ शीतलहर में अपनी किसानी को बड़े कॉर्पोरेट्स के शिकंजे से बचाने के लिए सड़कों पर है; नवउदारवादी नीतियों के कारण जो बेरोज़गारी पहले ही चालीस सालों में अधिकतम हो चुकी थी, कोरोना और उससे निपटने की नाकारा नीतियों के कारण भयावह स्तर को छू रही है; मानव विकास सूचकांक पर देश लगातार नीचे लुढ़क रहा है और अरबपतियों की आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है; दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के हुक़ूक़ की लड़ाई लड़नेवाले बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को झूठे मामले बनाकर जेलों में ठूँसा जा रहा है; हिन्दुत्व की झंडाबरदार राज्य सरकारें नागरिक स्वतंत्रताओं को ताक पर रखकर तथाकथित ‘लव जेहाद’ के खिलाफ़ क़ानून बनाने में लगी हैं और मानो विपरीत लक्षणा में उसे धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में बनाया गया क़ानून बता रही हैं; सत्ता में बैठे लोग झूठ, धमकी और भयादोहन का पूरी नंगई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और पहले दबे-ढँके तौर पर काम आने वाले इन हथियारों के इस्तेमाल में अब कोई पर्दादारी नहीं रह गई है; पत्रकारिता का बहुलांश केंद्र में बैठी सरकार के पक्ष में और जनता के खिलाफ़ खड़ा है; सरकार के विरोध में उठे हर आलोचनात्मक स्वर को रराष्ट्रविरोधी, अलगाववादी, पाकिस्तान समर्थक, ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ बताने में तमाम माध्यमों को झोंक दिया गया है; राष्ट्रवाद एक आततायी नारा बनकर उभरा है जिसका इस्तेमाल कभी भी, किसी के भी खिलाफ़ हो सकता है—वह नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध करते अल्पसंख्यक और उनके हिमायती हों, जल-जंगल-ज़मीन को बचाने का संघर्ष करते आदिवासी हों, या अपनी किसानी बचाने के लिए दिल्ली को घेरकर बैठे किसान।
ऐसे समय में रेणु की जन्मशती मनाते हुए मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनके साहित्य के साथ आज के इस परिदृश्य का क्या रिश्ता बनता है?
राजकमल से प्रकाशित होने से पहले मैला आँचल (1954) पटना के एक प्रकाशनगृह से छप चुका था। उस प्रकाशक के यहाँ भी इसे लगभग साल-भर इंतज़ार करना पड़ा था। ग़रज़ कि पिछली सदी के पचास के दशक की शुरुआत में उपन्यास लिखा जा चुका था। ऐसे उपन्यास को पकने और काग़ज़ पर उतरने में जितना वक़्त लगना चाहिए, उसे देखते हुए यह कहना असंगत न होगा कि उपन्यास की कथा जिस कालखंड को घेरती है, यानी आज़ादी के थोड़ा पहले से आज़ादी के थोड़ा बाद तक का समय, वही उसका ‘जेस्टेशन पीरियड’ भी है। ध्यान दें तो यही समय था जब देश का संविधान भी रचा जा रहा था। 1931 की कराची कांग्रेस में एक स्वतंत्र भारत की जो परिकल्पना सामने आई थी, उसे संविधान के स्तर पर साकार करने के प्रयास चल रहे थे। आलोचना 63 में रमाशंकर सिंह ने अपने लेख ‘किसे चाहिए संविधान’ में बड़ी बारीकी से दिखाया है कि संविधान सभा की बैठकों में कितनी तरह की आवाज़ें शामिल थीं, और कितनी और आवाज़ें उसमें शामिल होने के लिए जद्दोजहद कर रही थीं। वे लिखते हैं, ‘भारत का संविधान बनते समय ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ काम करने वाले दल तो इसमें शामिल हुए ही, वे समूह भी शामिल हुए जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अंदर रहते हुए भारतीय समाज की संरचना को सुधारने और राजनीतिक रूप से सत्ता-संबंधों को कमज़ोरों के पक्ष में करने की मुहिम चला रखी थी। इसके अलावा इसमें दार्शनिक, साहित्यकार, वकील, अध्यापक, महिलाएँ, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, एंग्लो-इंडियन, सिख और देसी रियासतों के लोग शामिल हुए। ई. पी. थॉमसन के शब्द उधार लें तो भारत में मौजूद और कार्यरत सभी विचारों के लोग इसमें शामिल हुए’ (आलोचना 63, पृ. 128)।

कहने की ज़रूरत नहीं कि यह भागीदारी उस समावेशी राष्ट्रवाद की भावना के कारण हो पा रही थी जिसे भारत ने अपने उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष के बीच अर्जित किया था और जो, प्रभात पटनायक के शब्दों में, ‘एक अनोखी और अभूतपूर्व चीज़ थी।’ प्रभात पटनायक ने इस महत्त्वपूर्ण बात की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि भारत में उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष के बीच से जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ, वह यूरोप में तीस-साला युद्ध का अंत करने वाली वेस्टफ़ालिया की संधि के बाद उभरे राष्ट्रवाद का हमशक्ल नहीं था। सत्रहवीं सदी में घटित हुई उस शांति-संधि से राष्ट्र-राज्यों की व्यवस्था अस्तित्व में आई थी और राष्ट्र-राज्य की विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। पर भारत में जो उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद पैदा हुआ, वह उस राष्ट्रवाद से कई मायनों में बिल्कुल अलग, बल्कि उलट था। यूरोपीय बूर्जुआ राष्ट्रवाद ‘राष्ट्र’ को जनता से ऊपर रखता था और ‘राष्ट्रीय हित’ उसके लिए जनता के हित यानी उसके जीवन की भौतिक परिस्थितियों में सुधार का पर्याय नहीं था; अलबत्ता जनता से हमेशा ‘राष्ट्र’ के लिए क़ुर्बानी देने की उम्मीद की जाती थी। इससे ठीक उलट उपनिवेश-विरोधी राष्ट्रवाद में जनता सर्वोपरि थी और राष्ट्रीय हित का मतलब था, जनता का हित। इसके साथ ही, चूँकि इसे एक सामान्य शत्रु—औपनिवेशिक ताक़त—के खिलाफ़ सभी को एकजुट करना था, इसलिए यह समावेशी था। यह एक भूखंड में रहने वाले सभी बाशिंदों को अपने दायरे में शामिल करता था, इसमें कोई ‘आंतरिक शत्रु’ (एनिमी विद-इन) नहीं था, जबकि यूरोप में एक भाषा और एक सामुदायिक अनुभव को अपनी बुनियाद बनानेवाले राष्ट्रवाद ने सर्वत्र किसी ‘आंतरिक शत्रु’ की पहचान की, मिसाल के लिए, उत्तरी यूरोप में कैथोलिक, दक्षिणी यूरोप में प्रोटेस्टैंट, और हर जगह यहूदी (देखें, प्रभात पटनायक, ‘टू कॉनसेप्ट्स ऑफ़ नेशनलिज़म’, रोहित आज़ाद एवं अन्य द्वारा संपादित व्हाट द नेशन रियली वान्ट्स टु नो, हार्पर कॉलिन्स, नई दिल्ली, 2016)।
निस्संदेह, समावेशी राष्ट्रवाद की इस अवधारणा और वास्तविकता में प्रायः एक अंतराल रहा, पर राष्ट्रवाद का स्वर्ण-मानक मान लिये गए यूरोपीय राष्ट्रवाद से अवधारणा के स्तर पर भी इसका यह फ़र्क़ मायने रखता है। अवधारणा और वास्तविकता के बीच जो भी अंतराल रहा, उसकी एक व्याख्या यह हो सकती है कि ऐसा समावेशी राष्ट्रवाद हमेशा एक बनती हुई (और इसीलिए बिगड़ती हुई भी) चीज़ होता है। वह कभी भी एक ‘फिनिश्ड प्रोडक्ट’ नहीं हो सकता। वह लगातार एक रस्साकशी, एक दुहरे खिंचाव के बीच होता है, जिसके एक तरफ़ अधिक समावेशन की माँग होती है तो दूसरी तरफ़ अधिक अपवर्जी/एक्सक्लूसिव बनाए जाने की कोशिश। मिसाल के लिए, कौन नहीं जानता कि जिस समय देश का संविधान बन रहा था, उस समय हिन्दुत्व की ताक़तें यह गुहार लगा रही थीं कि जब हमारे पास मनुस्मृति है तो फिर एक नये संविधान की क्या ज़रूरत? दूसरी तरफ़ यह भी सच है कि संविधान सभा में जहाँ कई तरह की आवाज़ों को जगह मिल रही थी, वहीं कई आवाज़ें शामिल होने की जद्दोजहद करके भी अपनी जगह नहीं बना पाईं। रमाशंकर सिंह ने संविधान सभा की कार्यवाही-रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि मज़दूरों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रतिनिधित्व की आवाज़ वहाँ उठी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला (देखें, आलोचना 63, पृ. 135)।
संविधान की रचना के समानांतर मैला आँचल का लिखा जाना, बनते हुए राष्ट्र में उपेक्षितों की भागीदारी का दावा पेश करने जैसा था। उसे अपवर्जी राष्ट्रवाद के खिलाफ़ समावेशी राष्ट्रवाद के पक्ष में एक दृढ़ आग्रह/असर्शन की तरह देखा जाना चाहिए। यह उपन्यास अपनी पूरी प्रस्तुति से गोया यह कहना चाहता है कि हम भी हैं—ऐसे लोग जो ‘भारतमाता’ को ‘भारथमाता’ कहते हैं, जिनकी जुबान मानक हिंदी की ध्वनियों को सँभाल नहीं पाती, जिनके ख़ास अपने रीति-रिवाज़ हैं, अपना चाल-चलन है, अपने क़िस्म का भूगोल और अपनी तरह की विपदाएँ हैं, भयानक ग़रीबी और जहालत है जिसे डॉक्टर प्रशांत रोग के दो कीटाणु कहता है, जो भगतसिंह की भी जात पूछ सकते हैं और ‘अरे हो बुड़बक बभना, चुम्मा लेवे में जात नहीं रे जाए’ गाना भी गा सकते हैं— हम भी इसी मुल्क के हिस्से हैं, हमें भी देखो।
‘प्रस्तुति’ यहाँ पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त है। मैला आँचल में अवलोकन-बिंदुओं के बदलने का जो खेल है, वही यह सुनिश्चित करता है कि इसमें अंचल को देखने वाली निगाह कहीं बाहर की न लगे, ऐसा लगे कि अंचल ख़ुद बोल रहा है। इस बात से समावेशी राष्ट्रवाद के पक्ष में इस दृढ़ आग्रह का महत्त्व बहुत बढ़ जाता है। ज़्यादातर समय आपको यह महसूस होता है कि आप किसी भीतरी वाचक (कथा के ही एक पात्र; होमोडाईजेटिक नैरेटर) से कथा सुन रहे हैं, हालाँकि उस वाचक का वैसा कोई परिचय आपके सामने नहीं होता जैसा कि आम तौर पर भीतरी वाचकों का होता है। वह बिना नाम, बिना व्यक्तित्व का, पारंपरिक सर्वज्ञ वाचक जैसा अमूर्त वाचक होता है। इससे अवलोकन-बिंदु की आत्मनिष्ठता भी बनी रहती है और कही गई बात किसी एक के मत जैसी भी नहीं लगती। उपन्यास का अधिकांश, अंचल में चल रहे ऐसे संवाद की तरह लगता है जिसे बिना उद्धरण-चिह्नों के लिख दिया गया है। इस युक्ति को आप उपन्यास की शुरुआत से ही प्रभावी रूप में पाते हैं।
यद्यपि 1942 के जन-आंदोलन के समय इस गाँव में न तो फ़ौजियों का उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गाँव तक पहुँच पाई थी, किंतु ज़िले-भर की घटनाओं की ख़बर अफ़वाहों के रूप में यहाँ तक ज़रूर पहुँची थी।…मोगलाही टीशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोलबाजा में पूरे गाँव को घेरकर आग लगा दी गई, एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आँखों से देखा था—ठीक आग में भूनी गई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रहीं, कौआ भी नहीं खा सकता था; मलेटरी का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खानसामा है; वह झूठ बोलेगा? पूरे चार साल के बाद अब इस गाँव की बारी आई है। दुहाई माँ काली! दुहाई बाबा लरसिंह!
इस अंश में यह भी ग़ौर किया जा सकता है कि कथा कब बाहरी वाचक (यानी जो कथा का पात्र नहीं है; हेटेरोडाईजेटिक नैरेटर) के हाथ से निकलकर भीतरी वाचक के हाथ में चली जाती है, पता भी नहीं चलता। इस हस्तांतरण को आप बेहिचक ‘बेजोड़’ कह सकते हैं, अतुलनीय के अर्थ में भी और ‘सीमलेस’ (सीवन/जोड़ के बग़ैर) के अर्थ में भी। और यह किसी एक या दो अंशों की बात नहीं है। उपन्यास में आद्यंत इसे देखा जा सकता है। ‘वैन्टेज पॉइंट’ के इस खेल को अंचल की तरफ़ से ख़ुद बोलने के बजाय अंचल की आवाज़ों को ही मुखर करने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।
यह तरीक़ा, जिसमें गाँव या गाँव का ही कोई पक्ष—कोई जाति-आधारित टोला या कोई वर्ग—बोलता हुआ लगता है, अपने में अनोखा है और इसे आप रेणु के समकालीनों में तो नहीं ही पाएँगे, बाद में उनके नक़्शे-क़दम पर चलने वालों के यहाँ भी यह कहीं-कहीं ही मिलेगा (समकाल में पंकज मित्र के यहाँ इसका सबसे कुशल उपयोग दिखता है)। इस युक्ति पर जिस तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए था, संभवतः नहीं दिया गया। रामविलास शर्मा जैसे महत्त्वपूर्ण आलोचक ने तो इसका मज़ाक़ ही उड़ाया है। अपने सबसे ख़राब लेखों में से एक, ‘प्रेमचंद की परंपरा और आंचलिकता’ में वे एक जगह लिखते हैं, ‘मैला आँचल की भाषा-शैली बलचनमा वाली है। कुछ अंशों को छोड़कर लेखक भी अपने पात्रों की तरह बोलता है और व्याकरण संबंधी भूलें करता है (यह कहना कठिन है कि जानबूझकर या असावधानी से)।’ ‘जानबूझकर या असावधानी से’ के इस अपमानजनक व्यंग्य में रामविलास जी की राजनीतिक सीमाएँ बहुत खुलकर सामने आई हैं। मानक भाषा के खिलाफ़ अगर बोली के दृढ़ आग्रह को वे इस तरह देखते हैं तो इससे पता चलता है कि हिंदी जाति की उनकी संकल्पना कितनी संकीर्ण थी। इस तरह का आग्रह शायद उन्हें हिंदी जाति का एकाश्म गढ़ने के लिहाज़ से असुविधाजनक लगता रहा हो, इसीलिए वे इस क़दर हमलावर हुए। रामविलास जी का राष्ट्रवाद रेणु के मुक़ाबले अपनी प्रकृति में अपवर्जी है, यह मज़ाक़ उड़ाने की इस छोटी-सी हरकत से साफ़ हो जाता है। इसी लेख में एक जगह प्रेमचंद के बारे में उन्होंने कहा है, ‘उनके पात्रों में आंचलिकता से अधिक हिंदुस्तानीपन या हिंदीपन है।’ असल समस्या यही है। रामविलास जी के लिए हिंदुस्तानीपन अथवा हिंदीपन एक ऐसी शै है जिसका औपन्यासिक दायरे में आंचलिकता के साथ प्रतिलोम-अनुपाती संबंध है। भाषा के रूपक में देखें तो यह हिंदीपन मानक भाषा की तरह और आंचलिकता बोली की तरह नज़र आएगी। फिर यह सवाल तो उठेगा कि अगर मानक भाषा खड़ी बोली के आधार पर विकसित हुई, तो यह मानक हिंदीपन किस अंचल के आधार पर तैयार हुआ है, और जिस तरह एक शब्द के विभिन्न प्रचलित रूपों में से एक मानक रूप चुनकर मानकीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसी तरह क्या मानक हिंदीपन के लिए भी मानक प्रचलनों का चयन हुआ है? मैला आँचल का मज़ाक़ उड़ाते हुए इन सवालों के प्रति कोई सजगता हमारे हिंदी जाति के सिद्धांतकार के यहाँ नहीं मिलती।
रामविलास जी की यह टिप्पणी राजनीति के साथ-साथ साहित्यिक युक्तियों के संबंध में भी उनकी सीमाओं का निदर्शन है। मैला आँचल की भाषा-शैली को बलचनमा वाली बताने का कोई मतलब नहीं, सिवाय इसके कि बलचनमा में भी मानक भाषा का जगह-जगह परित्याग किया गया है। आप यह कैसे भूल सकते हैं कि बलचनमा प्रथम पुरुष वाचक वाला उपन्यास है, जबकि मैला आँचल में कोई प्रथम पुरुष वाचक नहीं है, फिर भी आपको महसूस होता है कि कथा-संसार के भीतर से ही कोई उसकी प्रस्तुति कर रहा है। यह न समझ आने पर ही इस तरह की टिप्पणी की जा सकती है कि ‘लेखक भी अपने पात्रों की तरह बोलता है’। जी नहीं, लेखक अपने पात्रों की तरह बोलता नहीं है, अपने पात्रों को ही कहानी बोलने पर नियुक्त कर देता है, भले ही अनाम-अरूप होने के कारण वे आपको बाहरी वाचक, जिसे हम ‘लेखक’ कहने के अभ्यस्त रहे हैं, की तरह प्रतीत हों।
किरांती चलित्तर कर्मकार कालीचरन के यहाँ आया है? बस, तब क्या है? करैला चढ़ा नीम पर। चलित्तर भी सोशलिस्ट पाटी में है? तब तो जरूर बम-पिस्तौल की टरेनि देने आया है। बम-पिस्तौल के सामने काली टोपीवालों की लाठी क्या करेगी?
चरखा-करघा, लाठी-भाला और बम-पिस्तौल! तीन टरेनि!
यहाँ, और ऐसे असंख्य अंशों में, लेखक/सर्वज्ञ वाचक बोल रहा है या कथा के अनाम-अरूप पात्र बोल रहे हैं? ‘क्रांति’ को ‘किरांती’, ‘पार्टी’ को ‘पाटी’ और ‘ट्रेनिंग’ को ‘टरेनि’ कौन बोल रहा है? साहित्यिक युक्ति के स्तर पर इस फ़र्क़ की पहचान न कर पाने वाले आलोचक से मैला आँचल के महत्त्व को रेखांकित करने की आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं!
वैसे यहाँ मामला शायद साहित्यिक युक्ति की पहचान न होने का उतना नहीं है जितना बनते हुए राष्ट्र में अंचल की दावेदारी के नागवार गुज़रने का। युक्ति उस दावेदारी का साधन है, इसलिए वह भी गले नहीं उतरी।
तो फिर इस प्रश्न पर भी विचार करना ज़रूरी हो जाता है कि क्या रेणु ने देश के क्षेत्रीय अंतर्विरोधों के बीच अपना पक्ष-निर्माण करते हुए अन्य अंतर्विरोधों को ताक़ पर रख दिया? क्या मैला आँचल में अंचल एक समांग श्रेणी के रूप में प्रस्तुत है? नहीं। उपन्यास में अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति के सवाल को, भूस्वामी बनाम मेहनतकश के सवाल को, अलग-अलग राजनीतिक धाराओं के ज़मीनी फ़र्क़ के सवाल को जिस तरह उठाया गया है, वह बताता है कि यहाँ दावेदारी सिर्फ़ उपेक्षित अंचल की नहीं, उसमें भी उपेक्षितों और पिछड़ों की है।
अरे! वह ज़माना चला गया जब राजपूतटोली और बाभनटोली के लोग बात-बात में लात-जूता चलाते थे। याद नहीं है? एक बार टहलू पासवान का गुरु घोड़ी पर चढ़कर आ रहा था। गाँव के अंदर यदि आता तो एक बात थी। गाँव के बाहर ही सिंघ जी ने घोड़ी पर से नीचे गिराकर जूते से मारना शुरू कर दिया था—‘साला दुसाध, घोड़ी पर चढ़ेगा!’…अब वह ज़माना नहीं है। गाँधी का ज़माना है। नया तहसीलदार है तो क्या? हमारा क्या बिगाड़ लेगा? न जगह न जमीन है; इस गाँव में नहीं उस गाँव में रहें, बराबर है।
यही पूरे उपन्यास की मूल भावना है। अगड़ी जातियों के खिलाफ़ पिछड़ी जातियों का उभार और जोतनेवालों के हक़ में भूमि-सुधार की मुहिम उपन्यास में बहुत प्रमुखता से चित्रित हैं। यही नहीं, इनके साथ अलग-अलग राजनीतिक धाराओं के क्या रिश्ते हैं, इनकी भी अचूक पहचान है। आश्चर्य नहीं कि सबसे प्रतिक्रियावादी धारा के तौर पर रेणु ने आरएसएस की पहचान की है। उपर्युक्त उद्धरण में जिस नए तहसीलदार, सिंघ जी (हरगौरी सिंह) का ज़िक्र आया है, वह मेरीगंज में आरएसएस का प्रतिनिधि भी है। काली टोपी वाले संयोजक जी उसी के घर ठहरते हैं। उपन्यास में बहुत कम जगह घेरने के बावजूद इस धारा का चरित्र बाकमाल बारीकी के साथ उभारा गया है। उपर्युक्त उद्धरण तो एक उदाहरण है ही, जहाँ आप पाते हैं कि जातिगत श्रेणीक्रम को बनाए रखने की आक्रामकता को लेखक ने एक आरएसएस वाले के हिस्से में डाला है; इसके अलावा भी अनेक प्रसंग हैं जहाँ इस संगठन का चरित्र खुलकर सामने आता है। जैसे एक प्रसंग है जहाँ सहदेव मिसिर के खिलाफ़ पंचायत में पिछड़ी जाति के कालीचरण के समर्थन में लोगों के एकजुट हो जाने के बाद ‘टू टू… टू टू,’ संयोजक जी सीटी फूँकते हैं।
एक दर्जन से भी ज़्यादा नौजवान राजपूतटोली से हाथ में लाठी लेकर दौड़ आए और पंचायत को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए।
‘सिंघ जी, इन लाठीवाले नौजवानों को आपने बुलाया है?… तो आप पंचायत नहीं, दंगा करवाना चाहते हैं?’ कालीचरन पूछता है।
पंचायत नहीं, दंगा करवाना—रेणु ने जैसे आरएसएस की नब्ज़ पकड़ ली है। इसी तरह, गाँव में जब भूमि-सुधार का आंदोलन तेज़ होता है, तबतहसीलदार हरगौरी सिंह काली टोपी वाले नौजवानों से कहते हैं, ‘इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गाँव में ही लोहा लेना पड़ेगा।’
भूमि-सुधार से हिंदू राज का क्या संबंध है, यह लेखक के सामने एकदम साफ़ है। समाजवादी और कम्युनिस्ट भूमि-सुधार के पक्ष में हैं, भले ही वासुदेव जैसे समाजवादी लालच में पड़कर भटक जाएँ; कांग्रेस भी सैद्धांतिक रूप से उसके पक्ष में है, लेकिन उसका वर्गाधार यह सुनिश्चित करता है कि वह इस एजेंडे पर दृढ़ न रहे; वहीं हिंदू राज की बात करने वाले बहुत स्पष्ट रूप से ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि-सुधार के विरोध में हैं। जो लोग हिन्दुत्व को सिर्फ़ मुसलमानों के खिलाफ़ मानते हैं, उन्हें मैला आँचल से भी पता चल सकता है कि हिन्दुत्व हर तरह की बराबरी के खिलाफ़ है और उसकी कार्यसूची में जातिगत, वर्गीय और लैंगिक बराबरी के विरोध का महत्त्व मुस्लिम-विरोध से किसी तरह कम नहीं है। एक जगह हरगौरी सिंह को संयोजक जी से यह कहते दिखाया गया है कि उसे यवनों से ज़्यादा ग़ुस्सा यवनों का समर्थन करने वाले हिंदुओं पर आता है। यह सुनते हुए आपको नहीं लगता कि बिल्कुल आज के किसी संघी ट्रोल की बात सुन रहे हैं?
वस्तुतः मैला आँचल अपनी कथा और प्रस्तुति, दोनों में उस अपवर्जी राष्ट्रवाद को दी गई एक रचनात्मक चुनौती है जिसका कॉपीराइट इस देश में आरएसएस के पास है और जो उपनिवेश-विरोधी संघर्ष से अर्जित समावेशी राष्ट्रवाद के बरख़िलाफ़ ठेठ यूरोपीय राष्ट्रवाद की नक़ल है—उस राष्ट्रवाद की नक़ल जो सौ फ़ीसद ‘विदेशी’ है, जिसका हमारी आज़ादी की लड़ाई से कोई संबंध नहीं है, और जिसके पैमाने पर मैला आँचल एक ‘एंटी-नेशनल’ कृति ठहरेगी और रेणु ‘टुकड़े टुकड़े गैंग’ के मेम्बर।
मैला आँचल ही नहीं, पूरी कथित आंचलिकता के पीछे समावेशी राष्ट्रवाद की स्पिरिट विद्यमान है, जिसकी अनदेखी करके रेणु के महत्त्व को संपूर्णता में नहीं समझा जा सकता। कोई आश्चर्य नहीं कि रेणु के महत्त्व की सही पहचान करने वाले आलोचक नित्यानंद तिवारी ही यह अमर वाक्य लिख सके : ‘स्वाधीनता आंदोलन और मैला आँचल की आंचलिकता—दोनों में वंशानुगत जैसी पहचान के आंतरिक लक्षण हैं’ (नया पथ, अप्रैल-जून 2020, पृष्ठ 12)।
वर्तमान परिदृश्य, जहाँ स्वाधीनता आंदोलन के सारे मूल्य सिर के बल खड़े किए जा चुके हैं और नव-उदार पूँजी का अपवर्जी हिन्दुत्व राष्ट्रवाद के साथ बहुत स्वाभाविक गठबंधन तबाही मचा रहा है, के साथ रेणु के रिश्ते को समझने की कुंजी भी यही है।
आलोचना के इस अंक में फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ पर दो महत्त्वपूर्ण लेख हैं। रेणु साहित्य के महत्त्व पर एक वरिष्ठ आलोचक और कवि रामनिहाल गुंजन तथा हमारे समय के एक बहुत महत्त्वपूर्ण कथाकार रणेंद्र के विस्तृत आलेख अंक की विशेष सामग्री की तरह हैं। ये जन्म-शताब्दी वर्ष में लिखे गए रस्मी लेख नहीं हैं, बल्कि दो हज़ार बीस में लिख रहे एक आलोचक और एक कथाकार की अपने साहित्य के एक पुरोधा के साथ की गई बहस हैं।
नए साल का यह पहला अंक ख़ासा बहसतलब है।
इस अंक से एक नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है। साहित्यिक बहसों का। हिन्दी में एक ज़माने से गम्भीर साहित्यिक बहसें देखने को नहीं मिली हैं। सामाजिक मीडिया पर कुछ न कुछ सर्द-गर्म चलता रहता है, लेकिन उस तुरंत जगह पर कोई परिपक्व वैचारिक बहस संभव नहीं है। नामवर जी से शब्द उधार लेकर इस सिलसिले को ‘वाद-विवाद-संवाद’ का नाम दिया गया है। इस बार राजाराम भादू शमशेर की कविता ‘टूटी हुई बिखरी हुई’ के स्त्री-पाठ पर बहस की शुरुआत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी इसमें शरीक हों।
कविता और काव्य-बोध पर दो बहसतलब आलेख इस बार अलग से लिए जा रहे हैं। रीतिकालीन कविता की आस्वाद-परम्परा पर सुजाता ने और आधुनिक कविता की पाठ-परम्परा पर अच्युतानंद ने नए सवाल उठाए हैं।
गोपाल प्रधान ने इस बार पिछले दशकों में सामने आई स्त्री की नई दावेदारी को समझने-समझाने वाली किताबों का लेखा-जोखा किया है।
इस अंक में स्त्री की केंद्रीयता अनेक रूपों में है। वाद-विवाद-संवाद के केंद्र में मूल सवाल प्रेम जैसी शाश्वत और सार्वभौम भावना की जेंडर-सापेक्षता का ही है। काव्य-सौंदर्य के संदर्भ में यही सवाल एक तरह से सुजाता ने भी उठाया है। लेकिन स्त्री की भावनात्मक अस्मिता की सबसे गूँजती हुई आवाज़ इस अंक की कविताओं में सुनाई देगी। हिंदी में स्त्री-अनुभव की ऐसी प्रामाणिक आवाज़ अब तक सुनने में नहीं आई थी, लेकिन ये कविताएँ स्त्री अनुभव तक की ही नहीं हैं। कवयित्री हैं अनुपम सिंह, जो हिंदी की युवा पीढ़ी की नुमाइंदगी करती हैं। दिलचस्प है कि इस अंक में हरीचरन प्रकाश की कहानी के केंद्र में भी दो युवा स्त्रियाँ ही हैं, जो इस नए ज़माने में स्त्री होने की नई चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
साल जाते-जाते मंगलेश डबराल और शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी हमसे छीन ले गया। इस अंक में मंगलेश डबराल को आलोचक आशुतोष भारद्वाज और कवि पंकज चतुर्वेदी ने अपने-अपने तरीक़े से याद किया है। मंगलेश डबराल का एक विचारोत्तेजक व्याख्यान भी है, जो उनका अंतिम था।
आलोचना के अगले अंक में हम शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी पर विशेष सामग्री देने की तैयारी कर रहे हैं। फ़ारुक़ी साहब भारतीय स्मृति के उपनिवेशीकरण के खिलाफ़ आलोचनात्मक और रचनात्मक संघर्ष चलाने वाले सबसे बड़ी साहित्यिक विभूति के रूप में याद किए जाते रहेंगे। भारतीय सौंदर्यबोध की स्वायत्तता पर, जिसे वे ‘सबके हिंदी’ कहा करते थे, उनका जबरदस्त इसरार मरते दम तक तक बना रहा।
इस बीच और भी कई अज़ीज़ लोग हमसे विदा ले गए। सत्यजित राय के सिनेमा को अभिनय की गहराई देने वाले सौमित्र चटर्जी, वरिष्ठ रंगकर्मी श्री कल्याण घोष, मलयाली कवि अच्युतन नंबूदरी, कवि अरविन्द सोरल, रविन्द्रनाथ द्विवेदी, कामरेड िज़या उल हक़, देशबंधु के प्रधान संपादक ललित सुरजन और मक़बूल पाकिस्तानी शायर नासिर तूराबी। आप सबकी रौशन यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।
[आलोचना सहस्त्राब्दी अंक-64 में प्रकाशित संजीव कुमार का संपादकीय]